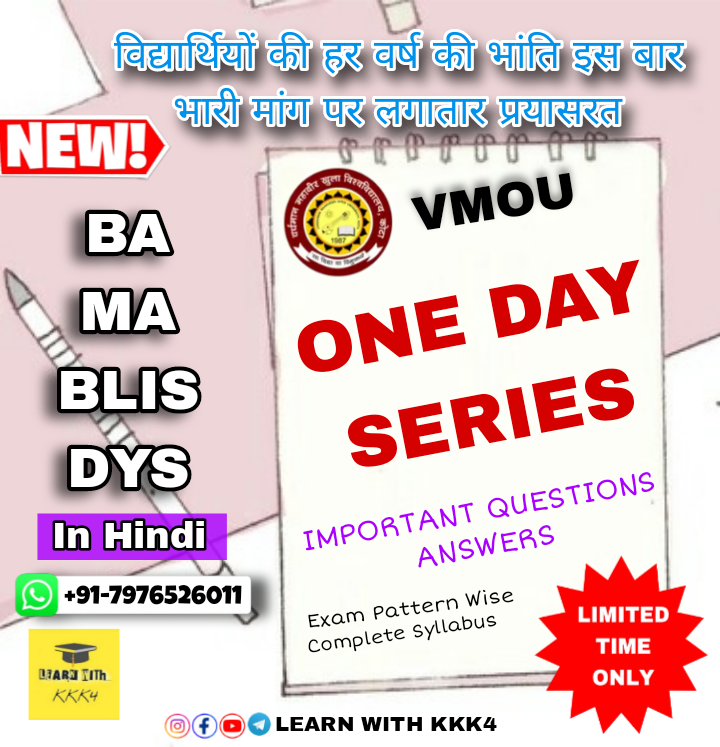VMOU MAPS-01 Paper MA 1st Year ; vmou exam paper
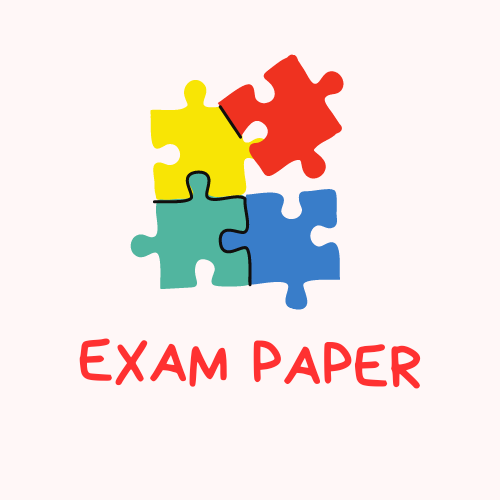
VMOU MA First Year के लिए राजनीति विज्ञान ( MAPS-01 , Political Thought ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
उत्तर:- अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.Republic’ के लेखक कौन हैं?
उत्तर:- ‘Republic’ के लेखक प्लेटो हैं।
प्रश्न-3.प्लेटो द्वारा लिखी गई दो पुस्तकों के नाम लिखिए
उत्तर:- ‘Republic’ और ‘Laws’ प्लेटो द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं।
प्रश्न-4.अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है?
उत्तर:- अरस्तु के अनुसार, नागरिक वह है जो राज्य के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भाग लेता है।
प्रश्न-5. क्रान्ति के अधिकार पर लॉक के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- लॉक ने कहा कि यदि सरकार नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो जनता को क्रांति का अधिकार है।
प्रश्न-6. उदात्त वनचर को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- उदात्त वनचर की अवधारणा रूसो ने दी, जिसमें आदिम मानव को नैतिक, निर्दोष और सभ्यता से श्रेष्ठ माना गया है।
प्रश्न-7. जे.एस. मिल द्वारा बताए गए स्वतंत्रता के दो प्रकार बताइए।
उत्तर:- जे.एस. मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Individual Liberty) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) को प्रमुख बताया।
प्रश्न-8. सम्प्रभुता पर हॉब्स के विचारों की विवेचना कीजिए
उत्तर:- हॉब्स के अनुसार सम्प्रभुता निरंकुश और indivisible होती है, जिसे शासक को लोगों की सुरक्षा हेतु सौंपा जाता है।
प्रश्न-9.व्यास के अनुसार राजा के आपद्धर्म (संकटकाल में अपनाए जाने वाला धर्म) बताइए।
उत्तर:- व्यास के अनुसार संकटकाल में राजा को धर्म की सामान्य मर्यादा से हटकर, राज्य की रक्षा, प्रजा की भलाई और व्यवस्था बनाए रखने हेतु कठोर निर्णय लेने चाहिए।
प्रश्न-10.प्लेटो के ‘दार्शनिक राजा’ की अवधारणा स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में वह व्यक्ति शासक होना चाहिए जो ज्ञान, नैतिकता और न्याय में पारंगत हो। ऐसा शासक ही ‘दार्शनिक राजा’ कहलाता है।
प्रश्न-11.अरस्तू के अनुसार यह कैसे संभव है कि किसी स्वामी का दास होना स्वामी और स्वयं दास के लिए हितकारी होगा?
उत्तर:- अरस्तू के अनुसार कुछ लोग स्वाभाविक दास होते हैं जिनके लिए स्वामी के अधीन रहना और सेवा करना उनके बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए हितकारी होता है।
प्रश्न-12. कौटिल्य के अनुसार ‘दण्डनीति’ क्या है?
उत्तर:- कौटिल्य के अनुसार दण्डनीति शासन की वह नीति है जिसके द्वारा राजा कानून, दंड और प्रशासनिक व्यवस्था से राज्य में शांति, अनुशासन और न्याय बनाए रखता है।
प्रश्न-13.”सीजर की वस्तुएँ सीजर को और पीटर की वस्तुएँ पीटर को” — इस वक्तव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- इसका अर्थ है कि मध्यकालीन राजनीतिक सोच में धर्म और राज्य के कार्यक्षेत्र अलग थे; धार्मिक विषय चर्च (पीटर) के अधीन और राजनीतिक विषय राजा (सीजर) के अधीन थे।
या
मध्ययुग में धर्म और राजनीति को अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में बांटा गया — धर्म चर्च (पीटर) के अधीन और राज्य सीज़र के अधीन।
प्रश्न-14. मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली के क्या विचार थे?
उत्तर:-मैकियावेली के अनुसार मनुष्य मूल रूप से स्वार्थी, धोखेबाज़ और सत्ता के प्रति लालची होता है, अतः एक कुशल शासक को व्यावहारिक, चतुर और कठोर होना चाहिए।
प्रश्न-15. “राज्य से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था की परिस्थितियों को हॉब्स ने बड़ी दयनीय तरीके से चित्रित किया है।” — वक्तव्य को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- हॉब्स के अनुसार राज्य से पहले की स्थिति में मानव जीवन भय, असुरक्षा और अराजकता से भरा था; इसलिए सामाजिक अनुबंध द्वारा एक सशक्त राज्य की आवश्यकता थी।
प्रश्न-16. सुखवाद (Hedonism) से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- सुखवाद एक नैतिक दर्शन है जिसके अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्ति है; यह व्यक्ति के आनंद को सर्वोच्च मूल्य मानता है, जैसे उपयोगितावाद में।
प्रश्न-17. प्लेटो के अनुसार मनुष्य में अन्तनिर्हित आत्मा के तीन गुण या पक्ष क्या हैं?
उत्तर:- चित्त (Appetite), आत्मा (Spirit), बुद्धि (Reason)
प्रश्न-18. ‘लेवियाथन’ का लेखक कौन है?
उत्तर:- थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes)
प्रश्न-19.दो तलवारों’ का सिद्धान्त क्या है?
उत्तर:- यह सिद्धान्त पोप और सम्राट के मध्य आध्यात्मिक व लौकिक शक्ति के विभाजन को दर्शाता है।
प्रश्न-20. लॉक के अनुसार कितने प्राकृतिक अधिकार होते हैं?
उत्तर:- तीन – जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति।
प्रश्न-21. “मैकियावली अपने युग का शिशु था।” यह कथन किसने कहा है?
उत्तर:- डोरी (Dunning) ने कहा।
प्रश्न-22.सामान्य इच्छा (General Will) क्या है?
उत्तर:- यह सामूहिक इच्छा है जो समाज के समस्त सदस्यों के सामान्य हित को दर्शाती है।
प्रश्न-23. ‘मध्यकालीन राजनीतिक चिन्तन’ की दो विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:- (1) धर्म पर आधारित, (2) ईश्वर और चर्च का प्रभाव सर्वोपरि।
प्रश्न-24. प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है?
उत्तर:- जब आत्मा के तीनों अंग अपने-अपने कार्य में रहते हैं, तो वही न्याय है।
प्रश्न-25. मनु को ‘प्रथम शिक्षक’ अथवा ‘प्रथम विधायक’ क्यों माना जाता है?
उत्तर:- क्योंकि उन्होंने धर्मशास्त्र के माध्यम से समाज और राज्य के नियम स्थापित किए।
प्रश्न-26. अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है?
उत्तर:- जो व्यक्ति विधियों के निर्माण और न्याय में भाग ले, वह नागरिक है।
प्रश्न-25. हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर:- पूर्ण, अविभाज्य, निरंकुश और स्थायी।
प्रश्न-28. प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में वर्णित सप्तांग सिद्धान्त क्या है?
उत्तर:- राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र – ये सात अंग राज्य के आधार हैं।
प्रश्न-29. बैंथम की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए।
उत्तर:- (1) ए फ्रैग्मेंट ऑन गवर्नमेंट, (2) द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन।
प्रश्न-30. राजनीति विज्ञान के लिए महाभारत के शांति पर्व का महत्व बताइए।
उत्तर:- यह राजा के कर्तव्य, न्याय, और राज्य संचालन के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करता है।
प्रश्न-31. मानव स्वभाव के बारे में मैकियावली के विचार ने किस प्रकार उनके राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया है?
उत्तर:- मानव स्वभाव स्वार्थी होता है, अतः राजनीति शक्ति, धोखे और व्यावहारिकता पर आधारित होनी चाहिए।
प्रश्न-32. प्राकृतिक अवस्था के बारे में हॉब्स और रूसो के विचारों में क्या भिन्नता है?
उत्तर:-हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अराजक है; रूसो के अनुसार शांतिपूर्ण और स्वतंत्र।
प्रश्न-33.प्लेटो के अनुसार राज्य में (अ) शासन के दायित्व और (ब) सैन्य दायित्व में कौनसे गुण प्रधान हैं ?
उत्तर:- अ) बुद्धि (Reason)
(ब) साहस (Courage)
प्रश्न-34.हॉब्स के लेवियाथन को निरंकुशवादी क्यों माना गया? (2 कारण)
उत्तर:- संप्रभु की शक्ति निरंकुश और सर्वोच्च होती है। नागरिकों को विद्रोह का अधिकार नहीं होता।
प्रश्न-35.अरस्तु द्वारा प्रस्तुत ‘अवकाश’ का सम्बन्ध निष्क्रियता से नहीं है।” — स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- अरस्तु के अनुसार ‘अवकाश’ आत्म-विकास, दर्शन, और नागरिक कर्तव्यों के लिए होता है, न कि केवल आराम या निष्क्रियता के लिए।
प्रश्न-36.कौटिल्य के अनुसार ‘दण्डनीति’ क्या है ?
उत्तर:- दण्डनीति राज्य की शांति, अनुशासन और न्याय बनाए रखने हेतु दंड देने की नीति है।
प्रश्न-37.लॉक और रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों में क्या अन्तर है?
उत्तर:- लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण थी, जबकि रूसो के अनुसार वह स्वतंत्र, समान लेकिन सभ्यता से भ्रष्ट थी।
प्रश्न-38.प्लेटो द्वारा प्रतिपादित “परिवार और संपत्ति का साम्यवाद” क्या है?
उत्तर:- प्लेटो के अनुसार अभिजात वर्ग के लिए परिवार और संपत्ति को साझा करके निजी स्वार्थों को समाप्त कर राज्य के हित को सर्वोच्च बनाना चाहिए।
प्रश्न-39.षाड्गुण्य नीति’ के छह सिद्धांत क्या हैं?
उत्तर:- सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध, सामाश्रय — ये युद्धकालीन कूटनीति के छह उपाय हैं।
प्रश्न-40.कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के कारण क्या हैं?
उत्तर:- अराजकता, सुरक्षा की आवश्यकता, न्याय और संगठन की आवश्यकता राज्य की उत्पत्ति के कारण हैं।
प्रश्न-41. मानव स्वभाव पर मैकियावेली के विचार क्या हैं?
उत्तर:- मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी, धोखेबाज़ और सत्ता-लोलुप होता है, इसलिए शासक को व्यावहारिक और कठोर होना चाहिए।
प्रश्न-42. लॉक के सामाजिक समझौते की प्रकृति क्या है?
उत्तर:-
प्रश्न-43. ‘प्राकृतिक अवस्था’ पर हॉब्स के विचार क्या हैं?
उत्तर:- प्राकृतिक अवस्था में “सभी का सभी के साथ युद्ध” था — असुरक्षा, भय और अराजकता से भरी स्थिति थी।
प्रश्न-44. बेंथम और मिल के सुखवाद में मूल अंतर क्या है?
उत्तर:- बेंथम मात्रात्मक सुख पर बल देते हैं, जबकि मिल गुणात्मक सुख (बौद्धिक व नैतिक सुख) को श्रेष्ठ मानते हैं।
प्रश्न45.
उत्तर:-
Section-B
प्रश्न-1.यूनानी राजनीतिक चिन्तकों के अनुसार सद्गुण के विचारों की विवेचना कीजिए
उत्तर:- “यूनानी राजनीतिक चिन्तकों ने सद्गुण को एक आदर्श राज्य और नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक माना। प्लेटो के अनुसार सद्गुण चार प्रकार की होती है: ज्ञान, साहस, संयम और न्याय। उसने न्याय को सर्वोच्च सद्गुण माना, जहाँ प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करता है। प्लेटो के अनुसार, शासकों में ज्ञान और बुद्धिमत्ता, रक्षकों में साहस और नागरिकों में संयम होना चाहिए। अरस्तू ने सद्गुण को मध्यम मार्ग कहा – अत्यधिक और न्यूनता के बीच का संतुलन। उदाहरणस्वरूप, साहस भय और दुस्साहस के बीच का गुण है। अरस्तू के अनुसार सद्गुण को शिक्षा और अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यूनानी चिन्तकों का मानना था कि सद्गुणी व्यक्ति ही उत्तम नागरिक हो सकता है और राज्य की भलाई के लिए कार्य कर सकता है। उनके विचारों में सद्गुण और राजनीति का गहरा संबंध है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.पोलिटी’ पर अरस्तू के विचार समझाइए।
उत्तर:- अरस्तू ने ‘पोलिटी’ (Polity) को शासन के उत्तम रूपों में एक माना है। उसने शासन के तीन सही रूप बताए: राजतंत्र (Monarchy), अभिजातशाही (Aristocracy) और ‘पोलिटी’। पोलिटी का अर्थ है – एक ऐसा शासन जहाँ राज्य का संचालन मध्यवर्ग द्वारा कानून के अनुसार किया जाता है। यह राजनैतिक स्थायित्व और न्याय का प्रतीक है। अरस्तू के अनुसार, जब सामान्य लोगों को राज्य के हित में सत्ता मिलती है और वे नियमों का पालन करते हैं, तब वह पोलिटी कहलाती है। पोलिटी में धनिकों और निर्धनों के हितों में संतुलन होता है, जिससे समाज में स्थिरता बनी रहती है। यह लोकतंत्र और अभिजातशाही का संतुलित रूप है, जिसमें कानून सर्वोपरि होता है। अरस्तू ने इसे सबसे व्यावहारिक और टिकाऊ शासन प्रणाली माना।
प्रश्न-3.महाभारत में वर्णित राजा के कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- महाभारत में राजा को धर्म और नीति का रक्षक माना गया है। राजा के मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित बताए गए हैं: (1) धर्म की स्थापना – राजा को धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए और प्रजा को भी धार्मिक मार्ग पर चलाना चाहिए; (2) न्याय का पालन – राजा को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और दोषियों को दंड देकर न्याय स्थापित करना चाहिए; (3) प्रजा की सुरक्षा – आंतरिक और बाहरी खतरों से राज्य की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है; (4) कर प्रणाली का संचालन – राजा को उचित कर वसूल कर राज्य चलाना चाहिए परन्तु कर वसूली में अति नहीं होनी चाहिए; (5) जनकल्याण – शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए योजनाएं बनाना। महाभारत में आदर्श राजा को ‘धर्मराज’ कहा गया है, जो नीति, धर्म और दया के मार्ग पर चलता है।
प्रश्न-4.कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित ‘षाड्गुण्य’ नीति को स्पष्ट कीजिए
उत्तर:- कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति (Shadgunya Neeti) ‘अर्थशास्त्र’ में प्रतिपादित छह रणनीतियों का समूह है, जिनका प्रयोग राज्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए किया जाता है। ये छह नीतियाँ हैं: (1) संधि – शांति स्थापित करने हेतु समझौता करना; (2) विग्रह – युद्ध करना; (3) यान – सैन्य तैयारी के साथ आगे बढ़ना; (4) आसन – स्थिर रहकर परिस्थिति का आकलन करना; (5) संश्रय – किसी शक्तिशाली राजा की शरण लेना; और (6) दैदिभाव – किसी अन्य राजा के साथ संयुक्त रूप से आक्रमण करना। कौटिल्य का मानना था कि इन नीतियों का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। यह नीति राजा को व्यवहारिक कूटनीति सिखाती है और राज्य की रक्षा तथा विस्तार में सहायक होती है।
प्रश्न-5.मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से पृथक करने पर जोर दिया” – इस कथन की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- मैकियावेली, जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है, ने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पृथक करने पर जोर दिया। उसने ‘द प्रिंस’ नामक ग्रंथ में लिखा कि शासक का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना होना चाहिए, भले ही उसके लिए छल-कपट, धोखा, हिंसा या अन्य अनैतिक साधनों का सहारा क्यों न लेना पड़े। उसने कहा, “शासक को सिंह और लोमड़ी दोनों की तरह होना चाहिए।” अर्थात उसे शक्ति और चालाकी का संतुलन रखना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार, नैतिकता केवल निजी जीवन में उपयोगी है, राजनीति में सफलता के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण आवश्यक है। इस प्रकार, उसने पहली बार राजनीति को धार्मिक और नैतिक मूल्यों से अलग करके एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया।
प्रश्न-6.हॉब्स को निरंकुशवाद का समर्थन क्यों माना जाता है?
उत्तर:- थॉमस हॉब्स को निरंकुशवाद (Absolutism) का समर्थक इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने एक ऐसी सम्प्रभु सत्ता की कल्पना की जिसे असीम, अविभाज्य और निरंकुश अधिकार प्राप्त हों। हॉब्स के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी, भयभीत और हिंसक होता है, जिससे “सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध” की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे बचने हेतु लोगों ने एक सामाजिक अनुबंध द्वारा अपनी सभी स्वतंत्रताओं को एक सम्प्रभु को सौंप दिया, जिससे वह शांति और व्यवस्था बनाए रखे। हॉब्स का सम्प्रभु न तो जनता के प्रति उत्तरदायी है, न ही उसका प्रतिकार संभव है। उसने सम्प्रभु को कानून बनाने, न्याय करने और युद्ध/शांति तय करने का अधिकार दिया। अतः हॉब्स की सोच निरंकुश सत्ता को वैधता प्रदान करती है।
प्रश्न-7.उपयोगितावाद पर मिल के विचारों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उन्होंने बेंथम के ‘अधिकतम सुख के सिद्धांत’ को स्वीकार किया, परंतु उसमें गुणात्मक भेद जोड़ा। मिल के अनुसार, “कुछ सुख दूसरों से श्रेष्ठ होते हैं।” जैसे – बौद्धिक सुख शारीरिक सुख से उच्चतर हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव कर चुका है, वह उच्चतर सुख को प्राथमिकता देगा। मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी समर्थन किया और माना कि जब तक किसी की स्वतंत्रता दूसरों को नुकसान न पहुँचाए, तब तक उसे रोका नहीं जाना चाहिए। उनके अनुसार, उपयोगितावाद का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक कल्याण है। उन्होंने नैतिकता और राजनीति दोनों में उपयोगितावाद की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया
प्रश्न-8.मानव स्वभाव एवं राज्य की उत्पत्ति पर लॉक के विचार स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- जॉन लॉक के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र, समान और तर्कशील होता है। वह हिंसक नहीं, बल्कि सहयोगी प्रवृत्ति का होता है। इस अवस्था में मनुष्य के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार होते हैं। परंतु इन अधिकारों की रक्षा हेतु कोई निश्चित संस्था नहीं होती, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं। इसलिए लोगों ने सामाजिक अनुबंध के माध्यम से राज्य की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कुछ अधिकार राज्य को सौंपे ताकि वह उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके। लॉक के अनुसार राज्य की सत्ता सीमित होती है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि राज्य अत्याचारी हो जाए तो जनता को उसे बदलने का अधिकार होता है।
प्रश्न-9. प्लेटो के न्याय सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए
उत्तर:- प्लेटो ने अपने ग्रंथ ‘गणराज्य’ में न्याय को राज्य का प्रमुख सद्गुण बताया है। उसके अनुसार, न्याय तब होता है जब समाज के तीनों वर्ग – शासक, रक्षक और उत्पादक – अपने-अपने कार्यों को निभाते हैं और एक-दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। प्लेटो ने कहा, “न्याय वह है जहाँ हर व्यक्ति अपना कार्य करता है।” उसने यह भी बताया कि आत्मा के तीन भाग – तर्क, साहस और इच्छा – जब संतुलन में होते हैं, तब व्यक्ति के भीतर भी न्याय होता है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत सामंजस्य, व्यवस्था और नैतिक संतुलन पर आधारित है।
प्रश्न-10. प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन में धर्म, नैतिकता और समाज कल्याण का प्रमुख स्थान रहा है। महाभारत, मनुस्मृति, रामायण और कौटिल्य का ‘अर्थशास्त्र’ इस चिंतन के प्रमुख स्रोत हैं। इसमें राजा को धर्मपालक, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल बताया गया है। राज्य को ‘धर्मराज्य’ माना गया, जहाँ शासन का उद्देश्य धर्म की स्थापना और लोक कल्याण है। कौटिल्य ने राजनीति को व्यावहारिक दृष्टि से देखा और कूटनीति, गुप्तचर व्यवस्था, युद्धनीति आदि को महत्व दिया। इसके अतिरिक्त बौद्ध और जैन विचारकों ने भी अहिंसा, सत्य और करुणा पर आधारित शासन की बात की। कुल मिलाकर, प्राचीन भारतीय चिंतन में राजनीति नैतिकता और धर्म से जुड़ी हुई है।
प्रश्न-11. लॉक की प्राकृतिक अधिकार सम्बन्धी धारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- लॉक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें वह प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights) कहता है। ये हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार ईश्वर प्रदत्त होते हैं और राज्य भी इन्हें समाप्त नहीं कर सकता। इन अधिकारों की रक्षा करना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। यदि राज्य इन अधिकारों का हनन करता है तो नागरिकों को उसे बदलने का अधिकार है। लॉक की यह धारणा आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा और मानव अधिकारों की नींव मानी जाती है।
प्रश्न-12. संत थॉमस एक्विनास के कानून सम्बन्धी विचारों का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- संत थॉमस एक्विनास ने ‘कानून’ को ईश्वर के आदेश और तर्क से जुड़ा माना। उन्होंने चार प्रकार के कानून बताए: (1) शाश्वत कानून – ईश्वर का सार्वभौमिक नियम; (2) प्राकृतिक कानून – मनुष्य के विवेक से उत्पन्न नियम; (3) मानव निर्मित कानून – समाज के लिए बनाए गए कानून; (4) धार्मिक कानून – ईश्वर की आज्ञाओं पर आधारित। एक्विनास का मानना था कि सभी मानव कानून प्राकृतिक और शाश्वत कानून के अनुरूप होने चाहिए। यदि कोई मानव कानून नैतिकता के विरुद्ध हो, तो उसे नहीं माना जाना चाहिए। उनके विचारों ने चर्च और राज्य के संबंधों को प्रभावित किया और मध्यकालीन ईसाई राजनीतिक सोच को दिशा दी।
प्रश्न-13. बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धान्त का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद (Utilitarianism) का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका मूल विचार है – “अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख।” उन्होंने सुख और दुख को गणनात्मक रूप से मापा और ‘हेडोनिक कैलकुलस’ की अवधारणा दी। उनके अनुसार, नीति, कानून और शासन का उद्देश्य जनता के सुख को बढ़ाना होना चाहिए। उन्होंने हर कार्य की नैतिकता को उसके परिणाम से जोड़ा। हालांकि, बेंथम के सिद्धांत की आलोचना भी हुई – जैसे यह व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा करता है और केवल बहुसंख्यक के सुख को महत्व देता है। परंतु, उनके विचारों ने लोकतंत्र, विधि सुधार और कल्याणकारी राज्य की नींव रखी।
प्रश्न-14. “मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिन्तन के जनक के रूप में जाना जाता है।” समीक्षा कीजिए।
उत्तर:- मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने पहली बार राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक कर स्वतंत्र क्षेत्र माना। ‘द प्रिंस’ में उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया और शासक को सत्ता प्राप्ति और सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी साधनों के प्रयोग की छूट दी। उसने कहा कि राजनीति में सफलता नैतिकता से नहीं, व्यावहारिकता से तय होती है। उसने चर्च के प्रभाव को कम करने और राष्ट्र-राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया। उसने शक्ति, कूटनीति और सैन्य बल को राजनीति के प्रमुख उपकरण बताया। उसकी यथार्थवादी शैली ने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को नई दिशा दी
प्रश्न-15. हॉब्स के सम्प्रभुता सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर:- हॉब्स के अनुसार सम्प्रभुता पूर्ण, अविभाज्य और निरंकुश होती है। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में उसने कहा कि लोग अपनी सभी स्वतंत्रताएँ सम्प्रभु को सौंप देते हैं ताकि वह शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। सम्प्रभु ही कानून निर्माता, न्यायाधीश और शासनकर्ता होता है। हॉब्स ने धर्म और राज्य को भी सम्प्रभु के अधीन माना। उसके अनुसार, सम्प्रभु की शक्ति पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उसका यह विचार निरंकुश शाही सत्ता को वैधता देता है। हालांकि, उसकी यह सोच आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत मानी जाती है, लेकिन उसकी सम्प्रभुता की परिभाषा ने राजनीतिक सिद्धांत को गहराई प्रदान की।
प्रश्न-16. रूसो की ‘लोकप्रिय सम्प्रभुता’ को समझाइए।
उत्तर:- रूसो के अनुसार सम्प्रभुता जनता में निहित होती है, न कि किसी राजा या शासक में। उसकी ‘लोकप्रिय सम्प्रभुता’ की अवधारणा ‘सामूहिक इच्छा’ (General Will) पर आधारित है। उसने कहा कि सामाजिक अनुबंध के माध्यम से लोग अपने अधिकारों को किसी शासक को नहीं, बल्कि सामूहिक इच्छा को सौंपते हैं। यह सामूहिक इच्छा ही सर्वोच्च कानून होती है और इसका उद्देश्य जनहित होता है। प्रत्येक नागरिक इस इच्छा में भाग लेता है और स्वयं को आज़ाद महसूस करता है। रूसो की यह अवधारणा आधुनिक लोकतंत्र, प्रतिनिधि शासन और नागरिक अधिकारों की नींव बन गई।
प्रश्न-17. अरस्तू के दासता सम्बन्धी विचारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- अरस्तू ने दासता को प्राकृतिक बताया। उसके अनुसार कुछ लोग जन्म से ही दूसरों के अधीन रहने के लिए होते हैं। उन्होंने दो प्रकार की दासता मानी: प्राकृतिक और विधिक। प्राकृतिक दासता में दास का मालिक के अधीन रहना उसकी भलाई के लिए होता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम लेकिन मानसिक रूप से कमजोर है, तो उसके लिए आज्ञाकारी रहना उचित है। अरस्तू ने यह भी कहा कि दास मानव होते हैं लेकिन पूर्ण नागरिक अधिकारों से वंचित रहते हैं। आज के मानवीय दृष्टिकोण से अरस्तू की यह सोच विवादास्पद है, परंतु उनके समय में इसे तर्कसंगत माना गया।
प्रश्न-18. लॉक के विचारों में उदारवादी तत्वों की विवेचना कीजिए
उत्तर:- जॉन लॉक को उदारवादी राजनीतिक चिन्तन का जनक माना जाता है। उनके विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, विधिक शासन और लोक-समझौते पर आधारित राज्य की अवधारणा प्रमुख है। लॉक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः स्वतंत्र, समान और तर्कशील होता है। उन्होंने राज्य की सत्ता को सीमित रखने की वकालत की और ‘सीमित सरकार’ का समर्थन किया। उन्होंने “प्राकृतिक अधिकार” — जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति — को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार माना। यदि सरकार इन अधिकारों का हनन करे तो जनता को विद्रोह का अधिकार है। उनकी विचारधारा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन को विशेष स्थान दिया गया है, जो आधुनिक लोकतंत्र की नींव बनाता है।
प्रश्न-19. ‘प्राकृतिक अवस्था’ के बारे में हॉब्स के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) वह स्थिति थी जहाँ कोई सरकार या कानून नहीं था। यह अवस्था पूर्ण अराजकता, भय और असुरक्षा से भरी थी। हॉब्स ने कहा, “मनुष्य मनुष्य के लिए भेड़िया है” (Man is a wolf to man)। इस अवस्था में जीवन “क्रूर, संक्षिप्त और असुरक्षित” था। अतः, लोग सुरक्षा हेतु एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता एक सार्वभौम सत्ता को सौंप देते हैं जिसे ‘लेवियाथन’ कहते हैं। यह सार्वभौम सत्ता पूर्ण और निरंकुश होती है। हॉब्स की यह अवधारणा निरंकुश राज्य की वैधता का दार्शनिक आधार बनती है।
प्रश्न-20. राज्य की नैतिकता के बारे में मैकियावली के विचार क्या थे?
उत्तर:- मैकियावली ने राजनीति को नैतिकता से अलग कर देखा। उसकी दृष्टि में राज्य की सफलता और स्थायित्व ही सर्वोपरि है, चाहे वह नैतिक साधनों से प्राप्त हो या अमानवीय तरीकों से। उन्होंने कहा कि शासक को नैतिकता की अपेक्षा व्यावहारिकता अपनानी चाहिए। “राज्य के हित में अधर्म भी धर्म बन जाता है।” उसके अनुसार शासक को शेर की शक्ति और लोमड़ी की चतुराई दोनों की आवश्यकता है। राज्य की नैतिकता का आधार शक्ति और परिणाम होता है, न कि ईश्वर या नैतिक धर्म। इसलिए मैकियावली को आधुनिक यथार्थवादी और शक्ति-केन्द्रित राजनीतिक विचारक माना जाता है।
प्रश्न-21. राज्य के महत्व के बारे में यूनानी राजनीतिक चिन्तकों के विचार स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- यूनानी राजनीतिक चिन्तकों ने राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में देखा। प्लेटो के अनुसार, राज्य आत्मा का विस्तार है; जैसे आत्मा में तीन भाग होते हैं, वैसे ही राज्य में तीन वर्ग होते हैं – शासक, रक्षक और उत्पादक। न्याय तभी स्थापित होता है जब ये तीनों वर्ग अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अरस्तू ने कहा, “मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है”, और राज्य का उद्देश्य मात्र जीवन नहीं बल्कि अच्छे जीवन की प्राप्ति है। यूनानी चिन्तकों के अनुसार राज्य का निर्माण मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है, लेकिन उसका उद्देश्य नैतिक और बौद्धिक विकास है। वे राज्य को आत्मनिर्भर, पूर्ण और सर्वोपरि संस्था मानते थे
प्रश्न-22. क्रांति के सामान्य कारणों के बारे मे अरस्तु के विचार समझाइए।
उत्तर:-अरस्तू ने ‘राजनीति’ नामक ग्रंथ में क्रांति (Revolution) के कारणों की गहन विवेचना की। उनके अनुसार क्रांति का मुख्य कारण असमानता, अन्याय, और सत्ता का दुरुपयोग होता है। जब शासक वर्ग सार्वजनिक भलाई के स्थान पर निजी हितों को प्राथमिकता देता है, तब असंतोष उत्पन्न होता है। आर्थिक विषमता, कर का अत्यधिक बोझ, राजनीतिक अधिकारों से वंचित वर्ग में विद्रोह की भावना उत्पन्न करता है। अरस्तू ने यह भी कहा कि लोगों में बदलाव की स्वाभाविक इच्छा होती है और यदि शासक संवेदनशील न हो, तो परिवर्तन क्रांति का रूप ले लेता है। उन्होंने कहा कि क्रांति का समाधान संतुलन, न्याय और सत्ता का विवेकपूर्ण वितरण है।
प्रश्न-23. प्राचीन भारतीय चिंतकों द्वारा युद्ध के समय अपनायी जाने वाली ‘षाड्गुन्य नीति’ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- षाड्गुण्य नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित एक युद्ध नीति है, जिसमें राज्य युद्धकालीन छह विकल्पों का चयन कर सकता है: (1) संधि – शांति समझौता, (2) विग्रह – युद्ध करना, (3) यान – तैयारी करके आगे बढ़ना, (4) स्थान – कूटनीतिक स्थिति बनाए रखना, (5) संश्रय – शक्तिशाली राज्य से सहायता लेना, (6) द्वैधीभाव – दोहरी नीति अपनाना। यह नीति राजा की शक्ति, समय, स्थान, और शत्रु की स्थिति पर निर्भर करती है। कौटिल्य ने कहा कि राजा को व्यावहारिक होना चाहिए और स्थिति के अनुसार नीति का चयन करना चाहिए। यह नीति चतुराई, कूटनीति और व्यावहारिकता पर आधारित है।
प्रश्न-24. कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित ‘मण्डल सिद्धान्त’ की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- कौटिल्य का मण्डल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पड़ोसी राज्य शत्रु होता है और उसका पड़ोसी मित्र होता है। इस सिद्धांत में 12 मण्डल (राज्य) होते हैं – राजा, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन आदि। इसका उद्देश्य यह है कि राजा को युद्ध और शांति की नीति बनाते समय अपने चारों ओर की राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। यह सिद्धांत रणनीतिक संतुलन और कूटनीतिक चतुराई पर आधारित है। इसमें “शत्रु का शत्रु मित्र होता है” की नीति पर ज़ोर दिया गया है। मण्डल सिद्धांत आज के अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ‘बैलेंस ऑफ पावर’ जैसी अवधारणाओं से मेल खाता है।
प्रश्न-25. मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स के विचारों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- थॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव को स्वार्थी, भयभीत और प्रतिस्पर्धात्मक बताया है। उसकी प्रमुख रचना Leviathan में उसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा और लाभ के लिए संघर्ष करता है। यह अवस्था पूर्ण अराजकता की होती है जहाँ “मनुष्य मनुष्य के लिए भेड़िया है” (Homo Homini Lupus)। हॉब्स के अनुसार मनुष्य अपनी सुरक्षा हेतु दूसरों पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए जीवन असुरक्षित होता है। वह कहता है कि डर और आत्म-रक्षा की भावना मानव का मूल स्वभाव है। इसलिए, मनुष्य एक सामाजिक अनुबंध करता है और एक सत्तावान संप्रभु को सत्ता सौंप देता है ताकि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे। हॉब्स की दृष्टि में नैतिकता और कानून राज्य के बाद ही आते हैं।
प्रश्न-26. बैंथम के उपयोगितावाद में मिल के सुधारों को समझाइए।
उत्तर:- प्रश्न 13
प्रश्न-27. प्लेटो की न्याय की अवधारणा क्या है?
उत्तर:- प्रश्न 9
प्रश्न-28. मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिन्तक क्यों माना गया है?
उत्तर:- प्रश्न 14 सेक्शन ब
प्रश्न-30. लॉक द्वारा व्यवस्थापिका पर लगाए गए सीमाओं (प्रतिबंधों) को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- जॉन लॉक ने Two Treatises of Government में सीमित सरकार की अवधारणा दी और कहा कि व्यवस्थापिका सर्वोच्च होते हुए भी निरंकुश नहीं हो सकती। उसके अनुसार व्यवस्थापिका को कुछ सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। (1) उसे उस उद्देश्य के अनुरूप कार्य करना चाहिए जिसके लिए सरकार का गठन हुआ, यानी नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा। (2) यह कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए – चाहे राजा हो या सामान्य व्यक्ति। (3) व्यवस्थापिका कर लगाने या संपत्ति पर नियंत्रण के लिए जनता की सहमति प्राप्त करे। (4) वह अपनी सत्ता किसी अन्य संस्था को नहीं सौंप सकती। लॉक ने सरकार को उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के लिए इन सीमाओं को अनिवार्य बताया। इससे लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन की नींव पड़ी।
Section-C
प्रश्न-1.जे.एस. मिल के स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों को समझाइए।
उत्तर:- जे. एस. मिल (John Stuart Mill) उन्नीसवीं शताब्दी के एक प्रमुख अंग्रेज़ दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक चिंतक थे। वे स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘On Liberty’ (1859) में स्वतंत्रता के सिद्धांत को विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया।
- स्वतंत्रता की परिभाषा:
मिल के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्ति को अपने इच्छित कार्य करने की स्वाधीनता, बशर्ते वह दूसरों को क्षति न पहुँचाए। उन्होंने इसे ‘नकारात्मक स्वतंत्रता’ कहा, जिसका अर्थ है राज्य या समाज का व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना। - आत्मनिष्ठ क्षेत्र (Self-regarding actions):
मिल ने ‘स्वतंत्रता का सिद्धांत’ प्रतिपादित करते हुए कहा कि व्यक्ति के वे सभी कार्य जो केवल उसे स्वयं को प्रभावित करते हैं, उन पर राज्य या समाज को कोई अधिकार नहीं है। जैसे – विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, रहन-सहन आदि। ये व्यक्ति के आत्मनिष्ठ क्षेत्र में आते हैं और इस पर प्रतिबंध उचित नहीं। - सामाजिक उत्तरदायित्व (Other-regarding actions):
जब कोई कार्य दूसरों को हानि पहुँचाता है, तब उस पर राज्य या समाज को हस्तक्षेप का अधिकार है। यह स्वतंत्रता का मर्यादित रूप है, जहाँ व्यक्ति के अधिकार वहीं तक हैं, जहाँ तक वे दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करें। - वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति:
मिल ने विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष समर्थन किया। उनके अनुसार समाज में विविध विचारों का प्रसार होना चाहिए, चाहे वे प्रचलित मतों के विरुद्ध ही क्यों न हों। यह वैचारिक टकराव सत्य तक पहुँचने का माध्यम है। - ‘न्यूनतम हस्तक्षेप’ सिद्धांत:
मिल ने सरकार की भूमिका को सीमित माना। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल वहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए जहाँ व्यक्ति या समूह के कार्य दूसरों के हित को नुकसान पहुँचाते हैं। यह सिद्धांत ‘Laissez-faire’ नीति के करीब है। - स्वतंत्रता और विकास:
मिल के अनुसार स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आत्मिक विकास का माध्यम भी है। एक स्वतन्त्र समाज में व्यक्ति की रचनात्मकता, चिंतनशक्ति और आत्मनिर्भरता बढ़ती है।
जे.एस. मिल का स्वतंत्रता संबंधी चिन्तन आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने व्यक्तिवादी स्वतंत्रता, वैचारिक विविधता और सीमित शासन का जो दर्शन प्रस्तुत किया, वह आधुनिक लोकतंत्रों की आधारशिला है। उनकी विचारधारा ने मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उदारवाद को गहराई से प्रभावित किया है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.अरस्तू प्रथम वैज्ञानिक राजनीतिक विचारक था।” समझाइए।
उत्तर:- अरस्तू (Aristotle) को “राजनीति का जनक” (Father of Political Science) कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति के अध्ययन को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। वे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। उन्होंने अपने समय की लगभग 158 यूनानी नगर-राज्यों का गहराई से अध्ययन कर राजनीति का एक व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया।
- अनुभवजन्य पद्धति का प्रयोग:
अरस्तू ने राजनीतिक अध्ययन में अनुभवजन्य (empirical) और तुलनात्मक पद्धति को अपनाया। उन्होंने अनेक राज्यों के संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक संरचना का तुलनात्मक विश्लेषण किया। यह वैज्ञानिक पद्धति राजनीति के अध्ययन में पहली बार लाई गई। - राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा:
अरस्तू ने राजनीति को “श्रेष्ठतम कला” कहा क्योंकि यह समाज की भलाई से जुड़ी है। उनके अनुसार राजनीति का उद्देश्य “सर्वोत्तम जीवन की प्राप्ति” है। उन्होंने इसे नैतिकता और दर्शन से जोड़ते हुए व्यावहारिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। - राज्य का उद्देश्य और प्रकृति:
अरस्तू के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी (Zoon Politikon) है। राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि नागरिकों को नैतिक और पूर्ण जीवन उपलब्ध कराना है। - शासन के प्रकार:
अरस्तू ने शासन के तीन शुद्ध रूप बताए –
(1) राजतंत्र (Monarchy)
(2) अरिस्टोक्रेसी (Aristocracy)
(3) पोलिटी (Polity)
तथा तीन विकृत रूप –
(1) तानाशाही (Tyranny)
(2) ओलिगार्की (Oligarchy)
(3) लोकतंत्र (Democracy)।
यह वर्गीकरण आज भी राजनीतिक विश्लेषण में उपयोग होता है। - मध्यवर्ग का महत्व:
अरस्तू ने राज्य में मध्यवर्ग की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि स्थिर और न्यायपूर्ण राज्य वही होता है जिसमें मध्यवर्ग शक्तिशाली होता है। यह विचार आधुनिक लोकतंत्र की नींव है। - संविधान और विधि:
अरस्तू ने संविधान को राज्य का प्राण कहा। उनके अनुसार प्रत्येक राज्य को ऐसा संविधान चाहिए जो उसके नागरिकों के नैतिक और सामाजिक मूल्यों के अनुसार हो।
अरस्तू का राजनीतिक चिन्तन तर्क, विश्लेषण और अनुभव के आधार पर था। उन्होंने राजनीति को आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिकता से जोड़ा। इस प्रकार, उन्होंने राजनीति को दर्शन से अलग करके उसे एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया। इसलिए उन्हें ‘प्रथम वैज्ञानिक राजनीतिक विचारक’ कहा जाता है।
प्रश्न-3. प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन में प्रतिपादित ‘सप्तांग सिद्धान्त’ की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- ‘सप्तांग सिद्धान्त’ (Saptanga Theory) प्राचीन भारतीय राजनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है, जिसका प्रमुख उल्लेख कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ और कामंदक के ‘नीतिसार’ में मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक राज्य सात आवश्यक अंगों से मिलकर बनता है। इन सात अंगों के संतुलन और सुदृढ़ता पर ही राज्य की स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि निर्भर करती है।
सप्तांग निम्नलिखित हैं:
- स्वामी (राजा):
राज्य का प्रमुख तत्व राजा होता है। राजा को धर्म, अर्थ और न्याय का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। वह योग्य, संयमी, विद्वान और न्यायप्रिय होना चाहिए। - अमात्य (मंत्री):
राज्य की नीति-निर्माण और प्रशासन में मंत्री वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे राजा के सलाहकार होते हैं और शासन को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। - जनपद (प्रजा और भू-भाग):
प्रजा राज्य का आधार है। जनपद का अर्थ न केवल भौगोलिक क्षेत्र से है, बल्कि वहाँ की जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि से भी है। - दुर्ग (किला):
दुर्ग सैन्य और प्रशासनिक सुरक्षा का प्रतीक है। यह शत्रु आक्रमण से रक्षा करता है। एक सुदृढ़ दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति को दर्शाता है। - कोश (कोष/धन):
कोश राज्य का वित्तीय संसाधन है। इससे युद्ध, प्रशासन और जनकल्याण के कार्य संचालित होते हैं। कुशल वित्त-प्रबंधन राज्य को आत्मनिर्भर बनाता है। - दंड (सेना):
राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए एक संगठित और अनुशासित सेना आवश्यक है। सेना आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की सुरक्षा देती है। - मित्र (सहयोगी राज्य):
राज्य को स्थायित्व और विस्तार के लिए मित्र राष्ट्रों की आवश्यकता होती है। कूटनीतिक संबंध, संधि और सहयोग नीति राज्य को मज़बूत बनाती है।
विशेषताएँ:
सप्तांग सिद्धांत राज्य की संरचना को एक समग्र और समन्वित दृष्टि से देखता है।
इसमें केवल राजा को ही नहीं, अपितु प्रजा, अर्थ, सुरक्षा और प्रशासन को भी समान रूप से महत्व दिया गया है।
यह सिद्धांत राज्य की स्थिरता, शक्ति और कल्याण का व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत करता है।
सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीति की गहराई और व्यावहारिकता को दर्शाता है। इसमें राज्य को केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि एक सजीव इकाई माना गया है जिसके सभी अंग आपस में जुड़े हुए हैं। यह सिद्धांत आज भी प्रशासन, रणनीति और राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से प्रासंगिक है।
प्रश्न-4. कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- कौटिल्य का ‘सप्तांग सिद्धांत’ प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति ‘अर्थशास्त्र’ में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक जीवित इकाई है, जो सात अंगों (तत्वों) से मिलकर बना होता है। ये सात अंग हैं — स्वामी (राजा), अमात्य (मंत्री), जनपद (प्रजा), दुर्ग (किला), कोष (धन), दण्ड (सेना) और मित्र (सहयोगी राज्य)।
- स्वामी (राजा): राजा राज्य का केंद्र होता है। वह बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वीर और धर्मनिष्ठ होना चाहिए। उसका आचरण प्रजा के लिए आदर्श होना चाहिए।
- अमात्य (मंत्री): योग्य, निष्ठावान एवं बुद्धिमान मंत्री शासन की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। वे नीतियों को बनाते और कार्यान्वित करते हैं।
- जनपद (प्रजा): प्रजा राज्य की आत्मा है। उनकी सुख-सुविधा और सुरक्षा राजा का प्राथमिक कर्तव्य है।
- दुर्ग (किला): बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग आवश्यक है। यह सामरिक दृष्टि से राज्य को सुरक्षित बनाता है।
- कोष (धन): समृद्ध कोष शासन के संचालन के लिए आवश्यक है। कर-संग्रह, व्यापार एवं संसाधन प्रबंधन के माध्यम से कोष को भरा जाता है।
- दण्ड (सेना): एक अनुशासित और सक्षम सेना राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।
- मित्र (सहयोगी राज्य): राजनीतिक स्थिरता और रक्षा के लिए मित्र राष्ट्रों का होना आवश्यक है। वे संकट के समय सहायता प्रदान करते हैं।
कौटिल्य के अनुसार ये सात अंग एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं और किसी भी अंग की कमजोरी राज्य की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। यह सिद्धांत राज्य की समग्र संरचना का वैज्ञानिक और यथार्थवादी विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
प्रश्न-5. मैकियावली के अनुसार राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक दशाओं की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- मैकियावली (Niccolò Machiavelli) एक यथार्थवादी राजनीतिक विचारक था, जिसने राज्य की स्थिरता के लिए व्यावहारिक और दूरदर्शी उपाय सुझाए। अपनी प्रसिद्ध कृति ‘द प्रिंस’ में उसने शासक को सुझाव दिया कि राज्य की स्थिरता बनाए रखने के लिए नैतिकता से अधिक सत्ता की वास्तविकता को समझना आवश्यक है।
राज्य की स्थिरता के लिए मैकियावली ने निम्नलिखित शर्तों को आवश्यक बताया:
- सशक्त नेतृत्व: शासक को निर्णायक, दृढ़ और दूरदर्शी होना चाहिए। वह संकटों में त्वरित और कठोर निर्णय लेने में सक्षम हो।
- जन समर्थन: राज्य तभी स्थिर रह सकता है जब प्रजा शासक से संतुष्ट हो। जनता का विश्वास और समर्थन शासक के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- बल प्रयोग की नीति: यदि आवश्यक हो, तो शासक को बल प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यह बल विवेकपूर्ण और समयानुकूल होना चाहिए।
- धर्म और परंपराओं का उपयोग: मैकियावली के अनुसार धर्म का प्रयोग जनता में अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए, भले ही शासक स्वयं धार्मिक न हो।
- राजनीतिक चातुर्य (Fox-like cunning): शासक को लोमड़ी की भाँति चालाक होना चाहिए ताकि वह षड्यंत्रों को पहचान सके और उनसे बच सके।
- सैनिक शक्ति: एक मजबूत सेना राज्य की रक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।
- नैतिकता से परे व्यवहार: शासक को परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णयों में नैतिक और अनैतिक दोनों उपायों का प्रयोग करने को तैयार रहना चाहिए।
मैकियावली का दृष्टिकोण पूर्णतः व्यावहारिक है। उसने आदर्श की बजाय यथार्थ को प्राथमिकता दी। उसके अनुसार राज्य की स्थिरता के लिए शासक को सफल होना चाहिए, भले ही उसे अनैतिक मार्ग अपनाने पड़ें।
प्रश्न-6. यूनानी राजनीतिक चिन्तन की विशेषताओं और महत्व की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- यूनानी राजनीतिक चिन्तन पश्चिमी राजनीतिक विचार परंपरा की नींव है। प्लेटो, अरस्तू, सुकरात जैसे दार्शनिकों ने राजनीति को नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता और राज्य की अवधारणा से जोड़ा। इनका चिंतन मुख्यतः 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फलित हुआ।
विशेषताएँ:
- दार्शनिक आधार: यूनानी चिंतन में राजनीति को दर्शन से जोड़ा गया। प्लेटो और अरस्तू ने राजनीति को नैतिकता और आदर्श राज्य से जोड़ा।
- न्याय और सद्गुण पर बल: प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य और आत्मा दोनों में संतुलन है। अरस्तू ने सद्गुण को राजनीतिक जीवन का आधार माना।
- नागरिकता की अवधारणा: यूनानी विचारकों ने नागरिक के कर्तव्य और अधिकारों पर विशेष बल दिया। उन्होंने सक्रिय नागरिक जीवन को आदर्श माना।
- राज्य का नैतिक उद्देश्य: यूनानियों के अनुसार राज्य का उद्देश्य मानव के नैतिक और बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करना है।
- लोकतंत्र और तानाशाही का विश्लेषण: प्लेटो और अरस्तू ने विभिन्न शासन प्रणालियों का विश्लेषण कर लोकतंत्र की सीमाओं को भी दर्शाया।
महत्त्व:
यूनानी चिन्तन ने राजनीति को एक विशिष्ट विषय के रूप में स्थापित किया।
राज्य, सरकार, कानून, न्याय और दायित्व जैसे मूलभूत राजनीतिक विचारों की नींव रखी।
यह चिन्तन आज भी राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या में उपयोगी है।
इस प्रकार यूनानी राजनीतिक चिन्तन ने आधुनिक राजनीतिक विचारों की नींव रखी और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है।
प्रश्न-7. हॉब्स के विचारों में समझौते की क्या शर्तें थीं और उसका क्या परिणाम रहा?
उत्तर:-थॉमस हॉब्स के सामाजिक संविदा सिद्धांत का आधार यह है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में युद्ध, भय और असुरक्षा के जीवन में जी रहा था। वहाँ कोई कानून, शांति या संपत्ति की गारंटी नहीं थी। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए मानव ने आपसी समझौते (Contract) द्वारा राज्य की स्थापना की।
समझौते की शर्तें:
- सभी व्यक्तियों की सहमति: सभी व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता छोड़कर एक सर्वशक्तिमान सत्ता को सौंप देंगे।
- संपूर्ण अधिकारों का हस्तांतरण: प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से एक संप्रभु (Sovereign) को सौंप दिया ताकि वह सभी के ऊपर शासन कर सके।
- द्विपक्षीय नहीं, एकपक्षीय अनुबंध: यह अनुबंध नागरिकों के बीच था, न कि संप्रभु और नागरिकों के बीच। संप्रभु इस अनुबंध का पक्ष नहीं था।
- संप्रभु को जवाबदेही नहीं: एक बार संप्रभु को अधिकार मिल गए, तो वह अपनी शक्ति के लिए नागरिकों के प्रति उत्तरदायी नहीं था।
परिणाम:
- एक मजबूत राज्य की स्थापना: इससे एक शक्तिशाली राज्य की नींव पड़ी, जो आंतरिक शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- संपत्ति और जीवन की रक्षा: राज्य अब नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करता है।
- स्वतंत्रता का समर्पण: नागरिकों ने अपनी स्वतंत्रता के बदले सुरक्षा प्राप्त की।
- निरंकुश सत्ता: संप्रभु की शक्ति असीम और निरंकुश मानी गई। वह कानून से ऊपर था।
- विद्रोह का अधिकार नहीं: नागरिकों को संप्रभु के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं था।
हॉब्स के अनुसार, अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक सर्वशक्तिमान संप्रभु की स्थापना की ताकि वे अपने भय और संघर्ष से मुक्त हो सकें। यद्यपि यह प्रणाली निरंकुश लग सकती है, हॉब्स के लिए यह सामाजिक शांति और स्थिरता के लिए अनिवार्य थी।
प्रश्न-8. क्रांति के सम्बन्ध में अरस्तु के विचारों का परीक्षण कीजिए।
उत्तर:- अरस्तू क्रांति को राज्य के लिए एक स्वाभाविक परंतु खतरनाक प्रक्रिया मानता था। वह यह मानता था कि यदि राज्य में असमानता, अन्याय और दमन की स्थिति बनी रहती है, तो वहाँ क्रांति अवश्य होती है। उसने ‘राज्य का पतन’ और ‘शासन-परिवर्तन’ को क्रांति का रूप बताया।
क्रांति के कारण:
- असमानता: समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता क्रांति का प्रमुख कारण होती है।
- न्याय की भावना का उल्लंघन: जब नागरिकों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वे विद्रोह करते हैं।
- अधिकारों में भेदभाव: जब कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिलते हैं और अन्य उपेक्षित रहते हैं।
- शासन का भ्रष्टाचार: नेताओं की अयोग्यता और भ्रष्टाचार क्रांति को जन्म देती है।
- राजनीतिक अस्थिरता: शासन के रूपों में लगातार परिवर्तन और अस्थिरता।
क्रांति की रोकथाम हेतु सुझाव:
- मिश्रित शासन प्रणाली: अरस्तू ने कहा कि लोकतंत्र और कुलीनतंत्र का संयोजन स्थायित्व प्रदान करता है।
- मध्यम वर्ग की भूमिका: उसने मध्यम वर्ग को राजनीतिक स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण बताया।
- न्याय की स्थापना: प्रत्येक वर्ग के साथ न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।
- संविधान का सम्मान: कानून और संविधान का पालन सभी को करना चाहिए।
अरस्तू क्रांति को नकारात्मक मानता है लेकिन उसकी आवश्यकता और कारणों को समझते हुए, उसने शासन व्यवस्था में सुधार के उपाय भी सुझाए। उसकी सोच आज भी राजनीतिक अस्थिरता के अध्ययन में प्रासंगिक मानी जाती है।
प्रश्न-9. प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों द्वारा प्रतिपादित राजा के कार्यों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा को ‘धर्म का संरक्षक’, ‘प्रजा का रक्षक’ और ‘न्याय का अधिष्ठाता’ माना गया है। मनु, याज्ञवल्क्य, कौटिल्य, महाभारत आदि ग्रंथों में राजा के अनेक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है।
प्रमुख कर्तव्य:
- धर्म की रक्षा: राजा का प्रथम कर्तव्य धर्म (नैतिकता और धार्मिकता) की स्थापना करना है। वह धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शासन करता है।
- प्रजा की सुरक्षा: राजा को अपनी प्रजा की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है।
- न्यायिक व्यवस्था: राजा को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना चाहिए। दंड नीति के अनुसार दुष्टों को दंड और सज्जनों को सम्मान देना चाहिए।
- राजस्व की व्यवस्था: कर वसूली, अर्थव्यवस्था, व्यापार और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा पर होती है।
- सेना का संचालन: राजा को एक सुदृढ़ सेना का संचालन करना चाहिए ताकि राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाया जा सके।
- अधिकारियों की नियुक्ति: योग्य और ईमानदार मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करना।
- प्रजा का कल्याण: सार्वजनिक कार्यों, जैसे सड़क, जल, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।
प्राचीन भारतीय चिंतकों ने राजा को न केवल प्रशासनिक बल्कि नैतिक और धार्मिक उत्तरदायित्वों से युक्त माना। एक आदर्श राजा वही होता है जो ‘लोककल्याण’ को अपना ध्येय बनाए।
प्रश्न-10. हॉब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संविदा सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- थॉमस हॉब्स का सामाजिक संविदा सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक चिंतन का आधार स्तंभ है। उसने बताया कि राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा हुई थी, न कि ईश्वर की इच्छा से।
प्राकृतिक अवस्था:
प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र था, परंतु वहाँ कोई कानून, सुरक्षा या व्यवस्था नहीं थी।
सभी एक-दूसरे से डरते थे। इसे हॉब्स ने “Man is a wolf to man” कहा।
इस स्थिति को हॉब्स ने “war of all against all” बताया।
सामाजिक संविदा:
असुरक्षा से बचने के लिए लोगों ने आपसी समझौते से एक संप्रभु को अपने अधिकार सौंपे।
यह अनुबंध नागरिकों के बीच था, न कि संप्रभु के साथ।
संप्रभु को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हुई, जिससे वह कानून बनाए और शांति बनाए रखे।
संप्रभु के गुण:
वह निरंकुश होता है।
वह कानून से ऊपर होता है।
विद्रोह का कोई अधिकार नहीं होता।
हॉब्स का सामाजिक संविदा सिद्धांत यह बताता है कि राज्य इसलिए बना क्योंकि व्यक्ति शांति, सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था चाहता था। राज्य की सत्ता संप्रभु को दी गई ताकि वह सबका कल्याण कर सके।
प्रश्न-11. राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में मैकियावली के विचारों का परीक्षण कीजिए।
उत्तर:- मैकियावली ने अपने ग्रंथ “The Prince” और “Discourses” में राज्य की स्थिरता (Stability of State) के लिए कई आवश्यक शर्तें बताई हैं। उसके अनुसार राज्य का मुख्य लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना, उसे बनाए रखना और स्थायित्व सुनिश्चित करना है।
मुख्य शर्तें:
- मजबूत नेतृत्व: राज्य के स्थायित्व के लिए एक शक्तिशाली और निर्णायक नेतृत्व आवश्यक है।
- दंड नीति: अपराधों पर कठोर दंड देना राज्य में अनुशासन बनाए रखता है।
- सैन्य शक्ति: राज्य की रक्षा के लिए एक स्वदेशी और सशक्त सेना होनी चाहिए।
- धोखे और चालाकी की अनुमति: यदि राज्य की भलाई के लिए छल-कपट करना पड़े तो वह उचित है।
- धार्मिकता का उपयोग: धर्म का प्रयोग जनता को नियंत्रित करने और एकता बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।
- जनता का समर्थन: राज्य को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रजा का समर्थन आवश्यक है।
- वास्तविकता पर आधारित नीतियाँ: शासक को आदर्शों के बजाय यथार्थ पर आधारित नीति अपनानी चाहिए।
मैकियावली की दृष्टि में राज्य की स्थिरता का मूल उद्देश्य शक्ति का संरक्षण और प्रजा का नियंत्रण है। उसकी यथार्थवादी नीति आज के समय में भी राजनीतिक रणनीति में प्रासंगिक मानी जाती है।
प्रश्न-11.उपयोगितावाद सिद्धान्त में मिल द्वारा किए गए संशोधन को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill) ने जेरमी बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत में महत्वपूर्ण संशोधन किए। जबकि बेंथम मात्र “सुख की मात्रा” को प्राथमिकता देते थे, मिल ने उसमें “सुख की गुणवत्ता” को भी शामिल किया।
मिल द्वारा किए गए मुख्य संशोधन निम्नलिखित हैं:
- सुख की गुणवत्ता बनाम मात्रा – मिल ने कहा कि सभी सुख समान नहीं होते। मानसिक सुख (जैसे – ज्ञान, कला, नैतिकता) शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ होते हैं। उदाहरण: “एक असंतुष्ट मानव, संतुष्ट सुअर से बेहतर है।”
- व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता – मिल ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित रहनी चाहिए जब तक वह दूसरों को नुकसान न पहुँचाए। यह विचार “On Liberty” में देखा जा सकता है।
- न्याय और नैतिकता का समावेश – मिल ने उपयोगितावाद में न्याय और नैतिक मूल्यों को भी महत्व दिया। उन्होंने माना कि न्याय और नैतिकता सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक हैं।
- दीर्घकालिक दृष्टिकोण – बेंथम का दृष्टिकोण तात्कालिक था, जबकि मिल ने कहा कि नीति निर्माण में दीर्घकालिक प्रभावों को भी देखा जाना चाहिए।
इस प्रकार मिल ने बेंथम के मात्रात्मक और यांत्रिक उपयोगितावाद को अधिक मानवीय, नैतिक और व्यावहारिक रूप प्रदान किया। मिल का उपयोगितावाद अधिक परिपक्व और आधुनिक समाज के अनुरूप माना जाता है।
प्रश्न-13. राज्य पर बेंथम के विचार बताइए।
उत्तर:- जेरमी बेंथम (Jeremy Bentham) एक प्रमुख अंग्रेज़ दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने उपयोगितावाद (Utilitarianism) को राज्य के सिद्धांत के साथ जोड़ा। बेंथम का मानना था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, जिसका अस्तित्व केवल इसलिए है कि वह अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान कर सके।
बेंथम का मुख्य सिद्धांत था:
“सर्वाधिक लोगों के लिए सर्वाधिक सुख” (Greatest Happiness of the Greatest Number)। उनके अनुसार, कोई भी कानून या राज्य व्यवस्था तभी उचित मानी जाएगी जब वह समाज के अधिकतर लोगों को अधिकतम लाभ पहुँचाए।
बेंथम ने राज्य को निम्नलिखित रूप में देखा:
- राज्य का उद्देश्य – नागरिकों के सुख और भलाई की रक्षा करना।
- कानून और शासन – न्याय वही है जो लोगों के सुख को बढ़ाए; इसलिए कानून बनाते समय जनसामान्य की भलाई का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- स्वतंत्रता – बेंथम के अनुसार स्वतंत्रता कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक उपयोगितावादी साधन है जो सामाजिक भलाई में सहायक है।
- लोकतंत्र का समर्थन – उन्होंने प्रतिनिधि लोकतंत्र और सार्वभौमिक मताधिकार का समर्थन किया।
बेंथम ने राज्य को एक उपकरण माना जिसका उद्देश्य सामाजिक उपयोगिता बढ़ाना है। वे राज्य को नैतिक और न्यायपूर्ण तभी मानते थे जब वह व्यावहारिक और लोककल्याणकारी हो।
प्रश्न14.राज्य के महत्त्व के बारे में यूनानी राजनीतिक चिन्तकों के विचार स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- यूनानी राजनीतिक चिन्तकों जैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को जीवन का आवश्यक अंग माना। उनके अनुसार राज्य केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक उन्नति का माध्यम है।
सुकरात ने राज्य को नैतिक जीवन का साधन माना। उन्होंने कहा कि राज्य व्यक्ति की आत्मा के समान होता है, जहाँ ज्ञान, साहस और इच्छा संतुलित होते हैं।
प्लेटो के अनुसार राज्य आत्मा की तर्ज पर बना है। उन्होंने कहा कि न्याय वह स्थिति है जब राज्य के तीन वर्ग (दार्शनिक – शासन, सैनिक – रक्षा, उत्पादक – सेवा) अपने-अपने कार्यों को निभाते हैं। व्यक्ति राज्य के भीतर ही न्यायपूर्ण और पूर्ण जीवन जी सकता है। उन्होंने दार्शनिक राजा की कल्पना की।
अरस्तु ने तो यहाँ तक कहा – “मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है”, और राज्य व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। उनका मानना था कि व्यक्ति राज्य से बाहर पशु या ईश्वर जैसा होता है। राज्य के बिना न नैतिकता संभव है और न ही न्याय।
यूनानी चिंतकों ने राज्य को स्वाभाविक, नैतिक और आवश्यक संस्था माना जो व्यक्ति को केवल सुरक्षा ही नहीं, अपितु नैतिक विकास और समाज में सामंजस्य प्रदान करती है। उनके लिए राज्य आत्मा की पूर्णता का भौतिक रूप था।
प्रश्न15.
उत्तर:-
vmou maps-01 paper , vmou ma 1st year exam paper , vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4