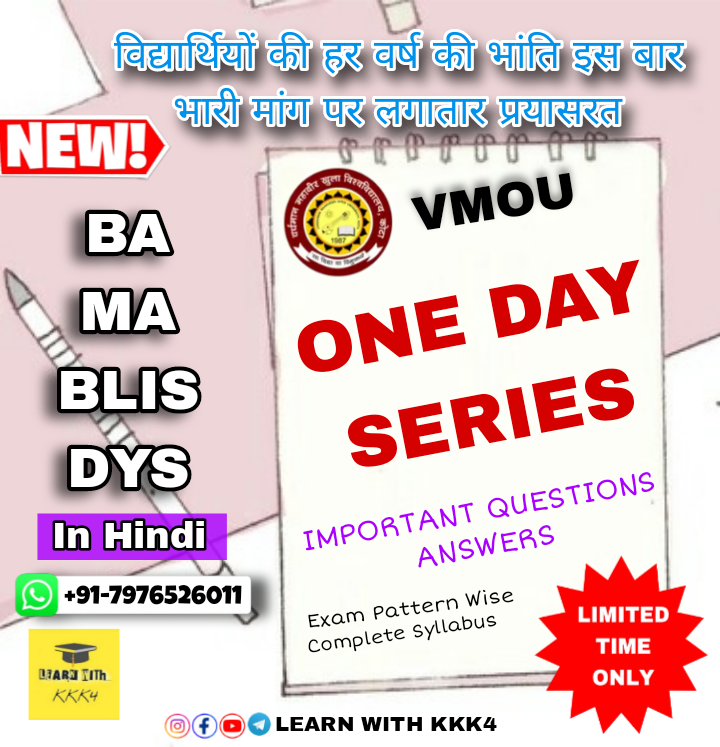VMOU MAHD-01 Paper MA 1ST Year
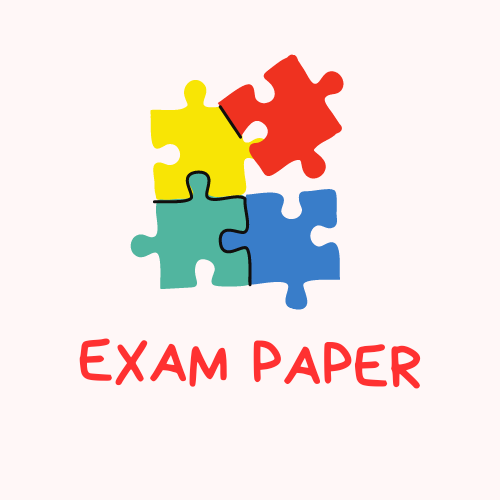
VMOU MA First Year के लिए हिन्दी साहित्य ( MAHD-01 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.विद्यापति कृत किन्हीं दो रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए।
उत्तर:- पदावली और कीर्तिलता विद्यापति की प्रमुख रचनाएँ हैं
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.पृथ्वीराज रासो के विवादास्पद होने के कोई दो कारण लिखिए
उत्तर:- ऐतिहासिक तथ्यों में असमानता और अनेक संस्करणों का होना इसे विवादास्पद बनाता है।
प्रश्न-3.सूफी काव्य में इश्क मज़ाजी और इश्क हकीकी से क्या तात्पर्य है ?
उत्तर:- इश्क मज़ाजी सांसारिक प्रेम है, जबकि इश्क हकीकी ईश्वर से आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है।
प्रश्न-‘4 बिहारी सतसई’ की कोई दो विशेषताएं बताइए।
उत्तर:- संक्षिप्तता में गूढ़ भाव, और श्रृंगारिक व नैतिक विषयों की कलात्मक अभिव्यक्ति इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं।
प्रश्न-5 कवि भूषण के काव्य की विशिष्टता लिखिए।
उत्तर:- वीर रस, ओजस्विता और शिवाजी व औरंगज़ेब जैसे पात्रों की प्रशस्ति उनकी काव्य की विशेषता है।
प्रश्न-6कबीर काव्य में ‘साखी’ शब्द को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- साखी दोहे के रूप में कबीर की शिक्षापरक वाणी है, जो नैतिकता व भक्ति पर आधारित होती है।
प्रश्न-7 घनानंद की किन्हीं दो रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए।
उत्तर:- रीतिकाव्य और अनुराग बांसुरी उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।
प्रश्न-8 तुलसीदास की किन्हीं दो काव्य रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए।
उत्तर:- रामचरितमानस , कवितावली और विनय पत्रिका
प्रश्न-9 रीतिसिद्ध काव्यधारा का तात्पर्य क्या है ?
उत्तर:- रीतिसिद्ध काव्यधारा में काव्यशास्त्र के नियमों और श्रृंगारिक तत्वों पर विशेष बल दिया जाता है।
प्रश्न-10 ‘विनयपत्रिका’ की काव्य संवेदना को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- ‘विनयपत्रिका’ में भक्ति, आत्मसमर्पण, दीनता और रामभक्ति की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है।
प्रश्न-11. सूरदास की सख्य भक्ति भावना से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- सूरदास की सख्य भक्ति में गोपियों की तरह कृष्ण से मित्रवत प्रेम संबंध की भावना व्यक्त की गई है।
प्रश्न-12 मीरा का जीवन परिचय संक्षेप में लिखिए।
उत्तर:- मीरा 16वीं शताब्दी की भक्त कवयित्री थीं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पित कर दिया।
प्रश्न-13 मैथिल कोकिल’ किस कवि को कहा जाता है ?
उत्तर:- विद्यापति को ‘मैथिल कोकिल’ कहा जाता है।
प्रश्न-14 पद्माकर की किन्हीं दो काव्य कृतियों का नामोल्लेख कीजिए।
उत्तर:- जंगनामा और हित तरंगिणी पद्माकर की प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं।
प्रश्न-15 भूषण की कविता में राष्ट्रीय भावना को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-भूषण की कविता में मुगलों के विरुद्ध हिंदवी स्वाभिमान, शिवाजी व छत्रसाल की वीरता की प्रशंसा कर राष्ट्रीय चेतना व्यक्त की गई है।
प्रश्न-16 घनानन्द को रीतिमुक्त काव्यधारा का प्रमुख कवि क्यों माना जाता है ?
उत्तर:- क्योंकि उनकी कविता में निजी पीड़ा, विरह, और भावप्रवणता रीतिकालीन औपचारिकता से हटकर है।
प्रश्न-17 रीतिमुक्त बद्ध काव्यधारा से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:- ऐसी काव्यधारा जो शृंगारिक रीति-नियमों से मुक्त होकर भक्ति, अनुभूति और आत्मानुभूति को अभिव्यक्त करती है।
प्रश्न-18 विद्यापति को कौन-कौनसी उपाधियाँ मिलीं?
उत्तर:- मैथिल कोकिल, गीतशिरोमणि, अभिनव जयदेव।
प्रश्न-19. बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं?
उत्तर:- शृंगारप्रधान रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं।
प्रश्न-20. अति सूधो सनेह को मारग है’ पंक्ति किस कवि की है?
उत्तर:- सूरदास।
प्रश्न-21. ‘नैन नचाई कह्यो मुसकाई लला फिरि अइयौ खेलन होरी’ पंक्ति किस कवि की है?
उत्तर:- सूरदास।
प्रश्न-22. जायसी के पद्मावत की भाषा कौनसी है
उत्तर:- अवधी मिश्रित फारसी शब्दों के साथ।
प्रश्न-23. किन्हीं तीन रासो ग्रन्थों के नाम लिखिए।
उत्तर:- पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो
प्रश्न-24. विद्यापति की ‘पदावली’ किस भाषा में रचित है?
उत्तर:- मैथिली भाषा में।
प्रश्न-25 कबीरदास भक्तिकालीन की किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं?
उत्तर:- निर्गुण भक्ति काव्यधारा।
प्रश्न-26. जायसी की रचनाओं के नाम लिखिए।
उत्तर:- पद्मावत, अखरावट, चंद्रावती।
प्रश्न-27. तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था?
उत्तर:- रामबोला।
प्रश्न-28. अष्टछाप के कवियों के नाम लिखिए।
उत्तर:- सूरदास, कुंभनदास, नंददास, परमानंददास, गोविंदस्वामी, कृष्णदास, छीतस्वामी, चतुर्भुजदास
प्रश्न-29. भूषण की कविता में कौनसा रस है एवं उनके काव्य की मुख्य विशेषता क्या है?
उत्तर:- वीर रस; विशेषता—ओजपूर्ण शैली, राष्ट्रभक्ति और वीरता का चित्रण।
प्रश्न-30. मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी?
उत्तर:-माधुर्यभाव प्रधान सगुण भक्ति, जहाँ कृष्ण को पति रूप में आराध्य माना।
प्रश्न-31.
उत्तर:-
प्रश्न-32.
उत्तर:-
प्रश्न-33.
उत्तर:-
प्रश्न-34.
उत्तर:-
प्रश्न-35.
उत्तर:-
प्रश्न-36.
उत्तर:-
प्रश्न-37.
उत्तर:-
प्रश्न-38.
उत्तर:-
प्रश्न-39
उत्तर:-
प्रश्न-40.
उत्तर:-
Section-B
प्रश्न-1.मीरा के काव्य में लोकसंस्कृति का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- मीरा का काव्य भारतीय लोकसंस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। उनके भजनों में लोक-जीवन, परंपराएँ, त्योहार, रीति-रिवाज और ग्रामीण समाज की सादगी की स्पष्ट झलक मिलती है। मीरा ने अपने काव्य में ग्रामीण भाषा, लोकप्रचलित प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया है, जिससे उनकी रचनाएँ सहज, सरल और जनमानस के हृदय से जुड़ी हुई लगती हैं।उनके पदों में लोकगीतों की तर्ज पर रचना, रासलीला की छवियाँ, गोवर्धन पूजा, फाग, होली, झूला आदि लोकत्योहारों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने राधा-कृष्ण की लीलाओं को ग्रामीण स्त्री के भावों से जोड़कर प्रस्तुत किया है। गाय, ग्वाल-बाल, कुएं, पीहर-ससुराल, सखियाँ, ये सभी लोकजीवन के अंग उनके भजनों में विद्यमान हैं।
मीरा के गीतों में लोकभाषा राजस्थानी व ब्रज की मिश्रित शैली मिलती है, जो उनके भक्ति भाव को जन-जन तक पहुँचाती है। इस प्रकार मीरा का काव्य न केवल भक्ति साहित्य का अनमोल रत्न है, बल्कि भारतीय लोकसंस्कृति का गहरा प्रतिबिंब भी है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.पद्माकर के काव्य में प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- पद्माकर, रीतिकालीन कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके काव्य में प्रकृति का अत्यंत सुंदर और जीवंत चित्रण मिलता है। वे प्रकृति को न केवल सौंदर्य के रूप में देखते हैं, बल्कि उसे काव्य भावों की अभिव्यक्ति का साधन भी बनाते हैं।
पद्माकर ने ऋतुओं, पुष्पों, पक्षियों, पर्वतों, नदियों और वनों का वर्णन बड़े ही चित्रात्मक ढंग से किया है। बसंत ऋतु, वर्षा, सरसों के खेत, कोयल की कूक, कमल, कदंब वृक्ष आदि उनकी रचनाओं में प्रमुखता से स्थान पाते हैं।
उन्होंने प्रकृति को श्रृंगारिक दृष्टिकोण से देखा — प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से प्रेमी-प्रेमिका की मनःस्थितियाँ प्रकट कीं। उनके काव्य में प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि वह नायक-नायिका की भावनाओं की संवाहिका बनकर प्रस्तुत होती है।
‘जगद्विनोद’, ‘पद्मावती’, ‘रसमाधुरी’ आदि में उनका प्रकृति वर्णन अत्यंत आकर्षक एवं संवेदनशील है। पद्माकर के प्रकृति चित्रण में रंग, गंध, रूप, गति — सभी का सामंजस्य मिलता है, जो उन्हें प्रकृति सौंदर्य के कवि के रूप में प्रतिष्ठित करता है।
प्रश्न-3.कबीरदास के समाज सुधारक रूप की समीक्षा कीजिए।
उत्तर:- कबीरदास केवल संत और कवि ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उनका समूचा काव्य जाति-पाँति, धर्मांधता, पाखंड और सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध एक सशक्त आवाज़ के रूप में सामने आया।
कबीर का जन्म एक मुसलमान जुलाहा परिवार में हुआ, लेकिन वे न हिन्दू बने न मुसलमान। वे धर्मों की रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। उन्होंने दोनों धर्मों की कुरीतियों की आलोचना की — जैसे हिन्दुओं की मूर्ति पूजा और मुसलमानों के कट्टर कर्मकांड।
उनका प्रसिद्ध दोहा है:
“पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहार।
ता ते तो चाकी भली, पीस खाय संसार॥”
कबीर ने सत्य, प्रेम, सेवा, नामस्मरण और आत्मचिंतन को श्रेष्ठ मार्ग बताया। वे निर्गुण भक्ति मार्ग के प्रवर्तक थे, जिसमें ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापक माना गया।
उन्होंने स्त्री-पुरुष समानता, कर्म की महत्ता और मानवता की भावना को बल दिया। उनके काव्य ने समाज के निम्न वर्गों को चेतना दी और उन्हें आत्मगौरव प्रदान किया।
इस प्रकार कबीरदास समाज सुधारक के रूप में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और सत्य के प्रचारक बनकर सामने आते हैं।
प्रश्न-4.गीतिकाव्य परम्परा में विद्यापति का स्थान निर्धारित कीजिए।
उत्तर:- विद्यापति गीतिकाव्य परंपरा के अत्यंत प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। वे मैथिली भाषा के प्रथम महाकवि और ‘मैथिल कोकिल’ के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके गीत मुख्यतः राधा-कृष्ण के प्रेम विषयक हैं, जिनमें श्रृंगार रस की परिपक्वता मिलती है।
गीतिकाव्य में विद्यापति ने भाव, भाषा और छंद की मधुरता से नायिका-नायक के प्रेम को अत्यंत कोमलता के साथ प्रस्तुत किया। उनके गीतों में स्त्री-हृदय की अंतरंग भावनाएँ अत्यंत सजीव रूप में चित्रित हैं, जिससे वे लोकगीतों के निकट प्रतीत होते हैं।
उन्होंने गीतों में भाषा की सजीवता, अलंकारों की स्वाभाविकता और लय की मधुरता को बनाए रखा, जो गीतिकाव्य की पहचान है। विद्यापति के पदों की प्रसिद्धि इतनी अधिक हुई कि ब्रजभाषा, अवधी और राजस्थानी के भक्त कवियों ने भी उनकी शैली को अपनाया।
प्रश्न-5.घनानंद’ प्रेम की पीर के कवि हैं। इस कथन की समीक्षा कीजिए।
उत्तर:- घनानंद रीतिकाल के अंतिम चरण के प्रमुख कवि हैं, जिन्हें ‘प्रेम की पीर’ का कवि कहा जाता है। उनके काव्य में श्रृंगार रस का आध्यात्मिक रूप देखा जाता है। वे कृष्ण भक्त थे, परंतु उनका प्रेम केवल भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि उसमें विरह, वेदना और मानवीय संवेदनाओं की गहनता भी विद्यमान है।
घनानंद की रचनाओं में प्रेम का मार्मिक चित्रण मिलता है — कहीं अनुराग है, कहीं वियोग, कहीं उपालम्भ, तो कहीं आत्मविलीनता। उनके प्रसिद्ध पदों में ‘घनानंद कहें रसिकन रास रचौ’ जैसे भाव प्रेम में समर्पण की उत्कटता दिखाते हैं।
उनका प्रेम संकोच रहित, आत्मा से जुड़ा हुआ और पीड़ा से परिपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन में भी प्रेम को सर्वोपरि माना और एक नर्तकी से प्रेम कर महल त्याग दिया था। यही अनुभव उनके काव्य में भी दिखाई देता है।
प्रश्न-6.तुलसीदास की काव्य रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
उत्तर:-तुलसीदास हिन्दी साहित्य के महानतम कवियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय भाषा में जन-जन तक पहुँचाया। उनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता, नैतिकता, नीति और भक्ति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है।
मुख्य रचनाएँ:
रामचरितमानस: तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध रचना है। यह भगवान राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें भक्ति, नीति और आदर्श जीवन मूल्यों का समावेश है।
विनयपत्रिका: यह 279 पदों की एक भावप्रधान रचना है जिसमें भक्त की विनय, करुणा और आत्मसमर्पण का मार्मिक चित्रण है।
कवितावली: इस रचना में राम के युद्ध-प्रसंगों का वीर रस में वर्णन किया गया है।
गीतावली: राम कथा को गीत शैली में प्रस्तुत करती है। इसमें श्रृंगार और भक्ति रस का सुंदर समावेश है।
प्रश्न-7.निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए :
नन्दक नन्दन कदम्बे तरुतरे टरलि बोलाव… वन्दहु नन्दकिसोरा॥
उत्तर:- सप्रसंग व्याख्या:
यह पद्यांश मैथिल कोकिल विद्यापति की ब्रज भाषा में रचित कृष्ण भक्ति रचना का भाग है। इसमें राधा और कृष्ण के मिलन की व्याकुलता को अत्यंत कोमल रूप में प्रस्तुत किया गया है।
संदर्भ:
यह पद ‘विद्यापति पदावली’ से लिया गया है, जिसमें राधा का सखी से संवाद है। इसमें राधा द्वारा कृष्ण की व्याकुल प्रतीक्षा का चित्रण है।
व्याख्या:
सखी कहती है कि राधा ने समय का संकेत देकर कृष्ण को मिलने के लिए बुलाया था, किंतु अब राधा स्वयं ही संकोचवश अपने घर से बार-बार दूत भेजकर उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन कृष्ण तो राधा के प्रेम में इतने व्याकुल हैं कि यमुना तट पर, उपवन में बार-बार आते-जाते हैं। वे बार-बार उस स्थान को देख रहे हैं जहाँ राधा से मिलन संभव हो। चारों ओर प्रेम की सुगंध और संकेत फैले हुए हैं। इस प्रेम की अद्भुत लीला देखकर कवि विद्यापति अंत में नंदकिशोर (कृष्ण) की वंदना करते हैं।
प्रश्न-8.निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए:
पद्यांश:
मोकों कहाँ ढूँढें बन्दे, मैं तो तेरे पास में… सब स्वासन की स्वाँस में।
उत्तर:- सप्रसंग व्याख्या:
यह पद कबीर की भक्ति भावना और निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा को दर्शाता है। इसमें उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता और सगुण-निर्गुण की सीमाओं को नकारते हुए अंत:करण में ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार किया है।
संदर्भ:
यह पद कबीर के भक्ति काव्य से लिया गया है जिसमें वे व्यक्ति को बाह्य आडंबर छोड़कर आत्मा में ईश्वर की खोज करने की प्रेरणा देते हैं।
व्याख्या:
कबीर कहते हैं, “हे मनुष्य! तू मुझे कहाँ ढूंढ़ता है? मैं तो तेरे भीतर, तेरे पास में ही हूँ।” वे स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर किसी विशेष स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, काबा या कैलास में नहीं है। न वह कर्मकांड में है, न योग और वैराग्य में। जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे हृदय से खोज करता है, उसे ईश्वर पल भर में मिल सकता है। ईश्वर हर जीव की साँसों में, उसके अस्तित्व में विद्यमान है।
निष्कर्ष:
कबीर का यह पद आत्मज्ञान, साधना और अंतरात्मा की खोज की ओर प्रेरित करता है। यह भक्ति की गहराई और सहजता का परिचायक है।
प्रश्न-9.आपसी की काव्य रचनाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।
उत्तर:- आलम आपसी अवधी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। वे मध्यकालीन काव्य परंपरा में भक्ति और प्रेम के सूफी मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका काव्य मुख्यतः प्रेम और अध्यात्म का मिश्रण है।
उनकी प्रमुख रचना ‘माधवानल-कामकंदला’ है, जिसमें उन्होंने एक प्रेम कथा को आधार बनाकर सूफी दर्शन के गूढ़ तत्वों की अभिव्यक्ति की है। इसमें सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम की ओर उन्मुख करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
आलम आपसी की भाषा अवधी है, जिसमें फारसी शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है। उनकी शैली भावपूर्ण, लयबद्ध और सहज है, जो जनमानस के निकट प्रतीत होती है।
उनकी काव्य-शैली में रहस्यवाद, रूपक शैली और प्रतीकों का प्रयोग प्रमुखता से दिखाई देता है। उन्होंने प्रेम को ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम माना और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई।
प्रश्न-10. ‘मीरा के काव्य में लोक संस्कृति की झाँकी दिखाई देती है।” इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- प्रश्न 1 सेक्शन-ब
प्रश्न-11. पद्माकर के काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- प्रश्न-2 सेक्शन ब
प्रश्न-12.निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए :
पद्यांश:
तेरी म्हां तो दरद दिवाणी… जद बैर सांवरो होय।
उत्तर:- सप्रसंग व्याख्या:
यह पद मीरा बाई की रचना है, जो उनके कृष्णप्रेम, आत्मबलिदान और विरह वेदना को दर्शाता है। मीरा की भक्ति एकनिष्ठ और भावपूर्ण है, जिसमें वे अपने प्राणप्रिय प्रभु को प्रेम के माध्यम से पाने की लालसा रखती हैं।
संदर्भ:
यह पद मीरा की भक्तिमयी पीड़ा और प्रभु प्रेम के समर्पण भाव का सुंदर उदाहरण है।
व्याख्या:
मीरा कहती हैं कि वे केवल अपने प्रभु के प्रेम में दीवानी हैं। उनके हृदय का दर्द कोई नहीं समझता। घायल हृदय की पीड़ा केवल वही जानता है जो स्वयं घायल हो। मीरा इस पीड़ा को लेकर दर-दर भटकी हैं, पर कोई वैद्य (उपचारक) नहीं मिला। वह अपने मन की पीड़ा प्रभु के सामने रखती हैं। अंत में वे कहती हैं, “हे प्रभु! मेरी यह पीड़ा तब ही मिटेगी जब तू मेरा हो जाएगा।”
निष्कर्ष:
मीरा का यह पद विरह-वेदना, आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इसमें लोकभाषा की सहजता और भावनाओं की गहराई का सुंदर समन्वय है।
प्रश्न-13. विद्यापति श्रृंगारिक या भक्त कवि थे? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- विद्यापति एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे, जिनकी रचनाओं में श्रृंगार और भक्ति दोनों का अद्भुत समन्वय मिलता है। वे मैथिली भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रारंभ में उन्होंने श्रृंगारिक पदों की रचना की जिनमें राधा-कृष्ण के मधुर प्रेम को आधार बनाया गया। इन पदों में राधा-कृष्ण की चेष्टाएँ, मिलन-विरह, मान-मनुहार आदि का बड़ा ही कोमल चित्रण हुआ है।
उदाहरण:
“सखि हे! मोरे उर अंतर में, सदा बसे कृष्ण मुरारी।”
इस प्रकार के पदों में श्रृंगार रस की माधुरी भक्ति में परिवर्तित हो जाती है।
कालांतर में विद्यापति ने भक्ति काव्य की ओर रुख किया और भगवान शिव की स्तुति में भी पद लिखे। उनकी भक्ति भावना विशेषतः ‘शिव स्तुति’ और ‘कीर्तन’ में प्रकट होती है।
निष्कर्ष:
विद्यापति मूलतः श्रृंगारिक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, परंतु उनमें भक्ति तत्व भी गहराई से विद्यमान है। इसलिए उन्हें ‘श्रृंगार-भक्ति के सेतु’ कवि के रूप में देखा जा सकता है।
प्रश्न-14. जायसी के प्रकृति-चित्रण की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी भक्त कवि थे जिन्होंने प्रकृति का चित्रण अत्यंत भावपूर्ण एवं प्रतीकात्मक शैली में किया। उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत में प्रकृति-चित्रण सौंदर्य और संवेदना का अनूठा मिश्रण है।
प्रकृति-चित्रण की विशेषताएँ:
- मानव भावनाओं की प्रतीक: जायसी ने प्रकृति को केवल दृश्य सौंदर्य नहीं, बल्कि भावनाओं की प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। वर्षा ऋतु में पद्मिनी की उदासी और लंका की हरियाली में रतनसेन का आकर्षण इस बात का प्रमाण है।
- मानवीकरण: उन्होंने पर्वत, नदी, फूल, पक्षियों आदि को मानवीय गुणों से युक्त किया। जैसे— “नैन जरत जल बरसै”— में आँखों से जल बरसने का भाव वर्षा से जोड़ा।
- सूफी दृष्टिकोण: प्रकृति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हुए उसकी उपयोगिता आध्यात्मिक यात्रा में भी दिखाई।
- चित्रात्मक वर्णन: उनके वर्णन इतने जीवंत हैं कि दृश्य आँखों के सामने सजीव हो उठते हैं।
निष्कर्ष:
जायसी का प्रकृति चित्रण न केवल सौंदर्यात्मक है, बल्कि उसमें सूफी चेतना और आत्मिक अनुभूति भी समाहित है।
प्रश्न-15. पृथ्वीराज रासो के काव्य शिल्प पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:-पृथ्वीराज रासो हिन्दी साहित्य का एक महत्वपूर्ण वीरगाथा कालीन काव्य है, जिसके रचयिता चंदबरदाई माने जाते हैं। यह काव्य वीर रस की परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है और इसमें तत्कालीन समाज, युद्ध, नीति, प्रेम आदि का समन्वय है।
काव्य शिल्प की विशेषताएँ:
- वीर रस की प्रधानता: काव्य का मूल स्वर वीरता, युद्ध, शौर्य और पराक्रम का है। पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन भव्यता के साथ किया गया है।
- छंदों की विविधता: इसमें दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है जो काव्य को विविधता प्रदान करता है।
- लोककथात्मक शैली: रासो में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कल्पनाओं और लोककथाओं का मेल हुआ है जिससे यह कथा-काव्य के रूप में प्रसिद्ध है।
- भाषा: रासो की भाषा ब्रजभाषा और अपभ्रंश मिश्रित है, जो समय के साथ कई बार परिवर्तित हुई है।
निष्कर्ष:
पृथ्वीराज रासो का काव्य शिल्प भले ही ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्णतः प्रमाणिक न हो, परंतु इसकी काव्यात्मक गुणवत्ता, वीर रस की प्रभावशीलता और लोककथा शैली इसे एक उत्कृष्ट रचना बनाती है।
प्रश्न-16. भूषण की काव्यगत विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
उत्तर:- भूषण हिन्दी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख वीर रस के कवि थे। उन्होंने शिवाजी, छत्रसाल और औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक पात्रों की वीरता का यशगान किया।
काव्यगत विशेषताएँ:
- वीर रस की प्रधानता: भूषण के काव्य का मुख्य भाव वीरता, साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान है। विशेषकर शिवाजी और छत्रसाल के युद्धों का वर्णन अत्यंत ओजपूर्ण है।
- ओज और प्रभावपूर्ण भाषा: उन्होंने अत्यंत ओजस्वी और प्रभावकारी भाषा का प्रयोग किया है, जिससे पाठक में जोश और प्रेरणा उत्पन्न होती है।
- अनुप्रास और अलंकारों का प्रयोग: कवि ने अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है जिससे काव्य में सौंदर्य और प्रभाव बढ़ता है।
- काव्य में आत्मगौरव: भूषण के पदों में आत्मगौरव, धार्मिक अस्मिता और राष्ट्रप्रेम की भावना स्पष्ट दिखाई देती है।
उदाहरण:
“भूषण बहुकवि, भूषण बखाने, बुंदेलों हरबोलों के मुँह, सुनी कहानी थी…”
निष्कर्ष:
भूषण का काव्य न केवल वीर रस का प्रतिनिधि है, बल्कि उसमें भारतीय संस्कृति और गौरव की भावना भी प्रकट होती है। वे अपने युग के ओजस्वी कवि माने जाते हैं।
प्रश्न-17.
उत्तर:-
प्रश्न-18.
उत्तर:-
प्रश्न-19.
उत्तर:-
प्रश्न-20.
उत्तर:-
प्रश्न-21.
उत्तर:-
प्रश्न-22.
उत्तर:-
प्रश्न-23.
उत्तर:-
प्रश्न-24.
उत्तर:-
प्रश्न-25.
उत्तर:-
Section-C
प्रश्न-1.सूरदास की भक्ति भावना पर एक लेख लिखिए
उत्तर:- तुलसीदास (1511–1623) हिन्दी भक्तिकाव्य के अतुलनीय रत्न हैं। उनकी भक्ति दृष्टि ‘रामभक्ति’ की थी—अखंड, निस्वार्थ और सर्वात्मीय। उन्होने अवधी भाषा में बसंत, चंद्रिका, सुरसरिता जैसी सरल व सारगर्भित रचनाओं कीं, जिनमें श्रीराम का जीवन, चरित्र और आदर्श सजीव होते हैं।
उनकी महाकृति ‘रामचरितमानस’ ईश्वर–राम के प्रति भक्त की निष्ठा और वात्सल्य-भक्ति की प्रमुख अभिव्यक्ति है। इसमें उन्होंने बालपन का वात्सल्य, पिता-पुत्र का संतानावेदन और मृत्यु तक का आचरण—सभी दृष्टान्तों में भक्ति को आत्मा से सींचा है। काशी में अविरल प्रवाहमान मानस की लोकप्रियता इस भक्ति ऊर्जा का बिगुल है ।
‘विनयपत्रिका’ में तुलसीदास स्वयं को मलिन जीव बताकर भगवान राम से विनय करते हैं—यह आत्मतर्पण और भक्ति की गहनता का प्रमाण है ।
उनका भक्ति दृष्टिकोण निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है:
- सगुण–साकार भक्ति – राम को साकार रूप में आराध्य मानना।
- वात्सल्य–भाव – राम के प्रति माता–बेटे जैसा प्रेम; जैसे कौशल्या-राम और सीता-राम के बीच दृष्टव्य ।
- निस्वार्थ समर्पण – तात्कालिक और दीर्घकालिक सुख की अपेक्षा से ऊपर भक्ति करना।
- भाषा और मनोभाषा का समावेश – रामचरितमानस अवधी में है, जो सामान्य जनमानस से रु-संचारित करती है।
- समाज सुधार – गण, वर्ग, भाषा की दीवारें तोड़ कर एक सार्वभौमिक भक्ति दर्शन प्रस्तुत किया।
इस प्रकार तुलसीदास की भक्ति भावना आत्मा–आत्मा झुकाव, वात्सल्य समर्पण और राष्ट्र–समर्थक दृष्टि से अभिन्न रूप में पाई जाती है। उनकी शैली साहित्य की लौकिकता से भक्ति की अद्भुत लौकिकता तक विस्तार करती है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.पद्मावत’ के आधार पर जायसी के काव्य सौंदर्य का मूल्यांकन
उत्तर:- पद्मावत’ मलिक मोहम्मद जायसी की अमर रचना है, जो हिन्दी सूफी काव्यधारा का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यह रचना प्रेमाख्यान पर आधारित है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सौंदर्य भी विद्यमान है। जायसी ने ‘पद्मावत’ के माध्यम से प्रेम को आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बनाया है।
‘पद्मावत’ में रूपक शैली का प्रयोग हुआ है। पद्मावती आत्मा का प्रतीक है, रत्नसेन जीवात्मा का और अलाउद्दीन लोभ और अज्ञान का प्रतीक है। यह काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय है क्योंकि इसमें प्रकृति का चित्रण, भावात्मक गहराई, प्रतीकात्मकता और बिंब योजना अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है।
काव्य में गूढ़ आध्यात्मिक संकेत भी हैं। भाषा में अवधी की मिठास और सूफी काव्य की भावात्मकता झलकती है। प्रेम को जायसी ने ‘इश्क हकीकी’ की ऊँचाई तक पहुँचाया है।
इस प्रकार, ‘पद्मावत’ केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि गूढ़ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अर्थों से युक्त एक अनुपम काव्य है, जो जायसी के काव्य सौंदर्य का सर्वोच्च उदाहरण है।
प्रश्न-3.कबीर काव्य के अनुभूति एवं अभिव्यंजना पक्ष का विवेचन कीजिए।
उत्तर:- कबीर भारत के मध्यकालीन संत-कवि थे, जिनका काव्य ‘निर्गुण भक्ति’ की अमर प्रतिमूर्ति है। उनके काव्य में अनुभूति (experience) और अभिव्यंजना (expression) दोनों पक्षों की अनोखी गहराई है।
अनुभूति पक्ष: कबीर ने व्यक्त अनुभव की गहराई को पहली बार इस स्तर पर व्यावहारिक रूप में रखा:
वे आध्यात्मिक उपासना और आत्म-साक्षात्कार को भौतिक क्रियाओं से ऊपर रखकर देखते थे।
“मन माफ़ कर दो माया, कुण्डलिया काट न जाओ” जैसे पद उनमें अनुभव की तुरंतीयता दर्शाते हैं।
इन्होंने धर्मांधता, जातपात, बाहरी संस्कारों आदि के विरोधी अनुभवों को प्रकट कर इसे आत्माभीषणुषील बनाकर व्यक्त किया।
अभिव्यंजना पक्ष:
साधारण दोहा, पर गहन जीवन दर्शन—दो पंक्तियों में दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक अनुभव संकुचित कर देना।
चाहे कटाक्ष, व्यंग्य, निराकरण, इन सब माध्यमों में अमर भावनाओं की अभिव्यंजना करते हैं, जो प्रत्येक शब्द में आत्मानुभव की खुराक देता है।
“बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय…”— इसमें आत्मनिरीक्षण और आत्म-परिष्कार की प्रेरणा है।
प्रश्न-4. “बिहारी के काव्य में भक्ति-नीति-श्रृंगार का समन्वय बखूबी हुआ है।” – विवेचना करे
उत्तर:- बिहारी लाल हिन्दी रीतिकालीन काव्य के प्रमुख कवि हैं। उनकी ‘बिहारी सतसई’ में तीनों तत्व—भक्ति, नीति और श्रृंगार—का समन्वय अत्यंत सुंदर ढंग से हुआ है। यह उनकी काव्य प्रतिभा की उत्कृष्टता को दर्शाता है।
भक्ति पक्ष में बिहारी ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, विशेषकर राधा-कृष्ण के प्रेम को सरस रूप में प्रस्तुत किया है। श्रृंगार पक्ष उनका प्रमुख गुण है, जिसमें संयोग-वियोग, मान-अपमान, लज्जा, संकेत, रूप-वर्णन आदि के अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक चित्र मिलते हैं।
नीति पक्ष में उन्होंने समाज, राजनीति और जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को एक-एक दोहों में संजोया है। उदाहरणस्वरूप, उन्होंने राजा के गुण, सेवक की भूमिका, स्त्री-पुरुष संबंध आदि पर नीतिपरक सुझाव दिए हैं।
बिहारी की भाषा ब्रज है, जिसमें गूढ़ अर्थ, अनुप्रास, यमक, और लक्षणा-व्यंजना का सुंदर उपयोग हुआ है। उनके दोहे कम शब्दों में गहन भाव और चित्र प्रस्तुत करते हैं।
इस प्रकार, बिहारी का काव्य न केवल श्रृंगार रस का भंडार है, बल्कि उसमें भक्ति और नीति की सघनता भी विद्यमान है, जो उसे बहुआयामी बनाती है।
प्रश्न-5. घनानंद के काव्य में अनुभूति एवं अभिव्यक्ति पक्ष का विवेचना कीजिए
उत्तर:- घनानंद रीतिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं, जिन्हें रीतिमुक्त काव्यधारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। उनके काव्य में आत्मानुभूति की गहराई और उस अनुभूति की सजीव अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। वे प्रेम की पीर के कवि हैं।
घनानंद का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि विरहात्मक और आध्यात्मिक ऊँचाई लिए हुए है। राधा-कृष्ण की उपासना करते हुए उन्होंने स्वयं को विरह की वेदना में पीड़ित प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम का आंतरिक अनुभव प्रत्यक्ष झलकता है।
अभिव्यक्ति की दृष्टि से घनानंद का काव्य अत्यंत मार्मिक और सजीव है। वे सरल, स्वाभाविक और सहज भाषा में गूढ़ भावनाएँ व्यक्त करने में सक्षम हैं। उनकी भाषा ब्रज है, जिसमें कोमलता, मधुरता और भाव की तीव्रता है।
उनकी रचनाओं में बिम्ब योजना, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिक अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। उनका काव्य पाठक के हृदय को छूता है क्योंकि उसमें वास्तविक पीड़ा और अनुभूत प्रेम की सच्चाई है।
इस प्रकार, घनानंद का काव्य अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही पक्षों से समृद्ध है, जिसमें हृदय की गहराई से उपजी पीड़ा को काव्यात्मक सौंदर्य में ढालकर प्रस्तुत किया गया है।
प्रश्न-6. रीतिमुक्त काव्य धारा में घनानंद के काव्य की भूमिका का सोदाहरण मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- घनानंद (17वीं–18वीं शताब्दी) रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जहाँ उन्होंने रीति-काव्य की शैली से बाहर आकर सरलीकरण और आत्म-गम्भीरता को बढ़ावा दिया। उनके काव्य की भूमिका निम्नलिखित दृष्टियों से महत्वपूर्ण है:
- स्व-लब्ध आत्मा की अभिव्यक्ति:
उनकी रचनाएँ (जैसे “घनानंद कहें रसिकन रास रचौ”) आत्म–अनुभूति से उपजी यथार्थ प्रेम और पीड़ा का संग्रह हुआ। वे प्रेम को पीर रूप में व्यक्त करते हैं—”प्रेम की पीर” कहने का मूल्य इसी गहनता में निहित है। - संयोजित भाषा-शैली:
ब्रजभाषा का सरल, सहज, संक्षिप्त प्रयोग, जिसमें भाव की तीव्रता थी—जिससे रीतिकालीन शैली का औपचारिक भराव गिरा; अब भाव संवाद साधता है। - जूझापन विरह में:
उनकी रचनाओं में वात्सल्य, श्रृंगारिक, भक्ति और विरह रस का सुंदर संतुलन है—लेकिन वह रीतिमुक्त है क्योंकि व्यक्ति के भाव मुखर हुए; खासकर उस विभूति-रस का, जिसे उन्होंने रेखांकित किया। उन्होंने सजीव अभिव्यक्ति—”मैं तड़पत हौं…” जैसी संवेदना रखी जिसमें स्वतंत्र आत्मा की पीड़ा छिपी थी। - सरलीकरण और भावपूर्ण समन्वय:
उनकी भाषा में जटिल शृंगार अलंकार की जगह आत्मीय अभिव्यक्तियों, मानव भावनाओं, और आत्ममंथन की अनुभूति को प्राथमिकता मिली।
उदाहरण: मशहूर पंक्ति “घनानंद कहें रसिकन रास रचौ, मोही स्वर्”—जहाँ रसिक लीलाएँ रचते हैं, उसी रच को कवि आत्मीय रूप दे रहा है। यहाँ दृश्य-श्रेणी से निकलकर स्व-भाव की गहराई सोदाहरण है।
प्रश्न-7. “मीरा के काव्य में उनके जीवनानुभवों की सच्चाई और मार्मिकता है।” इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-मीरा बाई की काव्य साधना उनके जीवन के गहरे अनुभवों की उपज है। वे महलों की राजकुमारी थीं परन्तु कृष्णभक्ति के मार्ग पर चलकर उन्होंने सांसारिक सुख, सामाजिक मान्यताएँ, पति, परिवार, समाज सबका त्याग किया। उनके काव्य में जो वेदना, तड़प, आत्मसमर्पण और प्रेम दिखाई देता है, वह किसी कल्पना की नहीं, बल्कि उनके भोगे हुए सत्य की गवाही देता है।
मीरा का जीवन संघर्ष और विरोध से भरा था। वे जिस समाज में रहीं, वहाँ एक स्त्री का खुले रूप में ईश्वर प्रेम व्यक्त करना असामान्य माना जाता था। पति की मृत्यु के बाद जब उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार किया, तब समाज ने उन्हें तिरस्कृत किया। किन्तु उन्होंने यह सब सहा और अपने काव्य में इस दर्द को स्वर दिया। उदाहरण के लिए—
“मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।”
इस एक पंक्ति में मीरा की भक्ति, आत्मसमर्पण और समाज के प्रति अस्वीकार की भावना समाहित है।
मीरा के पदों में विरह की पीड़ा, प्रभु दर्शन की तड़प, और स्त्री की मानसिक व्यथा बड़ी ही मार्मिकता से व्यक्त हुई है—
“निंदक कहें मीरा बावरी, संत कहें सुभाय।
मैं तो सांवरे के रंग रंगी, और न रंग न आय।।”
मीरा का प्रेम लोकजीवन की सीमाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक बन गया। उन्होंने सांसारिक बंधनों को झटक कर केवल ईश्वर की प्राप्ति को जीवन का ध्येय माना। उनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, जो सहज और भावपूर्ण है। इस सहजता ने उनके काव्य को जन-जन में लोकप्रिय बना दिया।
मीरा के पदों में आत्मानुभूति और आध्यात्मिक प्रेम की तीव्रता है। उन्होंने नारी मन की पीड़ा, उसकी व्यथा, और उसकी प्रेमाकुलता को अद्भुत तरीके से व्यक्त किया है। उनके पद केवल काव्य नहीं, बल्कि भावों की गाथा हैं।
निष्कर्षतः, मीरा के काव्य में जो सच्चाई और मार्मिकता है, वह उनके जीवनानुभवों की ही देन है। उनके काव्य की यही विशेषता उन्हें भक्तिकाल की अमर कवयित्री बनाती है।
प्रश्न-8. “पद्माकर के काव्य में रीतिकालीन कविता की सभी विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं।” इस कथन की सोदाहरण समीक्षा कीजिए।
उत्तर:- पद्माकर रीतिकाल के उत्तरार्ध के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में उस युग की समस्त काव्य प्रवृत्तियों का समावेश किया। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएँ थीं– नायिका-भेद, श्रृंगार-रस, राजाश्रयी परंपरा, अलंकार युक्त भाषा, प्रकृति चित्रण और संस्कृत निष्ठ ब्रजभाषा। पद्माकर का काव्य इन सभी तत्त्वों से भरपूर है।
- श्रृंगार रस की प्रधानता:
पद्माकर की कविता श्रृंगारिक भावों से ओत-प्रोत है। उनके काव्य में नायिका की चेष्टाएँ, नख-शिख वर्णन, मिलन-विरह के चित्र अत्यंत सौंदर्यपूर्ण ढंग से वर्णित हैं।
उदाहरण:
“सावन आयो रे झूला पड़्यो बनमाली रसिक रस बरसाने।”
यह पंक्ति न केवल ऋतु चित्रण करती है बल्कि उसमें नायिका की भावनाएँ भी व्यक्त होती हैं।
- प्रकृति चित्रण:
उन्होंने वर्षा, वसंत और शरद ऋतुओं का अत्यंत चित्रमय वर्णन किया है। उनके प्रकृति चित्रण में श्रृंगार का वातावरण दिखाई देता है। - नायिका-भेद:
उन्होंने अनेक प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है, जैसे– स्वाधीनपतिका, अभिसारिका, खंडिता, प्रोषितभर्तृका आदि, जो रीतिकाल की एक विशिष्ट प्रवृत्ति थी। - भाषा और शैली:
पद्माकर की भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है। उनकी शैली अलंकारिक और छंदबद्ध है। - अलंकार प्रयोग:
उपमा, रूपक, अनुप्रास जैसे अलंकार उनके काव्य में बहुलता से मिलते हैं। इससे उनकी कविता कलात्मक बन गई है। - राजाश्रयी प्रवृत्ति:
पद्माकर बुंदेलखंड के राजाओं के दरबार में रहते थे। उन्होंने आल्हा खंड के वीरों की प्रशंसा की है। ‘जेललपुर नजारा’, ‘छबीली बाना’ जैसी रचनाएँ इसका प्रमाण हैं।
निष्कर्षतः, पद्माकर की कविता में रीतिकाल की सारी प्रवृत्तियाँ – श्रृंगार, राजाश्रय, नायिका भेद, अलंकार, प्रकृति चित्रण आदि एकसाथ मिलती हैं। वे रीतिकालीन कविता की श्रेष्ठ परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं।
प्रश्न-9. तुलसीदास की भक्तिभावना पर सोदाहरण प्रकाश डालिए।
उत्तर:- तुलसीदास भक्तिकाल के महानतम कवि माने जाते हैं। उनकी भक्ति राम के प्रति थी, जिसे वे ‘सगुण साकार’ रूप में पूजते थे। तुलसीदास की भक्ति व्यक्तिगत श्रद्धा से आगे जाकर समाज को धर्म, नीति और मर्यादा का संदेश देती है।
- सगुण भक्ति का स्वरूप:
तुलसीदास ने राम को ईश्वर, राजा, आदर्श पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया। उनकी भक्ति में अनुशासन, आदर्श और नीति का समन्वय है।
उदाहरण:
“राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जाननहारा।”
- जीवन का उद्देश्य भक्ति:
उन्होंने जीवन के समस्त कर्तव्यों को रामभक्ति में समर्पित करने का आग्रह किया। - भक्ति में विनम्रता और आत्मसमर्पण:
तुलसी की भक्ति विनय से पूर्ण है। वे कहते हैं –
“तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोइ।” - समाज के लिए प्रेरणा:
‘रामचरितमानस’ न केवल भक्ति ग्रंथ है, बल्कि उसमें सामाजिक नीति, चरित्र और मर्यादा के आदर्श भी समाहित हैं। - राम के प्रति अखंड निष्ठा:
उन्होंने कहा –
“सियाराम मय सब जग जानी, करहु प्रनाम जोरि जुग पानी।”
निष्कर्षतः, तुलसीदास की भक्ति भावनात्मक नहीं, आदर्श और मर्यादा आधारित है। वे भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ भक्ति-कवि हैं, जिनकी भक्ति साहित्य और समाज दोनों को आलोकित करती है।
प्रश्न-10. पद्माकर के काव्य में प्रकृति-चित्रण विविध रूपों में हुआ है। स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- रीतिकाल के प्रमुख कवि पद्माकर का प्रकृति-चित्रण अत्यंत समृद्ध, रंगमय और चित्रात्मक है। वे अपने समय के उन कवियों में अग्रणी माने जाते हैं, जिन्होंने प्रकृति को न केवल सौंदर्य की दृष्टि से देखा, बल्कि उसे मनोभावों का संवाहक और प्रतीक भी बनाया। उनके काव्य में ऋतु-वर्णन, पुष्पों की विविधता, आकाश के दृश्य, जलधाराएँ, पक्षी और पशु—सभी जीवंत हो उठते हैं।
पद्माकर की कविता में विशेषकर वसंत और वर्षा ऋतु का चित्रण प्रभावशाली है। उन्होंने वसंत को श्रृंगारिक प्रेम के अनुकूल ऋतु मानते हुए नायिका-नायक की मनोदशा के अनुरूप चित्रित किया है:
“बासंती बयार बहै बृंदावन, सौरभ सनेह सुहावो।
सखियन संग कछु कहत कुंजन, रास रचावन धावो।”
इस पद्यांश में उन्होंने बृंदावन की वासंती बयार, फूलों की सुवास और रास-रंग के वातावरण को अभिव्यक्त किया है।
उनके प्रकृति वर्णन में रंग, गंध, ध्वनि और गति के सुंदर समन्वय मिलते हैं। वर्षा ऋतु के संदर्भ में वे मेघों के गर्जन, बिजली की चमक, मोर के नर्तन, और धरती की हरियाली को चित्रित करते हैं। उनका प्रकृति चित्रण स्थूल न होकर भावात्मक है।
पद्माकर का प्रकृति-चित्रण केवल बाह्य दृश्य तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मानवीय भावनाओं का सहचर बन जाता है। जब नायिका विरह में होती है, तो वर्षा का गर्जन उसे और अधिक पीड़ा देता है। वहीं मिलन के क्षणों में वही प्रकृति हर्ष का कारण बन जाती है।
पद्माकर की भाषा ब्रज है, जो उनके प्रकृति-चित्रण को माधुर्य और लावण्य प्रदान करती है। उनके उपमान और उत्प्रेक्षाएँ अत्यंत प्रभावशाली हैं। जैसे—कुंजों को चित्रशाला, बिजली को नागिन, और मेघों को हाथी कहा गया है।
प्रश्न-11. बिहारी के काव्य में श्रृंगार, नीति तथा भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। उदाहरण सहित समझाइये।
उत्तर:-बिहारीलाल हिंदी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध काव्यकृति “बिहारी सतसई” में केवल 700 दोहों के माध्यम से जीवन, प्रेम, नीति और भक्ति के विभिन्न पक्षों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में श्रृंगार, नीति और भक्ति का अद्भुत समन्वय त्रिवेणी के समान प्रवाहित होता है।
- श्रृंगार रस
बिहारी का काव्य मुख्यतः श्रृंगार पर आधारित है। उन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को अत्यंत गहनता से चित्रित किया है। उनकी कविताओं में राधा-कृष्ण की प्रेमलीला, नायिका की चेष्टाएँ, सौंदर्य वर्णन तथा प्रेम की गूढ़ अनुभूतियाँ दर्शनीय हैं:
“नयन नचाय कह्यो मुसकाय लला फिरि अइयो खेलन होरी।
भौंहन कैचि नकचिन्गरी दै गिरधर तासु भई मत चोरी।”
इस दोहे में नायिका की चतुराई और नायक की हार को रोचक ढंग से चित्रित किया गया है।
- नीति पक्ष
बिहारी सतसई में नीति संबंधी दोहे भी मिलते हैं, जिनमें समाज, व्यवहार, राजनीति और पारिवारिक जीवन से जुड़े गूढ़ ज्ञान की झलक मिलती है। उन्होंने नीति के माध्यम से मानव जीवन को दिशा देने का कार्य किया:
“बड़े बड़ाई न कीजिए, जो नीचु कहैं लजाय।
सिर ऊंचे कर बांधिए, खोटे सिक्के जाय।”
इसमें सामाजिक मर्यादा और व्यवहारिक बुद्धि का संदेश दिया गया है।
- भक्ति भावना
यद्यपि बिहारी को रीति काव्य का कवि माना गया है, परंतु उनके दोहों में भक्ति का भी सूक्ष्म संचार मिलता है। विशेषकर कृष्ण भक्ति में राधा-कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए भक्ति का भाव उजागर होता है:
“कबहुँकु कानन कुंज गही कबहुँकु गहि कर बैन।
कबहुँकु राधा हरि मिलन, बिहारी रसिक अनैन।”
यह दोहा राधा-कृष्ण की भक्ति और उनके आध्यात्मिक मिलन की अनुभूति को दर्शाता है।
निष्कर्षतः, बिहारी के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ-साथ नीति का बोध और भक्ति का माधुर्य मिलता है। यह त्रिवेणी प्रवाह उन्हें अन्य रीति कवियों से विशिष्ट बनाता है। उनकी भाषा ब्रज है, जिसमें अलंकारों की भरमार और भावों की गहराई मिलती है।
प्रश्न-12. मीरा के काव्य में लोकतत्व पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- मीरा बाई भक्तिकाल की प्रमुख संत-कवियित्री थीं, जिनका काव्य भाव, भक्ति और लोकजीवन की सजीव झलक से परिपूर्ण है। उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत आत्मानुभूति को स्वर दिया, बल्कि लोक जीवन की विविध परंपराओं, रीति-रिवाजों, गीतों और सांस्कृतिक प्रतीकों को भी अपने पदों में समाहित किया। यही विशेषता उनके काव्य को “लोककाव्य” का दर्जा दिलाती है।
- लोकभाषा का प्रयोग:
मीरा ने ब्रजभाषा, राजस्थानी और गुजराती मिश्रित बोली का प्रयोग किया, जो उस समय की सामान्य जन की भाषा थी। उन्होंने संस्कृत या पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपनी पीड़ा और प्रेम को जनमानस की भाषा में व्यक्त किया:
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
यहाँ “राम रतन धन” जैसे प्रतीक आम जनजीवन में आध्यात्मिक संपत्ति के रूप में प्रचलित हैं।
- लोकप्रचलित प्रतीकों का प्रयोग:
मीरा के पदों में गागर, माटी, रतन, रंग, मेहंदी, बिछुआ, नथ, कंगन आदि प्रतीक मिलते हैं, जो ग्रामीण और स्त्रीलोक जीवन के प्रतीक हैं:
गागर ना फूटे प्रेम की, चाह बुझे ना कोई।
मिरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले रास होई।
- लोकगीतों की शैली:
मीरा के पदों में आलाप, राग और ताल की छाया मिलती है। उनके गीत लोकगायन की शैली में गाए जाते थे और आज भी राजस्थान और उत्तर भारत के गाँवों में भक्ति और विवाह जैसे प्रसंगों में मीरा के पदों को गाया जाता है। वे जनगीतों की लय और भावात्मकता को बनाए रखती हैं।
- स्त्री दृष्टिकोण और लोकसंवेदना:
मीरा का काव्य स्त्री हृदय की संवेदनाओं का दस्तावेज़ है। उन्होंने एक लोक स्त्री के रूप में अपने पति के स्थान पर भगवान कृष्ण को स्वीकार किया और समाज द्वारा उपेक्षित जीवन को गर्व से अपनाया। यह विरोध भी लोक परंपरा की उस चेतना को उजागर करता है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन सर्वोपरि होता है।
- धार्मिक लोकविश्वासों का समावेश:
मीरा के पदों में राम, कृष्ण, संत, साधु, भजन, कीर्तन, मंदिर, मुरली, बंसी जैसे धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से लोकधर्म का गहरा प्रभाव दिखता है।
निष्कर्ष:
मीरा का काव्य किसी दरबारी या शास्त्रीय पृष्ठभूमि का नहीं, बल्कि जनमानस की आत्मा का स्वर है। उनके पदों में भक्ति की भावप्रवणता के साथ-साथ लोकजीवन की सहजता, सच्चाई और रंगीनता झलकती है। यही लोकतत्व उन्हें जनकवि बनाता है, जिनका काव्य आज भी लोगों की आस्था, जीवन और संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है।
प्रश्न-13.
उत्तर:-
प्रश्न-14.
उत्तर:-
प्रश्न-15.
उत्तर:-
vmou MAHD-01 paper , vmou MA Hindi 1st year exam paper , vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4