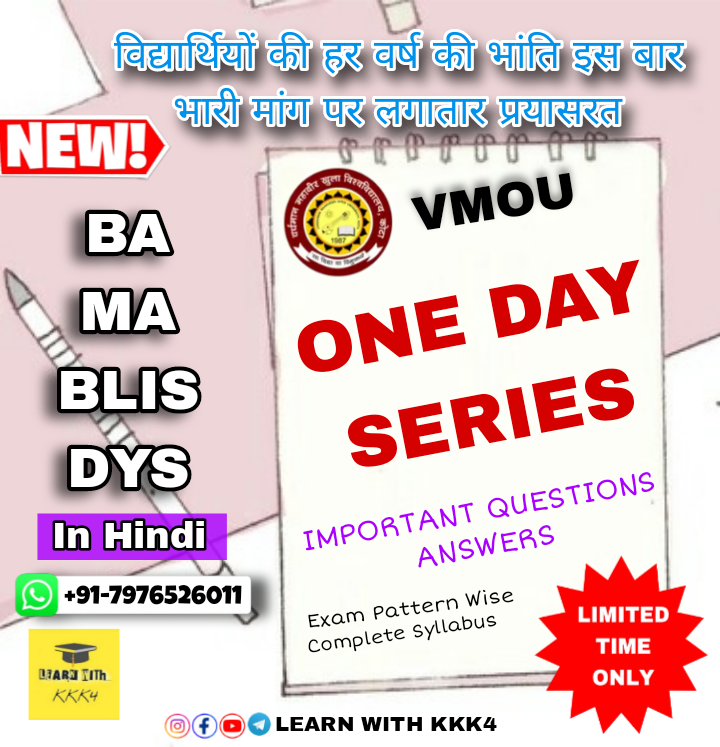VMOU MAGE-06 Paper MA Final Year ; vmou exam paper
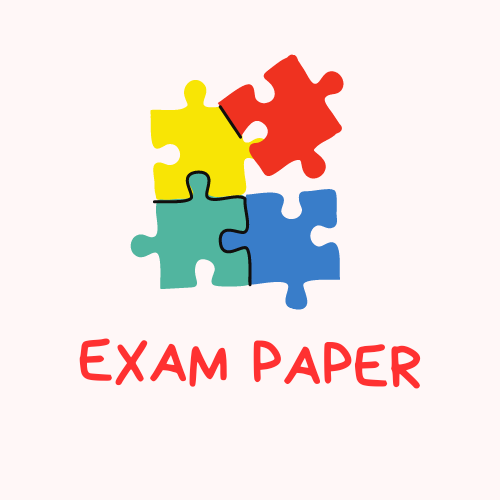
VMOU MA Final Year के लिए भूगोल (MAGE-06 , ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार
उत्तर:- भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4′ उत्तरी अक्षांश से 37°6′ उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 68°7′ पूर्व देशांतर से 97°25′ पूर्व देशांतर तक है।
प्रश्न-2.उत्तर-पूर्वी भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र
उत्तर:- उत्तर-पूर्वी भारत में असम के डिगबोई, नहरकटिया और मोरान प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-3.जेट स्ट्रीम (Jet Stream)
उत्तर:- जेट स्ट्रीम पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली तेज गति की ऊपरी पवनें होती हैं जो लगभग 9 से 14 किमी ऊँचाई पर बहती हैं।
प्रश्न-4. भारत के कॉफी उत्पादक राज्य
उत्तर:- कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु मुख्य कॉफी उत्पादक राज्य हैं।
प्रश्न-5. भारत के कोई दो औद्योगिक प्रदेश
उत्तर:- भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में हुगली औद्योगिक क्षेत्र और मुंबई-पुणे औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।
प्रश्न-6. भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि
उत्तर:- शुष्क क्षेत्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्षा की मात्रा कम (75 सेमी से कम) होती है जैसे राजस्थान
प्रश्न-6. अरावली पर्वत श्रेणी
उत्तर:- अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। अधिकांश भाग राजस्थान मे है
प्रश्न-7. वैश्विक तापन का भारत पर प्रभाव
उत्तर:- वैश्विक तापन से भारत में जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलना, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
प्रश्न-8. भारतीय मानक समय
उत्तर:- भारतीय मानक समय 82°30′ पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है, जो इलाहाबाद के पास स्थित है।
प्रश्न-9. Deccan Trap / दक्कन ट्रेप:
उत्तर:- दक्कन ट्रेप एक ज्वालामुखीय पठार है जो महाराष्ट्र, मध्य भारत में फैला हुआ है और काले बेसाल्ट चट्टानों से बना है।
प्रश्न-10. Indian Monsoon / भारतीय मानसून:
उत्तर:- भारतीय मानसून दक्षिण-पश्चिम दिशा से आने वाली मौसमी हवाओं द्वारा वर्षा लाने वाला एक मौसमी पवन तंत्र है।
प्रश्न-11. भारत के कोई दो औद्योगिक प्रदेश:
उत्तर:- 1. मुंबई-पुणे औद्योगिक क्षेत्र, (2) हुगली औद्योगिक क्षेत्र।
प्रश्न-12. Vindhyan mountain range / विंध्यन पर्वत श्रेणी:
उत्तर:- विंध्यन पर्वत मध्य भारत में स्थित एक प्राचीन और अवसादी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है।
प्रश्न-13. सरक्रीक विवाद:
उत्तर:- सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित ज्वारीय नदी के जल-सीमा निर्धारण को लेकर है
प्रश्न-14. McMahon Line (मैकमोहन रेखा)
उत्तर:- यह भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है जो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है।
प्रश्न-15. गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ
उत्तर:- गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि
प्रश्न-16. Coromandel Coast (कोरीमण्डल तट)
उत्तर:- यह भारत के पूर्वी समुद्री तट का भाग है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक फैला है।
प्रश्न-17. भारत के गन्ना उत्पादक राज्य
उत्तर:- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं।
प्रश्न-18. भारत के सूती वस्त्र उत्पादक केन्द्र
उत्तर:- मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, नागपुर और कोयंबटूर प्रमुख केन्द्र हैं।
प्रश्न-19. खाद्य सुरक्षा
उत्तर:- यह ऐसी स्थिति है जिसमें सभी लोगों को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन हर समय उपलब्ध होता है।
प्रश्न-20 प्रादेशिक विषमता
उत्तर:- यह देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक असमानता को दर्शाती है।
और सेक्शन स का प्रश्न 3 भी देखे
प्रश्न-21. राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश
उत्तर:- मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र
प्रश्न-22. भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसकी अक्षांशीय स्थिति 8°4′ से 37°6′ उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर 68°7′ से 97°25′ पूर्वी देशांतर के बीच है।
प्रश्न-23. हिमालय जल-प्रवाह प्रणाली
उत्तर:- हिमालय जल-प्रवाह प्रणाली में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ शामिल हैं, जो हिमालय से निकलकर भारत के मैदानों में बहती हैं।
प्रश्न-24. भारत में ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधन।
उत्तर:- भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो गैस, और लघु जल विद्युत जैसे गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास हो रहा है
प्रश्न-25. शहरी अधिवासों और ग्रामीण अधिवासों में अन्तर बताइए।
उत्तर:- शहरी अधिवासों में जनसंख्या घनत्व अधिक, सुविधाएँ विकसित होती हैं जबकि ग्रामीण अधिवासों में जनसंख्या कम व मुख्यतः कृषि पर आधारित होते हैं।
प्रश्न-26. भारत के प्रमुख लौह-इस्पात उत्पादक केन्द्र।
उत्तर:- भारत के प्रमुख लौह-इस्पात केन्द्रों में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और विशाखापत्तनम शामिल हैं।
प्रश्न-27. प्रादेशिक नियोजन
उत्तर:- प्रादेशिक नियोजन किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक विशेषताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण और विकास है
प्रश्न-28. मरुस्थली
उत्तर:- मरुस्थली वे शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जैसे थार मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है।
प्रश्न-26. भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का वर्णन कीविए
उत्तर:- भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती हैं, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 15,200 किमी है।
प्रश्न-27. भारत के चार प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखिए।
उत्तर:- हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तटीय मैदान और द्वीप समूह।
प्रश्न-28. बांगर एवं खादर में क्या अन्तर है ?
उत्तर:- बांगर पुरानी जलोढ़ भूमि होती है जबकि खादर नई जलोढ़ भूमि होती है जो बाढ़ से हर वर्ष नवीनीकृत होती है
प्रश्न-29. भारत के प्रमुख बन्दरगाहों के नाम बताइए।
उत्तर:- प्रमुख बंदरगाह हैं — मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, पारादीप, विशाखापत्तनम, और कांडला।
प्रश्न-30. राजस्थान का पूर्वी मैदान
उत्तर:- राजस्थान का पूर्वी मैदान मुख्यतः चंबल बेसिन में स्थित है और यह उपजाऊ भूमि एवं घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है।
Section-B
प्रश्न-1.भारत की स्थिति की भू-राजनीतिक महत्ता बताइए।
उत्तर:-भारत की भौगोलिक स्थिति एशिया के दक्षिण में स्थित है, जिसकी सीमाएँ सात देशों—पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती हैं। यह देश हिंद महासागर के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जिससे यह समुद्री मार्गों पर रणनीतिक नियंत्रण रखता है। भारत की स्थिति यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के मध्य व्यापारिक मार्गों को जोड़ती है, जिससे यह व्यापार और कूटनीति दोनों में प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत की निकटता ऊर्जा संपन्न पश्चिम एशिया, रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हिंद महासागर, और आर्थिक रूप से समृद्ध दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ इसे एक वैश्विक शक्ति बनने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, भारत क्षेत्रीय सहयोग संगठन जैसे सार्क, बिम्सटेक और आईओआरए का सदस्य होने के कारण दक्षिण एशिया में स्थायित्व और विकास को भी प्रभावित करता है। इस तरह भारत की स्थिति उसे वैश्विक मंच पर भू-राजनीतिक दृष्टि से एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्र बनाती है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.भारत में काली मिट्टी की विशेषताएँ एवं वितरण बताइए।
उत्तर:-काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, मुख्यतः ज्वालामुखीय चट्टानों के विघटन से बनी होती है। इसकी विशेषता यह है कि यह मिट्टी गहरी, चिकनी, और नमी को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम होती है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, लोहा और एलुमिनियम की भरपूर मात्रा होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी रहती है। यह कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए इसे “कॉटन सॉइल” भी कहते हैं।
भारत में काली मिट्टी का वितरण मुख्यतः दक्कन पठार के क्षेत्रों में पाया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी नदियों के बेसिन में भी काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास के अतिरिक्त सोयाबीन, तिलहन, बाजरा और ज्वार जैसी फसलें भी उपजाई जाती हैं। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता इसे शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाती है।
प्रश्न-3.भारत के वनों के प्रकार बताइए।
उत्तर:- भारत में विविध जलवायु और स्थलाकृतिक परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन्हें मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:
- उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन – ये वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान-निकोबार में पाए जाते हैं। यहाँ सालभर हरियाली रहती है। प्रमुख वृक्ष: शीशम, आबनूस, महोगनी।
- उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन – ये वन भारत के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं, जहाँ मध्यम वर्षा होती है। प्रमुख वृक्ष: सागौन, साल, अर्जुन।
- काँटेदार व शुष्क वन – राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष: बबूल, कीकर।
- पर्वतीय वन – हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऊँचाई के अनुसार वनस्पति बदलती है। प्रमुख वृक्ष: देवदार, चीड़, फर।
- ज्वारीय वन (मैंग्रोव) – सुंदरबन डेल्टा जैसे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष: सुंदर, गरन।
ये वन भारत की पारिस्थितिकी, वर्षा संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
प्रश्न-4.भारत में वन्यजीवों की विविधता की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- भारत में जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है, जहाँ विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। भारत दुनिया के 17 मेगाडाइवर्स देशों में से एक है। यहाँ स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर और कीटों की हजारों प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
भारत में शेर, बाघ, हाथी, गैंडा, तेंदुआ, भालू, हिरण, लंगूर, अजगर, मगरमच्छ, मोर, सारस, गिद्ध आदि प्रमुख वन्यजीव हैं। पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टा और पूर्वोत्तर भारत विविध वन्य जीवों के आवास स्थल हैं।
भारत सरकार ने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं। साथ ही, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी लागू किया गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट जैसी योजनाएँ चल रही हैं।
वन्यजीव न केवल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होते हैं, बल्कि जैविक विविधता का प्रतीक भी हैं।
प्रश्न-5.भारत की खनिज पेटियों पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- भारत में खनिजों का वितरण असमान है, परंतु कुछ प्रमुख खनिज पेटियाँ हैं जहाँ खनिज संसाधनों की अधिकता पाई जाती है:
- पूर्वी भारत की खनिज पट्टी – झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में फैली हुई यह क्षेत्र भारत की सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है। यहाँ लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज आदि पाए जाते हैं।
- पश्चिमी भारत की खनिज पट्टी – राजस्थान और गुजरात में प्रमुख रूप से जस्ता, तांबा, चूना पत्थर, अभ्रक, और फेल्सपार पाए जाते हैं।
- दक्षिणी भारत की खनिज पट्टी – कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सोना (कोलार), लौह अयस्क (बेल्लारी), और मैग्नेसाइट जैसे खनिज मिलते हैं।
- हिमालयी क्षेत्र – यहाँ सीमित मात्रा में तांबा, सीसा, और चूना पत्थर पाए जाते हैं।
खनिज संसाधन देश के औद्योगिक विकास में रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। इनका समुचित दोहन भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है।
प्रश्न-6.भारत की प्रमुख फसलों का वितरण एवं उत्पादन बताइए।
उत्तर:- भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विविध जलवायु और मिट्टी के कारण अनेक फसलों की खेती होती है। प्रमुख फसलें दो प्रकार की होती हैं – खाद्य फसलें और नकदी फसलें।
- धान – यह भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।
- गेंहू – उत्तर भारत में मुख्यतः उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य हैं।
- मक्का और ज्वार – महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में उगाए जाते हैं।
- कपास – काली मिट्टी वाले क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में।
- गन्ना – उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक हैं।
- तेलहन फसलें (सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली) – राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में अधिक होती हैं।
- दलहन (चना, अरहर, मसूर) – मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में।
भारत कृषि विविधता के कारण विश्व में प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में शामिल है।
प्रश्न-7.भारत में पर्यावरणीय प्रदूषण की स्थिति की विस्तार से विवेचना कीजिए।
उत्तर:- भारत में औद्योगीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। प्रमुख प्रदूषण प्रकार हैं:
- वायु प्रदूषण – वाहनों, उद्योगों, निर्माण कार्यों और पराली जलाने से वायु में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा बढ़ी है। दिल्ली जैसे महानगर सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- जल प्रदूषण – नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू गंदगी और रसायनों का बहाव जल को विषैला बना रहा है। गंगा, यमुना आदि प्रदूषित नदियों में शामिल हैं।
- ध्वनि प्रदूषण – शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक, लाउडस्पीकर, मशीनें आदि इसका प्रमुख कारण हैं।
- मृदा प्रदूषण – रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है।
सरकार द्वारा ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’, ‘नमामि गंगे’ जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, परंतु नागरिक जागरूकता और सामूहिक प्रयास के बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती।
प्रश्न-8.भारत की उत्तरी विशाल मैदान के भौतिक विभागों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भारत का उत्तरी विशाल मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों—गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र—द्वारा निर्मित एक समतल और उपजाऊ मैदान है। इसे सामान्यतः तीन प्रमुख भौतिक विभागों में बाँटा जाता है:
- पश्चिमी भाग (सिंधु मैदान): यह भाग पाकिस्तान और पंजाब-हरियाणा तक फैला है। यहाँ सिंचाई हेतु नहरें प्रमुख हैं और कृषि विकसित है।
- मध्य भाग (गंगा मैदान): उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों से बना है। धान, गेहूं, गन्ना आदि की खेती यहाँ होती है।
- पूर्वी भाग (ब्रह्मपुत्र मैदान): यह असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ भारी वर्षा होती है तथा बाढ़ की समस्या रहती है।
यह मैदान कृषि, जनसंख्या घनत्व और सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
प्रश्न-9. भारत में जनसंख्या विस्फोट एवं खाद्य सुरक्षा पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, विशेष रूप से खाद्यान्न की माँग निरंतर बढ़ रही है।
खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को पर्याप्त, पोषणयुक्त और सुरक्षित भोजन मिलना। भारत में ‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013’ लागू किया गया है, जिससे लगभग 80 करोड़ लोगों को सब्सिडी पर अनाज मिलता है।
जनसंख्या विस्फोट से कृषि भूमि का दवाब बढ़ता है, जल स्रोतों पर भार पड़ता है, और भंडारण एवं वितरण व्यवस्था पर भी तनाव आता है।
इस समस्या से निपटने के लिए परिवार नियोजन, महिलाओं की शिक्षा, कृषि तकनीक का सुधार, और भंडारण प्रणाली को मज़बूत करना आवश्यक है। साथ ही, सरकार और नागरिकों को मिलकर संसाधनों के संरक्षण की दिशा में कार्य करना होगा।
प्रश्न-10. भारत में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- भारत लौह अयस्क उत्पादन में विश्व के प्रमुख देशों में से एक है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन मुख्यतः चार क्षेत्रों में केंद्रित है:
- झारखंड और ओडिशा: सिंहभूम (झारखंड) और क्योंझर, सुंदरगढ़ (ओडिशा) में लौह अयस्क की प्रमुख खदानें हैं।
- कर्नाटक: बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर जिले प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।
- छत्तीसगढ़: दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव जिले में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
- गोवा और महाराष्ट्र: गोवा की खदानें भी समुद्री निर्यात में योगदान देती हैं।
भारत में लौह अयस्क का प्रयोग मुख्यतः इस्पात उद्योग में होता है तथा ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड इसके प्रमुख निर्यातक राज्य हैं।
प्रश्न-11. हरित क्रान्ति का भौगोलिक विवेचन कीजिए
उत्तर:- हरित क्रान्ति 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाई गई थी। इसका भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र विशेष में असमान रूप से पड़ा।
- क्षेत्रीय प्रभाव: हरित क्रान्ति का सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला जहाँ सिंचाई, उर्वरक और बीजों की सुविधा थी।
- फसल प्रभाव: यह क्रान्ति गेहूं और धान की उच्च उत्पादक किस्मों पर केंद्रित थी, जिससे अन्य फसलें उपेक्षित रहीं।
- पर्यावरणीय प्रभाव: रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं जल उपयोग में वृद्धि से मृदा क्षरण, जल स्तर में गिरावट और पारिस्थितिक असंतुलन हुआ।
- सामाजिक प्रभाव: अमीर किसानों को लाभ हुआ, परंतु छोटे किसानों के लिए यह क्रान्ति सीमित रही।
हरित क्रान्ति भारत के कुछ भागों को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सफल रही, परंतु इसकी सफलता सीमित क्षेत्रीय और सामाजिक दायरे तक रही।
प्रश्न-12. भारत में जल संकट को समझाइए।
उत्तर:- भारत में जल संकट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसके पीछे कई कारण हैं:
- असम वितरण: देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और कुछ में सूखा रहता है, जिससे जल असंतुलन होता है।
- भूजल दोहन: अत्यधिक सिंचाई और नगरीकरण के कारण भूजल स्तर तेजी से घट रहा है।
- प्रदूषण: औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू गंदगी के कारण नदियों व तालाबों का जल उपयोग योग्य नहीं रहता।
- जनसंख्या वृद्धि: जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में भारी कमी आई है।
- जल संरक्षण की कमी: पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा और वर्षा जल संचयन की कमी भी संकट का कारण है।
जल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण, पुनर्भरण एवं सतत प्रबंधन की आवश्यकता है।
प्रश्न-13. भारत में प्रादेशिक नियोजन पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करना है। भारत में यह योजना प्रक्रिया 1960 के बाद विशेष रूप से उभरी।
- क्षेत्रीय विषमता: कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में विकास तेज़ रहा, जबकि पूर्वोत्तर, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य पिछड़े रहे।
- नियोजन आयोग की भूमिका: पंचवर्षीय योजनाओं में प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए विशेष क्षेत्रीय योजनाएँ बनाई गईं।
- बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट: पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज और औद्योगिक छूट प्रदान की गई।
- क्षेत्रीय योजना उदाहरण: दामोदर घाटी योजना, पंचशील योजनाएँ, गढ़वाल-कुमाऊं क्षेत्रीय योजना आदि।
प्रादेशिक नियोजन भारत के समावेशी विकास के लिए आवश्यक है, ताकि सभी क्षेत्रों को समान अवसर प्राप्त हो सकें।
प्रश्न-14. प्रायद्वीपीय पठार के भौतिक विभागों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक प्राचीन और स्थायी भू-आकृतिक क्षेत्र है, जो दक्कन ट्रेप, ग्रेनाइट और ग्नीस चट्टानों से निर्मित है। यह पठार तीन प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है:
छोटा नागपुर पठार – यह झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में फैला हुआ है। यह पठार खनिजों से समृद्ध है और कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट आदि यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।
प्रायद्वीपीय पठार ऊँचाई में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः घटता जाता है और इसका जलप्रवाह भी इसी दिशा में होता है।
मालवा पठार – यह उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक फैला है। यह पठार काली मिट्टी (रेगुर) से ढका है।
दक्कन पठार – यह दक्षिण भारत का प्रमुख हिस्सा है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु आते हैं। यह पठार बेसाल्टिक चट्टानों से बना है और यहाँ अनेक नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा बहती हैं।
प्रश्न-15. भारत में कोयले के वितरण एवं उत्पादन पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- भारत कोयले के भंडारों में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल है। यहाँ मुख्यतः तीन प्रकार का कोयला पाया जाता है – एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। भारत में कोयले का उत्पादन मुख्यतः पूर्वी और मध्य भारत में केंद्रित है।
मुख्य कोयला क्षेत्र:
झारखंड: यहाँ झरिया, बोकारो और रानीगंज प्रमुख क्षेत्र हैं। यह देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है।
छत्तीसगढ़: कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं।
ओडिशा: तलचर और झारसुगुड़ा प्रमुख क्षेत्र हैं।
पश्चिम बंगाल: रानीगंज कोलफील्ड एक पुराना और समृद्ध क्षेत्र है।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र: सिंगरौली और चंद्रपुर जैसे क्षेत्र यहाँ स्थित हैं।
उत्पादन: भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, इस्पात उद्योग और अन्य भारी उद्योगों में किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है।
प्रश्न-16. भारत में मरुस्थलीकरण को समझाइए।
उत्तर:- मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे-धीरे रेगिस्तानी भूमि में परिवर्तित हो जाती है। भारत में मरुस्थलीकरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बनता जा रहा है।
मुख्य कारण:
- अत्यधिक चराई और वनों की कटाई
- भूमि का अत्यधिक दोहन और सिंचाई की गलत विधियाँ
- जलवायु परिवर्तन और कम वर्षा
- रेत के कणों का फैलाव
प्रभावित क्षेत्र: - राजस्थान का थार मरुस्थल – सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है।
- गुजरात, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से – धीरे-धीरे मरुस्थलीकरण की चपेट में आ रहे हैं।
निवारण के उपाय:
वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण
टिकाऊ कृषि प्रणाली अपनाना
जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई
भारत सरकार “राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण नियंत्रण कार्यक्रम (NADP)” के माध्यम से इस समस्या से निपटने का प्रयास कर रही है।
प्रश्न-17. भारत में मिट्टियों के प्रकार एवं वितरण का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो भौगोलिक स्थितियों, जलवायु और वनस्पति के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं।
मुख्य प्रकार की मिट्टियाँ:
काली मिट्टी (रेगुर): महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त।
जलोढ़ मिट्टी: उत्तर भारत के गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान में पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ होती है।
लाल मिट्टी: तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है।
लेटराइट मिट्टी: केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मिलती है। वर्षा क्षेत्र में विकसित।
रेतीली मिट्टी: राजस्थान और हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। जलधारण क्षमता कम होती है।
पहाड़ी मिट्टी: जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मिलती है।
मिट्टियाँ कृषि, जल संरक्षण, और वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका संरक्षण आवश्यक है।
प्रश्न-18. भारत के भौगोलिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए
उत्तर:-भारत की भौगोलिक संरचना विविधताओं से भरपूर है, जिसे निम्न प्रमुख प्रदेशों में बाँटा जा सकता है:
हिमालय क्षेत्र: उत्तर भारत में स्थित, तीन श्रेणियों – हिमाद्रि, हिमाचल और शिवालिक में विभाजित। यह क्षेत्र पर्वतीय, बर्फाच्छादित और भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है।
उत्तर भारतीय मैदान: सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र। यह कृषि के लिए उपयुक्त है।
प्रायद्वीपीय पठार: मध्य और दक्षिण भारत में स्थित यह क्षेत्र प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। यह खनिज संसाधनों से समृद्ध है।
थार मरुस्थल: पश्चिमी भारत में स्थित शुष्क क्षेत्र। यह रेत के टीलों और कम वर्षा वाला है।
तटीय मैदान: पूर्व और पश्चिम में फैले तटवर्ती क्षेत्र – जहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु और मत्स्य उद्योग प्रमुख हैं।
द्वीप समूह: अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह, सामरिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।
भारत की यह भौगोलिक विविधता यहाँ की जलवायु, कृषि, जीवनशैली और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है
प्रश्न-19. वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका को समझाइए
उत्तर:- भारत आज वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया है। इसकी भूमिका अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है:
राजनयिक भूमिका: भारत संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर सक्रिय है और विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है।
आर्थिक भूमिका: भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, और सेवा क्षेत्र में इसकी भागीदारी बढ़ रही है।
सैन्य और सुरक्षा क्षेत्र: भारत एक परमाणु शक्ति राष्ट्र है और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पर्यावरणीय नेतृत्व: भारत पेरिस जलवायु समझौते का समर्थक है और “अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन” का संस्थापक सदस्य है।
वैश्विक स्वास्थ्य: COVID-19 महामारी में भारत ने वैक्सीन मैत्री (Vaccine Maitri) अभियान द्वारा कई देशों को वैक्सीन सहायता दी।
संस्कृति और कूटनीति: योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और भारतीय भाषाओं का प्रसार भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है।
इस प्रकार, भारत वैश्विक राजनीति, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आर्थिक सहयोग में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है।
प्रश्न-20. भारत के वृहत् मैदान का विस्तृत वर्णन, उत्पत्ति तथा वर्गीकरण सहित कीजिए।
उत्तर:- भारत का वृहत् मैदान गंगा, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित विशाल जलोढ़ मैदान है, जो हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच स्थित है। इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर के अपक्षरण और नदियों द्वारा लाए गए तलछटों के जमाव से हुई। यह मैदान लगभग 2500 किमी लंबा और 240 से 320 किमी चौड़ा है।
इस मैदान को भौगोलिक दृष्टि से तीन भागों में बाँटा गया है:
पश्चिमी भाग (सिंधु घाटी मैदान): पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भाग शामिल हैं।
मध्य भाग (गंगा घाटी मैदान): उत्तर प्रदेश, बिहार तक फैला हुआ है।
पूर्वी भाग (ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान): असम एवं पूर्वोत्तर भारत तक विस्तृत है।
यह मैदान कृषि, परिवहन तथा जनसंख्या की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ एवं सिंचाई की सुविधा बेहतर है।
प्रश्न-21. हिमालय एवं प्रायद्वीपीय प्रवाह प्रणालियों में अन्तर बताइए।
उत्तर:- हिमालयी और प्रायद्वीपीय प्रवाह प्रणालियाँ भारत की दो प्रमुख जल निकासी प्रणालियाँ हैं, जिनमें अनेक भिन्नताएँ हैं:
उत्पत्ति: हिमालयी नदियाँ हिमनदों से निकलती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ झरनों और पहाड़ों से।
प्रवाह का स्वरूप: हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं।
घाटियाँ: हिमालयी नदियाँ गहरी घाटियाँ और भ्रंश घाटियाँ बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ पठारी क्षेत्र में उथली घाटियाँ बनाती हैं।
प्रवाह दिशा: हिमालयी नदियाँ प्रायः पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायः पूर्व या पश्चिम की ओर।
प्रमुख नदियाँ: हिमालयी – गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र; प्रायद्वीपीय – गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी।
इन दोनों प्रणालियों ने भारत की कृषि, जलस्रोत और सभ्यता को विकसित किया है।
प्रश्न-22. भारत में रंगों के आधार पर वर्गीकृत मृदा प्रकारों में विशिष्ट रासायनिक एवं खनिज विशेषताएँ होती हैं। विवेचना कीजिए।
उत्तर:- भारत में मृदाओं का वर्गीकरण उनके रंग के आधार पर किया गया है, जो उनके रासायनिक एवं खनिज संघटन को दर्शाता है:
काली मिट्टी (रेगूर): गहरी काली रंग की मिट्टी, बेसाल्टिक चट्टानों से बनी, इसमें चूना, लोहा और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कपास के लिए उपयुक्त है।
लाल मिट्टी: लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। यह दक्षिण और पूर्व भारत में मिलती है।
जलोढ़ मिट्टी: पीली से हल्की भूरी, अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें पोटाश और चूना अधिक होता है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है।
पीली मिट्टी: यह पश्चिमी भारत में पाई जाती है, जिसमें लोहा, चूना कम होता है।
पर्वतीय मिट्टी: ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है।
हर मृदा की विशिष्ट रासायनिक संरचना कृषि उपयुक्तता को प्रभावित करती है।
प्रश्न-23. भारत में हरित क्रांति के लाभ एवं सीमाएँ। विवेचना कीजिए।
उत्तर:-लाभ:
अन्न उत्पादन में वृद्धि: गेहूँ और चावल का उत्पादन विशेष रूप से बढ़ा।
भुखमरी में कमी: खाद्य संकट से राहत मिली।
कृषि में आधुनिकता: सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग बढ़ा।
रोजगार के अवसर: कृषि आधारित उद्योगों में वृद्धि हुई।
हरित क्षेत्र: पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख लाभान्वित क्षेत्र रहे।
सीमाएँ:
क्षेत्रीय असमानता: केवल कुछ राज्यों को लाभ मिला, अन्य उपेक्षित रह गए।
प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव: भूजल स्तर में गिरावट और मिट्टी की उर्वरता में कमी।
छोटे किसानों की उपेक्षा: महंगे बीज, उर्वरक आदि छोटे किसानों के लिए कठिन।
रासायनिक प्रदूषण: अत्यधिक कीटनाशकों के कारण पर्यावरणीय क्षति।
हरित क्रांति ने भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान की, परंतु इसकी दीर्घकालिक टिकाऊता पर पुनर्विचार आवश्यक है
प्रश्न-24. भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- भारत में सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन काल से स्थापित है। यह उद्योग कच्चे माल, जल, श्रमिक और बाजार पर आधारित है।
प्रमुख वितरण क्षेत्र:
महाराष्ट्र: मुंबई और नागपुर देश के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं। यहाँ कच्चा माल, बंदरगाह सुविधा और श्रमिक उपलब्ध हैं।
गुजरात: अहमदाबाद को “भारत का मैनचेस्टर” कहा जाता है।
पश्चिम बंगाल: कोलकाता में यह उद्योग अच्छा विकसित है।
उत्तर प्रदेश: कानपुर, वाराणसी में हथकरघा व विद्युतचालित इकाइयाँ हैं।
तमिलनाडु: कोयंबटूर और चेन्नई में सूती वस्त्र उद्योग विकसित है।
कारक:
जलवायु, श्रमिकों की उपलब्धता, बिजली, परिवहन, और निर्यात सुविधा इस उद्योग को प्रभावित करते हैं।
निष्कर्षतः, यह उद्योग ग्रामीण रोजगार, निर्यात और अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
प्रश्न-25. राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर:-हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के दक्षिण-पूर्व भाग में स्थित एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिले शामिल हैं।
भू-आकृति: यह क्षेत्र मालवा पठार का हिस्सा है, जो काली मिट्टी और बलुआ पत्थरों से युक्त है। यहाँ चंबल, पार्वती, कालीसिंध जैसी नदियाँ बहती हैं।
जलवायु: उप-आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसमें औसतन 75-100 सेमी वार्षिक वर्षा होती है।
मिट्टी: यहाँ की काली मिट्टी कपास व सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है।
कृषि: मुख्य फसलें गेहूँ, चावल, सोयाबीन, चना हैं। सिंचाई में चंबल घाटी परियोजना का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
खनिज संसाधन: कोटा पत्थर प्रसिद्ध है।
उद्योग: कोटा में थर्मल पावर प्लांट, कोटा स्टोन उद्योग, रासायनिक व विद्युत परियोजनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।
निष्कर्षतः, हाड़ौती क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, कृषि और उद्योग की दृष्टि से सम्पन्न और विकसित क्षेत्र है।
प्रश्न-26. हिमालय का प्रादेशिक विभाजन को समझाइए।
उत्तर:- हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और यह भारत, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत तक फैली हुई है। इसका प्रादेशिक विभाजन मुख्यतः तीन भागों में किया गया है:
- पश्चिमी हिमालय: यह भाग जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, और हिमाचल प्रदेश में फैला है। यहाँ के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख और पीर पंजाल हैं। यहाँ की जलवायु ठंडी व शुष्क है।
- मध्य हिमालय (हिमाचल हिमालय): यह क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में आता है। इसमें मशहूर घाटियाँ जैसे कि कुमाऊँ और गढ़वाल हैं। यह क्षेत्र पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- पूर्वी हिमालय: यह भाग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में फैला है। यहाँ की पर्वतमालाएँ कम चौड़ी परंतु अधिक ऊँचाई वाली हैं। यह क्षेत्र जैवविविधता से भरपूर है।
इस प्रकार, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भू-आकृतिक, जलवायवीय व सांस्कृतिक आधार पर किया गया है।
प्रश्न-27. भारत में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण पर मृदा के प्रभाव का परीक्षण कीजिए।
उत्तर:- भारत में मृदा की विविधता का सीधा प्रभाव प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण पर पड़ता है। भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के विकास के लिए अनुकूल होती हैं:
जलोढ़ मृदा: गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है। यहाँ घने पर्णपाती वन तथा बांस, साल आदि के वृक्ष विकसित होते हैं।
काली मृदा (रेगुर मृदा): यह मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलती है। इसमें अधिक नमी रोकने की क्षमता होती है, जिससे यहाँ सूखा प्रतिरोधी वनस्पतियाँ उगती हैं।
लाल मृदा: दक्षिण भारत में पाई जाती है, जो वनस्पति के लिए मध्यम उपजाऊ होती है। यहाँ झाड़ीदार वन तथा टीक और बबूल जैसे वृक्ष मिलते हैं।
रेतीली मृदा: राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति जैसे केक्टस, बबूल आदि मिलते हैं।
इस प्रकार मृदा की भौतिक व रासायनिक संरचना वनस्पति के प्रकार और घनत्व को प्रभावित करती है।
प्रश्न-28. भारत की गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे स्रोत हैं जो अक्षय हैं और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। भारत में इनके विकास की अत्यधिक संभावनाएँ हैं:
सौर ऊर्जा: भारत के अधिकांश भागों में साल भर सूरज की रोशनी मिलने के कारण यह प्रमुख गैर-परंपरागत स्रोत है। गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं।
पवन ऊर्जा: तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, और कर्नाटक में पवन ऊर्जा परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं।
जैव ऊर्जा: यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, और वन अपशिष्ट से प्राप्त होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बहुत उपयोगी है।
भूतापीय और समुद्री ऊर्जा: ये भविष्य की संभावनाएँ हैं जिनका प्रयोग सीमित रूप से हो रहा है।
गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत स्वच्छ, सस्ती व दीर्घकालिक ऊर्जा समाधान प्रदान करते हैं।
प्रश्न-29. भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भारत को कृषि जलवायु के आधार पर 15 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में बाँटा गया है। ये क्षेत्र मृदा, वर्षा, तापमान और फसल पैटर्न के आधार पर विभाजित हैं:
- पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र: सेब, आलू और जौ की खेती प्रमुख है।
- गंगा का मैदानी क्षेत्र: गेंहू, धान, गन्ना, दालें आदि उगाई जाती हैं।
- पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र: चाय, चावल और मक्का की खेती होती है।
- दक्कन का पठारी क्षेत्र: कपास, मूंगफली, ज्वार की खेती प्रमुख है।
- कांटेदार झाड़ी वाला क्षेत्र (राजस्थान): बाजरा, तिल और चना प्रमुख फसलें हैं।
- पूर्वी तटीय क्षेत्र: चावल, नारियल, गन्ना।
- पश्चिमी तटीय क्षेत्र: धान, सुपारी, मसाले आदि।
यह विभाजन किसानों को उपयुक्त फसलें चुनने, कृषि नीति निर्धारण और जल संसाधन प्रबंधन में सहायता करता है।
प्रश्न-30. भारत में रेल परिवहन के लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:-लाभ:
- व्यापक नेटवर्क: भारत में रेलवे का विशाल जाल है जो देश के दूरदराज़ क्षेत्रों को जोड़ता है।
- कम लागत: लंबी दूरी की यात्रा और भारी माल के लिए सस्ता माध्यम है।
- रोजगार: लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देता है।
- समाजिक एकता: विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों को जोड़ने में सहायक है।
हानियाँ:
- भीड़भाड़ और देरी: समय पर ट्रेनें नहीं चलती और अधिकतर ट्रेनों में भीड़ होती है।
- प्रबंधन समस्याएँ: भ्रष्टाचार, खराब रखरखाव और असुविधाजनक सेवाएँ समस्याएँ हैं।
- हादसे: दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।
- ऊर्जा खपत: अभी भी डीजल आधारित इंजनों का प्रयोग होता है जो प्रदूषण बढ़ाते हैं।
इस प्रकार, भारत में रेलवे परिवहन लाभकारी है, परंतु इसे अधिक सुरक्षित, तेज और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है।
Section-C
प्रश्न-1.इंदिरा गाँधी नहर परियोजना को विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (Indira Gandhi Canal Project – IGNP) भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, जिसे पहले ‘राजस्थान नहर’ के नाम से जाना जाता था। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई जल प्रदान करके हरित क्रांति की तर्ज पर कृषि उत्पादन बढ़ाना था।
परियोजना का इतिहास और उद्देश्य: इंदिरा गाँधी नहर परियोजना की योजना 1948 में बनी और निर्माण कार्य 1958 में प्रारंभ हुआ। यह परियोजना दो चरणों में पूर्ण हुई। इसका नाम 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य थार मरुस्थल के क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन और मानव जीवन को सहायता प्रदान करना है।
नहर की संरचना: यह नहर हरिके बैराज (पंजाब) से निकलकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होती हुई जैसलमेर और बाड़मेर तक जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से सतलज और ब्यास नदियों से जल प्राप्त करती है। इसमें मुख्य नहर, ब्रांच नहरें, वितरण प्रणाली और डिस्ट्रीब्यूटरी प्रणाली शामिल हैं।
लाभ:
- कृषि विकास – बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया गया।
- हरित क्रांति – गेहूँ, सरसों, बाजरा आदि की पैदावार बढ़ी।
- पेयजल आपूर्ति – ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध।
- पर्यावरणीय सुधार – हरियाली में वृद्धि, रेतीले तूफानों में कमी।
- औद्योगिक विकास – सिंचाई से जुड़ी इकाइयों की स्थापना।
चुनौतियाँ:
- जलभराव और लवणता – अधिक सिंचाई से भूजल स्तर बढ़ा।
- भूमि क्षरण – जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से।
- विस्थापन और सामाजिक समस्याएँ – भूमि अधिग्रहण से जनसंख्या प्रभावित।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवनदायिनी सिद्ध हुई है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सफल नहर परियोजनाओं में से एक है, जिसने शुष्क क्षेत्र को हरित क्षेत्र में बदलने में अहम भूमिका निभाई है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2. भारत में वर्षा का वितरण प्रतिरूप बताइए
उत्तर:- भारत में वर्षा का वितरण मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून पर आधारित है। मानसून के आगमन, विस्तार, तीव्रता एवं वापसी के आधार पर देश में वर्षा का वितरण क्षेत्रीय रूप से भिन्न होता है।
- प्रमुख वर्षा ऋतु:
भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण-पश्चिम मानसून है, जो जून से सितम्बर तक सक्रिय रहता है और कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75% प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ भागों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात भी वर्षा का कारण बनते हैं। - वर्षा का क्षेत्रीय वितरण:
अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र: पूर्वोत्तर भारत (मेघालय का मासिनराम, चेरापूंजी), पश्चिमी घाट, असम, बंगाल और तटीय कर्नाटक – यहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है।
मध्यम वर्षा क्षेत्र: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र आदि में 100–200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है।
अल्प वर्षा क्षेत्र: राजस्थान का पश्चिमी भाग, गुजरात का कच्छ, लद्दाख, तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा – यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
वर्षा का समय और स्वरूप:
मानसून असम में जून के पहले सप्ताह में आता है और धीरे-धीरे उत्तर और पश्चिम की ओर फैलता है। सितम्बर के अंत तक इसकी वापसी शुरू हो जाती है। कहीं-कहीं वर्षा तीव्र, अनवरत होती है तो कहीं रुक-रुक कर।
वर्षा की अस्थिरता:
भारतीय वर्षा में क्षेत्रीय, कालिक एवं तीव्रता की अस्थिरता पाई जाती है, जिससे सूखा, बाढ़ और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
मानव जीवन पर प्रभाव:
कृषि, जल आपूर्ति, ऊर्जा, परिवहन आदि मानसून पर निर्भर हैं। इसलिए वर्षा वितरण की असमानता देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है।
प्रश्न-3. प्रादेशिक विषमता की दशांने वाले प्रमुख सूचकों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- प्रादेशिक विषमता (Regional Disparity) से तात्पर्य भारत के विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी विकास के स्तर में असमानता से है। इस असमानता को विभिन्न सूचकों के माध्यम से समझा जा सकता है।
- प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income):
यह प्रमुख आर्थिक सूचक है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की तुलना में कहीं अधिक है। - औद्योगिक विकास:
पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य औद्योगिक रूप से विकसित हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्य, छत्तीसगढ़, बिहार आदि में औद्योगिक विकास की गति धीमी है। - कृषि उत्पादकता:
पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादन अधिक है, जबकि राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों में उत्पादकता कम है। - शिक्षा और साक्षरता दर:
केरल, तमिलनाडु में साक्षरता दर अधिक है, जबकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह कम है। - स्वास्थ्य सेवाएँ:
केरल जैसे राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी हैं, जबकि मध्य भारत के कुछ राज्य अभी भी मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। - बुनियादी ढाँचा (Infrastructure):
सड़क, बिजली, जल आपूर्ति जैसी सुविधाओं में भी राज्यों के बीच असमानता देखी जाती है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। - नगरीकरण स्तर:
महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में नगरीकरण का स्तर अधिक है, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों और बिहार में नगरीकरण न्यून है।
प्रादेशिक विषमता भारत के समग्र विकास में एक बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास, विशेष आर्थिक पैकेज, बुनियादी सेवाओं का विस्तार और क्षेत्रीय योजना बनाना आवश्यक है।
प्रश्न-4. भारत में नगरीकरण के विकास का वर्णन करते हुए इससे उत्पन्न समस्याओं का विवेचन कीजिए।
उत्तर:- नगरीकरण (Urbanization) से तात्पर्य जनसंख्या के नगरों की ओर प्रवास तथा नगरों के विस्तार से है। भारत में नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, विशेषकर स्वतंत्रता के बाद।
विकास की प्रक्रिया:
- स्वतंत्रता पूर्व नगरीकरण:
प्राचीन नगर जैसे वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र धार्मिक एवं व्यापारिक केंद्र थे। औपनिवेशिक काल में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बंदरगाह नगर विकसित हुए। - स्वतंत्रता के बाद:
औद्योगीकरण, सेवा क्षेत्र का विकास, एवं आधारभूत ढाँचे में वृद्धि से नगरीकरण तीव्र हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या नगरी क्षेत्रों में निवास करती है।
नगरीकरण के कारण:
ग्रामीण-शहरी प्रवास
औद्योगीकरण
सेवा क्षेत्र का विकास
शिक्षा एवं रोजगार की उपलब्धता
नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएँ:
- झुग्गी-झोपड़ियाँ और अव्यवस्थित बस्तियाँ
गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए आवास की कमी के कारण अवैध बस्तियों का विकास। - यातायात जाम और प्रदूषण
वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण वायु, ध्वनि प्रदूषण तथा जाम की समस्या। - जल संकट और स्वच्छता
बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में जल आपूर्ति, सीवेज, सफाई आदि की व्यवस्था अपर्याप्त। - बेरोजगारी और अपराध
शहरी क्षेत्र में रोजगार की सीमित संभावनाओं के कारण बेरोजगारी व अपराध दर बढ़ती है। - कचरा प्रबंधन की समस्या
ठोस अपशिष्ट निस्तारण की समुचित व्यवस्था का अभाव।
भारत में नगरीकरण विकास का प्रतीक है, लेकिन यदि यह अनियंत्रित रूप से होता है तो समस्याएँ उत्पन्न करता है। अतः योजनाबद्ध नगरीकरण, स्मार्ट सिटी योजना, आधारभूत सेवाओं का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास अत्यंत आवश्यक है।
प्रश्न-5. भारत को प्रमुख नदी बेसिनों में विभाजित कीजिए तथा उनका वर्णन कीजिए
उत्तर:- भारत में जल संसाधनों का वितरण नदी बेसिनों के आधार पर किया जा सकता है। एक नदी बेसिन वह क्षेत्र होता है जहाँ की सभी वर्षा जल धाराएँ किसी एक प्रमुख नदी में प्रवाहित होती हैं। भारत को मुख्यतः सात प्रमुख नदी बेसिनों में बाँटा गया है:
- गंगा बेसिन:
यह भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो उत्तर भारत के अधिकांश भाग को आच्छादित करता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि हैं। यह बेसिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला है। - ब्रह्मपुत्र बेसिन:
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में प्रवेश करती है। यह क्षेत्र अत्यधिक वर्षा वाला है और बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ लोहित, तिस्ता और मानस हैं। - सिंधु बेसिन:
सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ – झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज – पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बहती हैं। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है, परन्तु भारत में इसका उत्तरी-पश्चिमी भाग आता है। - नर्मदा और तापी बेसिन:
ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला है जबकि तापी बेसिन महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित है। - महानदी बेसिन:
महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह बेसिन छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के कुछ भागों को समेटे हुए है। - गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बेसिन:
यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। गोदावरी को ‘दक्षिण की गंगा’ कहा जाता है। कृष्णा और कावेरी बेसिन क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित हैं। - पश्चिमी घाट की छोटी नदियाँ:
ये नदियाँ छोटी होने के बावजूद वर्षा जल की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं और पश्चिमी समुद्र तट पर बहती हैं, जैसे – मांडवी, जुआरी, पेरियार आदि।
भारत में इन नदी बेसिनों का उपयोग सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन एवं जल परिवहन में होता है। जल संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु इन बेसिनों की समग्र योजना एवं संरक्षण आवश्यक है
प्रश्न-6. भारत में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की संभावना एवं विकास पर भौगोलिक लेख लिखिए।
उत्तर:- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों (कोयला, पेट्रोलियम) से अलग हैं और पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत स्वच्छ माने जाते हैं। भारत में इन ऊर्जा स्रोतों की विशाल संभावनाएँ हैं।
- प्रमुख अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत:
सौर ऊर्जा: भारत सूर्य रेखा के समीप स्थित होने से 300 से अधिक दिन सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएँ हैं।
पवन ऊर्जा: गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में समुद्री तट और पठारी क्षेत्रों में तेज हवाएँ चलती हैं जो पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त हैं।
जैव ऊर्जा: कृषि अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट तथा कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने की अपार संभावना है। यह ग्रामीण भारत के लिए उपयोगी है।
भूतापीय ऊर्जा: हिमालयी क्षेत्र, खासकर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भूतापीय संसाधनों की उपस्थिति है।
लहर एवं ज्वार ऊर्जा: समुद्र तटीय क्षेत्रों में यह ऊर्जा संसाधन धीरे-धीरे विकसित हो रहा है, विशेषकर गुजरात और तमिलनाडु में।
- विकास की दिशा में प्रयास:
भारत सरकार ने “राष्ट्रीय सौर मिशन”, “ऊर्जा संरक्षण अधिनियम”, “भारत अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी” (IREDA) के माध्यम से इन स्रोतों को बढ़ावा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने “अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन” की पहल की है। - संभावनाएँ और लाभ:
पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी
जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी
ग्रामीण रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा
सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान
- चुनौतियाँ:
उच्च प्रारंभिक लागत, तकनीकी ज्ञान की कमी, अवसंरचना की सीमाएँ और नीति समन्वय की आवश्यकता।
भारत में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास की अपार संभावनाएँ हैं। यदि सही नीति, निवेश और जनजागरूकता के साथ इनका उपयोग हो, तो भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
प्रश्न-7. भारत में नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए
उत्तर:- प्रश्न 4 सेक्शन स
प्रश्न-8. भारत की स्थिति, विस्तार, आकार एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल उपमहाद्वीप है। यह देश भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
स्थिति (Location):
भारत उत्तर गोलार्द्ध में स्थित है। यह भूमध्य रेखा से उत्तर में 8°4′ उत्तरी अक्षांश से लेकर 37°6′ उत्तरी अक्षांश तक और 68°7′ पूर्वी देशांतर से 97°25′ पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत का मानक समय 82°30′ पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो इलाहाबाद (प्रयागराज) के निकट नैनी से होकर गुजरता है।
विस्तार (Extent):
भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग 3,214 किलोमीटर है। यह देश एक त्रिभुजाकार आकृति में विस्तारित है जिसकी लंबाई और चौड़ाई काफी अधिक है।
आकार (Size):
भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश बनाता है। यह क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप का लगभग 2.4% और विश्व का लगभग 0.57% है।
सीमाएँ (Boundaries):
भारत की स्थल सीमाएँ कुल 15,200 किलोमीटर लम्बी हैं और समुद्री तटरेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की सीमाएँ आठ देशों से मिलती हैं:
- पाकिस्तान (पश्चिम में)
- अफगानिस्तान (उत्तर-पश्चिम में)
- चीन (उत्तर में)
- नेपाल (उत्तर में)
- भूटान (उत्तर-पूर्व में)
- बांग्लादेश (पूरब में)
- म्यांमार (पूर्व में)
- श्रीलंका (दक्षिण में – समुद्र के द्वारा)
भारत को हिन्द महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से समुद्री सीमाएँ प्राप्त हैं।
भारत की स्थिति व विस्तार न केवल इसे भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं, बल्कि यह राजनीतिक, सांस्कृतिक व व्यापारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्र है। इसकी सीमाएँ विविध देशों से जुड़ी होने के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय रणनीति व संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है।
प्रश्न9. चम्बल घाटी परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए।-
उत्तर:- चम्बल घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान और मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित चम्बल नदी पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण है।
परियोजना का आरंभ:
चम्बल घाटी परियोजना की शुरुआत 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई। यह परियोजना राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकारों की साझेदारी में विकसित की गई थी।
मुख्य घटक (Components):
इस परियोजना में निम्नलिखित प्रमुख बाँध और जलाशय शामिल हैं:
- गांधी सागर बाँध:
यह परियोजना का पहला बाँध है, जो मध्यप्रदेश में मंदसौर जिले के पास स्थित है।
इसकी ऊँचाई लगभग 64 मीटर है।
इसमें जलविद्युत उत्पादन की सुविधा भी है।
- राणा प्रताप सागर बाँध:
यह बाँध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है।
यहाँ जलविद्युत उत्पादन के अतिरिक्त सिंचाई की भी व्यवस्था है।
- जवाहर सागर बाँध:
यह बाँध कोटा जिले में स्थित है।
इसका उपयोग मुख्यतः बिजली उत्पादन हेतु किया जाता है।
- कोटा बैराज:
यह मुख्य रूप से सिंचाई हेतु बनाया गया है और कोटा जिले में स्थित है।
लाभ (Benefits):
राजस्थान और मध्यप्रदेश के लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है।
लाखों किलोवाट जलविद्युत का उत्पादन होता है।
कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जैसे शहरों को जल और ऊर्जा की आपूर्ति होती है।
परियोजना से क्षेत्रीय विकास, उद्योगों की स्थापना और रोजगार सृजन हुआ है।
चुनौतियाँ:
बाँधों के निर्माण से विस्थापन हुआ।
पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हुआ।
गाद जमाव और जलप्रदूषण की समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
चम्बल घाटी परियोजना एक सफल नदी घाटी परियोजना है जिसने राजस्थान और मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह परियोजना सिंचाई, ऊर्जा और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण है।
प्रश्न-10. भारत में पेट्रोलियम के वितरण एवं उत्पादन को समझाइए
उत्तर:- भारत में पेट्रोलियम एक प्रमुख खनिज ईंधन है जो औद्योगिक, परिवहन एवं घरेलू उपयोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है।
उत्पादन क्षेत्र (Production Areas):
भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
- बम्बई हाई (मुंबई अपतटीय क्षेत्र):
यह भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है।
1974 में यहाँ पेट्रोलियम की खोज हुई थी।
यह भारत के कुल उत्पादन का लगभग 38% भाग प्रदान करता है।
- असम (नौगांव, डिगबोई, मोरान, लाकवा):
भारत में पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले 1867 में डिगबोई में हुई थी।
आज भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है।
- गुजरात (अंकेलेश्वर, कलोल, नवा गाम):
यहाँ जमीन के नीचे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं।
गुजरात भारत के कुल उत्पादन का लगभग 15% प्रदान करता है।
- राजस्थान (बाड़मेर):
हाल के वर्षों में बाड़मेर के मंगला और भोगावत क्षेत्रों में पेट्रोलियम की खोज हुई है।
वितरण (Distribution):
भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन कुछ ही राज्यों तक सीमित है।
परंतु इसकी खपत पूरे देश में है, इसलिए पाइपलाइन, रेल और समुद्री मार्गों से पेट्रोलियम का वितरण किया जाता है।
प्रमुख रिफाइनरी स्थान: मथुरा, बरौनी, हल्दिया, कोची, पारादीप, जामनगर आदि।
भारत की स्थिति:
भारत में पेट्रोलियम की घरेलू आपूर्ति पर्याप्त नहीं है।
देश अपनी आवश्यकता का लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है।
इसलिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं जैसे कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास।
भारत में पेट्रोलियम उत्पादन सीमित क्षेत्रों में होता है लेकिन यह संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। इसके वितरण को सुव्यवस्थित कर देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।
प्रश्न-11. भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए
उत्तर:- भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण देश को अनेक सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
- संसाधनों पर दबाव:
जनसंख्या वृद्धि से जल, भोजन, ऊर्जा, भूमि आदि संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इससे संसाधनों की कमी और उपयोगिता में असमानता आती है। - बेरोजगारी और गरीबी:
नवीन रोजगार अवसर जनसंख्या वृद्धि की गति से नहीं बढ़ पाते। इससे बेरोजगारी बढ़ती है और गरीबी की स्थिति बनी रहती है। - शिक्षा और स्वास्थ्य पर बोझ:
सरकारी विद्यालयों और अस्पतालों पर बोझ बढ़ता है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। पर्याप्त शिक्षकों, डाक्टरों और संसाधनों की कमी हो जाती है। - पर्यावरणीय समस्याएँ:
वनों की कटाई, जल और वायु प्रदूषण, भूमि क्षरण आदि समस्याएँ जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हैं। अधिक जनसंख्या अधिक प्रदूषण को जन्म देती है। - शहरीकरण और झुग्गी बस्तियाँ:
ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ता है। इससे शहरी जनसंख्या अधिक होती है और झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या बढ़ती है। - खाद्य संकट:
अधिक जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की माँग बढ़ती है, जिससे खाद्य संकट और कुपोषण जैसी समस्याएँ पैदा होती हैं। - परिवहन और यातायात दबाव:
जनसंख्या बढ़ने से सड़क, रेल, बस आदि यातायात साधनों पर अत्यधिक दबाव होता है जिससे जाम, दुर्घटनाएँ और प्रदूषण बढ़ता है।
समाधान:
जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों का सशक्त प्रचार।
शिक्षा का प्रसार, विशेष रूप से महिलाओं में।
रोजगार के अवसरों का सृजन और ग्रामीण विकास।
तीव्र जनसंख्या वृद्धि भारत के समग्र विकास में बाधक है। इसके निवारण के लिए जनजागरूकता, नीति-निर्धारण और संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग की आवश्यकता है।
प्रश्न-12. भारत को भौतिक विभागों में बाँटिए तथा उत्तरी मैदान का विस्तार से वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भारत की भौगोलिक संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण है। इसे भौतिक आधार पर पाँच प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है:
- हिमालय पर्वतमाला
- उत्तरी या गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान
- प्रायद्वीपीय पठार
- थार मरुस्थल
- तटीय मैदान एवं द्वीप समूह
उत्तरी मैदान का विस्तृत वर्णन:
उत्तरी मैदान भारत के उत्तर में हिमालय की तलहटी और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित है। यह मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ (alluvial) निक्षेपों से बना है। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक है।
प्राकृतिक विशेषताएँ:
यह मैदान अत्यंत समतल है और समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 200 से 300 मीटर तक होती है। इसमें ढाल सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है।
उपविभाजन:
उत्तरी मैदान को तीन उपविभागों में बाँटा जाता है:
- पंजाब मैदान: यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है।
- गंगा मैदान: यह सबसे विस्तृत भाग है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला है।
- ब्रह्मपुत्र मैदान: असम राज्य में स्थित यह भाग ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है।
महत्त्व:
यह क्षेत्र भारत का कृषि प्रधान क्षेत्र है। गेहूँ, चावल, गन्ना, दलहन आदि की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर होती है। यह क्षेत्र जनसंख्या घनत्व में भी अत्यधिक है और कई महत्वपूर्ण नगर जैसे दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता आदि यहाँ स्थित हैं।
प्रश्न-13. भारत में कागज एवं लुग्दी उद्योग के वितरण एवं अवस्थितीय कारकों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- कागज एवं लुग्दी उद्योग:
यह उद्योग लकड़ी, बांस, घास, कपास की चिंदियों, रद्दी कागज आदि से कागज का निर्माण करता है। लुग्दी (Pulp) इसका प्रमुख कच्चा माल है।
भारत में प्रमुख कागज उद्योग केंद्र:
- पश्चिम बंगाल – उत्तरपाड़ा, बैरकपुर
- महाराष्ट्र – पुणे, बल्लारशाह
- उत्तर प्रदेश – सहारनपुर, लखनऊ
- मध्य प्रदेश – नेपानगर (देश का पहला समाचार पत्र कागज कारखाना)
- तमिलनाडु – सिवकासी, मेट्टूपालयम
- आंध्र प्रदेश – राजमुंद्री
- गुजरात – वापी
वितरण के अवस्थितीय कारक:
- कच्चा माल: बांस, लकड़ी, रद्दी कागज आदि का नजदीक होना। उदाहरण: मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत में बांस की उपलब्धता।
- जल की उपलब्धता: लुग्दी निर्माण में जल की बड़ी मात्रा आवश्यक होती है।
- ऊर्जा: कागज उत्पादन में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, अतः बिजली और कोयले की सुलभता जरूरी है।
- सस्ते परिवहन: कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन हेतु रेलवे और सड़क सुविधाएँ जरूरी हैं।
- बाजार: शिक्षा, प्रिंटिंग, पैकेजिंग आदि क्षेत्रों में कागज की माँग होने के कारण शहरी क्षेत्रों के पास उद्योग केंद्रित होते हैं।
- श्रम: सस्ते एवं प्रशिक्षित श्रमिकों की उपलब्धता भी एक प्रमुख कारण है।
भारत में कागज उद्योग ने विकास की ओर कदम बढ़ाया है, परंतु इसके लिए पर्यावरणीय संरक्षण और रीसायक्लिंग तकनीक अपनाना आवश्यक है।
प्रश्न-14. भारत में नदियों के एकीकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीजिए।
उत्तर:- नदियों के एकीकरण का अर्थ:
नदियों के एकीकरण (Interlinking of Rivers) का तात्पर्य विभिन्न नदियों को नहरों या अन्य माध्यमों से जोड़कर जल की कमी और बाढ़ की समस्या को संतुलित करना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) के माध्यम से इस योजना को आगे बढ़ाया है।
प्रस्तावित परियोजनाएँ:
- गंगा-कावेरी लिंक
- केन-बेतवा लिंक
- पार-तापी-नर्मदा लिंक
- दमनगंगा-पिंजाल लिंक आदि
सकारात्मक पक्ष:
- जल वितरण में संतुलन: बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से जल को सूखा क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि: खेती के लिए सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी।
- जल परिवहन: आंतरिक जल परिवहन में सुधार होगा।
- बिजली उत्पादन: बांधों के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन संभव है।
नकारात्मक पक्ष:
- पर्यावरणीय प्रभाव: वनों की कटाई, जैव विविधता पर खतरा और पारिस्थितिकी में असंतुलन हो सकता है।
- मानव विस्थापन: बड़े बांधों के कारण लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं।
- राज्यों के बीच विवाद: जल वितरण को लेकर राज्यों में टकराव हो सकता है।
- अत्यधिक लागत: यह परियोजना अत्यधिक पूंजी और समय की मांग करती है।
नदियों के एकीकरण की योजना संभावनाओं से परिपूर्ण है, परंतु इसे कार्यान्वित करने से पूर्व सामाजिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक पहलुओं का समुचित मूल्यांकन आवश्यक है।
प्रश्न-15. हरित क्रान्ति का क्या अर्थ है? हरित क्रान्ति का भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण कीजिए।
उत्तर:- हरित क्रांति का अर्थ:
हरित क्रांति से तात्पर्य उस कृषि परिवर्तन से है, जिसमें उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के साधन तथा आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि की गई। भारत में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई और इसका प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था।
मुख्य विशेषताएँ:
- उच्च उत्पादकता वाले बीजों (HYV) का उपयोग
- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग
- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
- कृषि यंत्रीकरण (ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि)
भारतीय कृषि पर प्रभाव:
सकारात्मक प्रभाव:
- उत्पादन में वृद्धि: विशेषकर गेहूँ और चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इससे सर्वाधिक लाभान्वित हुए।
- आत्मनिर्भरता: भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना और आयात पर निर्भरता कम हुई।
- कृषि तकनीक का विकास: नई तकनीकों और यंत्रों का प्रयोग बढ़ा जिससे कृषि क्षेत्र आधुनिक बना।
- कृषक आय में वृद्धि: कुछ क्षेत्रों में किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
नकारात्मक प्रभाव:
- क्षेत्रीय असमानता: हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों (जैसे पंजाब, हरियाणा) तक सीमित रहा, जबकि पूर्वी और दक्षिणी भारत वंचित रहे।
- प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव: भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, मृदा की उर्वरता में कमी आदि समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
- रासायनिक प्रदूषण: अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से जल एवं मृदा प्रदूषित हुए।
- छोटे किसानों को नुकसान: उन्नत तकनीक के लिए आवश्यक संसाधन छोटे किसानों के लिए सुलभ नहीं थे।
हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को एक नई दिशा दी, परंतु इसके दुष्प्रभावों के समाधान हेतु सतत कृषि विकास की आवश्यकता है।
vmou mage-06 paper , vmou ma final year exam paper , vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4