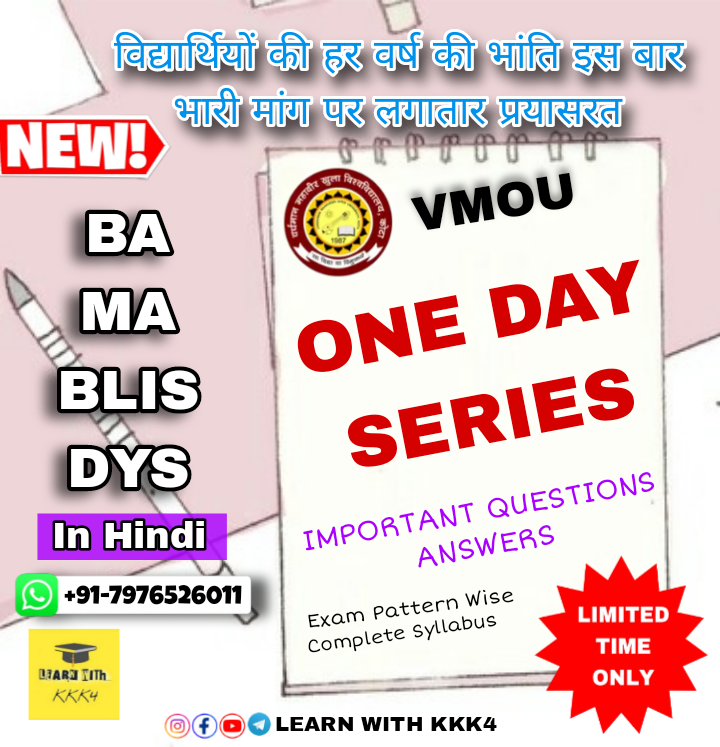VMOU MAHI-05 Paper MA Final Year (SEMESTER-III & IV); vmou exam paper
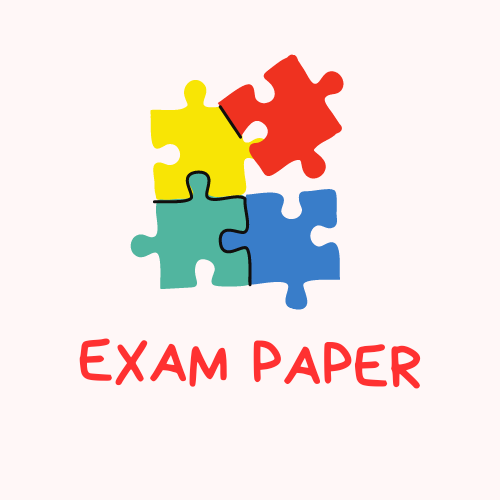
VMOU MA Final Year के लिए इतिहास ( MAHI-05 , प्राचीन भारत में राज्य एवं राजनीति ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.मंडल सिद्धान्त क्या है?
उत्तर:- मंडल सिद्धान्त चाणक्य द्वारा प्रतिपादित एक राजनैतिक सिद्धान्त है, जिसमें राज्य की सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों को मंडलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.प्राचीन भारत के किन्हीं दो करों के नाम लिखिए।
उत्तर:- भूमि कर (भाग) और उत्पाद कर (शुल्क)।
प्रश्न-3.रामायण किसने लिखा ?
उत्तर:- महर्षि वाल्मीकि ने
प्रश्न-4. इंडिका का लेखन कौन था?
उत्तर:- मेगस्थनीज
प्रश्न-5. किन्हीं दो महाजनपदों के नाम लिखिए।
उत्तर:- मगध और कौशल।
प्रश्न-6. मनु कौन थे?
उत्तर:- मनु प्राचीन भारत के विधिशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक और मनुस्मृति के रचयिता थे।
प्रश्न-7. किन्हीं दो आश्रमों के नाम लिखिए।
उत्तर:- ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम।
प्रश्न-8. कल्हण कौन था?
उत्तर:- कल्हण एक कश्मीरी इतिहासकार थे, जिन्होंने ‘राजतरंगिणी’ की रचना की थी।
प्रश्न-9. महाभारत का रचियता कौन था?
उत्तर:- महर्षि वेदव्यास
प्रश्न-10. विद्ध को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- विदथ वैदिक काल की एक सभा थी, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों पर विचार-विमर्श होता था।
प्रश्न-12 उत्तर पश्चिमी भारत के दो गणतंत्रों के नाम लिखिए।
उत्तर:- शाक्य और लिच्छवी
प्रश्न-13. महासम्मत को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- महासम्मत वह व्यक्ति होता था जिसे जनसामान्य की सहमति से राजा चुना जाता था।
प्रश्न-14. वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में बताइए।
उत्तर:- वर्णाश्रम व्यवस्था समाज को चार वर्णों और चार आश्रमों में विभाजित करने की प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी।
प्रश्न-15. नीतिसार का लेखक कौन था?
उत्तर:-नीतिसार के लेखक कामंदक थे।
प्रश्न-16. अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु क्या है?
उत्तर:- अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु शासन व्यवस्था, प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, न्याय एवं कूटनीति है।
प्रश्न-17. दो स्मृतियों के नाम लिखिए।
उत्तर:- मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति।
प्रश्न-18. विदथ की परिभाषा कीजिए।
उत्तर:- वेदिक काल में विदथ जनसभा का प्राचीन रूप था, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर विचार होता था।
प्रश्न-19. रत्निन कौन था?
उत्तर:- रत्निन राजा के दरबार का प्रमुख सभासद होता था, जो विशेष अधिकार और पदवी वाला अधिकारी होता था।
प्रश्न-20. प्रयाग प्रशस्ति’ के बारे में लिखिए।
उत्तर:- प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख है जो सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों और प्रशासनिक कार्यों का विवरण देता है।
प्रश्न-21. श्रेणी क्या है? दो श्रेणियों के नाम लिखिए।
उत्तर:- श्रेणी प्राचीन भारत में व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था; दो श्रेणियाँ हैं– लोहार श्रेणी और कुम्हार श्रेणी।
प्रश्न-22. दो उपनिषदों के नाम लिखिए।
उत्तर:-ईशोपनिषद और कठोपनिषद।
प्रश्न-23. अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु क्या है ?
उत्तर:- अर्थशास्त्र में राज्य संचालन, प्रशासन, न्याय, कर, युद्धनीति एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन है।
प्रश्न-24. रत्निन कौन था ?
उत्तर:- रत्निन वे प्रमुख अधिकारी या दरबारी थे जो राजा के राजसूय यज्ञ में भाग लेते थे।
प्रश्न-24. गीता क्या है
उत्तर:- गीता महाभारत का एक भाग है जिसमें श्रीकृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति का उपदेश दिया।
प्रश्न-25. प्राचीन भारत के दो राजनीतिक विचारकों के नाम लिखिए।
उत्तर:- कौटिल्य और मनु
प्रश्न-26. वर्णाश्रम धर्म को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- वर्णाश्रम धर्म वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के कार्य और कर्तव्य वर्ण (जाति) और आश्रम (जीवन-चरण) पर आधारित होते हैं।
प्रश्न-27. अश्वमेध यज्ञ का क्या महत्व है ?
उत्तर:- अश्वमेध यज्ञ शक्ति, साम्राज्य विस्तार और राजकीय श्रेष्ठता का प्रतीक था।
प्रश्न-28. राज्य के सप्तांग सिद्धान्त के नाम लिखो
उत्तर:- सेक्शन ब प्रश्न 2
प्रश्न-29. षाडगुण्य नीति
उत्तर:- षाडगुण्य का अर्थ है छह नीतियाँ – संधि (संधान), विग्रह (युद्ध), यान (चढ़ाई करना), आसन (तटस्थ रहना), संश्रय (शरण लेना) और द्वैधभाव (दोहरी नीति अपनाना)।
प्रश्न-30.अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु
उत्तर:-शासन व्यवस्था, प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, न्याय एवं कूटनीति है।
Section-B
प्रश्न-1.प्राचीन भारत के गणराज्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में राजतंत्र के साथ-साथ गणराज्य भी विकसित हुए थे। गणराज्य वह व्यवस्था थी जहाँ सत्ता एक व्यक्ति के बजाय एक सभा या समुदाय के हाथों में होती थी। ऐसे गणराज्य मुख्यतः उत्तर भारत, विशेषकर गंगा घाटी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित थे। प्रमुख गणराज्यों में लिच्छवि, मल्ल, शाक्य, वैज्जी और कौशल आदि का नाम लिया जा सकता है। इन गणराज्यों में नीति-निर्माण सभा द्वारा किया जाता था, जिसे ‘सभा’ या ‘संघ’ कहा जाता था। इनमें निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जाते थे। बौद्ध साहित्य और जैन ग्रंथों में इन गणराज्यों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। बुद्ध स्वयं शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। इन गणराज्यों की विशेषता यह थी कि ये अधिक लोकतांत्रिक थे और उनमें राजा नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि शासन चलाते थे। यह प्रणाली मौर्यकाल से पहले तक प्रभावी रही
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.राज्य के सप्तांग सिद्धान्त के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:- सप्तांग सिद्धान्त प्राचीन भारत में राज्य की संरचना को समझाने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है, जिसे कौटिल्य ने ‘अर्थशास्त्र’ में विस्तृत रूप से समझाया है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य सात अंगों से मिलकर बना होता है:
स्वामी (राजा) – शासन का प्रमुख, राज्य का सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता।
अमात्य (मंत्री) – शासन में सहयोग देने वाले मंत्रीगण।
जनपद – राज्य की जनता और भू-भाग।
दुर्ग – रक्षक किला, सुरक्षा हेतु आवश्यक।
कोष – राज्य का वित्तीय भंडार।
दंड – न्याय व दंड व्यवस्था, सेना।
मित्र – सहयोगी राज्य या राजा।
इन सात अंगों की संतुलित स्थिति से ही राज्य मजबूत और स्थायी बनता है। यह सिद्धान्त राज्य की स्थायित्व और नीति-निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।
प्रश्न-3.मगध साम्राज्य के उत्कर्ष पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रारंभ में हर्यक वंश के बिंबिसार (लगभग 546 ई.पू.) ने इसकी नींव रखी। उन्होंने विवाह, युद्ध और संधि जैसे उपायों से राज्य को विस्तृत किया। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने मगध को और सुदृढ़ बनाया। उन्होंने काशी और वैशाली जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार किया। इसके बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश ने शासन किया, जिनके अधीन मगध और भी शक्तिशाली हुआ।
मगध की उन्नति में इसकी भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि, लोहे के खनिज, गंगा नदी के मार्ग, और सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र ने प्रमुख भूमिका निभाई। अंततः मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को हटाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। thus, मगध भारत का पहला महान साम्राज्य बना, जिसने पूरे उत्तर भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया।
प्रश्न-4.मौर्यों के केन्द्रीय प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- मौर्य वंश के शासनकाल में केन्द्रीय प्रशासन अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत था। चन्द्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी, परंतु अशोक के समय में यह अपने चरम पर पहुँचा। शासन का प्रमुख केंद्र राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजा के अधीन एक मंत्री परिषद कार्य करती थी, जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्री शामिल थे। कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ और मेगस्थनीज की ‘इंडिका’ में मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है।
प्रमुख विभागों में – राजस्व विभाग, व्यापार विभाग, न्याय विभाग, गुप्तचर विभाग आदि थे। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक विशेष अधिकारी होता था, जैसे ‘संभागाध्यक्ष’ (राजस्व अधिकारी), ‘पुलिस अधिकारी’ और ‘न्यायाधीश’। प्रशासन के लिए लेखा विभाग और जासूसी व्यवस्था भी अत्यंत मजबूत थी। सम्राट अशोक के काल में धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की गई, जो सामाजिक और नैतिक कार्यों की निगरानी करते थे। मौर्य प्रशासन अपने समय का सबसे शक्तिशाली और अनुशासित प्रशासनिक ढांचा था।
प्रश्न-5.’शान्तिपर्व’ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- शान्तिपर्व’ महाभारत का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राजाभिषेक और उनके शासन-सम्बंधी विचारों को प्रस्तुत करता है। इसमें कुल 3 उपपर्व – राजधर्म पर्व, आपद्धर्म पर्व और मोक्षधर्म पर्व शामिल हैं। इस ग्रंथ में शासन की नैतिकता, राजा के कर्तव्य, मंत्रियों की भूमिका, न्याय, दंड नीति और मोक्ष मार्ग का विस्तृत वर्णन है।
भीष्म पितामह, जो युद्ध में घायल होकर शरशैय्या पर लेटे हैं, वे युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हैं। ‘शान्तिपर्व’ राज्यशास्त्र, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का अद्भुत संगम है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय राजनीति और धर्म के आदर्शों को स्पष्ट करता है।
प्रश्न-6.गुप्तकालीन राजनैतिक संगठनों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए।
उत्तर:- गुप्त काल (लगभग 320–550 ई.) को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग माना जाता है। इस काल में राजनैतिक संगठन एक केंद्रीकृत राजतंत्र के रूप में विकसित हुए। सम्राट गुप्तवंशी राजा सर्वशक्तिमान होता था, परंतु वह मंत्रिपरिषद की सलाह से शासन करता था। प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेश, जनपद, विशय (जिला) और ग्राम स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए जाते थे।
केन्द्रीय प्रशासन के अंतर्गत ‘सामंत’, ‘राजा’, ‘उपराजा’, ‘अमात्य’ जैसे अधिकारी कार्य करते थे। ग्राम प्रशासन में ‘ग्रामिक’ प्रमुख होता था।
गुप्तकाल में नगरपालिकाएँ, व्यापारिक संघ (श्रेणियाँ), तथा ग्राम सभाएँ भी प्रशासन में भाग लेती थीं। ‘प्रशस्तियाँ’ और ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि अधिकारीगण दान, न्याय और कर व्यवस्था के कार्य देखते थे। प्रशासनिक संगठन कुशल और स्थिर था।
प्रश्न-7.’अर्थशास्त्र’ के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:- ‘अर्थशास्त्र’ प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना चाणक्य (कौटिल्य या विष्णुगुप्त) ने की थी। यह ग्रंथ मौर्य काल में शासन, राजनीति, अर्थनीति और कूटनीति का व्यापक ज्ञान देता है। इसमें राजा की योग्यता, मंत्रियों की भूमिका, राज्य की संरचना (सप्तांग सिद्धान्त), कर व्यवस्था, न्याय प्रणाली, गुप्तचर तंत्र, युद्ध नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की विस्तृत व्याख्या की गई है।
यह ग्रंथ केवल आर्थिक विषयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण प्रशासनिक मार्गदर्शिका है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने ‘राजधर्म’ और ‘लोक कल्याण’ को शासन का मूल उद्देश्य बताया है। यह ग्रंथ आज भी राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में अत्यंत मूल्यवान माना जाता है।
प्रश्न-8.पुरूषार्थ चतुष्ट्य क्या है?
उत्तर:- पुरुषार्थ चतुष्ट्य प्राचीन भारतीय जीवन-दर्शन का मूल आधार है, जो चार मुख्य उद्देश्यों को दर्शाता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
धर्म – यह नैतिकता, कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है।
अर्थ – यह जीवनयापन के लिए धन, समृद्धि और संसाधनों की प्राप्ति है।
काम – यह इच्छाओं, सुख और प्रेम की पूर्ति से संबंधित है।
मोक्ष – यह जीवन-मुक्ति या आत्मा की अंतिम मुक्ति का लक्ष्य है।
इन चारों पुरुषार्थों का संतुलन ही एक आदर्श जीवन की पूर्ति मानी जाती है। मनु और अन्य धर्मशास्त्रों में पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है। धर्म को आधार मानकर अर्थ और काम की प्राप्ति तथा अंततः मोक्ष की प्राप्ति प्राचीन भारतीय समाज का आदर्श माना गया।
प्रश्न-9. ‘हरिषेण’ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- हरिषेण गुप्तकाल के एक प्रसिद्ध कवि, प्रशस्तिकार और सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि तथा मंत्री थे। उन्होंने इलाहाबाद स्तंभ पर खुदी समुद्रगुप्त की प्रशंसा में ‘प्रयाग प्रशस्ति’ की रचना की थी। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में और काव्य शैली में लिखी गई है।
हरिषेण ने समुद्रगुप्त की विजयों, धार्मिक नीति, दानशीलता और प्रशासनिक योग्यता का विवरण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी प्रशस्ति से गुप्तकालीन राजनीति, सैन्य अभियान और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है।
हरिषेण की रचना न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वह गुप्तकाल की साहित्यिक उत्कृष्टता का भी उदाहरण है।
प्रश्न-10 श्रेणियों के आर्थिक महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में श्रेणियाँ (Guilds) कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे, जिनका आर्थिक जीवन में अत्यंत महत्त्व था। ये श्रेणियाँ विशेष रूप से नगरों में फलती-फूलती थीं। प्रत्येक श्रेणी किसी विशेष व्यवसाय से संबंधित होती थी, जैसे कुम्हारों की श्रेणी, बुनकरों की श्रेणी, सुनारों की श्रेणी आदि।
इन श्रेणियों ने श्रमिकों को संगठित किया, उनके अधिकारों की रक्षा की और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की। वे कीमतों का निर्धारण, वेतन तय करना, प्रशिक्षण देना, और आपसी विवादों का समाधान करने जैसे कार्य करती थीं।
आर्थिक दृष्टि से, श्रेणियाँ वाणिज्य और उद्योग के केंद्र बनीं। वे वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करती थीं। इसके अलावा, कई श्रेणियाँ मंदिरों और राज्य को ऋण भी देती थीं, जिससे उनका राजनीतिक महत्त्व भी बढ़ता था।
प्रश्न-11. अशोक के अभिलेखों की ऐतिहासिक स्रोत के रूप में विवेचना कीजिए।
उत्तर:- अशोक के अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। ये अभिलेख पत्थरों, स्तंभों और गुफाओं पर ब्राह्मी, खरोष्ठी तथा यूनानी लिपियों में खुदवाए गए थे। इन अभिलेखों से अशोक के शासनकाल, धर्मनीति, प्रशासनिक व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है।
अशोक के अभिलेखों में प्रमुख रूप से धर्म प्रचार, अहिंसा, सत्य, करुणा, धार्मिक सहिष्णुता आदि मूल्यों पर बल दिया गया है। उन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार किया और इसे पूरे साम्राज्य में फैलाया।
इतिहासकारों के लिए ये अभिलेख समकालीन घटनाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इनमें अशोक के व्यक्तिगत विचार, नीतियाँ और जनता के प्रति उसका दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अशोक के शिलालेखों से ही हमें उसके साम्राज्य की सीमाएँ, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और जनता की स्थिति की जानकारी मिलती है।
इस प्रकार अशोक के अभिलेख न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेज हैं, बल्कि उस युग की सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियों का भी प्रतिबिंब हैं।
प्रश्न-12. वेदों के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- वेदों में न केवल धार्मिक और दार्शनिक विचार मिलते हैं, बल्कि उसमें राजनीतिक जीवन की भी स्पष्ट झलक मिलती है। ऋग्वेद में राजा, सभा, समिति, और सैन्य संगठन जैसे कई राजनीतिक तत्त्वों का वर्णन मिलता है।
वेदों के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और उसका मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा, न्याय का पालन और यज्ञ की व्यवस्था करना होता था। राजा का चुनाव कभी-कभी ‘राजसूय यज्ञ’ के माध्यम से होता था, जिससे महासम्मति की अवधारणा भी दिखाई देती है।
सभा और समिति जैसे दो प्रमुख संस्थाएं उस समय की जनतांत्रिक प्रवृत्तियों का संकेत देती हैं। सभा में वरिष्ठ व्यक्ति शामिल होते थे जबकि समिति में सामान्य जन भाग लेते थे।
वेदों में ‘राजधर्म’ का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें राजा के कर्तव्यों का वर्णन होता है। राजा को धर्म, सत्य, और न्याय के अनुसार शासन करने की सलाह दी गई है।
इस प्रकार वेदों में शासन व्यवस्था, राजधर्म, तथा प्रशासनिक संस्थाओं का जो चित्रण है, वह प्राचीन भारत की राजनीतिक चेतना का प्रमाण है।
प्रश्न-13. मौर्यकालीन राजनैतिक संगठनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
उत्तर:- मौर्यकालीन राजनैतिक संगठन अत्यंत सुदृढ़ और केंद्रीकृत थे। शासन प्रणाली का संचालन चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सलाह से किया और आगे चलकर अशोक ने इसे और व्यापक बनाया।
राज्य का प्रमुख राजा होता था, जो सर्वशक्तिमान माना जाता था। उसके अधीन विभिन्न विभाग होते थे, जैसे वित्त, सैन्य, न्याय और धर्म। मंत्रीपरिषद (अमात्य मंडल) प्रशासन में सहायक थी।
नगरपालिका व्यवस्था भी अत्यंत संगठित थी, जिसमें नगरीय अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। न्यायालय प्रणाली में ‘धर्मस्थीय’ और ‘कण्टकशोधन’ न्यायालय होते थे।
अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के विवरणों से ज्ञात होता है कि मौर्य साम्राज्य में जासूसी तंत्र, गुप्तचर विभाग, राजकीय कारागार, श्रेणियाँ तथा एक संगठित सेना की भी व्यवस्था थी।
इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासनिक संगठन ने भारत में प्रथम विशाल साम्राज्य की सफल शासन व्यवस्था को संभव बनाया।
प्रश्न-14. कण्टकशोधन न्यायालयों की भूमिका को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- कण्टकशोधन न्यायालय मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग था। इसका मुख्य कार्य अपराधियों का दमन करना और समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना था।
यह न्यायालय विशेष रूप से गुप्तचरों की सहायता से अपराधों की जांच करता था। चोरी, धोखाधड़ी, घूस, तस्करी और राज्य विरोधी गतिविधियों के मामलों की सुनवाई यहाँ होती थी।
यह न्यायालय बाजार नियंत्रण, माप-तौल की निगरानी, मूल्य निर्धारण और व्यापारिक अनुशासन को बनाए रखने में भी सहायक था। इसके न्यायधीशों को कठोर और निष्पक्ष माना जाता था।
इस न्यायालय का उद्देश्य “कण्टक” अर्थात समाज को क्षति पहुँचाने वाले तत्वों को समाप्त करना था।
इस प्रकार कण्टकशोधन न्यायालय ने समाज को अनुशासित बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम में अहम भूमिका निभाई।
प्रश्न-15. ग्रामणी के महत्व की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- ग्रामणी प्राचीन भारत में गाँव का प्रधान अधिकारी होता था। वह प्रशासन, न्याय, कर संग्रह और कानून व्यवस्था के पालन में प्रमुख भूमिका निभाता था।
ग्रामणी गाँव के लोगों और राज्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। कर वसूली, भूमि का वितरण, कृषि व्यवस्था की देखरेख, विवादों का निपटारा और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता जैसे कार्य उसके अधीन होते थे।
उसका चुनाव प्रायः गांव की सहमति से होता था और उसे लोकमत का समर्थन प्राप्त होता था।
ग्रामणी का कार्यक्षेत्र सीमित होते हुए भी वह स्थानीय शासन व्यवस्था की रीढ़ होता था। उसकी प्रशासनिक कुशलता से ही राज्य की नीतियाँ नीचे स्तर तक लागू होती थीं।
इस प्रकार ग्रामणी का स्थान प्राचीन ग्रामीण प्रशासन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण था।
प्रश्न-16. स्मृतियों के आधार पर धर्म की परिभाषा दीजिए।
उत्तर:- स्मृतियों के अनुसार धर्म वह आचरण है जो समाज की स्थिरता, शांति और कल्याण सुनिश्चित करता है। ‘मनुस्मृति’ धर्म को उन कर्तव्यों और नियमों का समुच्चय मानती है जो व्यक्ति को जीवन में नैतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से अनुशासित करते हैं। मनु के अनुसार – “धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध – ये धर्म के लक्षण हैं।” स्मृतियाँ धर्म को चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और समाज की परंपराओं के अनुसार परिभाषित करती हैं। धर्म न केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित है, बल्कि यह सामाजिक उत्तरदायित्व, न्याय, व्यवहार और नीति तक फैला हुआ है। धर्म व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार स्मृतियों में धर्म का स्वरूप व्यापक, व्यावहारिक और सामाजिक रूप से उपयोगी बताया गया है।
प्रश्न-17. षाडगुण्य नीति का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- षाडगुण्य नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सिद्धांत है, जो राजा की अंतरराष्ट्रीय नीति को दर्शाती है। इसका उद्देश्य यह बताना है कि एक राजा को अपने शत्रु राज्यों के प्रति कौन-सी नीति अपनानी चाहिए। षाडगुण्य का अर्थ है छह नीतियाँ – संधि (संधान), विग्रह (युद्ध), यान (चढ़ाई करना), आसन (तटस्थ रहना), संश्रय (शरण लेना) और द्वैधभाव (दोहरी नीति अपनाना)।
संधि – जब राजा अपने से शक्तिशाली शत्रु से संधि करता है।
विग्रह – जब राजा युद्ध करता है।
यान – जब वह शत्रु पर आक्रमण करता है।
आसन – जब वह न तटस्थ होता है न कोई कार्य करता है।
संश्रय – जब वह किसी शक्तिशाली राजा की शरण लेता है।
द्वैधभाव – जब वह एक राज्य से संधि और दूसरे से युद्ध करता है।
यह नीति बताती है कि राजा को अपनी शक्ति, शत्रु की शक्ति और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। यह कूटनीति के क्षेत्र में प्राचीन भारत का एक अद्वितीय योगदान है।
प्रश्न-18. राजत्व के दैवीय सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:-दैवीय सिद्धांत के अनुसार राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। यह मान्यता प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों और स्मृतियों में व्यापक रूप से मिलती है। मनुस्मृति में राजा को ‘नर-देव’ कहा गया है, अर्थात वह धरती पर देवता के समान है। यह सिद्धांत कहता है कि राजा का अधिकार ईश्वर से प्राप्त होता है और उसकी आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य होता है। इस विचारधारा के अनुसार राजा अन्य सामान्य मनुष्यों से श्रेष्ठ होता है और उसका कार्य ईश्वर की इच्छा को लागू करना होता है। वह धर्म की रक्षा करता है, न्याय देता है और समाज में व्यवस्था बनाए रखता है।
राजा को धर्म के अधीन भी माना गया है, अर्थात उसे धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। यह सिद्धांत शासक की सत्ता को वैधता प्रदान करता था और लोगों को उसके प्रति वफादार बनाता था। साथ ही यह सिद्धांत राजा को भी उत्तरदायी बनाता था कि वह अधार्मिक कार्य न करे। इस प्रकार दैवीय सिद्धांत ने राजसत्ता को नैतिकता और धर्म से जोड़ा।
प्रश्न-19. गणतंत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में कई गणतंत्रात्मक राज्य थे, जैसे वैशाली (लिच्छवि), कपिलवस्तु (शाक्य), मल्ल, बुलि आदि। इन गणराज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था सामूहिक निर्णयों पर आधारित थी। यहाँ एक व्यक्ति की बजाय एक सभा (संघ या संघीय सभा) शासन करती थी, जिसे “गणसभा” कहा जाता था। इस सभा में योग्य और प्रमुख वंशों के सदस्य भाग लेते थे। गणसभाएँ निर्णय लेने, युद्ध नीति तय करने, कर निर्धारण और न्याय वितरण जैसे कार्यों में सक्रिय थीं।
इन गणराज्यों में प्रशासनिक प्रमुख को “राजा” या “महास्थविर” कहा जाता था, परंतु उसका कार्य निर्वाचित था और वह गणसभा के प्रति उत्तरदायी होता था।
न्यायिक व्यवस्था भी सभा या निर्वाचित न्यायाधीशों द्वारा संचालित होती थी।
गणराज्य धर्म, नैतिकता और जनहित के आधार पर शासन करते थे, जिससे प्रजा को भागीदारी का अनुभव होता था। हालांकि बाद में राजशाही राज्यों की सैन्य और प्रशासनिक शक्ति के सामने ये गणराज्य टिक नहीं सके। फिर भी इनकी व्यवस्था प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक तत्वों का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है।
प्रश्न-20. राज्य के कार्यों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में राज्य के कार्य बहुआयामी थे, जिनका उद्देश्य प्रजा की रक्षा, कल्याण और धर्म की स्थापना था। धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्र और महाकाव्यों में राज्य के मुख्य कार्यों को स्पष्ट किया गया है।
रक्षण कार्य – राज्य का प्रमुख कार्य प्रजा की रक्षा करना था, चाहे वह बाहरी आक्रमण से हो या आंतरिक अपराध से।
विधि और न्याय – राजा धर्म और स्मृति पर आधारित न्याय प्रणाली को लागू करता था। न्यायपालिका राज्य का एक अनिवार्य अंग थी।
धर्म की स्थापना – राजा का कर्तव्य था कि वह धर्म का पालन करे और प्रजा को भी धर्माचरण हेतु प्रेरित करे।
राजस्व संग्रह – राज्य करों के माध्यम से धन एकत्र करता था, जिससे प्रशासन, सेना और जनकल्याण के कार्य किए जाते थे।
जनकल्याण – राज्य सड़कों, सिंचाई, अस्पताल, शिक्षा आदि की व्यवस्था करता था।
विदेश नीति – राजा को शांति, युद्ध, संधि आदि मामलों में विदेश नीति अपनानी होती थी।
इस प्रकार राज्य न केवल शासन का एक यंत्र था, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का संरक्षक भी था।
प्रश्न-
उत्तर:-
प्रश्न-
उत्तर:-
प्रश्न-
उत्तर:-
प्रश्न-
उत्तर:-
प्रश्न-
उत्तर:-
प्रश्न-
उत्तर:-
प्रश्न-
उत्तर:-
प्रश्न-
उत्तर:-
प्रश्न-
उत्तर:-
प्रश्न-
उत्तर:-
Section-C
प्रश्न-1.प्राचीन भारतीय राज्य एवं राजनीति के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- प्राचीन भारतीय राज्य एवं राजनीति के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये स्रोत हमें न केवल उस काल के शासन-प्रशासन की जानकारी देते हैं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी विवेचन करते हैं। इन स्रोतों को मुख्यतः चार वर्गों में बाँटा जा सकता है – वेद, धर्मशास्त्र, महाकाव्य तथा अन्य ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण।
- वैदिक साहित्य:
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में उस समय की जनजातीय राजनीतिक संरचना, सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ‘राजन’ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि राजा का चुनाव होता था। सभा और समिति जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। - धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ:
मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति जैसे ग्रंथों में राज्य, राजा के कर्तव्य, दंड नीति, न्याय प्रणाली तथा मंत्री व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ प्राचीन भारत की विधिक और राजनीतिक परंपराओं को स्पष्ट करते हैं। - महाकाव्य:
रामायण और महाभारत न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि इनमें राजनीतिक तत्व भी भरे पड़े हैं। रामायण में राम का आदर्श राजधर्म और शासन व्यवस्था को दर्शाया गया है, जबकि महाभारत के शांतिपर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों में नीति, न्याय और राज्य संचालन की विस्तृत व्याख्या है। - अर्थशास्त्र:
कौटिल्य का ‘अर्थशास्त्र’ एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें शासन प्रणाली, कर व्यवस्था, राजनय, गुप्तचर व्यवस्था और सैन्य संगठन का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ मौर्य काल की राजनीति को समझने में सहायक है। - बौद्ध और जैन साहित्य:
पाली और प्राकृत ग्रंथों जैसे कि अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय तथा भगवती सूत्र आदि में गणराज्यों और संघों का उल्लेख मिलता है। इनसे ज्ञात होता है कि कुछ क्षेत्रों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी प्रचलित थी। - विदेशी यात्रियों के विवरण:
मेगस्थनीज का ‘इंडिका’, ह्वेनसांग और फाह्यान के यात्रा विवरण भारतीय राजनीति और प्रशासन की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन यात्रियों ने भारत की शासन व्यवस्था, नगर नियोजन, सेना, कर व्यवस्था आदि का विवरण दिया है।
उपरोक्त साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारत की शासन प्रणाली, राजनीतिक संगठन, न्यायिक व्यवस्था और राज्य की अवधारणा का गहन अध्ययन संभव होता है। इन स्रोतों से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत की राजनीतिक परंपरा अत्यंत समृद्ध और विकसित थी।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.मौर्यकालीन राजनीतिक संगठनों का विवरण दीजिए।
उत्तर:- मौर्य काल (ईसा पूर्व 322–185) भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक युग था। इस युग में चन्द्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से एक सशक्त और केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की। मौर्यकालीन राजनीतिक संगठन अत्यंत विकसित, संगठित और केंद्रीकृत थे। इस काल के प्रशासनिक संगठन का वर्णन ‘अर्थशास्त्र’ और ‘इंडिका’ में मिलता है।
- राजा और उसका पद:
राजा सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। वह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – तीनों शक्तियों का प्रमुख था। चन्द्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सम्राटों ने शासन को संगठित रूप दिया। - मंत्री परिषद:
राजा के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति और अन्य विभागाध्यक्ष होते थे। कौटिल्य के अनुसार, मंत्री चतुर, ईमानदार और राजा के प्रति निष्ठावान होने चाहिए। - प्रशासनिक विभाग:
प्रशासन के अनेक विभाग थे – जैसे आयकर विभाग, व्यापार विभाग, यातायात विभाग, नगर प्रशासन, गुप्तचर विभाग आदि। हर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। - नगर प्रशासन:
मेगस्थनीज के अनुसार, राजधानी पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन की व्यवस्था 6 समितियों द्वारा की जाती थी, जिनमें उद्योग, जनगणना, सुरक्षा, व्यापार आदि की देखरेख की जाती थी। - गुप्तचर व्यवस्था:
मौर्य शासन की सबसे मजबूत प्रणाली उसकी गुप्तचर व्यवस्था थी। जासूसों के माध्यम से राजा प्रजा, अधिकारियों और शत्रुओं की गतिविधियों की जानकारी रखता था। - न्याय व्यवस्था:
राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, लेकिन न्यायिक अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। दंड नीति पर विशेष बल दिया जाता था ताकि अनुशासन बना रहे। - प्रांतीय और ग्राम प्रशासन:
राज्य को अनेक प्रांतों में बाँटा गया था। हर प्रांत का शासन ‘कुमार अमात्य’ करता था। ग्राम स्तर पर ‘ग्रामिक’ नामक अधिकारी होते थे।
मौर्यकालीन प्रशासन एक शक्तिशाली, केंद्रीकृत और संगठित शासन प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसकी विशेषता इसकी अनुशासित व्यवस्था, योजनाबद्ध प्रशासन और जासूसी तंत्र में दिखाई देती है।
प्रश्न-3. प्राचीन भारत की गणतंत्रात्मक प्रणाली पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में जहाँ राजतंत्र प्रचलित था, वहीं गणराज्य प्रणाली भी विकसित थी। गणराज्य ऐसी शासन प्रणाली थी जहाँ सत्ता एक व्यक्ति के बजाय एक समिति या सभा के पास होती थी। यह व्यवस्था विशेषतः बौद्ध काल में गंगा घाटी और उत्तर-पश्चिमी भारत में देखी जाती थी।
- गणराज्य का स्वरूप:
गणराज्य में राजा का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता था। कई गणराज्यों में राजा के स्थान पर सभापति होता था, और निर्णय सामूहिक रूप से सभा द्वारा लिए जाते थे। ‘संघ’ और ‘सभा’ जैसे शब्दों का प्रयोग इस प्रणाली के लिए होता था। - प्रमुख गणराज्य:
लिच्छवि, मल्ल, शाक्य, वैज्जी, बुलि और कुरु जैसे गणराज्य प्रसिद्ध थे। इनका उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। महात्मा बुद्ध स्वयं शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। - प्रशासनिक प्रणाली:
इन गणराज्यों में नीतियाँ सभा द्वारा तय की जाती थीं। सभा के सदस्य सीमित संख्या में होते थे और वे योग्य तथा प्रतिष्ठित नागरिक होते थे। निर्णय बहुमत से लिए जाते थे और कार्यपालिका का दायित्व भी इन्हीं के अधीन होता था। - विशेषताएँ:
सत्ता का विकेन्द्रीकरण।
उत्तरदायी शासन व्यवस्था।
न्यायिक प्रक्रिया का विकास।
बौद्ध और जैन धर्मों के प्रसार में सहायक।
- अवनति के कारण:
गणराज्यों की अस्थिरता, आंतरिक मतभेद, सैनिक कमजोरी और मौर्य जैसे केंद्रीकृत साम्राज्य के उदय के कारण इनकी संख्या घटने लगी।
प्राचीन भारत की गणराज्य प्रणाली एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचायक थी। यह दर्शाती है कि भारत में प्राचीन काल से ही सामूहिक शासन और जनसहभागिता की परंपरा रही है।
प्रश्न-4. प्राचीन भारत में राज्य के स्वरूप एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में राज्य की अवधारणा धर्म, अर्थ और लोककल्याण पर आधारित थी। राज्य को धर्म का संरक्षक और जनकल्याण का साधन माना गया। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें दैविक, सामाजिक अनुबंध और प्राकृतिक सिद्धांत प्रमुख हैं।
- राज्य का स्वरूप:
राज्य को एक संगठित संस्था माना गया, जो राजा के नेतृत्व में कार्य करता था। ‘सप्तांग सिद्धांत’ के अनुसार राज्य सात अंगों से मिलकर बना होता है – राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये सभी अंग मिलकर राज्य को सुचारु रूप से संचालित करते हैं। - राज्य के उद्देश्य:
धर्म की रक्षा: धर्म और नैतिकता की स्थापना।
न्याय व्यवस्था: प्रजा को न्याय देना और अपराधियों को दंड देना।
राजस्व संग्रह: कोष के माध्यम से राज्य संचालन।
सुरक्षा व्यवस्था: सेना और दुर्गों के माध्यम से बाहरी और आंतरिक सुरक्षा।
लोक कल्याण: सिंचाई, सड़क, धर्मशाला, शिक्षा आदि सुविधाएँ देना।
- राजा की भूमिका:
राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। वह राजधर्म का पालन करता था। उसे प्रजा पालक, धर्मरक्षक और न्यायाधीश के रूप में देखा गया है। राम, युधिष्ठिर और अशोक जैसे राजाओं को आदर्श माना गया। - प्रशासनिक ढांचा:
राज्य के विभिन्न विभाग होते थे – जैसे न्याय, कर, व्यापार, कृषि आदि। इनके लिए योग्य अमात्य और अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। - वैदिक और उत्तर वैदिक काल:
प्रारंभिक वैदिक काल में जनतांत्रिक प्रणाली दिखाई देती है, परंतु उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र प्रबल हो गया।
प्राचीन भारत में राज्य न केवल सत्ता का केंद्र था, बल्कि समाजिक व्यवस्था, नैतिक मूल्यों और लोक कल्याण का संरक्षक भी था। उसका उद्देश्य केवल शासन नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना करना था।
प्रश्न-5. धर्मशास्त्रों में वर्णित राजनीतिक विचारों पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- धर्मशास्त्र प्राचीन भारतीय समाज के नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के साथ-साथ राजनीतिक विचारों के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें राजा, राज्य, राजधर्म, दंड नीति, और शासन के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति आदि प्रमुख धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं जिनमें राजनीतिक अवधारणाओं का गहन विवेचन हुआ है।
राजा और राज्य की अवधारणा:
धर्मशास्त्रों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति धर्म की रक्षा, समाज की सुरक्षा और न्याय के संचालन हेतु हुई। राजा को ‘धर्मस्य रक्षक’ (धर्म का रक्षक) कहा गया है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है और उसकी सत्ता को ईश्वरीय सत्ता से जोड़कर देखा गया है।
राजधर्म:
धर्मशास्त्रों में राजधर्म पर विशेष बल दिया गया है। राजा का कर्तव्य है कि वह निष्पक्षता से न्याय करे, धर्म का पालन करे, प्रजा की रक्षा करे और उनके कल्याण हेतु कार्य करे। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि “राजा वह है जो धर्मपूर्वक राज्य करता है।”
न्याय व्यवस्था:
धर्मशास्त्रों में राजा को सर्वोच्च न्यायाधीश माना गया है। न्याय चार प्रकार के माने गए — व्यवहार (व्यवसायिक), अचार (सामाजिक), निर्णय (न्यायिक) और दंड (दंडात्मक)। न्याय के निर्धारण में प्रमाण, साक्ष्य, शपथ और साक्षात्कार की विधियों का प्रयोग होता था।
दंड नीति:
दंड नीति को शासन संचालन का अनिवार्य उपकरण माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार, “दंड ही धर्म की रक्षा करता है।” दंड का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि सुधार करना और समाज में अनुशासन स्थापित करना होता था।
राज्य की संरचना:
धर्मशास्त्रों में राज्य की प्रशासनिक इकाइयों, मंत्रिपरिषद, सेना, कर प्रणाली आदि का वर्णन भी मिलता है। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री, पुरोहित, सेनापति, और प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए जाते थे।
धर्मशास्त्रों में राजनीतिक विचार नैतिकता और धर्म पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य एक आदर्श, धर्म-सम्मत और न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करना था। इन ग्रंथों में केवल सत्ता के प्रयोग की बात नहीं की गई, बल्कि सत्ता के संयम, कर्तव्य और धर्म का भी गहराई से विवेचन किया गया है। अतः धर्मशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति की नींव को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
प्रश्न-6. कौटिल्य अर्थशास्त्र की न्यायप्रणाली का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- कौटिल्य का “अर्थशास्त्र” प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राज्य-प्रशासन, राजनीति, विधि एवं न्याय प्रणाली का वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप में वर्णन किया गया है। इसमें न्याय को राज्य की मूल आधारशिला माना गया है।
न्याय का उद्देश्य:
कौटिल्य के अनुसार न्याय प्रणाली का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, अपराधों को नियंत्रित करना और प्रजा को न्याय प्रदान करना था। उनका मानना था कि “न्याय ही राज्य का आधार है।”
न्यायालय की संरचना:
राज्य में कई स्तरों पर न्यायालय स्थापित किए गए थे—राजा का न्यायालय सर्वोच्च था, जिसे ‘धर्मस्थीय’ कहा जाता था। उसके बाद ‘धर्मस्थ’, ‘प्रादेशिक’ और ‘जनपदीय’ स्तर पर न्यायालय होते थे। स्थानीय विवादों के समाधान के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर भी न्यायिक व्यवस्था थी।
न्यायाधीश:
राजा स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, परंतु उसके सहयोग हेतु प्रधान न्यायाधीश (प्राधिविवक) और अन्य सहायक न्यायाधीश होते थे। इन न्यायाधीशों को विधि, धर्म और व्यवहार का गहन ज्ञान होना आवश्यक था।
विधिक स्रोत:
अर्थशास्त्र के अनुसार न्याय का निर्धारण चार स्रोतों पर आधारित था—(1) धर्म (धर्मशास्त्र), (2) व्यवहार (परंपरा), (3) युक्ति (तर्क), और (4) राजाज्ञा (राजा का आदेश)। यदि किसी मामले में धर्मशास्त्र मौन हो तो राजा तर्क और परंपरा के अनुसार निर्णय ले सकता था।
न्याय प्रक्रिया:
अर्थशास्त्र में न्यायिक प्रक्रिया को अत्यंत व्यवस्थित बताया गया है—मुकदमे की सुनवाई, साक्ष्य, दस्तावेज, गवाह, शपथ, प्रत्यक्ष प्रमाण आदि के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाता था। झूठ बोलने वाले को दंडित किया जाता था।
दंड नीति:
कौटिल्य के अनुसार, अपराध के अनुसार दंड निश्चित किया जाता था। दंड का उद्देश्य समाज में अनुशासन और भय बनाए रखना था। उन्होंने दंड को शासन का प्रमुख उपकरण माना।
कौटिल्य की न्याय प्रणाली व्यावहारिक, सुसंगठित और तर्कसंगत थी। इसमें दंड और सुधार दोनों पक्षों का समन्वय था। प्रजा की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी मानी गई थी। कौटिल्य का न्याय संबंधी दृष्टिकोण आज भी प्रशासनिक न्यायशास्त्र के लिए प्रेरणास्रोत है।
प्रश्न-7. प्राचीन भारत में विधि एवं उसके वर्गीकरण की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में विधि (Law) एक धार्मिक, नैतिक और सामाजिक व्यवस्था का अंग थी। ‘विधि’ का अर्थ होता है—नियम या नियमों का वह संहिता जो व्यक्ति, समाज और राज्य के आचरण को नियंत्रित करती है। भारतीय विधि व्यवस्था मुख्यतः धर्म पर आधारित थी, जिसे ‘धर्मशास्त्र’ कहा जाता है।
विधि के स्रोत:
प्राचीन भारतीय विधि चार प्रमुख स्रोतों पर आधारित थी—
- श्रुति: वेद, उपनिषद, ब्राह्मण आदि ग्रंथ।
- स्मृति: मनु, याज्ञवल्क्य, नारद आदि की स्मृतियाँ।
- आचार: समाज की मान्य परंपराएँ और रीति-रिवाज।
- स्वाभाविक धर्म: न्याय, तर्क और समयानुसार विकसित नियम।
विधि का वर्गीकरण:
प्राचीन भारतीय कानून को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया गया है—
- धर्म (Religious Law): यह विधि धार्मिक कर्तव्यों और नियमों से संबंधित थी जैसे पूजा-पाठ, यज्ञ, व्रत आदि।
- आचार (Moral Code): इसमें नैतिक आचरण, शील, सदाचार, समाज में सद्व्यवहार शामिल थे।
- व्यवहार (Civil Law): इस विधि के अंतर्गत दायित्व, ऋण, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, स्त्रीधन आदि विषय आते थे।
- प्रायश्चित्त (Criminal Law and Penalty): यह विधि अपराध, दंड और प्रायश्चित्त से संबंधित थी।
न्याय का आधार:
विधि का निर्णय धर्मशास्त्र, समाज की परंपरा, साक्ष्य और राजा की आज्ञा पर आधारित होता था। न्यायालयों द्वारा इन विधियों की व्याख्या और पालन कराया जाता था।
विशेषताएँ:
विधि धर्म और नैतिकता से जुड़ी थी।
इसमें व्यक्ति और समाज दोनों की भलाई का विचार था।
शूद्रों और स्त्रियों को विधि में सीमित अधिकार दिए गए थे।
राजा विधि का पालक और न्यायदाता माना गया।
प्राचीन भारत की विधि प्रणाली समाज की संरचना और धार्मिक मूल्यों पर आधारित थी। विधि केवल दंड देने का उपकरण नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और धर्म की रक्षा का माध्यम थी। आज भी कई भारतीय विधियाँ इन्हीं परंपराओं पर आधारित हैं।
प्रश्न-8. प्राचीन भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- प्रश्न 3 सेक्शन स
प्रश्न10.
उत्तर:-
प्रश्न-9.
उत्तर:-
vmou MAHI-05 paper , vmou MA final year exam paper , vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4