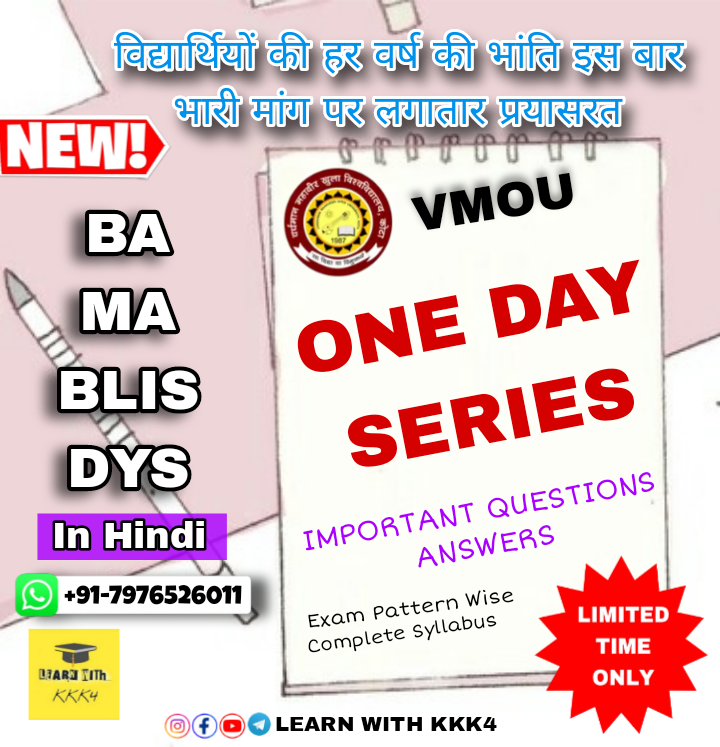VMOU MAGE-01 Paper MA Geography 1st Year (semester-I & II) ; vmou exam paper
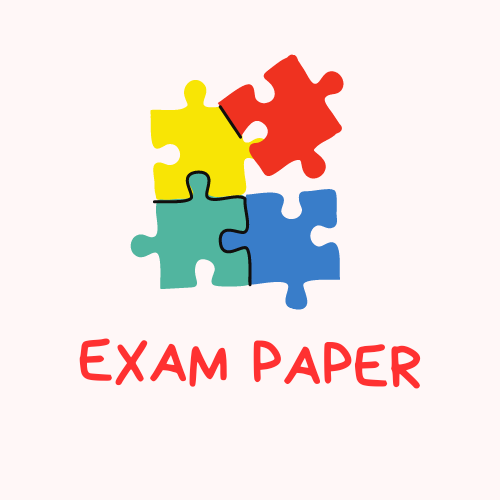
VMOU MA 1st Year के लिए भूगोल ( MAGE-01 , ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.Physical Landscape (भौतिक भूदृश्य)
उत्तर:- पृथ्वी की प्राकृतिक सतह जैसे पर्वत, नदियाँ, पठार आदि को भौतिक भूदृश्य कहा जाता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.Cultural Landscape (सांस्कृतिक भूदृश्य)
उत्तर:- यह मानव द्वारा निर्मित भौगोलिक परिदृश्य है जो संस्कृति की छाप को दर्शाता है
प्रश्न-3.Commercial Geography (वाणिज्य भूगोल)
उत्तर:- यह भूगोल की वह शाखा है जो व्यापार, उत्पादन और वितरण की भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन करती है।
प्रश्न-4. Spatial Analysis – स्थानिक विश्लेषण
उत्तर:- स्थानिक विश्लेषण भूगोल में किसी घटना या प्रक्रिया के स्थान, वितरण और आपसी संबंधों का अध्ययन है।
प्रश्न-5. Contribution of Roman Geographers रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान
उत्तर:- रोमन भूगोलवेत्ताओं ने व्यावहारिक भूगोल को बढ़ावा दिया और सैन्य तथा प्रशासनिक दृष्टि से मानचित्रण को विकसित किया।
प्रश्न-6. Contribution of Eratosthenes – इराटोस्थनीज का योगदान
उत्तर:-इराटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि का मापन किया और ‘भूगोल’ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया।
प्रश्न-7. Environmental-Determinism (वातावरण-निश्चयवाद)
उत्तर:- यह सिद्धांत मानता है कि मानव जीवन और गतिविधियाँ पूरी तरह से पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं।
प्रश्न-8. Principle of Terrestrial Unity (पार्थिव एकता का सिद्धान्त)
उत्तर:- यह सिद्धान्त पृथ्वी के सभी भागों में एक अंतर्संबंध और पारस्परिक प्रभाव को मान्यता देता है।
प्रश्न-9. Systematic Geography क्रमबद्ध भूगोल
उत्तर:-यह भूगोल की वह शाखा है जिसमें किसी विशेष तत्व (जैसे जलवायु, वनस्पति, कृषि) का पृथ्वी पर क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है।
प्रश्न-10. Oribis Terrarum (T in O) Map – ऑरभिस टेरारम (टी इन ओ) मानचित्र
उत्तर:- ऑरभिस टेरारम मानचित्र मध्यकालीन ईसाई मानचित्र था जिसमें पृथ्वी को ‘T’ और ‘O’ के रूप में चित्रित किया गया।
प्रश्न-11. British Geographers ब्रिटिश भूगोलवेत्ता
उत्तर:-ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने उपनिवेशवादी नीति के तहत खोज यात्रा, मानचित्र निर्माण एवं क्षेत्रीय भूगोल को बढ़ावा दिया।
प्रश्न-12. Political Geography राजनीतिक भूगोल
उत्तर:- यह भूगोल की वह शाखा है जो राजनीतिक इकाइयों जैसे राष्ट्र, सीमाएँ, और सत्ता वितरण का अध्ययन करती है।
प्रश्न-13. Applied Geography व्यावहारिक भूगोल
उत्तर:- यह भूगोल की वह शाखा है जो भौगोलिक ज्ञान का प्रयोग व्यावहारिक समस्याओं जैसे नगरीकरण, परिवहन, योजना आदि में करता है।
प्रश्न-14. Scientific Geography वैज्ञानिक भूगोल
उत्तर:- यह भूगोल का वह रूप है जो वैज्ञानिक विधियों, मापन, विश्लेषण तथा तथ्यों पर आधारित होता है।
प्रश्न-15. Marco Polo’s contribution in Renaissance – पुनर्जागरणकाल में मार्को पोलो का योगदान
उत्तर:- मार्को पोलो की यात्राओं ने यूरोप को एशिया की समृद्ध संस्कृति और व्यापार से परिचित कराया, जिससे पुनर्जागरण को प्रेरणा मिली।
प्रश्न-16. Dark Age अंध युग
उत्तर:- यह यूरोप का वह काल था जब भौगोलिक ज्ञान में गिरावट आई और वैज्ञानिक सोच का अभाव था (लगभग 5वीं से 15वीं सदी तक)।
प्रश्न-17. New Determinism – नव निश्चयवाद
उत्तर:- नव निश्चयवाद मानव और पर्यावरण के बीच द्विपक्षीय संबंध को मान्यता देता है, जहाँ मानव पर्यावरण को नियंत्रित भी कर सकता है।
प्रश्न-18. Region (प्रदेश)
उत्तर:- प्रदेश एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो भौतिक, सांस्कृतिक या आर्थिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया जाता है।
प्रश्न-19. पुराणों में जम्बूद्वीप
उत्तर:-पुराणों में जम्बूद्वीप को पृथ्वी का केन्द्रीय द्वीप माना गया है जहाँ मानव सभ्यता का केंद्र बताया गया है।
प्रश्न-20. Author of Cosmos (कॉसमीस के लेखक)
उत्तर:-कॉसमीस’ पुस्तक के लेखक अलेक्ज़ेंडर वॉन हम्बोल्ट (Alexander von Humboldt) थे।
प्रश्न-21. American Geographers अमेरिकी भूगोलवेत्ता
उत्तर:-अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल, पर्यावरणीय निर्धारणवाद तथा सांस्कृतिक भूगोल को विशेष रूप से विकसित किया।
प्रश्न-22. Areal Differentiation (क्षेत्रीय भिन्नता):
उत्तर:- यह भूगोल की वह संकल्पना है जो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं के अंतर को स्पष्ट करती है।
प्रश्न-23. Erdkunde – एर्डकुंडे
उत्तर:- एर्डकुंडे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर की अवधारणा है जिसमें भूगोल को पृथ्वी और मानव के परस्पर संबंधों का अध्ययन माना गया।
प्रश्न-24. Lebensraum (लेवेन्सराऊम)
उत्तर:- यह एक जर्मन अवधारणा है जिसका अर्थ है “जीवन के लिए स्थान”, जो भौगोलिक विस्तार की नीति को दर्शाती है।
प्रश्न-25. Systematic Geography – क्रमबद्ध भूगोल
उत्तर:- क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक भौगोलिक तत्व (जैसे जलवायु, कृषि) का विश्व स्तर पर विश्लेषण किया जाता है।
प्रश्न-26. Human Ecology (मानव पारिस्थितिकी):
उत्तर:- यह अध्ययन करता है कि मनुष्य और उसका पर्यावरण कैसे पारस्परिक रूप से एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।
प्रश्न-27. कासिमसि क्या है?
उत्तर:- Cosmos अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें प्राकृतिक और भौगोलिक घटनाओं का वैज्ञानिक विवरण है।
प्रश्न-28. आचारण भूगोल की परिभाषा दीजिए।
उत्तर:- आचारण भूगोल वह शाखा है जो मानव व्यवहार और उसके पर्यावरणीय निर्णयों का अध्ययन करती है।
प्रश्न-29. मानव भूगोल (Anthropogeography) क्या है?
उत्तर:-मानव भूगोल वह अध्ययन है जो मानव जाति के भौगोलिक वितरण और गतिविधियों का विश्लेषण करता है।
प्रश्न-30. Humanism (मानववाद):
उत्तर:- यह दृष्टिकोण भूगोल में मानवीय अनुभव, मूल्य और अभिप्राय को केंद्र में रखता है।
प्रश्न-31. कांट का भूगोल में क्या योगदान है?
उत्तर:- इमैन्युल कांट ने भूगोल को समकालीन घटनाओं का विज्ञान माना और उसे स्थानिक अध्ययन के रूप में स्थापित किया।
प्रश्न-32. Regional Planning (प्रादेशिक नियोजन):
उत्तर:- यह किसी क्षेत्र के संसाधनों, आवास, उद्योग व परिवहन के संतुलित विकास हेतु योजनाबद्ध प्रक्रिया है।
प्रश्न-33. सम्भवाद को समझाइए।
उत्तर:-सम्भवाद वह विचारधारा है जो मानती है कि मानव अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखकर विकास की संभावनाएं उत्पन्न कर सकता है।
प्रश्न-34. स्थान और काल किसे कहते हैं?
उत्तर:- स्थान भौगोलिक क्षेत्र है जहां घटनाएं घटित होती हैं और काल वह समय है जिसमें वे घटनाएं घटती हैं।
प्रश्न-35. हम्बोल्ट का योगदान क्या है?
उत्तर:- हम्बोल्ट ने आधुनिक भौतिक भूगोल की नींव रखी और प्रकृति को एकीकृत रूप में समझने का प्रयास किया।
प्रश्न-36. कालं ओ सावर कौन थे?
उत्तर:- कार्ल ओ. सावर एक अमेरिकी सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने सांस्कृतिक परिदृश्य की संकल्पना दी।
Section-B
प्रश्न-1.भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- भूगोल एक समग्र विषय है जो पृथ्वी की सतह पर स्थित प्राकृतिक और मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति द्वैतात्मक है – यह एक ओर भौतिक विज्ञानों से जुड़ता है जैसे भूविज्ञान, मौसम विज्ञान आदि, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञानों से भी जुड़ा है, जैसे समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि। भूगोल मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है – भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल।
भूगोल की प्रमुख विशेषता उसका स्थानिक दृष्टिकोण है, जिसमें किसी घटना या तत्व का स्थान, वितरण तथा पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण किया जाता है। यह विज्ञानात्मक विश्लेषण के साथ-साथ दार्शनिक दृष्टिकोण को भी अपनाता है, जिससे यह एक अंतर्विषयक विषय बन जाता है। भूगोल प्राकृतिक और मानव क्रियाओं के बीच संबंधों को समझने का प्रयास करता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का समन्वय विज्ञान भी कहा जाता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.टॉलेमी का भूगोल में योगदान स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- टॉलेमी (Claudius Ptolemy) एक ग्रीक विद्वान था जिसने दूसरी शताब्दी ईस्वी में भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी प्रसिद्ध कृति ‘Geographia’ आठ खंडों में थी, जिसमें उसने पृथ्वी की सतह का वर्णन, मानचित्र निर्माण की विधियाँ और स्थानों के निर्देशांक (Latitude और Longitude) दिए। उसने लगभग 8000 स्थानों के निर्देशांक प्रस्तुत किए जिससे मानचित्रण कार्य में क्रांति आई।
टॉलेमी ने भूमध्य रेखा और प्रधान देशांतर रेखा का उपयोग करते हुए स्थान निर्धारण की प्रणाली विकसित की। उसने ‘कॉनिक प्रोजेक्शन’ (Conic Projection) का प्रयोग किया जो मानचित्र बनाने में उपयोगी सिद्ध हुआ। भले ही उसकी कई गणनाएँ गलत सिद्ध हुईं, परंतु उसकी विधियाँ सदियों तक मानचित्रकारों द्वारा उपयोग की जाती रहीं।
इस प्रकार टॉलेमी ने भूगोल को गणितीय आधार प्रदान किया और उसे एक संगठित विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया।
प्रश्न-3. डब्ल्यू. एम. डेविस के भूगोल में योगदान को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- डब्ल्यू.एम. डेविस (William Morris Davis) एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जिन्हें ‘भू-आकृतिक विज्ञान का जनक’ (Father of Geomorphology) कहा जाता है। उन्होंने स्थलरूपों के विकास को समझने के लिए ‘स्थलरूप चक्र सिद्धांत’ (Cycle of Erosion Theory) प्रस्तुत किया।
इस सिद्धांत के अनुसार स्थलरूपों का विकास तीन अवस्थाओं में होता है – प्रारंभिक (Youth), मध्य (Mature) और वृद्धावस्था (Old Age)। प्रत्येक अवस्था में स्थलरूप की विशेषताएँ भिन्न होती हैं।
डेविस ने भौतिक भूगोल को एक वैज्ञानिक आधार दिया और स्थलरूपों के अध्ययन में समय और प्रक्रिया की भूमिका को महत्व दिया। उनका मॉडल प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।
हालांकि, बाद में कुछ भूगोलवेत्ताओं ने उनके मॉडल की आलोचना भी की क्योंकि यह अत्यधिक सामान्यीकृत था और जलवायु व संरचना की विविधता को कम महत्व देता था। फिर भी डेविस का योगदान भूगोल को वैज्ञानिक बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।
प्रश्न-पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भूगोलवेत्ताओं का भौगोलिक विचारधाराओं में योगदान को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को एक सामाजिक-आर्थिक विज्ञान के रूप में विकसित किया। उन्होंने भौगोलिक अध्ययन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) की विचारधारा को अपनाया और भूगोल को समाज, अर्थव्यवस्था और प्रकृति के आपसी संबंधों के अध्ययन का माध्यम माना।
सोवियत भूगोलवेत्ताओं जैसे वी.वी. डोकोउचाएव ने मृदा विज्ञान की आधारशिला रखी और मृदा निर्माण में जलवायु, जैविक तत्वों और स्थलाकृति की भूमिका को उजागर किया। एन.एन. बरांस्की ने आर्थिक भूगोल में क्षेत्रीय योजना और उत्पादन संरचना पर जोर दिया।
सोवियत भूगोल में मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को सामाजिक दृष्टिकोण से देखा गया। उन्होंने बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय योजना (Regional Planning) और संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया।
इस प्रकार सोवियत भूगोल ने भौगोलिक अध्ययन को सामाजिक संदर्भ में विस्तारित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।
प्रश्न-5.भारत में आधुनिक भूगोल के विकास पर विस्तार से वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भारत में आधुनिक भूगोल का विकास औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के आगमन के साथ हुआ। प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारत की भौगोलिक जानकारी के लिए सर्वेक्षण (Survey) कार्य किए। 1767 में स्थापित “सर्वे ऑफ इंडिया” ने आधुनिक मानचित्रण की नींव रखी।
स्वतंत्रता के बाद भारतीय विश्वविद्यालयों में भूगोल एक शैक्षणिक विषय के रूप में उभरा। प्रो. एस.पी. चटर्जी, प्रो. राधाकृष्णन, प्रो. वासुदेवन जैसे विद्वानों ने भारतीय भूगोल को नई दिशा दी। भूगोल में क्षेत्रीय योजना, संसाधन प्रबंधन, पर्यावरणीय अध्ययन, नगरीकरण, और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों का समावेश हुआ।
1970 के बाद से भूगोल में मात्रात्मक पद्धति, सैटेलाइट इमेजरी, और GIS तकनीक का उपयोग बढ़ा, जिससे इसका स्वरूप अधिक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक हो गया। वर्तमान में भारत में भूगोल का अध्ययन न केवल शैक्षणिक बल्कि प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है।
प्रश्न-6.भूगोल में ‘डेविस’ के योगदान को समझाइए।
उत्तर:- विलियम मॉरिस डेविस (W.M. Davis) अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भू-आकृतिक अध्ययन (Geomorphology) के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत “स्थलाकृति चक्र” (Cycle of Erosion) है, जिसे “डेविसियन मॉडल” भी कहा जाता है।
उन्होंने बताया कि स्थलाकृति का विकास तीन चरणों में होता है—प्रारंभिक (Youth), मध्य (Maturity), और वृद्धावस्था (Old age)। इन चरणों के अनुसार नदी घाटियों, पर्वतों और मैदानों का विकास होता है। यह एक कालानुक्रमिक प्रक्रिया है जो उन्नयन और अपरदन के संतुलन पर आधारित है।
डेविस ने स्थलाकृति को भूगोल का केंद्रीय विषय माना और इस क्षेत्र में भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने प्रकृति के क्रमिक परिवर्तन की अवधारणा दी और इससे भूगोल में प्रक्रिया और समय का महत्त्व स्थापित हुआ।
यद्यपि उनके मॉडल की आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने आलोचना की, फिर भी उनका योगदान स्थलाकृति विज्ञान को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित करने में अहम रहा।
प्रश्न-7.”भौतिक एवं मानव भूगोल का द्वैतवाद मिथ्या है।” स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- भौतिक भूगोल प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, नदियाँ, जलवायु आदि का अध्ययन करता है जबकि मानव भूगोल मानव गतिविधियों, बस्तियों, जनसंख्या, संस्कृति आदि पर केंद्रित होता है। परंतु इन दोनों शाखाओं का पृथक् अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मानव सदैव प्राकृतिक वातावरण में ही क्रियाशील रहता है।
आधुनिक भूगोल में यह स्वीकार किया गया है कि मानव और प्रकृति में पारस्परिक संबंध है। उदाहरण के लिए, कृषि, उद्योग और बस्तियाँ पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, जबकि मानव द्वारा पर्यावरण पर भी प्रभाव डाला जाता है।
इसलिए यह कहना कि भौतिक और मानव भूगोल दो स्वतंत्र विषय हैं, पूर्णतः सत्य नहीं है। वर्तमान में एकीकृत भूगोल (Integrated Geography) की धारणा को महत्व दिया जा रहा है जिसमें भौतिक और मानव घटकों का समन्वित अध्ययन किया जाता है।
इस प्रकार द्वैतवाद की अवधारणा अब अप्रासंगिक हो गई है और समग्र दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है।
प्रश्न-8.फ्रेडरिक रेटजेल का भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान है ?
उत्तर:- फ्रेडरिक रेटजेल (Friedrich Ratzel) जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल और राजनीतिक भूगोल का जनक माना जाता है। उन्होंने भूगोल में ‘वातावरण निश्चयवाद’ (Environmental Determinism) की अवधारणा को विकसित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि मानव जीवन और गतिविधियाँ मुख्यतः भौतिक पर्यावरण, विशेष रूप से जलवायु, स्थलरूप और संसाधनों पर निर्भर करती हैं।
रेटजेल का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत “जीवित राज्य” (Organic Theory of State) है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रों की तुलना जीवित जीवों से की। उन्होंने “Leibensraum” (जीवन क्षेत्र) की संकल्पना दी, जिसके अनुसार राष्ट्रों को जीवित रहने के लिए विस्तार करना आवश्यक होता है। यह विचार बाद में जर्मन राजनीति में विवादास्पद रूप में प्रयुक्त हुआ।
उनकी रचनाएँ जैसे “Anthropogeographie” ने मानव भूगोल के विकास में दिशा प्रदान की। उनका कार्य भूगोल को एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक अनुशासन बनाने में महत्त्वपूर्ण रहा।
प्रश्न-9. इमैन्युल कान्ट का भूगोल में योगदान बताइए।
उत्तर:- इमैन्युल कान्ट (Immanuel Kant) एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी में भूगोल को दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने भूगोल को ‘स्थानिक विज्ञान’ (Spatial Science) की संज्ञा दी और इसे अन्य विज्ञानों से पृथक पहचान दी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भूगोल का मुख्य कार्य पृथ्वी की सतही घटनाओं का स्थान और वितरण के आधार पर अध्ययन करना है।
कान्ट ने भूगोल को चार भागों में विभाजित किया – भौतिक भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और धार्मिक भूगोल। उन्होंने शिक्षा में भूगोल को आवश्यक विषय माना और इसे ऐतिहासिक ज्ञान का पूरक बताया। उनका यह दृष्टिकोण कि भूगोल वस्तुओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है, आज भी अत्यंत प्रासंगिक है।
कान्ट के विचारों ने आधुनिक भूगोल को दिशा दी और भूगोल को एक तर्कसंगत और व्यवस्थित विज्ञान के रूप में स्थापित किया।
प्रश्न-10. विडाल डी ला ब्लाष का भूगोल में योगदान का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- विडाल डी ला ब्लाष (Vidal De La Blache) फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे जिन्हें “संभाव्यवाद” (Possibilism) के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि मनुष्य केवल पर्यावरण का दास नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि और तकनीक से पर्यावरण को अनुकूल बना सकता है।
उनकी प्रमुख रचना “Principes de Géographie Humaine” में उन्होंने मानव भूगोल को एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक दिशा दी। उन्होंने ‘पैसाज़’ (Paysage) या ‘सांस्कृतिक परिदृश्य’ की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रत्येक क्षेत्र का भूगोल वहाँ के मानव और पर्यावरण की संयुक्त अभिव्यक्ति है।
विडाल का कार्य फ्रांसीसी भूगोल की परंपरा को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण रहा। उन्होंने भूगोल को केवल प्राकृतिक तत्वों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसमें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक पहलुओं को भी जोड़ा।
प्रश्न-11. मानव पारिस्थितिकी क्या है ?
उत्तर:- मानव पारिस्थितिकी (Human Ecology) वह अध्ययन क्षेत्र है जो मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों को विश्लेषित करता है। इसमें देखा जाता है कि किस प्रकार मानवीय गतिविधियाँ पर्यावरण को प्रभावित करती हैं और कैसे पर्यावरण मानवीय जीवन को आकार देता है।
यह शाखा समाजशास्त्र, भूगोल, पर्यावरण विज्ञान और मानवशास्त्र जैसे विषयों से जुड़ती है। मानव पारिस्थितिकी में आवास, भूमि उपयोग, संसाधनों का दोहन, प्रदूषण, जनसंख्या वितरण, और जैव विविधता के संरक्षण जैसे मुद्दों का अध्ययन किया जाता है।
इस विचारधारा की शुरुआत शिकागो स्कूल द्वारा की गई, जहां यह देखा गया कि शहरीकरण, औद्योगीकरण और जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण और सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज यह पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने और सतत विकास की योजनाएँ बनाने में सहायक है।
प्रश्न-12. भूगोल में अतिवाद की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- भूगोल में अतिवाद (Radicalism) का उदय 1970 के दशक में हुआ। यह आंदोलन पारंपरिक और मात्रात्मक भूगोल के विरोध में था क्योंकि वे सामाजिक असमानता, गरीबी, और शोषण जैसे मुद्दों की अनदेखी कर रहे थे। अतिवादी भूगोल ने भूगोल के सामाजिक न्याय और राजनीतिक पक्ष पर ज़ोर दिया।
इसका मूल आधार मार्क्सवादी विचारधारा था, जिसमें समाज में वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी शोषण की व्याख्या की गई। अतिवादी भूगोलवेत्ताओं जैसे डेविड हार्वी ने स्थान, समाज और सत्ता के बीच संबंध को उजागर किया। वे मानते थे कि केवल स्थानिक वितरण को समझना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं को भी समझना आवश्यक है।
अतिवाद ने भूगोल को सामाजिक विज्ञानों से जोड़ने में सहायता की और इसे अधिक मानवीय और क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रदान किया। यद्यपि यह दृष्टिकोण सभी भूगोलवेत्ताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, परंतु इसने भूगोल में एक नई बहस और विमर्श को जन्म दिया।
प्रश्न-13. पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए तथा इसके विकास पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- पर्यावरण निश्चयवाद (Environmental Determinism) वह विचारधारा है जिसके अनुसार मानव जीवन, संस्कृति और विकास मुख्य रूप से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। इसके अनुसार जलवायु, स्थलरूप, मृदा, वनस्पति आदि मानव व्यवहार और समाज के स्वरूप को निर्धारित करते हैं।
इस विचारधारा की शुरुआत ग्रीक दार्शनिकों जैसे हिप्पोक्रेट्स और अरस्तू से हुई। आधुनिक युग में फ्रेडरिक रैटजेल और एलन हंटिंग्टन ने इसे और विस्तृत रूप दिया। हंटिंग्टन ने जलवायु को मानव सभ्यता के विकास का मूल कारण माना।
हालांकि, बीसवीं शताब्दी के मध्य में इस सिद्धांत की आलोचना हुई क्योंकि इसने मानव की सक्रिय भूमिका को नकार दिया। इसके बाद संभाव्यवाद (Possibilism) का उदय हुआ जिसने कहा कि मानव पर्यावरण की सीमाओं में रहते हुए भी विकास कर सकता है।
इस प्रकार पर्यावरण निश्चयवाद ने प्रारंभिक भूगोलीय चिंतन को दिशा दी, परंतु समय के साथ इसका स्थान अधिक संतुलित दृष्टिकोणों ने ले लिया।
प्रश्न-14. भूगोल पर मात्रात्मक क्रान्ति के प्रभाव की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- मात्रात्मक क्रांति (Quantitative Revolution) 1950-60 के दशक में भूगोल में हुई एक प्रमुख परिवर्तन थी, जिसमें सांख्यिकीय तकनीकों और गणितीय मॉडलों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य भूगोल को एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाना था।
इस क्रांति ने भूगोल को अधिक विश्लेषणात्मक, वस्तुनिष्ठ और मापनक्षम बनाया। इसमें स्थानिक वितरण, प्रवृत्तियों, दूरी, और क्षेत्रीय विश्लेषण में मापन तकनीकों का उपयोग बढ़ा। कंप्यूटर और GIS तकनीकों के उपयोग से आंकड़ों का विश्लेषण संभव हुआ।
इस क्रांति के कारण व्यवहारवादी भूगोल, स्थानिक संगठन के सिद्धांत, मॉडल-निर्माण, और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाएं भूगोल का हिस्सा बनीं। इससे भूगोल की सामाजिक स्वीकार्यता और व्यावहारिक उपयोगिता में वृद्धि हुई।
हालांकि, इसकी आलोचना भी हुई क्योंकि इसने मानवीय पक्षों, सामाजिक न्याय और अनुभवजन्य पहलुओं को नजरअंदाज किया। फिर भी, मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल को एक आधुनिक, व्यावसायिक और नीति-निर्धारण में उपयोगी विषय बना दिया।
प्रश्न-15. भूगोल की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भूगोल एक समग्र विज्ञान है जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं एवं मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति द्वैतात्मक है, जिसमें भौतिक (प्राकृतिक) और मानव (सामाजिक) दोनों घटक शामिल होते हैं। यह विज्ञान-आधारित, अनुभवजन्य तथा विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति रखता है। भूगोल समय और स्थान की दृष्टि से घटनाओं की व्याख्या करता है।
भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यह स्थलाकृतिक संरचनाओं, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जल संसाधनों, जनसंख्या, नगरों, उद्योगों, परिवहन, सांस्कृतिक विविधता आदि का अध्ययन करता है। भूगोल को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है: भौतिक भूगोल (Physical Geography) और मानव भूगोल (Human Geography)। इसके अतिरिक्त पर्यावरण भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल जैसे उपविषय भी विकसित हुए हैं। भूगोल का उपयोग क्षेत्रीय योजना, आपदा प्रबंधन, पर्यावरणीय संरक्षण, और सतत विकास में किया जाता है।
प्रश्न-16. जर्मन भूगोलवेताओं के योगदान का ब्यौरा दीजिए।
उत्तर:- जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने आधुनिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे विश्लेषणात्मक पद्धति, क्षेत्रीय अध्ययन और भू-निर्धारण सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- अलेक्जेंडर वॉन हंबोल्ट: इन्हें आधुनिक भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। इन्होंने प्रकृति को एकीकृत रूप में देखने का दृष्टिकोण दिया और पर्यावरणीय संबंधों पर बल दिया।
- कार्ल रिटर: इन्होंने मानव भूगोल की नींव रखी और स्थानिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझाया।
- फ्रेडरिक रेटजेल: इन्होंने “Anthropogeography” की संकल्पना दी और राजनीतिक भूगोल में ‘लेबेन्सराऊम’ का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
- अल्फ्रेड हेत्तनर: इन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान के रूप में परिभाषित किया और “कोरोलॉजिकल” (स्थानिक संबंधों) दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया।
- वाल्टर क्रेन्स: इन्होंने मानव भूगोल में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को जोड़ा।
जर्मन भूगोल विचारशील, सैद्धांतिक और क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित है।
प्रश्न-17. भूगोल अंतरा अनुशासनिक विज्ञान है। स्पष्ट कीजिए
उत्तर:- भूगोल एक अंतर्विषयी (Interdisciplinary) विज्ञान है क्योंकि यह अनेक विषयों से जुड़कर उनके तत्वों को समाहित करता है। यह न केवल भौतिक विज्ञान (जैसे- भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान) बल्कि समाज विज्ञान (जैसे- समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र) से भी संबंध रखता है।
भौतिक भूगोल में पर्यावरण, जलवायु, वनस्पति, और स्थलरूपों का अध्ययन होता है, जबकि मानव भूगोल में जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और नगर नियोजन आदि का विश्लेषण होता है। यह तकनीकी विषयों जैसे- GIS, सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग के साथ भी समन्वय करता है।
उदाहरणस्वरूप, पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, या संसाधन प्रबंधन को समझने के लिए हमें भूगोल के साथ-साथ पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का भी सहारा लेना पड़ता है।
इस प्रकार, भूगोल एक सेतु की भूमिका निभाता है, जो भौतिक और सामाजिक विज्ञानों को जोड़ता है। यही कारण है कि भूगोल को एक समन्वयात्मक और बहु-विषयी विज्ञान माना जाता है।
प्रश्न-18. प्रादेशिक नियोजन के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- प्रादेशिक नियोजन (Regional Planning) का उद्देश्य किसी क्षेत्र के संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना होता है। यह नियोजन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है:
- राष्ट्रीय स्तर (National Level): इसमें पूरे देश के विकास की रणनीति बनाई जाती है। जैसे भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ।
- राज्य/प्रांतीय स्तर (State Level): इसमें किसी राज्य की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ बनाई जाती हैं।
- जिला स्तर (District Level): यहाँ पर योजनाओं को अधिक स्थानीय जरूरतों के अनुसार लागू किया जाता है।
- स्थानीय स्तर (Local Level): गाँव, नगर और क्षेत्रीय पंचायतों में विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।
- कार्यात्मक क्षेत्रीय स्तर (Functional Region): यहाँ आर्थिक या औद्योगिक क्षेत्रों जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), औद्योगिक बेल्ट आदि पर ध्यान दिया जाता है।
इस प्रकार प्रादेशिक नियोजन बहु-स्तरीय प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर तक विकास को समन्वित करती है।
प्रश्न-19. यथार्थवाद क्या है ?
उत्तर:- यथार्थवाद (Realism) एक दार्शनिक और साहित्यिक सिद्धांत है जो वस्तुनिष्ठ और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। यह विश्वास करता है कि दुनिया जैसी है, वैसी ही उसे देखा और समझा जाना चाहिए, न कि कल्पनाओं या आदर्शों के माध्यम से।
भूगोल में यथार्थवाद का अर्थ है – स्थलों, स्थानों और पर्यावरणीय घटनाओं का अध्ययन तथ्यात्मक, प्रत्यक्ष अनुभव और आंकड़ों के आधार पर करना। यह सिद्धांत भू-राजनीति में भी प्रयोग होता है, जहाँ यह माना जाता है कि राष्ट्र अपने हितों की रक्षा के लिए व्यावहारिक निर्णय लेते हैं, नैतिकता या आदर्शवाद के आधार पर नहीं।
यथार्थवाद ज्ञान, निर्णय और क्रिया में वास्तविकता की प्राथमिकता को स्वीकार करता है और भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रस्तुत करता है।
प्रश्न-20. भूगोल की प्रकृति में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- भूगोल एक गतिशील विषय है जिसकी प्रकृति समय के साथ बदलती रही है। प्रारंभ में यह विषय वर्णनात्मक था और स्थलों का विवरण मात्र प्रदान करता था। प्राचीन काल में यह धार्मिक और खगोलीय दृष्टिकोण से जुड़ा था। मध्यकाल में भूगोल यात्रा वृत्तांतों पर आधारित रहा। आधुनिक युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने इसे एक विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विषय बना दिया।
बीसवीं शताब्दी में “मात्रात्मक क्रांति” (Quantitative Revolution) के कारण भूगोल में सांख्यिकीय विधियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। इसके बाद “मानववादी भूगोल”, “अतिवादी भूगोल” और “नारीवादी भूगोल” जैसे नए दृष्टिकोण उभरकर सामने आए। आज भूगोल एक अंतर्विषयी (Interdisciplinary) विज्ञान बन चुका है जो पर्यावरण, समाज, अर्थशास्त्र, राजनीति, और तकनीक से जुड़ा हुआ है।
इस प्रकार, भूगोल की प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील रही है, जो समय, स्थान और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होती रही है।
प्रश्न-21. ‘हृदय स्थल सिद्धान्त’ पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:-‘हृदय स्थल सिद्धांत’ (Heartland Theory) को ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हॉफर्ड मैकिंडर (Halford Mackinder) ने 1904 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार, विश्व राजनीति में शक्ति का नियंत्रण उस क्षेत्र के पास रहेगा जो यूरेशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग – जिसे हृदय स्थल (Heartland) कहा गया – पर नियंत्रण रखता है।
मैकिंडर ने कहा – “जो कोई पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण करेगा, वह हृदय स्थल पर नियंत्रण करेगा; जो हृदय स्थल पर नियंत्रण करेगा, वह विश्व द्वीप (यूरेशिया + अफ्रीका) पर शासन करेगा; और जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा, वह संपूर्ण विश्व पर शासन करेगा।”
यह सिद्धांत भू-राजनीति (Geopolitics) का आधार बना और द्वितीय विश्व युद्ध तथा शीत युद्ध की रणनीतियों को प्रभावित किया। हालांकि आज यह पूर्णतः लागू नहीं होता, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व है और यह बताता है कि कैसे भौगोलिक स्थिति, वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है।
प्रश्न-22. महत्वपूर्ण फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के योगदान का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल में मानववादी दृष्टिकोण, क्षेत्रीय विश्लेषण और सांस्कृतिक भूगोल का विकास किया।
- पॉल विदाल डी ला ब्लाश: इन्होंने ‘संभाव्यवाद’ (Possibilism) का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने ‘मानव भूगोल’ के संस्थापक के रूप में योगदान दिया और “Paysage” (भूदृश्य) पर विशेष बल दिया।
- जीन ब्रुनेस: इन्होंने समुद्री भूगोल (Maritime Geography) में योगदान दिया और भू-राजनीतिक अध्ययन को बढ़ावा दिया।
- एलीजे रेइक्लूस: इन्होंने सामाजिक भूगोल की नींव रखी और भूगोल को जनता के उपयोग के योग्य बनाने की बात की।
- एम. डे मार्टोन: इन्होंने भौतिक भूगोल, विशेषकर भू-आकृतिक अध्ययन में उल्लेखनीय कार्य किया।
फ्रांसीसी भूगोल की प्रमुख विशेषता यह है कि यह मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंध को संतुलित रूप से देखता है और क्षेत्रीय विश्लेषण को महत्त्व देता है।
प्रश्न-23. भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर:- भूगोल का वैज्ञानिक पक्ष यह है कि यह प्राकृतिक घटनाओं और मानव गतिविधियों का विश्लेषण तथ्यों, आंकड़ों, अवलोकन और मानचित्रों के माध्यम से करता है। इसमें स्थानिक वितरण, पृथ्वी की संरचना, जलवायु परिवर्तन, संसाधन वितरण आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। GIS, रिमोट सेंसिंग, GPS जैसी आधुनिक तकनीकें इसका वैज्ञानिक आधार मजबूत बनाती हैं।
वहीं भूगोल का दार्शनिक पक्ष यह है कि यह मानव और प्रकृति के संबंधों को गहराई से समझने का प्रयास करता है। यह विचार करता है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच कैसा अंतःसंबंध है, मनुष्य किस हद तक स्वतंत्र है और पर्यावरण किस हद तक निर्धारक है। इसके दर्शन में निश्चयवाद, संभववाद, यथार्थवाद, नव-निर्धारणवाद आदि सिद्धांत सम्मिलित हैं।
इस प्रकार भूगोल न केवल एक विज्ञान है, बल्कि एक विचारधारा और दृष्टिकोण भी है जो हमें अपने स्थान और पर्यावरण को बेहतर समझने में सहायक होता है।
प्रश्न-24. भौगोलिक अध्ययन में नूतन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- आधुनिक भूगोल में कई नूतन प्रवृत्तियाँ उभरी हैं जिन्होंने अध्ययन की दिशा और पद्धति को बदल दिया है:
- तकनीकी प्रवृत्तियाँ: GIS (Geographic Information System), रिमोट सेंसिंग, और GPS जैसी तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इससे भू-स्थानिक डेटा का विश्लेषण सटीकता से किया जा सकता है।
- पर्यावरणीय जागरूकता: जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, जैव विविधता संरक्षण आदि विषयों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
- स्थानीय से वैश्विक स्तर तक अध्ययन: भूगोल अब स्थानीय समस्याओं के साथ-साथ वैश्विक मुद्दों जैसे वैश्वीकरण, शहरीकरण, आप्रवासन आदि का विश्लेषण भी करता है।
- अंतर्विषयक दृष्टिकोण: भूगोल अब समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि से समन्वय करके बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
- लैंगिक और सामाजिक न्याय: नारीवादी भूगोल, सामाजिक न्याय भूगोल जैसे नए उपविषयों का विकास हुआ है।
इस प्रकार भूगोल का क्षेत्र निरंतर विस्तृत और तकनीकी रूप से समृद्ध होता जा रहा है।
प्रश्न-25. भूगोल का शास्त्रीय युग क्या है? वर्णन कीजिए।
उत्तर:-भूगोल का शास्त्रीय युग (Classical Age of Geography) लगभग 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का समय माना जाता है, जिसमें प्राचीन ग्रीक और रोमन विद्वानों ने भूगोल के सिद्धांतों को व्यवस्थित किया। इस युग में भूगोल को दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान और मानचित्रण से जोड़ा गया।
इस युग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- सैद्धांतिक योगदान: हेरोडोटस, हिप्पार्कस, स्ट्रैबो, और टॉलेमी जैसे विद्वानों ने पृथ्वी की आकृति, परिधि, जलवायु क्षेत्र, स्थान निर्धारण आदि पर कार्य किया।
- मानचित्र निर्माण: टॉलेमी ने “गिओग्राफिया” नामक ग्रंथ में अनेक मानचित्रों और स्थान निर्देशांक का उल्लेख किया।
- खगोल एवं गणित से संबंध: भूगोल को गणित और खगोल विज्ञान से जोड़ा गया, जिससे यह एक वैज्ञानिक अनुशासन बना।
- व्यापक दृष्टिकोण: इस काल के भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी को सम्पूर्णता में देखा तथा वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया।
यह युग भूगोल के वैचारिक एवं बौद्धिक विकास की नींव रखने वाला रहा।
प्रश्न-26. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए:
उत्तर:- (a) अल-बेरुनी (Al-Biruni)
अल-बेरुनी (973-1048 ई.) एक प्रसिद्ध अरब विद्वान, खगोलशास्त्री और भूगोलवेत्ता थे। वे महमूद गजनवी के साथ भारत आए और भारतीय संस्कृति, भूगोल और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया। उनकी पुस्तक “तहकीक माले-हिन्द” में भारत के भौगोलिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। उन्होंने धरती की परिधि की माप भी दी थी और मानचित्र निर्माण में योगदान दिया।
(b) क्लाडियस टॉलेमी (Cladius Ptolemy)
क्लाडियस टॉलेमी एक ग्रीक भूगोलवेत्ता और खगोलशास्त्री थे जिन्होंने दूसरी शताब्दी में “गियोग्राफिया” नामक ग्रंथ लिखा। उन्होंने अक्षांश और देशांश की प्रणाली विकसित की, और विश्व का मानचित्र बनाया जिसमें 8000 से अधिक स्थानों का वर्णन था। टॉलेमी की मानचित्र प्रणाली मध्यकालीन यूरोप में मानक बनी रही। उनका योगदान आधुनिक मानचित्रण के विकास की नींव है।
प्रश्न-27. पुनर्जागरण काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- पुनर्जागरण (Renaissance) काल 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में आया एक बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने मध्य युग की रूढ़ियों को तोड़ा और आधुनिक युग की नींव रखी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- मानवतावाद (Humanism): यह काल व्यक्ति की बुद्धि, स्वतंत्रता और गरिमा पर बल देता है। धर्म की बजाय तर्क और अनुभव को प्राथमिकता दी गई।
- विज्ञान और खोज: कोपर्निकस, गैलीलियो, और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड और भौतिक विज्ञान की नई व्याख्याएं दीं।
- कला और साहित्य में उन्नति: लियोनार्दो दा विंची, माइकलएंजेलो जैसे कलाकारों और शेक्सपियर जैसे साहित्यकारों ने रचनात्मकता को नया रूप दिया।
- भूगोल में योगदान: इस काल में वास्को-डी-गामा, कोलंबस आदि द्वारा समुद्री मार्गों की खोज हुई, जिससे नई भूमि और जनसंख्या के अध्ययन में भूगोल समृद्ध हुआ।
- मुद्रण कला का विकास: गुटेनबर्ग की छपाई तकनीक ने ज्ञान के प्रसार को गति दी।
प्रश्न-28. नियतिवाद व संभववाद में क्या अंतर है?
उत्तर:- नियतिवाद (Determinism) और संभववाद (Possibilism) भूगोल के दो प्रमुख सिद्धांत हैं जो मानव और प्रकृति के संबंध को अलग-अलग रूप में व्याख्यायित करते हैं।
- नियतिवाद (Environmental Determinism): यह सिद्धांत मानता है कि मानव जीवन और उसकी गतिविधियाँ पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं। जलवायु, स्थलरूप, मिट्टी, और जल संसाधन मानव के क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। इसका प्रमुख समर्थक फ्रेडरिक रेटजेल था।
- संभववाद (Possibilism): यह सिद्धांत कहता है कि प्रकृति केवल विकल्प प्रदान करती है, लेकिन अंतिम निर्णय मानव लेता है। मानव अपने बौद्धिक विकास से पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है। इसका प्रमुख प्रवर्तक पॉल विदाल डी ला ब्लाश था।
मुख्य अंतर:
नियतिवाद में प्रकृति को सक्रिय और मानव को निष्क्रिय माना गया है।
संभववाद में मानव को सक्रिय और प्रकृति को विकल्पों की प्रदाता माना गया है।
प्रश्न-30. द्वैतवाद क्या है? प्राकृतिक तथा मानव भूगोल का इस संदर्भ में वर्णन कीजिए।
उत्तर:- द्वैतवाद (Dualism) भूगोल में दो विपरीत प्रवृत्तियों या दृष्टिकोणों के सह-अस्तित्व को कहा जाता है। भूगोल में मुख्य द्वैतवाद प्राकृतिक बनाम मानव भूगोल के रूप में देखा जाता है।
- प्राकृतिक भूगोल (Physical Geography): यह पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं जैसे स्थलरूप, जलवायु, नदियाँ, झीलें, मृदा आदि का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करना होता है।
- मानव भूगोल (Human Geography): यह मानव की जनसंख्या, संस्कृति, बस्तियाँ, आर्थिक क्रियाएँ और उनके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन करता है। यह सामाजिक विज्ञानों से अधिक प्रभावित होता है।
द्वैतवाद का महत्व:
द्वैतवाद ने भूगोल में विशेषीकरण को जन्म दिया, जिससे भौतिक और मानव भूगोल के स्वतंत्र उपविषय विकसित हुए। हालांकि, आज का भूगोल एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें दोनों घटकों को परस्पर संबंधित माना जाता है।
प्रश्न-31. आधुनिक भारत में भौगोलिक अध्ययनों पर एक विस्तृत नोट लिखिए।
उत्तर:- आधुनिक भारत में भूगोल का विकास औपनिवेशिक काल से आरंभ हुआ। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रशासकों ने भारत के मानचित्रण, संसाधनों और जनसंख्या का अध्ययन शुरू किया।
शैक्षिक संस्थान: 1920 के बाद भारत में विश्वविद्यालयों में भूगोल विभागों की स्थापना हुई जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय आदि।
भारतीय विद्वान: प्रो. एस.पी. चटर्जी, प्रो. रेखा चौधरी, प्रो. रमेश सिंह आदि ने भौगोलिक शोध को आगे बढ़ाया।
भूगोल की शाखाएँ: आधुनिक भारत में भौतिक भूगोल के साथ-साथ मानव भूगोल, क्षेत्रीय नियोजन, पर्यावरण भूगोल, शहरी भूगोल, और GIS आधारित भूगोल पर भी कार्य हो रहा है।
राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका: भारतीय भूगोल परिषद (IGI), सर्वे ऑफ इंडिया, ISRO आदि संस्थान शोध को बढ़ावा दे रहे हैं।
तकनीकी उपयोग: सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, और GIS के माध्यम से आज भारत में भूगोल अधिक वैज्ञानिक और उपयोगी बना है।
प्रश्न-32. भौगोलिक ज्ञान में इरेटोस्थनीज के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- इरेटोस्थनीज (Eratosthenes) को “भूगोल का जनक” माना जाता है। वह यूनानी गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना बहुत सटीक रूप से की थी, जो कि लगभग सही थी — मात्र कुछ सौ किलोमीटर का अंतर था। यह उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गणनात्मक क्षमता को दर्शाता है।
इरेटोस्थनीज ने “गेस्टी ग्राफिका” (Geographika) नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के विभाजन, जलवायु क्षेत्र (Climatic Zones), अक्षांश-देशांश की संकल्पना और विश्व मानचित्र की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने भूमध्यरेखा और पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप को स्पष्ट किया। उनके द्वारा निर्धारित ग्रिड पद्धति बाद में आधुनिक मानचित्रण का आधार बनी।
उनका योगदान यह था कि उन्होंने भूगोल को केवल विवरणात्मक न मानकर उसे वैज्ञानिक और गणनात्मक रूप प्रदान किया। इरेटोस्थनीज का कार्य न केवल प्राचीन भूगोल में, बल्कि आधुनिक भूगोल की नींव में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
प्रश्न-33. पार्थिव एकता के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- पार्थिव एकता (Terrestrial Unity) का सिद्धांत यह दर्शाता है कि पृथ्वी एक समग्र और परस्पर जुड़ी हुई इकाई है। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के सभी भाग एक-दूसरे से भौतिक, जैविक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक स्थान की गतिविधियाँ अन्य स्थानों को भी प्रभावित कर सकती हैं।
इस सिद्धांत की जड़ें भूगोल की होलिस्टिक दृष्टिकोण में हैं, जो समस्त पृथ्वी को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में देखता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी क्षेत्र में वनों की कटाई होती है तो उसका प्रभाव न केवल उस क्षेत्र के पर्यावरण पर पड़ेगा, बल्कि वह वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देगा।
यह सिद्धांत पर्यावरणीय समस्याओं, वैश्विक व्यापार, पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में सहायक होता है। आधुनिक भूगोल इस सिद्धांत को आधार बनाकर पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है और मानव तथा प्राकृतिक तत्त्वों की एकता को महत्व देता है।
प्रश्न-34. प्रत्यक्षवाद पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:-प्रत्यक्षवाद (Positivism) एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत प्रत्यक्ष अनुभव और वैज्ञानिक परीक्षण है। इस विचारधारा की स्थापना अगस्ट कॉम्टे (Auguste Comte) ने की थी। भूगोल में प्रत्यक्षवाद का अर्थ है कि भौगोलिक अध्ययन को वैज्ञानिक विधियों, मापन, सांख्यिकी, एवं परीक्षणों के माध्यम से किया जाए।
20वीं शताब्दी के मध्य में यह दृष्टिकोण भूगोल में विशेष रूप से प्रचलित हुआ। भूगोलवेत्ताओं ने स्थलों, जलवायु, जनसंख्या आदि के अध्ययन में मात्रात्मक विधियों और गणनात्मक तकनीकों का प्रयोग आरंभ किया। इससे भूगोल अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बना।
प्रत्यक्षवाद ने भूगोल को सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अनुसार किसी भौगोलिक घटना की व्याख्या तभी मान्य है जब वह अनुभव और परीक्षण पर आधारित हो। यद्यपि इस दृष्टिकोण की आलोचना भी हुई कि यह मानवीय मूल्यों और व्याख्यात्मक आयामों की उपेक्षा करता है, फिर भी इसने भूगोल को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में आगे बढ़ाया।
प्रश्न-35. सांस्कृतिक भूदृश्य को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- सांस्कृतिक भूदृश्य (Cultural Landscape) उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जिस पर मानव ने अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रभाव डाला हो। इसमें कृषि भूमि, नगर, सड़कें, धार्मिक स्थल, भवन, जलाशय आदि शामिल होते हैं जो मानव की संस्कृति, परंपरा, और सामाजिक गतिविधियों के अनुरूप निर्मित होते हैं।
इस अवधारणा को सबसे पहले कार्ल सॉअर (Carl Sauer) ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार प्रकृति द्वारा निर्मित प्राकृतिक भूदृश्य को मानव अपनी आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार बदल देता है, जिससे सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण होता है।
यह परिभाषा मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करती है। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों द्वारा किए गए परिवर्तन इस बात के प्रमाण हैं कि संस्कृति किस प्रकार भौगोलिक स्थानों को रूपांतरित करती है। सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन क्षेत्रीय भूगोल, मानव भूगोल और पर्यावरणीय भूगोल में अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
प्रश्न-36. भूगोल में द्वैतवाद पर टिप्पणी लिखिए
उत्तर:- भूगोल में द्वैतवाद (Dualism) का अर्थ है भूगोल में दो विभिन्न दृष्टिकोणों या शाखाओं के बीच अंतर या विरोध। यह द्वैतवाद प्राचीन काल से ही भूगोल के अध्ययन में दिखाई देता है। प्रमुख द्वैतवाद निम्नलिखित हैं:
- प्राकृतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल – प्राकृतिक भूगोल प्रकृति के तत्वों जैसे जलवायु, स्थलरूप, वनस्पति आदि का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल मानव की गतिविधियों, संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है।
- वर्णनात्मक बनाम विश्लेषणात्मक भूगोल – पहले भूगोल विवरणात्मक था जिसमें केवल स्थानों और घटनाओं का वर्णन होता था, जबकि आधुनिक भूगोल विश्लेषणात्मक है जिसमें कारण-प्रभाव और प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।
- क्षेत्रीय बनाम प्रणालीगत भूगोल – क्षेत्रीय भूगोल किसी विशिष्ट क्षेत्र की समग्र विशेषताओं का अध्ययन करता है जबकि प्रणालीगत भूगोल विषय-आधारित होता है जैसे जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि।
भूगोल में द्वैतवाद ने इसे और अधिक गहराई और विस्तार प्रदान किया, जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों से पृथ्वी और मानव क्रियाओं का अध्ययन संभव हो पाया।
Section-C
प्रश्न-1.भूगोल के विषयक्षेत्र एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- भूगोल एक व्यापक एवं बहुआयामी विषय है, जो पृथ्वी की सतह, उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक व मानवीय तत्वों एवं उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। यह एक ऐसी विज्ञान शाखा है जो “कहाँ” (स्थान), “क्या” (वस्तु/घटना), “क्यों” (कारण), और “कैसे” (प्रक्रिया) जैसे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करती है।
भूगोल का विषयक्षेत्र:
- भौतिक भूगोल (Physical Geography): इसमें प्रकृति की विविध इकाइयों जैसे स्थलरूप (Landforms), जलवायु, वनस्पति, मिट्टी एवं जलस्रोतों का अध्ययन किया जाता है।
- मानव भूगोल (Human Geography): यह मानव गतिविधियों जैसे जनसंख्या, बसावट, कृषि, उद्योग, परिवहन, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करता है।
- पर्यावरण भूगोल (Environmental Geography): यह मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतःसंबंधों की पड़ताल करता है और पर्यावरणीय समस्याओं जैसे प्रदूषण, पारिस्थितिकी असंतुलन आदि का अध्ययन करता है।
- क्षेत्रीय भूगोल (Regional Geography): इसमें पृथ्वी के विशिष्ट भागों जैसे महाद्वीपों, देशों, राज्यों या नगरों का समग्र अध्ययन किया जाता है।
- तकनीकी भूगोल (Technical Geography): इसमें भू-स्थानिक तकनीकों जैसे रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (GPS) का प्रयोग किया जाता है।
भूगोल की प्रकृति:
- विज्ञान और कला दोनों: भूगोल में वैज्ञानिक विधियों के साथ-साथ मानवीय दृष्टिकोण का समावेश भी होता है, जिससे यह विज्ञान और कला दोनों बन जाता है।
- स्थानिक अध्ययन: भूगोल स्थानिक परिप्रेक्ष्य में घटनाओं का विश्लेषण करता है – कौन-सी घटना कहाँ, क्यों और किस प्रभाव में घट रही है।
- समन्वयकारी प्रकृति: भूगोल विभिन्न विषयों जैसे जीवविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान के साथ समन्वय स्थापित करता है।
- डायनामिक प्रकृति: भूगोल समय के साथ बदलता रहता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या प्रवास, शहरीकरण आदि।
- प्रयोगात्मक और व्यवहारिक: भूगोल का ज्ञान व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है जैसे आपदा प्रबंधन, योजना निर्माण, पर्यावरणीय नीति आदि में इसका प्रयोग होता है।
भूगोल न केवल पृथ्वी की संरचना व प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, बल्कि मानव और प्रकृति के अंतर्संबंधों को भी उजागर करता है। यह विषय अंतरविषयक दृष्टिकोण को अपनाते हुए वैश्विक व स्थानीय समस्याओं को समझने में सहायक सिद्ध होता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.आधुनिक भारत में भौगोलिक अध्ययन की नवीन प्रवृत्तियों का विवरण दीजिए।
उत्तर:- आधुनिक भारत में भूगोल विषय का स्वरूप समय के साथ परिवर्तित हुआ है। पारंपरिक वर्णनात्मक शैली की अपेक्षा अब विश्लेषणात्मक, तकनीकी और समाजोपयोगी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत में भौगोलिक अध्ययन में कई नवीन प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आई हैं।
- तकनीकी भूगोल का विकास:
रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing), GIS (Geographic Information System) और GPS (Global Positioning System) जैसी तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ा है।
आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और संसाधन मानचित्रण में इनका प्रयोग हो रहा है।
- पर्यावरण भूगोल पर बल:
जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक असंतुलन, वन विनाश, प्रदूषण आदि मुद्दों पर शोध और अध्ययन में वृद्धि हुई है।
- क्षेत्रीय एवं स्थानिक विश्लेषण:
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकास असमानताओं, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वितरण के स्थानिक विश्लेषण पर बल दिया जा रहा है।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल:
जातीयता, जनजातीय अध्ययन, भाषा, धर्म और संस्कृति के भूगोल पर नवीन शोध किए जा रहे हैं।
- आर्थिक भूगोल की नवीन प्रवृत्तियाँ:
वैश्वीकरण, उदारीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।
कृषि, उद्योग और व्यापारिक भूगोल में क्षेत्रीय परिवर्तन को समझा जा रहा है।
- महिला एवं लिंग भूगोल:
लिंग आधारित स्थानिक असमानताओं, महिला सुरक्षा, कार्यक्षेत्र आदि विषयों का अध्ययन आधुनिक प्रवृत्ति बन गया है।
- बहुविषयक दृष्टिकोण (Interdisciplinary Approach):
समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और योजना विज्ञान के साथ भूगोल का समन्वय किया जा रहा है।
- आपदा प्रबंधन भूगोल:
भारत में प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, भूकंप, सूखा) के अध्ययन और GIS आधारित आपदा पूर्वानुमान प्रणाली का विकास हो रहा है।
आधुनिक भारत में भूगोल का अध्ययन तकनीकी, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक दिशा में बढ़ रहा है। नई तकनीकों, पर्यावरणीय जागरूकता और सामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भूगोल आज एक अत्यंत उपयोगी और बहुआयामी विषय बन चुका है।
प्रश्न-3. प्राचीन भारत में भौगोलिक उपलब्धियों के मुख्य पक्ष प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में भौगोलिक चिंतन का विकास धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ था। भारतीय ऋषियों, विद्वानों और यात्रियों ने अपने अनुभवों व दृष्टिकोणों से भूगोल के विविध पक्षों को स्पष्टीकरण दिया। इन उपलब्धियों को निम्नलिखित प्रमुख पक्षों में विभाजित किया जा सकता है:
- धार्मिक और पुराणों में भूगोल:
वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में भौगोलिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्थान है। ‘ऋग्वेद’ में नदियों, पर्वतों और प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ‘जम्बूद्वीप’ की संकल्पना विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण में मिलती है, जिसमें भारत को एक द्वीप के रूप में चित्रित किया गया है। सप्तसिंधु, हिमालय, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों का वर्णन धार्मिक महत्व के साथ भूगोलिक जानकारी भी देता है। - खगोलशास्त्र और गणना:
भारतीय खगोलशास्त्रियों ने पृथ्वी की आकृति, उसकी स्थिति, सूर्य की गति, ग्रहण आदि की वैज्ञानिक व्याख्या दी। आर्यभट्ट (499 ई.) ने पृथ्वी को गोल बताया तथा उसकी परिधि की गणना भी की। वराहमिहिर ने ‘बृहत्संहिता’ में विभिन्न ऋतुओं, जलवायु, नक्षत्रों और दिशाओं का वर्णन किया। - नदियों और जल संसाधनों की जानकारी:
प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नदियों का उल्लेख उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व के साथ मिलता है। सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के उद्गम, प्रवाह और संगम स्थलों का वर्णन मिलता है। इससे उस समय की जलसंपदा एवं भूगोल की गहरी समझ का परिचय मिलता है। - यात्राएं और यात्रा-वृत्तांत:
चाणक्य (कौटिल्य) के ‘अर्थशास्त्र’ में प्रशासनिक इकाइयों, नगरों, मार्गों, पर्वतों, समुद्रतटों, व्यापारिक केंद्रों आदि का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है। ह्वेनसांग और फाह्यान जैसे चीनी यात्रियों ने भारत के भूगोल पर रोशनी डाली। पाटलिपुत्र, वाराणसी, मथुरा आदि नगरों का वर्णन उनके यात्रा-वृत्तांतों में मिलता है। - कृषि एवं पर्यावरण ज्ञान:
कृषि के लिए मौसम, मिट्टी, जलवायु और फसल चक्र की जानकारी आवश्यक थी, जो प्राचीन भारत के किसानों और विद्वानों को थी। ‘कृषिपराशर’ और ‘वृहत्संहिता’ में कृषि जलवायु और मौसम परिवर्तन का विश्लेषण मिलता है। - मानचित्र और दिशाएं:
यद्यपि भौगोलिक मानचित्र की आधुनिक धारणा प्राचीन भारत में नहीं थी, परंतु दिशाओं, समुद्री मार्गों, पर्वतों और नदियों की सटीक जानकारी दी जाती थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान आदि दिशाओं का उल्लेख वेदों से लेकर धार्मिक ग्रंथों तक मिलता है।
प्राचीन भारत में भूगोल की अवधारणा धार्मिक, खगोलीय, आर्थिक, पर्यावरणीय और यात्रा संबंधी ज्ञान से जुड़ी हुई थी। यह ज्ञान भारत की सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक चेतना को दर्शाता है। इन उपलब्धियों ने न केवल तत्कालीन समाज को दिशा दी, बल्कि आज भी उनके अध्ययन से भूगोल की मूल अवधारणाओं को समझा जा सकता है।
प्रश्न-4. जर्मन भौगोलिक चिंतन के विषय पक्ष बताइए।
उत्तर:- भूगोल के आधुनिक स्वरूप के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब भूगोल एक वर्णनात्मक विषय था, तब जर्मन विद्वानों ने इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। जर्मन भौगोलिक चिंतन के प्रमुख विषय पक्ष निम्नलिखित हैं:
- वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग:
जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयास किया। उन्होंने अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण और तुलना की विधियों को अपनाया। इससे भूगोल केवल विवरणात्मक न रहकर विश्लेषणात्मक विषय बना। - प्राकृतिक निर्धारणवाद (Environmental Determinism):
कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रेटजेल जैसे विद्वानों ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य का जीवन और संस्कृति भौगोलिक वातावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं। रेटजेल ने इस सिद्धांत को राजनीतिक भूगोल तक विस्तारित किया। - जीवनी शक्ति और लेबेन्सरॉम सिद्धांत:
रेटजेल ने ‘लेबेन्सरॉम’ (Lebensraum) का विचार प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि राज्य एक जीवंत जीव की तरह होता है और उसे विस्तार की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत ने राजनीतिक भूगोल को नई दिशा दी। - मानव भूगोल की आधारशिला:
कार्ल रिटर को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। उन्होंने मानव और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया। उनके अनुसार, पृथ्वी ईश्वर की बनाई एक रचना है और मानव जाति के विकास के लिए उसे समझना आवश्यक है। - क्षेत्रीय भूगोल (Regional Geography):
जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन किया और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों का वर्गीकरण किया। उन्होंने स्थान विशेष की भौगोलिक पहचान को प्राथमिकता दी। - शिक्षण एवं संस्थागत विकास:
जर्मनी में लाइपजिग, बर्लिन और बॉन विश्वविद्यालयों में भूगोल का उच्चस्तरीय शिक्षण प्रारंभ हुआ। ऑस्कर पेस्चेल और अल्ब्रेख्ट पेंक जैसे भूगोलवेत्ता इसी परंपरा में थे जिन्होंने भूगोल को शैक्षणिक अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित किया। - भू-आकृति विज्ञान में योगदान:
जर्मन भूगोलवेत्ता अल्ब्रेख्ट पेंक ने ग्लेशियर और भूमि आकृतियों का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने भू-आकृति विज्ञान (Geomorphology) को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित किया।
जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप, विषयवस्तु और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया। उनके चिंतन ने भूगोल को न केवल एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित किया बल्कि आधुनिक युग की सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी उसकी भूमिका सुनिश्चित की।
प्रश्न-5. भूगोल क्या है? भूगोल की परिभाषा कीजिए एवं इसके उपागमों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- भूगोल वह शास्त्र है जो पृथ्वी की सतह, उसके स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों तथा मानव की गतिविधियों का अध्ययन करता है। यह एक समन्वित विज्ञान है, जो प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के बीच के संबंधों की व्याख्या करता है।
भूगोल की परिभाषाएँ:
- एराटोस्थनीज ने सबसे पहले ‘भूगोल’ शब्द का प्रयोग किया और इसे “पृथ्वी के वर्णन का विज्ञान” कहा।
- रिचेथोफेन के अनुसार – “भूगोल प्रकृति के परिदृश्य का विज्ञान है।”
- हेटनर के अनुसार – “भूगोल पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं के स्थानिक अंतर एवं उनकी सहसंबंध की व्याख्या करता है।”
भूगोल के उपागम (Approaches):
भूगोल का अध्ययन विभिन्न उपागमों से किया जाता है, जो इस प्रकार हैं:
- प्रादेशिक उपागम (Regional Approach):
यह उपागम किसी एक विशेष क्षेत्र का समग्र अध्ययन करता है।
इस पद्धति में जलवायु, स्थलरूप, कृषि, उद्योग, जनसंख्या इत्यादि को मिलाकर किसी क्षेत्र की विशेषताओं को समझा जाता है।
- प्रणालीगत उपागम (Systematic Approach):
यह उपागम विषयवस्तु के आधार पर भूगोल को वर्गीकृत करता है। जैसे – जलवायु भूगोल, मृदा भूगोल, जनसंख्या भूगोल आदि।
इसमें एक तत्व का अध्ययन सम्पूर्ण पृथ्वी पर किया जाता है।
- स्थानिक उपागम (Spatial Approach):
यह उपागम वस्तुओं के स्थान, वितरण तथा पारस्परिक संबंधों की जांच करता है।
इसमें भू-स्थानिक तकनीकों (GIS, Remote Sensing) का उपयोग होता है।
- मानविक उपागम (Humanistic Approach):
इसमें मानव अनुभव, मूल्य, आस्थाओं तथा सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।
यह उपागम मानव भूगोल को और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है।
- पारिस्थितिक उपागम (Ecological Approach):
यह उपागम मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता है।
इसमें मानव की पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है।
भूगोल न केवल पृथ्वी की भौतिक बनावट का अध्ययन है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के संबंधों को समझने का एक समग्र प्रयास है। इसके विभिन्न उपागम भूगोल को एक जीवंत एवं प्रयोगात्मक विज्ञान बनाते हैं।
प्रश्न-6. भूगोल में निश्चयवाद और संभाववाद के बारे में आप क्या समझते हैं?
उत्तर:-भूगोल में निश्चयवाद (Determinism) और संभाववाद (Possibilism) दो प्रमुख दार्शनिक दृष्टिकोण हैं, जो मानव और पर्यावरण के संबंध को अलग-अलग दृष्टि से व्याख्यायित करते हैं।
- निश्चयवाद (Determinism):
परिभाषा:
निश्चयवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार मानव जीवन और गतिविधियाँ पूरी तरह प्रकृति और पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती हैं।
मुख्य विचार:
पर्यावरण ही मानव का भाग्य निर्धारण करता है।
मानव का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर्यावरण की सीमाओं के भीतर ही संभव है।
उदाहरण: प्राचीन मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, क्योंकि वहाँ उपजाऊ भूमि और जल की उपलब्धता थी।
प्रमुख समर्थक:
फ्रेडरिक रैटजेल (Friedrich Ratzel)
एलन हंटिंगटन (Ellen Huntington)
आलोचना:
यह दृष्टिकोण मानव को निष्क्रिय मानता है।
यह तकनीकी विकास और मानव की निर्णयात्मक क्षमता को नजरअंदाज करता है।
- संभाव्यवाद (Possibilism):
परिभाषा:
संभाव्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार पर्यावरण कुछ सीमाएँ अवश्य निर्धारित करता है, परंतु मानव अपनी बुद्धि और तकनीकी विकास के माध्यम से उन सीमाओं को पार कर सकता है।
मुख्य विचार:
मानव पर्यावरण के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया करता है।
तकनीक के सहारे रेगिस्तान को हरियाली में बदला जा सकता है।
उदाहरण: इजराइल ने मरुस्थलीय भूमि में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती को संभव बनाया।
प्रमुख समर्थक:
विडाल डी. ला ब्लाश
लुसिएन फेब्रे
महत्त्व:
यह दृष्टिकोण मानव की रचनात्मकता और स्वतंत्रता पर बल देता है।
यह आधुनिक भूगोल, विशेषकर मानव भूगोल की नींव है।
निश्चयवाद और संभाववाद दोनों दृष्टिकोण भूगोल में मानव-प्रकृति संबंध को समझने में सहायक हैं। निश्चयवाद जहाँ प्रकृति को प्रधान मानता है, वहीं संभाववाद मानव की भूमिका को प्रमुखता देता है। आज का भूगोल एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें मानव और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों को समन्वित रूप से समझा जाता है।
प्रश्न-7. भूगोल के क्षेत्र में यूनानी तथा रोमन भूगोलवेत्ताओं के योगदान की तुलना कीजिए।
उत्तर:- यूनानी और रोमन सभ्यताओं ने भूगोल के प्रारंभिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों सभ्यताओं के भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी की बनावट, मानचित्र निर्माण और विश्व की संरचना को समझने का प्रयास किया।
यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान:
- हेरोडोटस (Herodotus): ‘इतिहास का जनक’ माने जाने वाले हेरोडोटस ने नील नदी, मिस्र, फारस और उनके भूगोल का वर्णन किया।
- एरेटोस्थनीज (Eratosthenes): इन्होंने “भूगोल” शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और पृथ्वी की परिधि का वैज्ञानिक मापन किया।
- हिप्पार्कस (Hipparchus): खगोलीय भूगोल के क्षेत्र में योगदान देते हुए, इन्होंने अक्षांश-देशांश की अवधारणा दी।
- प्लेटो एवं अरस्तू: इन्होंने पृथ्वी की गोलाई का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
- टॉलेमी (Ptolemy): इनका ग्रंथ Geographia मानचित्र निर्माण की दृष्टि से ऐतिहासिक है। इन्होंने विश्व मानचित्र बनाया।
रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान:
- स्ट्रैबो (Strabo): इनका प्रमुख ग्रंथ Geographica है, जिसमें इन्होंने 17 खंडों में उस समय ज्ञात सम्पूर्ण विश्व का विवरण दिया।
- प्लिनी द एल्डर (Pliny the Elder): इन्होंने Natural History नामक ग्रंथ में भूगोल, जीव-जंतु, वनस्पति, खनिज आदि का वर्णन किया।
- मेला (Pomponius Mela): इन्होंने पृथ्वी को पाँच जलवायु पट्टियों में विभाजित किया।
- विट्रुवियस: इन्होंने नगर नियोजन और भवन निर्माण के भूगोल के सैद्धांतिक पहलुओं पर विचार किया।
तुलनात्मक विश्लेषण:
यूनानी भूगोल अधिक वैज्ञानिक और दार्शनिक था, जबकि रोमन भूगोल अधिक व्यावहारिक और वर्णनात्मक।
यूनानी भूगोलवेत्ता गणनात्मक विश्लेषण और खगोलशास्त्र पर बल देते थे, जबकि रोमन भूगोलवेत्ता सैन्य, प्रशासनिक और उपनिवेशीय दृष्टिकोण से भूगोल का अध्ययन करते थे।
टॉलेमी और एरेटोस्थनीज जैसे यूनानी विद्वानों का कार्य अधिक मानचित्रात्मक और सैद्धांतिक था, वहीं स्ट्रैबो और प्लिनी का लेखन अधिक भौगोलिक विवरणात्मक।
यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया, जबकि रोमन भूगोलवेत्ताओं ने इसे प्रशासनिक और व्यावहारिक दिशा दी। दोनों का योगदान भूगोल की नींव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।
प्रश्न-8. क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-
प्रश्न-9. व्यावहारिक (अनुप्रयुक्त) भूगोल को विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- अनुप्रयुक्त भूगोल (Applied Geography) भूगोल का वह शाखा है जो भौगोलिक ज्ञान का व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग करता है। यह भूगोल को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जनकल्याण और नीति-निर्माण से जोड़ता है।
अनुप्रयुक्त भूगोल की परिभाषा:
फिशर के अनुसार, “अनुप्रयुक्त भूगोल वह है जो भौगोलिक सिद्धांतों एवं तथ्यों का प्रयोग समाज की समस्याओं के समाधान हेतु करता है।”
मुख्य क्षेत्र:
- शहरी एवं ग्रामीण योजना: नगरों के विकास, ट्रैफिक प्रबंधन, हाउसिंग योजनाओं आदि में भूगोल की सहायता से योजना बनाई जाती है।
- पर्यावरणीय प्रबंधन: प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, भूकंप), प्रदूषण नियंत्रण, पारिस्थितिकी संतुलन हेतु भूगोल की जानकारी आवश्यक होती है।
- संसाधन प्रबंधन: जल, खनिज, ऊर्जा संसाधनों के नियोजन में भूगोलकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- पर्यटन विकास: किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर पर्यटन नीति बनाई जाती है।
- राजनीतिक भूगोल: सीमाओं, निर्वाचन क्षेत्रों, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में भूगोल के ज्ञान का उपयोग किया जाता है।
- GIS एवं Remote Sensing: उपग्रह चित्रों एवं भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग आधुनिक अनुप्रयुक्त भूगोल का हिस्सा है।
महत्त्व:
योजना निर्माण में सहायक
नीति निर्धारण हेतु आधार
पर्यावरणीय संतुलन के लिए मार्गदर्शक
प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी और प्रबंधन
आर्थिक विकास की दिशा में सहायता
अनुप्रयुक्त भूगोल वह पुल है जो सैद्धांतिक भूगोल को समाज की व्यवहारिक आवश्यकताओं से जोड़ता है। यह आधुनिक युग में भूगोल की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है और इसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी बनाता है।
प्रश्न-10. भूगोल में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के योगदान को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने आधुनिक भूगोल के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे यह विषय प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित हो सका।
प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं का योगदान:
- अलेक्जेंडर वॉन हंबोल्ट (Alexander von Humboldt):
इन्हें आधुनिक भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है।
इन्होंने स्थानिक वितरण, जलवायु, वनस्पति, और स्थलरूपों के बीच संबंध स्थापित किया।
उनकी प्रसिद्ध कृति “कॉसमॉस” में संपूर्ण प्रकृति का समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।
- कार्ल रिटर (Carl Ritter):
मानव भूगोल के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा।
इन्होंने भूगोल को ऐतिहासिक और नैतिक दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास किया।
उन्होंने भूगोल को मानव जाति के विकास के अध्ययन का एक साधन माना।
- फ्रेडरिक रैटजेल (Friedrich Ratzel):
इन्होंने “राजनीतिक भूगोल” और “संस्कृति भूगोल” की नींव रखी।
‘जैविक सिद्धांत’ और ‘स्थानिक विस्तार’ जैसे विचार प्रस्तुत किए।
उन्होंने ‘डिटरमिनिज्म’ (पर्यावरण निश्चयवाद) को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया।
- अल्फ्रेड हेत्तनर (Alfred Hettner):
इन्होंने क्षेत्रीय भूगोल के विचार को महत्व दिया।
‘कोरोलॉजिकल दृष्टिकोण’ की स्थापना की, जिसमें स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
- वाल्थर पेंक (Walther Penck):
इन्होंने स्थलरूप विकास के सिद्धांत दिए।
इन्होंने डेविस के स्थलाकृति चक्र की आलोचना करते हुए वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया।
जर्मन भूगोल की विशेषताएँ:
विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण।
गहन क्षेत्रीय अध्ययन।
पर्यावरण एवं मानव संबंधों की वैज्ञानिक व्याख्या।
राजनीतिक भूगोल का विकास।
जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विश्लेषणात्मक आधार प्रदान किया। इनके योगदान ने न केवल यूरोपीय भूगोल को प्रभावित किया बल्कि वैश्विक स्तर पर भूगोल के स्वरूप और अध्ययन पद्धतियों को भी दिशा दी।
प्रश्न-11. भूगोल के क्षेत्र में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- मध्यकाल में जब यूरोप में वैज्ञानिक सोच का अभाव था, तब अरब विद्वान भूगोल, खगोल, गणित तथा अन्य विज्ञानों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। ग्रीक और भारतीय ज्ञान को संजोकर उन्होंने अपने प्रयोगों व यात्रा-विवरणों के माध्यम से भूगोल को समृद्ध किया। अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
- यूनानी ज्ञान का संरक्षण और अनुवाद:
अरब विद्वानों ने प्लेटो, अरस्तू, टॉलेमी जैसे यूनानी भूगोलवेत्ताओं के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया। बैतुल हिक्मा (House of Wisdom) जैसे संस्थानों में इनका अध्ययन कर भूगोल को नया जीवन मिला। टॉलेमी की ‘Geographia’ को अल-मामून के काल में अरबी में अनूदित किया गया। - मानचित्र निर्माण में योगदान:
अरब भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी (1100-1165 ई.) ने ‘Tabula Rogeriana’ नामक विश्व का मानचित्र बनाया जो अपने समय का अत्यंत सटीक मानचित्र माना जाता है। इस मानचित्र में भारत, अफ्रीका, यूरोप और एशिया की विस्तृत जानकारी दी गई थी। - यात्रा विवरण और स्थान ज्ञान:
अरब यात्री जैसे इब्न बतूता और अल-मसूदी ने अपनी यात्राओं के माध्यम से विभिन्न भूभागों, नगरों, जलवायु, लोगों, भाषा और व्यापार मार्गों का विवरण दिया। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत में भारत, मध्य एशिया, चीन और अफ्रीका की भूगोलिक स्थितियों का वर्णन मिलता है। - जलवायु और पर्यावरणीय ज्ञान:
अरब विद्वानों ने जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया तथा भूमध्य रेखा के आधार पर पृथ्वी को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया। अल-ख्वारिज़्मी और अल-फाराबी ने तापमान, वर्षा, हवाओं और मौसम की विशेषताओं का विश्लेषण किया। - समुद्री भूगोल (Marine Geography):
अरब व्यापारी और नाविक समुद्री मार्गों के ज्ञाता थे। उन्होंने हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों की सटीक जानकारी दी। उनकी इस समझ ने आगे चलकर वास्को-डि-गामा जैसे यूरोपीय नाविकों को भारत तक पहुंचने में सहायता की। - गणनात्मक भूगोल और खगोलशास्त्र:
अरब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की परिधि और आकार की गणना करने के प्रयास किए। अल-बैरुनी ने भारत में आकर पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्व बल के सिद्धांतों पर शोध किया। उन्होंने ‘तहकीक मा लिल-हिंद’ नामक ग्रंथ में भारत की भूगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन किया।
अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान केवल ज्ञान को संरक्षित करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने स्वयं भी अनुभव, प्रयोग और निरीक्षण के माध्यम से भूगोल को समृद्ध किया। उनका कार्य यूरोपीय पुनर्जागरण और आधुनिक भूगोल की नींव रखने में सहायक सिद्ध हुआ।
प्रश्न-12. विडाल डी. ला ब्लाश द्वारा प्रतिपादित मानव भूगोल के मूल तत्वों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:-विडाल डी. ला ब्लाश (Vidal de la Blache) फ्रांस के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, जिन्हें मानव भूगोल का जनक (Father of Human Geography) कहा जाता है। उन्होंने “संभाव्यता” (Possibilism) का सिद्धांत प्रस्तुत कर मानव भूगोल को एक नवीन दिशा दी।
विडाल डी. ला ब्लाश की प्रमुख अवधारणाएँ:
- संभाव्यता (Possibilism):
उनके अनुसार, पर्यावरण मानव पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखता।
मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को बदल सकता है।
जैसे – रेगिस्तान में सिंचाई द्वारा खेती संभव बनाना।
- जैविक क्षेत्र (Genre de vie):
ब्लाश ने ‘जीवनशैली’ को विशेष महत्त्व दिया।
उन्होंने कहा कि किसी समाज की जीवनशैली उसके भू-आबोहवा, संस्कृति और परंपराओं से मिलकर बनती है।
यह जीवनशैली उस समाज के भूगोल को आकार देती है।
- क्षेत्रीय भूगोल पर बल:
उन्होंने भूगोल को एक क्षेत्रीय विज्ञान माना।
प्रत्येक क्षेत्र अपने भौगोलिक व सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण अद्वितीय होता है।
- नव मानव भूगोल की नींव:
उन्होंने भूगोल को केवल भौतिक दृष्टिकोण से न देखकर उसमें मानव तत्वों को भी जोड़ा।
इसके माध्यम से उन्होंने भूगोल को अधिक मानवीय और व्यवहारिक बनाया।
- निर्णयात्मक स्वतंत्रता (Human Freedom):
विडाल के अनुसार, मानव कोई निष्क्रिय प्राणी नहीं है, वह निर्णय लेने में स्वतंत्र है।
इसी स्वतंत्रता के कारण विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न मानव सभ्यताएँ विकसित हुईं।
विडाल डी. ला ब्लाश ने मानव भूगोल को एक मानव-केंद्रित अनुशासन के रूप में स्थापित किया। उनकी ‘संभाव्यता’ की संकल्पना आज भी मानव भूगोल के अध्ययन में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने पर्यावरण और मानव के बीच संतुलन पर बल देकर आधुनिक भूगोल की नींव रखी।
प्रश्न-13. भूगोल में संभववाद की संकल्पना की स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- संभववाद (Possibilism) भूगोल की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसका विकास पर्यावरण निश्चयवाद (Determinism) के प्रत्युत्तर में हुआ। यह विचारधारा मानती है कि भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित तो करता है, किंतु मानव अपनी बुद्धि, तकनीक और इच्छाशक्ति के आधार पर पर्यावरणीय सीमाओं को पार कर सकता है।
संभववाद की परिभाषा:
संभववाद वह सिद्धांत है, जो यह मानता है कि प्रकृति मनुष्य के लिए अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है और इनमें से कौन-सी संभावना को अपनाया जाए, यह मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी योग्यता पर निर्भर करता है।
प्रमुख विचारक:
- पॉल विडाल डी ला ब्लाश (Paul Vidal de la Blache):
संभववाद के जनक माने जाते हैं।
उन्होंने “मनुष्य प्रकृति का अधिपति है, दास नहीं” का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
‘Possibilism’ शब्द का सबसे पहले व्यवस्थित प्रयोग उन्होंने किया।
- लुसिएन फेब्रे (Lucien Febvre):
इन्होंने कहा, “प्रकृति बाध्यता नहीं, संभाव्यता है।”
उन्होंने मानवीय स्वतंत्रता और सामाजिक कारकों पर बल दिया।
संभववाद की विशेषताएँ:
- मनुष्य की स्वतंत्रता:
मनुष्य को अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। - तकनीकी विकास का महत्व:
तकनीक के माध्यम से मनुष्य कठिन से कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों को अनुकूल बना सकता है। - मानव-केंद्रित दृष्टिकोण:
इसमें मानव को सक्रिय भूमिका में माना गया है। - संस्कृति और समाज की भूमिका:
विभिन्न समाज एक ही भौगोलिक वातावरण में भिन्न प्रकार की जीवनशैली अपना सकते हैं।
संभववाद के उदाहरण:
रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा खेती (इजराइल)।
बर्फीले क्षेत्रों में आईग्लू बनाकर जीवन।
समुद्र के ऊपर कृत्रिम द्वीपों का निर्माण (दुबई)।
संभववाद ने भूगोल में मानव की भूमिका को केंद्र में लाकर पर्यावरण और मानव के संबंधों को संतुलित दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान किया। यह विचारधारा आधुनिक भूगोल में सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी पहलुओं को समझने में अत्यंत सहायक है।
vmou MAGE-01 paper , vmou MA GEOGRAPHY year exam paper ,vmou exam paper 2030 vmou exam paper 2028-29 vmou exam paper 2027 vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4
VMOU EXAM PAPER