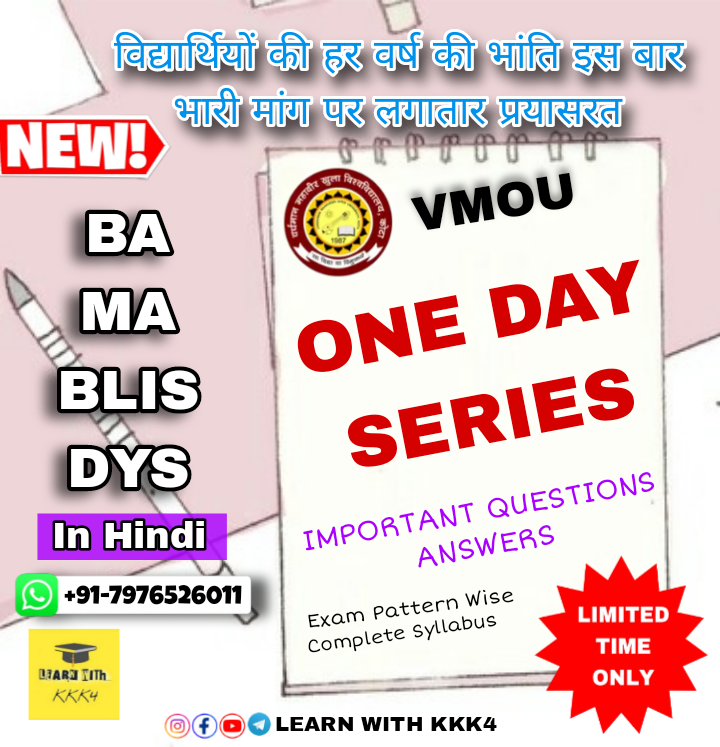VMOU MAPSY-01 Paper MA Previous Year ; vmou exam paper
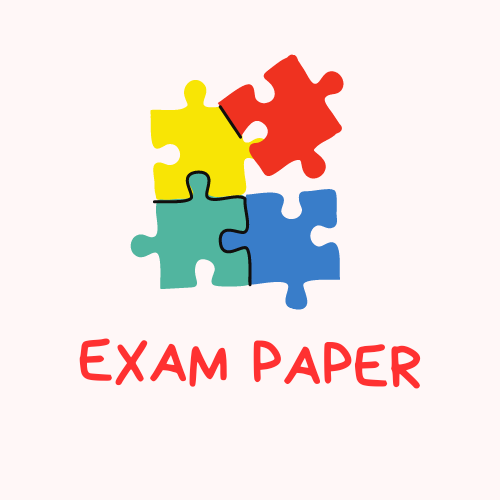
VMOU MA Previous Year के लिए Psychology ( MAPSY-01 , Psychological Research Methods ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.परामर्श मनोविज्ञान की परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- परामर्श मनोविज्ञान एक शाखा है जो व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक समस्याओं को समझकर उन्हें मार्गदर्शन और समाधान प्रदान करती है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.वस्तुनिष्ठता क्या है?
उत्तर:- ब कोई निष्कर्ष व्यक्ति विशेष की भावना या पक्षपात से प्रभावित न हो और सभी के लिए समान हो, तो उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं।
प्रश्न-3.व्यवहारवाद के जनक कौन थे?
उत्तर:- जॉन बी. वॉटसन (John B. Watson)
प्रश्न-4. रिसर्च शब्द की उत्पत्ति किस फ्रेंच शब्द से हुई है?
उत्तर:- रिसर्च शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द “recherche” से हुई है, जिसका अर्थ है “खोजना” या “जांच करना”।
प्रश्न-5. वैज्ञानिक विधि की चार प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषताएँ हैं: वस्तुनिष्ठता, परीक्षणशीलता, नियंत्रित अवलोकन, और सामान्यीकरण।
प्रश्न-6. ‘मूलभूत अनुसंधान’ का क्या अर्थ है ?
उत्तर:- मूलभूत अनुसंधान का अर्थ है ज्ञान को बढ़ाने हेतु सिद्धांतों और अवधारणाओं की खोज करना, बिना किसी व्यावहारिक उद्देश्य के।
प्रश्न-7. कौनसे वर्ष प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी ?
उत्तर:-1879 ई. में विल्हेम वुण्ट द्वारा जर्मनी के लाइपज़िग विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी।
प्रश्न-8. एक अच्छे परीक्षण के चार गुणों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- (1) विश्वसनीयता, (2) वैधता, (3) उद्देश्यपूर्णता, (4) उपयोगिता।
प्रश्न-9. रेटिंग स्केल से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:- रेटिंग स्केल एक मापनी है जिससे किसी गुण, व्यवहार या अभिवृत्ति की तीव्रता को मापा जाता है, जैसे- “बहुत अच्छा” से “बहुत खराब” तक।
प्रश्न-10.अनुसंधान को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:-अनुसंधान एक पद्धतिपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नवीन तथ्यों की खोज, सत्यापन या सिद्धांतों का विकास किया जाता है।
प्रश्न-11. ‘कार्योत्तर अनुसंधान’ का क्या अर्थ है?
उत्तर:-कार्योत्तर अनुसंधान वह होता है जिसमें कारणों की पहचान प्रभाव घटित होने के बाद की जाती है, यानी प्रभाव के आधार पर कारण का अध्ययन।
प्रश्न-12. समाज मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- समाज मनोविज्ञान वह शाखा है जो व्यक्ति के व्यवहार पर सामाजिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करती है।
प्रश्न-13. अनुप्रयुक्त अनुसंधान से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:- अनुप्रयुक्त अनुसंधान वह होता है जो व्यावहारिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए किया जाता है, जैसे—किसी शिक्षण विधि की प्रभावशीलता का परीक्षण।
प्रश्न-14. आश्रित चर की परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- आश्रित चर वह होता है जो स्वतंत्र चर में परिवर्तन के कारण प्रभावित होता है, जैसे—शिक्षण विधि (स्वतंत्र चर) से परीक्षा परिणाम (आश्रित चर) में बदलाव।
प्रश्न-15. ‘प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी’ के लेखक कौन थे ?
उत्तर:-विल्हेल्म वुण्ट (Wilhelm Wundt)
प्रश्न-16. प्रायोगिक अनुसंधान की चार कमियों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- 1) महँगा होता है, (2) समय अधिक लगता है, (3) नैतिक सीमाएँ होती हैं, (4) प्रयोगशाला की स्थिति हमेशा यथार्थ से मेल नहीं खाती।
प्रश्न-17. तीन सूचना संग्रहण के उपकरणों के नाम लिखिए।
उत्तर:- (1) प्रश्नावली, (2) साक्षात्कार, (3) अवलोकन।
प्रश्न-18. शून्य परिकल्पना की परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- शून्य परिकल्पना वह होती है जिसमें यह माना जाता है कि दो चर के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध या अंतर नहीं है।
प्रश्न-19. गेस्टाल्टवाद की विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:-गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत है कि “समग्र भागों के योग से बड़ा होता है”, यह अनुभव, बोध और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समग्र रूप में देखता है।
प्रश्न-20. नियंत्रित समूह से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:-नियंत्रित समूह वह होता है जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव नहीं डाला जाता, ताकि तुलना कर परिणामों की शुद्धता जांची जा सके।
प्रश्न-21. नवीन तथ्यों को जानने के प्राथमिक तरीके लिखिए।
उत्तर:- अवलोकन, प्रयोग, सर्वेक्षण और साक्षात्कार नवीन तथ्यों को जानने के प्राथमिक तरीके हैं।
प्रश्न-22. परिकल्पना क्या है?
उत्तर:-परिकल्पना एक संभावित कथन या अनुमान है, जिसे अनुसंधान में परीक्षण योग्य बनाया जाता है ताकि किसी घटना या संबंध की सत्यता जांची जा सके।
प्रश्न-23. परिकल्पना के प्रकार लिखिए।
उत्तर:- मुख्य प्रकार – शून्य परिकल्पना (Null), वैकल्पिक परिकल्पना (Alternative), दिशात्मक और अदिश परिकल्पना।
प्रश्न-24. एक सांख्यिकीय परिकल्पना बनाइए।
उत्तर:-शून्य परिकल्पना (H₀): “विद्यालय A और B के छात्रों के औसत अंक में कोई अंतर नहीं है।
प्रश्न-25. परिकल्पनाओं के स्रोत बताइए।
उत्तर:- रिकल्पनाओं के स्रोत हैं – पूर्व अध्ययन, अनुभव, सैद्धांतिक ढाँचा, साहित्य समीक्षा, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, और तार्किक चिंतन।
प्रश्न-26. सामान्यीकरण क्या है?
उत्तर:- सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष अध्ययन या अनुभव के आधार पर व्यापक नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं जो अन्य परिस्थितियों पर भी लागू हो सकें।
प्रश्न-27. अनुसंधान के संदर्भ में ‘समस्या’ से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:-अनुसंधान में समस्या का अर्थ उस प्रश्न या स्थिति से है जिसका उत्तर ज्ञात नहीं है और जिसे साक्ष्य द्वारा सुलझाना आवश्यक होता है।
प्रश्न-28. समाजमिति विधि का विकास किस वर्ष हुआ था
उत्तर:- समाजमिति विधि का विकास 1934 ई. में मनोवैज्ञानिक जे. एल. मोरेनो द्वारा किया गया था।
प्रश्न-29. ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ कौनसी हैं ?
उत्तर:- ज्ञान प्राप्त करने की प्रमुख विधियाँ हैं: अनुभव, प्राधिकरण, तर्क-वितर्क (तार्किकता), वैज्ञानिक विधि और अंतर्ज्ञान।
प्रश्न-30. अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना किसने की थी
उत्तर:- G. Stanley Hall
प्रश्न-31. विज्ञान की पहली विशेषता लिखिए।
उत्तर:-वस्तुनिष्ठ (Objective)
प्रश्न-32. मैकगुान द्वारा प्रदत्त प्रयोग के प्रकारों को लिखिए।
उत्तर:- प्राकृतिक प्रयोग, क्षेत्रीय प्रयोग और प्रयोगशाला प्रयोग।
प्रश्न-33. न्यादर्श की विश्वसनीयता किसे कहते हैं?
उत्तर:- न्यादर्श की विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि यदि नमूना बार-बार लिया जाए तो परिणाम स्थिर, एकसमान और सटीक मिलें।
प्रश्न-34. प्रसार विश्लेषण किसने विकसित किया?
उत्तर:- रोनाल्ड ए. फिशर (Ronald A. Fisher) ने
प्रश्न-35. माध्य की मानक त्रुटि का सूत्र लिखिए।
उत्तर:-माध्य की मानक त्रुटि = σ / √n, जहाँ σ = मानक विचलन और n = नमूना आकार।
Section-B
प्रश्न-1.मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
मानव व्यवहार पर केन्द्रित: इसका उद्देश्य मानव व्यवहार के कारणों को जानना और उसे नियंत्रित करना होता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यह अनुभवों और व्यवहार को मापने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है।
निरपेक्षता: अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त रहकर वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित कार्य करता है।
पुनरावृत्ति (Replication): अनुसंधान इस प्रकार किया जाता है कि अन्य शोधकर्ता भी उसी प्रक्रिया को दोहराकर वही परिणाम प्राप्त कर सकें।
नियंत्रण (Control): प्रयोगों में स्वतंत्र और निर्भर चरों को नियंत्रित किया जाता है जिससे निष्कर्ष अधिक सटीक होते हैं।
सत्यापन योग्य: शोध के निष्कर्षों को सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
सिस्टमेटिक प्रक्रिया: अनुसंधान एक योजनाबद्ध और चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत होता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.शोध परिकल्पना के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर:- शोध परिकल्पना (Research Hypothesis) एक अनुमानित कथन होती है जो दो या अधिक चर के बीच संबंध को व्यक्त करती है। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:
- सकारात्मक परिकल्पना (Positive Hypothesis): यह दर्शाती है कि चरों के बीच सीधा संबंध है।
उदाहरण: “अधिक अध्ययन समय से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं।” - नकारात्मक परिकल्पना (Negative Hypothesis): यह परिकल्पना चरों के बीच प्रतिकूल संबंध दर्शाती है।
उदाहरण: “अधिक मोबाइल उपयोग से विद्यार्थियों के अंक घटते हैं।” - शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis): यह कहती है कि दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है।
उदाहरण: “अध्ययन समय और परीक्षा परिणाम के बीच कोई संबंध नहीं है।” - वैकल्पिक परिकल्पना (Alternative Hypothesis): यह शून्य परिकल्पना के विपरीत होती है और संबंध को दर्शाती है।
उदाहरण: “अध्ययन समय का परीक्षा परिणाम पर प्रभाव पड़ता है।”
इन परिकल्पनाओं की जांच सांख्यिकीय विधियों से की जाती है, जिससे अनुसंधान में सटीक निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
प्रश्न-3.बुद्धि परीक्षणों के वर्गीकरण की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- बुद्धि परीक्षण (Intelligence Test) व्यक्ति की मानसिक योग्यता को मापने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है:
- व्यक्तिक (Individual Test): यह एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से लिया जाता है। जैसे—बिने-साइमन परीक्षण।
- समूह परीक्षण (Group Test): एक साथ कई व्यक्तियों पर एक ही समय में लागू किया जा सकता है। जैसे—ARMY Alpha Test।
- मौखिक परीक्षण (Verbal Test): इसमें भाषा आधारित प्रश्न होते हैं जैसे—शब्दार्थ, वाक्य निर्माण।
- गैर-मौखिक परीक्षण (Non-verbal Test): इसमें चित्र या संकेतों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे—Raven’s Progressive Matrices।
- प्रदर्शनात्मक परीक्षण (Performance Test): इनमें व्यक्ति से वस्तु को जोड़ना, निर्माण करना आदि क्रियाएं कराई जाती हैं।
इन वर्गों का प्रयोग व्यक्ति की बुद्धि को उसकी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार मापने हेतु किया जाता है।
प्रश्न-4. अन्वेषणात्मक अनुसंधान किस प्रकार व्याख्यात्मक अनुसंधान से भिन्न है ?
उत्तर:-अन्वेषणात्मक अनुसंधान और व्याख्यात्मक अनुसंधान दोनों ही वैज्ञानिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य और प्रक्रिया अलग होती है।
अन्वेषणात्मक अनुसंधान (Exploratory Research) प्रारंभिक चरण में किया जाता है जब किसी विषय पर बहुत कम जानकारी होती है। इसका उद्देश्य किसी नई समस्या, अवधारणा या स्थिति के बारे में प्रारंभिक जानकारी जुटाना होता है। इसमें लचीलापन होता है और यह अधिकतर गुणात्मक होता है।
व्याख्यात्मक अनुसंधान (Explanatory Research) किसी ज्ञात घटना या व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने हेतु किया जाता है। इसका उद्देश्य कारण-कार्य सम्बन्ध स्थापित करना होता है। यह संरचित, मात्रात्मक और सांख्यिकीय विश्लेषण आधारित होता है।
उदाहरण के लिए:
“क्यों कुछ विद्यार्थी अधिक तनाव में रहते हैं?” — व्याख्यात्मक अनुसंधान
“विद्यार्थियों में तनाव के लक्षण क्या हैं?” — अन्वेषणात्मक अनुसंधान
प्रश्न-5. मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में सांख्यिकी की भूमिका बताइए।
उत्तर:- मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में सांख्यिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह डेटा को संग्रहित, विश्लेषित एवं व्याख्यायित करने में सहायक होती है। इसकी प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:
- डेटा विश्लेषण: सांख्यिकीय विधियों से अनुसंधान में एकत्र किए गए आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है जिससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
- निष्कर्ष निकालना: सांख्यिकी की सहायता से हम यह तय कर सकते हैं कि कोई परिणाम सामान्य है या संयोगवश आया है।
- परिकल्पना परीक्षण: यह शोध परिकल्पनाओं की पुष्टि या खंडन में सहायक होती है।
- संबंध एवं भिन्नता का अध्ययन: विभिन्न चर के बीच संबंधों को समझने के लिए सहसंबंध एवं विभेदन परीक्षण आदि तकनीकों का उपयोग होता है।
- प्रयोग नियंत्रण: सांख्यिकी द्वारा निष्कर्षों की विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।
- भविष्यवाणी: आँकड़ों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है।
इस प्रकार, सांख्यिकी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान को वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक बनाती है।
प्रश्न-6.परिकल्पनाओं के कार्यों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- परिकल्पना (Hypothesis) अनुसंधान की दिशा को निर्धारित करने वाला एक संभावित उत्तर या कथन होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
- अनुसंधान को दिशा देना: परिकल्पना यह निर्धारित करती है कि अनुसंधान किस दिशा में किया जाएगा।
- समस्या को केंद्रित करना: यह अनुसंधान की समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।
- डेटा संग्रह में सहायता: यह तय करने में मदद करती है कि किस प्रकार का डाटा एकत्र करना है।
- परिणामों की व्याख्या: यह परिणामों के विश्लेषण और व्याख्या में सहायक होती है।
- सिद्धांत निर्माण: सफल परिकल्पनाएँ आगे चलकर सिद्धांत का आधार बन सकती हैं।
- सम्बन्ध स्थापित करना: यह चरों के बीच संभावित संबंध को प्रदर्शित करती है।
इस प्रकार, परिकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान की रीढ़ होती है।
प्रश्न-7.शोध समस्या चुनने के आधारों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- Section-C Question-2
प्रश्न-8.प्रयोगात्मक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं
उत्तर:- प्रयोगात्मक नियंत्रण (Experimental Control) का तात्पर्य उन विधियों से है जिनके द्वारा अनुसंधानकर्ता यह सुनिश्चित करता है कि अध्ययन के दौरान केवल स्वतंत्र चर (Independent Variable) ही निर्भर चर (Dependent Variable) को प्रभावित करे।
जब कोई प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कई ऐसे बाहरी कारक हो सकते हैं जो परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हीं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को प्रयोगात्मक नियंत्रण कहा जाता है। इसके माध्यम से शोधकर्ता उन सभी संभावित भ्रम उत्पन्न करने वाले चरों (Confounding Variables) को नियंत्रित करता है।
उदाहरण: यदि हम यह अध्ययन कर रहे हैं कि पढ़ाई का समय परीक्षा में प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है, तो अन्य कारकों जैसे नींद, पोषण, तनाव आदि को नियंत्रित रखना आवश्यक होता है।
प्रयोगात्मक नियंत्रण अनुसंधान को अधिक विश्वसनीय बनाता है और कारण-कार्य संबंध स्थापित करने में सहायक होता है।
प्रश्न-9. कार्योत्तर अनुसंधान क्या होता है ?
उत्तर:- कार्योत्तर अनुसंधान (Ex-Post Facto Research) वह अनुसंधान होता है जिसमें घटना घटने के बाद उसके कारणों की खोज की जाती है। इसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर (Independent Variable) को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि यह देखा जाता है कि पहले घटित घटनाओं का परिणाम क्या रहा।
यह अनुसंधान प्रयोगात्मक नहीं होता, बल्कि प्रेक्षण (Observation) व आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित होता है। इस प्रकार के अनुसंधान में सामान्यतः कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है।
उदाहरण: यदि कोई शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि किशोरों में सामाजिक मीडिया के उपयोग का उनके आत्मसम्मान पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वह पहले से मौजूद डेटा व घटनाओं का अध्ययन करेगा।
इस प्रकार, कार्योत्तर अनुसंधान उन स्थितियों के लिए उपयुक्त होता है जहाँ प्रयोग संभव नहीं होता या नैतिक रूप से अनुचित होता है।
प्रश्न-10. साक्षात्कार के विभिन्न स्तर पर महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- साक्षात्कार अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से जानकारी एकत्र करता है। इसके विभिन्न स्तरों पर ध्यान देने योग्य बातें निम्न हैं:
- पूर्व-निर्धारित (Structured) साक्षात्कार: इसमें प्रश्न पहले से तय होते हैं। आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता सभी प्रश्नों को स्पष्टता और क्रम में पूछे।
- अर्ध-संरचित (Semi-structured): इसमें कुछ प्रश्न तय होते हैं और कुछ स्थिति अनुसार पूछे जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता को लचीलापन रखना चाहिए।
- असंरचित (Unstructured): इसमें कोई तय प्रश्न नहीं होते। वार्तालाप स्वाभाविक रूप में होता है। साक्षात्कारकर्ता को संवेदनशील व ध्यानपूर्वक सुनने वाला होना चाहिए।
- गहराई साक्षात्कार (In-depth Interview): इसमें विषय को गहराई से जानने हेतु लंबा संवाद होता है। प्रश्नों का क्रम व शैली लचीली होती है।
प्रत्येक स्तर पर गोपनीयता, सम्मान, स्पष्टता और सहानुभूति आवश्यक होती है।
प्रश्न-11. विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
उत्तर:-विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली है जो तथ्यों के अवलोकन, परीक्षण और प्रयोग पर आधारित होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- वस्तुनिष्ठता (Objectivity): वैज्ञानिक खोजें व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मुक्त होती हैं।
- प्रेक्षणीयता (Observability): वैज्ञानिक घटनाएँ प्रेक्षण के योग्य होती हैं जिन्हें मापा और देखा जा सकता है।
- पुनरावृत्तता (Replicability): वैज्ञानिक निष्कर्षों की पुनरावृत्ति अन्य शोधकर्ताओं द्वारा की जा सकती है।
- सार्वभौमिकता (Universality): वैज्ञानिक नियम सभी जगह और समय पर लागू होते हैं।
- पूर्वानुमेयता (Predictability): विज्ञान के माध्यम से भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है।
- नियंत्रण (Control): वैज्ञानिक प्रयोगों में परिवर्तनीय कारकों को नियंत्रित किया जाता है।
- कारण और प्रभाव संबंध (Cause-Effect Relationship): विज्ञान घटनाओं के कारणों और प्रभावों की खोज करता है।
इन विशेषताओं के कारण विज्ञान को विश्वसनीय और प्रमाणिक ज्ञान का स्रोत माना जाता है।
प्रश्न-12. अनुसन्धान परिकल्पना एवं अनुसन्धान समस्या में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-अनुसन्धान परिकल्पना (Hypothesis) और अनुसन्धान समस्या (Research Problem) दोनों अनुसंधान की आधारशिला हैं, परन्तु इनमें स्पष्ट भिन्नता होती है।
अनुसन्धान समस्या एक प्रश्नात्मक स्वरूप होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में जिज्ञासा या समस्या को स्पष्ट करती है। यह अनुसंधान की दिशा तय करती है और शोधकर्ता को बताती है कि “क्या अध्ययन करना है।” उदाहरण: “क्या बाल मजदूरी का मुख्य कारण गरीबी है?”
अनुसन्धान परिकल्पना एक संभावित उत्तर या पूर्वानुमान होता है जो अनुसंधान समस्या के संभावित समाधान का सुझाव देता है। यह जांचने योग्य (testable) होता है। उदाहरण: “बाल मजदूरी गरीबी से जुड़ी होती है।”
मुख्य अंतर:
अनुसंधान समस्या प्रश्न रूप में होती है; परिकल्पना उत्तर के रूप में।
समस्या अनुसंधान का विषय तय करती है; परिकल्पना जांचने योग्य कथन होती है।
अनुसंधान परिकल्पना को परीक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि समस्या केवल समस्या को चिन्हित करती है।
प्रश्न-13. एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- एक अच्छा परीक्षण (Good Test) वह होता है जो वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो और परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करे। उसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- विश्वसनीयता (Reliability): एक अच्छा परीक्षण बार-बार प्रयोग करने पर समान परिणाम देता है।
- वैधता (Validity): परीक्षण वही मापे, जो वह मापने का दावा करता है।
- मानकीकरण (Standardization): परीक्षण की प्रक्रिया, समय, वातावरण आदि सब कुछ समान रूप से लागू होना चाहिए।
- प्रश्नों की स्पष्टता: परीक्षण की भाषा सरल, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए।
- उपयुक्तता: परीक्षण संबंधित विषय के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए।
- सुरक्षा: परीक्षण के परिणामों को गोपनीय रखा जाना चाहिए।
- उपयोगिता: परीक्षण व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाया जा सके।
इन विशेषताओं के आधार पर ही किसी परीक्षण की गुणवत्ता और वैज्ञानिकता सुनिश्चित की जाती है।
प्रश्न-14. विभिन्न प्रकार की प्रायिकता न्यादर्शन विधियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- प्रायिकता (Probability) नमूनाकरण विधियों में प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं:
- साधारण यादृच्छिक नमूनाकरण (Simple Random Sampling): प्रत्येक इकाई को समान अवसर मिलता है, जैसे लॉटरी प्रणाली।
- सिस्टमेटिक सैम्पलिंग (Systematic Sampling): प्रत्येक kवें सदस्य को चुना जाता है। जैसे हर 10वें छात्र का चयन।
- स्तरीकृत नमूनाकरण (Stratified Sampling): पूरी जनसंख्या को उप-समूहों में बाँटकर प्रत्येक से नमूने लिए जाते हैं।
- समूह नमूनाकरण (Cluster Sampling): जनसंख्या को समूहों में बाँटकर कुछ समूहों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है।
- मल्टीस्टेज सैम्पलिंग: इसमें ऊपर की विधियों का संयोजन किया जाता है।
लाभ: निष्पक्षता, सामान्यीकरण की संभावना, सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक।
प्रश्न-15. अनुसन्धान के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- अनुसन्धान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है:
रिपोर्ट लेखन: संपूर्ण अनुसंधान को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना।
समस्या की पहचान: अध्ययन का मुख्य विषय तय करना।
समीक्षा साहित्य (Literature Review): पहले से उपलब्ध शोध कार्यों का अध्ययन।
परिकल्पना निर्माण: एक संभावित उत्तर या समाधान तय करना।
अनुसन्धान डिज़ाइन: विधियाँ, उपकरण, नमूना आदि तय करना।
नमूना चयन: अध्ययन के लिए उपयुक्त जनसंख्या का चयन।
डेटा संग्रहण: उपयुक्त तकनीकों द्वारा जानकारी एकत्र करना।
डेटा विश्लेषण: सांख्यिकीय तरीकों से डेटा की व्याख्या।
निष्कर्ष और सुझाव: प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर परिणाम प्रस्तुत करना।
प्रश्न-16. मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान में कम्प्यूटर के अनुप्रयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में कम्प्यूटर एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। इसका प्रयोग डाटा संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुति में किया जाता है।
मुख्य अनुप्रयोग:
- डेटा संग्रहण: ऑनलाइन प्रश्नावली या टेस्टों के माध्यम से।
- डेटा विश्लेषण: सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर (जैसे SPSS, R) का प्रयोग करके आंकड़ों की गणना।
- सिमुलेशन और मॉडलिंग: व्यवहार के पूर्वानुमान के लिए कम्प्यूटर मॉडल।
- प्रस्तुति: रिपोर्ट, ग्राफ, चार्ट आदि को प्रस्तुत करने में सहायक।
- संज्ञानात्मक परीक्षण: कम्प्यूटर आधारित रिएक्शन टाइम, मेमोरी टेस्ट आदि।
लाभ: समय की बचत, सटीकता, विश्वसनीयता और आसान विश्लेषण।
कम्प्यूटर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान को वैज्ञानिक, तेज और प्रभावी बनाता है।
प्रश्न-17. हिमकंदक न्यादर्शन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- हिमकंदक न्यादर्शन (Snowball Sampling) एक असंभाव्य (non-probability) नमूनाकरण विधि है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब लक्षित जनसंख्या तक सीधा पहुँचना कठिन हो।
इस विधि में शोधकर्ता सर्वप्रथम एक उत्तरदाता से जानकारी प्राप्त करता है और फिर उससे अन्य उपयुक्त उत्तरदाताओं का पता पूछता है। यह प्रक्रिया ऐसे ही आगे बढ़ती है जैसे हिमकण गिरकर बर्फ के गोले का आकार बढ़ाते हैं, इसलिए इसे “हिमकंदक” विधि कहा जाता है।
उदाहरण: जब किसी अवैध कार्य में संलग्न लोगों जैसे मादक पदार्थ उपभोक्ताओं पर शोध करना हो।
विशेषताएँ:
यह विधि सामाजिक नेटवर्कों में अधिक उपयोगी होती है।
गुप्त या सीमित समूहों में कारगर होती है।
समय और संसाधनों की बचत करती है।
सीमाएँ:
नमूना पक्षपाती हो सकता है।
परिणामों का सामान्यीकरण कठिन होता है।
उत्तरदाताओं की विश्वसनीयता हमेशा सुनिश्चित नहीं होती।
प्रश्न-18. उत्तम न्यादर्श की विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- उत्तम न्यादर्श (Best Sampling) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जनसंख्या से इस प्रकार नमूने चुने जाते हैं कि वे पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करें। उत्तम न्यादर्श की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- प्रतिनिधित्व (Representativeness): चुना गया नमूना पूरी जनसंख्या का सटीक प्रतिनिधित्व करता है।
- सटीकता (Accuracy): इसमें त्रुटियाँ न्यूनतम होती हैं जिससे निष्कर्ष विश्वसनीय होता है।
- निरपेक्षता (Objectivity): नमूना चयन की प्रक्रिया पूर्वाग्रह रहित होती है।
- लचीलापन (Flexibility): यह विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार समायोज्य होता है।
- आर्थिकता (Economical): संसाधनों की बचत के साथ अधिकतम जानकारी प्राप्त होती है।
- व्यवहार्यता (Practicability): इसे आसानी से लागू किया जा सकता है।
उत्तम न्यादर्श अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाता है और प्राप्त निष्कर्षों को विश्वसनीय बनाता है। अतः अनुसंधान में उचित न्यादर्श तकनीक का चुनाव अत्यंत आवश्यक होता है।
प्रश्न-19. निर्धारण मापनी के प्रकारों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- निर्धारण मापनी (Rating Scale) का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं को मापने हेतु किया जाता है। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:
- साधारण मापनी (Ordinal Scale): इसमें गुणों को किसी क्रम में रखा जाता है जैसे – अच्छा, सामान्य, खराब।
- नाममात्र मापनी (Nominal Scale): इसमें केवल नाम या वर्ग के आधार पर मापन होता है, जैसे – लिंग (पुरुष/महिला), धर्म आदि।
- अंतराल मापनी (Interval Scale): इसमें माप के बीच समान अंतर होता है पर शून्य का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे – तापमान।
- न्यूनतम मापनी (Ratio Scale): इसमें पूर्ण शून्य होता है और गणना की जा सकती है, जैसे – ऊँचाई, वजन।
- लिकर्ट मापनी (Likert Scale): यह व्यक्ति की सहमति या असहमति को मापने हेतु 5-बिंदु या 7-बिंदु मापनी होती है। जैसे – “पूरी तरह सहमत से पूरी तरह असहमत”।
ये मापनियाँ मनोवैज्ञानिक व शैक्षणिक शोध में अत्यंत उपयोगी होती हैं।
प्रश्न-20. मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य तथा उपयोगिताओं की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसी व्यक्ति की मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक या व्यवहारिक विशेषताओं को मापने का वैज्ञानिक साधन है। इसके प्रमुख उद्देश्य व उपयोग इस प्रकार हैं:
- नैदानिक उद्देश्य: मानसिक रोगों की पहचान व निदान के लिए प्रयोग।
- शैक्षिक उद्देश्य: छात्रों की योग्यता, रुचि और सीखने की कठिनाइयों को जानने हेतु।
- नियोजन उद्देश्य: कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में उपयुक्त व्यक्ति का चयन।
- अनुसंधान में: व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं की माप व विश्लेषण के लिए।
- व्यक्तित्व मूल्यांकन: व्यक्ति के व्यक्तित्व, अभिवृत्ति व मनोवैज्ञानिक रुझानों को जानने हेतु।
मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहार को वैज्ञानिक तरीके से समझने व निर्णय लेने में सहायता करता है।
प्रश्न-21. ‘शोध अभिकल्प’ के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- शोध अभिकल्प (Research Design) अनुसंधान की रूपरेखा है जो पूरे शोध को निर्देशित करती है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- शोध की दिशा तय करना: यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार का डेटा एकत्र किया जाएगा।
- संसाधनों का उचित उपयोग: समय, धन और श्रम का बेहतर नियोजन किया जाता है।
- चर नियंत्रण: अनुसंधान में चरों को नियंत्रित कर विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करना।
- त्रुटि में कमी: उचित डिजाइन अनुसंधान में संभावित त्रुटियों को न्यूनतम करता है।
- तुलना और निष्कर्ष: परिणामों की तुलना और निष्कर्ष निकालने में सुविधा।
- विश्वसनीयता व वैधता: निष्कर्षों की पुनरावृत्ति और उपयोगिता सुनिश्चित करता है।
इस प्रकार, शोध अभिकल्प अनुसंधान की सफलता की आधारशिला होता है।
प्रश्न-22. अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान के प्रकारों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- अनुसंधान को उसके उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:
- वर्णनात्मक अनुसंधान (Descriptive Research): इसका उद्देश्य किसी घटना, स्थिति या प्रक्रिया का वर्णन करना होता है। जैसे – किसी विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता का अध्ययन।
- व्याख्यात्मक अनुसंधान (Explanatory Research): यह अनुसंधान कारण-प्रभाव संबंधों को स्पष्ट करता है। जैसे – परीक्षा के परिणाम पर अध्ययन के घंटों का प्रभाव।
- अन्वेषणात्मक अनुसंधान (Exploratory Research): इसका उद्देश्य किसी नए क्षेत्र की खोज करना होता है। इसमें शोधकर्ता किसी अपरिचित विषय पर प्रारंभिक जानकारी एकत्र करता है।
- पूर्वानुमानात्मक अनुसंधान (Predictive Research): इसका उद्देश्य भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना होता है।
- अनुप्रयुक्त अनुसंधान (Applied Research): इसका उद्देश्य किसी व्यावहारिक समस्या का समाधान खोजना होता है।
इन सभी प्रकारों का चयन अनुसंधान की प्रकृति और लक्ष्य के आधार पर किया जाता है।
प्रश्न-23. साक्षात्कार के विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:-साक्षात्कार अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है, जो विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न रूप में प्रयुक्त होती है। प्रत्येक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है:
- पूर्व-साक्षात्कार स्तर:
उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए।
प्रश्नों की रूपरेखा पहले से तैयार करनी चाहिए।
साक्षात्कारकर्ता का प्रशिक्षण होना चाहिए।
- साक्षात्कार के समय:
अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए।
उत्तरदाता के साथ सम्मानजनक एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
प्रश्न स्पष्ट एवं सरल भाषा में पूछने चाहिए।
उत्तरदाता को बीच में टोकना नहीं चाहिए।
- साक्षात्कार के बाद:
उत्तरों को ठीक से रिकॉर्ड करना चाहिए।
विश्लेषण हेतु निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए।
यदि आवश्यक हो तो उत्तरदाता से फॉलोअप करना चाहिए।
इन बातों को ध्यान में रखकर साक्षात्कार की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है और विश्वसनीय व वैध निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं।
प्रश्न-24. एक अनुसन्धान प्रतिवेदन के विभिन्न अवयवों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:-एक अनुसंधान प्रतिवेदन (Research Report) शोध प्रक्रिया का सार प्रस्तुत करता है। इसके प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं:
शीर्षक पृष्ठ (Title Page): रिपोर्ट का शीर्षक, शोधकर्ता का नाम, संस्था आदि।
पूर्वकथन (Preface): कार्य की भूमिका और उद्देश्य।
सारांश (Abstract): संक्षेप में पूरा शोध।
परिचय (Introduction): समस्या की पृष्ठभूमि और उद्देश्य।
समीक्षा साहित्य: पूर्ववर्ती शोधों का वर्णन।
विधियाँ (Methodology): नमूना, उपकरण, प्रक्रिया आदि।
डेटा विश्लेषण और व्याख्या: परिणामों की प्रस्तुति।
निष्कर्ष और सुझाव: प्रमुख निष्कर्ष व उनके व्यावहारिक पक्ष।
परिशिष्ट (Appendices): प्रश्नावली, तालिकाएँ आदि।
संदर्भ सूची (References): प्रयुक्त पुस्तकों, लेखों का उल्लेख।
प्रश्न-25. कार्योत्तर अनुसंधान की सीमाओं की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- कार्योत्तर अनुसंधान (Ex-post-facto Research) वह अनुसंधान होता है जिसमें शोधकर्ता किसी घटना के घटित होने के बाद उसका कारण जानने का प्रयास करता है। इसकी सीमाएँ निम्नलिखित हैं:
- नियंत्रण की कमी: शोधकर्ता स्वतंत्र चर को नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि घटना पहले ही घट चुकी होती है।
- कारण-प्रभाव संबंध की अस्पष्टता: चूँकि चर नियंत्रित नहीं होते, अतः यह तय करना कठिन होता है कि कौन-सा कारण किस प्रभाव का कारण बना।
- पूर्वाग्रह की संभावना: चूँकि शोधकर्ता स्वयं घटना में हस्तक्षेप नहीं करता, अतः उपलब्ध डेटा पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है।
- विश्वसनीयता में कमी: पूर्वघटित घटनाओं पर आधारित जानकारी की सत्यता संदेहास्पद हो सकती है।
- सामान्यता की कमी: इसके निष्कर्ष सभी परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकते।
- सांख्यिकीय कठिनाइयाँ: आँकड़ों के विश्लेषण में जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
इन सीमाओं के बावजूद, यह विधि उन परिस्थितियों में उपयोगी होती है जहाँ प्रयोगात्मक शोध संभव नहीं होता।
प्रश्न-26. विधियात्मक शोधों के क्षेत्रों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:-विधियात्मक शोध (Methodological Research) उन अनुसंधानों को कहा जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान की विधियों, उपकरणों एवं तकनीकों का विकास एवं सुधार होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
- मापन उपकरणों का विकास: जैसे – बुद्धिलब्धि (IQ) परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण आदि।
- डाटा विश्लेषण की तकनीकें: जैसे – सांख्यिकीय विधियाँ, गुणात्मक विश्लेषण की विधियाँ आदि।
- न्यादर्श (Sampling) की तकनीकें: यादृच्छिक एवं अयादृच्छिक नमूना चयन पद्धतियों का विकास।
- प्रयोगात्मक डिजाइन: जैसे – पूर्व-परीक्षण–पश्चात परीक्षण, नियंत्रण समूह तकनीक आदि।
- साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के प्रारूप: इन उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार।
- सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की विधियाँ: जैसे – केस स्टडी, ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि आदि।
इस शोध का उद्देश्य अनुसंधान प्रक्रिया को अधिक सटीक, प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाना होता है।
प्रश्न-27. ‘निर्धारण मापनी’ के प्रकारों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- निर्धारण मापनी (Rating Scale) वह तकनीक है जिससे व्यक्ति की अभिवृत्तियों, व्यवहारों या प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसके मुख्य प्रकार हैं:
- सारणीबद्ध मापनी (Numerical Rating Scale): इसमें 1 से 5 या 1 से 10 तक की संख्या दी जाती है। जैसे—1 = अत्यंत असंतुष्ट, 5 = अत्यंत संतुष्ट।
- वर्णात्मक मापनी (Descriptive Rating Scale): इसमें वर्णात्मक स्तर होते हैं जैसे “अच्छा”, “संतोषजनक”, “खराब”।
- लिकर्ट मापनी (Likert Scale): इसमें वक्तव्य के प्रति सहमति या असहमति को 5 या 7 बिंदु मापनी में व्यक्त किया जाता है।
- सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल: दो विरोधी विशेषणों के बीच व्यक्ति का दृष्टिकोण मापा जाता है।
यह मापन विधियाँ व्यक्तियों की धारणाओं और प्रतिक्रियाओं को मापने में उपयोगी होती हैं।
प्रश्न-28. उद्देश्य की कसौटी के आधार पर परीक्षण के प्रमुख प्रकारों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- परीक्षणों को उनके उद्देश्यों के आधार पर दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है:
- उपलब्धि परीक्षण (Achievement Test):
इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी विशेष विषय में कितना ज्ञान प्राप्त किया है। उदाहरणस्वरूप, बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा आदि। - योग्यता परीक्षण (Aptitude Test):
इस परीक्षण का उद्देश्य किसी व्यक्ति की भविष्य में किसी कार्य को करने की क्षमता का अनुमान लगाना होता है। जैसे—इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (JEE), आईक्यू टेस्ट। - रुचि परीक्षण (Interest Test):
यह यह ज्ञात करने के लिए होता है कि व्यक्ति की रुचियाँ किन क्षेत्रों में हैं। - व्यक्तित्व परीक्षण (Personality Test):
यह परीक्षण व्यक्ति की भावनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल्यांकन करता है।
इन परीक्षणों का चयन अनुसंधान के उद्देश्य और प्रकृति के अनुसार किया जाता है।
प्रश्न-29. चरों में विशेष सम्बन्ध के आधार पर परिकल्पनाओं के प्रकारों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:-परिकल्पना एक संभावित उत्तर या निष्कर्ष होता है जिसे अनुसंधान के दौरान प्रमाणित या खंडित किया जाता है। चरों में विशेष संबंध के आधार पर परिकल्पनाओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं:
सकारात्मक परिकल्पना (Positive Hypothesis): इसमें दो चरों के बीच सकारात्मक संबंध की बात होती है, जैसे—”अभ्यास बढ़ने से प्रदर्शन में वृद्धि होती है।”
ऋणात्मक परिकल्पना (Negative Hypothesis): यह परिकल्पना नकारात्मक या विपरीत संबंध दर्शाती है, जैसे—”तनाव बढ़ने से कार्यकुशलता घटती है।”
शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis): इसमें यह मान लिया जाता है कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है, जैसे—”धूम्रपान और एकाग्रता के बीच कोई संबंध नहीं है।”
दिशात्मक परिकल्पना (Directional Hypothesis): इसमें यह बताया जाता है कि संबंध किस दिशा में होगा—सकारात्मक या नकारात्मक।
अदिशात्मक परिकल्पना (Non-directional Hypothesis): इसमें केवल यह कहा जाता है कि दो चर संबंधित हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं होती।
प्रश्न-30. अनुसंधान की दृष्टि से जनसंख्या के मुख्य प्रकार की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- अनुसंधान में जनसंख्या (Population) का अर्थ उस समुच्चय से है, जिससे नमूना लिया जाता है। अनुसंधान की दृष्टि से जनसंख्या के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं:
- लक्षित जनसंख्या (Target Population): वह समूचा समूह, जिस पर अनुसंधानकर्ता अध्ययन करना चाहता है। उदाहरण: सभी कॉलेज विद्यार्थी।
- उपलब्ध जनसंख्या (Accessible Population): वह जनसंख्या जिसका अनुसंधानकर्ता द्वारा व्यवहार में अध्ययन किया जाना संभव है। जैसे केवल एक कॉलेज के विद्यार्थी।
- नमूना जनसंख्या (Sample Population): वास्तविक वे व्यक्ति जो अनुसंधान में शामिल किए जाते हैं।
- सैद्धांतिक जनसंख्या (Theoretical Population): इसमें केवल विचारात्मक रूप से पूरे समूह की कल्पना की जाती है। जैसे “समस्त किशोरावस्था के लोग।”
इन प्रकारों को स्पष्ट पहचानकर ही सही प्रकार का नमूना चयन किया जा सकता है।
प्रश्न-31. समूह को समान करने की विभिन्न विधियों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- शोध में जब दो या दो से अधिक समूहों की तुलना करनी होती है, तब आवश्यक होता है कि वे समूह पूर्व से ही समान हों। समूहों को समान करने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं:
- यादृच्छिक चयन विधि (Randomization): इसमें प्रतिभागियों को बिना किसी पक्षपात के समूहों में बाँटा जाता है। यह पूर्वाग्रह को कम करती है।
- युग्मन विधि (Matching): इसमें समूहों को कुछ विशेषताओं जैसे – आयु, लिंग, बुद्धि आदि के आधार पर समान बनाया जाता है।
- सांख्यिकीय नियंत्रण (Statistical Control): इसमें सह-चर (Covariate) को नियंत्रित करने के लिए सांख्यिकीय तकनीक जैसे – ANCOVA का उपयोग किया जाता है।
- साम्यकरण विधि (Equating Method): जैसे – औसत स्कोर, मानक विचलन आदि के आधार पर समूहों को संतुलित किया जाता है।
- पूर्व-परीक्षण विधि (Pre-test Method): इसमें परीक्षण से पहले समूहों के प्रदर्शन को मापा जाता है और उसी के आधार पर उनका मिलान किया जाता है।
इन विधियों से शोध के निष्कर्षों की विश्वसनीयता एवं वैधता में वृद्धि होती है।
प्रश्न-32. न्यायदर्शन के मुख्य स्तरों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- न्यादर्शन (Sampling) किसी जनसंख्या (population) से एक प्रतिनिधि समूह (sample) को चुनने की प्रक्रिया है। इसके मुख्य स्तर निम्नलिखित हैं:
जनसंख्या की परिभाषा (Defining Population): सबसे पहले उस जनसंख्या को स्पष्ट किया जाता है जिससे नमूना लिया जाना है।
नमूना इकाई का निर्धारण (Determining Sampling Unit): यह वह इकाई होती है जिससे नमूना लिया जाएगा, जैसे व्यक्ति, विद्यालय, क्षेत्र आदि।
नमूना फ्रेम तैयार करना (Preparing Sampling Frame): इसमें जनसंख्या के सभी सदस्य सूचीबद्ध किए जाते हैं।
नमूना आकार निर्धारण (Determining Sample Size): यह तय किया जाता है कि कितने लोगों या इकाइयों को नमूने में शामिल किया जाएगा।
नमूना चयन की विधि (Selecting Sampling Technique): संभाव्यता या असंभाव्यता में से किसी एक विधि का चयन किया जाता है।
नमूना एकत्रण (Sample Collection): चयनित विधि से नमूने को एकत्र किया जाता है।
नमूना का परीक्षण और विश्लेषण (Testing & Analysis): एकत्रित नमूने पर अनुसंधान किया जाता है।
प्रश्न-33. असम्भाव्य न्यादर्शन के प्रकारों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- असंभाव्यता न्यादर्शन (Non-Probability Sampling) वह विधि है जिसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने की समान संभावना नहीं होती। इसके मुख्य प्रकार हैं:
- सुविधाजनक न्यादर्शन (Convenience Sampling):
इसमें वे नमूने लिए जाते हैं जो आसानी से उपलब्ध होते हैं। यह सरल परंतु पक्षपातपूर्ण हो सकता है। - उद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन (Purposive Sampling):
इसमें चयनकर्ता अपने अनुभव और उद्देश्य के अनुसार उपयुक्त नमूने का चयन करता है। - कोटा न्यादर्शन (Quota Sampling):
इसमें जनसंख्या को कुछ वर्गों में बाँटा जाता है और प्रत्येक वर्ग से निर्धारित संख्या में नमूने लिए जाते हैं। - स्नोबॉल न्यादर्शन (Snowball Sampling):
इसमें एक व्यक्ति के माध्यम से अन्य प्रतिभागियों तक पहुँचा जाता है, जो विशेष समुदायों के लिए उपयोगी होता है।
यह विधियाँ विशेष परिस्थितियों में उपयोगी होती हैं, परंतु निष्कर्षों की सामान्यता सीमित होती है।
प्रश्न-34. चरों के मुख्य प्रकारों के बारे में चर्चा कीजिए।
उत्तर:- चर (Variable) वह गुण है जो विभिन्न इकाइयों में भिन्न हो सकता है। अनुसंधान में मुख्यतः निम्न प्रकार के चरों का प्रयोग होता है:
- स्वतंत्र चर (Independent Variable): यह वह चर होता है जिसे प्रयोगकर्ता नियंत्रित करता है। यह प्रभाव डालने वाला चर होता है।
- निर्भर चर (Dependent Variable): यह परिणाम का सूचक होता है और स्वतंत्र चर के कारण प्रभावित होता है।
- नियंत्रित चर (Controlled Variable): यह वे चर होते हैं जिन्हें स्थिर रखा जाता है ताकि उनका प्रभाव परिणाम पर न पड़े।
- मध्यस्थ चर (Intervening Variable): यह स्वतंत्र और निर्भर चर के बीच संबंध को प्रभावित करता है।
- मापक चर (Moderator Variable): यह स्वतंत्र चर और निर्भर चर के संबंध की दिशा या ताकत को बदलता है।
इन चरों की समझ अनुसंधान में संबंध स्थापित करने और विश्लेषण करने के लिए आवश्यक होती है।
प्रश्न-35. गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुसंधान में अन्तर लिखिए।
उत्तर:- SECTION-C
Section-C
प्रश्न-1.मनोवैज्ञानिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? इसको विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर:- मनोवैज्ञानिक अनुसंधान (Psychological Research) वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभूतियों, सोच, स्मृति, बुद्धि, अभिप्रेरणा आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह अनुसंधान व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलापों को समझने और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान खोजने में सहायक होता है।
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं— किसी व्यवहार या मानसिक घटना का वर्णन करना, भविष्यवाणी करना, नियंत्रण प्राप्त करना और सिद्धांत विकसित करना। यह अनुसंधान वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है और इसमें आंकड़ों का विश्लेषण, परीक्षण और निष्कर्ष शामिल होता है।
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के प्रकार:
- मौलिक अनुसंधान (Basic Research):
इसका उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करना होता है। यह सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होता है। जैसे – स्मृति की प्रक्रिया पर अध्ययन। - प्रयोगात्मक अनुसंधान (Experimental Research):
इसमें स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध को नियंत्रित परिस्थितियों में परीक्षण किया जाता है। - वर्णनात्मक अनुसंधान (Descriptive Research):
यह अनुसंधान किसी घटना, व्यक्ति या समूह के व्यवहार का निरीक्षण करके उसका वर्णन करता है। - सहसंबंधात्मक अनुसंधान (Correlational Research):
इसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच सांख्यिकीय संबंध की जांच की जाती है, परंतु कारण-प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जाता। - गुणात्मक अनुसंधान (Qualitative Research):
यह अनुसंधान अनुभव, सोच, दृष्टिकोण और सामाजिक संदर्भों की व्याख्या करता है। इसमें साक्षात्कार, केस स्टडी आदि तकनीकों का प्रयोग होता है। - मात्रात्मक अनुसंधान (Quantitative Research):
इसमें आंकड़ों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करके उनके विश्लेषण से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। - अन्वेषणात्मक अनुसंधान (Exploratory Research):
यह अनुसंधान किसी नये विषय, समस्या या व्यवहार की प्राथमिक समझ विकसित करने हेतु किया जाता है। - व्यवहारिक अनुसंधान (Applied Research):
यह अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है, जैसे – परीक्षा में भय को कम करना।
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन का महत्वपूर्ण साधन है, जिससे न केवल मनोविज्ञान का ज्ञान-विस्तार होता है, बल्कि समाज में उत्पन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.शोध समस्या को परिभाषित कीजिए। शोध समस्या चुनने का आधार बताइए।
उत्तर:- शोध समस्या (Research Problem) वह स्पष्ट, सुसंगत और महत्त्वपूर्ण विषय या प्रश्न होता है जिसे अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन का केन्द्र बनाता है। यह ऐसा बौद्धिक प्रश्न होता है जिसका उत्तर ज्ञात नहीं होता और जिसके समाधान के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है।
शोध समस्या की परिभाषा:
गुड और स्केट्स के अनुसार – “शोध समस्या वह कठिनाई या विरोधाभास है, जिसे अनुसंधान द्वारा हल करने की आवश्यकता होती है।”
शोध समस्या के लक्षण:
यह स्पष्ट, संक्षिप्त और संदेहात्मक होनी चाहिए।
इसका समाधान व्यावहारिक और उपयोगी होना चाहिए।
यह पूर्व साहित्य और तथ्यों से जुड़ी होनी चाहिए।
शोध समस्या चुनने के आधार:
- रुचि और प्रेरणा:
अनुसंधानकर्ता को उस विषय में व्यक्तिगत रुचि होनी चाहिए ताकि कार्य निरंतरता से पूर्ण हो सके। - प्रासंगिकता और उपयोगिता:
समस्या सामाजिक, शैक्षिक या व्यवहारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। - उपलब्ध संसाधन:
अनुसंधान के लिए आवश्यक समय, उपकरण, साहित्य, आँकड़े और मार्गदर्शक की उपलब्धता होनी चाहिए। - समस्या की नवीनता:
समस्या में नवीनता होनी चाहिए ताकि यह ज्ञान के विस्तार में सहायक हो। - सैद्धांतिक आधार:
समस्या किसी सिद्धांत या मॉडल पर आधारित हो ताकि उसका परीक्षण और विश्लेषण संभव हो सके। - नैतिकता:
समस्या का विषय नैतिक दृष्टिकोण से स्वीकार्य होना चाहिए। - मापन की सुविधा:
चुनी गई समस्या को मापना और आंकड़ों के माध्यम से परीक्षण करना संभव होना चाहिए।
शोध समस्या अनुसंधान की दिशा निर्धारित करती है। एक उपयुक्त समस्या का चयन अनुसंधान की सफलता में अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है।
प्रश्न-3. शोध अभिकल्प की विषयवस्तु का वर्णन कीजिए।
उत्तर:-शोध अभिकल्प (Research Design) किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान की आधारशिला होता है। यह एक रूपरेखा या योजना होती है, जिसके माध्यम से शोधकर्ता यह तय करता है कि अनुसंधान कैसे किया जाएगा, किस पद्धति से डाटा एकत्रित होगा, उसका विश्लेषण कैसे होगा तथा निष्कर्ष किस प्रकार निकाले जाएंगे।
शोध अभिकल्प की विषयवस्तु (Content) मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं से मिलकर बनी होती है:
- समस्या की स्पष्ट परिभाषा:
शोध अभिकल्प का प्रारंभ समस्या की स्पष्ट व्याख्या से होता है। यह बताता है कि शोध किस मुद्दे या प्रश्न पर केंद्रित है। - उद्देश्यों का निर्धारण:
शोध का उद्देश्य क्या है, इसे स्पष्ट रूप से अभिकल्प में दर्शाया जाता है। उद्देश्य विशेष रूप से अनुसंधान की दिशा और सीमा को निर्देशित करते हैं। - परिकल्पना (Hypothesis):
यदि अनुसंधान परिकल्पना-आधारित है तो अभिकल्प में स्पष्ट रूप से परिकल्पना का उल्लेख होता है। यह संभावित उत्तरों का पूर्वानुमान होता है जिसे परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। - जनसंख्या और नमूना:
शोध में अध्ययन की जाने वाली जनसंख्या तथा उस जनसंख्या से चयनित नमूने की प्रकृति, आकार और चयन की विधि को वर्णित किया जाता है। - डेटा संग्रह की विधियाँ:
शोध में प्रयुक्त डेटा संग्रह की विधियाँ (जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रयोग) तथा उनके औचित्य को भी विषयवस्तु में सम्मिलित किया जाता है। - उपकरण और साधन:
शोध में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, स्केल आदि की जानकारी भी दी जाती है। - डेटा विश्लेषण की योजना:
एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण कैसे किया जाएगा (जैसे सांख्यिकीय विधियाँ), इसका विवरण भी अभिकल्प का हिस्सा होता है। - समय और बजट:
अनुसंधान की अवधि और संभावित लागत का अनुमान भी शोध अभिकल्प में किया जाता है। - नैतिक विचार (Ethical Considerations):
शोध में गोपनीयता, प्रतिभागियों की सहमति और अन्य नैतिक मानकों को भी ध्यान में रखा जाता है।
शोध अभिकल्प किसी शोध कार्य का ब्लूप्रिंट होता है जो शोध को सुव्यवस्थित, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। इसके बिना अनुसंधान प्रक्रिया बिखरी हुई और अनियंत्रित हो सकती है।
प्रश्न-4. मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- मनोवैज्ञानिक परीक्षण (Psychological Test) व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक क्षमताओं, रुचियों, दृष्टिकोणों, व्यक्तित्व इत्यादि को मापने का एक वैज्ञानिक उपकरण है। इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति के मानसिक लक्षणों को परखा और मापा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की अनेक विशेषताएँ होती हैं जो उन्हें अन्य प्रकार के परीक्षणों से अलग बनाती हैं।
मनोवैज्ञानिक परीक्षण की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- मानकीकरण (Standardization):
मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि वह निश्चित प्रक्रियाओं और शर्तों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होता है। इससे परिणामों की तुलनात्मकता सुनिश्चित होती है। - विश्वसनीयता (Reliability):
परीक्षण के परिणाम बार-बार देने पर समान आएँ, इसे विश्वसनीयता कहते हैं। एक विश्वसनीय परीक्षण में त्रुटियाँ न्यूनतम होती हैं। - वैधता (Validity):
परीक्षण वास्तव में वही मापता है जिसके लिए उसे निर्मित किया गया है। यदि कोई बुद्धि परीक्षण वास्तव में बुद्धि को मापता है, तभी वह वैध है। - वस्तुनिष्ठता (Objectivity):
परीक्षण का मूल्यांकन किसी भी व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होता है। परिणामों का निर्धारण निश्चित मानदंडों पर आधारित होता है। - संवेदनशीलता (Sensitivity):
मनोवैज्ञानिक परीक्षण इतने संवेदनशील होते हैं कि वे व्यक्ति के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अंतर को भी पहचान सकते हैं। - तुलनात्मकता (Comparability):
इन परीक्षणों द्वारा प्राप्त स्कोर को अन्य व्यक्तियों या समूहों के स्कोर से तुलनात्मक रूप से देखा जा सकता है। - प्रयोग में सरलता:
अच्छे परीक्षणों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उनका प्रयोग करना सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो। - मूल्यांकन की सुविधा:
परीक्षणों में स्कोरिंग कुंजी होती है जिससे अंकों का निष्कर्ष निकालना आसान होता है। - उपयोगिता:
मनोवैज्ञानिक परीक्षण शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं।
मनोवैज्ञानिक परीक्षण वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए गए उपकरण होते हैं जो व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं और विशेषताओं को मापने में सहायक होते हैं। इनकी विशेषताएँ इन्हें प्रभावी और विश्वसनीय बनाती हैं।
प्रश्न-5. प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है? इसकी विशेषताएँ एवं महत्व बताइए।
उत्तर:- प्रयोगात्मक अनुसंधान (Experimental Research) एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें किसी विशिष्ट स्थिति या वातावरण में स्वतंत्र चर (Independent Variable) में परिवर्तन कर यह देखा जाता है कि उससे आश्रित चर (Dependent Variable) पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह अनुसंधान नियंत्रित प्रयोगशाला या कक्षाओं में किया जाता है, जिससे कारण-प्रभाव संबंध स्थापित किया जा सके।
प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषताएँ:
- नियंत्रण (Control):
इसमें अनुसंधानकर्ता सभी बाहरी चरों को नियंत्रित करता है ताकि केवल स्वतंत्र चर का प्रभाव ही आश्रित चर पर पड़े। - कारण-प्रभाव संबंध:
यह अनुसंधान यह स्पष्ट करता है कि किसी विशेष कारण (चर) के कारण कौन-सा परिणाम हुआ। - परिकल्पना परीक्षण:
इसमें अनुसंधानकर्ता एक परिकल्पना को पूर्वनिर्धारित करता है और प्रयोग के द्वारा उसे परीक्षण करता है। - पूर्व और पश्च परीक्षण:
एक ही समूह पर परीक्षण से पहले और बाद में मापन किया जाता है, जिससे अंतर की तुलना की जा सके। - प्रयोग और नियंत्रण समूह:
एक समूह पर स्वतंत्र चर लागू किया जाता है (प्रयोग समूह), जबकि दूसरे पर नहीं (नियंत्रण समूह)।
प्रयोगात्मक अनुसंधान का महत्व:
- विश्वसनीयता और वैधता:
यह अनुसंधान विधि सबसे विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ मानी जाती है। - नवीन सिद्धांतों का विकास:
नए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। - व्यवहारिक समस्याओं का समाधान:
व्यवहार, अधिगम, स्मृति, चिंता आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान इस अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है। - शैक्षिक सुधार:
शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, कक्षा प्रबंधन आदि के प्रभावी प्रयोग में सहायता मिलती है। - नैतिक शोध दृष्टिकोण:
यह अनुसंधान वैज्ञानिकता, तर्कशीलता और निष्पक्षता की कसौटियों पर खरा उतरता है।
प्रयोगात्मक अनुसंधान मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक शक्तिशाली उपकरण है, जिससे वैज्ञानिक तरीके से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और कारणात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
प्रश्न-6. परिकल्पना के विभिन्न वर्गीकरणों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:-परिकल्पना (Hypothesis) वह तात्कालिक उत्तर होता है जिसे परीक्षण द्वारा सत्यापित किया जाता है। यह अनुसंधान की दिशा तय करती है। परिकल्पना के विभिन्न वर्गीकरण निम्नलिखित हैं:
- प्रकृति के आधार पर:
सकारात्मक परिकल्पना (Positive Hypothesis):
जब दो चरों के बीच प्रत्यक्ष संबंध बताया जाए।
उदाहरण: “अधिक अध्ययन से परीक्षा परिणाम बेहतर होते हैं।”
नकारात्मक परिकल्पना (Negative Hypothesis):
जब दो चरों के बीच विपरीत संबंध बताया जाए।
उदाहरण: “तनाव बढ़ने से कार्य क्षमता घटती है।”
- संरचना के आधार पर:
सरल परिकल्पना (Simple Hypothesis):
इसमें दो चरों के बीच संबंध होता है।
उदाहरण: “नींद की अवधि और एकाग्रता में संबंध होता है।”
जटिल परिकल्पना (Complex Hypothesis):
इसमें एक से अधिक स्वतंत्र या निर्भर चरों के बीच संबंध दर्शाया जाता है।
उदाहरण: “पोषण, व्यायाम और नींद, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।”
- दिशा के आधार पर:
दिशात्मक परिकल्पना (Directional Hypothesis):
इसमें संबंध की दिशा स्पष्ट होती है।
उदाहरण: “योग अभ्यास से चिंता में कमी आती है।”
अदिशात्मक परिकल्पना (Non-directional Hypothesis):
इसमें केवल संबंध होने की बात कही जाती है, दिशा नहीं बताई जाती।
उदाहरण: “योग अभ्यास और चिंता के बीच कोई संबंध है।”
- परीक्षण की विधि के आधार पर:
शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis – H₀):
यह मानती है कि कोई प्रभाव या संबंध नहीं है।
उदाहरण: “योग और चिंता के बीच कोई संबंध नहीं है।”
वैकल्पिक परिकल्पना (Alternative Hypothesis – H₁):
यह मानती है कि प्रभाव या संबंध मौजूद है।
उदाहरण: “योग और चिंता के बीच संबंध है।”
परिकल्पना अनुसंधान की रीढ़ होती है। इसके विभिन्न प्रकार अनुसंधान की आवश्यकता, उद्देश्य और विधियों पर निर्भर करते हैं। सही परिकल्पना से निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय बनते हैं।
प्रश्न-7. असंभाव्य न्यादर्श के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- न्यादर्शन (Sampling) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनसंख्या से कुछ प्रतिनिधि इकाइयाँ चुनी जाती हैं। असंभाव्य न्यादर्श (Non-Probability Sampling) में प्रत्येक इकाई को चयन में समान अवसर नहीं मिलता। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:
- सुविधाजनक न्यादर्श (Convenience Sampling):
इसमें शोधकर्ता अपने निकट, उपलब्ध और सरल इकाइयों का चयन करता है।
उदाहरण: विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध छात्रों पर अध्ययन करना। - उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श (Purposive or Judgmental Sampling):
इसमें शोधकर्ता अपने अनुभव और उद्देश्य के अनुसार उपयुक्त इकाइयों का चयन करता है।
उदाहरण: केवल अनुभवयुक्त शिक्षकों का चयन कर उनके कार्य-प्रदर्शन पर शोध। - कोटा न्यादर्श (Quota Sampling):
इसमें जनसंख्या को कुछ श्रेणियों में बाँटकर प्रत्येक श्रेणी से निर्धारित संख्या में इकाइयाँ ली जाती हैं।
उदाहरण: महिला और पुरुष उपभोक्ताओं से समान संख्या में नमूना लेना। - स्नोबॉल न्यादर्श (Snowball Sampling):
यह उन जनसंख्याओं के लिए प्रयोग होता है जो छिपी हुई या दुर्लभ हों। एक इकाई से दूसरी, फिर तीसरी ऐसे श्रृंखला में नमूने प्राप्त किए जाते हैं।
उदाहरण: मादक द्रव्य उपयोगकर्ताओं का अध्ययन। - स्वेच्छिक न्यादर्श (Voluntary Sampling):
इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो स्वयं अनुसंधान में भाग लेने के लिए आगे आते हैं।
उदाहरण: अखबार में विज्ञापन देकर इच्छुक उत्तरदाताओं से डाटा प्राप्त करना।
असंभाव्य न्यादर्श विधियाँ तब उपयोगी होती हैं जब संसाधन सीमित हों, या संभाव्य विधियाँ व्यावहारिक न हों। हालांकि, इनके परिणाम सामान्यीकरण के लिए सीमित होते हैं लेकिन विशेष प्रकार के अनुसंधानों में यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं।
प्रश्न-8. मनोवैज्ञानिक परीक्षण का स्वरूप एवं प्रकार विस्तार से बताइए।
उत्तर:- मनोवैज्ञानिक परीक्षण (Psychological Test) एक मापन उपकरण है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं जैसे – बुद्धि, अभिप्रेरणा, स्मृति, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, रुचि, रचनात्मकता आदि का मूल्यांकन किया जाता है।
यह परीक्षण एक मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत होता है जिसमें उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को संख्यात्मक रूप में प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया जाता है।
मनोवैज्ञानिक परीक्षण का स्वरूप (Nature):
- मानकीकरण (Standardization):
सभी उत्तरदाताओं के लिए समान प्रक्रिया, समय और सामग्री प्रयोग की जाती है। - विश्वसनीयता (Reliability):
परीक्षण बार-बार एक जैसे परिणाम देता है तो वह विश्वसनीय माना जाता है। - वैधता (Validity):
परीक्षण वह मापता है जो वास्तव में मापना चाहता है। - उद्देश्यपूर्णता:
परिणामों का विश्लेषण निष्पक्षता के आधार पर किया जाता है। - सांख्यिकीय आधार:
स्कोरिंग व व्याख्या सांख्यिकीय विधियों पर आधारित होती है।
मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार:
- बुद्धिलब्धि परीक्षण (Intelligence Tests):
जैसे – स्टैनफोर्ड-बिनेट टेस्ट, वेश्लर इंटेलिजेंस स्केल। - व्यक्तित्व परीक्षण (Personality Tests):
निरपेक्ष परीक्षण (Objective Tests): जैसे – MMPI, 16 PF।
प्रक्षेपी परीक्षण (Projective Tests): जैसे – रोर्शाच इंकब्लॉट टेस्ट, TAT।
- रुचि परीक्षण (Interest Tests):
छात्रों या कर्मियों की अभिरुचियों का मापन करने वाले परीक्षण। - दृष्टिकोण परीक्षण (Attitude Tests):
जैसे – सामाजिक मुद्दों पर दृष्टिकोण का मापन। - अभिप्रेरणा परीक्षण (Motivation Tests):
जैसे – नीड फॉर अचीवमेंट स्केल। - प्राप्ति परीक्षण (Achievement Tests):
यह किसी विषय में अर्जित ज्ञान या दक्षता को मापते हैं। - रचनात्मकता परीक्षण (Creativity Tests):
जैसे – टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग।
मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसी व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक व भावनात्मक विशेषताओं को मापने का वैज्ञानिक साधन है। इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति की क्षमताओं को समझकर उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा सकती है।
प्रश्न-9. उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से शोध प्रस्ताव तैयार करने के सोपानों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:-शोध प्रस्ताव (Research Proposal) एक पूर्व योजना होती है जिसमें अनुसंधान की समस्या, उद्देश्य, पद्धति, उपकरण तथा संभावित निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण होता है। एक अच्छा शोध प्रस्ताव अनुसंधान कार्य की दिशा निर्धारित करता है। शोध प्रस्ताव तैयार करने के निम्नलिखित मुख्य सोपान होते हैं:
- समस्या की पहचान (Identification of Problem):
सबसे पहले शोधार्थी को एक उपयुक्त, नवीन और शोधयोग्य समस्या का चयन करना होता है। जैसे- “विद्यालयों में छात्र तनाव के कारणों का अध्ययन” एक शोध समस्या हो सकती है। - समीक्षा साहित्य (Review of Literature):
पूर्व में संबंधित विषय पर हुए कार्यों का गहन अध्ययन किया जाता है। इससे शोध की नवीनता और उपयोगिता स्पष्ट होती है। - उद्देश्यों का निर्धारण (Formulation of Objectives):
शोध के स्पष्ट और मापनीय उद्देश्य तय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, “विद्यालयी छात्रों में तनाव के मुख्य कारणों की पहचान करना” एक उद्देश्य हो सकता है। - परिकल्पना का निर्माण (Formulation of Hypothesis):
यदि शोध परिकल्पना-आधारित है, तो संभाव्य उत्तरों का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। जैसे: “विद्यार्थियों में परीक्षा तनाव का मुख्य कारण माता-पिता की अपेक्षाएँ हैं।” - शोध पद्धति का चयन (Selection of Methodology):
शोध का प्रकार (मात्रात्मक/गुणात्मक), नमूना आकार, उपकरण, आँकड़ा संग्रहण की विधि आदि का निर्धारण किया जाता है। - डेटा संग्रहण तकनीक (Tools and Techniques):
प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन आदि विधियों का विवरण दिया जाता है। - डेटा विश्लेषण (Data Analysis):
संग्रहित डेटा को किस सांख्यिकीय विधियों से विश्लेषित किया जाएगा, इसका वर्णन किया जाता है। - समय-सीमा और बजट (Time Schedule and Budget):
कार्य योजना को चरणबद्ध रूप में समय और व्यय के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। - महत्व और अपेक्षित निष्कर्ष (Significance and Expected Outcomes):
शोध के सामाजिक, शैक्षिक या वैज्ञानिक महत्व का उल्लेख किया जाता है।
उदाहरण:
अगर कोई शोधार्थी “कॉलेज छात्रों में मोबाइल की लत” पर शोध करना चाहता है, तो वह समस्या का चयन, उद्देश्य निर्धारण, पुराने शोधों की समीक्षा, एक सर्वेक्षण आधारित प्रश्नावली, 100 छात्रों का यादृच्छिक चयन और सांख्यिकीय विश्लेषण की योजना बनाएगा।
प्रश्न-10. मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की प्रकृति का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- मनोवैज्ञानिक अनुसंधान (Psychological Research) मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका उद्देश्य व्यवहार को समझना, व्याख्या करना, भविष्यवाणी करना और आवश्यकता होने पर नियंत्रण करना होता है। यह अनुसंधान विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, प्रयोगों, और आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित होता है।
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की प्रकृति की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- वैज्ञानिक प्रकृति:
यह वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है, जिसमें समस्याओं की पहचान, परिकल्पना निर्माण, डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष शामिल होते हैं। - व्यवहार केंद्रित:
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान मानव और कभी-कभी पशु व्यवहार को केंद्र में रखता है, जैसे—सीखना, स्मृति, भावनाएँ, प्रेरणा आदि। - प्रेक्षण और प्रयोग आधारित:
इसमें प्रयोगशाला और क्षेत्र में प्रयोग तथा व्यवस्थित प्रेक्षण की सहायता से डेटा संग्रह किया जाता है। - मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों:
यह अनुसंधान मात्रात्मक (संख्यात्मक) आँकड़ों के साथ-साथ गुणात्मक (गुणवत्ता आधारित) जानकारी पर भी आधारित होता है। - उद्देश्यपरकता:
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होता है। शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों का इसमें कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। - नैतिकता आधारित:
इसमें शोध प्रतिभागियों की गोपनीयता, स्वैच्छिक भागीदारी और कल्याण का विशेष ध्यान रखा जाता है। - सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण:
यह अनुसंधान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पुष्टि करता है और उन्हें व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में लागू करता है। - विकसित होता क्षेत्र:
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निरंतर विकसित हो रहा है और नये-नये क्षेत्रों जैसे—साइकोलॉजिकल ए.आई., न्यूरोसाइंस आदि को भी समाहित करता है।
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और उद्देश्यपरक प्रयास है, जिसका लक्ष्य मानव व्यवहार को समझना और समाज तथा व्यक्ति के कल्याण हेतु उसका उपयोग करना है।
प्रश्न-11. अनुसन्धान के सन्दर्भ में जनसंख्या के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- अनुसंधान में ‘जनसंख्या’ (Population) का तात्पर्य उस समूह से है जिससे संबंधित तथ्यों और आँकड़ों को एकत्र किया जाता है। यह समूह व्यक्ति, वस्तु, घटनाएँ या संस्थाएँ हो सकते हैं जिनका अध्ययन किसी विशेष शोध उद्देश्य के लिए किया जाता है।
जनसंख्या के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं:
- लक्ष्य जनसंख्या (Target Population):
यह वह संपूर्ण समूह होता है जिसके बारे में शोधकर्ता निष्कर्ष निकालना चाहता है। जैसे—भारत के सभी कॉलेज छात्र। - नमूना योग्य जनसंख्या (Accessible Population):
यह लक्ष्य जनसंख्या का वह भाग होता है जिसे शोधकर्ता वास्तविक रूप से संपर्क कर सकता है। उदाहरण—किसी एक राज्य के कॉलेज छात्र। - नमूना (Sample):
जनसंख्या का वह छोटा भाग जिसे अध्ययन के लिए चुना जाता है। यह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। नमूना जितना अच्छा होगा, निष्कर्ष उतने ही सटीक होंगे। - सांख्यिकीय जनसंख्या:
इसमें प्रत्येक तत्व का विश्लेषण आँकड़ों और संख्यात्मक विधियों से किया जाता है। यह मात्रात्मक शोध में अधिक उपयोगी होती है। - सैद्धांतिक जनसंख्या (Theoretical Population):
यह वह आदर्श समूह होता है जिसके आधार पर शोध मॉडल तैयार किया जाता है, चाहे वह वास्तविक रूप में उपलब्ध न हो। - सामयिक जनसंख्या (Temporal Population):
किसी विशेष समय अवधि में उपलब्ध जनसंख्या को इस श्रेणी में रखा जाता है, जैसे—COVID-19 महामारी के दौरान मरीजों की जनसंख्या। - भौगोलिक जनसंख्या (Geographic Population):
किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या, जैसे—दिल्ली के स्कूली बच्चे।
अनुसंधान में जनसंख्या की स्पष्ट पहचान आवश्यक होती है क्योंकि इसका सही चयन अनुसंधान की विश्वसनीयता, वैधता और उपयोगिता को निर्धारित करता है। शोधकर्ता को जनसंख्या के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ही उपयुक्त नमूना चुनना चाहिए।
प्रश्न-12. साधारण यादृच्छिक न्यादर्श की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:-साधारण यादृच्छिक नमूनाकरण (Simple Random Sampling) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। इसकी प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं:
- लॉटरी विधि (Lottery Method):
यह सबसे सरल विधि है। जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को एक संख्या दी जाती है और फिर लॉटरी ड्रा के माध्यम से आवश्यक संख्या चुनी जाती है।
उदाहरण: 100 छात्रों में से 10 छात्रों को चुनना हो, तो 100 पर्चियाँ बनाकर एक बॉक्स में डालकर 10 पर्चियाँ निकाली जाती हैं। - सारणी विधि (Table of Random Numbers):
इसमें सांख्यिकीय पुस्तक में दी गई यादृच्छिक अंकों की सारणी (जैसे टिश्यूरी की तालिका) का प्रयोग कर चयन किया जाता है।
उदाहरण: यदि छात्र क्रमांक 001 से 500 तक हैं, तो यादृच्छिक अंकों की तालिका से 10 उपयुक्त संख्याएँ लेकर चयन किया जाता है। - कंप्यूटर आधारित चयन (Computer Based Random Selection):
आधुनिक समय में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे MS Excel, SPSS आदि की सहायता से यादृच्छिक संख्याएँ उत्पन्न कर नमूना चुना जाता है।
उदाहरण: Excel में =RANDBETWEEN(1,100) कमांड से यादृच्छिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। - डाइस रोलिंग विधि (Dice Method):
यह छोटे नमूनों के लिए उपयुक्त है। उदाहरणतः पासे को कई बार फेंककर प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाता है।
विशेषताएँ:
सभी इकाइयों को चयन का समान अवसर होता है।
पक्षपात रहित पद्धति होती है।
सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त।
साधारण यादृच्छिक नमूनाकरण अनुसंधान में निष्पक्षता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत प्रभावी है।
vmou MAPSY-01 paper , vmou MA 1ST YEAR year exam paper ,vmou exam paper 2030 vmou exam paper 2029-28 vmou exam paper 2027 vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4
VMOU EXAM PAPER