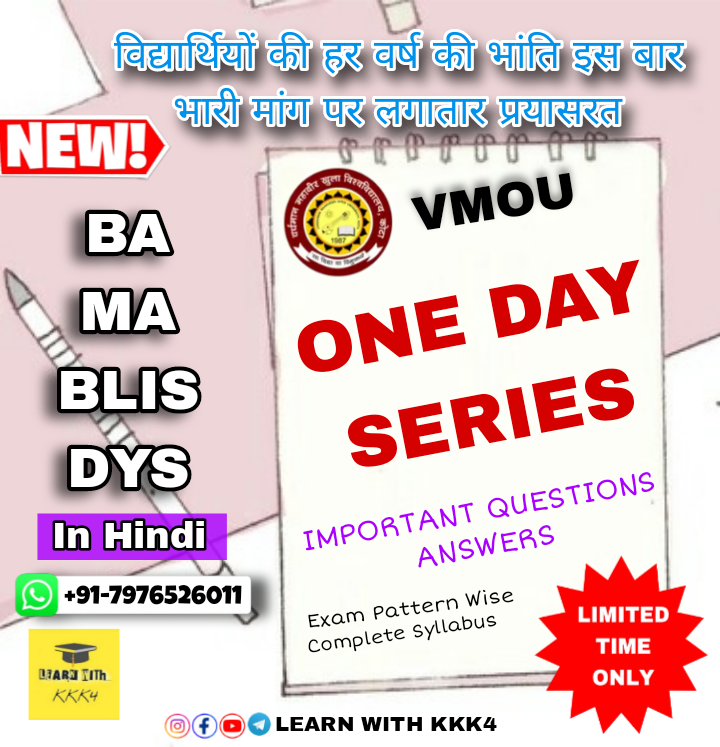VMOU MAPS-05 Paper MA Final Year ; vmou exam paper
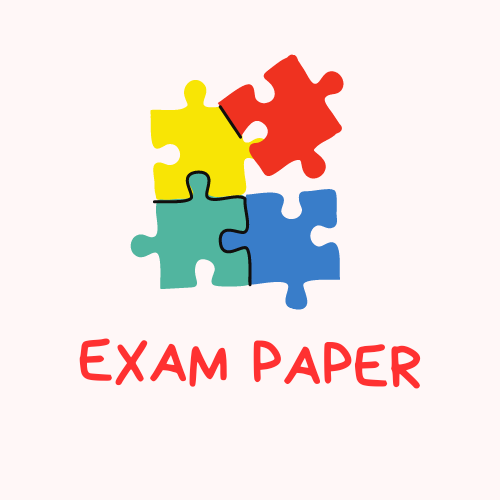
VMOU MA Final Year के लिए राजनीति विज्ञान ( MAPS-05 , ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं दो विचारकों के नाम का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोज़िक।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.समुदायवादी राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:- यह सिद्धांत व्यक्ति की पहचान और नैतिकता को समुदाय और संस्कृति से जुड़ा मानता है, न कि स्वतंत्र रूप से।
प्रश्न-3.परम्परागत राजनीति सिद्धान्त क्या है?
उत्तर:- परम्परागत राजनीति सिद्धान्त राजनीति के नैतिक, दार्शनिक व संस्थागत पक्षों पर ध्यान देता है, जिसमें न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता आदि मूल्यों की विवेचना की जाती है।
प्रश्न-4. परम्परागत राजनीतिक सिद्धांत की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- यह नैतिक मूल्यों और आदर्श राज्य की संकल्पना पर आधारित होता है; साथ ही ऐतिहासिक ग्रंथों और दर्शन पर अधिक निर्भर करता है।
प्रश्न-5. समुदायवादी राजनीति सिद्धान्त के किन्हीं दो विचारकों के नाम बताइए।
उत्तर:- चार्ल्स टेलर और माइकल सैंडल
प्रश्न-6. क्लासिकल राजनीति दर्शन के पुनः उद्भव से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- क्लासिकल राजनीति दर्शन के पुनः उद्भव का अर्थ है प्लेटो, अरस्तू जैसे दार्शनिकों के नैतिक और सामाजिक मूल्यों की आधुनिक राजनीति में वापसी।
प्रश्न-7. परम्परागत राजनीति सिद्धान्त के कोई दो विचारकों के नाम का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- प्लेटो और अरस्तू
प्रश्न-8. आधुनिक राजनीति सिद्धान्त की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- आधुनिक राजनीति सिद्धान्त आलोचनात्मक विश्लेषण पर आधारित होता है और यह बहुलवाद तथा स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर बल देता है।
प्रश्न-9. निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए:
उत्तर:- (अ) Anarchy, State and Utopia — रॉबर्ट नोज़िक
(ब) After Virtue — अलैस्टेयर मैकइंटायर
प्रश्न-10. निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए :
उत्तर:- अ) After Virtue: A Study in Moral Theory
उत्तर: इस पुस्तक के लेखक एलास्डेयर मैकइंटायर (Alasdair MacIntyre) हैं।
(ब) Anarchy, State and Utopia
उत्तर: इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट नोज़िक (Robert Nozick) हैं।
प्रश्न-11. निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए:
उत्तर:- (अ) Rationalism in Politics — माइकल ओकेशॉट
(च) Spheres of Justice — माइकल वॉल्ज़र
प्रश्न-12. निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए:
उत्तर:- (अ) सोर्सेज ऑफ दि सेल्फ — चार्ल्स टेलर
(ब) स्फिअर्स ऑफ जस्टिस — माइकल वाल्ज़र
प्रश्न-13. एरिक श्रोगेलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है?
उत्तर:-एरिक वोगेलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान मनुष्य के अस्तित्व और आदेश (Order) की खोज है, जो आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अनुभवों से जुड़ा होता है।
प्रश्न-14. राजनीतिक दर्शन के कैंब्रिज स्कूल से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- कैंब्रिज स्कूल राजनीतिक विचारों को उनके ऐतिहासिक संदर्भों में समझने की पद्धति को अपनाता है।
प्रश्न-15. व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:-व्यवहारवादी सिद्धान्त राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है, जो आंकड़ों, व्यवहार, मतदाता प्रवृत्तियों और अनुभवजन्य विधियों पर आधारित होता है।
प्रश्न-16. अनभिज्ञता के आवरण” से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:- यह जॉन रॉल्स की अवधारणा है, जिसमें व्यक्ति बिना अपनी सामाजिक स्थिति जाने न्याय के सिद्धांत तय करता है
प्रश्न-17. ‘अत्यल्प राज्य’ पर नोज़िक के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:-नोज़िक ने अत्यल्प राज्य को वैध माना, जो केवल सुरक्षा, अनुबंध पालन और न्याय सुनिश्चित करने तक सीमित हो।
प्रश्न-18. ऑकशॉट के अनुसार अन्वेषण की किन्हीं दो विधियों के नाम बताइए।
उत्तर:-ऑकशॉट के अनुसार अन्वेषण की दो विधियाँ हैं— ऐतिहासिक पद्धति और दार्शनिक पद्धति।
प्रश्न-19. रॉल्स के अनुसार ‘मूल स्थिति’ क्या है?
उत्तर:-रॉल्स की ‘मूल स्थिति’ एक काल्पनिक स्थिति है जहाँ व्यक्ति न्याय के सिद्धांत तय करने के लिए पर्दा अज्ञान के पीछे होते हैं।
प्रश्न-20. नैतिक दर्शन की वर्तमान स्थिति पर मैकण्टायर के विचारों का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- मैकइंटायर का मानना है कि आधुनिक नैतिक दर्शन विखंडित हो गया है और पारंपरिक सद्गुणों की पुनर्स्थापना आवश्यक है।
प्रश्न-21. नवकान्टवादी राजनीति सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- नवकान्टवादी सिद्धान्त इमानुएल कांट की नैतिकता व तर्कशीलता पर आधारित है, जो स्वतंत्रता व न्याय पर बल देता है।
प्रश्न-22. न्याय के अधिकृतता के सिद्धान्त में आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- यह सिद्धान्त रॉबर्ट नोज़िक द्वारा प्रतिपादित है, जिसमें संपत्ति पर अधिकार न्यायपूर्ण अधिग्रहण, स्थानांतरण और सुधार के सिद्धांतों से तय होता है।
प्रश्न-23. “आधुनिक स्व” से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:- “आधुनिक स्व” का तात्पर्य एक आत्मसचेत, स्वतंत्र और विवेकशील व्यक्ति से है जो अपनी पहचान स्वयं निर्धारित करता है।
प्रश्न-24. इतिहास पर वोगेलिन के विचार बताइए।
उत्तर:- वोगेलिन इतिहास को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मानते हैं जो मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक खोज को दर्शाता है।
प्रश्न-25. विकसित राजनीतिक सिद्धान्त में मैकइण्टायर के दो योगदानों का उल्लेख कीजिए
उत्तर:- मैकइण्टायर ने नैतिकता के सामुदायिक आधार और सद्गुणों की राजनीति (Virtue Ethics) को पुनः स्थापित किया और “After Virtue” जैसी कृति प्रस्तुत की।
प्रश्न-26. मैकइंटायर के अनुसार उदारवाद की दो आलोचनाएँ:
उत्तर:- यह परंपरा और नैतिकता से कटा हुआ है।
यह व्यक्तिवाद को अत्यधिक प्राथमिकता देता है।
प्रश्न-27. मैकइंटायर के अनुसार नैतिक पतन के किन्हीं दो चरणों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- मैकइंटायर के अनुसार नैतिक पतन के चरण हैं— परंपरागत नैतिक ढांचे का विघटन और नैतिक भाषा का विखंडन।
प्रश्न-28. मार्क्सवाद की मैकइंटायर द्वारा आलोचना की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- मैकइंटायर ने मार्क्सवाद की आधुनिकता और नैतिकता की विफलता की आलोचना करते हुए सामुदायिक नैतिकता पर बल दिया।
प्रश्न-29. राजनीतिक यथार्थ पर योगेलिन के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- योगेलिन ने राजनीतिक यथार्थ को आध्यात्मिक अनुभव और प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों से जोड़ा, जिसे आधुनिकता भुला चुकी है।
प्रश्न-30. मूल संरचना पर रॉल्स के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- रॉल्स के अनुसार मूल संरचना समाज की न्याय प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के संस्थानों की मूलभूत रूपरेखा होती है।
प्रश्न-31. इच्छा स्वतंत्रवादी राजनीति सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- इच्छा स्वतंत्रवादी सिद्धान्त व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकार को सर्वोच्च मानते हुए राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करना चाहता है।
Section-B
प्रश्न-1.’अनिश्चितता के आवरण’ पर रॉल्स के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक A Theory of Justice में ‘अनिश्चितता का आवरण’ (Veil of Ignorance) एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह विचार “मौलिक निष्पक्षता” को स्थापित करने हेतु दिया गया है। रॉल्स के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के तहत न्यायसंगत समाज की संरचना करना चाहे, तो उसे एक काल्पनिक स्थिति में होना चाहिए — जिसे वह ‘मूल स्थिति’ (Original Position) कहते हैं।
इस स्थिति में, व्यक्ति को अपनी जाति, लिंग, धर्म, वर्ग, योग्यता और आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं होती। इसे ही ‘अनिश्चितता का आवरण’ कहा गया है। इस स्थिति में, लोग अपने स्वार्थ से परे जाकर समाज के लिए न्यायपूर्ण सिद्धांतों का चयन करेंगे, जिससे समाज में समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी।
रॉल्स के अनुसार, इस स्थिति में दो न्याय के सिद्धांत उभरते हैं — (1) समान स्वतंत्रता का सिद्धांत और (2) सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब वे सबसे कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाएं। इस प्रकार, रॉल्स का ‘अनिश्चितता का आवरण’ सामाजिक न्याय की निष्पक्ष आधारशिला प्रस्तुत करता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.बर्लिन के ‘स्वतंत्रता की दो अवधारणाओं’ की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- आइज़ैाह बर्लिन ने स्वतंत्रता की दो प्रमुख अवधारणाएँ प्रस्तुत कीं — नकारात्मक स्वतंत्रता (Negative Liberty) और सकारात्मक स्वतंत्रता (Positive Liberty)। उनका प्रसिद्ध निबंध Two Concepts of Liberty 1958 में प्रकाशित हुआ।
नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी अवरोधों की अनुपस्थिति — अर्थात् जब व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करने की स्वतंत्रता हो। यह विचार मुख्यतः उदारवादियों द्वारा समर्थित है जो मानते हैं कि राज्य को व्यक्तिगत मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए।
सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है आत्म-नियंत्रण या आत्म-निर्णय की क्षमता — व्यक्ति का अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का अधिकार। यह विचार सामूहिकता और कल्याणकारी राज्य के पक्ष में जाता है, जिसमें राज्य व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के विकास हेतु आवश्यक संसाधन प्रदान करता है।
बर्लिन ने चेताया कि सकारात्मक स्वतंत्रता यदि अत्यधिक रूप ले ले, तो यह अधिनायकवाद को जन्म दे सकती है। उन्होंने संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रकार, बर्लिन की यह अवधारणा स्वतंत्रता की प्रकृति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
प्रश्न-3.उदारवाद की आलोचना पर मैकइण्टायर के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- एलेस्टेयर मैकइण्टायर एक प्रसिद्ध समुदायवादी (Communitarian) विचारक हैं जिन्होंने आधुनिक उदारवाद की आलोचना की है। उनकी पुस्तक After Virtue (1981) में उन्होंने नैतिकता और राजनीतिक विचार के पतन पर प्रकाश डाला।
मैकइण्टायर का मानना है कि उदारवाद व्यक्ति को एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखता है, जो समुदाय और परंपरा से अलग है। वह कहते हैं कि यह दृष्टिकोण व्यक्ति की पहचान और नैतिक विकास की वास्तविकता को नजरअंदाज करता है। उनके अनुसार, व्यक्ति का अस्तित्व और नैतिकता समुदाय, परंपरा और सामाजिक भूमिका से जुड़ा होता है।
उदारवाद द्वारा प्रस्तुत ‘न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत’ मैकइण्टायर को अस्वीकार्य लगते हैं, क्योंकि वे स्थानीय संस्कृति, नैतिकता और ऐतिहासिक अनुभवों को महत्व नहीं देते। वे मानते हैं कि नैतिकता और न्याय के मूल्य ऐतिहासिक संदर्भों में विकसित होते हैं।
इस प्रकार, मैकइण्टायर ने उदारवाद की व्यक्तिगतता की अवधारणा की आलोचना करते हुए, एक नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जो समुदाय पर आधारित हो।
प्रश्न-राजनीति सिद्धान्त को वीगेलिन के योगदान की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- एरिक वीगेलिन एक राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीति और आध्यात्मिकता के बीच गहरे संबंध पर जोर दिया। वे मानते थे कि राजनीतिक व्यवस्था का पतन तभी होता है जब वह आध्यात्मिक वास्तविकता से कट जाती है। उनकी प्रमुख कृति “The New Science of Politics” में उन्होंने प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि समाज में व्यवस्था केवल तभी संभव है जब वह “ऑर्डर ऑफ बीइंग” यानी अस्तित्व की संरचना से मेल खाती हो। वीगेलिन ने आधुनिक विचारधाराओं, विशेष रूप से मार्क्सवाद और नाजीवाद को “ग्नोस्टिक” कहकर खारिज किया क्योंकि वे अधार्मिक रूप से स्वर्ग को धरती पर लाना चाहते थे। उनका योगदान इस बात में रहा कि उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता संघर्ष न मानकर उसे आध्यात्मिक अनुशासन और नैतिक मार्गदर्शन का साधन माना। इससे राजनीतिक सिद्धान्त को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखने की नई दिशा मिली।
प्रश्न-5.एक समुदायवादी राजनीतिक विचारक के रूप में मैकइण्टायर के योगदान की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- एलेस्टेयर मैकइण्टायर ने After Virtue (1981) में समुदायवादी विचारधारा को मजबूती प्रदान की। उन्होंने आधुनिक नैतिक और राजनीतिक विचार को आलोचना का विषय बनाया और ‘सद्गुणों’ (Virtues) की पुनर्परिभाषा की।
मैकइण्टायर के अनुसार, नैतिकता केवल तर्क या सिद्धांतों से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से विकसित परंपराओं और सामाजिक भूमिकाओं से निकलती है। उन्होंने यह कहा कि आधुनिक समाज में नैतिकता व्यक्तिगत पसंद बन गई है, जिससे सामाजिक सामंजस्य और उद्देश्य समाप्त हो गया है।
समुदायवादी दृष्टिकोण में व्यक्ति की पहचान, उसके समुदाय, संस्कृति और परंपरा से जुड़ी होती है। मैकइण्टायर ने यह स्पष्ट किया कि न्याय और सद्गुण की समझ केवल ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों में की जा सकती है।
उनका विचार है कि किसी भी समाज को नैतिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें परंपरा, नैतिक अनुशासन और सामुदायिक मूल्यों को पुनर्जीवित किया जाए। इस प्रकार, वे समुदायवादी राजनीतिक सिद्धांत को गहराई और दिशा प्रदान करते हैं।
प्रश्न-6.राजनीति सिद्धान्त को बर्लिन के योगदान की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- आइज़ैया बर्लिन एक प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतकार थे जिन्होंने स्वतंत्रता और बहुलतावाद की अवधारणा को नया दृष्टिकोण दिया। उनकी सबसे चर्चित अवधारणा “नकारात्मक” और “सकारात्मक” स्वतंत्रता की है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है—बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता आत्म-नियंत्रण और आत्म-निर्धारण से जुड़ी है। बर्लिन ने यह चेताया कि सकारात्मक स्वतंत्रता की अतिशयता, अधिनायकवाद की ओर ले जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक सिद्धान्तों को एकमात्र सच्चाई की तरह प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मानवीय मूल्य परस्पर संघर्षशील हो सकते हैं और सभी को एक साथ पूर्ण रूप से नहीं अपनाया जा सकता। उन्होंने मूल्य बहुलता (Value Pluralism) को बढ़ावा दिया और यह समझाया कि विभिन्न संस्कृतियाँ और व्यक्ति अलग-अलग मूल्यों को सही मान सकते हैं। बर्लिन का योगदान इस बात में है कि उन्होंने उदारवाद को नई वैचारिक स्पष्टता दी और लोकतंत्र में विविध दृष्टिकोणों के सहअस्तित्व की आवश्यकता को रेखांकित किया।
प्रश्न-7.क्लासिकल राजनीति सिद्धान्त के पुनः उद्भव पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- क्लासिकल राजनीति सिद्धांत (Classical Political Theory) का पुनः उद्भव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ जब व्यवहारवादी आंदोलन (Behaviouralism) की सीमाएं स्पष्ट होने लगीं। व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन को केवल तथ्यों और अनुभवजन्य (empirical) विश्लेषण तक सीमित कर दिया था, जिससे मूल्य और नैतिकता की उपेक्षा हुई।
इसके प्रतिक्रिया स्वरूप 1960 के दशक में क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत की पुनः स्थापना हुई। इस पुनरुद्धार के प्रमुख विचारक जैसे लिओ स्ट्रॉस, माइकल ओक्सशॉट, और एरिक वोगेलिन ने तर्क दिया कि राजनीति केवल सत्ता और व्यवहार नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों की भी चर्चा है।
इस पुनरुद्धार ने राजनीतिक विचारधारा, परंपरा, दर्शन और ऐतिहासिक संदर्भों को पुनः केंद्र में लाया और राजनीतिक सिद्धांत को अधिक नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण प्रदान किया।
प्रश्न-8.”सामाजिक अभिधारणा” पर टेलर के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- चार्ल्स टेलर एक समकालीन राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने ‘सामाजिक अभिधारणा’ (Social Thesis) की संकल्पना प्रस्तुत की। इस विचार के अनुसार, व्यक्ति की पहचान और मूल्यों का निर्माण केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, बल्कि समाज और संस्कृति से गहराई से जुड़ा होता है।
टेलर का मानना है कि मानवीय पहचान “संवादात्मक” (dialogical) होती है, अर्थात् हम अपने अस्तित्व और नैतिक मूल्यों को दूसरों के साथ संवाद के माध्यम से विकसित करते हैं। यह सामाजिक संदर्भ ही हमें यह समझने में सहायता करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा।
इस प्रकार, सामाजिक अभिधारणा हमें यह बताती है कि नैतिकता और पहचान जैसे मुद्दे केवल व्यक्तिगत विकल्प नहीं, बल्कि सामाजिक वातावरण और मान्यताओं से निर्मित होते हैं। टेलर का यह दृष्टिकोण सामूहिक संस्कृति और पहचान की राजनीति को समझने में अत्यंत सहायक है।
प्रश्न-9. राजनीतिक यथार्थ के विभिन्न आयामों पर वोगेलिन के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:-एरिक वोगेलिन एक जर्मन-अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक यथार्थ की व्याख्या आध्यात्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से की। वे मानते थे कि राजनीतिक व्यवस्था केवल सत्ता, संस्थानों और नीतियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें मनुष्य की चेतना, आध्यात्मिक अनुभव और प्रतीकों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है। उन्होंने “आध्यात्मिक अनुक्रम” (spiritual order) और “गनोस्टिक सोच” (gnosticism) की अवधारणाओं का प्रयोग कर यह समझाया कि आधुनिक विचारधाराएँ मनुष्य की आध्यात्मिक जड़ों से विचलन का परिणाम हैं। उनके अनुसार, जब राजनीतिक यथार्थ को केवल भौतिकता तक सीमित किया जाता है, तो वह अधूरी और संकटग्रस्त हो जाती है। इसलिए वोगेलिन ने राजनैतिक यथार्थ के धार्मिक, ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक आयामों को जोड़ते हुए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
प्रश्न-10. आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त की विभिन्न प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त में अनेक प्रवृत्तियाँ उभरी हैं, जो विविध दृष्टिकोणों से राजनीति की व्याख्या करती हैं। प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं:
व्यवहारवादी प्रवृत्ति – यह अनुभवजन्य अनुसंधान और सांख्यिकीय विधियों पर आधारित है।
उत्तर-व्यवहारवाद – यह मूल्यों और नैतिकता को पुनः राजनीति में लाने पर बल देता है।
उदारवाद और नवउदारवाद – व्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति और सीमित सरकार की वकालत करते हैं।
मार्क्सवादी प्रवृत्ति – वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद की आलोचना और समानता को केंद्र में रखती है।
नारीवादी दृष्टिकोण – लिंग आधारित असमानताओं की आलोचना और लैंगिक न्याय पर बल।
समुदायवाद – व्यक्ति की पहचान और न्याय को समुदाय से जोड़ता है।
उत्तरआधुनिकता – यह सार्वभौमिक सच्चाइयों का खंडन करती है और बहुलता को स्वीकारती है।
इन प्रवृत्तियों ने राजनीतिक सिद्धान्त को अधिक बहुआयामी और जीवन के विविध पहलुओं से जुड़ा बना दिया है।
प्रश्न-11.आधुनिक पहचान के आयामों पर टेलर के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- चार्ल्स टेलर एक प्रमुख समुदायवादी विचारक हैं, जिन्होंने आधुनिक समाज में पहचान (identity) के संकट को रेखांकित किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आधुनिक पहचान केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ी होती है।
टेलर के अनुसार, व्यक्ति की पहचान को ‘मान्यता’ (Recognition) की आवश्यकता होती है। यदि समाज किसी व्यक्ति या समूह की सांस्कृतिक विशिष्टता को नहीं पहचानता, तो व्यक्ति की आत्मछवि और सम्मान प्रभावित होता है। इसीलिए टेलर ने “मान्यता की राजनीति” (Politics of Recognition) का समर्थन किया।
उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक समाज में वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद और धर्मनिरपेक्षता ने पारंपरिक पहचानों को चुनौती दी है। व्यक्ति अब अपने मूल्यों और समुदाय से कटता जा रहा है, जिससे अस्थिरता और आत्म-परिचय का संकट पैदा होता है।
इस प्रकार, टेलर ने पहचान को केवल आत्मनिर्धारण का विषय न मानकर उसे सामाजिक मान्यता और संवाद से जुड़ा हुआ बताया, जो आधुनिक राजनीति को गहराई से प्रभावित करता है।
प्रश्न-12. जॉन रॉल्स की मूल संरचना की अवधारणा की समीक्षा कीजिए।
उत्तर:- जॉन रॉल्स की “मूल संरचना” (Basic Structure) की अवधारणा उनकी पुस्तक “A Theory of Justice” में प्रमुखता से उभरती है। उनके अनुसार समाज की मूल संरचना उन प्रमुख संस्थाओं का ढांचा है जो लोगों के अधिकार, कर्तव्यों और अवसरों का वितरण तय करती हैं—जैसे संविधान, न्याय व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और अर्थव्यवस्था। रॉल्स के अनुसार न्याय के सिद्धांतों को समाज की मूल संरचना पर लागू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को समान अवसर मिलें और सबसे कमजोर वर्ग को लाभ हो। उन्होंने ‘न्याय का पहला सिद्धांत’ समान स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि ‘दूसरा सिद्धांत’ सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को तभी उचित मानता है जब वे सबसे पिछड़े वर्ग के हित में हों। आलोचक यह तर्क देते हैं कि रॉल्स की मूल संरचना पर अत्यधिक बल देने से व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारियों की अनदेखी हो सकती है। फिर भी, यह अवधारणा सामाजिक न्याय की कल्पना को संस्थागत रूप में लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
प्रश्न-13. वितरण के निर्धारक कारकों पर वाल्जर के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- माइकल वाल्जर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “Spheres of Justice” में वितरण न्याय (Distributive Justice) की पारंपरिक अवधारणाओं की आलोचना की और बहुलवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि समाज में कई प्रकार की ‘सामाजिक वस्तुएँ’ होती हैं—जैसे धन, शिक्षा, राजनीतिक अधिकार, सम्मान आदि—और इनका वितरण अलग-अलग मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। वाल्जर के अनुसार किसी एक ही सिद्धांत से सभी वस्तुओं का वितरण करना अनुचित होगा। उदाहरणस्वरूप, शिक्षा का वितरण योग्यता के आधार पर हो सकता है, जबकि राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिए जाने चाहिए। उन्होंने “कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी” की अवधारणा दी, जिसमें किसी एक क्षेत्र में प्राप्त लाभ का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में नहीं फैलना चाहिए। जैसे, अमीर व्यक्ति शिक्षा या राजनीति में वर्चस्व नहीं पा सके। वाल्जर का विचार समाज के विविध आयामों में न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने की कोशिश करता है और वितरण के निर्धारक कारकों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़ता है।
प्रश्न-14. अत्यल्प राज्य’ पर नोज़िक के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- रॉबर्ट नोज़िक एक प्रमुख इच्छा-स्वतंत्रतावादी (Libertarian) विचारक थे जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “Anarchy, State and Utopia” (1974) में ‘अत्यल्प राज्य’ (Minimal State) की अवधारणा प्रस्तुत की। नोज़िक के अनुसार, राज्य का एकमात्र वैध कार्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। वह किसी भी प्रकार की पुनर्वितरणात्मक (redistributive) नीतियों का विरोध करते हैं क्योंकि ये व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं।
नोज़िक का मानना था कि करों के माध्यम से संपत्ति का पुनर्वितरण एक प्रकार की “अनिवार्य श्रम प्रणाली” (forced labor) है। वह यह भी तर्क देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार रखता है यदि वह उसे न्यायपूर्ण ढंग से अर्जित करता है। ऐसे में, राज्य को केवल एक रात्रि प्रहरी (night-watchman) के रूप में सीमित रहना चाहिए।
इस प्रकार, नोज़िक की ‘अत्यल्प राज्य’ की संकल्पना व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है और किसी भी प्रकार की राज्य की नैतिक सीमाओं को रेखांकित करती है।
प्रश्न-15. राजनीति में विवेकवाद की ऑकशॉट की आलोचना का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:-माइकल ऑकशॉट ने राजनीति में विवेकवाद (Rationalism) की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीति केवल तर्क और सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने अपनी पुस्तक “Rationalism in Politics and Other Essays” में तर्क दिया कि राजनीतिक निर्णय अनुभव, परंपरा और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होते हैं, न कि केवल अमूर्त सिद्धांतों पर। उनके अनुसार विवेकवादी सोच में यह मान लिया जाता है कि समाज की समस्याओं का समाधान शुद्ध तर्क और योजनाओं से किया जा सकता है, जबकि वास्तविकता अधिक जटिल होती है। ऑकशॉट ने “प्रशासनिक” बनाम “राजनीतिक” दृष्टिकोण को अलग किया—जहाँ प्रशासनिक दृष्टिकोण ठोस नियमों पर आधारित होता है और राजनीतिक दृष्टिकोण संवाद, परंपरा और सहमति पर। उनकी आलोचना का उद्देश्य आधुनिक राज्य की अतितार्किक योजनाओं को चुनौती देना था। ऑकशॉट की विचारधारा परंपरावाद और उदार विचारों का मिश्रण है, जो राजनीति को नैतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में देखने की प्रेरणा देती है।
प्रश्न-16. राजनीति विज्ञान की विवेचना में मूल्यों की भूमिका की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- राजनीति विज्ञान केवल तथ्यों का अध्ययन नहीं, बल्कि मूल्यों से जुड़ा एक विश्लेषणात्मक अनुशासन भी है। राजनीतिक विचार जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और मानव अधिकार मूलतः मूल्यपरक अवधारणाएँ हैं।
मूल्यों के बिना राजनीति विज्ञान केवल सत्ता, संस्थानों और व्यवहारों की यांत्रिक व्याख्या तक सीमित रह जाता है। क्लासिकल और समकालीन विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, जॉन रॉल्स आदि ने राजनीति में नैतिकता और मूल्यों की महत्ता को रेखांकित किया है।
मूल्य राजनीतिक निर्णयों की दिशा निर्धारित करते हैं और सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इसलिए, राजनीति विज्ञान में मूल्यों की भूमिका अनिवार्य और अनिवार्यतः नैतिक दृष्टिकोण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रश्न-17. पश्चिमी संस्कृति पर मेकइंटायर के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- अलास्डेयर मैकइंटायर ने अपनी प्रसिद्ध कृति “After Virtue” में पश्चिमी संस्कृति और नैतिकता की गंभीर आलोचना की है। उनका तर्क है कि आधुनिक पश्चिमी समाज में नैतिक भाषा का विखंडन हो गया है, जिससे नैतिक निर्णय अराजक और निरर्थक बन गए हैं। वे मानते हैं कि आधुनिक संस्कृति ने परंपरागत नैतिक मूल्यों और सद्गुणों को त्याग दिया है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक जीवन दिशाहीन हो गया है। मैकइंटायर का मानना है कि नैतिकता को समझने के लिए हमें प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तू की ‘सद्गुण नैतिकता’ की ओर लौटना चाहिए, जिसमें मनुष्य का उद्देश्य ‘उत्कृष्ट जीवन’ (eudaimonia) प्राप्त करना है। उन्होंने आधुनिक उदारवाद, व्यक्तिवाद और तर्कवाद की भी आलोचना की, जो समाज को केवल व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में देखता है। मैकइंटायर ने सामुदायिक नैतिक संरचना की आवश्यकता पर बल दिया और तर्क दिया कि नैतिकता को संस्कृति, परंपरा और सामाजिक भूमिका के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
प्रश्न-18. राजनीतिक यथार्थ पर वोगेलिन के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- एरिक वोगेलिन एक जर्मन-अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने आधुनिकता और राजनीतिक यथार्थ की आलोचनात्मक विवेचना की। उनका मानना था कि राजनीति केवल संस्थागत प्रक्रिया नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक यथार्थ से जुड़ी होती है।
वोगेलिन ने राजनीतिक यथार्थ को “Order” (व्यवस्था) और “Existence” (अस्तित्व) के बीच संबंध के रूप में देखा। उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक विचारधाराएँ जैसे मार्क्सवाद, फासीवाद और वैज्ञानिक भौतिकवाद मनुष्य की आध्यात्मिक अनुभूति की उपेक्षा करती हैं, जिससे राजनीतिक विघटन और अधिनायकवाद उत्पन्न होता है।
उन्होंने ‘ग्नोस्टिसिज़्म’ (Gnosticism) की आलोचना करते हुए कहा कि आधुनिक राजनीतिक विचार मनुष्य को स्वयं ईश्वर के स्थान पर रख देते हैं। वोगेलिन का राजनीतिक यथार्थ आध्यात्मिक अनुभव, प्रतीकों और परंपराओं की पुनर्व्याख्या पर आधारित है।
प्रश्न-19. नोविक के न्याय के अधिकारिता के सिद्धान्त का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:-रॉबर्ट नोज़िक की Entitlement Theory of Justice उनकी पुस्तक “Anarchy, State, and Utopia” में प्रस्तुत की गई है। यह सिद्धांत न्याय को इस आधार पर परिभाषित करता है कि क्या किसी संपत्ति या संसाधन को वैध तरीकों से प्राप्त किया गया है। उन्होंने तीन मुख्य सिद्धांत दिए—अर्जन का सिद्धांत, हस्तांतरण का सिद्धांत और सुधार का सिद्धांत। अर्जन का अर्थ है कि किसी वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार तभी वैध होता है जब उसने उसे न्यायसंगत तरीके से प्राप्त किया हो; हस्तांतरण का अर्थ है वैध तरीके से संपत्ति का स्वामित्व दूसरे को देना; और सुधार का तात्पर्य है गलत ढंग से प्राप्त संपत्ति का सुधार। नोज़िक राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं और टैक्स को ‘जबरन श्रम’ की तरह मानते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत सामाजिक असमानताओं को वैध ठहरा देता है और सबसे कमजोर वर्ग की उपेक्षा करता है। फिर भी, यह विचार निजी संपत्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता है।
प्रश्न-20. ‘अन्वेषण की विधि’ पर ऑकशॉट के विचारों का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- माइकल ऑकशॉट एक रूढ़िवादी राजनीतिक चिंतक थे, जिन्होंने ज्ञान और राजनीतिक गतिविधियों को समझने के लिए विभिन्न ‘अन्वेषण की विधियों’ (Modes of Investigation) का विश्लेषण किया। उनकी प्रमुख कृति Experience and Its Modes (1933) में यह विचार विकसित हुआ।
ऑकशॉट के अनुसार, अनुभव को समझने के विभिन्न तरीके होते हैं, जिन्हें वे ‘मोड्स ऑफ एक्सपीरियंस’ कहते हैं। इनमें प्रमुख हैं — ऐतिहासिक विधि, वैज्ञानिक विधि, और व्यावहारिक (practical) विधि। प्रत्येक विधि का अपना दृष्टिकोण, भाषा और मानदंड होता है।
राजनीतिक अन्वेषण को ऑकशॉट एक “व्यावहारिक विधि” के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि राजनीति का उद्देश्य पूर्ण समाधान देना नहीं है, बल्कि पारंपरिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए संघर्षों का प्रबंधन करना है।
उन्होंने आदर्शवाद और तर्कवादी योजनाओं का विरोध किया, और परंपरा तथा अनुभव आधारित राजनीतिक निर्णयों को महत्व दिया। इस प्रकार, ऑकशॉट की ‘अन्वेषण की विधि’ की अवधारणा ज्ञान और राजनीति को गहराई से समझने का मार्ग प्रदान करती है।
प्रश्न-21. एक रूढ़िवादी राजनीतिक विचारक के रूप में ऑकट का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- माइकल ऑकट (Michael Oakeshott) एक प्रमुख रूढ़िवादी राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने परंपरा और अनुभव आधारित राजनीति की वकालत की। उनका मानना था कि राजनीति कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक कला है जो ऐतिहासिक अनुभव और सामाजिक परंपराओं पर आधारित होती है।
ऑकट आधुनिक आदर्शवादी विचारधाराओं जैसे मार्क्सवाद और उदारवाद की आलोचना करते थे। वे मानते थे कि समाज को कोई पूर्वनिर्धारित योजना या यूटोपिया की ओर ले जाना खतरनाक है। उन्होंने “Rationalism in Politics” में तर्क दिया कि राजनीति को विवेक से नहीं बल्कि अभ्यास और परंपरा से संचालित किया जाना चाहिए।
एक रूढ़िवादी विचारक के रूप में, ऑकट समाज में धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक परिवर्तन का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि स्थायित्व, निरंतरता और परंपरा राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं।
प्रश्न-22. वाल्जर के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- माइकल वाल्जर एक अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक हैं जिन्होंने Spheres of Justice (1983) में बहुलवादी न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने पारंपरिक उदारवादी और मार्क्सवादी न्याय सिद्धांतों की आलोचना करते हुए “संपत्ति की जटिल समानता” (Complex Equality) की अवधारणा दी।
वाल्जर का तर्क है कि समाज में विभिन्न ‘क्षेत्र’ (spheres) होते हैं — जैसे शिक्षा, राजनीति, स्वास्थ्य, धन आदि — और प्रत्येक क्षेत्र के न्याय के अपने मानदंड होने चाहिए। एक क्षेत्र की सफलता को दूसरे क्षेत्र में वर्चस्व पाने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए।
उदाहरण के लिए, आर्थिक धन से राजनीतिक शक्ति नहीं खरीदी जानी चाहिए। यदि एक व्यक्ति को किसी एक क्षेत्र में लाभ है, तो वह लाभ केवल उसी क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए। इससे सभी क्षेत्रों में शक्ति का असमान वितरण रोका जा सकता है।
इस प्रकार, वाल्जर का न्याय सिद्धांत एक नैतिक बहुलवाद पर आधारित है, जो विभिन्न सामाजिक संदर्भों में न्याय को अलग-अलग ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर बल देता है।
प्रश्न-23. जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धान्त का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- जॉन रॉल्स की A Theory of Justice (1971) ने आधुनिक न्याय सिद्धान्त में क्रांति ला दी। उन्होंने “न्याय को समानता का रूप” (Justice as Fairness) कहा और दो सिद्धांत दिए:
समान स्वतंत्रता का सिद्धांत – प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रताएँ मिलनी चाहिए।
असमानता का सिद्धांत – सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ केवल तभी न्यायसंगत हैं जब वे सबसे कमज़ोर वर्ग के हित में हों (Difference Principle)।
रॉल्स का “आवरण अज्ञानता” (Veil of Ignorance) प्रयोग न्याय की निष्पक्षता सिद्ध करने का उपकरण है। आलोचकों का मानना है कि यह आदर्श स्थिति वास्तविक जीवन से दूर है। फिर भी, रॉल्स का सिद्धांत सामाजिक न्याय और उदारवाद के समन्वय का एक प्रभावशाली मॉडल प्रस्तुत करता है।
प्रश्न-24. “मूल संरचना” पर रॉल्स के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- जॉन रॉल्स की पुस्तक “A Theory of Justice” में “मूल संरचना” (Basic Structure) की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। रॉल्स के अनुसार, किसी समाज की मूल संरचना में वे संस्थाएँ आती हैं जो व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य और अवसरों के वितरण को निर्धारित करती हैं – जैसे संविधान, न्यायपालिका, शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक ढांचा आदि।
रॉल्स मानते हैं कि न्याय की संकल्पना को लागू करने के लिए समाज की मूल संरचना को न्यायसंगत बनाना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने “न्याय के दो सिद्धांत” दिए, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और सामाजिक-आर्थिक असमानताएं सबसे कमज़ोर वर्ग के हित में हों।
इस प्रकार, रॉल्स की ‘मूल संरचना’ की अवधारणा सामाजिक न्याय को संस्थागत स्वरूप प्रदान करती है और राज्य की भूमिका को एक न्यायपूर्ण संरचना बनाने में निर्देशित करती है।
प्रश्न-25. मेकइंटायर द्वारा मार्क्सवाद की आलोचना की विवेचना कीजिए
उत्तर:- एलेस्टर मेकइंटायर (Alasdair MacIntyre) एक नैतिक दार्शनिक हैं जिन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना उसके नैतिक अधार की कमी के आधार पर की। उन्होंने अपनी पुस्तक “After Virtue” में कहा कि आधुनिक विचारधाराओं, जिनमें मार्क्सवाद भी शामिल है, नैतिकता और सद्गुणों की परंपरा से कट चुके हैं।
मेकइंटायर का मानना है कि मार्क्सवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित है जो मानवीय नैतिकता और सद्गुणों को महत्व नहीं देता। इसके अतिरिक्त, वह तर्क देते हैं कि मार्क्सवाद समाज के नैतिक ढांचे को बदलने की योजना तो प्रस्तुत करता है, परंतु वह यह स्पष्ट नहीं करता कि ‘अच्छा जीवन’ (Good Life) क्या है।
इस प्रकार, मेकइंटायर ने मार्क्सवाद को उसकी नैतिक अस्पष्टता और परंपरागत सद्गुणों की उपेक्षा के लिए आलोचना का शिकार बनाया, और नैतिकता की गहराई में जाकर राजनीतिक सिद्धांत को पुनर्परिभाषित किया।
प्रश्न-26. मैकाइण्टायर को उदारवाद की आलोचना कीजिए।
उत्तर:- अलास्डेयर मैकाइण्टायर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक After Virtue (1981) में आधुनिक उदारवाद की आलोचना करते हुए नैतिकता और राजनीति में परंपरागत गुणों (virtues) की वापसी की माँग की। उनके अनुसार, उदारवाद व्यक्ति को स्वायत्त इकाई मानता है, जो अपने नैतिक उद्देश्य स्वयं तय करता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को उसके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों से काट देता है। मैकाइण्टायर का मानना है कि सद्गुणों और नैतिक परंपराओं के बिना कोई भी न्याय या नैतिकता संभव नहीं है। उन्होंने अरस्तू की सद्गुण आधारित नैतिकता को पुनर्जीवित किया और नैतिक विमर्श को समुदाय, परंपरा और सामाजिक प्रथाओं से जोड़ने की बात की। उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण उदारवाद की नैतिक रिक्तता को उजागर करता है।
प्रश्न-27. सद्गुण आधारित नैतिक जीवन पर मेकइण्टायर के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- अलास्डेयर मेकइण्टायर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक After Virtue (1981) में सद्गुण (virtue) आधारित नैतिकता की पुनर्स्थापना की। वे मानते हैं कि आधुनिक नैतिकता विखंडित और उद्देश्यहीन हो गई है क्योंकि यह पारंपरिक नैतिक ढाँचों से कट गई है। उन्होंने अरस्तू की सद्गुण नैतिकता को पुनर्जीवित किया, जिसमें नैतिकता जीवन के “अंतिम लक्ष्य” (telos) की प्राप्ति से जुड़ी होती है। उनके अनुसार सद्गुण—जैसे ईमानदारी, साहस, न्याय—के बिना नैतिक जीवन असंभव है। उन्होंने आधुनिक “व्यक्तिवाद” की आलोचना की और सामाजिक परंपराओं और समुदाय के भीतर नैतिकता के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। मेकइण्टायर का दृष्टिकोण नैतिकता को फिर से अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाता है।
प्रश्न-28. राजनीति विज्ञान की विवेचना में मूल्यों की भूमिका की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- राजनीति विज्ञान न केवल सत्ता, संस्था और नीतियों का अध्ययन है, बल्कि यह मूल्य आधारित विचारों—जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता, और नैतिकता—का भी गहन विश्लेषण करता है। व्यवहारवादी युग में मूल्यों को तटस्थता के नाम पर नजरअंदाज किया गया, परन्तु उत्तर-व्यवहारवादी चरण में यह स्पष्ट हुआ कि राजनीति के बिना मूल्य-निरपेक्ष अध्ययन अधूरा है। मूल्य राजनीति को दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। उदाहरणतः, लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्य मौलिक हैं। राजनीतिक सिद्धांतकार जैसे जॉन रॉल्स, चाल्जर और मेकइण्टायर ने मूल्यों के आधार पर न्याय और नैतिकता की पुनर्व्याख्या की। इस प्रकार, मूल्यों की भूमिका राजनीति को केवल यथार्थ का नहीं, बल्कि “क्या होना चाहिए” का अध्ययन भी बनाती है।
प्रश्न-29. एक इच्छास्वतंत्रवादी राजनीतिक विचारक के रूप में नोजिक का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- रॉबर्ट नोजिक एक प्रमुख इच्छास्वतंत्रवादी (Libertarian) विचारक थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक Anarchy, State, and Utopia (1974) में न्यूनतम राज्य (Minimal State) का समर्थन किया।
नोजिक का मानना था कि व्यक्ति की निजी संपत्ति और स्वतंत्रता सर्वोच्च है। उन्होंने किसी भी प्रकार के पुनर्वितरण (Redistribution) का विरोध किया। उनके अनुसार, जब राज्य कर के माध्यम से अमीर से लेकर गरीब को देता है, तो यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन है।
उन्होंने ‘अधिकार आधारित न्याय सिद्धांत’ (Entitlement Theory of Justice) दिया, जिसके तीन घटक हैं — (1) न्यायपूर्ण अर्जन, (2) न्यायपूर्ण अंतरण, और (3) अन्याय के सुधार। यदि संपत्ति का अधिग्रहण और स्थानांतरण न्यायपूर्ण ढंग से हुआ है, तो राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।
नोजिक की आलोचना यह है कि उनका सिद्धांत सामाजिक समानता को नजरअंदाज करता है। परंतु, स्वतंत्रता के पक्ष में उनका दृष्टिकोण इच्छास्वतंत्रवाद का स्पष्ट और प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण है।
Section-C
प्रश्न-1.आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को समझने के लिए हमें 20वीं सदी के उत्तरार्ध से हुए बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना आवश्यक है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पारंपरिक विचारों से अलग होकर अधिक वैज्ञानिक, व्यावहारिक, मूल्य-सापेक्ष और बहुलवादी दृष्टिकोण अपनाता है।
आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले इसका मूल्य-आधारित दृष्टिकोण है। पारंपरिक राजनीतिक विश्लेषण सत्ता, राज्य या सरकार पर केंद्रित था, जबकि आधुनिक सिद्धांत न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, पहचान, लिंग और बहुलता जैसे मानवीय मूल्यों पर बल देता है।
दूसरी विशेषता इसका बहुलवादी स्वरूप है। यह विभिन्न विचारधाराओं जैसे उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, उत्तर-आधुनिकता, पर्यावरणवाद आदि को शामिल करता है, जिससे यह एक समावेशी विमर्श बन गया है। यह अब एकवर्णीय विश्लेषण न होकर बहु-आयामी बन चुका है।
तीसरी विशेषता है इसका अंतर्विषयक (interdisciplinary) स्वरूप। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अब समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन, मानवशास्त्र आदि क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य करता है। इससे इसकी व्याख्या अधिक समग्र और गहन होती है।
चौथी विशेषता है इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण। आधुनिक सिद्धांत न केवल पूर्ववर्ती विचारों की आलोचना करता है बल्कि सामाजिक यथार्थ की भी आलोचनात्मक व्याख्या करता है। यह सत्ता के दुरुपयोग, सामाजिक असमानताओं और सांस्कृतिक वर्चस्व के विरुद्ध मुखर होता है।
पाँचवीं विशेषता इसका व्यवहारिक और उपयोगी पक्ष है। यह केवल सैद्धांतिक विमर्श तक सीमित न रहकर नीति-निर्माण, प्रशासन, सामाजिक न्याय और सार्वजनिक जीवन को दिशा देने का कार्य करता है।
अंततः आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य न केवल सत्ता और राज्य की भूमिका को समझना है, बल्कि यह समाज के वंचित, पीड़ित और हाशिए पर पड़े वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में विचार प्रस्तुत करता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.राजनीतिक सिद्धांत को टेलर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- चार्ल्स टेलर एक समकालीन कनाडाई राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने आधुनिकता, पहचान, बहुसांस्कृतिकता और उदारवाद पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। टेलर को समुदायवादी (Communitarian) परंपरा से जोड़ा जाता है, लेकिन उनका कार्य इससे कहीं अधिक व्यापक है।
टेलर की प्रमुख अवधारणा पहचान की राजनीति (Politics of Recognition) है। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान के साथ मान्यता मिलना आवश्यक है। पहचान का दमन, व्यक्ति की आत्म-मूल्य की भावना को नष्ट करता है।
उन्होंने “The Politics of Recognition” (1992) निबंध में यह तर्क दिया कि बहुसांस्कृतिक समाजों में सभी समुदायों को समान गरिमा के साथ स्थान मिलना चाहिए। यह विचार समावेशी लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
टेलर का दूसरा बड़ा योगदान समुदायवाद की व्याख्या है। वे कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके समुदाय और परंपराओं से जुड़ी होती है। वह शुद्ध रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता, जैसा कि उदारवादी विचारक मानते हैं। इस विचार से उन्होंने उदारवाद की सीमाओं को उजागर किया।
उन्होंने धर्म और आधुनिकता के संबंध में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। “A Secular Age” (2007) में उन्होंने बताया कि आधुनिक धर्मनिरपेक्षता केवल धार्मिक परित्याग नहीं है, बल्कि वह धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभवों के नए स्वरूपों की ओर इशारा करती है।
मूल्यांकन:
टेलर के विचार आज की बहुसांस्कृतिक और वैश्विक दुनिया में अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने ‘आत्म की खोज’, ‘सांस्कृतिक मान्यता’, और ‘सार्वजनिक संवाद’ को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया।
उनकी आलोचना यह कहकर की जाती है कि पहचान की राजनीति कभी-कभी बहुलता के स्थान पर विभाजन को जन्म देती है। फिर भी, टेलर ने आधुनिक राजनीति को नई दिशा दी, जिसमें व्यक्ति केवल अधिकार का नहीं, बल्कि मान्यता का भी अधिकारी है।
प्रश्न-3. जॉन रॉल्स के न्याय के दो सिद्धांतों का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- जॉन रॉल्स आधुनिक राजनीतिक दर्शन के प्रमुख विचारकों में से एक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक “A Theory of Justice” (1971) में न्याय के दो सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिन्हें ‘न्याय का सिद्धांत’ (Theory of Justice) कहा जाता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है।
पहला सिद्धांत – समान स्वतंत्रता का सिद्धांत (Principle of Equal Liberty):
रॉल्स के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को समान बुनियादी स्वतंत्रताओं का अधिकार होना चाहिए, जैसे – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण प्रक्रिया का अधिकार आदि। यह सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा, सम्मान और स्वायत्तता की रक्षा करता है।
दूसरा सिद्धांत – सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दो शर्तों पर स्वीकार्यता (Difference Principle):
(1) ये असमानताएँ सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए लाभकारी होनी चाहिए।
(2) सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित होनी चाहिए।
रॉल्स मानते हैं कि यदि कोई असमानता है तो वह तभी न्यायोचित मानी जाएगी जब वह समाज के सबसे कमजोर लोगों की स्थिति को बेहतर बनाए।
मूल्यांकन:
रॉल्स का सिद्धांत उदारवाद की नई व्याख्या है जिसमें वह स्वतंत्रता और समानता के संतुलन की बात करते हैं। उनके विचार सामाजिक न्याय की व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करते हैं, जो शोषित वर्गों को भी न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं।
रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना मार्क्सवादी, नारीवादी और कम्युनिटेरियन विचारकों ने की है। मार्क्सवादी इसे पूंजीवाद की एक नरम व्याख्या मानते हैं। नारीवादी आलोचना करते हैं कि यह सिद्धांत पितृसत्तात्मक ढांचे की अनदेखी करता है। कम्युनिटेरियन विचारक कहते हैं कि यह व्यक्ति को समुदाय से अलग कर देखता है।
फिर भी, रॉल्स का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने आधुनिक काल में न्याय को एक व्यापक और औचित्यपूर्ण ढांचे में प्रस्तुत किया।
प्रश्न-4. नोजिक को एक इच्छा स्वतंत्रबादी राजनीतिक विचारक के रूप में मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- रॉबर्ट नोजिक (Robert Nozick) 20वीं सदी के प्रमुख इच्छा स्वतंत्रबादी (Libertarian) राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कृति “Anarchy, State and Utopia” (1974) में जॉन रॉल्स के कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की तीव्र आलोचना की और न्यूनतम राज्य (Minimal State) की वकालत की।
- स्वतंत्रता पर बल:
नोजिक के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन, शरीर और संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। राज्य को केवल इन अधिकारों की रक्षा तक सीमित रहना चाहिए। कराधान और पुनर्वितरण जैसी नीतियाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं। - न्यूनतम राज्य की अवधारणा:
नोजिक का मानना है कि न्यायसंगत राज्य वही है जो केवल अपराध, धोखा, और हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके अलावा राज्य का कोई और कार्य नहीं होना चाहिए। - अधिकार आधारित न्याय सिद्धांत:
नोजिक के अनुसार, न्याय तीन तत्वों पर आधारित होता है—
(1) न्यायसंगत अधिग्रहण (Just Acquisition),
(2) न्यायसंगत अंतरण (Just Transfer), और
(3) यदि कोई अनुचित अधिग्रहण हुआ हो तो उसका सुधार (Rectification of Injustice)।
मूल्यांकन:
नोजिक का सिद्धांत व्यक्तिवाद और स्वतंत्र बाजार की कट्टर समर्थन करता है।
यह कराधान को “मजबूरी में श्रम” (forced labor) मानता है।
आलोचकों के अनुसार, यह विचार सामाजिक असमानता और वंचित वर्गों की उपेक्षा करता है।
यह न्याय की सामूहिक अवधारणा को नहीं मानता, जिससे सामाजिक न्याय की भावना को ठेस पहुँचती है।
तुलना में:
जहाँ रॉल्स समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देते हैं, वहीं नोजिक व्यक्तिगत अधिकारों को सर्वोच्च मानते हैं।
नोजिक का सिद्धांत पूंजीवादी संरचना को मजबूत करता है, परंतु सामाजिक कल्याण की अवधारणा को सीमित करता है।
नोजिक एक विशुद्ध इच्छा स्वतंत्रबादी चिन्तक हैं, जो राज्य की भूमिका को अत्यंत सीमित मानते हैं। उनकी विचारधारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को केंद्र में रखती है, परंतु सामाजिक न्याय के व्यापक उद्देश्य की उपेक्षा करती है। उनका सिद्धांत शुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है।
प्रश्न-5. सन् 1971 के बाद के राजनीति सिद्धान्त की विभिन्न प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- सन् 1971 के बाद के राजनीति सिद्धांत में अनेक नवीन प्रवृत्तियाँ उभरीं, जिनका उद्देश्य राजनीति को अधिक मानवीय, समावेशी और व्यावहारिक बनाना था। इस समय “न्याय का सिद्धांत” (1971) के प्रकाशन के साथ ही जॉन रॉल्स द्वारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की एक नई शुरुआत हुई। इसके बाद के दशकों में कई महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ सामने आईं, जिनकी विवेचना निम्नलिखित है:
- न्याय की पुनर्व्याख्या: जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत ने राजनीति में नैतिकता के महत्त्व को पुनः स्थापित किया। इसके पश्चात नोज़िक, वाल्ज़र और सेन जैसे विचारकों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से न्याय को पुनर्परिभाषित किया।
- समुदायवाद (Communitarianism): 1980 और 1990 के दशक में एलैस्टेयर मैक्किन्टायर, माइकल सैंडल और चार्ल्स टेलर जैसे विचारकों ने यह तर्क दिया कि व्यक्ति समाज से पृथक नहीं है, बल्कि सामाजिक संबंधों में निहित है। इसने उदारवादी सिद्धांतों की आलोचना की।
- नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत: नारीवादियों ने यह दिखाया कि पारंपरिक राजनीति सिद्धांत लिंग-आधारित अन्याय को अनदेखा करता है। सिंथिया एनलो, कैरोल पेटमैन आदि ने सत्ता और पितृसत्ता के संबंधों पर बल दिया।
- पर्यावरणीय राजनीति सिद्धांत: 1970 के बाद पर्यावरणीय संकटों के कारण राजनीतिक चिंतन में पारिस्थितिकी और सतत विकास पर जोर दिया गया। इसे “हरित राजनीतिक सिद्धांत” कहा गया।
- उत्तर-आधुनिकता (Postmodernism): इस प्रवृत्ति ने सार्वभौमिक सच्चाइयों और महान आख्यानों (grand narratives) को चुनौती दी। मिशेल फूको, डेरिडा जैसे विचारकों ने सत्ता, ज्ञान और भाषिक संरचनाओं की भूमिका को रेखांकित किया।
- बहुसांस्कृतिकता (Multiculturalism): विल किमलिका, भिक्खु पारेख जैसे चिंतकों ने विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया। यह प्रवृत्ति सांस्कृतिक विविधता को राजनीतिक मान्यता देने का प्रयास है।
- उत्पीड़ित समूहों की राजनीति: इस दौर में दलित, आदिवासी, नस्लीय अल्पसंख्यकों एवं LGBTQ समुदाय की पहचान, अधिकार और प्रतिनिधित्व के मुद्दे केंद्र में आए।
1971 के बाद राजनीतिक सिद्धांत ने उदारवाद की सीमाओं को चुनौती देते हुए अधिक समावेशी, आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया। इन प्रवृत्तियों ने राजनीतिक चिंतन को केवल संस्थाओं तक सीमित न रखकर सामाजिक न्याय, पहचान और सत्ता के विस्तृत सरोकारों से जोड़ा।
प्रश्न-6. जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धान्त का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- जॉन रॉल्स की पुस्तक “A Theory of Justice” (1971) में प्रस्तुत सिद्धांत ने आधुनिक राजनीतिक चिंतन में क्रांति ला दी। उन्होंने “न्याय” को सामाजिक संस्थाओं का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण माना और इसे “नैतिक समानता” के आधार पर परिभाषित किया। उनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-सांस्थानिक ढांचे को इस प्रकार संगठित करना था जिससे सबसे कमज़ोर वर्ग को अधिकतम लाभ मिल सके।
मुख्य तत्त्व:
- मूल संरचना (Basic Structure): समाज की मूल संस्थाएं (जैसे – विधायिका, न्यायपालिका, शिक्षा प्रणाली) न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित होनी चाहिए।
- मूल्यनिष्ठ स्थिति (Original Position): रॉल्स ने ‘कल्पनात्मक अनुबंध’ का प्रयोग किया, जिसमें व्यक्ति “अज्ञान के परदे” (veil of ignorance) के पीछे होते हैं और उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि वे किस वर्ग, जाति, धर्म आदि से हैं।
- दो न्याय सिद्धांत:
(i) समान स्वतंत्रता का सिद्धांत: प्रत्येक व्यक्ति को समान मौलिक स्वतंत्रताएँ प्राप्त होनी चाहिए।
(ii) अंतर सिद्धांत (Difference Principle): सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ तभी स्वीकार्य हैं जब वे समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लिए लाभकारी हों।
मूल्यांकन:
सकारात्मक पक्ष:
यह सिद्धांत समानता और स्वतंत्रता में संतुलन स्थापित करता है।
यह पारंपरिक उपयोगितावाद की आलोचना करता है, जो कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा करता है।
इसका ‘अज्ञान का परदा’ विचार नैतिक दृष्टि से निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है।
नकारात्मक पक्ष:
आलोचकों ने इसे अत्यधिक अमूर्त और आदर्शवादी कहा है।
नोज़िक ने इसे स्वतंत्रता पर आघात मानते हुए आलोचना की।
सामुदायवादी चिंतकों ने इसे अत्यधिक व्यक्तिवादी और समाज से कटा हुआ बताया।
रॉल्स का न्याय सिद्धांत समकालीन राजनीतिक विचारों की दिशा निर्धारित करने वाला एक ऐतिहासिक प्रयास है। यद्यपि इस पर अनेक आलोचनाएँ हुईं,फिर भी यह सिद्धांत आज भी न्याय, समानता और अधिकारों पर होने वाले विमर्श की आधारशिला बना हुआ है।
प्रश्न-7. सामाजिक अभिधारणा पर टेलर के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- चार्ल्स टेलर (Charles Taylor) एक प्रसिद्ध समकालीन राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने ‘सामाजिक अभिधारणा’ (Social Thesis) के माध्यम से यह प्रतिपादित किया कि व्यक्ति की पहचान केवल आत्मचिंतन या आंतरिक गुणों से नहीं बनती, बल्कि यह समाज में उसकी स्थिति, सांस्कृतिक संदर्भों, और पारस्परिक मान्यताओं से निर्मित होती है।
टेलर के अनुसार, व्यक्ति का “स्व” (Self) एक सामाजिक निर्माण है। समाज में उपलब्ध सांस्कृतिक प्रतीकों, भाषाई अभिव्यक्तियों, सामाजिक भूमिकाओं और संस्थागत संरचनाओं के माध्यम से व्यक्ति की आत्म-चेतना विकसित होती है। वह मानते हैं कि मानवीय पहचान सामाजिक रूप से निर्मित होती है और इसे समझने के लिए हमें व्यक्ति के सामाजिक संदर्भ को समझना आवश्यक है।
टेलर का यह विचार जॉन लॉक और देकार्त जैसे दार्शनिकों के आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण के विपरीत है, जिन्होंने व्यक्ति को एक स्वतंत्र, विचारशील और आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखा था। टेलर इस मत को खंडित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य की पहचान एक संवादात्मक प्रक्रिया है, जो अन्य व्यक्तियों और समाज के साथ संबंधों के माध्यम से बनती है।
टेलर की सामाजिक अभिधारणा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका – टेलर के अनुसार, व्यक्ति की पहचान उस संस्कृति में रची-बसी होती है जिसमें वह रहता है।
- मान्यता (Recognition) का महत्व – टेलर यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को उसकी पहचान के साथ मान्यता देना आवश्यक है। यह मान्यता सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है।
- विकासशील स्व – टेलर मानते हैं कि व्यक्ति की पहचान स्थिर नहीं होती, बल्कि यह एक सतत विकासशील प्रक्रिया है।
इस प्रकार, टेलर की सामाजिक अभिधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि व्यक्ति को एक सामाजिक संदर्भ में रखकर ही उसकी पहचान, नैतिकता, और राजनीतिक दायित्वों को समझा जा सकता है। उनका यह दृष्टिकोण समकालीन पहचान की राजनीति (politics of recognition) को सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है।
प्रश्न-8. समुदायवादी राजनीतिक सिद्धान्त का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- समुदायवादी राजनीतिक सिद्धांत (Communitarian Political Theory) 1980 के दशक में उदारवाद (Liberalism) की आलोचना के रूप में उभरा। इसके प्रमुख विचारकों में माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, माइकल वाल्जर और एलिस्डेयर मैकइंटायर शामिल हैं। यह सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति की पहचान और नैतिक मूल्य समुदाय के भीतर ही निर्मित होते हैं।
मुख्य तत्त्व –
- सामूहिक पहचान – समुदायवादी मानते हैं कि व्यक्ति की पहचान सामाजिक संबंधों, संस्कृति और परंपराओं से बनती है।
- सामाजिक दायित्व – यह सिद्धांत व्यक्ति के अधिकारों के साथ-साथ उसके सामाजिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को भी महत्व देता है।
- संवेदनशील राज्य – समुदायवादी राज्य को केवल निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं मानते, बल्कि वह समुदाय के मूल्यों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए।
मूल्यांकन –
सकारात्मक पक्ष:
समुदायवाद व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध को संतुलित करता है।
यह नैतिकता, परंपरा और सांस्कृतिक विविधता को राजनीतिक विमर्श में स्थान देता है।
यह उदारवाद की अत्यधिक व्यक्तिवादी प्रवृत्ति की आलोचना करता है।
नकारात्मक पक्ष:
आलोचकों का मानना है कि समुदायवाद सामूहिकता को इतना बढ़ावा देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो सकती है।
यह सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता कि यदि समुदाय के मूल्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हों तो क्या किया जाए।
अतः समुदायवादी सिद्धांत एक संतुलित राजनीतिक विमर्श प्रदान करता है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ता है। यह आधुनिक बहुसांस्कृतिक समाजों के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
प्रश्न-9. एक रूढ़िवादी विचारक के रूप में ऑकशॉट का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- माइकल ऑकशॉट (Michael Oakeshott) एक प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिक सिद्धांतकार थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली रूढ़िवादी (conservative) विचारकों में गिना जाता है। उन्होंने परंपरा, व्यावहारिक ज्ञान और संस्थाओं की भूमिका को आधुनिक राजनीतिक जीवन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना।
ऑकशॉट के अनुसार, राजनीति एक “प्रयोजनमुक्त संवाद” (politics as a conversation) है। वे मानते थे कि राजनीति का उद्देश्य किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है, बल्कि वह मानवीय जीवन को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाए रखने की प्रक्रिया है।
रूढ़िवाद के संदर्भ में ऑकशॉट का प्रमुख योगदान यह है कि वे परिवर्तन के प्रति सावधानी बरतने की बात करते हैं। उनके अनुसार, समाज की संस्थाओं और परंपराओं को तात्कालिक तर्क या जोश में बदलना उचित नहीं, क्योंकि वे लंबे अनुभव और परीक्षण से विकसित हुई हैं।
ऑकशॉट “rationalism in politics” की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार, राजनीति को केवल तर्कशक्ति और योजना के आधार पर संचालित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव समाज जटिल होता है और व्यावहारिक ज्ञान (practical knowledge) की आवश्यकता होती है।
उनकी विचारधारा में आदर्शवाद की जगह यथार्थवाद प्रमुख है। वे सामाजिक प्रयोगों और क्रांतिकारी विचारों से दूरी बनाकर संस्थागत निरंतरता को महत्व देते हैं। वे मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अनुशासन भी है।
मूल्यांकन:
ऑकशॉट की आलोचना यह कहकर की गई कि उनका रूढ़िवाद यथास्थिति को बनाकर रखने वाला है और सामाजिक सुधारों को हतोत्साहित करता है। इसके बावजूद, उन्होंने राजनीति में नैतिकता, अनुभव और परंपरा की भूमिका को पुनः प्रतिष्ठित किया। उनके विचार आज भी राजनीतिक संतुलन, विधि के शासन और सामाजिक स्थिरता को समझने में उपयोगी हैं।
प्रश्न-10. वाल्ज़र के न्याय सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- माइकल वाल्ज़र (Michael Walzer) एक प्रमुख राजनीतिक चिंतक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक “Spheres of Justice” (1983) में बहुआयामी न्याय (complex equality) का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि न्याय सार्वभौमिक या एकरूप नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न सामाजिक संदर्भों में भिन्न-भिन्न होता है।
मुख्य तत्त्व:
- बहुआयामी न्याय (Complex Equality): समाज में कई क्षेत्र (spheres) होते हैं – जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, बाजार आदि – और प्रत्येक क्षेत्र में न्याय की परिभाषा भिन्न होती है।
- असमानताओं की स्वायत्तता: एक क्षेत्र की सफलता का लाभ दूसरे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः – धन के बल पर राजनीतिक शक्ति नहीं खरीदी जानी चाहिए।
- सांस्कृतिक सापेक्षता: न्याय को परिभाषित करने के लिए स्थानीय नैतिक मान्यताओं और सामाजिक प्रसंगों को समझना आवश्यक है। यह सार्वभौमिक न्याय की अवधारणा का विरोध करता है।
मूल्यांकन:
सकारात्मक पक्ष:
यह सिद्धांत न्याय की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को मान्यता देता है।
यह सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने की दिशा में योगदान देता है।
यह समानता को अधिक व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत करता है।
नकारात्मक पक्ष:
कुछ विद्वानों ने इसे न्याय के सार्वभौमिक मानदंडों की उपेक्षा कहा है।
इससे स्थानीय अन्याय को सांस्कृतिक मान्यता देकर वैध ठहराया जा सकता है।
यह राजनीतिक रूप से निर्णय लेना कठिन बना देता है क्योंकि यह स्पष्ट मानकों का अभाव रखता है।
वाल्ज़र का न्याय सिद्धांत आधुनिक समाज की विविधता को ध्यान में रखकर एक अधिक यथार्थपरक और संदर्भ-संवेदनशील दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र के लिए एक उपयोगी ढाँचा प्रस्तुत करता है।
प्रश्न-11. एक समुदायवादी राजनीतिक विचारक के रूप में मैक्किन्टायर का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:-एलैस्टेयर मैक्किन्टायर (Alasdair MacIntyre) एक प्रमुख समुदायवादी (Communitarian) राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “After Virtue” (1981) में आधुनिक नैतिक और राजनीतिक चिंतन की आलोचना करते हुए समुदाय, परंपरा और सद्गुण आधारित जीवन की वकालत की।
मूल विचार:
- नैतिकता का पतन: मैक्किन्टायर का तर्क था कि आधुनिक समाज में नैतिक भाषा खोखली हो गई है क्योंकि हमने सद्गुणों की परंपरा और नैतिक उद्देश्य (telos) को त्याग दिया है।
- सद्गुण आधारित नैतिकता (Virtue Ethics): उन्होंने अरस्तू की परंपरा में लौटने का आह्वान किया, जिसमें व्यक्ति का नैतिक विकास समुदाय के भीतर संभव है।
- व्यक्ति की सामाजिकता: मैक्किन्टायर का मानना है कि व्यक्ति समाज से पृथक नहीं होता। उसकी पहचान और नैतिकता उसके समुदाय की परंपराओं से निर्मित होती है।
- आधुनिक उदारवाद की आलोचना: उन्होंने उदारवाद की उस धारणा का विरोध किया जिसमें व्यक्ति को एक स्वायत्त, विकल्प चुनने वाला प्राणी माना गया है। वे मानते हैं कि नैतिक निर्णय समुदाय की परंपरा से उत्पन्न होते हैं।
मूल्यांकन:
सकारात्मक पक्ष:
मैक्किन्टायर ने आधुनिक समाज में नैतिक उद्देश्य और चरित्र निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित किया।
उन्होंने समुदाय और परंपरा के महत्व को पुनः स्थापित किया।
यह दृष्टिकोण नैतिकता को व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया मानता है।
नकारात्मक पक्ष:
उनकी आलोचना परंपरा के अंधानुकरण को प्रेरित कर सकती है।
यह दृष्टिकोण विविधता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है।
कुछ आलोचकों के अनुसार यह उदार समाज के मूल्यों को खतरे में डाल सकता है।
एलैस्टेयर मैक्किन्टायर ने समुदाय और सद्गुण आधारित नैतिकता पर बल देते हुए आधुनिक नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों को एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान किया। एक समुदायवादी के रूप में उनका योगदान समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की बहसों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
VMOU MAPS-05 Paper vmou exam paper , vmou ma final year exam paper ,vmou exam paper 2029 vmou exam paper 2028 vmou exam paper 2027 vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4
VMOU EXAM PAPER