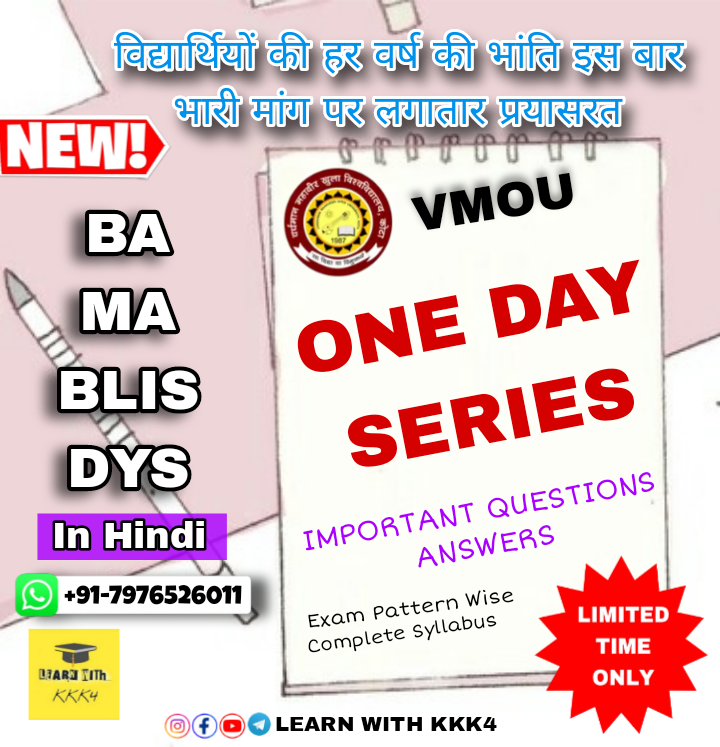VMOU HI-03 Paper BA 2ND Year (semester-III) ; vmou exam paper
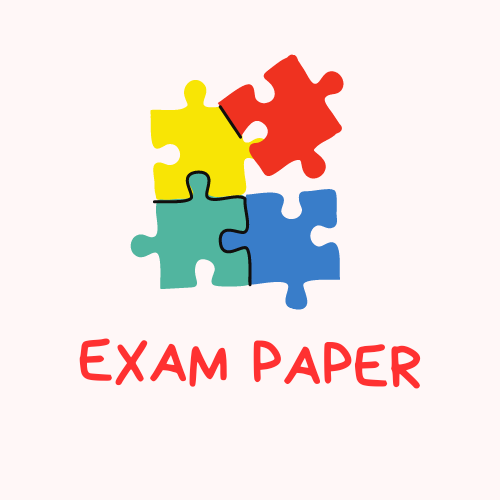
VMOU BA 2nd Year के लिए History ( HI-03 , ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.खानवा का युद्ध कब लड़ा गया?
उत्तर:- 16 मार्च 1527 ई. को बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.राणा सांगा कौन थे?
उत्तर:- राणा सांगा मेवाड़ के शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े।
प्रश्न-3. कुंभा कौन था?
उत्तर:- कुंभा मेवाड़ का प्रसिद्ध राजा था, जिसे राणा कुंभा कहा जाता है; वह एक महान स्थापत्य प्रेमी और योद्धा था।
प्रश्न-4. अबुल फज़ल कौन था?
उत्तर:- अबुल फज़ल अकबर का प्रमुख दरबारी, इतिहासकार और ‘आइन-ए-अकबरी’ तथा ‘अकबरनामा’ का लेखक था।
प्रश्न-5. अल-बेरूनी कौन था? उसकी पुस्तक का नाम लिखिए।
उत्तर:- अल-बेरूनी एक फारसी विद्वान था, जिसने ‘तहकीक-ए-हिंद’ नामक पुस्तक में भारत का विवरण लिखा
प्रश्न-6. रामचरितमानस के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- तुलसीदास
प्रश्न-7. शिवाजी के दो किलों के नाम बताइए।
उत्तर:- रायगढ़ और प्रतापगढ़
प्रश्न-8. शिवाजी के प्रशासन में अमात्य का क्या कार्य था?
उत्तर:- शिवाजी के प्रशासन में अमात्य राज्य के वित्त और लेखा विभाग का प्रमुख था, जो राजस्व और खर्चों का लेखा-जोखा रखता था।
प्रश्न-9. दो सैयद भाइयों के नाम लिखिए।
उत्तर:- सैयद अब्दुल्ला और सैयद हुसैन अली
प्रश्न-10. हिंदुओं पर कौनसा कर लगाया जाता था?
उत्तर:- हिंदुओं पर जज़िया कर लगाया जाता था, जो एक धार्मिक कर था।
प्रश्न-11. बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की?
उत्तर:- 1347 ई. में अलाउद्दीन बहमन शाह ने
प्रश्न-12. जीतल क्या था ?
उत्तर:- जीतल मध्यकालीन भारत में प्रचलित एक ताँबे का सिक्का था जिसका प्रयोग सामान्य खरीद-फरोख्त में होता था।
प्रश्न-13. गुलाम वंश के किस शासक ने ‘रक्त व लौह की नीति अपनाई ?
उत्तर:-गुलाम वंश के शासक बलबन ने ‘रक्त और लौह’ की कठोर नीति अपनाई जिससे शासन में सख़्ती आई।
प्रश्न-14. दो हिंदू स्मारकों के नाम लिखिए।
उत्तर:-खजुराहो के मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर
प्रश्न-15. दो मुस्लिम इमारतों के नाम लिखिए।
उत्तर:-कुतुब मीनार और ताजमहल
प्रश्न-16. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की?
उत्तर:- विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 ई. में की थी।
प्रश्न-17. कुतुबमीनार के बारे में लिखिए।
उत्तर:- कुतुबमीनार दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध मीनार है, जिसकी ऊँचाई लगभग 73 मीटर है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था
प्रश्न-18. Alberuni कौन था?
उत्तर:- अलबरूनी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान, इतिहासकार और खगोलशास्त्री था, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया और “तहकीक-ए-हिंद” नामक ग्रंथ लिखा
प्रश्न-19. बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की ?
उत्तर:- बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 ई. में गुलबर्गा को राजधानी बनाकर की थी।
प्रश्न-20. दीन-ए-इलाही को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- दीन-ए-इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक आंदोलन था, जो विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाकर बना था।
प्रश्न-21. Describe Jaziya – जजिया का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- जजिया एक प्रकार का कर था जो इस्लामी शासक गैर-मुस्लिमों से उनकी सुरक्षा के बदले लिया करते थे।
प्रश्न-22. खानवा के युद्ध के परिणाम बताए।
उत्तर:- खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा को हराकर जीता, जिससे भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई।
प्रश्न-23. खानवा के युद्ध के दो कारणों की लिखिए।
उत्तर:- बाबर का भारत में स्थायी राज्य स्थापित करना और राणा सांगा की शक्ति को चुनौती देना इसके दो प्रमुख कारण थे।
प्रश्न-24. तुजुक-ए-बाबरी के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- तुजुक-ए-बाबरी के लेखक बाबर थे, जो मुग़ल सम्राट थे और उन्होंने इसे अपनी आत्मकथा के रूप में फारसी में लिखा था।
प्रश्न-25. शिवाजी के प्रशासन में अमात्य की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- अमात्य शिवाजी के मंत्रिमंडल का सदस्य था, जो वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता था।
प्रश्न-26. ‘रहेला’ ग्रंथ किसने लिखा?
उत्तर:- ‘रहेला’ ग्रंथ अफगान यात्री इब्न बतूता ने लिखा था, जिसमें उसकी भारत यात्रा का विवरण है।
प्रश्न-27. वतन जागीरों के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:- वतन जागीरें वे जागीरें थीं जो जागीरदारों को पैतृक रूप से दी जाती थीं और वे उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त करते थे।
प्रश्न-28. उलेमाएँ कौन थे?
उत्तर:- उलेमा मुस्लिम धर्मशास्त्री होते थे जो इस्लामी कानून, शिक्षा और धार्मिक मामलों का मार्गदर्शन करते थे।
प्रश्न-29. ‘नुस्खा-ए-दिलकुशा’ किसने लिखी?
उत्तर:- ‘नुस्खा-ए-दिलकुशा’ मराठा सेनापति भाऊसाहेब के सचिव भिम्मा ने लिखी थी, जो पानीपत युद्ध से संबंधित है।
प्रश्न-30. बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की?
उत्तर:- बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ई. में हसन गंगू बहमनी ने की थी।
Section-B
प्रश्न-1.जौहर पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
उत्तर:- “जौहर” एक प्राचीन राजपूती परंपरा थी, जिसमें युद्ध में पराजय निश्चित जानकर महिलाओं द्वारा आत्मसम्मान की रक्षा हेतु सामूहिक अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए जाते थे। यह प्रथा विशेषतः मेवाड़, चित्तौड़ और अन्य राजपूत राज्यों में देखने को मिलती है।
जौहर का उद्देश्य शत्रु के हाथों अपमानजनक स्थिति में पड़ने से बचना था। जब पुरुष युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त होते थे, तब महिलाएँ अपने बच्चों सहित जौहर कुंड में प्रवेश कर अग्नि को समर्पित हो जाती थीं।
प्रसिद्ध जौहर घटनाओं में रानी पद्मिनी (चित्तौड़, 1303 ई., अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण), रानी कर्णावती (1535 ई., बहादुर शाह का आक्रमण) प्रमुख हैं।
यद्यपि यह परंपरा अत्यंत हृदयविदारक थी, लेकिन इसमें राजपूत स्त्रियों के अद्वितीय साहस, आत्मसम्मान और बलिदान की भावना स्पष्ट झलकती है। आधुनिक दृष्टिकोण से यह एक अमानवीय परंपरा मानी जाती है, किंतु ऐतिहासिक संदर्भ में यह असाधारण नारी-शक्ति और शौर्य का प्रतीक है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.अलबक की राजनीति का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- अलबर (बलबन) दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली सुल्तान था। उसकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य केंद्र में सुल्तान की शक्ति को सर्वोच्च बनाना था। बलबन ने “नियम और भय” (Niyam aur Danda) की नीति अपनाई। उसने दरबारी शिष्टाचार में ‘सिजदा’ और ‘पैबोसी’ जैसी फारसी परंपराएं लागू कीं जिससे सुल्तान की महानता को दर्शाया जा सके।
बलबन ने ‘नौबल्स’ (अमीरों) की शक्ति को सीमित किया और विद्रोही राजपूतों को दबाने के लिए कठोर नीति अपनाई। उसने ‘बाहरी आक्रमणों’ से सुरक्षा हेतु सेना को सुदृढ़ किया और ‘दरबार में अनुशासन’ को प्राथमिकता दी। बलबन की न्याय प्रणाली कठोर थी, पर न्यायसंगत थी।
इस प्रकार, बलबन ने सुल्तान की सर्वोच्चता को स्थापित करने और सल्तनत को केंद्रीकृत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
प्रश्न-3.मुग़लों की समाज व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- मुग़ल कालीन समाज विविधता से भरपूर था और उसमें धर्म, जाति, वर्ग तथा व्यवसाय के आधार पर विभाजन था। समाज में हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग थे, परन्तु हिन्दू बहुसंख्यक थे।
उच्च वर्ग में शाही परिवार, अमीर, मनसबदार और जमींदार शामिल थे। मध्य वर्ग में व्यापारी, कारीगर, शिक्षक और विद्वान आते थे, जबकि निम्न वर्ग में कृषक, मजदूर और दास थे।
मुग़ल समाज में धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती थी, विशेषकर अकबर के शासन में। महिलाओं की स्थिति आमतौर पर सीमित थी, पर कुछ महिलाएं, जैसे नूरजहाँ, राजनीति में प्रभावशाली बनीं।
समाज में जाति व्यवस्था प्रचलित थी और व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। कारीगरों और शिल्पियों को राज्य संरक्षण मिलता था। कुल मिलाकर मुग़ल समाज संरचित, परन्तु विविधतापूर्ण था।
प्रश्न-4. खिलजी साम्राज्यवाद की विवेचना कीजिए
उत्तर:- खिलजी वंश (1290-1320 ई.) ने एक सशक्त और आक्रामक साम्राज्यवाद को अपनाया। इसके प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। उसने रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत तक विजय अभियान चलाया। दक्षिण भारत में मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान चलाए गए और देवगिरि, वारंगल तथा होयसाल राजाओं को पराजित कर उनसे भारी धन-संपत्ति वसूली गई।
अलाउद्दीन ने साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने के लिए सैन्य और प्रशासनिक सुधार किए। उसने बाजार नियंत्रण, मूल्य निर्धारण, भूमि कर प्रणाली में बदलाव किए और अमीरों की शक्ति सीमित की। खिलजी साम्राज्यवाद का मुख्य उद्देश्य भारत के अधिकतम भू-भाग पर नियंत्रण और आर्थिक दोहन था। दक्षिण भारत को पूर्ण रूप से अपने अधीन न करते हुए उसने वहां के शासकों से कर वसूलने की नीति अपनाई।
इस प्रकार खिलजी साम्राज्यवाद ने राजनीतिक विस्तार, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक केंद्रीकरण के माध्यम से एक शक्तिशाली शासन प्रणाली की नींव रखी।
प्रश्न-5. पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणामों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहीम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था।
इस युद्ध में बाबर की छोटी लेकिन संगठित और बारूद का प्रयोग करने वाली सेना ने लोदी की बड़ी सेना को पराजित किया। इब्राहीम लोदी युद्ध में मारा गया।
इस युद्ध के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं:
दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और लोदी वंश समाप्त हुआ।
भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई और बाबर दिल्ली तथा आगरा का शासक बना।
यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद, तोपों और आधुनिक युद्ध तकनीकों के प्रयोग का आरंभिक उदाहरण बना।
उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायी परिवर्तन हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई।
इस युद्ध ने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी और बाबर के वंशजों ने भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की नींव रखी।
प्रश्न-6.अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध राणा हमीर के प्रतिरोध का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- राणा हमीर (हमीरदेव) मेवाड़ के एक प्रतापी शासक थे, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया। 1303 ई. में जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था, तब राणा रत्नसिंह वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। इसके पश्चात चित्तौड़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया।
राणा हमीर ने संघर्ष कर पुनः चित्तौड़ को स्वतंत्र कराया। उन्होंने मेवाड़ की खोई हुई गरिमा को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने एक सशक्त सेना का गठन किया और स्थानीय क्षत्रियों को एकजुट किया। उनकी रणनीति और नेतृत्व क्षमता के कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं मेवाड़ में टिक नहीं सकीं। राणा हमीर को चित्तौड़ का पुनः संस्थापक माना जाता है और उन्हें “हमीर हठ” के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है। उनका प्रतिरोध अलाउद्दीन की नीतियों और अत्याचारों के विरुद्ध राजपूती स्वाभिमान की प्रतीक बन गया।
प्रश्न-7.मुग़लों की कर व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- मुग़लों की कर व्यवस्था मुख्यतः भूमि कर पर आधारित थी। अकबर ने टोडरमल की सहायता से एक प्रभावशाली भू-राजस्व व्यवस्था लागू की जिसे ‘जाब्ती प्रणाली’ कहा जाता है।
भूमि की उपज का औसत निकालकर उस पर 1/3 भाग राज्य कर के रूप में निर्धारित किया गया। यह कर नकद में लिया जाता था, जिससे शासन को नियमित आय प्राप्त होती थी।
मुगल शासन में किसानों की भलाई का ध्यान रखा गया। राज्य कर संग्रहण में अमीन और कारकुन जैसे अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। यदि फसल खराब हो जाती थी तो कर में छूट भी दी जाती थी।
हालाँकि, कुछ काल में स्थानीय जागीरदारों की कठोरता और कर वसूली की प्रणाली किसानों के लिए कष्टदायक सिद्ध हुई। फिर भी अकबर और शाहजहाँ के शासन में कर व्यवस्था तुलनात्मक रूप से न्यायसंगत रही।
प्रश्न-8. नूरजहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- नूरजहाँ का असली नाम मेहरुन्निसा था। वह जहाँगीर की पत्नी और मुग़ल दरबार की अत्यंत प्रभावशाली महिला थीं। उनका विवाह 1611 ई. में जहाँगीर से हुआ था।
नूरजहाँ न केवल सुंदर और बुद्धिमती थीं, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थीं। जहाँगीर की नशे की लत और कमजोर स्वास्थ्य के कारण शासन की बागडोर नूरजहाँ ने अपने हाथों में ले ली थी। वह “नूरजहाँ जुंटा” नामक राजनीतिक गुट की नेता बन गईं।
नूरजहाँ के नाम से सिक्के जारी हुए और सरकारी आदेशों पर उनके हस्ताक्षर होते थे। उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। नूरजहाँ ने जहाँगीर के शासनकाल को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जहाँगीर की मृत्यु के बाद नूरजहाँ ने राजनीतिक जीवन से निवृत्ति ले ली और शांतिपूर्वक जीवन बिताया। उनकी जीवनगाथा मुग़ल इतिहास में स्त्री शक्ति और प्रभाव की अनोखी मिसाल है।
प्रश्न-9. दीन-ए-इलाही का वर्णन कीजिए
उत्तर:- दीन-ए-इलाही अकबर द्वारा 1582 ई. में स्थापित एक धार्मिक विचारधारा थी। यह कोई पूर्ण धर्म नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर तैयार किया गया एक आध्यात्मिक मार्ग था। इसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना और साम्राज्य में सांप्रदायिक एकता स्थापित करना था।
अकबर ने हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और ईसाई विद्वानों के साथ “इबादतखाना” में संवाद किया और महसूस किया कि सत्य किसी एक धर्म में सीमित नहीं है। इसी आधार पर उसने दीन-ए-इलाही की स्थापना की।
इसके अनुयायियों से मांसाहार, शराब, लोभ आदि से दूर रहने को कहा गया। वे सम्राट को ‘ईश्वर का प्रतिनिधि’ मानते थे।
हालाँकि यह संप्रदाय बहुत सीमित रहा और केवल कुछ दरबारी जैसे बीरबल ही इसके सदस्य बने। अकबर के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया।
दीन-ए-इलाही अकबर की धर्मनिरपेक्ष सोच और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, जिसने भारतीय समाज में धर्मों के मध्य संवाद की शुरुआत की।
प्रश्न-10. तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- तुर्क आक्रमण के समय (11वीं-12वीं शताब्दी) भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत दुर्बल थी। देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था, जिनमें आपसी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष व्याप्त था। राजाओं के बीच एकता का अभाव था, जिससे बाहरी आक्रमणकारियों को अवसर मिला।
राजपूत शासक वीर तो थे, परंतु उनके युद्ध नीति में दूरदर्शिता की कमी थी। धर्म और जाति के नाम पर सामाजिक विभाजन था। आर्थिक दृष्टि से भारत सम्पन्न था, जिससे विदेशी लुटेरे आकर्षित हुए। इस समय महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए और अंततः तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की।
प्रश्न-11. शिवाजी के प्रशासन का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- शिवाजी का प्रशासनिक ढांचा अत्यंत संगठित और सुदृढ़ था। उन्होंने एक केंद्रीयकृत व्यवस्था स्थापित की थी जिसमें राजा सर्वोच्च होता था। वे न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे।
शिवाजी ने आठ मंत्रियों की परिषद बनाई जिसे “अष्टप्रधान” कहा जाता था। इसमें पेशवा (प्रधानमंत्री), अमात्य (राजस्व), सुमंत (विदेश), मनत्री (गुप्तचर), सेनापति (सेना प्रमुख), न्यायाधीश, पंडितराव (धार्मिक कार्य) और सचिव (लेखांकन) सम्मिलित थे।
राजस्व प्रणाली भी सुसंगठित थी। उन्होंने मालगुजारी की दर को कम कर किसानों को राहत दी। चुप्त लेखा-परीक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त किए।
सेना संगठन में शिवाजी ने विशेष ध्यान दिया। उन्होंने नियमित सेना रखी, जिसमें पैदल, घुड़सवार और नौसेना सम्मिलित थीं।
न्याय व्यवस्था में राजा अंतिम अपील का माध्यम था। वे धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे और मुस्लिमों के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे।
शिवाजी का प्रशासनिक ढांचा एक आदर्श हिंदवी स्वराज की मिसाल है।
प्रश्न-12. प्रथम पानीपत युद्ध के क्या परिणाम थे?
उत्तर:- प्रथम पानीपत युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहीम लोदी के बीच लड़ा गया।
इस युद्ध में बाबर ने तोपों और संगठित सेना के सहारे विजय प्राप्त की।
मुख्य परिणाम निम्नलिखित हैं:
दिल्ली में लोदी वंश का अंत हुआ।
भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई।
भारत में तोपों और बारूद के युद्ध का आरंभ हुआ।
उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई।
यह युद्ध भारत के इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुआ।
प्रश्न-13. तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए।
उत्तर:-तुर्क आक्रमण (11वीं-12वीं शताब्दी) के समय भारत की राजनीतिक स्थिति विखंडित और दुर्बल थी। देश छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। राजाओं में आपसी संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या थी, जिससे बाहरी आक्रमण के प्रति एकजुट प्रतिरोध नहीं हो सका।
राजपूत राज्य जैसे दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, बंगाल आदि अपनी-अपनी सीमाओं तक सीमित थे। उनमें सामूहिक सुरक्षा की भावना का अभाव था। सामाजिक रूप से जातिवाद और ऊँच-नीच की भावना प्रबल थी।
धार्मिक रूप से ब्राह्मणवाद का प्रभाव था और बौद्ध धर्म कमजोर पड़ चुका था। आर्थिक दृष्टि से भारत समृद्ध था, किंतु राजनीतिक कमजोरी ने उसे विदेशी आक्रमणों के लिए आसान लक्ष्य बना दिया।
महमूद ग़ज़नवी और मोहम्मद गौरी जैसे तुर्क आक्रांताओं ने इस स्थिति का लाभ उठाया और भारत पर बार-बार आक्रमण किए।
इस प्रकार, भारत की बिखरी हुई राजनीतिक संरचना, सामाजिक दुर्बलता और सैन्य असंगठितता तुर्क आक्रमणों का प्रमुख कारण बनी।
प्रश्न-14. शाहजहाँ की दक्षिण नीति की समीक्षा कीजिए।
उत्तर:- शाहजहाँ की दक्षिण नीति का उद्देश्य दक्षिण भारत के राज्यों को मुग़ल साम्राज्य के अधीन लाना था। उसने बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर जैसे राज्यों को कमजोर करने की कोशिश की।
शाहजहाँ ने 1633 में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया, जो उसकी दक्षिण नीति की सबसे बड़ी सफलता थी। इसके बाद उसने बीजापुर और गोलकुंडा पर दबाव बनाया, लेकिन ये राज्य पूर्णतः मुग़ल अधीन नहीं हो पाए।
उसने दक्षिण में अपने बेटे औरंगज़ेब को सूबेदार नियुक्त किया, जिससे वहां मुग़ल प्रभाव बढ़ा। हालांकि, अधिक सैन्य अभियान और स्थानीय विरोध के कारण उसे स्थायी सफलता नहीं मिली।
शाहजहाँ की नीति में संयम और सैन्य शक्ति दोनों का उपयोग था, परंतु दीर्घकालिक दृष्टि से यह पूर्ण सफल नहीं रही। यह औरंगज़ेब के काल में और अधिक उग्र रूप में सामने आई।
प्रश्न-15. “सिक्के इतिहास के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत हैं।” व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- सिक्के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। वे तत्कालीन शासकों, धर्म, संस्कृति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हैं।
सिक्कों पर अंकित तिथियाँ, राजा का नाम, उपाधियाँ, देवी-देवताओं की छवियाँ और लेख हमें उस काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति से परिचित कराते हैं।
जैसे मौर्य काल के पंचमार्क सिक्के, कुषाणों के यूनानी-रोमन प्रभाव वाले सिक्के, गुप्तकाल के स्वर्ण मुद्रा आदि महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं।
सिक्के स्थायी होते हैं और उनके माध्यम से इतिहासकार काल-निर्धारण भी कर सकते हैं। इसलिए इन्हें सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है।
प्रश्न-16. मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? इसके लाभ व हानियाँ लिखिए
उत्तर:- मनसबदारी व्यवस्था मुग़ल प्रशासन की एक विशिष्ट प्रणाली थी, जिसे अकबर ने शुरू किया। इसमें प्रत्येक अधिकारी को “मनसब” यानी पद दिया जाता था, जो उसकी रैंक और वेतन तय करता था।
मनसबदारों को ज़ात (व्यक्तिगत रैंक) और सवार (सेना की संख्या) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था। वे सुल्तान के प्रति वफादार रहते थे और समय पर सेना उपलब्ध करवाते थे।
लाभ:
इससे केंद्रीकृत प्रशासन मजबूत हुआ।
सेना का संगठन सुसंगठित रहा।
योग्य व्यक्तियों को स्थान मिला।
हानियाँ:
मनसबदार अधिकतर वेतनभोगी थे, जिससे वित्तीय भार बढ़ा।
कुछ मनसबदारों ने निजी हित साधे और भ्रष्टाचार बढ़ा।
यह प्रणाली स्थानीय स्वतंत्रता को कमजोर करती थी।
यह व्यवस्था मुग़ल शासन के विस्तार और स्थायित्व में सहायक रही, परंतु दीर्घकाल में वित्तीय और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हुईं।
प्रश्न-17. मनसबदारी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को बताइए।
उत्तर:- मनसबदारी व्यवस्था मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। यह ‘मनसब’ अर्थात पद/रैंक पर आधारित थी। प्रत्येक मनसबदार को एक रैंक दी जाती थी, जिसे ‘जात’ और ‘सवार’ द्वारा दर्शाया जाता था।
‘जात’ से व्यक्ति की सामाजिक हैसियत और वेतन निर्धारित होता था, जबकि ‘सवार’ से वह संख्या तय होती थी जितने घुड़सवार सैनिक मनसबदार को रखने होते थे। मनसबदारों को नकद वेतन दिया जाता था, कभी-कभी जागीर भी दी जाती थी।
इस व्यवस्था की विशेषता यह थी कि यह जाति या वंश के आधार पर नहीं, योग्यता और निष्ठा के आधार पर पद प्रदान करती थी। इसके अंतर्गत प्रशासनिक और सैनिक दोनों कर्तव्य निभाने होते थे।
यह प्रणाली मुगल साम्राज्य को एक केंद्रीकृत प्रशासनिक स्वरूप प्रदान करती थी और सम्राट की शक्ति को मज़बूत करती थी। यह व्यवस्था औरंगज़ेब के काल तक चलती रही।
प्रश्न-18. कृष्णदेवराय की उपलब्धियाँ बताइए।
उत्तर:- कृष्णदेवराय (शासनकाल: 1509-1529 ई.) विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। वे तुलुव वंश से थे और अपने पराक्रम, प्रशासनिक क्षमता और सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं।
राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने बहमनी सुल्तानों, बीजापुर और गोलकोंडा जैसे मुस्लिम शासकों को पराजित कर साम्राज्य को सुदृढ़ किया। उन्होंने उड़ीसा, मदुरै और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में भी विजय प्राप्त की।
प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने सिंचाई, सड़क निर्माण, भूमि व्यवस्था और न्याय प्रणाली को सुधारित किया। कृषकों के लिए अनेक योजनाएँ चलाईं।
सांस्कृतिक रूप से वे एक महान संरक्षक थे। वे स्वयं तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ के विद्वान थे। उन्होंने ‘अमुक्तमाल्यद’ नामक प्रसिद्ध तेलुगु काव्य की रचना की। उनके दरबार में आठ प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें ‘अष्टदिग्गज’ कहा जाता है।
कृष्णदेवराय के काल को विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनकी उपलब्धियाँ उन्हें दक्षिण भारत का एक महान शासक सिद्ध करती हैं।
प्रश्न-19. “सिक्के इतिहास के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत हैं।” विवेचना कीजिए।
उत्तर:- सिक्के इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। ये शासकों के समय, राजनीतिक परिस्थितियों, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की जानकारी देते हैं।
सिक्कों पर राजा का नाम, उपाधियाँ, वर्ष, धर्म, प्रतीक, भाषा, लिपि आदि अंकित होते हैं। उदाहरण के लिए, गुप्तकालीन सिक्कों से हमें समृद्धि, कला तथा धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी मिलती है।
सिक्कों से व्यापारिक संबंधों, विदेशी संपर्कों तथा मुद्राओं के विनिमय की जानकारी भी मिलती है। वे किसी कालखंड की अर्थव्यवस्था का दर्पण होते हैं।
कई बार जब लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते, तब सिक्के एकमात्र साक्ष्य के रूप में सामने आते हैं। ये शासकों की वैधता और अधिकार का प्रमाण होते हैं।
इस प्रकार, सिक्के केवल मुद्रा नहीं बल्कि इतिहास का जीता-जागता दस्तावेज होते हैं।
प्रश्न-20. बलबन के राजतंत्र के सिद्धांत की समझाइए।
उत्तर:- सुल्तान बलबन (1266-1287 ई.) ने दिल्ली सल्तनत को मज़बूती देने के लिए ‘राजत्व के सिद्धांत’ को प्रबल बनाया। उसने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना और ‘जिल्ल-ए-इलाही’ (ईश्वर की छाया) की संकल्पना को बढ़ावा दिया।
उसका मानना था कि सुल्तान को कठोर, निरंकुश और दिव्य अधिकार प्राप्त शासक होना चाहिए ताकि राज्य में अनुशासन और स्थिरता बनी रहे। बलबन ने ‘न्याय’ और ‘दण्ड’ (जब्त) को राज्य का मूल आधार बताया।
उसने अमीरों और दरबारियों की शक्ति को कम किया, दरबारी अनुशासन सख्त बनाया और ‘सिजदा’ तथा ‘पैबोस’ जैसी प्रथाओं को लागू किया जिससे सुल्तान की श्रेष्ठता प्रदर्शित हो।
बलबन ने धर्मगुरुओं और कुलीन वर्ग को दरबार से दूर कर दिया और केवल सुल्तान को राज्य का केन्द्र बिंदु बनाया। उसका राजतंत्र सिद्धांत भारत में सुल्तानी निरंकुशता की नींव था।
प्रश्न-21. कर-प्रणाली के स्वरूप की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- मध्यकालीन भारत में कर-प्रणाली (Taxation System) मुख्यतः भूमि आधारित थी। भूमि से उपज के अनुसार कर वसूला जाता था। यह कर “भोग”, “उपजीव” या “राजस्व” कहलाता था।
अलाउद्दीन खिलजी ने उपज के अनुसार 50% कर निर्धारित किया था, जो कठोर था। अकबर ने टोडरमल के माध्यम से ‘दहसाला प्रणाली’ लागू की, जिसमें उपज का औसत निकालकर कर तय किया जाता था।
कर नकद या अनाज में लिया जाता था। इसके अलावा, व्यापार कर, पशु कर, सिंचाई कर, विवाह कर आदि भी लगाए जाते थे। कभी-कभी विशेष कर जैसे “जजिया” (गैर-मुस्लिमों पर) भी वसूला जाता था।
कर-प्रणाली स्थानीय अधिकारी जैसे अमील, करोरी, मुकद्दम, आदि के माध्यम से संचालित होती थी। कभी-कभी इसमें भ्रष्टाचार भी होता था।
समय के साथ कर प्रणाली में सुधार होते रहे, लेकिन कृषकों पर बोझ बना रहा।
इस प्रकार भारत की कर-प्रणाली कृषि पर आधारित, क्षेत्रीय रूप से विविध और कभी-कभी शोषणकारी रही।
प्रश्न-22. जौहर एवं सती प्रथा की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- जौहर प्रथा युद्ध के समय राजपूत स्त्रियों द्वारा आत्मरक्षा हेतु अपनाई जाती थी। जब पराजय निश्चित होती थी, तो स्त्रियाँ अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्याग देती थीं। यह प्रथा मेवाड़, चित्तौड़ और राणा रत्नसिंह के समय प्रसिद्ध हुई।
सती प्रथा में पति की मृत्यु पर पत्नी को उसकी चिता में जलाया जाता था। यह प्रथा सामाजिक परंपराओं के तहत प्रचलित थी और इसे धार्मिक गौरव का रूप दिया गया था।
दोनों प्रथाएँ स्त्रियों के प्रति समाज की कठोरता को दर्शाती हैं। सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड बेंटिक द्वारा कानूनी रूप से समाप्त किया गया।
इन प्रथाओं की आलोचना सामाजिक सुधारकों ने की और इन्हें अमानवीय माना गया।
प्रश्न-23. चित्तौड़ किले के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:- चित्तौड़ किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह भारत के सबसे विशाल और ऐतिहासिक किलों में से एक है। यह किला अरावली पर्वत की पहाड़ियों पर बना हुआ है और लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैला है।
यह किला मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। बाद में यह गुहिल, सिसोदिया और अन्य राजपूत शासकों का प्रमुख गढ़ बना।
चित्तौड़ किला तीन प्रसिद्ध ‘जौहर’ की घटनाओं का साक्षी रहा है — रानी पद्मिनी (1303), रानी कर्णावती (1535) और तीसरा अकबर के समय।
किले में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, पद्मिनी महल, राणा कुंभा महल आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। विजय स्तंभ राणा कुम्भा द्वारा महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया।
चित्तौड़ किला राजपूती वीरता, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है।
प्रश्न-24. मनसबदारी प्रथा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- मनसबदारी प्रथा मुग़ल शासक अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। ‘मनसब’ का अर्थ होता है – पद या दर्जा। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों को सैन्य और नागरिक कार्यों के लिए मनसब प्रदान किया जाता था।
प्रत्येक मनसबदार को दो अंक दिए जाते थे – जात और सवार। ‘जात’ से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और वेतन तय होता था, जबकि ‘सवार’ से उसके अधीन घुड़सवार सैनिकों की संख्या निश्चित होती थी।
मनसबदारों को नकद वेतन या जगीरें प्रदान की जाती थीं। वे मुग़ल प्रशासन के मूल स्तंभ माने जाते थे।
इस प्रणाली से सेना का विस्तार, नियंत्रण और संगठन आसान हुआ। और शासक को सेना पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ।
हालांकि, कालांतर में इस प्रणाली में भ्रष्टाचार बढ़ा और सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। फिर भी, मनसबदारी प्रथा मुग़ल प्रशासन की एक विशेषता थी और लंबे समय तक बनी रही।
प्रश्न-25. समाज की प्रति मीरा के योगदान को बताइए।
उत्तर:- मीरा बाई एक महान भक्त कवयित्री थीं, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए समाज को भक्ति और समर्पण का संदेश दिया।
उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल कायम की, जब उन्होंने रूढ़ियों और सामाजिक बंधनों को तोड़ा।
मीरा के भजनों में प्रेम, त्याग, आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास दिखाई देता है।
उन्होंने जाति, लिंग और धार्मिक सीमाओं को तोड़ते हुए भक्ति आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाया।
उनका जीवन समाज में समानता, सहिष्णुता और भक्ति मार्ग का आदर्श बना। आज भी उनके भजन लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं।
प्रश्न-26. तुलसीदास के समाज के प्रति योगदान का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- तुलसीदास (1532–1623 ई.) एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने ‘रामचरितमानस’ की रचना की, जो हिंदी भाषा में लिखी गई और जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय हुई।
तुलसीदास ने समाज को धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराया। उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया और समाज में प्रेम, समर्पण और सेवा की भावना को जगाया।
उनकी रचनाएँ जाति-पाति से ऊपर उठकर सभी के लिए समान रूप से उपयोगी थीं। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक पाखंड, ब्राह्मणवाद की कट्टरता और सामाजिक विषमता का विरोध किया।
‘रामराज्य’ की कल्पना द्वारा उन्होंने एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया जहाँ न्याय, करुणा और सेवा भाव प्रधान थे।
तुलसीदास ने लोगों को आत्मबल, धर्मपरायणता और नैतिक आचरण की प्रेरणा दी। उनके साहित्य ने भारतीय समाज में भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ किया।
इस प्रकार तुलसीदास का योगदान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार और जनजागरण के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रश्न-27. रणथंभौर किले के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:- रणथंभौर किला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह किला प्राचीनता, वास्तुकला और वीरता का प्रतीक माना जाता है।
इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के शासकों द्वारा किया गया था। यह अरावली और विन्ध्य की पहाड़ियों के बीच स्थित है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर आता है।
रणथंभौर का किला रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और कई बार इस पर आक्रमण हुए। 1301 ई. में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी।
इस किले में कई मंदिर, महल और जलाशय स्थित हैं। यह स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है।
आज यह किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है।
Section-C
प्रश्न-1.भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भारतीय इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोतों का विशेष महत्त्व है। इन स्रोतों से न केवल घटनाओं की जानकारी मिलती है, बल्कि तत्कालीन समाज, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की भी झलक मिलती है। भारतीय साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बाँटा जा सकता है – धार्मिक और लौकिक।
(1) धार्मिक ग्रंथ:
वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद – वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करते हैं।
उपनिषद: दार्शनिक ग्रंथ हैं जो आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष पर प्रकाश डालते हैं।
रामायण और महाभारत: ये महाकाव्य धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं।
पुराण: अठारह पुराणों में इतिहास, भूगोल, वंशावलियाँ और धर्म का वर्णन मिलता है।
(2) लौकिक साहित्य:
सूत ग्रंथ: अर्थशास्त्र (कौटिल्य द्वारा), जो मौर्यकाल की राजनीति और प्रशासन का महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
राजतरंगिणी: कल्हण द्वारा रचित, कश्मीर के इतिहास का विस्तृत वर्णन करती है।
हर्षचरित: बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी देती है।
बौद्ध साहित्य: त्रिपिटक, जातक कथाएँ – बौद्ध धर्म के साथ-साथ तत्कालीन समाज और राजनीति को समझने का स्रोत हैं।
जैन साहित्य: आगम ग्रंथ, जो जैन धर्म और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं।
इसके अलावा विदेशी यात्रियों जैसे फाह्यान, ह्वेनसांग, अलबरूनी और इब्न बतूता की रचनाएँ भी मूल्यवान साहित्यिक स्रोत हैं। इन स्रोतों की सहायता से हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.क्षेत्रीय शक्तियों बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात के उदय पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत की सत्ता जब कमजोर हुई, तब देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इन शक्तियों ने स्वतंत्र रूप से शासन किया और अपने-अपने क्षेत्रों में सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को प्रोत्साहित किया। प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं: बंगाल, जौनपुर, मालवा और गुजरात।
- बंगाल:
बंगाल में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना 14वीं शताब्दी में शम्सुद्दीन इलियास शाह ने की। बंगाल की भौगोलिक स्थिति ने इसे राजनीतिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक समृद्धि का अवसर दिया। बंगाल में मुस्लिम संस्कृति और बंगाली भाषा का सुंदर समन्वय हुआ। यहाँ हुसैन शाह के काल में कला और साहित्य का विकास हुआ। - जौनपुर:
जौनपुर सल्तनत की स्थापना फिरोज तुगलक के शासनकाल में मलिक सरवर ने की थी। यह शक्ति शार्क वंश के अधीन विकसित हुई। जौनपुर एक प्रमुख शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बना, जिसे “शिराज-ए-हिंद” कहा गया। यहाँ फारसी भाषा और इस्लामी शिक्षा का विस्तार हुआ। - मालवा:
मालवा में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना दिलावर खाँ गौरी ने की। यहाँ खलीलुल्लाह और गियासुद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने कला, वास्तुकला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। मांडू मालवा की राजधानी बनी, जहाँ स्थापत्यकला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। - गुजरात:
गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जफर खाँ मुज़फ्फर ने की थी। मुजफ्फर वंश के शासकों ने व्यापार, कला और स्थापत्य को प्रोत्साहित किया। अहमदाबाद नगर की स्थापना अहमदशाह ने की, जो व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बना।
इन सभी क्षेत्रीय शक्तियों ने न केवल अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, बल्कि सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय गौरव को भी पुनर्जीवित किया। उनके काल में कला, साहित्य, संगीत, स्थापत्य और व्यापार का अद्वितीय विकास हुआ। यद्यपि ये शक्तियाँ बाद में मुगलों के अधीन आ गईं, फिर भी इनके योगदान को इतिहास में सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता है।
प्रश्न-भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोत (Archaeological Sources) अत्यंत महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। इन स्रोतों से हमें उन कालों की जानकारी मिलती है, जब कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। पुरातत्व स्रोतों के अंतर्गत स्थायी संरचनाएँ, अभिलेख, मुद्राएँ, औज़ार, हथियार, अस्थियाँ, मृदभांड (मिट्टी के बर्तन), भवन अवशेष आदि आते हैं।
भारत में पुरातात्विक खोज का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ जब सर अलेक्ज़ेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की स्थापना की। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में की गई, जिससे शहरी जीवन, जल प्रबंधन और व्यापार व्यवस्था की जानकारी मिली।
मुख्य पुरातात्विक स्रोत:
- स्थापत्य अवशेष: मंदिर, स्तूप, गुफाएँ और महल जैसे स्थापत्य ढांचे प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे — साँची का स्तूप, नालंदा विश्वविद्यालय, एलोरा की गुफाएँ।
- अभिलेख (Inscriptions): ये पत्थर, धातु, स्तंभों या ताम्रपत्रों पर खुदे होते हैं। जैसे — अशोक के शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख आदि। इनसे राजाओं की नीतियों, युद्धों और धर्म का विवरण मिलता है।
- मुद्राएँ (Coins): सिक्कों से आर्थिक स्थिति, व्यापारिक संपर्क, धर्म और राजाओं की सत्ता का अनुमान होता है। जैसे — कुषाण, गुप्त और मौर्य वंश के सिक्के।
- मृदभांड और औजार: ये मानव सभ्यता की तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं। हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड, खेती के औज़ार, शिकार और युद्ध के हथियार इसका उदाहरण हैं।
- कब्रें और अस्थियाँ: ये जीवनशैली, मृत्यु संस्कार और समाजिक ढांचे को दर्शाते हैं।
भारतीय इतिहास की प्राचीनतम जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। ये स्रोत न केवल ऐतिहासिक घटनाओं की पुष्टि करते हैं, बल्कि समाज, संस्कृति, धर्म, कला और जीवनशैली की झलक भी प्रदान करते हैं।
प्रश्न-4. शिवाजी पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- छत्रपति शिवाजी महाराज (1630–1680) मराठा साम्राज्य के संस्थापक और भारत के महानतम राष्ट्रनायकों में से एक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के सेनानायक थे और माता जीजाबाई एक धर्मपरायण महिला थीं, जिनका शिवाजी के संस्कारों पर गहरा प्रभाव पड़ा।
शिवाजी ने युवावस्था में ही आदिलशाही शासन के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी। उन्होंने किलों पर अधिकार कर और गुरिल्ला युद्ध नीति (गणिमी कावा) द्वारा बड़े-बड़े शक्तिशाली दुर्ग जीत लिए। उन्होंने तोरणा, राजगढ़, पुरंदर, सिंधुदुर्ग, प्रतापगढ़ जैसे किलों को जीता।
शिवाजी एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था लागू की और किसानों को सुरक्षा व न्याय प्रदान किया। उनके मंत्रिमंडल को ‘अष्टप्रधान परिषद’ कहा जाता था। उन्होंने सेना को नियमित वेतन पर रखा और अनुशासनात्मक प्रणाली लागू की।
1664 में उन्होंने सूरत पर आक्रमण कर मुगलों को बड़ी आर्थिक क्षति पहुंचाई। 1666 में औरंगजेब द्वारा उन्हें आगरा बुलवाकर बंदी बना लिया गया, लेकिन वे चतुराई से वहाँ से निकल भागे। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें “छत्रपति” की उपाधि मिली।
शिवाजी की धार्मिक नीति उदार थी। वे एक कट्टर हिंदू होते हुए भी मुसलमानों की मस्जिदों, औरतों या धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वे धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक उद्देश्य से युद्ध करते थे। उन्होंने भारत में एक स्वदेशी हिन्दू राज्य की नींव रखी जो बाद में पेशवाओं के अधीन बढ़ता गया।
निष्कर्षतः, शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता, वीर सेनानायक, दूरदर्शी शासक और धार्मिक सहिष्णु नेता थे। उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का विचार जाग्रत किया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना।
प्रश्न-5. भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये स्रोत प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को समझने में सहायक होते हैं। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—धार्मिक और लौकिक।
- धार्मिक साहित्य:
धार्मिक साहित्य में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते हैं।
वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद) वैदिक युग की सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था का ज्ञान कराते हैं।
महाभारत और रामायण सामाजिक मूल्यों, युद्धों, और राजनीतिक संरचना की जानकारी देते हैं।
पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, राजवंशों का वर्णन, धार्मिक अनुष्ठानों की व्याख्या होती है।
- लौकिक साहित्य:
इसमें इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र व दर्शन से संबंधित ग्रंथ आते हैं।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकाल की शासन प्रणाली, प्रशासन व अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है।
बाणभट्ट का हर्षचरित हर्षवर्धन के जीवन और शासन का विवरण देता है।
कालिदास की रचनाएँ (रघुवंश, कुमारसंभव) तत्कालीन समाज व संस्कृति को प्रतिबिंबित करती हैं।
राजतरंगिणी (कल्हण द्वारा रचित) कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताती है।
- विदेशी यात्रियों के वृत्तांत:
चीनी यात्रियों (फाह्यान, ह्वेनसांग) और अरब लेखकों (अल-बेरूनी, इब्न बतूता) की रचनाएँ भारत की राजनीति, शिक्षा, धर्म व जीवनशैली का मूल्यवान विवरण प्रदान करती हैं।
इस प्रकार, साहित्यिक स्रोत भारतीय इतिहास की गहराई और विविधता को उजागर करते हैं।
प्रश्न-6. क्षेत्रीय शक्तियों (बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात) के उदय पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- दिल्ली सल्तनत के कमजोर पड़ने के साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र या अर्ध-स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें क्षेत्रीय शक्तियाँ कहा जाता है। बंगाल, जौनपुर, मालवा और गुजरात इनमें प्रमुख थे।
- बंगाल:
बंगाल की स्वतंत्र सत्ता की नींव शम्सुद्दीन इलियास शाह (1342 ई.) ने रखी।
यह शक्ति आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थी और यहाँ की राजधानी गौड़ एक प्रमुख व्यापार केंद्र बनी।
हुसैन शाह के काल में बंगाल ने सांस्कृतिक और राजनीतिक ऊँचाई प्राप्त की।
- जौनपुर:
जौनपुर राज्य की स्थापना फिरोजशाह तुगलक के वंशज मलिक सरवर ने की।
यह राज्य शिक्षा और स्थापत्य कला का केंद्र बना।
इब्राहिम शर्की जैसे शासकों के काल में जौनपुर ने स्वतंत्र शक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त की।
- मालवा:
मालवा की राजधानी मांडू थी और यहाँ ग़ोरी वंश ने शासन किया।
होशंगशाह और महमूद खिलजी जैसे शासकों ने राज्य का विस्तार किया।
मालवा स्थापत्य कला और चित्रकला का केंद्र बना।
- गुजरात:
अहमदशाह प्रथम ने गुजरात सल्तनत की नींव रखी।
इस क्षेत्र में व्यापार अत्यंत समृद्ध था, विशेषकर कपड़ा, मोती और मसालों का।
मुजफ्फरशाही वंश ने गुजरात को सांस्कृतिक उन्नति दी।
इन क्षेत्रीय शक्तियों ने भारतीय इतिहास में विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और प्रशासनिक नवाचार को जन्म दिया। दिल्ली सल्तनत के पतन के समय इन्होंने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी।
प्रश्न-7. फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति का परीक्षण कीजिए।
उत्तर:- फिरोज तुगलक (1351-1388 ई.) दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। वह एक धार्मिक, रूढ़िवादी और कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति पर उलेमाओं और इस्लामी सिद्धांतों का गहरा प्रभाव था। उसने अपनी धार्मिक नीतियों के माध्यम से राज्य में इस्लामी सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया।
फिरोज की धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार और विस्तार करना था। उसने गैर-मुस्लिमों पर जजिया कर को फिर से कठोरता से लागू किया, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी इससे मुक्त नहीं रखा। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाया और वहाँ मस्जिदें बनवाईं।
फिरोज तुगलक ने इस्लामी कानून (शरीयत) को सख्ती से लागू किया। दंड नीति में भी उसने शरीयत का पालन किया और अनेक बार कठोर सजाएँ दी गईं। उसका शासनकाल धर्मनिरपेक्षता की अपेक्षा धार्मिक पक्षपात का परिचायक रहा।
हालाँकि उसने कई धार्मिक कार्य किए – जैसे मदरसे, मस्जिदें, खानकाहों का निर्माण, कुरान के प्रचार हेतु संस्थाओं की स्थापना – परंतु उसकी नीति में असहिष्णुता झलकती थी। उसने असैनिक प्रशासन में उलेमाओं और धार्मिक विद्वानों को महत्त्वपूर्ण पद दिए, जिससे धर्म का हस्तक्षेप बढ़ा।
फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति मुस्लिम कट्टरता की परिचायक थी, जिसने राज्य की सामाजिक एकता को प्रभावित किया और हिंदू प्रजा में असंतोष बढ़ाया। उसकी नीतियाँ धार्मिक सहिष्णुता से दूर थीं, जो आगे चलकर सल्तनत की कमजोरी का कारण बनीं।
प्रश्न-8. अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- अकबर (1556–1605) मुगल साम्राज्य का तीसरा और सबसे महान शासक था। उसकी सबसे प्रभावशाली नीतियों में से एक थी उसकी राजपूत नीति, जिसने मुगल शासन को स्थायित्व और लोकप्रियता प्रदान की।
अकबर ने राजपूतों को पराजित करने की बजाय उनके साथ मित्रता और सहयोग की नीति अपनाई। उन्होंने कई राजपूत राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उनसे वैवाहिक संबंध भी किए। उदाहरण के लिए, उन्होंने आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधा बाई से विवाह किया। यह संबंध केवल वैवाहिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी था।
राजपूतों को उच्च प्रशासनिक पद दिए गए जैसे मानसिंह, भगवानदास, तोदरमल आदि। मानसिंह को अकबर के नवरत्नों में भी स्थान प्राप्त था। राजपूतों को सेना और प्रशासन में बराबर की भागीदारी मिली, जिससे वे मुगलों के विश्वासपात्र बन गए।
अकबर ने मेवाड़ के शासक राणा प्रताप को अपने अधीन लाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। फिर भी अकबर ने उनके प्रति भी कोई धार्मिक दमन नहीं किया। हल्दीघाटी का युद्ध (1576) इस संघर्ष का उदाहरण है।
अकबर की राजपूत नीति ने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और साम्राज्य को स्थायित्व दिया। इस नीति के फलस्वरूप मुगल शासन अधिक मजबूत और व्यापक बना। यह नीति धार्मिक सहिष्णुता और व्यावहारिक राजनीति का उत्तम उदाहरण है।
अकबर की राजपूत नीति समन्वय, सहयोग और सहिष्णुता पर आधारित थी, जिसने साम्राज्य की नींव को स्थायी बनाया और बाद के शासकों को एक प्रभावशाली प्रशासनिक ढांचा सौंपा।
प्रश्न-9. अकबर की राजपूत नीति का परीक्षण कीजिए।
उत्तर:- अकबर की राजपूत नीति मुग़ल साम्राज्य की सबसे सफल राजनीतिक रणनीतियों में से एक मानी जाती है। उसने बल के स्थान पर संवाद और समावेशन की नीति अपनाई जिससे राजपूतों को मुग़ल सत्ता में शामिल किया गया और साम्राज्य को स्थायित्व मिला।
अकबर की राजपूत नीति के मुख्य बिंदु:
- राजपूतों से वैवाहिक संबंध: अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधा बाई से विवाह किया। इस प्रकार उसने हिंदू राजपरिवारों को सम्मान दिया।
- राजपूतों को उच्च पद: अकबर ने अनेक राजपूत सरदारों को मनसबदारी दी और प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। जैसे — राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, राजा भगवानदास आदि।
- धार्मिक सहिष्णुता: अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। उसने ‘इबादत खाना’ की स्थापना की जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों से संवाद हुआ।
- आधिपत्य स्वीकार: अधिकांश राजपूत रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। उन्होंने युद्धों के बजाय मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे।
- विद्रोही राजपूतों के प्रति नीति: जो राजपूत अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, उनके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई, जैसे — राणा प्रताप। परंतु अकबर ने कभी अपमानजनक व्यवहार नहीं किया।
अकबर की राजपूत नीति के परिणाम:
साम्राज्य को राजनीतिक स्थायित्व मिला।
प्रशासन में राजपूतों की भागीदारी से अखिल भारतीय एकता मजबूत हुई।
धर्मनिरपेक्षता की भावना विकसित हुई।
परंतु मेवाड़ जैसे क्षेत्र पूरी तरह अधीन नहीं हो सके।
अकबर की राजपूत नीति ने मुग़ल शासन को मजबूती दी और उसे एक सर्वधर्म समभाव आधारित शासन बनाने में सफलता दिलाई। यह नीति उसकी दूरदर्शिता और राजनीतिक चातुर्य का प्रतीक है।
प्रश्न-10. मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष को रेखांकित कीजिए।
उत्तर:- महाराणा प्रताप भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वे मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक थे और उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। उनका संकल्प था कि वे कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि उनके समकालीन कई राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
महाराणा प्रताप के संघर्ष का सबसे प्रमुख अध्याय हल्दीघाटी का युद्ध (1576 ई.) था। इस युद्ध में उन्होंने मुगल सेना से डटकर मुकाबला किया। यद्यपि यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन इससे प्रताप की वीरता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण का परिचय मिला। अकबर ने उन्हें अधीन करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया।
हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने पहाड़ों और जंगलों में रहकर छापामार युद्ध नीति अपनाई। उन्होंने धीरे-धीरे मेवाड़ के अनेक क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया। भामाशाह जैसे समर्पित सेवकों की सहायता से उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया।
महाराणा प्रताप का संघर्ष केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी प्रेरणादायक था। उन्होंने घास की रोटी खाई, किंतु मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। उनके इस संघर्ष ने आने वाली पीढ़ियों को आत्मबल, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।
उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई, लेकिन वे इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में अमर हो गए जो अंतिम साँस तक स्वतंत्रता के लिए लड़ा।
प्रश्न-11. मुगलों के पतन के क्या कारण थे?
उत्तर:- मुगल साम्राज्य जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के काल में अपने चरम पर था, 18वीं शताब्दी में तेजी से पतन की ओर बढ़ा। इस पतन के कई कारण थे:
- औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति – उन्होंने जजिया कर पुनः लगाया, मंदिर तोड़े और गैर-मुस्लिमों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई, जिससे राजपूत, सिख और मराठे उनके विरोधी हो गए।
- लगातार युद्ध – विशेषकर दक्षिण भारत में औरंगजेब के लंबे युद्धों ने खजाने को खाली कर दिया और सेना को थका दिया।
- उत्तराधिकार संघर्ष – हर बादशाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर भाई-भाई में संघर्ष होता था, जिससे साम्राज्य कमजोर होता गया।
- क्षेत्रीय शक्तियों का उदय – मराठा, सिख, जाट, राजपूत और नवाबों ने स्वतंत्रता की नीति अपनाई, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई।
- ब्रिटिश और यूरोपीय हस्तक्षेप – अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने हस्तक्षेप शुरू किया और धीरे-धीरे सत्ता हथियाने लगे।
- प्रशासनिक भ्रष्टाचार – अधिकारी स्वार्थी और भ्रष्ट हो गए, जिससे आम जनता का विश्वास शासन से उठ गया।
- सांस्कृतिक ठहराव और नवाचार की कमी – मुगलों ने पुराने तौर-तरीकों को बनाए रखा, जबकि यूरोप औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति कर रहा था।
धार्मिक कट्टरता, युद्ध, आंतरिक संघर्ष और बाहरी हस्तक्षेप मुगलों के पतन के प्रमुख कारण बने। यह साम्राज्य एक विशाल ढांचा था जो अपनी ही कमजोरियों से ढह गया।
प्रश्न-12. सामंतवाद के विकास के कारणों का परीक्षण कीजिए
उत्तर:- सामंतवाद (Feudalism) एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसमें भूमि के बदले सेवा या कर के आधार पर संबंध स्थापित होता है। भारत और यूरोप में अलग-अलग कारणों से सामंतवाद विकसित हुआ, परंतु कुछ सामान्य कारण भी दिखाई देते हैं।
भारत में सामंतवाद के विकास के प्रमुख कारण:
- गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक विकेन्द्रीकरण: गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। क्षेत्रीय शक्तियों ने स्वतंत्रता ग्रहण की और भूमि पर अपना अधिकार स्थापित किया।
- भूमि अनुदान प्रणाली (Land Grants): ब्राह्मणों और सैनिकों को भूमि अनुदान देने की परंपरा से सामंत वर्ग उभरा। ये लोग बाद में स्थानीय शासनकर्ता बन गए।
- स्थानीय प्रशासन में सामंतों की भूमिका: राजा ने प्रशासन का बोझ कम करने के लिए सामंतों को अधिकार दिए। वे कर वसूली, न्याय और सैन्य कार्यों में स्वतंत्र हो गए।
- युद्धों का प्रभाव: निरंतर युद्धों और आक्रमणों के कारण शक्तिशाली योद्धाओं को भूमि देकर उनका समर्थन प्राप्त किया गया, जिससे वे क्षेत्रीय शक्तियों में परिवर्तित हो गए।
- कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था: कृषकों और ज़मींदारों के बीच भूमि आधारित संबंधों से एक स्थायी सामंतवादी ढांचा खड़ा हो गया।
- धार्मिक समर्थन: धर्म ने भी सामंतों को वैधता दी। ब्राह्मणों को भूमि दान कर राजा ने अपने शासन को धार्मिक समर्थन दिलाया।
परिणाम:
ग्रामीण समाज में प्रभु–कृषक संबंध मजबूत हुआ।
राजनीतिक विकेन्द्रीकरण बढ़ा और केंद्र कमजोर हुआ।
कृषक वर्ग का शोषण बढ़ा।
सामंतों के बीच आपसी संघर्ष और सत्ता की लड़ाई शुरू हुई।
सामंतवाद का विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम था। यह प्रणाली एक ओर प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक असमानता और कृषक शोषण का भी प्रतीक है।
प्रश्न-13. सामंतवाद के विकास के कारणों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर:- सामंतवाद एक ऐसी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था है जिसमें भूमि प्रमुख उत्पादन साधन होता है और समाज राजा, सामंत (जमींदार), और कृषक जैसे वर्गों में बँटा होता है। भारत और यूरोप दोनों में सामंतवाद का विकास विशेष ऐतिहासिक कारणों से हुआ।
भारत में सामंतवाद के विकास के कारण:
- गुप्तकालीन प्रशासनिक परिवर्तन – गुप्तकाल में भूमि कर की वसूली के लिए राजाओं ने अधिकारियों को भूमि दान में दी, जिससे वे धीरे-धीरे स्वायत्त हो गए और सामंत बन गए।
- भूमि दान की परंपरा – ब्राह्मणों को कृषि योग्य भूमि दान दी जाती थी, जिससे सामाजिक शक्ति उनके हाथ में आई।
- मौर्य और गुप्त शासन के पतन के बाद – केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और स्थानीय शक्तियाँ मजबूत हुईं, जिससे सामंतों का उदय हुआ।
- कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था – व्यापार की जगह कृषि पर आधारित व्यवस्था में भूमि और उसे नियंत्रित करने वाले सामंत प्रभावशाली बन गए।
- विदेशी आक्रमणों और सुरक्षा की आवश्यकता – शासकों ने सुरक्षा हेतु सामंतों को क्षेत्रीय नियंत्रण सौंपा, जिन्होंने बाद में अपने क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया।
यूरोप में सामंतवाद के कारण:
- रोमन साम्राज्य का पतन – केंद्रीय सत्ता के विघटन के बाद सुरक्षा और प्रशासन के लिए स्थानीय प्रभुओं ने नियंत्रण संभाला।
- स्थानीयकरण की प्रवृत्ति – गांवों में आत्मनिर्भर इकाइयाँ बनीं और भूमि स्वामी ही प्रभुत्वशाली हो गए।
- धार्मिक संस्थानों का समर्थन – चर्च ने सामंतवाद को वैधता दी और भूमि का बड़ा हिस्सा उनके पास रहा।
सामंतवाद का विकास राजनैतिक अस्थिरता, भूमि केंद्रित अर्थव्यवस्था, सुरक्षा की आवश्यकता और सामाजिक संरचना में परिवर्तन के कारण हुआ। यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन था जो बाद में मध्यकालीन समाज की रीढ़ बना।
VMOU HI-03 Paper , vmou ba 2nd year exam paper , vmou exam paper , vmou exam paper question answer , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4
VMOU EXAM PAPER