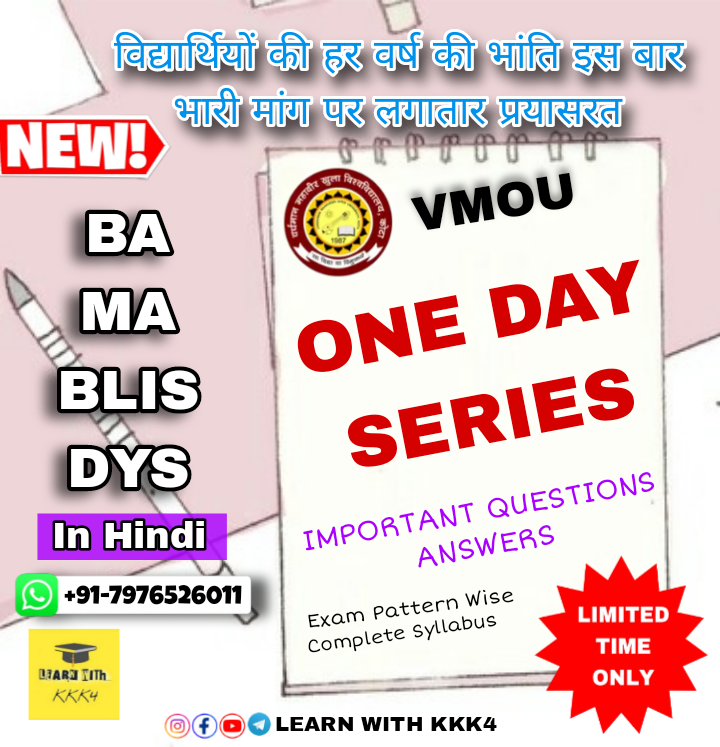VMOU MASO-06 Paper MA Final Year ; vmou exam paper
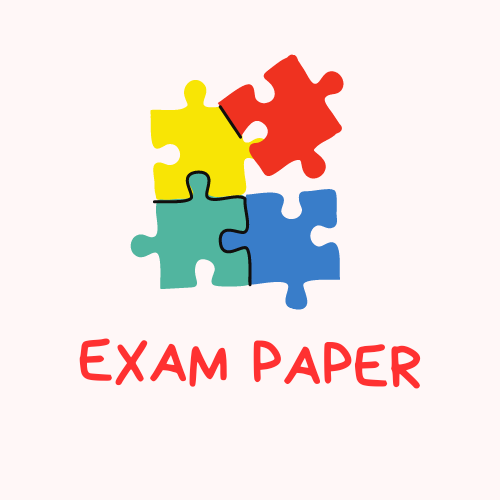
VMOU MA Final Year के लिए Sociology ( MASO-06 , ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.प्रत्यक्षवाद से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- प्रत्यक्षवाद वह दृष्टिकोण है जिसमें समाज का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों, अवलोकन और अनुभवजन्य तथ्यों के आधार पर किया जाता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.प्रेत से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:-प्रेत एक संस्कृतिक त्रैविक तत्व है जो पूर्वजों की आत्मा का प्रतीक होता है और पारंपरिक समाजों में इसका सामाजिक महत्व होता है।
प्रश्न-3.विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- विश्वसनीयता का अर्थ है किसी अनुसंधान या परीक्षण के परिणामों की स्थिरता और पुनरावृत्ति की क्षमता।
प्रश्न-4. सामाजिक तथ्य को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- सामाजिक तथ्य वे बाह्य और बाध्यकारी तत्व हैं जो व्यक्ति पर समाज द्वारा थोपे जाते हैं।
प्रश्न-5. ‘आदर्श प्रारूप’ अवधारणा किसके द्वारा दी गई?
उत्तर:- मैक्स वेबर द्वारा दी गई थी, जो समाज के विश्लेषण हेतु एक सैद्धांतिक उपकरण है।
प्रश्न-6. आदर्श प्रारूप से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- आदर्श प्रारूप वे सैद्धांतिक ढाँचे हैं जो किसी सामाजिक परिघटना को विश्लेषण हेतु आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं।
प्रश्न-7.दास कैपिटल’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- कार्ल मार्क्स
प्रश्न-8. ‘मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- लुईस ए. कोज़र (Lewis A. Coser)
प्रश्न-9. ‘द पॉजिटिव फिलॉसफी’ के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- ऑगस्त कॉम्टे (Auguste Comte)
प्रश्न-10. ‘माइंड एण्ड सोसाइटी’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- विलफ्रेडो पेरेटो
प्रश्न-11. ‘द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म’ के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- मैक्स वेबर (Max Weber)
प्रश्न-12. ‘द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन’ के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- टैल्कॉट पारसन्स (Talcott Parsons)
प्रश्न-13. द सर्कुलेशन ऑफ इलीट” के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- विलफ्रेडो पेरेटो
प्रश्न-13.a सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- रॉबर्ट के. मर्टन
प्रश्न-14. सामाजिक तथ्यों के प्रकारों के नाम लिखिए।
उत्तर:- भौतिक, अमूर्त, नैतिक और सामूहिक अभ्यस्त क्रियाएँ
प्रश्न-15. अनुसंधान में सांख्यिकी की आवश्यकता की कारण स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- सांख्यिकी अनुसंधान में डाटा के संग्रह, विश्लेषण, निष्कर्ष तथा वैधता प्रदान करने हेतु आवश्यक होती है, जिससे निष्पक्ष और सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं।
प्रश्न-16. शक्तिहीनता से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:- शक्तिहीनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति निर्णय लेने या प्रभाव डालने में स्वयं को असमर्थ पाता है।
प्रश्न-17. सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के कोई दो नियम लिखिए
उत्तर:- सामाजिक तथ्यों का वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन होना चाहिए।
समाजशास्त्री को अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना चाहिए।
प्रश्न-18. वस्तैहन की स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- वस्तैहन एक विधि है जिसमें समाजशास्त्री दूसरों की क्रियाओं को उनके दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है।
प्रश्न-19. सामाजिक क्रिया को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:-सामाजिक क्रिया वह मानव व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होता है और जिसका उद्देश्य सामाजिक संदर्भ में अर्थपूर्ण होता है।
प्रश्न-20. पॉटलेच से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:-पॉटलेच एक प्रकार का आदिवासी समारोह होता है जिसमें संपत्ति का दान करके सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त की जाती है।
प्रश्न-21. प्रतिशोधात्मक कानून को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:-प्रतिशोधात्मक कानून वे नियम हैं जो अपराध के लिए कठोर दंड देकर सामाजिक एकता की रक्षा करते हैं।
प्रश्न-22 चर के प्रकारों के नाम लिखिए।
उत्तर:- चर के प्रमुख प्रकार हैं—स्वतंत्र चर, निर्भर चर, नियंत्रित चर और अव्यक्त चर।
प्रश्न-23. इन्द्वात्मकता को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- इन्द्वात्मकता वह प्रक्रिया है, जिसमें विरोधी विचारों के संघर्ष से नया सत्य उत्पन्न होता है, यह विचार हीगेल और मार्क्स द्वारा प्रमुखता से दिया गया।
प्रश्न-24. ‘निगमन’ को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- निगमन वह तार्किक प्रक्रिया है, जिसमें सामान्य सिद्धांतों से विशेष निष्कर्ष निकाले जाते हैं; यह वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रमुख विधि मानी जाती है।
प्रश्न-25. नौकरशाही की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- (1) स्पष्ट नियम व अनुशासन (2) पदानुक्रमात्मक संरचना तथा कार्यों का विभाजन।
प्रश्न-26. भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:-भौतिकवाद वह विचारधारा है जो मानती है कि केवल भौतिक वस्तुएँ ही वास्तविक हैं और चेतना, विचार आदि भौतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं।
प्रश्न-27. ‘त्रिक (Triad) ‘ से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:- तीन व्यक्तियों का समूह, जिसमें पारस्परिक संबंध अधिक जटिल होते हैं, उसे त्रिक (Triad) कहा जाता है।
प्रश्न-28. तार्किक क्रिया को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- तार्किक क्रिया वह होती है जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक और तर्क के आधार पर की जाती है।
प्रश्न-29. तार्किकीकरण से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- तार्किकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें परंपरागत और भावनात्मक सोच की जगह तर्क, योजना और दक्षता को प्रमुखता दी जाती है।
प्रश्न-30. उदविकास से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- उदविकास वह प्रक्रिया है, जिसमें जीव-जंतु या सामाजिक संरचनाएँ समय के साथ क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक जटिल और अनुकूल रूप में विकसित होती हैं।
प्रश्न-31. सामूहिक चेतना को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- सामूहिक चेतना समूह के सदस्यों में साझा विश्वासों, मूल्यों और सोच की भावना को दर्शाती है।
प्रश्न-32.परम्परा को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- परम्परा उन मान्यताओं, रीति-रिवाजों और व्यवहारों का संचय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं।
प्रश्न-33. सामाजिक तथ्यर्थी के प्रकार बतइए
उत्तर:- सामाजिक तथ्य दो प्रकार के होते हैं: भौतिक (Material) और अमूर्त (Non-material) सामाजिक तथ्य
प्रश्न-34. टोटम से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- टोटम किसी जाति या समूह द्वारा पूजित प्रतीकात्मक पशु, पौधा या वस्तु होता है जो उनके सामाजिक एकता का प्रतीक होता है।
प्रश्न-35. प्रकार्य को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- प्रकार्य समाज के किसी अंग द्वारा समाज में योगदान देने की प्रक्रिया है जिससे व्यवस्था बनी रहती है।
प्रश्न-35. प्रकट प्रकार्य एवं प्रच्छन्न प्रकार्य के मध्य कोई दो अंतर लिखिए।
उत्तर:- प्रकट प्रकार्य स्पष्ट और जानबूझकर होते हैं, जबकि प्रच्छन्न प्रकार्य अप्रत्यक्ष और अनजाने होते हैं।
प्रकट प्रकार्य का उद्देश्य ज्ञात होता है, जबकि प्रच्छन्न प्रकार्य अनपेक्षित होते हैं।
प्रश्न-36. अलगाववाद की परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- अलगाववाद वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने श्रम, उत्पाद, समाज और स्वयं से भावनात्मक व सामाजिक दूरी अनुभव करता है।
प्रश्न-37. विज्ञान की काई दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है।
यह परीक्षण योग्य तथ्यों पर आधारित होता है।
प्रश्न-38. ‘प्रकार्य’ की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- प्रकार्य से तात्पर्य समाज की संरचना में किसी तत्व या प्रक्रिया द्वारा निभाई गई भूमिका से है।
प्रश्न-39. वेबर के पद्धतिशास्त्र की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- वेबर ने समझात्मक दृष्टिकोण (Verstehen) पर बल दिया।
उन्होंने आदर्श प्रकारों (Ideal Types) का प्रयोग किया।
प्रश्न-40. सामूहिक चेतना से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- सामूहिक चेतना समाज के सदस्यों के साझा विश्वासों, मूल्यों और दृष्टिकोणों का बोध है।
Section-B
प्रश्न-1.एक आनुभविक समाजशास्त्री के रूप में दुर्खीम के विचारों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- दुर्खीम को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक और अनुभवजन्य अनुशासन के रूप में स्थापित किया। एक आनुभविक समाजशास्त्री के रूप में उन्होंने तर्क, अवलोकन और तुलनात्मक पद्धति पर बल दिया। उनका मानना था कि समाज को अध्ययन की वस्तु (object of study) की तरह देखा जाना चाहिए, जैसे भौतिक विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है।
दुर्खीम ने “सामाजिक तथ्य” की अवधारणा प्रस्तुत की, जिन्हें उन्होंने बाह्य, बाध्यकारी और वस्तुगत बताया। उन्होंने आत्महत्या पर अपने अध्ययन में सांख्यिकीय पद्धति और तुलनात्मक विश्लेषण का उपयोग करते हुए यह दिखाया कि आत्महत्या जैसे व्यक्तिगत कार्य भी सामाजिक कारणों से प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने धर्म, शिक्षा और कानून जैसे सामाजिक संस्थानों का अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से किया।
इस प्रकार, दुर्खीम का समाजशास्त्र अनुभववाद और वैज्ञानिक विधियों पर आधारित था, जो सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठ व्याख्या करता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.एक प्रत्यक्षवादी समाजविज्ञानी के रूप में कॉम्टे के विचारों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- ऑगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रत्यक्षवाद (Positivism) की स्थापना की, जिसका अर्थ है कि समाज का अध्ययन उसी वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए जिससे प्रकृति का अध्ययन होता है। उनके अनुसार, समाजशास्त्रीय ज्ञान अनुभव, परीक्षण और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए, न कि धार्मिक या दार्शनिक अनुमान पर। उन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक घटनाओं की तरह निश्चित नियमों के अधीन होती हैं। इस विचार ने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉम्टे का मानना था कि ज्ञान तीन अवस्थाओं से गुजरता है — धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक, और समाज अब वैज्ञानिक चरण में प्रवेश कर चुका है जहाँ वास्तविकता को केवल प्रत्यक्ष अनुभवों और निरीक्षण से समझा जा सकता है।
प्रश्न-3.सामाजिक अनुसंधान को तर्कसंगत रूप से प्रायोजित करने के चरणों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- सामाजिक अनुसंधान को तर्कसंगत और वैज्ञानिक बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है:
समस्या का चयन: अनुसंधान की प्रक्रिया की शुरुआत किसी सामाजिक समस्या की पहचान से होती है जिसे अध्ययन करना है।
समीक्षा और साहित्य सर्वेक्षण: पूर्ववर्ती अनुसंधानों और सिद्धांतों की समीक्षा की जाती है जिससे विषय की गहराई को समझा जा सके।
उद्देश्य और परिकल्पना निर्माण: अनुसंधान के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और संबंधित परिकल्पना का निर्माण किया जाता है।
अनुसंधान डिज़ाइन: अध्ययन के तरीके जैसे सर्वेक्षण, साक्षात्कार, केस स्टडी आदि का निर्धारण किया जाता है।
डेटा संग्रह: प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों से आंकड़ों का संग्रह किया जाता है।
डेटा विश्लेषण: संकलित आंकड़ों को सांख्यिकीय या गुणात्मक विधियों से विश्लेषित किया जाता है।
निष्कर्ष और प्रतिवेदन: परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और रिपोर्ट तैयार की जाती है।
प्रश्न-4. अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- अनुसंधान प्रक्रिया एक क्रमबद्ध पद्धति है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक तथ्यों की खोज की जाती है। इसके मुख्य चरण निम्नलिखित हैं:
- समस्या की पहचान – शोध प्रक्रिया की शुरुआत एक स्पष्ट और यथार्थ शोध समस्या की पहचान से होती है।
- साहित्य समीक्षा – पूर्व में हुए संबंधित अनुसंधानों का अध्ययन किया जाता है।
- उद्देश्य निर्धारण – शोध के प्रमुख उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं को स्पष्ट किया जाता है।
- शोध विधि का चयन – उपयुक्त अनुसंधान डिज़ाइन (सर्वेक्षण, केस स्टडी, प्रयोग आदि) का चुनाव किया जाता है।
- डेटा संग्रहण – प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों से सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं।
- डेटा विश्लेषण – एकत्रित आँकड़ों का सांख्यिकीय अथवा गुणात्मक तरीके से विश्लेषण किया जाता है।
- निष्कर्ष और प्रतिवेदन – शोध निष्कर्षों को व्याख्यायित कर रिपोर्ट या शोध प्रबंध तैयार किया जाता है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य वैज्ञानिक ढंग से सामाजिक तथ्यों को समझना होता है।
प्रश्न-5.नौकरशाही की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- मैक्स वेबर ने नौकरशाही (Bureaucracy) को एक आदर्श संगठनात्मक संरचना के रूप में प्रस्तुत किया। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- विभाजन और विशिष्टता – कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है और हर व्यक्ति का एक निश्चित कार्यक्षेत्र होता है।
- नियमों का पालन – संगठन नियमों और प्रक्रियाओं से संचालित होता है।
- अधिकार का पदानुक्रम – संगठन में एक स्पष्ट पदानुक्रम होता है जहाँ ऊपर से नीचे तक आदेशों का पालन होता है।
- तकनीकी योग्यता – पदों पर नियुक्ति योग्यता और परीक्षा के आधार पर होती है।
- निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता – निजी भावनाओं की बजाय नियम और नीति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
- दस्तावेजीकरण – सभी कार्यों को लिखित रूप में दर्ज किया जाता है।
वेबर ने नौकरशाही को आधुनिक समाज में प्रभावशाली प्रशासनिक प्रणाली माना, पर साथ ही इसे “लोहे का पिंजरा” भी कहा क्योंकि यह मानव स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है।
प्रश्न-6.विज्ञानों के संस्तरण पर कॉम्टे के विचार प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर:- कॉम्टे ने ज्ञान के विकास को एक श्रेणीबद्ध रूप में देखा जिसे उन्होंने “विज्ञानों का संस्तरण” कहा। उन्होंने विज्ञानों को उनकी सैद्धांतिक जटिलता और निर्भरता के अनुसार एक क्रम में रखा। इस श्रेणी में सबसे सरल और सामान्य विज्ञान गणित है, इसके बाद खगोलशास्त्र, भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान और अंत में समाजशास्त्र आता है। उनका तर्क था कि समाजशास्त्र सबसे जटिल विज्ञान है क्योंकि इसमें सबसे अधिक परिवर्तनीयताएं होती हैं। प्रत्येक विज्ञान अगले विज्ञान की नींव तैयार करता है। उदाहरण के लिए, भौतिकी गणित पर निर्भर करती है, रसायनशास्त्र भौतिकी पर, और इसी प्रकार समाजशास्त्र जीवविज्ञान पर। इस संस्तरण का उद्देश्य समाजशास्त्र को वैज्ञानिकता प्रदान करना और अन्य विज्ञानों के समान गंभीरता से ग्रहण करना था।
प्रश्न-7.सामाजिक विज्ञानों के पद्धतिशास्त्र की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- सामाजिक विज्ञानों का पद्धतिशास्त्र (Methodology) उन तरीकों और तकनीकों का अध्ययन है जिनके द्वारा सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक यथार्थ को समझने और व्याख्या करने के लिए उपयुक्त विधियाँ विकसित करना है।
सामाजिक विज्ञानों में दो प्रमुख पद्धतियाँ हैं—प्रत्यक्षवादी (Positivist) और व्याख्यात्मक (Interpretative)। प्रत्यक्षवादी पद्धति में वैज्ञानिक तरीके, आंकड़ों का विश्लेषण और वस्तुनिष्ठ अवलोकन का प्रयोग होता है। दुर्खीम और कॉम्टे इस दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवर्तक थे। इसके विपरीत, व्याख्यात्मक पद्धति में व्यक्ति की मानसिकता, उद्देश्य और अर्थ की समझ को महत्व दिया जाता है, जैसा कि वेबर ने ‘Verstehen’ में प्रतिपादित किया।
इसके अतिरिक्त केस स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन, सर्वेक्षण, साक्षात्कार और ऐतिहासिक विश्लेषण जैसी पद्धतियाँ भी उपयोग की जाती हैं। इन विधियों से समाज के जटिल पहलुओं को गहराई से समझा जा सकता है।
इस प्रकार, सामाजिक विज्ञानों की पद्धति बहुआयामी है, जो वस्तुनिष्ठता और व्याख्या दोनों को संतुलित करने का प्रयास करती है।
प्रश्न-8.डी.पी. मुकर्जी की परम्पराओं के द्वंद्वात्मक उपागम पर एक लघु टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- डी.पी. मुकर्जी भारतीय समाज के अध्ययन में परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्वात्मक (Dialectical) संबंध को महत्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार परंपरा कोई स्थिर या जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि वह निरंतर परिवर्तनशील होती है जो सामाजिक चेतना और क्रियाओं के माध्यम से विकसित होती है।
उन्होंने परंपरा को ‘सृजनात्मक परंपरा’ कहा जिसमें न केवल भूतकाल की निरंतरता है बल्कि उसमें आधुनिकता के साथ संवाद और टकराव की क्षमता भी है। मुकर्जी मानते थे कि भारतीय समाज को समझने के लिए केवल पाश्चात्य प्रतिमानों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। भारतीय परंपरा में ‘धर्म’, ‘कर्म’, और ‘समाज’ की अवधारणाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं जो आधुनिक प्रक्रियाओं से टकराती हैं और नई सामाजिक संरचनाओं को जन्म देती हैं।
उनका दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि परंपरा और आधुनिकता के बीच द्वंद्व ही समाज की गतिशीलता का आधार है। इस द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायता मिलती है।
प्रश्न-9. वेबर के पद्धतिशास्त्र की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए विशिष्ट पद्धति का विकास किया जिसे “व्याख्यात्मक समाजशास्त्र” कहा गया। वे वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता को स्वीकार करते थे लेकिन मानते थे कि सामाजिक क्रिया की समझ के लिए “अर्थ” (meaning) की व्याख्या आवश्यक है।
उनकी प्रमुख पद्धतियाँ थीं:
वरष्टेहन (Verstehen): यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है ‘समझना’। इसके द्वारा वेबर यह कहते हैं कि समाजशास्त्री को क्रियाओं के पीछे के उद्देश्य और भावना को समझना चाहिए।
आदर्श प्रकार (Ideal Type): यह विश्लेषण का एक उपकरण है जो वास्तविकता के विभिन्न रूपों को सरल और आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है ताकि तुलना की जा सके।
वेबर ने यह भी कहा कि मूल्य-मुक्त अध्ययन जरूरी है ताकि पूर्वग्रहों से बचा जा सके।
प्रश्न-10. विलासी वर्ग के सिद्धान्त पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- विलासी वर्ग का सिद्धांत अमेरिकी समाजशास्त्री थॉर्स्टीन वेब्लेन द्वारा The Theory of the Leisure Class (1899) में प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने इस वर्ग को एक ऐसा वर्ग बताया जो श्रम नहीं करता, बल्कि विलासिता और दिखावे के जीवन को प्राथमिकता देता है।
वेब्लेन ने ‘दिखावटी उपभोग’ (Conspicuous Consumption) की अवधारणा दी, जिसके अनुसार यह वर्ग वस्तुओं का उपभोग केवल अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करता है, न कि उनकी उपयोगिता के लिए। उदाहरण के लिए, महंगे कपड़े पहनना, समय और संसाधनों की बर्बादी करना, सेवकों का रखाव आदि।
यह वर्ग श्रम को हेय दृष्टि से देखता है और अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरों से अलग व्यवहार करता है। वेब्लेन ने इस प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए कहा कि यह सामाजिक असमानता और आर्थिक गैर-बराबरी को बढ़ावा देती है।
विलासी वर्ग का यह सिद्धांत आधुनिक उपभोक्तावादी समाज की आलोचना में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रश्न-11. विज्ञानों के संस्तरण में कॉम्टे के योगदान को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों के क्रमिक विकास और उनकी जटिलता के आधार पर ‘विज्ञानों का संस्तरण’ (Hierarchy of Sciences) सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने ज्ञान की श्रेणीबद्ध संरचना को तीन अवस्थाओं – धार्मिक, दार्शनिक, और वैज्ञानिक – के माध्यम से समझाया।
कॉम्टे ने विज्ञानों को सबसे सरल से सबसे जटिल की ओर व्यवस्थित किया। उनका अनुक्रम इस प्रकार था:
- गणित
- खगोल विज्ञान
- भौतिकी
- रसायन
- जीवविज्ञान
- समाजशास्त्र (Social Physics)
उनके अनुसार समाजशास्त्र सबसे जटिल विज्ञान है क्योंकि इसमें सभी अन्य विज्ञानों की विशेषताओं का समावेश होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए अन्य विज्ञानों की समझ आवश्यक है।
कॉम्टे का यह सिद्धांत समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने का प्रयास था, जिससे यह सिद्ध हो सके कि सामाजिक घटनाओं को भी वैज्ञानिक विधि से समझा जा सकता है।
प्रश्न-12. व्यवस्था की पूर्व आवश्यकता के पक्षों को समझाइए।
उत्तर:- टाल्कट पार्सन्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था (Social System) की अवधारणा के अनुसार किसी भी व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएँ होती हैं, जिन्हें AGIL स्कीमा में वर्गीकृत किया गया है:
- A – अनुकूलन (Adaptation): व्यवस्था को अपने पर्यावरण के अनुरूप ढलना चाहिए और संसाधनों को जुटाना चाहिए।
- G – लक्ष्य प्राप्ति (Goal Attainment): समाज को अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
- I – एकीकरण (Integration): समाज के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य और सहयोग होना चाहिए।
- L – प्रतिरक्षा (Latency): सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक प्रेरणाओं को बनाए रखने के लिए समाज को मानदंडों का पालन करना चाहिए।
इन पूर्व आवश्यकताओं के बिना कोई भी सामाजिक व्यवस्था दीर्घकालिक रूप से स्थिर नहीं रह सकती। पार्सन्स के अनुसार यह मॉडल समाज के संतुलन और स्थायित्व को बनाए रखने में सहायक होता है।
प्रश्न-13. सामाजिक तथ्य के लक्षण स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- दुर्खीम ने ‘सामाजिक तथ्य’ (Social Fact) की अवधारणा को समाजशास्त्रीय अध्ययन की मूल इकाई माना। सामाजिक तथ्य वे तरीके, नियम, मूल्य और विश्वास हैं जो समाज में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखते हैं और व्यक्तियों पर प्रभाव डालते हैं।
सामाजिक तथ्य के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं:
- बाह्यता (Externality): सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं। ये व्यक्ति के जन्म से पहले से मौजूद होते हैं और समाज द्वारा निर्मित होते हैं।
- बाध्यता (Constraint): ये व्यक्ति पर एक प्रकार का सामाजिक दबाव डालते हैं, जिससे व्यक्ति को इनका पालन करना पड़ता है। उदाहरण: भाषा, नैतिक मूल्य आदि।
- सामूहिक चेतना (Collectivity): सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होते हैं। ये समाज के बहुसंख्यक लोगों द्वारा साझा किए जाते हैं।
- वस्तुगतता (Objectivity): इनका अध्ययन एक वस्तु की तरह किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर।
इस प्रकार, सामाजिक तथ्य समाज के नियम और ढांचे को बनाते हैं, और समाजशास्त्रियों के लिए विश्लेषण की मुख्य इकाई होते हैं।
प्रश्न-14. यांत्रिकी एवं सावयवी एकता में अंतर कीजिए।
उत्तर:- एमिल दुर्खीम ने समाजों की एकता को दो प्रकारों में बाँटा — यांत्रिकी (Mechanical) और सावयवी (Organic) एकता।
यांत्रिकी एकता पारंपरिक समाजों में पाई जाती है जहाँ लोगों का जीवन समान होता है, उनके मूल्य और विश्वास एक जैसे होते हैं। कार्य विभाजन बहुत कम होता है और सामाजिक नियंत्रण अधिक होता है।
सावयवी एकता आधुनिक समाजों में देखी जाती है जहाँ लोगों में विविधता होती है, कार्यों का विशेषीकरण होता है, और पारस्परिक निर्भरता अधिक होती है।
इस प्रकार, यांत्रिकी एकता समानता पर आधारित होती है जबकि सावयवी एकता विभाजन और पारस्परिक निर्भरता पर।
प्रश्न-15. सामाजिक क्रिया की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- सामाजिक क्रिया (Social Action) का सिद्धांत मैक्स वेबर ने प्रतिपादित किया। वेबर के अनुसार, सामाजिक क्रिया वह मानवीय क्रिया है जिसका अर्थ दूसरों के व्यवहार से संबंधित होता है और जिसे व्यक्ति उद्देश्यपूर्वक करता है।
सामाजिक क्रिया की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- अर्थपूर्ण (Meaningful): प्रत्येक सामाजिक क्रिया के पीछे कोई न कोई अर्थ या उद्देश्य होता है।
- उद्देश्यपूर्ण (Goal-Oriented): व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक क्रिया करता है।
- संबंधात्मक (Relational): सामाजिक क्रिया का संबंध अन्य व्यक्तियों की अपेक्षित प्रतिक्रियाओं से होता है।
- स्वैच्छिक (Voluntary): यह क्रिया व्यक्ति की इच्छा और समझ पर आधारित होती है।
- प्रकारभेद (Types): वेबर ने चार प्रकार की सामाजिक क्रियाएँ बताई—परंपरागत, स्नेहात्मक, मूल्य-तर्कसंगत और साध्य-तर्कसंगत।
इस प्रकार, सामाजिक क्रिया सामाजिक जीवन की आधारशिला है और इसका विश्लेषण समाजशास्त्र का मूल कार्य है।
प्रश्न-16. सामाजिक क्रिया के आवश्यक तत्वों की स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया (Social Action) का अर्थ है वह क्रिया जो किसी व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति अर्थपूर्ण तरीके से की जाती है। इसके आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं:
- कर्म करनेवाला व्यक्ति (Actor): क्रिया को करने वाला व्यक्ति आवश्यक होता है जो सोच-समझकर क्रिया करता है।
- अर्थपूर्ण उद्देश्य: सामाजिक क्रिया हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है, उसमें व्यक्ति किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है।
- दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति: सामाजिक क्रिया तब होती है जब वह दूसरों की उपस्थिति या उनके व्यवहार को ध्यान में रखकर की जाए।
- प्रभाव डालने की मंशा: व्यक्ति अपनी क्रिया के माध्यम से दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास करता है।
इन तत्वों के माध्यम से सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक केंद्रीय विषय बनाया गया है।
प्रश्न-17. दमनकारी कानून पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:-दमनकारी कानून (Repressive Law) की संकल्पना एमिल दुर्खीम द्वारा दी गई थी। यह ऐसे सामाजिक ढांचे में पाया जाता है जहाँ समाज यांत्रिक एकता (Mechanical Solidarity) पर आधारित होता है। ऐसे समाजों में सभी लोग एक जैसे होते हैं और व्यक्तिगत भिन्नता कम होती है।
दमनकारी कानून का उद्देश्य सामाजिक नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड देना होता है, जिससे समाज की सामूहिक चेतना की रक्षा की जा सके। यह कानून अपराधी को दंडित कर समाज में डर और अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है।
उदाहरण स्वरूप, पारंपरिक समाजों में चोरी, हत्या या धर्म-भंग जैसे अपराधों पर मृत्युदंड या शारीरिक दंड दिया जाता था। यह दमनकारी कानून का प्रतीक है।
दुर्खीम का मानना था कि जैसे-जैसे समाज आधुनिक होता है, दमनकारी कानून की जगह सुधारात्मक कानून (Restitutive Law) ले लेता है।
प्रश्न-18. वेबलेन के आर्थिक प्रतिस्पर्धा के नियमों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- थॉरस्टीन वेबलेन ने पारंपरिक आर्थिक विचारों की आलोचना करते हुए “प्रतिस्पर्धात्मक उपभोग” (Conspicuous Consumption) की धारणा दी। वेबलेन के अनुसार आर्थिक प्रतिस्पर्धा केवल उत्पादन या लाभ कमाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करने का भी माध्यम बन जाती है।
मुख्य नियम:
- प्रतिष्ठा की चाह – व्यक्ति महंगे वस्त्र, घर या सेवाएँ खरीदते हैं ताकि अपनी सामाजिक स्थिति प्रदर्शित कर सकें।
- अर्थव्यवस्था का सामाजिक पक्ष – आर्थिक व्यवहार केवल लाभ-हानि तक सीमित नहीं होता, वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए।
- आडंबरपूर्ण उपभोग – प्रतिस्पर्धा में लोग आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं ताकि वे समाज में उच्च दिख सकें।
- श्रम-विरोधी वर्ग – उच्च वर्ग मेहनत से बचता है और वैभवपूर्ण जीवन शैली अपनाता है, जिससे सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है।
वेबलेन की यह दृष्टि आधुनिक पूंजीवादी समाज की वास्तविकताओं को उजागर करती है जहाँ आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक पहचान से जुड़ जाती है।
प्रश्न-19. दुर्खीम द्वारा दिए गए श्रम विभाजन के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- दुर्खीम ने अपने ग्रंथ “The Division of Labour in Society” में श्रम विभाजन को सामाजिक एकता और एकजुटता के आधार के रूप में देखा। उन्होंने दो प्रकार की एकता की बात की — यांत्रिक एकता (Mechanical Solidarity) और कार्बनिक एकता (Organic Solidarity)।
यांत्रिक एकता पारंपरिक समाजों में पाई जाती है जहाँ सभी लोग एक जैसे कार्य करते हैं और सामूहिक चेतना मजबूत होती है। इसमें व्यक्तित्व का विकास कम होता है। इसके विपरीत, आधुनिक समाजों में कार्बनिक एकता पाई जाती है, जहाँ श्रम विभाजित होता है और प्रत्येक व्यक्ति विशेष कार्य करता है। इससे व्यक्तित्व का विकास होता है और समाज में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है।
दुर्खीम के अनुसार, श्रम विभाजन केवल आर्थिक दक्षता नहीं बढ़ाता बल्कि यह सामाजिक एकता का भी आधार बनता है। जब श्रम का विभाजन नैतिक भावना से संचालित हो, तो यह समाज को स्थिर करता है। लेकिन यदि यह अराजकता (anomie) की ओर ले जाए, तो सामाजिक बिखराव हो सकता है।
प्रश्न-20. दुर्खीम के आत्महत्या के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखा और उसके चार प्रकार बताए:
- एनोमिक आत्महत्या – यह तब होती है जब सामाजिक नियमों का अभाव होता है, जैसे आर्थिक संकट या सामाजिक अस्थिरता।
- अल्ट्रूिस्टिक आत्महत्या – यह तब होती है जब व्यक्ति समाज के प्रति अत्यधिक समर्पित होता है, जैसे सैनिकों की आत्मबलिदान की भावना।
- इगोइस्टिक आत्महत्या – यह तब होती है जब व्यक्ति समाज से कट जाता है और सामाजिक एकता कमजोर होती है।
- फेटलिस्टिक आत्महत्या – यह अत्यधिक नियंत्रण और दमन के कारण होती है, जैसे जेल में बंद कैदी।
दुर्खीम का मानना था कि आत्महत्या केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक कारणों से भी होती है।
प्रश्न-21. दुर्खीम के अनुसार धर्म की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- एमिल दुर्खीम ने धर्म को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा और अपने ग्रंथ The Elementary Forms of Religious Life में इसकी व्याख्या की। उनके अनुसार धर्म का मूल उद्देश्य सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना को सुदृढ़ करना है।
दुर्खीम के अनुसार, धर्म पवित्र (Sacred) और अपवित्र (Profane) के बीच विभाजन करता है। पवित्र चीजों से जुड़े अनुष्ठान, विश्वास और प्रतीक धर्म का निर्माण करते हैं। उनका मानना था कि देवता, दरअसल समाज का ही प्रतीक होते हैं।
धर्म, व्यक्ति को उसके सामाजिक समूह से जोड़ता है और सामूहिकता की भावना को उत्पन्न करता है। यह नैतिकता और अनुशासन को बनाए रखने में सहायक होता है।
दुर्खीम ने यह भी कहा कि धार्मिक व्यवहार, अंततः सामाजिक व्यवहार होता है। इसलिए धर्म की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आवश्यक है।
प्रश्न-22. पवित्र तथा साधारण वस्तुओं के लक्षण बताइए।
उत्तर:- एमिल दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में ‘पवित्र’ (Sacred) और ‘साधारण’ (Profane) वस्तुओं में भेद किया। इसके अनुसार:
पवित्र वस्तुएँ:
- समाज द्वारा विशेष आदर और श्रद्धा के साथ देखी जाती हैं।
- ये वस्तुएँ धार्मिक अनुष्ठानों, परंपराओं और विश्वासों से जुड़ी होती हैं।
- इनके प्रति अनुशासन, नियम और निषेध होते हैं (जैसे – मंदिर, मूर्ति, ग्रंथ)।
- पवित्र वस्तुएँ साधारण जीवन से ऊपर मानी जाती हैं।
साधारण वस्तुएँ:
- ये दैनिक जीवन की सामान्य वस्तुएँ होती हैं।
- इनसे कोई विशेष धार्मिक भावना नहीं जुड़ी होती।
- इनका प्रयोग सामान्य भौतिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- ये वस्तुएँ समाज द्वारा विशेष संरक्षण या आदर की पात्र नहीं होतीं।
दुर्खीम के अनुसार, धर्म का आधार वस्तुओं का यह पवित्र और साधारण के रूप में विभाजन ही होता है।
प्रश्न-23. आदर्श प्रारूप क्या नहीं है? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- आदर्श प्रारूप (Ideal Type) की संकल्पना मैक्स वेबर द्वारा दी गई थी। यह किसी सामाजिक घटना की विशुद्ध (pure) और विश्लेषणात्मक अवधारणा होती है। यह वास्तविकता का सटीक प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि विश्लेषण के लिए एक मानक रूप (model) प्रदान करता है।
आदर्श प्रारूप क्या नहीं है:
- यह वास्तविकता नहीं है: यह किसी सामाजिक तथ्य या व्यवहार की सटीक प्रतिकृति नहीं होता। वास्तविक दुनिया में आदर्श प्रारूप जैसा कोई तत्व शुद्ध रूप में मौजूद नहीं होता।
- यह नैतिक आदर्श नहीं है: इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता। यह अच्छा या बुरा नहीं बताता।
- यह तथ्य नहीं बल्कि उपकरण है: यह विश्लेषण के लिए एक बौद्धिक उपकरण (Analytical Tool) है, जिससे वास्तविकता को बेहतर समझा जा सके।
उदाहरण के लिए, “नौकरशाही का आदर्श प्रकार” एक ऐसा मॉडल है जिसमें सभी नियमों और ढांचों को पूर्ण रूप से लागू किया गया हो, लेकिन असल जीवन में ऐसा नहीं होता।
इस प्रकार, आदर्श प्रारूप वस्तुनिष्ठता के लिए बनाया गया कल्पनात्मक ढांचा है, न कि वास्तविक या आदर्श समाज।
प्रश्न-24. कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्रीय योगदान पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:-कार्ल मार्क्स आधुनिक समाजशास्त्र के महान विचारकों में से एक थे। उन्होंने समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा दी। उनका मानना था कि समाज की बुनियादी संरचना उसकी आर्थिक प्रणाली होती है। उत्पादन के साधनों के स्वामित्व पर आधारित वर्ग संघर्ष, समाज परिवर्तन का मुख्य कारण है।
मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में दो वर्गों की पहचान की: पूंजीपति (Bourgeoisie) और श्रमिक (Proletariat)। उनके अनुसार पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है और यह संघर्ष अंततः समाजवादी क्रांति की ओर ले जाएगा।
उन्होंने 疏外 (Alienation) का सिद्धांत भी दिया, जिसमें श्रमिक अपनी मेहनत से ही कट जाता है। उनके विचारों ने समाजशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र को गहराई से प्रभावित किया। मार्क्स के समाजशास्त्रीय विश्लेषण ने सामाजिक अन्याय, असमानता और वर्ग संरचना की समझ को नई दिशा दी।
प्रश्न-25. परेटो के “अभिजन के सक्रिय सिद्धांत” की समीक्षा कीजिए।
उत्तर:- विलफ्रेडो परेटो ने ‘अभिजन का सक्रिय सिद्धांत’ (Circulation of Elites) प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार समाज में हमेशा दो प्रकार के अभिजन (Elites) होते हैं—शेर जैसे अभिजन (conservative and forceful) और लोमड़ी जैसे अभिजन (चतुर और कूटनीतिज्ञ)। यह सिद्धांत बताता है कि समय के साथ पुराने अभिजन समाप्त हो जाते हैं और नए अभिजन उनका स्थान ले लेते हैं।
मुख्य बिंदु:
- अभिजन चक्र: समाज में अभिजनों का लगातार परिवर्तन होता है। यह चक्र समाज की स्थिरता बनाए रखता है।
- राजनीतिक अस्थिरता: जब पुरानी अभिजनों की शक्ति समाप्त होती है और वे परिवर्तन को रोकते हैं, तो क्रांति की संभावना बढ़ जाती है।
- अवकाश और उद्भव: निम्न वर्ग से भी अभिजन उत्पन्न हो सकते हैं, जो उच्च वर्ग में प्रवेश करते हैं।
समीक्षा:
यह सिद्धांत शक्ति और नेतृत्व के परिवर्तन को समझाने में सहायक है। परंतु यह आर्थिक कारकों, सामाजिक न्याय और वर्ग-संघर्ष की अनदेखी करता है। यह संरचनात्मक कारकों को कम महत्व देता है।
इस प्रकार, परेटो का सिद्धांत समाज में शक्ति के परिवर्तन की एक यथार्थवादी लेकिन आंशिक व्याख्या प्रस्तुत करता है।
प्रश्न-26. पूँजीवाद के नैतिकतावादी पक्षों की स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- पूंजीवाद के नैतिक पक्षों को समझने में मैक्स वेबर का योगदान विशेष है। उन्होंने अपने ग्रंथ The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism में यह तर्क दिया कि पूंजीवाद की जड़ें प्रोटेस्टैंट ईसाई धर्म, विशेषकर कैल्विनिज़्म की नैतिकता में हैं।
वेबर के अनुसार पूंजीवाद केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक नैतिक दृष्टिकोण भी है जो कठोर परिश्रम, अनुशासन, समय का प्रबंधन और मितव्ययिता को बढ़ावा देता है। पूंजीवादी नैतिकता में ‘धन अर्जन’ को ईश्वर की कृपा का चिन्ह माना गया, जिससे लोगों में पूंजी संचय की प्रवृत्ति बढ़ी।
इस प्रकार, पूंजीवाद केवल भौतिक लालच पर आधारित नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रेरणा भी थी, जिसने इसे पश्चिमी समाज में उन्नत किया।
प्रश्न-27. अनुसन्धान में विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता क्यों आवश्यक है?
उत्तर:- विश्वसनीयता से परिणाम दोहराए जा सकते हैं और प्रामाणिकता से परिणाम सटीक होते हैं, जिससे अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।
प्रश्न-28. वेब्लन का आर्थिक प्रतिस्पर्धा का नियम स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- थॉर्नस्टीन वेब्लन ने “आर्थिक प्रतिस्पर्धा” के सिद्धांत को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने ‘प्रदर्शनीय उपभोग’ (Conspicuous Consumption) का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें उच्च वर्ग अपने सामाजिक दर्जे को प्रदर्शित करने के लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदता है।
वेब्लन का मानना था कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा केवल लाभ प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रतिष्ठा, सम्मान और सामाजिक स्थिति पाने की प्रतिस्पर्धा भी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रतिस्पर्धा असमानता को बढ़ावा देती है क्योंकि उच्च वर्ग के उपभोग की नकल निम्न वर्ग करता है, जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है।
उनके अनुसार आधुनिक पूंजीवादी समाज में प्रतिस्पर्धा ने कार्य की वास्तविक उपयोगिता की जगह प्रदर्शन और दिखावे को महत्व देना शुरू कर दिया है। यह विचार उपभोक्तावाद और वर्गीय संघर्ष को समझने में सहायक है।
प्रश्न-29. प्रकार्य को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- प्रकार्य किसी सामाजिक संरचना या तत्व द्वारा समाज में निभाई जा रही उपयोगी भूमिका को कहते हैं।
प्रश्न-30. पार्सन्स की क्रिया व्यवस्था के पक्षों की विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-ताल्कोट पार्सन्स ने समाज को एक क्रिया व्यवस्था (Action System) के रूप में देखा, जिसमें व्यक्ति और संस्थाएं परस्पर जुड़ी होती हैं। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को चार कार्यात्मक उप-प्रणालियों में बाँटा जिसे AGIL स्कीमा कहा जाता है:
- Adaptation (A): यह पर्यावरण से संसाधनों को ग्रहण करने और उनमें समायोजन करने की क्षमता है। आर्थिक संस्थाएं इसका उदाहरण हैं।
- Goal Attainment (G): यह लक्ष्यों की पूर्ति और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का कार्य करता है। राजनीतिक संस्थाएं इस कार्य को निभाती हैं।
- Integration (I): यह समाज के विभिन्न हिस्सों में सामंजस्य स्थापित करता है। सामाजिक संस्थाएं और कानूनी ढाँचा इसका कार्य करते हैं।
- Latency (L): यह सामाजिक मान्यताओं और मूल्यों का संरक्षण करता है। शिक्षा और परिवार इसकी मुख्य संस्थाएं हैं।
विशेषताएँ:
यह एक प्रणालीगत दृष्टिकोण है जो संतुलन और स्थायित्व पर बल देता है।
यह समाज के हर अंग को एक कार्यात्मक भूमिका के रूप में देखता है।
यह मॉडल जटिल समाजों को समझने में सहायक है।
हालाँकि, पार्सन्स की प्रणाली आलोचना का शिकार भी हुई क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन और संघर्ष की अनदेखी करता है।
प्रश्न-31. ऐतिहासिक भौतिकतावाद के तत्वों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- ऐतिहासिक भौतिकतावाद (Historical Materialism) कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि समाज का इतिहास आर्थिक आधार (आर्थिक ढांचा) पर आधारित होता है।
मुख्य तत्व इस प्रकार हैं:
- आर्थिक आधार और अधिरचना: समाज की संरचना दो भागों में होती है—आर्थिक आधार (उत्पादन प्रणाली) और अधिरचना (राजनीति, धर्म, कानून)।
- वर्ग संघर्ष: समाज की प्रगति वर्गों के बीच संघर्ष से होती है, जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच।
- ऐतिहासिक विकास: इतिहास की गति उत्पादन संबंधों में परिवर्तन से होती है। जब पुराने उत्पादन संबंध बाधा बनने लगते हैं, तो क्रांति होती है।
- सामाजिक परिवर्तन: ऐतिहासिक भौतिकतावाद के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का कारण भौतिक (आर्थिक) होता है, न कि केवल विचारधारा।
यह सिद्धांत समाज और इतिहास को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का मार्ग प्रशस्त करता है।
प्रश्न-32. इंद्रवाद पर हीगल के विचारों की स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- question-3 section – c
प्रश्न-33. मर्डन द्वारा दिए गए प्रकार्य के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- रॉबर्ट के. मर्टन ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में प्रकार्य (Function) के दो मुख्य प्रकारों की पहचान की:
- प्रकट प्रकार्य (Manifest Function): ये वे प्रकार्य होते हैं जो स्पष्ट रूप से देखे और समझे जा सकते हैं, जैसे शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना।
- गुप्त प्रकार्य (Latent Function): ये वे प्रकार्य होते हैं जो अप्रत्याशित होते हैं और तत्काल स्पष्ट नहीं होते, जैसे शिक्षा के माध्यम से सामाजिक संपर्क बनना।
मर्टन ने यह भी कहा कि कुछ सामाजिक गतिविधियों के प्रतिकूल प्रकार्य (Dysfunctions) भी हो सकते हैं जो समाज के लिए हानिकरक होते हैं। उनके वर्गीकरण ने समाजशास्त्रीय अध्ययन को अधिक गहराई प्रदान की और यह समझाया कि प्रत्येक सामाजिक संरचना कई स्तरों पर काम करती है।
प्रश्न-34. वर्ग-संघर्ष पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:-वर्ग-संघर्ष (Class Conflict) की अवधारणा कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित की गई। उन्होंने समाज को दो मुख्य वर्गों में बाँटा—पूंजीपति (Bourgeoisie) और मजदूर वर्ग (Proletariat)। पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, जबकि मजदूर वर्ग श्रम करता है।
मार्क्स के अनुसार, पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करता है, जिससे दोनों वर्गों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष आर्थिक असमानता, संसाधनों के वितरण और राजनीतिक सत्ता के कारण होता है। यह केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी गहरा होता है।
वर्ग-संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत है। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि यह संघर्ष मजदूर वर्ग की विजय और वर्गविहीन समाज की स्थापना की ओर ले जाएगा।
प्रासंगिकता: आज भी यह सिद्धांत सामाजिक असमानता, श्रमिक आंदोलनों, और आर्थिक नीतियों के विश्लेषण में उपयोगी है।
इस प्रकार, वर्ग-संघर्ष समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता और असमानता को समझने का एक प्रभावशाली उपकरण है।
प्रश्न-35. सामाजिक तथ्य के वर्गीकरण के नियम स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- एमिल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य (Social Facts) को समाजशास्त्र के अध्ययन की मूल इकाई माना और इनके वर्गीकरण हेतु कुछ नियम बताए:
- बाह्यता और विवशता पर आधारित – सामाजिक तथ्य समाज के बाहर होते हैं और व्यक्ति पर बलपूर्वक लागू होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है।
- मूल्य और मानदंड के आधार पर – जैसे नैतिकता, धर्म, कानून आदि मानदंडात्मक तथ्य होते हैं, जबकि जनसंख्या, जन्म दर, विवाह दर आदि सांख्यिकीय तथ्य होते हैं।
- सामूहिक चेतना के आधार पर – जो तथ्य समाज की सामूहिक चेतना को व्यक्त करते हैं उन्हें सामूहिक सामाजिक तथ्य कहा जाता है।
- सामाजिक संस्थाओं के अनुसार – धर्म, शिक्षा, परिवार, राज्य आदि संस्थाओं से संबंधित तथ्यों को उनके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।
दुर्खीम का उद्देश्य था कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित किया जाए, इसलिए उसने सामाजिक तथ्यों के स्पष्ट वर्गीकरण पर बल दिया।
प्रश्न-36. नौकरशाही के सामाजिक परिणामों को विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- नौकरशाही (Bureaucracy) की संकल्पना मैक्स वेबर ने दी थी, जिसे आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली का मूल माना जाता है। यह एक संगठित संरचना है, जिसमें नियम-कानून, पदानुक्रम, औपचारिकता, और दक्षता पर बल दिया जाता है।
सकारात्मक सामाजिक परिणाम:
नौकरशाही समाज में व्यवस्था और अनुशासन लाती है।
यह निष्पक्षता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करती है।
बड़े पैमाने पर सेवाओं का कुशलतापूर्वक संचालन संभव बनाती है।
नकारात्मक सामाजिक परिणाम:
यह व्यक्तियों को केवल ‘फाइल’ में बदल देती है, जिससे मानवीय संबंधों का ह्रास होता है।
अत्यधिक नियमबद्धता नवाचार और रचनात्मकता को दबा देती है।
‘लालफीताशाही’ और निर्णय-प्रक्रिया में विलंब आम हो जाता है।
यह एक अमानवीय और यांत्रिक व्यवस्था बन जाती है।
इस प्रकार, नौकरशाही समाज के लिए आवश्यक होते हुए भी यदि अनियंत्रित हो जाए तो सामाजिक ठहराव और असंतोष का कारण बन सकती है।
प्रश्न-37. पूँजीवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- पूँजीवाद (Capitalism) एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन — जैसे भूमि, पूँजी, मशीन आदि — निजी स्वामित्व में होते हैं और लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें बाजार आधारित प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार और श्रम बाजार की स्वतंत्रता प्रमुख विशेषताएँ होती हैं।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
यह नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करता है।
निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि करता है।
हालाँकि, इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं:
आय और संपत्ति की असमानता बढ़ती है।
श्रमिकों का शोषण होता है, क्योंकि श्रम को भी एक वस्तु की तरह देखा जाता है।
सामाजिक वर्ग विभाजन और असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है।
मार्क्स ने पूँजीवाद को एक शोषणकारी व्यवस्था कहा, जो अंततः अपने अंत की ओर अग्रसर होती है। पूँजीवाद के सकारात्मक पहलू होते हुए भी इसमें सामाजिक न्याय और समानता के लिए सुधार की आवश्यकता होती है।
प्रश्न-38.वेबेलियन का नियम विस्तार से लिखिए।
उत्तर:- थॉर्स्टीन वेब्लेन (Thorstein Veblen) एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने उपभोग की संस्कृति और अभिजात वर्ग के व्यवहार का विश्लेषण किया। उन्होंने “विलासी उपभोग” (Conspicuous Consumption) की अवधारणा दी।
उनके अनुसार समाज में उच्च वर्ग अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शनकारी उपभोग करता है। वेब्लेन ने कुछ नियमों और सिद्धांतों के माध्यम से यह समझाया कि कैसे उपभोग सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है।
मुख्य बिंदु:
वस्तुएँ उपयोगिता के बजाय सामाजिक दर्जा दिखाने के लिए खरीदी जाती हैं।
अभिजात वर्ग का यह व्यवहार निम्न वर्ग में भी अनुकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है।
इससे सामाजिक मूल्य बदलते हैं और उपभोग ही सफलता का मापक बन जाता है।
वेब्लेन के सिद्धांतों ने उपभोक्तावादी समाज और सामाजिक वर्ग संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
प्रश्न-39. पारसंत के व्यवस्था सिद्धान्त पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- टाल्कॉट पारसंस (Talcott Parsons) ने सामाजिक व्यवस्था (Social System) को समझाने के लिए “System Theory” का विकास किया। उनके अनुसार समाज एक जटिल प्रणाली है, जिसमें विभिन्न अंग एक-दूसरे से जुड़े होते हैं और सामंजस्य बनाए रखते हैं।
पारसंस ने चार प्रमुख कार्यात्मक आवश्यकताओं की बात की जिन्हें उन्होंने AGIL मॉडल कहा:
- Adaptation (A) – पर्यावरण से संसाधन ग्रहण करना।
- Goal Attainment (G) – लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना।
- Integration (I) – विभिन्न घटकों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- Latency (L) – सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों का संरक्षण।
उनका मानना था कि सामाजिक व्यवस्था तभी स्थिर रह सकती है जब यह चारों कार्यात्मक आवश्यकताएँ संतुलित रूप से पूरी हों। पारसंस का यह सिद्धांत सामाजिक स्थायित्व और संतुलन को समझाने में सहायक है, परंतु इसकी आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह सामाजिक परिवर्तन की उपेक्षा करता है।
प्रश्न-40. मर्टन द्वारा दिए गए प्रकात्मिक सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- रॉबर्ट के. मर्टन ने कार्यात्मकतावाद (Functionalism) को विस्तार देते हुए यह बताया कि किसी भी सामाजिक संरचना के स्पष्ट (Manifest) और अस्पष्ट (Latent) कार्य होते हैं।
मुख्य बिंदु:
स्पष्ट कार्य वे होते हैं जो उद्देश्यपूर्वक किए जाते हैं।
अस्पष्ट कार्य वे होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सभी सामाजिक संरचनाएँ सकारात्मक कार्य नहीं करतीं; कुछ दुष्परिणाम (Dysfunctions) भी उत्पन्न करती हैं।
आलोचना:
मर्टन का कार्यात्मक दृष्टिकोण संतुलन और स्थिरता पर अधिक जोर देता है, जिससे संघर्ष और असमानता की उपेक्षा होती है।
यह नवाचार और विद्रोह जैसे सामाजिक परिवर्तन के कारकों को पर्याप्त महत्व नहीं देता।
कुछ विचारक इसे बहुत संरचनात्मक और अमूर्त मानते हैं।
फिर भी, मर्टन ने कार्यात्मकतावाद को एक अधिक लचीली और आलोचनात्मक दृष्टि प्रदान की, जिससे सामाजिक संरचनाओं की विविधता को बेहतर ढंग से समझा जा सका।
प्रश्न-41. धर्म के सम्बन्ध में वेबर के विचारों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- मैक्स वेबर ने धर्म को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था माना, जो सामाजिक संरचना और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। वेबर की प्रसिद्ध कृति “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” में उन्होंने बताया कि कैसे प्रोटेस्टेंट धर्म, विशेषतः काल्विनिज्म, ने पूँजीवाद के विकास को प्रेरित किया।
वेबर के अनुसार:
धर्म केवल आध्यात्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि यह लोगों के आर्थिक और सामाजिक व्यवहार को निर्देशित करता है।
धार्मिक नैतिकता जैसे परिश्रम, अनुशासन, ईमानदारी, और मितव्ययिता ने पूँजीवादी विचारधारा को जन्म दिया।
उन्होंने विभिन्न धर्मों जैसे हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, और कन्फ्यूशियस धर्म का तुलनात्मक अध्ययन भी किया।
वेबर ने धर्म को एक ऐसी शक्ति माना जो सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि धर्म और अर्थव्यवस्था के बीच गहरा संबंध होता है।।
प्रश्न-42. अभिजन के परिसंचरण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-(Theory of Circulation of Elites) का प्रतिपादन इतालवी विचारक विल्फ्रेडो पैरेटो ने किया। उन्होंने समाज में शक्ति और नेतृत्व की प्रक्रिया को समझाने के लिए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया।
मुख्य बातें:
समाज में दो प्रकार के अभिजन होते हैं: शेर जैसे (बल आधारित) और लोमड़ी जैसे (चतुराई आधारित)।
कोई भी अभिजन वर्ग स्थायी नहीं होता। समय के साथ उनमें बदलाव होता है – नीचे के वर्गों के कुछ व्यक्ति अभिजन बनते हैं और पुराने अभिजन नीचे गिर जाते हैं।
यह प्रक्रिया “अभिजन परिसंचरण” कहलाती है, जो समाज में गतिशीलता बनाए रखती है।
यदि यह परिसंचरण नहीं होता, तो समाज में असंतोष और क्रांति का खतरा बढ़ जाता है।
पैरेटो ने दिखाया कि सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए समाज में नेतृत्व का परिवर्तन आवश्यक है। उनका सिद्धांत राजनीतिक समाजशास्त्र में महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
प्रश्न-43. पार्सन्स के क्रिया सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-टैल्कॉट पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को समझाने के लिए एक “क्रिया प्रणाली” (Action System) का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने सामाजिक क्रिया को चार उप-प्रणालियों में विभाजित किया, जिन्हें AGIL मॉडल के रूप में जाना जाता है:
- A – Adaptation (अनुकूलन): समाज को अपने पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करने और उन्हें अनुकूलित करने की क्षमता।
- G – Goal Attainment (लक्ष्य प्राप्ति): सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति और उनकी दिशा तय करना।
- I – Integration (एकीकरण): समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर सामंजस्य बनाए रखना।
- L – Latency (प्रतीक्षा/रूपांतरण): सांस्कृतिक मूल्यों और प्रेरणाओं को संरक्षित रखना।
पार्सन्स ने माना कि हर समाज में यह चार कार्य आवश्यक होते हैं और यह कार्य विभिन्न संस्थाएँ जैसे परिवार, शिक्षा, राजनीति आदि निभाती हैं। उनका यह सिद्धांत समाज की स्थिरता और संतुलन को समझने के लिए उपयोगी है।
Section-C
प्रश्न-1.अगस्त कॉम्टे के समाजशास्त्रीय योगदान को विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- अगस्त कॉम्टे (1798-1857) को समाजशास्त्र का जनक (Father of Sociology) कहा जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया। उनके विचार प्रत्यक्षवाद (Positivism) पर आधारित थे। उनका मुख्य उद्देश्य समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कर समाज में व्यवस्था और प्रगति स्थापित करना था।
कॉम्टे के प्रमुख समाजशास्त्रीय योगदान इस प्रकार हैं:
- प्रत्यक्षवाद (Positivism):
कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार समाज का अध्ययन उसी प्रकार करना चाहिए जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है – यानि अनुभव, अवलोकन, प्रयोग और तुलनात्मक विधियों द्वारा। यह विचार समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक स्वरूप देता है। - समाज के विकास के तीन चरण (Law of Three Stages):
कॉम्टे ने मानव समाज के बौद्धिक विकास को तीन चरणों में विभाजित किया:
धार्मिक या सैद्धांतिक चरण (Theological Stage): इस चरण में समाज ईश्वर और अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करता है।
दार्शनिक या मध्यवर्ती चरण (Metaphysical Stage): इसमें समाज अमूर्त और दार्शनिक विचारों के माध्यम से घटनाओं को समझता है।
वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी चरण (Positive Stage): इस चरण में समाज वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सत्य को खोजता है।
- समाजशास्त्र की संकल्पना:
कॉम्टे ने पहली बार ‘Sociology’ शब्द का प्रयोग किया और इसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने समाजशास्त्र को दो शाखाओं में विभाजित किया:
सामाजिक स्थैतिकी (Social Statics): यह समाज की संरचना और स्थायित्व का अध्ययन करता है।
सामाजिक गतिकी (Social Dynamics): यह समाज में होने वाले परिवर्तनों और विकास की प्रक्रिया को समझता है।
- सामाजिक पुनर्गठन का सिद्धांत:
कॉम्टे का मानना था कि समाज में सकारात्मक विचारधारा और विज्ञान के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था लाई जा सकती है। उन्होंने समाज में नैतिकता, सहयोग और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर बल दिया। - धर्म और नैतिकता पर जोर:
हालाँकि कॉम्टे नास्तिक थे, परंतु उन्होंने “मानवता के धर्म” (Religion of Humanity) की संकल्पना दी। उनका मानना था कि समाज को नैतिकता और मानवतावाद के आधार पर संगठित करना चाहिए।
अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उनके विचारों ने न केवल समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया, बल्कि आधुनिक समाज के निर्माण में भी मार्गदर्शन किया।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.भावां के द्वंद्वात्मकता को विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मकता (Dialectics) जर्मन दार्शनिक हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रभावित है, लेकिन मार्क्स ने उसे एक भौतिकवादी दृष्टिकोण में परिवर्तित किया। जहाँ हेगेल की द्वंद्वात्मकता विचारों की द्वंद्वात्मकता थी, वहीं मार्क्स की द्वंद्वात्मकता भौतिक परिस्थितियों और वर्ग-संघर्ष पर आधारित है। इसे “ऐतिहासिक भौतिकवाद” (Historical Materialism) भी कहा जाता है।
मार्क्स का मानना था कि इतिहास में सभी परिवर्तन द्वंद्व के माध्यम से होते हैं, अर्थात् विरोधी शक्तियों के संघर्ष के कारण। समाज में यह द्वंद्व आर्थिक वर्गों के बीच होता है — शोषक वर्ग (जैसे पूँजीपति) और शोषित वर्ग (जैसे श्रमिक)। यह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया थीसिस (स्थित व्यवस्था), एंटीथीसिस (विरोध) और सिंथीसिस (नवीन व्यवस्था) के रूप में आगे बढ़ती है।
मार्क्स के अनुसार, प्रत्येक ऐतिहासिक अवस्था में एक विशेष उत्पादन प्रणाली होती है, और यह प्रणाली अंततः अपने भीतर विरोधाभास उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, पूँजीवाद में, पूँजीपति अधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों का शोषण करते हैं, जिससे वर्ग-संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष अंततः क्रांति को जन्म देता है, जिससे एक नई सामाजिक व्यवस्था (जैसे समाजवाद) की स्थापना होती है।
मार्क्स की द्वंद्वात्मकता का उद्देश्य केवल समाज को समझना नहीं बल्कि उसे बदलना है। उन्होंने कहा था: “दार्शनिकों ने अब तक केवल दुनिया की व्याख्या की है, जबकि बात यह है कि उसे बदला जाए।”
मार्क्स की द्वंद्वात्मकता एक क्रांतिकारी पद्धति है जो यह दर्शाती है कि समाज का विकास विरोधाभासों के संघर्ष के माध्यम से होता है और यह प्रक्रिया ऐतिहासिक और आर्थिक कारकों से संचालित होती है।
प्रश्न-3. इन्द्रवाद पर हीगेल एवं मार्क्स के विचारों का तुलनात्मक स्पष्टीकरण दीजिए।
उत्तर:- हीगेल और मार्क्स दोनों ने द्वंद्वात्मक पद्धति (Dialectics) का प्रयोग अपने दर्शन में किया, किंतु दोनों के दृष्टिकोण और उद्देश्यों में मौलिक अंतर हैं। हीगेल का द्वंद्वात्मक पद्धति एक आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित था जबकि मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिकवादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ था।
हीगेल का द्वंद्ववाद:
हीगेल एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को एक विचारात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा। उनके अनुसार विचार ही यथार्थ का मूल है और संसार का विकास विचारों के संघर्ष और विकास से होता है। उन्होंने तर्क किया कि कोई भी विचार जब जन्म लेता है (थीसिस), तो उसके विरोध में एक प्रतिविचार (एंटीथीसिस) आता है, और दोनों के संलयन से एक उच्च स्तर का विचार (सिंथीसिस) उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को वे “आत्मा” या “विश्व आत्मा” की प्रगति मानते हैं।
मार्क्स का द्वंद्ववाद:
कार्ल मार्क्स ने हीगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार किया, परंतु उसे “भौतिकवादी द्वंद्ववाद” (Dialectical Materialism) का रूप दिया। उनके अनुसार विचार नहीं, बल्कि भौतिक स्थितियाँ और आर्थिक संबंध ही समाज में परिवर्तन लाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन के साधनों और वर्ग संघर्ष के आधार पर समाज में द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, जो नए सामाजिक ढांचे को जन्म देते हैं।
तुलनात्मक दृष्टिकोण:
पहलू हीगेल मार्क्स
दृष्टिकोण आदर्शवादी भौतिकवादी
प्राथमिकता विचार/चेतना भौतिक स्थिति/आर्थिक संबंध
प्रक्रिया थीसिस – एंटीथीसिस – सिंथेसिस वर्ग संघर्ष के माध्यम से
उद्देश्य आत्मा की पूर्णता वर्गहीन समाज की स्थापना
परिवर्तन का आधार विचारों का संघर्ष आर्थिक संघर्ष
जहाँ हीगेल का द्वंद्ववाद दर्शन और चेतना के विकास को केंद्र में रखता है, वहीं मार्क्स का दृष्टिकोण भौतिक आधार पर सामाजिक परिवर्तन को बल देता है। दोनों की द्वंद्वात्मक पद्धति में समानता तो है, परंतु उनका दार्शनिक आधार भिन्न है। मार्क्स ने हीगेल को “पैरों के बल उल्टा” कर दिया, अर्थात् आदर्श के बजाय भौतिकता को प्राथमिकता दी।
प्रश्न-4. अगस्त कॉन्टे के द्वारा चलाए गए ज्ञान के विकास के स्तर विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- अगस्त कॉन्टे (Auguste Comte) को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने ज्ञान के विकास की प्रक्रिया को तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया जिसे उन्होंने “तीन अवस्थाओं का सिद्धांत” (Law of Three Stages) कहा। यह सिद्धांत बताता है कि मानव समाज और उसकी सोच कैसे विकसित होती है।
- धार्मिक अवस्था (Theological Stage):
यह ज्ञान का प्रारंभिक चरण होता है। इस अवस्था में मानव अपनी सभी जिज्ञासाओं का उत्तर अलौकिक शक्तियों और ईश्वर से जोड़कर देता है। मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं जैसे वर्षा, तूफान, भूकंप आदि को देवी-देवताओं का क्रोध मानता है। इस चरण में तीन उप-अवस्थाएँ होती हैं:
फेटिशिज्म (Fetishism): जहाँ निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानकर पूजा की जाती है।
पॉलीथिअज्म (Polytheism): अनेक देवी-देवताओं में विश्वास।
मोनोथिअज्म (Monotheism): एक ईश्वर में विश्वास।
- दार्शनिक अवस्था (Metaphysical Stage):
इस चरण में मानव धार्मिक विचारों से कुछ ऊपर उठता है लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं बनता। यहाँ प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या अमूर्त सिद्धांतों या दर्शनशास्त्रीय तत्वों द्वारा की जाती है। जैसे “प्रकृति की शक्ति”, “भाग्य”, “आत्मा” आदि का प्रयोग समझाने के लिए किया जाता है। यह एक संक्रमणकालीन अवस्था है जो धार्मिकता और वैज्ञानिकता के बीच स्थित है।
- वैज्ञानिक अवस्था (Positive/Scientific Stage):
यह मानव ज्ञान का सबसे परिपक्व और विकसित स्तर होता है। इसमें व्यक्ति तर्क, अनुभव और वैज्ञानिक विधियों से ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ घटनाओं की व्याख्या वैज्ञानिक तथ्यों, प्रयोगों और प्रमाणों के आधार पर की जाती है। अगस्त कॉन्टे ने इसे “पॉज़िटिव स्टेज” कहा क्योंकि इसमें सकारात्मक और ठोस ज्ञान प्राप्त होता है।
अगस्त कॉन्टे का यह सिद्धांत मानव बौद्धिक विकास की प्रक्रिया को क्रमिक रूप से दर्शाता है। यह सिद्धांत न केवल समाजशास्त्र में बल्कि ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि मानव चेतना कैसे धार्मिक से वैज्ञानिक सोच की ओर अग्रसर होती है।
प्रश्न-5. ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical Materialism) कार्ल मार्क्स (Karl Marx) द्वारा प्रतिपादित एक प्रमुख सिद्धांत है जो इतिहास की गति और समाज में परिवर्तन को भौतिक परिस्थितियों, खासकर आर्थिक संरचना के आधार पर समझाता है।
ऐतिहासिक भौतिकवाद की मूल अवधारणा:
मार्क्स के अनुसार, “भौतिक जीवन की स्थितियाँ, विशेषकर उत्पादन के साधन और उनके संबंध, सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक विकास के मूल आधार होते हैं।”
मुख्य तत्त्व:
- अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्थान: मार्क्स मानते थे कि समाज की बुनियादी संरचना उसकी अर्थव्यवस्था होती है, न कि धर्म या विचारधारा। आर्थिक संरचना ही समाज के अन्य पहलुओं को तय करती है।
- अवधारणा: आधार और अधिरचना (Base and Superstructure):
आधार (Base): उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंध।
अधिरचना (Superstructure): धर्म, राजनीति, कानून, विचारधारा आदि। आधार में बदलाव आने से अधिरचना भी बदलती है।
- वर्ग संघर्ष (Class Struggle): ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है – शोषक और शोषित के बीच संघर्ष। यह संघर्ष सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न करता है।
- समाज की अवस्थाएँ: मार्क्स ने इतिहास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया:
आदिम साम्यवाद (Primitive Communism)
दास प्रथा (Slave Society)
सामंती समाज (Feudalism)
पूँजीवाद (Capitalism)
समाजवाद (Socialism)
साम्यवाद (Communism)
ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास को वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत समाज के परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया को आर्थिक दृष्टिकोण से व्याख्यायित करता है, जिससे सामाजिक क्रांति और परिवर्तन को समझा जा सकता है।
प्रश्न-6. पेरेटो के चक्रीय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- विलफ्रेडो पेरेटो (Vilfredo Pareto), एक इटालियन समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने एलिट सर्कुलेशन थ्योरी (Circulation of Elites) प्रस्तुत की। यह सिद्धांत समाज के शक्ति-संतुलन में निरंतर परिवर्तन को दर्शाता है।
पेरेटो के चक्रीय सिद्धांत की मूल धारणा:
पेरेटो के अनुसार समाज में दो प्रकार की अभिजात वर्ग (Elites) होते हैं:
- शेर (Lions): ये परंपरावादी, अनुशासनप्रिय और सैन्य शक्तियों पर आधारित होते हैं।
- लोमड़ी (Foxes): ये चतुर, चालाक और धोखे द्वारा सत्ता प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं।
समाज में सत्ता इन्हीं दो वर्गों के बीच चक्र की भांति घूमती रहती है – एक समय पर ‘शेर’ सत्ता में होते हैं, तो कभी ‘लोमड़ी’ सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। यह चक्रीय प्रक्रिया सतत चलती रहती है।
मुख्य बिंदु:
कोई भी अभिजात वर्ग स्थायी नहीं होता।
हर अभिजात वर्ग अंततः भ्रष्ट हो जाता है और एक नया वर्ग उसे प्रतिस्थापित करता है।
सामान्य जनता इस प्रक्रिया में निष्क्रिय भूमिका निभाती है।
आलोचनात्मक विश्लेषण:
- ऐतिहासिक प्रमाण:
पेरेटो का सिद्धांत इतिहास के अनेक उदाहरणों से मेल खाता है – जैसे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति आदि। - सीमाएँ:
यह सिद्धांत सत्ता परिवर्तन को केवल दो ही वर्गों में सीमित करता है।
इसमें आम जनता की भूमिका नगण्य मानी गई है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाती।
यह परिवर्तन को अनिवार्य बताता है लेकिन सामाजिक सुधार या विकास की संभावना को नकारता है।
पेरेटो का चक्रीय सिद्धांत सामाजिक शक्ति संरचना में निरंतर बदलाव की व्याख्या करता है, परंतु इसमें जनता की भूमिका, विचारधाराओं और अन्य सामाजिक कारकों की उपेक्षा की गई है।
प्रश्न-7. सामाजिक क्रिया को परिभाषित कीजिए। सामाजिक क्रिया के प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:-सामाजिक क्रिया (Social Action) की संकल्पना जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने दी थी। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी क्रिया किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति या संभावित प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर करता है, तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है।
परिभाषा:
मैक्स वेबर के अनुसार – “सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जो किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है और जिसका अर्थ दूसरों के व्यवहार से संबंधित होता है तथा वह उस पर प्रभाव डालती है।”
उदाहरण के लिए: कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है, यह सामाजिक क्रिया है क्योंकि यह विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से की जाती है।
सामाजिक क्रिया के प्रकार:
मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को चार प्रकारों में विभाजित किया:
- परंपरागत क्रिया (Traditional Action):
यह क्रिया परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक मान्यताओं के आधार पर की जाती है। जैसे – त्योहारों पर पूजा करना। - भावनात्मक क्रिया (Affective Action):
यह क्रिया भावना या आवेग के प्रभाव में होती है। जैसे – गुस्से में किसी को डांटना। - मूल्य-युक्त क्रिया (Value-Rational Action):
यह क्रिया किसी मूल्य या आदर्श के आधार पर की जाती है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। जैसे – देशभक्ति के लिए बलिदान देना। - उद्देश्य-युक्त क्रिया (Goal-Rational Action):
यह क्रिया सोच-समझकर और किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। जैसे – नौकरी पाने के लिए परीक्षा देना।
सामाजिक क्रिया समाज के संचालन और मानव व्यवहार की समझ में सहायक है। वेबर की यह अवधारणा समाजशास्त्र की एक मौलिक और महत्त्वपूर्ण अवधारणा है।
प्रश्न-8. समाजशास्त्र की एक विषय के रूप में उत्पत्ति में यूरोपीय योगदान की सविस्तार लिखिए।
उत्तर:- समाजशास्त्र का उद्भव एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुआ। इसकी उत्पत्ति सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक परिवर्तनों के कारण संभव हो सकी, जिनमें यूरोप की विशेष भूमिका रही।
- फ्रांसीसी क्रांति (1789):
फ्रांसीसी क्रांति ने ‘स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व’ के आदर्श को जन्म दिया। पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और सामंती ढांचे का पतन हुआ। इससे सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई, जिसे समझने और व्यवस्थित करने हेतु समाजशास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई। - औद्योगिक क्रांति:
18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन प्रणाली, शहरीकरण और श्रमिक वर्ग के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे समाज में आर्थिक विषमता और सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं, जो समाजशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय बनीं। - ज्ञानोदय युग (Enlightenment):
17वीं-18वीं शताब्दी में यूरोप में ज्ञानोदय काल ने तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को प्रोत्साहित किया। पारंपरिक धार्मिक विश्वासों के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति और अनुभववाद को महत्व मिला। इसी विचारधारा ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की आधारशिला रखी। - दर्शन और विज्ञान का प्रभाव:
दार्शनिकों जैसे जॉन लॉक, रूसो, कांट, और बाद में समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्ट कॉम्टे ने तर्क और अनुभव के आधार पर समाज को समझने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। कॉम्टे ने ‘सोशियोलॉजी’ शब्द को पहली बार प्रयोग किया और इसे समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया। - यूरोपीय समाज की विविधता:
राज्य, धर्म, वर्ग, जाति, राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद और पूँजीवाद जैसी जटिल सामाजिक प्रक्रियाएँ यूरोप में सक्रिय थीं। इनके विश्लेषण हेतु एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता थी।
यूरोप में राजनीतिक क्रांतियाँ, औद्योगीकरण, बौद्धिक आंदोलन और सामाजिक अस्थिरता ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित किया। समाज की समस्याओं को वैज्ञानिक रूप में समझने की यह आवश्यकता ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बनी।
प्रश्न-9. मर्टन के प्रकार्यवाद को समझाइए।
उत्तर:- रॉबर्ट के. मर्टन (Robert K. Merton) एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री थे, जिन्होंने कार्यात्मकता (Functionalism) को आधुनिक रूप प्रदान किया। उन्होंने “मध्यम-स्तरीय सिद्धांत” (Middle Range Theory) और प्रकार्यवाद (Functional Analysis/Functionalism) की अवधारणाओं को स्पष्ट किया।
मर्टन के प्रकार्यवाद के प्रमुख तत्त्व:
- प्रकट एवं अप्रकट क्रियाएँ (Manifest and Latent Functions):
प्रकट क्रियाएँ: ये वे क्रियाएँ हैं जिनके उद्देश्य स्पष्ट और जानबूझकर किए जाते हैं। जैसे शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना।
अप्रकट क्रियाएँ: ये वे क्रियाएँ हैं जो अनजाने में या अज्ञात रूप से समाज पर प्रभाव डालती हैं। जैसे शिक्षा सामाजिक नियंत्रण भी करती है।
- दुष्प्रभाव (Dysfunction): मर्टन ने बताया कि सभी सामाजिक क्रियाएँ समाज के लिए लाभकारी नहीं होतीं। कुछ क्रियाओं के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। यह अवधारणा पारंपरिक प्रकार्यवाद से अलग थी, जो समाज को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण मानता था।
- नेट बैलेंस की अवधारणा (Net Balance): मर्टन के अनुसार, किसी भी सामाजिक संस्था की कुल उपयोगिता उसके लाभ और हानि दोनों को देखकर तय की जानी चाहिए।
- सामाजिक संरचना और अनामिता (Anomie): मर्टन ने “स्ट्रेन थ्योरी” के माध्यम से बताया कि जब समाज में लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों के बीच विरोध होता है, तब व्यक्ति सामाजिक मानदंडों से भटक सकता है। इससे सामाजिक विचलन (deviance) उत्पन्न होता है।
मर्टन का प्रकार्यवाद पारंपरिक प्रकार्यवाद से अधिक यथार्थवादी और व्यावहारिक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक संस्थाओं के कार्य बहु-स्तरीय होते हैं और उनका समाज पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकता है। उनकी दृष्टि ने समाजशास्त्र को एक नई दिशा दी।
प्रश्न-10. वेबर के सामाजिक क्रिया के विचारों का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:-मैक्स वेबर जर्मनी के समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को समझने के लिए “सामाजिक क्रिया” (Social Action) की अवधारणा दी। उन्होंने समाजशास्त्र को एक “व्याख्यात्मक विज्ञान” (Interpretive Science) कहा और इसका उद्देश्य व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं के अर्थ को समझना बताया।
सामाजिक क्रिया की परिभाषा:
वेबर के अनुसार, सामाजिक क्रिया वह मानव क्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व या व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है, और उसका उद्देश्य कोई अर्थपूर्ण सामाजिक संदर्भ होता है।
सामाजिक क्रिया के प्रकार:
- परंपरागत क्रिया (Traditional Action):
यह क्रिया सामाजिक परंपराओं और आदतों पर आधारित होती है। उदाहरण: त्योहारों पर पूजा करना। - भावात्मक क्रिया (Affective Action):
यह भावनाओं और आवेगों से प्रेरित होती है। उदाहरण: क्रोध में आकर कोई कार्य करना। - मूल्य-तर्कसंगत क्रिया (Value Rational Action):
इसमें कार्य किसी मूल्य या नैतिक सिद्धांत के पालन के लिए किया जाता है, बिना परिणाम की चिंता किए। - उपाय-तर्कसंगत क्रिया (Means-End Rational Action):
यह क्रिया लक्ष्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपायों के चुनाव पर आधारित होती है। उदाहरण: नौकरी पाने हेतु परीक्षा की तैयारी।
विश्लेषण:
वेबर ने सामाजिक क्रिया को व्यक्तिपरक अर्थों से जोड़ते हुए समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया।
उन्होंने तात्त्विक रूप से यह समझाया कि सभी सामाजिक व्यवहार अर्थपूर्ण होते हैं और उन्हें उनके सामाजिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
वेबर की यह अवधारणा सामाजिक संरचनाओं से अधिक व्यक्ति की क्रिया पर बल देती है, जिससे यह मनोविज्ञान से प्रभावित प्रतीत होती है।
आलोचना:
कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि वेबर की दृष्टि बहुत अधिक व्यक्तिपरक है और सामाजिक संरचना की भूमिका को कम आँकती है।
यह दृष्टिकोण अधिक जटिल समाजों की व्याख्या करने में सीमित रह जाता है।
फिर भी, यह समाजशास्त्रीय विश्लेषण में मानव की एजेंसी को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा समाजशास्त्र में व्यक्ति की भूमिका और उसके अर्थपूर्ण व्यवहार को समझने में सहायक है। इसने समाजशास्त्र को केवल संरचना तक सीमित न रखकर उसे अर्थपूर्ण मानवीय क्रिया की दिशा में विस्तृत किया।
प्रश्न-11. अलगाव को परिभाषित कीजिए तथा अलगाव प्रक्रिया की प्रारंभ होने के कारणों को विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- अलगाव (Alienation) वह सामाजिक स्थिति है, जब कोई व्यक्ति स्वयं से, अपने कार्य से, समाज से या अन्य लोगों से कटाव महसूस करता है। यह अवधारणा प्रमुख रूप से कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत की थी।
अलगाव की परिभाषा:
मार्क्स के अनुसार — “अलगाव वह स्थिति है जिसमें श्रमिक अपने श्रम, उत्पादन और मानव स्वभाव से विमुक्त हो जाता है।” व्यक्ति को लगता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य उसके जीवन का हिस्सा नहीं है।
अलगाव के प्रकार (Types of Alienation):
- कार्य से अलगाव: मजदूर अपने श्रम को अपना नहीं मानता।
- उत्पाद से अलगाव: वह वस्तु जो मजदूर बनाता है, वह उसकी नहीं होती।
- स्वयं से अलगाव: व्यक्ति अपनी रचनात्मकता और आत्मा से कट जाता है।
- अन्य लोगों से अलगाव: समाज में संबंध यांत्रिक और औपचारिक हो जाते हैं।
अलगाव के कारण (Causes of Alienation):
- पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली:
पूँजीवाद में श्रमिक केवल एक यंत्र की तरह कार्य करता है। उसका श्रम वस्तु में परिवर्तित हो जाता है जिसे वह स्वयं उपभोग नहीं कर सकता। - कार्य का अति-विशेषीकरण:
जब कार्य को अत्यधिक विभाजित किया जाता है, तो श्रमिक केवल एक छोटा हिस्सा करता है, जिससे उसे सम्पूर्ण प्रक्रिया से जुड़ाव नहीं रहता। - सामाजिक असमानता:
शोषण, वर्ग-भेद और संसाधनों का असमान वितरण व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है। - यांत्रिक जीवन शैली:
आधुनिक समाज में तकनीक और प्रतियोगिता ने मानवीय संबंधों को कमजोर किया है। - आत्म-अभिव्यक्ति की कमी:
जब व्यक्ति अपने विचार, रचनात्मकता और इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, तो उसमें अलगाव की भावना उत्पन्न होती है।
अलगाव एक गंभीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है। इसे दूर करने के लिए आवश्यक है कि समाज में कार्य की मानवीयता, समानता, रचनात्मकता और सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए।
प्रश्न-12. परेटी के चक्रीय सिद्धांत को विस्तार से स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- विलफ्रेडो परेटो एक इटालियन समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने “एलीट का चक्रीय सिद्धांत” (Circulation of Elites) प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, समाज में सदैव दो प्रकार के वर्ग होते हैं – शासक (एलीट) और शासित (जनसाधारण)। ये वर्ग स्थायी नहीं होते, बल्कि इनमें सतत परिवर्तन (Circulation) होता रहता है।
मुख्य विचार:
परेटो के अनुसार, किसी भी समाज में शासक वर्ग (Elite) धीरे-धीरे भ्रष्ट और अयोग्य हो जाता है। तब उसके स्थान पर नया, सक्षम वर्ग उभरता है और सत्ता संभालता है। यह प्रक्रिया “एलीट का परिसंचरण” कहलाती है।
प्रकार:
परेटो ने दो प्रकार के एलीट का उल्लेख किया:
- शेर जैसे एलीट (Lions):
ये परंपरावादी, कठोर और बल का प्रयोग करने वाले होते हैं। जैसे – सैन्य या नौकरशाही शासक। - लोमड़ी जैसे एलीट (Foxes):
ये चतुर, चालाक और कूटनीति का उपयोग करने वाले होते हैं। जैसे – व्यापारी या राजनेता।
सिद्धांत की प्रक्रिया:
कोई भी एलीट वर्ग जब समाज पर शासन करता है, तो समय के साथ वह भ्रष्ट हो जाता है।
समाज के नीचे के वर्गों से कुछ सक्षम लोग ऊपर उठते हैं और पुराने एलीट वर्ग की जगह लेते हैं।
यह बदलाव धीरे-धीरे या कभी-कभी क्रांतिकारी रूप में होता है।
परेटो का यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि समाज में शक्ति का वितरण स्थिर नहीं रहता, बल्कि निरंतर बदलाव होता रहता है। यह परिवर्तन समाज की गतिशीलता का प्रतीक है।
प्रश्न-13. मर्टन के संरचनात्मक प्रकार्यवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
उत्तर:-रॉबर्ट के. मर्टन अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने टाल्कॉट पार्सन्स की संरचनात्मक प्रकार्यवाद (Structural Functionalism) को विकसित और संशोधित किया। मर्टन ने इस सिद्धांत को अधिक व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक रूप प्रदान किया।
मर्टन का योगदान:
- मैनिफेस्ट एवं लैटेंट फल (Manifest and Latent Functions):
मर्टन ने स्पष्ट (मैनिफेस्ट) और अप्रकट (लैटेंट) कार्यों की अवधारणा दी।
मैनिफेस्ट क्रियाएं वे होती हैं जो जानबूझकर और घोषित होती हैं।
लैटेंट क्रियाएं वे होती हैं जो अनजाने में और अनजाने प्रभाव उत्पन्न करती हैं।
उदाहरण: शिक्षा प्रणाली का मैनिफेस्ट उद्देश्य ज्ञान देना है, जबकि लैटेंट उद्देश्य सामाजिक वर्गीकरण भी हो सकता है।
- दिसफंक्शन (Dysfunction):
मर्टन ने माना कि सभी संस्थाएं केवल संतुलन बनाए नहीं रखतीं, वे सामाजिक असंतुलन या तनाव भी उत्पन्न कर सकती हैं। - सामाजिक संरचना एवं विचलन (Social Structure and Anomie):
मर्टन ने “Strain Theory” प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि जब सामाजिक लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के साधनों में अंतर होता है, तो व्यक्ति विचलित हो सकता है।
आलोचना:
मर्टन ने पार्सन्स के व्यापक सिद्धांत को अधिक विशिष्ट और परीक्षण योग्य बनाया, परंतु उन पर भी संरचनावाद पर अति निर्भरता का आरोप लगा।
वे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिक विस्तार से नहीं समझा सके।
मर्टन की संरचनात्मक प्रकार्यवाद अब भी व्यक्ति की भूमिका और संघर्ष के पहलुओं की अनदेखी करता है।
मर्टन का संरचनात्मक प्रकार्यवाद समाज के कार्यात्मक विश्लेषण को अधिक सटीकता से प्रस्तुत करता है। उनकी अवधारणाएं समाजशास्त्र के क्षेत्र में व्यवहारिक विश्लेषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि इसकी सीमाएँ हैं, परंतु यह सामाजिक संस्थाओं और क्रियाओं को समझने में सहायक सिद्ध होता है।
प्रश्न-14. विलासी वर्ग के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- “विलासी वर्ग का सिद्धांत” (Theory of Leisure Class) अमेरिकी समाजशास्त्री थॉर्स्टीन वेब्लेन (Thorstein Veblen) द्वारा 1899 में प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत के माध्यम से वेब्लेन ने आधुनिक पूंजीवादी समाज में उच्च वर्गों की जीवनशैली, दिखावे और उपभोग की प्रवृत्तियों की आलोचना की।
मुख्य अवधारणाएँ:
- विलासी वर्ग (Leisure Class):
यह वह वर्ग होता है जो शारीरिक श्रम से मुक्त होता है और केवल मानसिक या सामाजिक कार्य करता है। यह वर्ग अपनी संपत्ति और स्थिति का प्रदर्शन करता है। - दिखावटी उपभोग (Conspicuous Consumption):
वेब्लेन के अनुसार, उच्च वर्ग के लोग महँगे वस्त्र, गहने, बड़ी गाड़ियाँ और विलासितापूर्ण जीवनशैली अपनाते हैं ताकि वे अपने सामाजिक स्तर का प्रदर्शन कर सकें। - दिखावटी खालीपन (Conspicuous Leisure):
यह वर्ग ऐसी गतिविधियाँ करता है जो किसी उत्पादक कार्य से संबंधित नहीं होतीं, जैसे – विदेशी यात्राएँ, शौकीन आयोजन, क्लब, इत्यादि। - श्रम का तिरस्कार:
वेब्लेन का कहना है कि यह वर्ग शारीरिक श्रम को तुच्छ समझता है और केवल ‘प्रतिष्ठित’ कार्यों को ही मान्यता देता है।
आलोचना:
वेब्लेन का यह सिद्धांत पूँजीवादी समाज की असमानताओं को उजागर करता है। यह बताता है कि कैसे संपन्न वर्ग केवल उपभोग और दिखावे में लगा रहता है, जिससे संसाधनों का असमान वितरण होता है।
“विलासी वर्ग का सिद्धांत” आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह उपभोक्तावाद और सामाजिक असमानता को समझने में सहायता करता है। आधुनिक समाज में ब्रांड, फैशन और महंगे जीवनशैली की प्रवृत्ति इस सिद्धांत की पुष्टि करती है।
प्रश्न-15. नौकरशाही की परिभाषा कीजिए। नौकरशाही की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- नौकरशाही (Bureaucracy) का अर्थ है — प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित एवं नियमबद्ध ढंग से चलाने की एक प्रणाली। इस अवधारणा को विस्तृत रूप से जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर (Max Weber) ने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार नौकरशाही एक आदर्श प्रकार (Ideal Type) है जो दक्षता, अनुशासन और तटस्थता पर आधारित होती है।
नौकरशाही की परिभाषा (Definition):
मैक्स वेबर के अनुसार — “नौकरशाही एक प्रशासनिक प्रणाली है जिसमें कार्य विभाजन, नियमों का पालन, पदानुक्रम, लिखित दस्तावेजों की व्यवस्था और पेशेवर कुशलता के आधार पर कार्य होते हैं।”
नौकरशाही की मुख्य विशेषताएँ (Characteristics of Bureaucracy):
- स्पष्ट पदानुक्रम (Clear Hierarchy):
नौकरशाही में एक स्पष्ट अधिकार श्रृंखला होती है, जिसमें उच्च पद से लेकर निम्न स्तर तक कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण होता है। - कार्य विभाजन (Division of Labour):
प्रत्येक पदाधिकारी को विशेष कार्य सौंपा जाता है, जिससे दक्षता और विशेषज्ञता सुनिश्चित होती है। - नियमबद्धता (Rule Orientation):
नौकरशाही के सभी कार्य पूर्व निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होते हैं, जिससे तटस्थता और पारदर्शिता बनी रहती है। - निरपेक्षता (Impersonality):
नौकरशाही के सदस्य व्यक्तिगत भावनाओं और पक्षपात से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। - चयन प्रक्रिया (Merit-based Recruitment):
नौकरशाही में पदों पर नियुक्ति योग्यता, प्रतियोगिता और तकनीकी दक्षता के आधार पर की जाती है। - पद स्थायित्व (Job Security):
नौकरशाही में कर्मचारियों को स्थायित्व प्राप्त होता है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। - लिखित अभिलेख (Written Documentation):
प्रत्येक कार्य का लेखा-जोखा बनाए रखना अनिवार्य होता है, जिससे जवाबदेही और सूचना का प्रवाह सुगम होता है।
नौकरशाही एक ऐसी प्रशासनिक संरचना है जो संगठनात्मक कार्यों को कुशल, व्यवस्थित और निष्पक्ष ढंग से संचालित करने में सहायक होती है।
vmou MASO-06 paper , vmou ma final year exam paper ,vmou exam paper 2030 vmou exam paper 2028-29 vmou exam paper 2027 vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4
VMOU EXAM PAPER