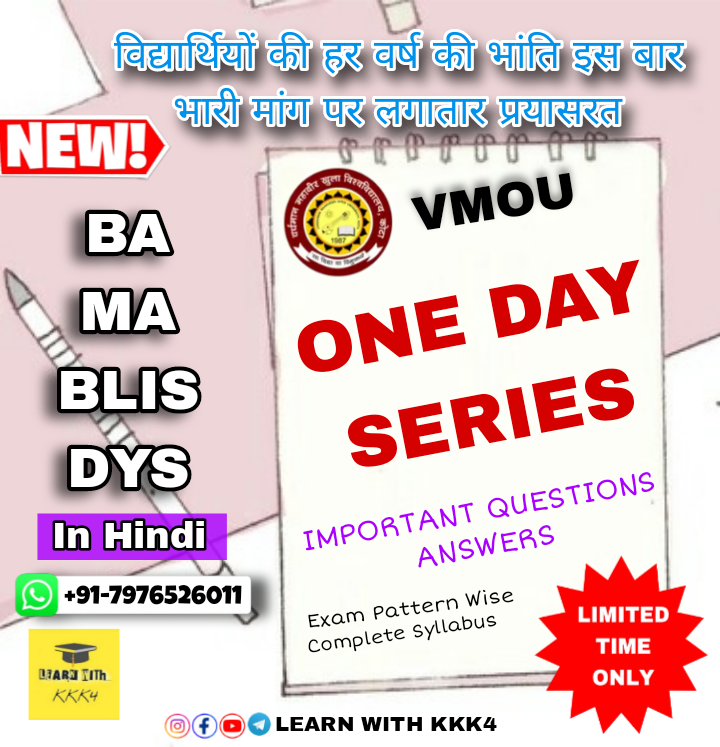VMOU MAGE-07 Paper MA Final Year ; vmou exam paper
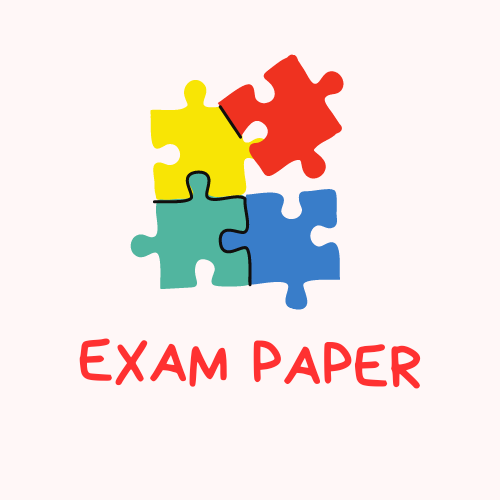
VMOU MA Final Year के लिए GEOGRAPHY ( MAGE-07 , कृषि भूगोल (geography of agriculture) ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.कृषि को एक आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- कृषि एक आर्थिक क्रिया है जिसमें भूमि, श्रम और पूंजी के माध्यम से खाद्य व कच्चे माल का उत्पादन कर आय एवं रोजगार प्राप्त किया जाता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.Dispersal of Agriculture (कृषि का प्रसरण)
उत्तर:- कृषि का प्रसरण मानव सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी, जलवायु व सांस्कृतिक कारणों से हुआ, जिससे विविध कृषि प्रणालियाँ विकसित हुईं।
प्रश्न-3.Loess Soil (वेबस मृदा):
उत्तर:- यह एक प्रकार की महीन, पीली-भूरे रंग की जलोढ़ मृदा है जो पवन द्वारा जमा होती है और कृषि के लिए उपजाऊ होती है।
प्रश्न-4. Shifting Agriculture (स्थानान्तरित कृषि):
उत्तर:- ह एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसमें भूमि को कुछ समय तक उपयोग के बाद छोड़कर नई भूमि पर कृषि की जाती है, जैसे झूम खेती।
प्रश्न-5. कृषि भूगोल का विषय-क्षेत्र (Scope of Agricultural Geography):
उत्तर:- कृषि भूगोल कृषि की प्रकृति, वितरण, उत्पादन, विपणन एवं कृषक की सामाजिक-आर्थिक दशा का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है।
प्रश्न-6. कृषि प्रादेशीकरण क्या है ?
उत्तर:- कृषि प्रादेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और सामाजिक-आर्थिक दशाओं के आधार पर कृषि की प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया जाता है।
प्रश्न-7. कृषि भूगोल का अर्थ (Meaning of Agricultural Geography):
उत्तर:- यह भूगोल की वह शाखा है जो कृषि क्रियाओं, कृषि उत्पादन व उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन पर्यावरणीय एवं मानव कारकों के संदर्भ में करती है।
प्रश्न-8. सिंचाई की सघनता (Intensity of Irrigation):
उत्तर:- किसी क्षेत्र में कुल सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोये गए क्षेत्रफल से अनुपात सिंचाई की सघनता कहलाता है, जो कृषि विकास का संकेतक होता है
प्रश्न-9. भूमि काश्तकारी (Land Tenancy):
उत्तर:- जब कोई कृषक भूमि का स्वामी न होकर किराये पर भूमि लेकर खेती करता है, तो उसे काश्तकारी या पट्टेदारी व्यवस्था कहा जाता है।
प्रश्न-10. White Revolution (श्वेत क्रांति):
उत्तर:- यह भारत में दुग्ध उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया थी, जिससे देश दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना।
प्रश्न-11. जल गुणवत्ता मानक (Water Quality Criteria):
उत्तर:- फसल की उत्पादकता हेतु जल की भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों की स्वीकृत सीमाएँ जल गुणवत्ता मानक कहलाती हैं।
प्रश्न-12. भूमि उपयोग के आंकड़ों के स्रोत (Sources of Landuse Data):
उत्तर:- भूमि उपयोग के आंकड़े भू-रिकॉर्ड, उपग्रह चित्रण, सर्वेक्षण रिपोर्ट, कृषिआंकड़े निदेशालय व राज्य राजस्व विभागों से प्राप्त होते हैं।
प्रश्न-13 भूमि उपयोग की संकल्पना को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- भूमि उपयोग से तात्पर्य उस तरीके से है जिससे मनुष्य विभिन्न गतिविधियों के लिए भूमि का उपयोग करता है, जैसे कृषि, उद्योग, आवास, वन आदि।
प्रश्न-14. Economic Rent (आर्थिक लगान):
उत्तर:- यह भूमि उपयोग से प्राप्त वह अतिरिक्त लाभ है जो भूमि की विशेषता या स्थिति के कारण होता है।
प्रश्न-15. Agroecology (कृषि पारिस्थितिकी):
उत्तर:- यह कृषि को पर्यावरणीय सिद्धांतों के साथ जोड़कर स्थायी उत्पादन सुनिश्चित करने वाली प्रणाली है।
प्रश्न-16 केन्डाल की शस्य संयोजन विधि (Kendal’s Method of Crop Combination):
उत्तर:- केन्डाल ने क्षेत्र में प्रमुख फसलों के प्रतिशत के आधार पर सांख्यिकीय विधि द्वारा शस्य संयोजन का निर्धारण किया।
प्रश्न-17. Commodity Approach (जिंसवार उपागम):(अस्तुपरक उपागम)
उत्तर:-यह उपागम कृषि का अध्ययन विशिष्ट फसल या उत्पाद के आधार पर करता है, जिससे उत्पादन, वितरण व विपणन की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है।यह उपागम कृषि के अध्ययन में विशिष्ट जिंसों (जैसे गेहूं, धान) के उत्पादन, वितरण और व्यापार पर केंद्रित होता है।
प्रश्न-18. कृषि प्रदेश को परिभाषित कीजिए (Define Agricultural Region):
उत्तर:- ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ समान जलवायु, मृदा, फसल-पद्धति एवं कृषि गतिविधियाँ पाई जाती हैं, उसे कृषि प्रदेश कहते हैं।
प्रश्न-19. राजकीय कृषि।
उत्तर:- राजकीय कृषि वह व्यवस्था है जिसमें भूमि सरकार के स्वामित्व में होती है और कृषि कार्य राज्य द्वारा नियोजित कर्मचारियों के माध्यम से किया जाता है।
प्रश्न-20. Cropping Pattern (फसल प्रारूप):
उत्तर:- फसल प्रारूप का अर्थ है किसी क्षेत्र में विभिन्न ऋतुओं में बोई जाने वाली फसलों का क्रम, जो जलवायु, मिट्टी व सिंचाई पर निर्भर करता है।
प्रश्न-21. Land Capability (भू-क्षमता):
उत्तर:- किसी भूमि की कृषि योग्य उपयोगिता को भू-क्षमता कहते हैं, जो मिट्टी, ढाल, जलवायु और जल उपलब्धता पर आधारित होती है।
प्रश्न-22. Size of Holding (जोत का आकार):
उत्तर:- जोत का आकार किसी किसान के स्वामित्व या उपयोग की भूमि को दर्शाता है, जो कृषि उत्पादन, यांत्रिकीकरण और लाभप्रदता को प्रभावित करता है।
प्रश्न-23. Sources of Agricultural Data (कृषि आंकड़ों के स्रोत):
उत्तर:- कृषि आंकड़ों के मुख्य स्रोत जनगणना, कृषि सर्वेक्षण, सैटेलाइट चित्रण, मंडी रिपोर्ट और सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट हैं।
प्रश्न-24. शस्य विविधता।
उत्तर:- शस्य विविधता वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिससे जोखिम कम होता है और आय के स्रोत बढ़ते हैं।
प्रश्न-25. Crop Balance (शस्य संतुलन):
उत्तर:- फसल संतुलन वह स्थिति है जहाँ विभिन्न फसलों का उत्पादन क्षेत्रीय आवश्यकताओं और पोषण संतुलन के अनुसार संतुलित रूप से किया जाता है।
प्रश्न-26. Crop Concentration (शस्य सघनता):
उत्तर:- किसी विशेष क्षेत्र में एक या कुछ फसलों की सघनता को शस्य सघनता कहते हैं, जिससे कृषि विविधता में कमी और उत्पादन में विशेषीकरण देखा जाता है।
प्रश्न-27. कृषि भूमि उपयोग में प्रतिमानों की आवश्यकता।
उत्तर:- कृषि भूमि उपयोग में प्रतिमान आवश्यक हैं क्योंकि ये वैज्ञानिक निर्णय लेने, संसाधनों के उचित प्रबंधन और भूमि की दीर्घकालिक उपज क्षमता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं।
प्रश्न-28. भूमि उपयोग सर्वेक्षण हेतु नियोजन।
उत्तर:- भूमि उपयोग सर्वेक्षण हेतु नियोजन में उद्देश्यों की परिभाषा, तकनीकों का चयन, डाटा संग्रह और विश्लेषण की रणनीति बनाना शामिल होता है ताकि भूमि का उचित उपयोग हो सके।
प्रश्न-29. Sustainable Development in Agriculture (कृषि में सतत् विकास):
उत्तर:- सतत कृषि विकास का अर्थ है ऐसी कृषि पद्धतियाँ अपनाना जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए दीर्घकालीन उत्पादन व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें।
प्रश्न-30. Critical Values (क्रांतिक मूल्य):
उत्तर:- कृषि में ये वे सीमांत मूल्य होते हैं, जिनसे नीचे जाने पर फसल की वृद्धि और उत्पादन प्रभावित होने लगता है, जैसे नमी या पोषक तत्व।
प्रश्न-31. Agricultural Efficiency (कृषि दक्षता):
उत्तर:- कृषि दक्षता भूमि, श्रम व पूंजी के न्यूनतम उपयोग से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की क्षमता है, जो तकनीक व प्रबंधन से बढ़ाई जा सकती है।
प्रश्न-32. Land Reforms (भूमि सुधार):
उत्तर:- भूमि सुधार का उद्देश्य भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना, जोत सीमा तय करना और भूमि का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना होता है।
प्रश्न-33. Cropping Intensity (शस्य गहनता):
उत्तर:- यह प्रति वर्ष एक खेत में बोई गई फसलों की संख्या को दर्शाता है, जितनी अधिक बार फसल बोई जाती है, शस्य गहनता उतनी ही अधिक होती है।
प्रश्न-34. Terra Rossa:
उत्तर:- यह लाल रंग की चूना-पत्थर से बनी उपजाऊ मिट्टी होती है, जो भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अंगूर जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है।
प्रश्न-35. ICRISAT (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.):
उत्तर:- यह “International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics” है, जो अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसलों पर अनुसंधान करता है।
प्रश्न-36. Agriculture Land Use (कृषि भूमि उपयोग):
उत्तर:- यह भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए करने की प्रक्रिया है, जिसमें फसलें उगाना, चरागाह, बागवानी और वानिकी शामिल होते हैं।
Section-B
प्रश्न-1.कृषि भूगोल के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- कृषि भूगोल एक विशिष्ट भूगोल शाखा है, जिसका विकास 20वीं शताब्दी में तीव्र गति से हुआ। प्रारंभ में यह विषय केवल कृषि गतिविधियों के वितरण और प्रकारों पर केंद्रित था, परंतु समय के साथ इसमें तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं का समावेश हुआ। प्रथम चरण में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लाश ने कृषि को मानव और प्रकृति के संबंधों का उदाहरण बताया। 1920 के दशक में अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने कृषि क्षेत्रों की पहचान की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कृषि भूगोल ने मात्रात्मक तकनीकों और स्थूल विश्लेषण को अपनाया। इस विषय में वॉन थ्यूनन, जे.एच. ग्रेगोरी, व्हिटलेसी जैसे विद्वानों का विशेष योगदान रहा। आज कृषि भूगोल में जलवायु, मृदा, सिंचाई, बाजार, नीति और वैश्वीकरण जैसे अनेक घटकों का समावेश होता है, जिससे यह अधिक बहुआयामी और व्यावहारिक बन गया है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.फसल विविधीकरण एवं विशेषीकरण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- फसल विविधीकरण (Crop Diversification) का अर्थ है – एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करना। इसका उद्देश्य जोखिम को कम करना, भूमि का पूर्ण उपयोग करना और आय में वृद्धि करना होता है। यह प्रणाली विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ जलवायु विविधतापूर्ण होती है और बाजार की माँग बदलती रहती है।
फसल विशेषीकरण (Crop Specialization) का अर्थ है – किसी क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल पर विशेष ध्यान देना। उदाहरण के लिए पंजाब में गेहूं या महाराष्ट्र में गन्ने की विशेष खेती। इसका उद्देश्य अधिक उत्पादकता और तकनीकी दक्षता प्राप्त करना होता है।
अंतर यह है कि विविधीकरण में कई फसलें होती हैं जिससे जोखिम कम होता है, जबकि विशेषीकरण में केवल एक फसल पर निर्भरता अधिक होती है जिससे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता है। विविधीकरण सतत विकास के अनुकूल है जबकि विशेषीकरण बाजार केंद्रित होता है।
प्रश्न-3.भूमि वर्गीकरण की अमेरिकन व भारतीय विधियों में क्या अन्तर है ? भूमि वर्गीकरण की दोनों विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
उत्तर:- अमेरिकन विधि मुख्यतः भूमि की क्षमता (Land Capability) पर आधारित होती है। यह भूमि के ढाल, गहराई, जल निकासी, मृदा प्रकार, अपरदन की प्रवृत्ति आदि के आधार पर आठ श्रेणियों (Class I to VIII) में विभाजित करती है। यह प्रणाली कृषि योग्यता को दर्शाती है, जैसे कि Class I भूमि सभी प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जबकि Class VIII भूमि कृषि योग्य नहीं होती।
भारतीय विधि भूमि उपयोग की व्यावहारिकता और कृषकों की जरूरतों पर आधारित होती है। इसे भूमि उपयोग क्षमता सर्वेक्षण (Land Use Capability Survey) कहा जाता है। इसमें भूमि को कृषियोग्य, वानिकी, चारागाह एवं गैर-कृषि उपयोग हेतु वर्गीकृत किया जाता है। इसमें पारंपरिक जानकारी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं जलवायु को भी ध्यान में रखा जाता है।
इस प्रकार, अमेरिकन विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है जबकि भारतीय विधि स्थानीय आवश्यकताओं एवं व्यवहारिक पक्षों पर आधारित होती है।
प्रश्न-कृषि विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- कृषि विकास अनेक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले, जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसमें वर्षा, तापमान और धूप की मात्रा शामिल है। अनुकूल जलवायु फसल उत्पादन को बढ़ावा देती है। दूसरा कारक मिट्टी की उर्वरता है, जो अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। सिंचाई सुविधाएं भी विकास में बड़ी भूमिका निभाती हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अपर्याप्त होती है। प्रौद्योगिकी और यंत्रीकरण के विकास ने उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, बीजों की गुणवत्ता, उर्वरकों और कीटनाशकों की उपलब्धता भी कृषि को प्रभावित करते हैं। बाजार व्यवस्था, कृषि मूल्य नीति, और सरकारी सहायता जैसे संस्थागत कारक भी महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा, कृषि अनुसंधान, और परिवहन सुविधा भी कृषि विकास में सहायक हैं। अतः, कृषि विकास एक बहु-आयामी प्रक्रिया है, जो विभिन्न कारकों के परस्पर सहयोग से ही संभव है।
प्रश्न-5.कृषि को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- कृषि न केवल भौतिक कारकों पर निर्भर करती है, बल्कि सामाजिक कारक भी इसकी दिशा और दशा को प्रभावित करते हैं। प्रमुख सामाजिक कारकों में परंपराएं, जाति व्यवस्था, भूमि स्वामित्व का स्वरूप, परिवार की संरचना, शिक्षा का स्तर, सामाजिक संगठन तथा श्रम की उपलब्धता शामिल हैं। भारत जैसे देश में कई क्षेत्रों में कृषि तकनीकों में परिवर्तन सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं के कारण धीमा रहा है। किसान परिवारों में जोतों का विभाजन कृषि भूमि को छोटा करता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। जाति व्यवस्था भी कृषि कार्यों में विभाजन को निर्धारित करती है, जिससे सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। शिक्षा का अभाव आधुनिक तकनीकों को अपनाने में बाधा बनता है। साथ ही, सामाजिक संगठनों की भूमिका कृषक सहयोग, बीज वितरण, और बाजार उपलब्धता में महत्त्वपूर्ण होती है। अतः सामाजिक कारक कृषि के विकास में बाधा या सहयोग दोनों रूपों में कार्य करते हैं।
प्रश्न-6. कृषि को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- कृषि पर अनेक आर्थिक कारकों का सीधा प्रभाव पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक भूमि की उपलब्धता और जोत का आकार है; बड़ी जोतों पर आधुनिक कृषि करना सरल होता है। बाजारों की निकटता भी कृषि को प्रभावित करती है क्योंकि उत्पादों को बेचने की सुविधा मिलती है। मूल्य निर्धारण नीति, समर्थन मूल्य तथा कृषि बीमा जैसी सरकारी योजनाएँ किसानों को प्रोत्साहित करती हैं। सिंचाई, खाद, बीज, मशीनरी जैसी आदानों की उपलब्धता और उनकी कीमतें भी कृषि को प्रभावित करती हैं। मजदूरी की दर और श्रमिकों की उपलब्धता से भी कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त कृषि ऋण और सहकारी संस्थाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक सहायता के बिना आधुनिक कृषि संभव नहीं है। इस प्रकार, आर्थिक कारक कृषि की दिशा, स्वरूप और उत्पादकता को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं।
प्रश्न-7.विश्व में कृषि की उत्पत्ति तथा उसके प्रसार पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- कृषि की उत्पत्ति मानव सभ्यता के विकास का आधार रही है। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण युग में मानव ने भोजन एकत्र करने के स्थान पर भोजन उत्पादन करना आरंभ किया। सबसे पहले कृषि की शुरुआत पश्चिमी एशिया के मेसोपोटामिया क्षेत्र में मानी जाती है, जहाँ गेहूं, जौ, मटर आदि की खेती की गई। इसके बाद मिस्र, सिंधु घाटी, चीन और मेक्सिको में स्वतंत्र रूप से कृषि का विकास हुआ।
प्रारंभ में कृषि वर्षा पर आधारित और सरल उपकरणों से की जाती थी। समय के साथ सिंचाई, हल, बैलों का उपयोग, खाद व बीजों में सुधार जैसी तकनीकों ने कृषि को उन्नत बनाया। कृषि का प्रसार व्यापार, उपनिवेशवाद, युद्ध, यात्राओं और प्रवास के माध्यम से हुआ। विशेषकर यूरोपीय देशों ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में कृषि विधियाँ फैलाईं।
आज कृषि का स्वरूप वैश्विक बन चुका है, जहाँ एक क्षेत्र की फसलें दूसरे क्षेत्रों में भी उगाई जाती हैं। इस प्रकार कृषि की उत्पत्ति और प्रसार ने मानव सभ्यता को स्थायित्व और सामाजिक विकास प्रदान किया।
प्रश्न-8.कृषि विकास को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों को समझाइए और भारत से उदाहरण दीजिए।
उत्तर:- कृषि विकास में भौतिक कारक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख भौतिक कारकों में जलवायु, मृदा, स्थलाकृति, जल की उपलब्धता एवं प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं।
जलवायु: तापमान और वर्षा कृषि की दिशा तय करते हैं। जैसे भारत में असम या पश्चिम बंगाल में अधिक वर्षा के कारण धान की खेती होती है जबकि पंजाब-हरियाणा में गेहूं।
मृदा: उपजाऊ मिट्टी जैसे काली मिट्टी कपास के लिए और जलोढ़ मिट्टी चावल-गेंहू के लिए उपयुक्त है। उदाहरणतः महाराष्ट्र में काली मिट्टी कपास की खेती को बढ़ावा देती है।
स्थलाकृति: समतल भूमि कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जैसे गंगा का मैदानी भाग।
जल स्रोत: सिंचाई की उपलब्धता कृषि को प्रभावित करती है। जैसे पंजाब में भाखड़ा नांगल जैसे बाँधों ने सिंचाई सुविधा दी।
प्राकृतिक आपदाएँ: बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि कृषि को नुकसान पहुँचाते हैं।
प्रश्न-9. ब्रिटेन और अमेरिका के भूमि उपयोग वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- ब्रिटेन में भूमि उपयोग का वर्गीकरण मुख्यतः निम्न प्रकार से किया गया है:
- कृषि भूमि (Arable Land)
- चारागाह भूमि (Pasture Land)
- वन भूमि (Forests)
- नगरीय क्षेत्र (Urban Land)
- अनुपयुक्त भूमि (Waste Land)
ब्रिटेन में उच्च घनत्व वाली आबादी के कारण कृषि भूमि सीमित है, परन्तु अत्यधिक यंत्रीकृत है। चारागाहों का उपयोग पशुपालन के लिए होता है।
अमेरिका में भूमि उपयोग अधिक विविध और क्षेत्रीय है:
- विस्तृत कृषि क्षेत्र (Commercial Farmland)
- रैंचिंग भूमि (Ranching Land)
- वन क्षेत्र (Forests)
- नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र
- संरक्षण क्षेत्र (Protected Areas)
अमेरिका में भूमि का उपयोग अधिक यंत्रीकृत, व्यापारिक और निर्यातोन्मुखी होता है। वहाँ कृषि के बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रवृत्ति है, जबकि ब्रिटेन में सीमित भूमि का अधिकतम उपयोग किया जाता है।
प्रश्न-10.भूमि उपयोग के आँकड़ों के प्रकार एवं उनके मानचित्रण की समस्याओं का परीक्षण कीजिए।
उत्तर:- भूमि उपयोग के आंकड़ों को विभिन्न आधारों पर एकत्रित किया जाता है, जैसे—प्रशासनिक अभिलेख, उपग्रह चित्र, जनगणना, और क्षेत्रीय सर्वेक्षण। प्रमुख प्रकार हैं:
(1) कृषि भूमि आंकड़े
(2) वन भूमि आंकड़े
(3) शहरी/आवासीय आंकड़े
(4) औद्योगिक उपयोग आंकड़े
(5) बंजर और अनुपयुक्त भूमि
मानचित्रण की समस्याएँ:
आंकड़ों की अद्यतनता की कमी
मापन विधियों की असमानता
स्थानिक विस्तार का अभाव
GIS और रिमोट सेंसिंग तकनीक की सीमित पहुँच
मानव संसाधन और विशेषज्ञों की कमी
इन समस्याओं को सुलझाने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण, मानकीकरण, और सटीक डेटा संग्रहण प्रणाली की आवश्यकता है। सही मानचित्रण से भूमि योजना और कृषि विकास को दिशा दी जा सकती है।
प्रश्न-11. कृषि में सिंचाई, मशीनीकरण एवं उर्वरकों की भूमिका को सुस्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- सिंचाई, मशीनीकरण एवं उर्वरक कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के प्रमुख साधन हैं। सिंचाई के माध्यम से फसलों को आवश्यक जल उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वर्षा पर निर्भरता कम होती है और बहुफसली प्रणाली अपनाई जा सकती है। भारत में नहरें, ट्यूबवेल एवं जलाशयों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। मशीनीकरण कृषि कार्यों में समय और श्रम की बचत करता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि यंत्रों से भूमि की जुताई, बुवाई, सिंचाई और कटाई सरल हो जाती है। यह उत्पादन की लागत घटाने में सहायक है। उर्वरकों के प्रयोग से मृदा की उर्वरता बनाए रखी जाती है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। रासायनिक और जैविक उर्वरकों दोनों का संतुलित प्रयोग आवश्यक है। ये तीनों घटक मिलकर आधुनिक कृषि को सफल बनाते हैं और किसानों की आय में वृद्धि करते हैं।
प्रश्न-12. कृषि विकास के स्तरों के मापकों को समझाइये।
उत्तर:- कृषि विकास को मापने के लिए विभिन्न मापकों का उपयोग किया जाता है, जो कृषि की प्रगति और उत्पादकता को दर्शाते हैं। प्रमुख मापक निम्नलिखित हैं:
- फसल उत्पादकता – प्रति हेक्टेयर उपज कृषि विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है।
- सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत – अधिक सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र अधिक विकसित माने जाते हैं।
- उन्नत बीज और उर्वरकों का प्रयोग – इनके उपयोग की मात्रा कृषि प्रौद्योगिकी अपनाने का संकेत देती है।
- मशीनों का प्रयोग – ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि का उपयोग यंत्रीकरण को दर्शाता है।
- फसल विविधता – विविध फसलें और नकदी फसलों की उपस्थिति विकास का संकेत है।
- कृषि से आय का स्तर – प्रति कृषक औसत आय जितनी अधिक होगी, कृषि उतनी ही विकसित मानी जाएगी।
- बाजार और भंडारण की उपलब्धता – विकसित क्षेत्रों में विपणन व्यवस्था सशक्त होती है।
- सरकारी योजनाओं और सहायता की पहुँच – कृषि नीतियों का प्रभाव भी मापक होता है।
इन मापकों के आधार पर क्षेत्रीय कृषि विकास की तुलना की जाती है।
प्रश्न-13. कृषि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- कृषि के प्रकार प्राकृतिक दशाओं, संसाधनों की उपलब्धता और सामाजिक-आर्थिक कारकों पर निर्भर करते हैं। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:
पारिस्थितिक कृषि (Organic Farming) – इसमें रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है।
परम्परागत कृषि – यह आदिकालीन कृषि प्रणाली है जिसमें पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग होता है।
व्यावसायिक कृषि – इसमें कृषि एक व्यवसाय की तरह की जाती है, जैसे गेहूं, कॉफी आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन।
संवहन कृषि (Subsistence Farming) – इसमें उत्पादन केवल परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है।
सघन कृषि – सीमित भूमि में अधिक श्रम और पूंजी लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया।
विशेषीकृत कृषि – इसमें कोई एक ही फसल या उत्पादन जैसे डेयरी, फल, फूल आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
शिफ्टिंग कृषि – इसमें भूमि को कुछ वर्षों के बाद बदल दिया जाता है, जैसे झूम खेती।
प्रश्न-14. कृषि भूगोल के अध्ययन के क्रमबद्ध दृष्टिकोण पर संक्षेप में लिखिए।
उत्तर:- कृषि भूगोल के अध्ययन में क्रमबद्ध दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक विधि है, जिसमें कृषि क्रियाओं का विश्लेषण विभिन्न घटकों के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टिकोण में पहले उद्देश्य की पहचान की जाती है, फिर डाटा संग्रह, वर्गीकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें जलवायु, मृदा, फसल प्रकार, कृषि प्रणाली, उत्पादन और विपणन जैसे तत्वों का गहन अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण में स्थानिक वितरण के साथ-साथ कृषि के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार, यह दृष्टिकोण कृषि भूगोल को केवल वर्णनात्मक न बनाकर एक विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक विषय बनाता है। इससे कृषि के क्षेत्रीय स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है।
प्रश्न-15. भूमि वर्गीकरण के भारतीय प्रारूप की आवश्यकता तथा आधार की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- भारत जैसे विविध भौगोलिक देश में भूमि का वैज्ञानिक वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है ताकि भूमि का प्रभावी, संतुलित और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित हो सके। भूमि की उत्पादकता, उपयोग क्षमता, और पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रारूप अपनाया गया है।
आवश्यकता:
भूमि का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित करना
भूमि क्षरण रोकना
कृषि विकास और योजना बनाना
जलवायु के अनुसार फसल चयन करना
आधार:
(1) भौगोलिक स्थिति
(2) मृदा प्रकार एवं संरचना
(3) जल उपलब्धता
(4) ढाल और ऊँचाई
(5) पारिस्थितिकीय विशेषताएँ
भारत में आठ श्रेणियों का भूमि वर्गीकरण किया गया है जैसे—खेती योग्य, वन भूमि, चारागाह, बंजर आदि। यह वर्गीकरण भूमि उपयोग नियोजन में सहायक होता है।
प्रश्न-16. भूमि उपयोग नियोजन के लिये भूमि वर्गीकरण आवश्यक है।’ वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भूमि उपयोग नियोजन किसी क्षेत्र की भूमि का अधिकतम, संतुलित और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। यह कार्य तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक भूमि का उचित वर्गीकरण न हो। भूमि वर्गीकरण का अर्थ है – भूमि को उसकी भौतिक, रासायनिक और उपयोगिता विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बाँटना। इससे यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि कौन-सी भूमि कृषि, वन, चारागाह, बस्ती, उद्योग या संरक्षण हेतु उपयुक्त है। बिना वर्गीकरण के भूमि का अनियोजित उपयोग होता है जिससे मृदा अपरदन, उपज में कमी, और पर्यावरणीय क्षरण जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। भूमि उपयोग नियोजन के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जा सकता है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार, भूमि वर्गीकरण एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, जिस पर टिकाऊ और समावेशी भूमि उपयोग नियोजन आधारित होता है।
प्रश्न-17. भूमि उपयोग सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं ? इसकी आवश्यकता, सिद्धान्त तथा योजना को समझाइए।
उत्तर:- भूमि उपयोग सर्वेक्षण (Landuse Survey) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में भूमि के विभिन्न प्रकारों—जैसे कृषि, वन, आवासीय, औद्योगिक आदि—के उपयोग की जानकारी एकत्र की जाती है। इसकी आवश्यकता इसलिए होती है ताकि भूमि के विवेकपूर्ण, न्यायसंगत एवं टिकाऊ उपयोग की योजना बनाई जा सके। यह सर्वेक्षण भूमि की उपलब्धता, गुणवत्ता, उपयोग की प्रवृत्ति एवं परिवर्तन को समझने में सहायक होता है।
मुख्य सिद्धांत:
(1) भूमि का वर्गीकरण उपयोग और क्षमता के अनुसार होना चाहिए।
(2) पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है।
(3) स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए।
(4) संसाधनों का संरक्षण और बहाल करना जरूरी है।
योजना के अंतर्गत:
भूमि मानचित्रण, GIS तकनीक का उपयोग, डाटा विश्लेषण, नीति निर्माण तथा क्षेत्रवार भूमि विकास योजनाएँ बनाई जाती हैं। इससे कृषि, उद्योग और आवासीय विकास संतुलित रूप से किया जा सकता है।
प्रश्न-18. भूमि उपयोग सर्वेक्षण की नीतियों एवं नियोजन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- भूमि उपयोग सर्वेक्षण कृषि और योजना निर्माण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि भूमि का कितना भाग किस प्रकार की गतिविधियों (जैसे कृषि, वानिकी, आवास, उद्योग) में उपयोग हो रहा है।
नीतियाँ:
भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए ‘राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति’ बनाई गई है, जिसमें भूमि की उचित वर्गीकृत जानकारी एकत्र कर उसे संतुलित और सतत विकास के लिए नियोजित करना मुख्य उद्देश्य है।
नियोजन:
भूमि उपयोग योजना में यह सुनिश्चित किया जाता है कि भूमि का सर्वाधिक उपयुक्त और टिकाऊ उपयोग हो। इसके अंतर्गत बंजर भूमि का विकास, अति उपयोग को रोकना, वनों का संरक्षण, शहरीकरण का नियमन आदि आते हैं।
GIS (Geographic Information System), रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके भूमि उपयोग की स्थिति को बेहतर समझा जाता है। भूमि उपयोग सर्वेक्षण दीर्घकालीन नीतिगत विकास और पर्यावरणीय संतुलन हेतु आधार प्रदान करता है।
प्रश्न-19. कृषि भूगोल में क्षेत्र सर्वेक्षण को समझाइए।
उत्तर:-क्षेत्र सर्वेक्षण कृषि भूगोल का एक महत्वपूर्ण तकनीकी पक्ष है, जिसमें किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की कृषि स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मृदा, जलवायु, जल स्रोत, फसलें, भूमि उपयोग, उत्पादन स्तर, श्रम व्यवस्था आदि तत्वों का प्रत्यक्ष निरीक्षण और डाटा संग्रह किया जाता है।
क्षेत्र सर्वेक्षण दो प्रकार का होता है: (1) प्राइमरी सर्वेक्षण – जिसमें प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र में जाकर जानकारी एकत्र की जाती है; और (2) सेकेंडरी सर्वेक्षण – जिसमें पुस्तकों, रिपोर्टों, आंकड़ों से जानकारी ली जाती है। इस प्रक्रिया में प्रश्नावली, साक्षात्कार, फोटो, मानचित्र आदि का उपयोग किया जाता है।
क्षेत्र सर्वेक्षण से क्षेत्र विशेष की कृषि की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे नीतियों के निर्माण, योजना-निर्माण और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है।
प्रश्न-20. विटलेसी के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- जे. एच. विटलेसी ने 1936 में कृषि के वैश्विक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया था। यह वर्गीकरण जलवायु, भूमि उपयोग, फसल विविधता, और सामाजिक-आर्थिक आधार पर आधारित था। प्रमुख कृषि प्रदेश निम्न हैं:
- नमी युक्त वाणिज्यिक कृषि क्षेत्र – अमेरिका, यूरोप आदि में।
- शुष्क क्षेत्र की वाणिज्यिक कृषि – जैसे गेहूं उत्पादन।
- शुष्क पशुपालन क्षेत्र – ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि।
- उष्णकटिबंधीय वाणिज्यिक कृषि – केले, कॉफी, गन्ना।
- धान उत्पादन क्षेत्र – दक्षिण-पूर्व एशिया।
- शिफ्टिंग कृषि क्षेत्र – अफ्रीका, भारत का उत्तर-पूर्व।
- बाजार बागवानी क्षेत्र – शहरों के समीप।
- सघन कृषक जीवन निर्वाह क्षेत्र – भारत, चीन।
- सघन कृषि – धान पर आधारित क्षेत्र
- सघन कृषि – गेहूं आधारित क्षेत्र
- नव उपनिवेश कृषि क्षेत्र
- चरागाह और वानिकी मिश्रित क्षेत्र
- मिश्रित कृषि क्षेत्र
विटलेसी का यह वर्गीकरण विश्व की कृषि प्रणालियों को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।
प्रश्न-21. कृषि अवस्थिति सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए। किसी एक कृषि अवस्थिति सिद्धान्त का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
उत्तर:- कृषि अवस्थिति सिद्धान्त यह स्पष्ट करते हैं कि कृषि क्रियाएँ किसी विशेष स्थान पर क्यों होती हैं और उनके वितरण का क्या तर्क है। ये सिद्धान्त भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारणों के आधार पर कृषि के स्थान निर्धारण को समझाते हैं।
मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:
- वॉन थ्यूनन का अवस्थिति सिद्धांत
- वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत (कृषि में आंशिक उपयोग)
- लोस्च का सिद्धांत
- क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत
वॉन थ्यूनन का सिद्धांत सर्वाधिक चर्चित है। इसके अनुसार यदि कोई एक बाजार शहर हो और चारों ओर एकसमान भौगोलिक दशाएँ हों, तो कृषि की भिन्न-भिन्न गतिविधियाँ उस बाजार से दूरी के अनुसार वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित होती हैं। बाजार के सबसे पास अधिक खराब होने वाले एवं अधिक परिवहन लागत वाली वस्तुएँ उगाई जाती हैं, जैसे सब्जियाँ व दुग्ध उत्पादन। दूरी बढ़ने पर अनाज, फिर पशुपालन और अंत में वानिकी होती है।
यह सिद्धांत परिवहन लागत और भूमि मूल्य के मध्य संबंध स्पष्ट करता है।
प्रश्न-22. शस्य संयोजन को स्पष्ट करते हुए उसकी विभिन्न विधियों को विवेचना कीजिए।
उत्तर:- शस्य संयोजन (Crop Combination) का अर्थ है – किसी क्षेत्र विशेष में एक साथ उगाई जाने वाली फसलों का समूह। यह अध्ययन कृषि भूगोल में महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह यह दर्शाता है कि कौन-सी फसलें किस क्षेत्र में कितनी मात्रा में एक साथ उगाई जाती हैं।
विधियाँ:
- वीवर की विधि (Weaver’s Method) – इसमें प्रत्येक फसल की वास्तविक क्षेत्रफल में भागीदारी को आँकड़ा बनाकर संयोजन ज्ञात किया जाता है।
- डोमिनेंस विधि – इसमें केवल उन्हीं फसलों को शामिल किया जाता है जिनका क्षेत्रफल कुल कृषि भूमि का न्यूनतम 10% हो।
- सिग्मा विधि (Sigma Method) – इसमें फसलों के मानक विचलन को आधार बनाकर संयोजन का निर्धारण होता है।
- बिना सीमा विधि (No Threshold Method) – इसमें सभी फसलों को बिना सीमा के शामिल किया जाता है।
शस्य संयोजन से कृषि योजनाएँ बनाने, उर्वरक व सिंचाई प्रबंधन करने और कृषि क्षेत्रीयता निर्धारित करने में मदद मिलती है
प्रश्न-23. कृषि में मृदा तथा जल के सन्तुलन के प्रभाव की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- कृषि उत्पादन में मृदा और जल का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। मृदा की उर्वरता, बनावट, संरचना और जैविक तत्व सीधे तौर पर फसल की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। यदि मृदा में नमी, पोषक तत्व या पीएच असंतुलन होता है तो फसल वृद्धि बाधित होती है। अत: मृदा परीक्षण और सुधार आवश्यक हैं।
इसी प्रकार जल संतुलन का भी अत्यधिक महत्व है। जल की कमी से सूखा और फसल हानि होती है जबकि अधिकता से जलभराव और मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संतुलित जल प्रबंधन में सिंचाई प्रणाली, जल संचयन, ड्रेनेज आदि शामिल हैं। यदि मृदा और जल का सही संतुलन स्थापित किया जाए तो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस संतुलन से खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और किसान की आय में वृद्धि संभव होती है।
प्रश्न-24. भारत के जल संसाधनों का मूल्यांकन कीजिए और इनकी कृषि से सम्बंधित प्रमुख समस्याओं को इंगित कीजिए।
उत्तर:- भारत में जल संसाधनों की कुल वार्षिक उपलब्धता लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर आँकी गई है, जिसमें से लगभग 1123 BCM उपयोगी जल है। प्रमुख जल स्रोत हैं – वर्षा, नदियाँ, भूजल और झीलें। भारत में सिंचाई हेतु सबसे अधिक निर्भरता भूजल पर है, विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में।
परंतु, जल संसाधनों से जुड़ी कृषि समस्याएं भी गंभीर हैं:
- वर्षा की अनिश्चितता – भारत में वर्षा मानसून पर आधारित है, जो असमान और अनिश्चित होती है।
- जलवायु परिवर्तन – इससे सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ी हैं।
- भूजल का अत्यधिक दोहन – कई क्षेत्रों में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है।
- सिंचाई संरचनाओं की कमी – छोटे किसानों को सिंचाई की सुविधाएं नहीं मिलती।
- जल प्रबंधन में असमानता – कुछ राज्यों में जल प्रचुर है तो कुछ में अत्यल्प।
- जल प्रदूषण – नदियों और जलाशयों में कृषि रसायनों के कारण जल गुणवत्ता घट रही है।
समाधान हेतु जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सूक्ष्म सिंचाई जैसे उपाय आवश्यक हैं।
प्रश्न-25. भारतीय कृषि की विशिष्ट समस्याओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। उन्हें दूर करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएँगे ?
उत्तर:- भारतीय कृषि अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख हैं:
(1) जोतों का अति-विखंडन
(2) सिंचाई की अपर्याप्तता
(3) पारंपरिक तकनीक का प्रयोग
(4) उर्वरकों और कीटनाशकों का असंतुलित प्रयोग
(5) विपणन की असुविधा
(6) ऋण भार
(7) भूमि अधिग्रहण और जलवायु परिवर्तन
समाधान हेतु सुझाव:
समेकित जोत योजना और भूमि सुधार
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रचार
किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण
कृषि ऋण पर रियायत और बीमा सुविधा
आधुनिक भंडारण और विपणन सुविधाएं
कृषि यंत्रीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा
इन उपायों से भारतीय कृषि को अधिक उत्पादनशील, टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सकता है।
प्रश्न-26. वान थ्यूनन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और इसकी कमियाँ बताइए।
उत्तर:- वान थ्यूनन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत 1826 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि कृषि क्रियाएं किसी शहर या बाजार के चारों ओर किस प्रकार स्थित होती हैं। उन्होंने छह वृत्ताकार क्षेत्रों की कल्पना की, जो उत्पादन लागत, परिवहन दूरी, भूमि किराया आदि पर आधारित थीं। पास के क्षेत्रों में सड़ी-गली वस्तुएँ जैसे दूध, सब्जियाँ होती हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में सस्ते, कम नाशवान उत्पाद जैसे अनाज।
आलोचनात्मक विश्लेषण:
यह सिद्धांत एक आदर्श स्थिति पर आधारित है, जहाँ एक एकल बाजार, समतल भूमि, समान परिवहन सुविधा, और एकरूप जलवायु की कल्पना की गई है।
कमियाँ:
- यह आधुनिक युग की जटिल बाजार व्यवस्था और बहु-केन्द्रीय नगरीय संरचना को नहीं दर्शाता।
- इसमें तकनीकी विकास और परिवहन साधनों के आधुनिकीकरण को नहीं जोड़ा गया।
- राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों की अनदेखी की गई है।
फिर भी, यह सिद्धांत कृषि अवस्थिति के अध्ययन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक प्रयास माना जाता है।
प्रश्न-27. आधुनिक साधनों एवं तकनीकी दृष्टि से सिंचाई पद्धति एवं तकनीक का विवरण दीजिए।
उत्तर:- आधुनिक युग में सिंचाई की पद्धतियों में कई नवीन तकनीकों का विकास हुआ है, जिससे जल की बचत एवं उत्पादन में वृद्धि संभव हुई है। प्रमुख आधुनिक सिंचाई तकनीकें निम्नलिखित हैं:
सौर ऊर्जा आधारित पंप: सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में लाभकारी हैं।
ड्रिप सिंचाई (बूँद-बूँद): यह विधि जल को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाती है। यह जल की अत्यधिक बचत करती है और शुष्क क्षेत्रों में उपयोगी है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसका प्रयोग हो रहा है।
स्प्रिंकलर सिंचाई: इसमें जल को पाइपों द्वारा छिड़काव के रूप में खेतों में फैलाया जाता है। यह असमतल भूमि पर प्रभावी है।
लाइनेयर मूविंग सिंचाई: इसमें एक चलती हुई पाइपलाइन द्वारा सिंचाई होती है, जो बड़े खेतों के लिए उपयुक्त है।
स्मार्ट सेंसर तकनीक: इससे मिट्टी में नमी की मात्रा मापी जाती है और उसी के अनुसार सिंचाई की जाती है।
प्रश्न-28. भारत से उदाहरण देते हुए कृषि पर जलवायु के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर:- जलवायु कृषि का प्रमुख निर्धारक तत्व है। भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है, इस कारण जलवायु में थोड़े से परिवर्तन से भी कृषि उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
उदाहरणस्वरूप, पंजाब और हरियाणा में अनुकूल जलवायु के कारण गेहूँ और धान की उपज अधिक होती है। वहीं राजस्थान में शुष्क जलवायु होने के कारण बाजरा और ग्वार जैसी शुष्क फसलें अधिक उगाई जाती हैं। पश्चिमी घाटों में अधिक वर्षा होने से वहाँ चाय, कॉफी और मसालों की खेती प्रमुख होती है।
इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, जैसे तापमान वृद्धि, वर्षा की अनिश्चितता, और सूखा या बाढ़ की घटनाएं कृषि उत्पादन को अस्थिर कर देती हैं। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र और कर्नाटक में अल्पवर्षा के कारण सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, जो कृषि पर जलवायु प्रभाव का ताज़ा उदाहरण है।
प्रश्न-29. विश्व में कृषि के प्रकार बताइए तथा बागानी कृषि का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
उत्तर:- विश्व में कृषि के कई प्रकार प्रचलित हैं, जो भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। प्रमुख प्रकार हैं:
(1) स्थानांतरित कृषि
(2) परंपरागत सब्सिस्टेंस कृषि
(3) गहन कृषि
(4) वाणिज्यिक कृषि
(5) बागानी या प्लांटेशन कृषि
(6) शुष्क कृषि
(7) मिश्रित कृषि
(8) डेयरी कृषि
(9) आर्गेनिक कृषि
बागानी कृषि (Plantation Agriculture) मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसमें एक ही प्रकार की फसल बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उद्देश्य से उगाई जाती है। यह आमतौर पर विदेशी निवेश, उन्नत तकनीक एवं संगठित श्रम पर आधारित होती है। प्रमुख फसलें—चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, नारियल, और तंबाकू होती हैं। भारत में असम और दार्जिलिंग में चाय बागान, कर्नाटक में कॉफी बागान प्रसिद्ध हैं।
प्रश्न-30. कृषि अवस्थिति मॉडल को समझाइए।
उत्तर:- कृषि अवस्थिति मॉडल (Agricultural Location Models) का उद्देश्य यह जानना है कि कृषि गतिविधियाँ किसी क्षेत्र में कहाँ और क्यों स्थित हैं। इनमें सबसे प्रमुख है वॉन थ्यूनन का अवस्थिति सिद्धांत।
वॉन थ्यूनन मॉडल (Von Thünen Model): यह मॉडल जर्मन अर्थशास्त्री वॉन थ्यूनन ने 1826 में प्रस्तुत किया। इसके अनुसार किसी नगर के चारों ओर कृषि क्रियाओं का वितरण परिवहन लागत और भूमि मूल्य के आधार पर विभिन्न वलयों में होता है:
- निकटतम क्षेत्र – डेयरी और फल-सब्जियाँ (जल्द खराब होने वाली वस्तुएं),
- दूसरा वलय – लकड़ी और ईंधन की फसलें,
- तीसरा वलय – अनाज फसलें,
- सबसे दूर – पशुपालन।
अन्य आधुनिक मॉडल जैसे लोश और क्रिस्टलर द्वारा भी अवस्थिति सिद्धांत दिए गए हैं, जो परिवहन, बाजार और लागत को आधार मानते हैं।
प्रश्न-31. भारत में कृषि प्रदेशों के परिसीमांकन में काम में ली गयी विधियों की सम्झाइए।
उत्तर:- भारत में कृषि प्रदेशों के परिसीमांकन (Delimitation) हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग किया गया है, जिससे देश को भिन्न-भिन्न कृषि विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया जा सके।
मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं:
- फसल संयोजन (Crop Combination) विधि: इसमें किसी क्षेत्र की प्रमुख फसलों का संयोजन निर्धारित कर कृषि प्रदेशों का विभाजन किया जाता है।
- शस्य सघनता (Crop Intensity) विधि: प्रति वर्ष प्रति क्षेत्र में ली जाने वाली फसलों की संख्या के आधार पर क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है।
- कृषि विशेषीकरण (Agricultural Specialization) विधि: इसमें देखा जाता है कि किस क्षेत्र में कौन-सी फसल प्रमुखता से उगाई जाती है।
- भौगोलिक विशेषताओं पर आधारित विधि: जलवायु, मिट्टी, वर्षा, तापमान आदि को ध्यान में रखकर प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है।
डॉ. लक्ष्मी नारायण और डॉ. शांतिलाल मेहता ने भारत को विभिन्न कृषि प्रदेशों में बाँटा है। इन विधियों से कृषि नीति निर्माण, सिंचाई योजना एवं क्षेत्रीय विकास में सहायता मिलती है।
प्रश्न-32. मृदा के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- मृदा वर्गीकरण का तात्पर्य मृदाओं को उनके रंग, बनावट, संरचना, जलधारण क्षमता एवं खनिज तत्वों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बाँटना है। भारत में मृदा का वर्गीकरण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार से किया गया है:
- जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil): गंगा-यमुना और ब्रह्मपुत्र घाटियों में पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ होती है।
- काली मृदा (Black Soil): महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आदि में पाई जाती है। यह कपास के लिए उपयुक्त होती है।
- लाल मृदा (Red Soil): दक्षिण भारत में पाई जाती है, इसमें लोहा अधिक होता है।
- जलोढ़ मृदा (Laterite Soil): भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, पोषक तत्व कम होते हैं।
- रेतीली मृदा (Desert Soil): राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाती है, जलधारण क्षमता कम होती है।
- पर्वतीय मृदा (Mountain Soil): हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, बागवानी के लिए उपयुक्त।
मृदा वर्गीकरण से फसल चयन, उर्वरक प्रबंधन और भूमि सुधार में सहायता मिलती है।
प्रश्न-33. सामान्य भूमि उपयोग के विधितंत्र की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- सामान्य भूमि उपयोग (General Land Use) के विधितंत्र का उद्देश्य यह जानना है कि भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है और उसमें कौन-कौन से घटक सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा छह प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत भूमि उपयोग का वर्गीकरण किया जाता है:
- वन क्षेत्र (Forest Area),
- कृषि योग्य भूमि (Net Sown Area),
- बंजर एवं अनुपयुक्त भूमि,
- चारागाह एवं अन्य वृक्षारोपण क्षेत्र,
- गैर-कृषि उपयोग की भूमि,
- कृषि के लिए बार-बार प्रयुक्त भूमि।
इन श्रेणियों को निर्धारित करने हेतु उपग्रह चित्रण, भूमि अभिलेख, सर्वेक्षण, और GIS तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भूमि उपयोग योजनाओं के लिए भू-संवेदन (Remote Sensing), मानचित्रण और सांख्यिकीय तकनीकों का विशेष योगदान है।
सामान्य भूमि उपयोग विधि से संसाधनों की बेहतर योजना और सतत विकास की रणनीति बनाई जा सकती है।
प्रश्न-34. कृषि उत्पादकता एवं दक्षता मापने की समस्याओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- कृषि उत्पादकता मापना एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि यह अनेक कारकों पर निर्भर करती है – जैसे भूमि की गुणवत्ता, तकनीक, जलवायु, श्रम, बीज, उर्वरक आदि। प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं:
- विविधता: विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु, मृदा और कृषि विधियों में विविधता के कारण उत्पादकता की तुलना कठिन होती है।
- माप की इकाइयाँ: कहीं प्रति हेक्टेयर उपज को मापा जाता है, तो कहीं कुल उत्पादन को, जिससे तुलनात्मक विश्लेषण कठिन होता है।
- तकनीकी अंतर: परंपरागत और आधुनिक कृषि विधियों में अंतर के कारण दक्षता में भारी अंतर होता है।
- प्राकृतिक आपदाएं: सूखा, बाढ़ आदि जैसे कारक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जिससे माप में भिन्नता आती है।
- आंकड़ों की कमी: विश्वसनीय व अद्यतन आंकड़ों का अभाव उत्पादकता के सही मूल्यांकन में बाधा है।
इसलिए कृषि उत्पादकता की सटीक माप के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण और मानकीकृत मापदंडों की आवश्यकता है।
प्रश्न-35. फसल संयोजन प्रदेश निर्धारण की विधियों व तकनीक को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- फसल संयोजन (Crop Combination) का अर्थ है किसी क्षेत्र में एक साथ उगाई जाने वाली फसलों का समूह। इन संयोजनों को जानना कृषि क्षेत्र नियोजन, विपणन एवं नीतिगत निर्णयों में सहायक होता है।
फसल संयोजन क्षेत्र निर्धारण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं:
- विवरणात्मक विधि (Descriptive Method): इसमें क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों को सूचीबद्ध किया जाता है।
- वीन्स विधि (Weaver’s Method): यह सांख्यिकीय विधि है जिसमें प्रत्येक फसल के क्षेत्रफल का कुल कृषि भूमि से प्रतिशत निकाला जाता है। इससे डॉमिनेंट फसलें और संयोजन की पहचान होती है।
- डेंटीग विधि (Doi’s Method): यह रेखीय संयोजन सूचकांक (Index) के आधार पर कार्य करती है।
इन विधियों से फसल विविधता, फसल चक्र, और भूमि उपयोग क्षमता का विश्लेषण किया जा सकता है।
प्रश्न-36. उदाहरण देते हुए कृषि दक्षता तथा उत्पादकता की अवधारणा की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- कृषि दक्षता (Agricultural Efficiency) और कृषि उत्पादकता (Agricultural Productivity) दो अलग अवधारणाएँ हैं, जो कृषि विकास को मापने के लिए उपयोग होती हैं।
कृषि दक्षता का अर्थ है – उपलब्ध संसाधनों (भूमि, जल, श्रम, पूंजी) का अधिकतम लाभकारी उपयोग करना। इसमें उत्पादन लागत कम एवं लाभ अधिक होता है। उदाहरणतः – पंजाब में उन्नत यंत्रों और सिंचाई व्यवस्था से गेहूँ की खेती अत्यधिक दक्षता के साथ होती है।
कृषि उत्पादकता से आशय है – प्रति इकाई क्षेत्र (जैसे प्रति हेक्टेयर) में होने वाला कृषि उत्पादन। यह केवल उत्पादन की मात्रा को मापती है, न कि संसाधनों के उपयोग को। उदाहरण के लिए, केरल में प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन पश्चिमी राजस्थान से अधिक है, इसलिए उसकी उत्पादकता अधिक है।
दक्षता एवं उत्पादकता दोनों ही कृषि नीति, खाद्य सुरक्षा, आय व समृद्धि से जुड़ी हैं। इनसे यह तय होता है कि कृषि क्षेत्र किस हद तक लाभकारी एवं विकासशील है।
प्रश्न-37. भूमिस्वामित्व का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- भूमिस्वामित्व (Land Tenure) का अर्थ भूमि के स्वामित्व, अधिकार, नियंत्रण और उपयोग के नियमों से है। यह प्रणाली यह निर्धारित करती है कि कौन भूमि का मालिक है, उसे कैसे उपयोग किया जा सकता है, और कौन-से अधिकार उस पर लागू होते हैं।
भारत में पारंपरिक रूप से तीन प्रकार की भूमिस्वामित्व प्रणालियाँ रही हैं:
- जमींदारी प्रणाली: इसमें जमींदार भूमि का मालिक होता था और किसान उससे किराया देता था।
- रैयतवारी प्रणाली: इसमें किसान ही भूमि का स्वामी होता था और सीधे सरकार को लगान देता था।
- महलवारी प्रणाली: भूमि का स्वामित्व ग्राम समुदाय के पास होता था और लगान सामूहिक रूप से दिया जाता था।
भूमि सुधारों के बाद स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तन हुआ। भूमि छीनने, बंटवारे, किरायेदारी और सीमित जोत की समस्याएँ आज भी कई क्षेत्रों में बनी हुई हैं। भूमिस्वामित्व प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित करती है।
Section-C
प्रश्न-1.कृषि उद्भव एवं प्रसरण का विस्तार से विवरण दीजिए।/कृषि उद्भव एवं प्रसार का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
उत्तर:- कृषि मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसका उद्भव लगभग 10,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ माना जाता है। कृषि की उत्पत्ति ने मानव को एक स्थान पर बसने, स्थायी बस्तियाँ बसाने और समाज का निर्माण करने का अवसर दिया। यह परिवर्तन शिकारी-संग्रहकर्ता जीवन से स्थायी कृषक समाज की ओर बढ़ने का प्रतीक था।
कृषि का उद्भव:
कृषि का उद्भव विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्र रूप से हुआ। इसके प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं:
- प्राचीन निकट पूर्व (फर्टाइल क्रेसेंट): वर्तमान ईरान, इराक, सीरिया क्षेत्र में गेहूं, जौ, मटर आदि की खेती शुरू हुई।
- चीन: यहाँ चावल और बाजरे की खेती प्रारंभ हुई।
- दक्षिण अमेरिका: एंडीज़ क्षेत्र में मक्का, आलू, मिर्च आदि की खेती हुई।
- भारत: सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं, जौ, कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
- अफ्रीका: सहारा के दक्षिणी भाग में ज्वार, बाजरा जैसे अनाजों की खेती शुरू हुई।
कृषि का प्रसरण:
कृषि का प्रसरण दो प्रकार से हुआ –
- संस्कृति प्रसार (Diffusion): जब कृषक समुदायों का अन्य क्षेत्रों में विस्तार हुआ और उन्होंने वहां के लोगों को कृषि के तौर-तरीके सिखाए।
- स्वतंत्र विकास: कुछ क्षेत्रों में स्थानीय पर्यावरण और वनस्पति के आधार पर स्वतंत्र रूप से कृषि पद्धतियाँ विकसित हुईं।
प्रसरण के मार्ग:
भारत में कृषि पश्चिम से फर्टाइल क्रेसेंट क्षेत्र से सिंधु घाटी के माध्यम से पहुँची।
चीन से धान की खेती दक्षिण पूर्व एशिया में फैली।
अमेरिका से मक्का, आलू, टमाटर आदि की खेती यूरोप व एशिया में पहुँची।
कृषि के विकास के चरण:
शुरुआती चरण: छोटे पैमाने पर अनाजों की खेती और पालतू पशु।
स्थायी कृषि: हल चलाना, सिंचाई और बीज चयन तकनीकें विकसित हुईं।
व्यावसायिक कृषि: अधिशेष उत्पादन, बाजार व्यवस्था और कृषि यंत्रीकरण का विकास।
इस प्रकार कृषि का उद्भव और प्रसरण मानव सभ्यता के विकास में एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने मानव जीवन की दिशा और संरचना को परिवर्तित कर दिया।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.व्हिटल्सी द्वारा दिए गए ‘विश्व की कृषि प्रणालियों’ की विवेचना कीजिए और उनमें से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- जॉन व्हिटल्सी (John Whittlesey) ने 1936 में “Agricultural Systems of the World” नामक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने जलवायु, भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक परंपराएं, तकनीकी स्तर और भूमि उपयोग के आधार पर विश्व की कृषि को पांच व्यापक श्रेणियों और 13 उपप्रणालियों में विभाजित किया। यह वर्गीकरण कृषि के भौगोलिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।
व्हिटल्सी की 13 कृषि प्रणालियाँ इस प्रकार हैं:
- नामाडिक हर्डिंग (Nomadic Herding)
- शिफ्टिंग कल्टीवेशन (Shifting Cultivation)
- रैन्चिंग (Livestock Ranching)
- सेडेंटरी इंटेंसिव राइस कल्टीवेशन (Intensive Subsistence – Rice)
- सेडेंटरी इंटेंसिव नॉन-राइस कल्टीवेशन (Intensive Subsistence – Non-Rice)
- प्लांटेशन कृषि (Plantation Agriculture)
- मिश्रित कृषि (Mixed Farming)
- डेयरी फार्मिंग (Dairy Farming)
- व्यावसायिक अनाज कृषि (Commercial Grain Farming)
- भूमध्यसागरीय कृषि (Mediterranean Agriculture)
- हॉर्टिकल्चर (Market Gardening and Truck Farming)
- वाइन कल्टीवेशन
- स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर और अन्य कृषि
- स्थानांतरित कृषि (Shifting Cultivation):
यह प्रणाली मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में पाई जाती है जैसे अमेज़न बेसिन, अफ्रीका के कुछ भाग और पूर्वोत्तर भारत। इसमें किसान वन भूमि को काटकर जला देते हैं और राख की उर्वरता का उपयोग कर कुछ वर्षों तक खेती करते हैं। फिर भूमि को छोड़कर अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं।
विशेषताएँ:
सरल औजारों का उपयोग।
पारंपरिक ज्ञान पर आधारित।
उत्पादन स्वयं की आवश्यकता के लिए।
भूमि पर अत्यधिक दबाव और वनों की क्षति।
- प्लांटेशन कृषि (Plantation Agriculture):
यह व्यावसायिक और निर्यातमुखी कृषि प्रणाली है जिसमें एक ही फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है जैसे चाय, कॉफी, रबर, कपास आदि। यह प्रणाली उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है।
विशेषताएँ:
पूंजी निवेश और मशीनों का अधिक प्रयोग।
श्रमिक आधारित प्रणाली।
विदेशी बाजार पर निर्भरता।
विशेष रूप से उपनिवेशों में विकसित हुई।
व्हिटल्सी की कृषि प्रणालियाँ कृषि के वैश्विक स्वरूप को समझने में सहायक हैं। यह मॉडल मानव और प्रकृति के बीच संबंधों को प्रकट करता है और विभिन्न कृषि प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन का आधार प्रदान करता है।
प्रश्न-3. भारत में हरित क्रान्ति के उपादान, प्रभाव व परिणामों का विवरण दीजिए।
उत्तर:- भारत में हरित क्रांति (Green Revolution) 1960 के दशक में एक कृषि सुधार आंदोलन के रूप में आरंभ हुई, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। यह मुख्यतः उच्च उपज वाली किस्मों (HYV), सिंचाई, उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग पर आधारित थी।
मुख्य उपादान (Components):
- उच्च उपज देने वाली किस्में (HYV): गेहूं और चावल की नई किस्मों का प्रयोग।
- सिंचाई व्यवस्था: नहरों, ट्यूबवेल्स आदि से सिंचाई का विस्तार।
- रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग।
- आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग: ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि।
- सरकारी नीतियाँ: न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऋण सुविधा, बीज वितरण केंद्र।
प्रभाव:
- उत्पादन में वृद्धि: विशेषतः गेहूं उत्पादन में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वृद्धि हुई।
- आत्मनिर्भरता: भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ।
- कृषि क्षेत्र में व्यावसायीकरण: किसान अब बाजार के लिए उत्पादन करने लगे।
- ग्रामीण रोजगार: यंत्रों के उपयोग से रोजगार के नए अवसर बने।
नकारात्मक परिणाम:
- क्षेत्रीय असमानता: लाभ केवल कुछ राज्यों तक सीमित रहा।
- सामाजिक असमानता: बड़े किसानों को ही अधिक लाभ मिला।
- प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव: भूजल स्तर में गिरावट, भूमि की उर्वरता में कमी।
- रासायनिक प्रदूषण: जल और मृदा प्रदूषण की समस्या।
हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न संकट से उबारा और कृषि को एक नई दिशा दी, लेकिन इसके साथ ही संसाधनों के असंतुलित उपयोग और क्षेत्रीय-सामाजिक विषमता की समस्याएं भी उत्पन्न हुईं। वर्तमान में सतत कृषि की दिशा में सुधार की आवश्यकता है।
प्रश्न-4. कृषि प्रदेश क्या है? डी. ह्विटलेसी के अनुसार बृहत् कृषि प्रदेशों को बताइए तथा किसी एक का सविस्तार वर्णन कीजिए।
उत्तर:- कृषि प्रदेश (Agricultural Region) उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कृषि की प्रकार, विधियाँ, फसलों की प्रकृति, भूमि उपयोग प्रणाली, एवं कृषकों की जीवनशैली आदि में व्यापक समानताएँ पाई जाती हैं। कृषि प्रदेश निर्धारण में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी कारकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
डी. ह्विटलेसी (D. Whittlesey) ने 1936 में कृषि के आधार पर विश्व को पाँच प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। उन्होंने भू-प्राकृतिक, सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में रखकर इन प्रदेशों का निर्धारण किया। उनके अनुसार निम्नलिखित बृहत् कृषि प्रदेश हैं:
- आर्थिक कृषि (Commercial Grain Farming)
- निर्यात प्रधान वृक्ष कृषि (Plantation Agriculture)
- आयामी पशुपालन (Nomadic Herding)
- अर्ध-व्यवसायिक पशुपालन (Livestock Ranching)
- वृत्तीय कृषि (Mediterranean Agriculture)
- घन-वासी कृषि (Intensive Subsistence Agriculture)
- स्थानांतरित कृषि (Shifting Cultivation)
घन-वासी गहन कृषि (Intensive Subsistence Agriculture) का सविस्तार वर्णन:
यह कृषि प्रणाली मुख्यतः एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों—जैसे भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि में पाई जाती है। इसमें छोटे-छोटे भूखण्डों पर अधिक मात्रा में श्रम का प्रयोग कर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं।
विशेषताएँ:
फसलें मुख्यतः खाद्यान्न होती हैं जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, जौ आदि।
सिंचाई पर अत्यधिक निर्भरता।
परंपरागत उपकरणों का उपयोग।
परिवार-आधारित श्रमिक प्रणाली।
भूमि का तीव्र उपयोग—एक वर्ष में दो या तीन बार फसल।
इस प्रणाली का उद्देश्य घरेलू उपभोग हेतु फसल उत्पादन होता है, न कि व्यापार। यह प्रणाली संसाधन-समृद्ध नहीं होती, फिर भी जीविका का एक सशक्त साधन होती है।
प्रश्न-5. भारत की कृषि नीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर:- भारत की कृषि नीति वह नीति है जो सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास, खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य “हरित क्रांति” के बाद आत्मनिर्भरता एवं किसानों की आय में वृद्धि है।
मुख्य तत्व:
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था।
हरित क्रांति के माध्यम से उत्पादन वृद्धि।
बीज, उर्वरक, कीटनाशक पर सब्सिडी।
कृषि ऋण व बीमा योजनाएँ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)।
ई-नाम (e-NAM) पोर्टल से कृषि विपणन सुधार।
समालोचनात्मक विश्लेषण:
सकारात्मक पक्ष:
खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता।
किसानों को न्यूनतम मूल्य गारंटी।
सिंचाई, उन्नत बीज, एवं यंत्रीकरण को प्रोत्साहन।
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान का विस्तार।
नकारात्मक पक्ष:
MSP प्रणाली सीमित फसलों व राज्यों तक सीमित।
सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से राहत अपर्याप्त।
कृषि में निजी निवेश की कमी।
छोटे व सीमांत किसानों को योजनाओं का लाभ सीमित।
भूमि सुधारों की निष्क्रियता।
भारत की कृषि नीति ने देश को खाद्यान्न सुरक्षा तो प्रदान की है, परन्तु किसान की आय, आत्महत्या की समस्या, भूमि सुधार व जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर यह अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। आज की आवश्यकता है कि नीति को अधिक समावेशी, टिकाऊ एवं किसान-केंद्रित बनाया जाए।
प्रश्न-6. भारत से उदाहरण देते हुए कृषि विकास के प्रभावी भौतिक कारकों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- किसी भी देश की कृषि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जिनमें भौतिक कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कृषि की विविधता इन्हीं भौतिक कारकों का परिणाम है।
- जलवायु (Climate):
भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है।
उदाहरण: पंजाब और हरियाणा में अच्छी वर्षा एवं सिंचाई की सुविधा के कारण गेहूं और धान की अधिक पैदावार होती है।
राजस्थान में कम वर्षा होने से बाजरा और ज्वार जैसी शुष्क भूमि वाली फसलें उगाई जाती हैं।
- मृदा (Soil):
मिट्टी की गुणवत्ता और प्रकार फसल निर्धारण में महत्त्वपूर्ण है।
उदाहरण:
काली मिट्टी (रेगुर): महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में कपास की खेती के लिए उपयुक्त।
जलोढ़ मिट्टी: गंगा के मैदानों में चावल, गेहूं, गन्ना आदि की खेती।
रेतीली मिट्टी: थार मरुस्थल में सीमित सिंचित खेती।
- स्थलाकृति (Relief):
मैदानी क्षेत्रों में कृषि करना आसान होता है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती अपनाई जाती है।
उदाहरण: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में चाय और फल-फूलों की खेती।
- जल संसाधन (Water Resources):
सिंचाई की सुविधा कृषि उत्पादकता को बढ़ाती है।
उदाहरण: पंजाब में भाखड़ा-नंगल परियोजना ने कृषि को बहुत बढ़ावा दिया।
सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल का अभाव कृषि को सीमित करता है।
- प्राकृतिक आपदाएँ:
बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि जैसी आपदाएँ कृषि को प्रभावित करती हैं।
उदाहरण: बिहार में गंगा की बाढ़ से हर वर्ष कृषि को नुकसान होता है।
- सूर्यप्रकाश की उपलब्धता:
फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। भारत की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है।
इस प्रकार, भारत के विभिन्न राज्यों की कृषि प्रणाली भौतिक कारकों के प्रभाव में विकसित हुई है और यही कारण है कि भारत में कृषि विविध और क्षेत्र विशेष पर आधारित है।
प्रश्न-7. वॉन थ्यूनन के ‘कृषि अवस्थिति सिद्धान्त’ की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- वॉन थ्यूनन (Johann Heinrich von Thünen) ने 1826 में “Isolated State” नामक पुस्तक में कृषि अवस्थिति सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत बताता है कि कृषि गतिविधियाँ किसी केंद्रीय बाजार से दूरी के आधार पर कैसे व्यवस्थित होती हैं। यह मॉडल आर्थिक लाभ, परिवहन लागत और भूमि किराये पर आधारित है।
सिद्धांत की मुख्य बातें:
एक पृथक राज्य जिसकी एक केन्द्रीय बाजार हो।
सभी दिशाओं में एकसमान जलवायु और भूमि।
परिवहन का केवल भूमि मार्ग और लागत दूरी के अनुसार बढ़ती है।
किसान लाभ अधिकतम करने के लिए कार्य करते हैं।
थ्यूनन के अनुसार कृषि क्षेत्र की व्यवस्था:
- सबसे अंदरूनी वृत्त – डेयरी और बागवानी (शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएँ)
- दूसरा वृत्त – वनों की लकड़ी (निर्माण और ईंधन हेतु)
- तीसरा वृत्त – फसल कृषि (जैसे अनाज)
- चौथा वृत्त – पशुपालन
- अंतिम – निर्जन क्षेत्र या वाणिज्यिक वनों की कटाई
सकारात्मक पक्ष:
भूमि उपयोग और बाजार दूरी के बीच संबंध स्पष्ट करता है।
लाभ अधिकतम और परिवहन लागत पर ध्यान देता है।
कृषि भौगोलिक विश्लेषण में पहला वैज्ञानिक प्रयास।
आलोचना:
पृथक राज्य जैसी धारणा अव्यावहारिक है।
परिवहन के साधन विविध होते हैं और केवल दूरी पर निर्भर नहीं करते।
भौगोलिक विविधता की अनदेखी करता है।
आधुनिक बाजार संरचना और तकनीकी विकास को ध्यान में नहीं रखता।
वॉन थ्यूनन का सिद्धांत यद्यपि आदर्श परिस्थितियों पर आधारित है, लेकिन यह कृषि अवस्थिति के आर्थिक पहलुओं को समझने में अत्यंत उपयोगी है। आज भी यह सिद्धांत कृषि योजना और स्थानिक विश्लेषण के लिए आधार प्रदान करता है।
प्रश्न-8. भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा ऐसे किन्हीं दो प्रदेशों की कृषि एवं जलवायु दशाओं का सह-सम्बन्ध दर्शाइए।
उत्तर:- भारत को कृषि-जलवायु विशेषताओं के आधार पर ‘राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)’ ने 15 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। यह विभाजन तापमान, वर्षा, मिट्टी, आर्द्रता एवं कृषि संभावनाओं पर आधारित है। ये हैं:
- पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र
- पूर्वी हिमालयी क्षेत्र
- गंगीय मैदान (पश्चिमी, मध्य, पूर्वी)
- ब्रह्मपुत्र घाटी
- मध्य भारत
- पश्चिमी भारत
- गुजरात क्षेत्र
- पश्चिमी पठार एवं घाट
- मध्य पठार
- दक्षिणी पठार
- पूर्वी तटीय क्षेत्र
- पश्चिमी तटीय क्षेत्र
- पूर्वोत्तर भारत
- द्वीपीय क्षेत्र
(1) गंगीय मैदान (पूर्वी)
जलवायु – समशीतोष्ण, आर्द्र जलवायु।
वर्षा – 100–200 सेमी।
कृषि – मुख्यतः चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, गन्ना।
सह-संबंध – प्रचुर वर्षा एवं उपजाऊ दोमट मिट्टी के कारण कृषि उत्पादन अधिक है। गंगा नदी जलस्रोत का मुख्य साधन है।
(2) पश्चिमी भारत (राजस्थान)
जलवायु – शुष्क व अर्द्ध-शुष्क।
वर्षा – 25–75 सेमी।
कृषि – बाजरा, ज्वार, चना, मूँगफली।
सह-संबंध – वर्षा की कमी के कारण सूखा-प्रतिरोधी फसलों का उत्पादन होता है। जलवायु कृषि की सीमाएँ तय करती है, सिंचाई पर अधिक निर्भरता।
इस प्रकार जलवायु एवं कृषि के बीच गहरा सह-संबंध पाया जाता है जो क्षेत्र विशेष की कृषि पद्धतियों को प्रभावित करता है।
प्रश्न-9. कृषि विकास को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों को समझाइए और भारत से उदाहरण दीजिए।
उत्तर:-
प्रश्न-10. भूमि उपयोग के आंकड़ों के स्रोत एवं समस्याओं की विशिष्टता की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- भूमि उपयोग डेटा किसी देश की योजना, विकास और कृषि नीतियों के निर्माण में अत्यंत आवश्यक होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि उपयोग संबंधित आँकड़े न केवल आर्थिक योजनाओं में उपयोगी हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं।
भूमि उपयोग आंकड़ों के प्रमुख स्रोत:
- राजस्व अभिलेख: गाँव स्तर पर पटवारी द्वारा भूमि की जानकारी एकत्र की जाती है।
- सेटेलाइट इमेजरी: रिमोट सेंसिंग तकनीक द्वारा भूमि की वास्तविक स्थिति का आकलन।
- सर्वे ऑफ इंडिया: भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा स्थलाकृति और उपयोग डेटा।
- भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान: समय-समय पर रिपोर्टें प्रकाशित करता है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO): सर्वेक्षण आधारित सांख्यिकी प्रदान करता है।
भूमि उपयोग आंकड़ों की समस्याएँ:
- प्राकृतिक विविधता: भारत में भौगोलिक विविधता अधिक है, जिससे आंकड़े एकरूप नहीं होते।
- अद्यतन की कमी: राजस्व रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं होते।
- तकनीकी दोष: सेटेलाइट डेटा में मौसम, बादल या तकनीकी त्रुटियाँ।
- संबंधित विभागों के बीच समन्वय की कमी: आंकड़ों का अंतर-विभागीय समन्वय न होना।
- मानकीकरण का अभाव: राज्यों द्वारा विभिन्न मापदंडों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।
- ग्रामीण-शहरी अंतर: शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग बदलता रहता है, जिससे डेटा अस्थिर हो जाता है।
- सूक्ष्म स्तर पर जानकारी का अभाव: डेटा अधिकतर राज्य या जिले स्तर पर होते हैं, ग्राम स्तर पर कम।
उदाहरण:
कई राज्यों में भूमि उपयोग श्रेणियाँ जैसे – कृषि योग्य भूमि, वन, बंजर, चरागाह आदि भिन्न रूपों में दर्ज होती हैं, जिससे तुलनात्मक अध्ययन कठिन होता है।
समाधान के उपाय:
तकनीकी साधनों का उपयोग बढ़ाना जैसे GIS, रिमोट सेंसिंग।
डेटा एकत्रण की एकरूप प्रक्रिया तैयार करना।
समय-समय पर सर्वेक्षण और अपडेट करना।
अतः भूमि उपयोग आंकड़ों की विश्वसनीयता और सटीकता विकास योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है। इसके लिए आंकड़ों के स्रोतों का सुदृढ़ीकरण और समस्याओं का समाधान जरूरी है।
VMOU MAGE-07 Paperr , vmou ma final year exam paper , vmou exam paper 2030 2029 2028 2027 , vmou exam paper 2025-26 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4
VMOU EXAM PAPER