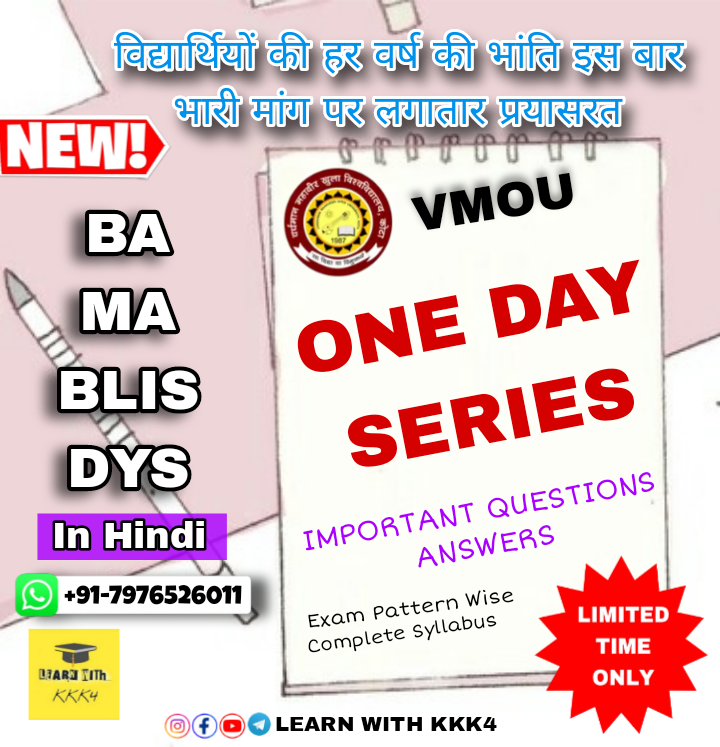VMOU GE-04 Paper BA 2ND Year (SEMESTER-III & IV) ; vmou exam paper
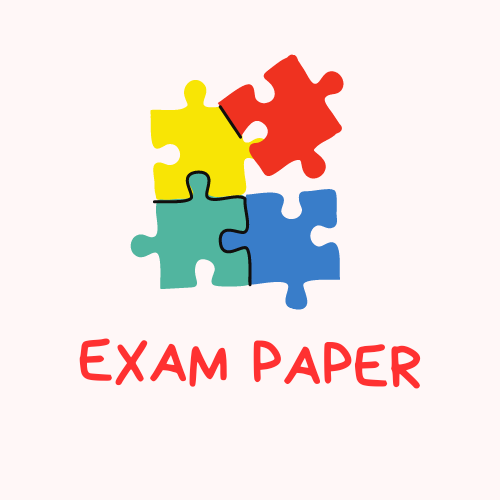
VMOU BA 2nd Year के लिए भूगोल ( GE-04 , संसाधन भूगोल ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.संसाधन का सतत विकास
उत्तर:- संसाधनों का ऐसा उपयोग जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे।
प्रश्न-2.नवीनकरणीय संसाधन
उत्तर:-वे प्राकृतिक संसाधन जो समय के साथ पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे—सौर ऊर्जा, जल, पवन।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-3.पारिस्थितिक संतुलन
उत्तर:- प्राकृतिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच स्थिर संबंध को पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं।
प्रश्न-4. Soil Profile (मृदा परिचोदिका)
उत्तर:- भूमि की सतह से नीचे विभिन्न क्षैतिज परतों का अनुक्रम मृदा परिचोदिका कहलाता है।
प्रश्न-5. Types of Iron-Ore (लौह अयस्क के प्रकार)
उत्तर:- मुख्य लौह अयस्क प्रकार हैं—हैमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट।
प्रश्न-6. भू-तापीय ऊर्जा
उत्तर:- पृथ्वी के अंदर से प्राप्त गर्मी से उत्पन्न ऊर्जा को भू-तापीय ऊर्जा कहते हैं
प्रश्न-7. कृषीय घनत्व
उत्तर:- कृषीय घनत्व उस जनसंख्या को दर्शाता है जो प्रति इकाई कृषि भूमि पर निवास करती है।
प्रश्न-8. Life Expectancy (जीवन प्रत्याशा)
उत्तर:- किसी देश या क्षेत्र में जन्म के समय अनुमानित औसत आयु को जीवन प्रत्याशा कहते हैं।
प्रश्न-9. पम्पास (Pampas):
उत्तर:- पम्पास दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में विस्तृत घास के मैदान हैं, जो गेहूं और मवेशी पालन के लिए प्रसिद्ध हैं।
प्रश्न-10. शंकुधारी वन के प्रमुख वृक्ष
उत्तर:- शंकुधारी वनों में प्रमुख वृक्षों में चीड़, देवदार, फर, और स्प्रूस शामिल हैं जो ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं।
प्रश्न-11. आणविक ऊर्जा (Atomic Energy):
उत्तर:- आणविक ऊर्जा नाभिकीय विखंडन या संलयन की प्रक्रिया से प्राप्त होती है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन तथा चिकित्सा में होता है।
प्रश्न-12. सतत विकास (Sustainable Development):
उत्तर:- सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता न हो।
प्रश्न-13. पवन ऊर्जा (Wind Energy):
उत्तर:- पवन ऊर्जा वायु की गति से टरबाइन घुमाकर बिजली उत्पन्न करने की स्वच्छ व अक्षय विधि है।
प्रश्न-14. जैवविविधता (Biodiversity):
उत्तर:- जैवविविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों की विविधता से है
प्रश्न-15. Resource conservation – संसाधन संरक्षण
उत्तर:- संसाधन संरक्षण का तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग करना है ताकि वे भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहें।
प्रश्न-16. शंकुधारी बनों के प्रमुख वृक्ष
उत्तर:- शंकुधारी बनों के प्रमुख वृक्षों में चीड़, फर, स्प्रूस और देवदार शामिल हैं।
प्रश्न-17. आणविक ऊर्जा
उत्तर:- आणविक ऊर्जा परमाणु विखंडन या संलयन की प्रक्रिया से प्राप्त स्वच्छ और उच्च क्षमता वाली ऊर्जा है।
प्रश्न-18. Biodiversity – जैवविविधता
उत्तर:- जैवविविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव-जंतुओं, पौधों और सूक्ष्मजीवों की विविधता को दर्शाती है।
प्रश्न-19. पोषणीय या सतत विकास
उत्तर:- सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के संतुलन के साथ वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।
प्रश्न-20. Shifting Agriculture (स्थानान्तरीय कृषि):
उत्तर:- स्थानान्तरीय कृषि एक पारंपरिक कृषि प्रणाली है जिसमें किसान भूमि के एक टुकड़े पर कुछ वर्ष खेती करने के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं।
प्रश्न-21. अभ्रक के मुख्य उत्पादक देश
उत्तर:- भारत, चीन, रूस, अमेरिका और ब्राजील अभ्रक के प्रमुख उत्पादक देश हैं।
प्रश्न-22. Optimum Population (अनुकूलतम जनसंख्या):
उत्तर:- अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या स्तर है जो देश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए जीवन-स्तर को बनाए रखती है।
प्रश्न-23. संसाधन प्रबंधन (Resource Management):
उत्तर:- यह संसाधनों के समुचित दोहन, संरक्षण और पुनः उपयोग की प्रक्रिया है जिससे उनकी दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
प्रश्न-24. प्रवास (Migration):
उत्तर:- यह लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से स्थानांतरण है।
प्रश्न-25. जनसंख्या दबाव (Population Pressure):
उत्तर:- यह तब उत्पन्न होता है जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र के उपलब्ध संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर हो जाती है
प्रश्न-26. शुष्क कृषि (Dry Farming):
उत्तर:- यह उन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है जहाँ वर्षा अल्प होती है और सिंचाई के साधनों की कमी होती है।
प्रश्न-27. ट्रांस-साइबेरियन रेलमार्ग (Trans-Siberian Railways):
उत्तर:- यह रूस में स्थित विश्व की सबसे लंबी रेलमार्ग है जो मास्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है।
प्रश्न-28. टुंड्रा (Tundra):
उत्तर:- यह आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाने वाला वनस्पति रहित या बहुत कम वनस्पति वाला हिमाच्छादित क्षेत्र है।
प्रश्न-29. तैगा व सवाना क्या है?
उत्तर:- तैगा शीतोष्ण कटिबंध की शंकुधारी वनों वाली क्षेत्रीय पारिस्थितिकी प्रणाली है।
सवाना उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की घासभूमि है जहाँ विरल वृक्ष पाए जाते हैं।
प्रश्न-30. निर्वहनीय कृषि को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- निर्वहनीय कृषि वह कृषि प्रणाली है जो किसान द्वारा केवल अपने उपभोग हेतु की जाती है।
Section-B
प्रश्न-1.संसाधन भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्त्व पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- संसाधन भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, उपयोग, संरक्षण तथा उनके मानवीय प्रभावों का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति अंतर्विषयक है, जिसमें भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और पर्यावरणीय अध्ययन का समावेश होता है।
इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें जल, मृदा, खनिज, वन, ऊर्जा, मानव संसाधन आदि शामिल हैं। संसाधन भूगोल यह विश्लेषण करता है कि संसाधनों का स्थानिक वितरण कैसे होता है, किस प्रकार के भौगोलिक कारक उन्हें प्रभावित करते हैं, और उनका किस प्रकार दोहन किया जाता है।
संसाधन भूगोल का महत्त्व आधुनिक समय में और बढ़ गया है क्योंकि संसाधनों की अत्यधिक खपत, प्रदूषण तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन ने संसाधनों के संतुलित उपयोग की आवश्यकता को बल दिया है। यह सतत विकास की दिशा में नीति निर्धारण, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण तथा पर्यावरणीय संरक्षण में मार्गदर्शक सिद्ध होता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बताइए।
उत्तर:- संसाधनों को उनके स्रोत, पुनः प्राप्ति की क्षमता, उपयोगिता तथा स्वामित्व के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य वर्गीकरण निम्न प्रकार है:
- स्रोत के आधार पर:
प्राकृतिक संसाधन: जल, वायु, खनिज, वन, मृदा आदि।
मानव संसाधन: मानव श्रम, बुद्धि, कौशल आदि।
- पुनः प्राप्ति की क्षमता के आधार पर:
नवीकरणीय संसाधन: जो प्राकृतिक चक्र द्वारा पुनः प्राप्त हो सकते हैं, जैसे जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा।
अवनवीकरणीय संसाधन: जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, जिनका दोहन सीमित है।
- उपयोग के आधार पर:
वास्तविक संसाधन: जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं।
संभावित संसाधन: जो भविष्य में उपयोग के योग्य हो सकते हैं।
- स्वामित्व के आधार पर:
व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन।
यह वर्गीकरण संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और सतत विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है।
प्रश्न-3.मृदा के प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- भारत में मृदा के प्रकारों का वर्गीकरण उनके रंग, संरचना, उत्पत्ति और जलधारण क्षमता के आधार पर किया जाता है। प्रमुख मृदा प्रकार निम्नलिखित हैं:
जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil):
यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानों में पाई जाती है। यह उपजाऊ होती है और गेंहू, चावल आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है।
काली मृदा (Black Soil):
इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात में मिलती है। कपास की खेती के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है।
लाल मृदा (Red Soil):
आयरन की अधिकता से यह लाल रंग की होती है। यह दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है।
जलोढ़ मृदा (Laterite Soil):
उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जल धारण क्षमता कम होती है।
मरुस्थली मृदा (Desert Soil):
राजस्थान व थार क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जैविक पदार्थों की कमी होती है।
पर्वतीय मृदा (Mountain Soil):
यह हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। फलों व चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है।
प्रश्न-4.लौह अयस्क के भौगोलिक वितरण पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- भारत में लौह अयस्क का व्यापक भौगोलिक वितरण है। भारत विश्व के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादकों में से एक है। लौह अयस्क मुख्यतः चार प्रकार का होता है: मैगनेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट, जिसमें हेमेटाइट सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है।
मुख्य लौह अयस्क उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं:
- ओडिशा – यहाँ की बारबिल, किरेबुरु, बोनाई और सुंदरगढ़ खानें प्रसिद्ध हैं।
- झारखंड – सिंहभूमि क्षेत्र में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं।
- छत्तीसगढ़ – बैलाडिला क्षेत्र देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है।
- कर्नाटक – बेल्लारी, चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग प्रमुख क्षेत्र हैं।
- गोवा – यहाँ समुद्र के समीप लौह अयस्क खनन होता है, विशेषकर निर्यात के लिए।
इन क्षेत्रों से लौह अयस्क का उपयोग इस्पात उद्योग में तथा विदेशों में निर्यात हेतु किया जाता है।
प्रश्न-5.जल विद्युत् उत्पादन के महत्त्व व इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को समझाइए।
उत्तर:- जल विद्युत् अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह जल प्रवाह की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके मुख्य लाभ हैं:
- यह प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल है।
- यह दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोत है।
- इससे सिंचाई, मछली पालन, पर्यटन आदि में भी लाभ होता है।
- इसका रख-रखाव सरल होता है।
भौगोलिक दशाएँ जो जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक हैं:
- तेज ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र, जिससे जल गिरावट से ऊर्जा प्राप्त हो सके।
- प्रचुर मात्रा में जल स्रोत, जैसे नदियाँ और झीलें।
- चट्टानी और स्थिर भूमि संरचना, ताकि बांध टिकाऊ हो।
- जनसंख्या और उद्योगों की नजदीकी, ताकि बिजली की आपूर्ति व्यावसायिक रूप से लाभदायक हो।
भारत में भाखड़ा नांगल, टिहरी, हीराकुंड और नागार्जुनसागर जैसी परियोजनाएँ जल विद्युत उत्पादन के उत्तम उदाहरण हैं।
प्रश्न-6.वैश्विक ऊर्जा संकट पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- वैश्विक ऊर्जा संकट 21वीं सदी की एक गंभीर चुनौती बन चुका है। यह संकट ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न हुआ है।
मुख्य कारण:
- जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता।
- वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि और औद्योगीकरण।
- ऊर्जा की असमान वितरण प्रणाली।
- नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का अपर्याप्त विकास।
परिणाम:
- ऊर्जा की कीमतों में तीव्र वृद्धि।
- विकासशील देशों में ऊर्जा की भारी कमी।
- वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता।
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट।
समाधान:
- नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, जल) का विकास।
- ऊर्जा संरक्षण और दक्षता को बढ़ावा देना।
- वैश्विक सहयोग और नीति-निर्माण में संतुलन।
- सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाना।
ऊर्जा संकट का समाधान मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य है।
प्रश्न-7.जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारणों का वर्णन करते हुए इसके परिणामों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:-जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि से है।
मुख्य कारण:
- मृत्यु दर में गिरावट एवं चिकित्सा सुविधाओं में सुधार।
- कृषि व खाद्य उत्पादन में वृद्धि।
- शिक्षा व जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता की कमी।
- सामाजिक-धार्मिक कारण, जैसे अधिक संतान की इच्छा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन साधनों की पहुँच की कमी।
परिणाम:
- संसाधनों पर दबाव – जल, भोजन, ऊर्जा की कमी।
- बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि।
- शहरीकरण और झुग्गी बस्तियों का विकास।
- पर्यावरणीय क्षरण और प्रदूषण।
- स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं पर भार।
जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु जनजागरण, शिक्षा, रोजगार और परिवार नियोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए।
प्रश्न-8.विश्व संसाधन प्रदेशों पर भौगोलिक टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- विश्व को संसाधनों की उपलब्धता और उपयोगिता के आधार पर विभिन्न संसाधन प्रदेशों में बाँटा गया है। ये प्रदेश प्राकृतिक संपदा, तकनीक, जनसंख्या घनत्व और विकास स्तर के आधार पर अलग-अलग पहचान रखते हैं।
मुख्य संसाधन प्रदेश:
- उच्च संसाधन संपन्न प्रदेश – जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान; जहाँ खनिज, जल, ऊर्जा व तकनीकी संसाधन प्रचुर हैं।
- मध्यम संसाधन संपन्न प्रदेश – दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया; यहाँ प्राकृतिक संसाधन तो हैं, परंतु तकनीकी और आर्थिक विकास अपेक्षाकृत कम है।
- कम संसाधन संपन्न प्रदेश – अफ्रीका, मध्य एशिया; जहाँ संसाधनों की उपलब्धता कम है या उनका दोहन नहीं हो पाया है।
- ऊर्जा संसाधन प्रदेश – मध्य पूर्व, रूस; जहाँ तेल और गैस के भंडार विशाल हैं।
- खनिज संसाधन क्षेत्र – ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा आदि।
इन क्षेत्रों का अध्ययन वैश्विक विकास, व्यापार और पर्यावरणीय नीतियों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
प्रश्न-9. अनवकरणीय संसाधनों पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:-अनवकरणीय संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और जिनकी पुनःपूर्ति नहीं हो सकती या बहुत धीमी गति से होती है। इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग भविष्य में उनकी कमी या समाप्ति का कारण बन सकता है। प्रमुख अनवकरणीय संसाधनों में खनिज (जैसे लौह, तांबा), जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस) एवं रेडियोधर्मी पदार्थ (यूरेनियम, थोरियम) शामिल हैं। इन संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, परंतु इनका दोहन कुछ ही वर्षों में हो जाता है। अनवकरणीय संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण, पारिस्थितिक असंतुलन और ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल ऊर्जा का विकास एवं उपयोग कर हम अनवकरणीय संसाधनों पर निर्भरता कम कर सकते हैं। सतत विकास की दिशा में यह आवश्यक है कि हम इन संसाधनों का विवेकपूर्ण और संयमित उपयोग करें।
प्रश्न-10. जल संरक्षण के क्या उपाय हैं?
उत्तर:- जल संरक्षण का अर्थ है जल का संरक्षण, पुनःचक्रण और उसका विवेकपूर्ण उपयोग ताकि भविष्य में जल संकट से बचा जा सके। इसके प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:
वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting): वर्षा के जल को संग्रहित कर भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग करना।
सिंचाई में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग: ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली से जल की बर्बादी को रोका जा सकता है।
घरों में जल की बचत: नलों को बंद रखना, रिसाव रोकना और पानी का दोबारा उपयोग करना।
वन संरक्षण: वनों के संरक्षण से जल स्रोतों का संरक्षण होता है और वर्षा भी नियमित होती है।
औद्योगिक जल शोधन: उद्योगों में जल को पुनः प्रयोग के लिए शुद्ध करना।
सामुदायिक जागरूकता: लोगों में जल की महत्ता के प्रति जागरूकता फैलाना।
जल एक सीमित संसाधन है और इसके संरक्षण से न केवल पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है बल्कि मानव जीवन की निरंतरता भी सुनिश्चित होती है।
प्रश्न-11. प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- प्राकृतिक वनस्पति को अनेक भौगोलिक, जलवायवीय एवं मानवीय कारक प्रभावित करते हैं। इन प्रमुख कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं:
जलवायु: तापमान और वर्षा का वनस्पति पर गहरा प्रभाव होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं जबकि शुष्क क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ होती हैं।
मिट्टी (मृदा): विभिन्न प्रकार की मृदाएँ अलग-अलग वनस्पतियों का समर्थन करती हैं। काली मिट्टी में कपास उगता है, रेतीली मिट्टी में झाड़ियाँ पाई जाती हैं।
ऊँचाई (उच्चता): जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, वनस्पति में परिवर्तन आता है। समुद्र तल के पास उष्णकटिबंधीय वन और ऊँचाई पर शंकुधारी वन मिलते हैं।
सौर ऊर्जा: सूर्य का प्रकाश वनस्पति के लिए आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करती है।
मानव हस्तक्षेप: वनों की कटाई, कृषि विस्तार, शहरीकरण आदि से प्राकृतिक वनस्पति प्रभावित होती है।
इन सभी कारकों के परस्पर प्रभाव से किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप निर्धारित होता है।
प्रश्न-12. विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र बताइए।
उत्तर:- कोयला विश्व की प्रमुख पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों में से एक है और इसका उपयोग विद्युत उत्पादन, इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग आदि में होता है। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
चीन: विश्व में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ शांक्सी, शांदोंग, और मंगोलिया प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं।
भारत: झारखंड (झरिया, बोकारो), छत्तीसगढ़ (कोरबा), ओडिशा (तालचेर) एवं पश्चिम बंगाल (रानीगंज) प्रमुख क्षेत्र हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): यहाँ एपलाचियन पर्वत क्षेत्र (पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया) तथा इलिनोइस बेसिन में कोयला उत्पादित होता है।
ऑस्ट्रेलिया: क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में कोयला भंडार हैं। यह कोयले का प्रमुख निर्यातक देश भी है।
रूस: साइबेरिया क्षेत्र में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
इन क्षेत्रों से प्राप्त कोयला विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।
प्रश्न-13. विषुवतरेखीय (भूमध्यरेखीय) बनों की विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:- विषुवतरेखीय वन वे घने एवं सदाबहार वन हैं जो भूमध्यरेखा के समीप स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
घनत्व और ऊँचाई: ये वन अत्यधिक घने और बहुस्तरीय होते हैं, जिनमें वृक्षों की ऊँचाई 40 से 60 मीटर तक होती है।
सदाबहार प्रकृति: यहाँ वर्ष भर वर्षा होने के कारण पेड़-पौधे हर समय हरे रहते हैं।
जैव विविधता: ये वन जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इनमें लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
तीव्र प्रतिस्पर्धा: प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए यहाँ पौधों में तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है।
अवस्थापन: ये वन अमेजन बेसिन (दक्षिण अमेरिका), कांगो बेसिन (अफ्रीका), दक्षिण-पूर्व एशिया (इंडोनेशिया, मलेशिया) में पाए जाते हैं।
उपयोग: इन वनों से कठोर लकड़ी (टीक, महोगनी), औषधियाँ तथा रबर आदि प्राप्त होते हैं।
इन वनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी के ‘फेफड़े’ माने जाते हैं।
प्रश्न-14. यूरोप में आंतरिक जल परिवहन पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- यूरोप विश्व के उन महाद्वीपों में से एक है जहाँ आंतरिक जल परिवहन अत्यधिक विकसित है। यहाँ की नदियाँ, नहरें और झीलें परिवहन के लिए अनुकूल हैं।
- प्रमुख नदियाँ: राइन, डैन्यूब, एल्बे, वोल्गा आदि नदियाँ आंतरिक जल परिवहन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- नहरें: यूरोप में राइन-डैन्यूब नहर, मैन-डैन्यूब नहर, और नॉर्थ सी-बाल्टिक नहर जैसी कृत्रिम नहरें परिवहन को सरल बनाती हैं।
- विशेषताएँ:
नदियाँ पूरे वर्ष नौवहन योग्य हैं।
जलमार्गों पर आधुनिक बंदरगाह, गोदाम और क्रेनों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
परिवहन सस्ता, पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित एवं भारी सामानों के लिए उपयुक्त है।
महत्त्वपूर्ण क्षेत्र: जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, रूस आदि देशों में आंतरिक जल परिवहन का प्रमुख विकास हुआ है।
इस प्रकार यूरोप में आंतरिक जल परिवहन आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
प्रश्न-15. तीव्र जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:-तीव्र जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसके दुष्परिणाम अनेक क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं:
प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव: अधिक जनसंख्या संसाधनों का अत्यधिक दोहन करती है जिससे जल, भूमि, वन आदि पर दबाव बढ़ता है।
बेरोजगारी: जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ता, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है।
शहरी समस्याएँ: अधिक जनसंख्या के कारण झुग्गी-बस्तियाँ, ट्रैफिक जाम, कचरा प्रबंधन जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव: स्कूल, अस्पतालों की कमी तथा संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण गुणवत्ता पर असर पड़ता है।
पर्यावरण प्रदूषण: अधिक आबादी से अधिक कचरा, गाड़ियों की संख्या और प्रदूषण में वृद्धि होती है।
अपराध और सामाजिक तनाव: गरीबी, बेरोजगारी से अपराधों और सामाजिक असंतोष में वृद्धि होती है।
इसलिए जनसंख्या नियंत्रण हेतु जनजागरण, शिक्षा, परिवार नियोजन आदि उपाय आवश्यक हैं।
प्रश्न-16. मानव विकास सूचकांक को समझाइए।
उत्तर:- मानव विकास सूचकांक (HDI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित एक सांख्यिकीय मापक है जो किसी देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। इसमें तीन प्रमुख घटकों को सम्मिलित किया जाता है:
स्वास्थ्य: व्यक्ति की औसत आयु (Life expectancy at birth)।
शिक्षा: औसत स्कूली शिक्षा अवधि और अपेक्षित शिक्षा अवधि।
आय: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI per capita)।
HDI का मान 0 से 1 के बीच होता है। 0.800 से ऊपर वाले देश उच्च विकास वाले माने जाते हैं। HDI किसी देश की केवल आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि सामाजिक व मानव संसाधनों की गुणवत्ता को भी दर्शाता है। यह नीति-निर्माताओं को यह समझने में मदद करता है कि देश का विकास किस दिशा में हो रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। भारत का HDI हाल के वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ा है, लेकिन अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है।
प्रश्न-17. संसाधन पर्याप्तता की संकल्पना क्या है?
उत्तर:- संसाधन पर्याप्तता (Resource Adequacy) का तात्पर्य यह सुनिश्चित करने से है कि किसी क्षेत्र या देश में मौजूदा और संभावित संसाधन, विशेष रूप से ऊर्जा और खनिज, भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। यह संकल्पना ऊर्जा नियोजन, औद्योगिक विकास और टिकाऊ विकास के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जब किसी क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता और उनकी मांग के बीच संतुलन बना रहता है, तो उसे संसाधन पर्याप्तता कहा जाता है। इसके लिए संसाधनों की खोज, संरक्षण, कुशल उपयोग और नवीकरणीय विकल्पों की खोज अत्यंत आवश्यक होती है। उदाहरणस्वरूप, बिजली आपूर्ति प्रणाली में संसाधन पर्याप्तता का अर्थ यह होता है कि मांग के समय उपयुक्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सके।
प्रश्न-18. मृदा परिषोदिका को समझाइए
उत्तर:- मृदा परिषोदिका (Soil Profile) से आशय मृदा के विभिन्न क्षैतिज स्तरों या परतों से है, जो एक कटाव या गड्ढे में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मृदा की ये परतें अलग-अलग रंग, बनावट, संरचना और जैविक पदार्थों की मात्रा में भिन्न होती हैं। सामान्यतः मृदा परिषोदिका को चार मुख्य परतों में बाँटा जाता है:
A-क्षेत्र (Topsoil): यह ऊपरी परत होती है जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक होती है। यह खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है।
B-क्षेत्र (Subsoil): इसमें खनिज अधिक होते हैं और जीवांश कम। यह परत A क्षेत्र से कठोर होती है।
C-क्षेत्र (Parent Material): यह वह परत है जो अपरदन से टूटी चट्टानों से बनी होती है।
R-क्षेत्र (Bedrock): यह सबसे नीचे की कठोर चट्टान होती है, जो मृदा निर्माण का मूल स्रोत है।
प्रश्न-19. संसाधनों की परिवर्तनशील संकल्पना या टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- संसाधनों की परिवर्तनशीलता (Resource Dynamism) का अर्थ यह है कि कोई भी संसाधन समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अपनी उपयोगिता, मूल्य और महत्व में बदलाव ला सकता है। यह एक गतिशील संकल्पना है, क्योंकि एक समय में अनुपयोगी समझा जाने वाला तत्व भविष्य में महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है।
उदाहरण के रूप में, प्राचीन समय में खनिज तेल का कोई महत्व नहीं था, परंतु आज यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार, सूर्य की ऊर्जा को पहले विशेष उपयोग नहीं समझा जाता था, परंतु आज यह एक प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन बन चुका है।
संसाधनों की परिवर्तनशीलता के प्रमुख कारण हैं –
तकनीकी विकास
सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में परिवर्तन
पर्यावरणीय दबाव
वैकल्पिक संसाधनों की खोज
यह संकल्पना हमें यह सिखाती है कि संसाधन स्थायी नहीं होते, बल्कि मानव की दृष्टि और आवश्यकता के अनुसार उनका स्वरूप और महत्व बदलता रहता है।
प्रश्न-20 भारत में ताँबा उत्पादन पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- भारत में ताँबा एक महत्वपूर्ण गैर-लौह धातु है जिसका उपयोग विद्युत, निर्माण, संचार और वाहन उद्योग में होता है। भारत में ताँबे के भंडार सीमित हैं, परंतु इसका खनन और परिशोधन बड़े स्तर पर होता है। भारत में ताँबे का उत्पादन मुख्यतः निम्नलिखित राज्यों में होता है:
- झारखंड: सिंहभूम ज़िला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है।
- राजस्थान: खेतड़ी और झुनझुनू क्षेत्र ताँबे के लिए प्रसिद्ध हैं।
- मध्य प्रदेश: बालाघाट क्षेत्र में ताँबे का अच्छा भंडार है।
भारत में ताँबा खनन के साथ-साथ स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग कार्य भी होता है। प्रमुख कंपनियाँ जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) इस कार्य में अग्रणी हैं।
भारत की ताँबा खपत इसकी घरेलू उत्पादन क्षमता से अधिक है, इसलिए ताँबा आयात भी किया जाता है।
प्रश्न-21. सौर ऊर्जा पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- सौर ऊर्जा (Solar Energy) सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, जिसे विभिन्न तकनीकों द्वारा विद्युत या ताप ऊर्जा में बदला जाता है। यह एक नवीकरणीय, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा स्रोत है, जो भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है।
सौर ऊर्जा के उपयोग:
सौर पैनलों द्वारा बिजली उत्पादन
सोलर कुकर, हीटर व ड्रायर
कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए सौर पंप
ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी व मोबाइल चार्जिंग
भारत में सौर ऊर्जा का विकास:
भारत “अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन” (ISA) का नेतृत्व कर रहा है और “राष्ट्रीय सौर मिशन” के तहत 2030 तक 100 GW सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में विशाल सौर पार्क स्थापित किए गए हैं।
सौर ऊर्जा के प्रयोग से न केवल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटती है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है।
प्रश्न-22. विश्व में जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। कुछ क्षेत्र अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले हैं, जबकि कुछ स्थान विरल जनसंख्या वाले हैं।
सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र:
पूर्वी व दक्षिणी एशिया: चीन, भारत, बांग्लादेश आदि
यूरोप के कुछ भाग: ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड
नाइल घाटी (मिस्र): जलस्रोत और उपजाऊ भूमि के कारण
विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र:
ध्रुवीय क्षेत्र: अंटार्कटिका, आर्कटिक
मरुस्थलीय क्षेत्र: सहारा, थार
घने वन क्षेत्र: अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन
ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र: हिमालय, एंडीज
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक:
जलवायु
जल स्रोत
भूमि की उपजाऊता
औद्योगीकरण
सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं
प्रश्न-23. जल संसाधन ह्रास को रोकने के उपाय बताइए।
उत्तर:- जल संसाधनों का ह्रास (Degradation) वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या है, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और अनियंत्रित उपयोग है। इसे रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं:
- जल संरक्षण: वर्षा जल संचयन, तालाबों और झीलों की सफाई एवं पुनर्जीवन।
- प्रदूषण नियंत्रण: घरेलू, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट को जल स्रोतों में जाने से रोकना।
- सिंचाई की आधुनिक तकनीकें: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का उपयोग।
- जन जागरूकता: लोगों को जल की महत्ता और संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
- सरकारी नीतियाँ: जल उपयोग का नियमबद्ध नियोजन और भूजल दोहन पर नियंत्रण।
- पुनः उपयोग: अपशिष्ट जल का उपचार कर पुनः उपयोग करना।
इन उपायों को अपनाकर जल संसाधनों को दीर्घकालिक रूप से संरक्षित किया जा सकता है।
प्रश्न-24. विश्व में मत्स्य उद्योग के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- विश्व में मत्स्य उद्योग का विकास उन क्षेत्रों में अधिक हुआ है जहाँ समुद्र तट लम्बे हैं, ठंडा जल प्रवाह होता है और प्लवक (plankton) की मात्रा अधिक होती है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र: इसमें नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा और अमेरिका के समुद्री तट आते हैं। यहाँ कॉड, हैडॉक और हेरिंग जैसी मछलियाँ पाई जाती हैं।
उत्तरी प्रशांत क्षेत्र: जापान, रूस और अमेरिका के पश्चिमी तट इस क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन करता है।
दक्षिण-पूर्व एशिया: थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों में छोटे जहाजों और पारंपरिक तरीकों से मछली पकड़ी जाती है।
हम्बोल्ट क्षेत्र: पेरू और चिली का पश्चिमी तट। यहाँ एंकोवीटा मछली की बहुतायत है।
अंटार्कटिक क्षेत्र: यहाँ क्रिल और अन्य समुद्री जीवों का शिकार होता है।
इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन आधुनिक तकनीकों, गहरे समुद्र में जाल बिछाने, और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के साथ संचालित होता है।
प्रश्न-25. ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों पर टिप्पणी कीजिए
उत्तर:- गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे स्रोत हैं जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों (कोयला, पेट्रोल, डीजल) के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाते हैं और पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
सौर ऊर्जा: सूर्य की किरणों से विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह स्वच्छ और अनंत स्रोत है।
पवन ऊर्जा: पवन टरबाइन के माध्यम से हवा की गति को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है।
जैव ऊर्जा (बायोमास): जैविक पदार्थों जैसे गोबर, फसल अवशेष आदि से गैस या ऊर्जा प्राप्त की जाती है।
भूतापीय ऊर्जा: पृथ्वी की भीतरी गर्मी से प्राप्त ऊर्जा, विशेषकर ज्वालामुखीय क्षेत्रों में।
समुद्री ऊर्जा: ज्वार-भाटा एवं तरंग ऊर्जा से बिजली उत्पादन किया जाता है।
ये संसाधन टिकाऊ विकास की दिशा में सहायक होते हैं क्योंकि इनसे प्रदूषण नहीं फैलता और पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम होती है।
प्रश्न-26. भारत में कोयला उत्पादन पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- भारत कोयला उत्पादन में विश्व के शीर्ष देशों में से एक है। कोयला भारत की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति का मुख्य साधन है। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार हैं:
झारखंड: यहाँ बोकारो, धनबाद, झरिया प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं।
छत्तीसगढ़: कोरबा और राइगढ़ कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं।
ओडिशा: तालचेर और संबलपुर में विशाल कोयला भंडार हैं।
पश्चिम बंगाल: रानीगंज कोयला क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से पहला कोयला खनन क्षेत्र है।
मध्य प्रदेश: सिंगरौली और शहडोल क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।
भारत में कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन, इस्पात उद्योग, और सीमेंट उद्योग में होता है। भारत की प्रमुख कोयला कंपनियाँ कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज हैं।
प्रश्न-27. जल विद्युत का उपयोग एवं महत्ता बताइए।
उत्तर:- जल विद्युत (Hydro-electricity) वह ऊर्जा है जो जल के प्रवाह से टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाती है। यह नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। इसका उपयोग और महत्ता इस प्रकार है:
बिजली उत्पादन: यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बिजली प्रदान करता है।
कृषि क्षेत्र में उपयोग: सिंचाई पंपों को चलाने में जल विद्युत महत्वपूर्ण है।
औद्योगिक उपयोग: उद्योगों में आवश्यक विद्युत की पूर्ति होती है।
पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायक: इसमें प्रदूषण नहीं होता और कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होता।
जलाशयों का बहुउद्देशीय उपयोग: बाँधों के निर्माण से सिंचाई, मत्स्य पालन और पर्यटन में वृद्धि होती है।
भारत में भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, टिहरी, और सरदार सरोवर जैसे बड़े बाँध जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं।
प्रश्न-28. मानव विकास सूचकांक पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- मानव विकास सूचकांक (HDI – Human Development Index) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित एक सूचकांक है जो किसी देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को मापता है। इसमें तीन मुख्य घटक होते हैं:
- स्वास्थ्य: जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) को दर्शाता है।
- शिक्षा: औसत एवं अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष।
- आय: प्रति व्यक्ति आय (GNI per capita)।
HDI का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास न देखकर समग्र मानवीय विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। HDI की गणना 0 से 1 के बीच होती है, जिसमें 1 उच्चतम विकास और 0 न्यूनतम विकास को दर्शाता है।
भारत का HDI स्तर मध्यम श्रेणी में आता है। HDI नीति निर्माताओं को सामाजिक सेवाओं के सुधार में दिशा देने का काम करता है।
प्रश्न-29. ट्रांस-साइबेरियन रेलमार्ग पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- ट्रांस-साइबेरियन रेलमार्ग विश्व की सबसे लंबी रेलमार्ग है जो रूस के मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक तक जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 9,300 किलोमीटर है। इस रेलमार्ग का निर्माण 1891 में शुरू हुआ और 1916 में पूर्ण हुआ।
यह रेलमार्ग रूस के यूरोपीय भाग को सुदूर पूर्व से जोड़ता है और साइबेरिया के विशाल क्षेत्र को यातायात से जोड़ने में सहायक है। यह मार्ग यूराल पर्वत, साइबेरिया, और अमूर नदी क्षेत्र से होकर गुजरता है।
महत्त्व:
यह माल और यात्रियों की ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण है।
इसके माध्यम से रूस के खनिज, लकड़ी और अन्य संसाधनों को परिवहन मिलता है।
यह एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक पुल का काम करता है।
यह सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है।
प्रश्न-30. प्रशांत महासागरीय संसाधन प्रदेश पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यह महासागरीय संसाधन प्रदेश कई देशों को आर्थिक रूप से लाभ प्रदान करता है।
मुख्य संसाधन:
मत्स्य संसाधन: ट्यूना, साल्मन और क्रिल जैसी मछलियाँ विशाल मात्रा में पाई जाती हैं।
खनिज संसाधन: समुद्र तल से मैंगनीज नोड्यूल, कोबाल्ट, तांबा और अन्य बहुमूल्य धातुएँ प्राप्त होती हैं।
तेल एवं गैस: समुद्र की गहराई में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं।
जलवायु प्रभाव: एल-नीनो जैसी घटनाएँ इस क्षेत्र में वैश्विक जलवायु पर प्रभाव डालती हैं।
महत्त्व: इस क्षेत्र में जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों की तटीय रेखाएँ हैं, जो इस महासागर के संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हैं।
Section-C
प्रश्न-1.संसाधन भूगोल की प्रकृति एवं विषय-क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए।
उत्तर:- संसाधन भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं सांस्कृतिक संसाधनों के वितरण, उपयोग एवं संरक्षण का अध्ययन करती है। यह विषय पर्यावरण और मानव के बीच अंतःक्रिया को समझने में सहायक है।
- प्रकृति (Nature):
संसाधन भूगोल एक अनुप्रयुक्त (Applied) एवं विश्लेषणात्मक शाखा है। यह संसाधनों की उपलब्धता, संभाव्यता, दोहन, प्रबंधन तथा उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। यह बहु-विषयी दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र एवं विज्ञान की समन्वित भूमिका होती है। - विषय-क्षेत्र (Scope):
(i) संसाधनों का वर्गीकरण: यह प्राकृतिक (जल, भूमि, खनिज, वन, जीव-जंतु), मानव (जनशक्ति, तकनीक) एवं सांस्कृतिक संसाधनों के वर्गीकरण का अध्ययन करता है।
(ii) स्थानिक वितरण: संसाधनों का वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर स्थानिक वितरण एवं असमानता का अध्ययन।
(iii) उपयोग एवं उपभोग: संसाधनों के वर्तमान एवं संभावित उपयोग, दोहन के तरीके तथा उपभोग के पैटर्न का मूल्यांकन।
(iv) संरक्षण एवं सतत विकास: संसाधनों की समाप्ति की संभावना को देखते हुए संरक्षण के उपायों तथा सतत विकास की नीतियों का अध्ययन।
(v) मानवीय हस्तक्षेप: मानव द्वारा संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे – शहरीकरण, औद्योगीकरण, वनों की कटाई, आदि का अध्ययन।
(vi) तकनीकी विकास: संसाधन पहचान, उपयोग एवं प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों जैसे GIS, रिमोट सेंसिंग, मॉडलिंग आदि की भूमिका।
- महत्त्व (Significance):
सतत विकास की योजना हेतु आधार।
क्षेत्रीय असमानताओं को समझने का माध्यम।
पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु दिशा।
नीति निर्धारण में उपयोगी जानकारी प्रदान करना।
अतः संसाधन भूगोल न केवल संसाधनों की भौगोलिक उपलब्धता को उजागर करता है, बल्कि उनके समुचित उपयोग और संरक्षण की दिशा में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.अभ्रक के उपयोग तथा विश्व वितरण को समझाइए।
उत्तर:-
- अभ्रक का परिचय (Introduction):
अभ्रक (Mica) एक खनिज है जो परतदार संरचना का होता है तथा इसे आसानी से चिप्स में विभाजित किया जा सकता है। यह विद्युतरोधी, तापरोधी तथा लचीलापन जैसी गुणों के कारण औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। - अभ्रक के उपयोग (Uses of Mica):
(i) विद्युत उद्योग: अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग ट्रांसफॉर्मर, मोटर, और केपेसिटर में इन्सुलेटर के रूप में होता है।
(ii) इलेक्ट्रॉनिक्स: मोबाइल, कंप्यूटर, माइक्रोचिप्स आदि में उपयोग।
(iii) सौंदर्य प्रसाधन: अभ्रक पाउडर का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों जैसे फाउंडेशन, आईशैडो आदि में चमक के लिए होता है।
(iv) निर्माण उद्योग: अभ्रक का उपयोग पेंट, छत सामग्री और अग्निरोधक वस्तुओं में होता है।
(v) रक्षा उद्योग: मिसाइल, युद्धक विमान आदि के तापरोधी हिस्सों में अभ्रक का उपयोग।
- अभ्रक का विश्व वितरण (World Distribution of Mica):
(i) भारत: विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक। प्रमुख राज्य – झारखंड (कोडरमा), बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश।
(ii) चीन: भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक।
(iii) अमेरिका: यहाँ उच्च गुणवत्ता की अभ्रक खदानें हैं, परन्तु उत्पादन सीमित है।
(iv) रूस: यूराल क्षेत्र में अभ्रक के भंडार हैं।
(v) ब्राजील: दक्षिण अमेरिका का प्रमुख अभ्रक उत्पादक।
(vi) कनाडा और कोरिया: भी महत्त्वपूर्ण अभ्रक उत्पादक देश हैं।
अभ्रक बहुआयामी उपयोग वाला खनिज है जिसका वैश्विक उद्योगों में विशिष्ट स्थान है। इसके सतत उपयोग हेतु खनन के वैकल्पिक एवं पर्यावरण मित्र उपायों की आवश्यकता है
प्रश्न-3. मानसून एशिया संसाधन प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- परिचय:
मानसून एशिया वह क्षेत्र है जो दक्षिण, दक्षिण-पूर्व एवं पूर्व एशिया के भागों को सम्मिलित करता है। इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है जिसमें ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। इस क्षेत्र को एक समृद्ध संसाधन प्रदेश माना जाता है।
भौगोलिक विस्तार:
यह क्षेत्र भारत, चीन, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया आदि देशों को सम्मिलित करता है।
प्रमुख विशेषताएँ:
(i) कृषि प्रधान क्षेत्र: मानसून एशिया कृषि पर आधारित है। यहाँ चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, चाय, कपास आदि की खेती प्रमुख है।
(ii) जलवायु विशेषता: गर्म और आर्द्र ग्रीष्म तथा शीतकालीन ऋतु में शुष्क मौसम।
(iii) जनसंख्या घनत्व: यह विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है।
(iv) वन संपदा: यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार, मानसूनी एवं बाँस के जंगल पाए जाते हैं।
(v) खनिज संसाधन: कोयला (चीन, भारत), लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन (मलेशिया), तांबा आदि खनिजों की प्रचुरता।
(vi) जल संसाधन: बड़ी नदियाँ – गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांग्त्से, मेकोंग आदि से सिंचाई, जल परिवहन एवं ऊर्जा उत्पादन।
(vii) औद्योगिक विकास: हाल के दशकों में इस क्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास हुआ है – चीन, जापान, कोरिया, भारत प्रमुख देश हैं।
(viii) सामाजिक संरचना: कृषक बहुल समाज, पारंपरिक जीवनशैली, विविध भाषा, धर्म व संस्कृति।
मानसून एशिया संसाधन प्रदेश प्राकृतिक संपदा, श्रमशक्ति एवं विविधता से परिपूर्ण है। यदि संसाधनों का संतुलित उपयोग हो, तो यह क्षेत्र विश्व का आर्थिक ध्रुव बन सकता है।
प्रश्न-4. विश्व में वनों के प्रकार एवं वितरण पर प्रकाश डालिए
उत्तर:- वन पृथ्वी के पर्यावरण का आधार हैं। यह न केवल जैव विविधता के संरक्षण में सहायक हैं, बल्कि मानव जीवन के लिए लकड़ी, ईंधन, औषधि, जलवायु नियंत्रण आदि अनेक उपयोगों में सहायक हैं।
- वनों के प्रकार (Types of Forests):
(i) उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन:
– स्थान: अमेज़न बेसिन, कांगो, दक्षिण-पूर्व एशिया।
– विशेषता: वर्ष भर हरे-भरे, भारी वर्षा, घने वृक्ष – महोगनी, एबोनी।
(ii) उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन:
– स्थान: भारत, ब्राजील, थाईलैंड।
– विशेषता: ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिरती हैं – साल, सागौन।
(iii) समशीतोष्ण सदाबहार वन:
– स्थान: दक्षिण चीन, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण-पूर्व अमेरिका।
– वृक्ष: ओक, मैग्नोलिया।
(iv) समशीतोष्ण पर्णपाती वन:
– स्थान: यूरोप, पूर्वी अमेरिका, पूर्वी एशिया।
– वृक्ष: मेपल, बीच, ओक।
(v) शंकुधारी वन (Taiga):
– स्थान: कनाडा, रूस, स्कैंडेनेविया।
– वृक्ष: स्प्रूस, फर्स, पाइंस।
(vi) भूमध्यसागरीय वन:
– स्थान: भूमध्यसागर तट, कैलिफोर्निया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया।
– वृक्ष: जैतून, सिट्रस।
(vii) मृदु वृक्ष वन (Savanna):
– स्थान: अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत।
– विशेषता: घास के मैदानों में छितरे वृक्ष।
- वितरण (Distribution):
वनों का वितरण जलवायु, मृदा, वर्षा और मानव हस्तक्षेप पर निर्भर करता है। उदाहरण:
अमेज़न – उष्णकटिबंधीय वर्षा वन।
साइबेरिया – शंकुधारी वन।
भारत – मिश्रित वन।
यूरोप – पर्णपाती वन।
वन पृथ्वी की जैव विविधता एवं पारिस्थितिक संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनके संरक्षण हेतु वैश्विक स्तर पर प्रयास आवश्यक हैं।
प्रश्न-5. वनो के प्रकार एवं वितरण पर लेख लिखे।
उत्तर:- वन पृथ्वी के जैविक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु नियंत्रण, जैव विविधता, मृदा संरक्षण और आर्थिक संसाधनों के रूप में भी उपयोगी हैं। विश्व भर में वनों के प्रकार भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वर्षा तथा तापमान पर निर्भर करते हैं।
- उष्णकटिबंधीय वर्षावन (Tropical Rainforests):
ये वन विषुवतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे – अमेज़न बेसिन (दक्षिण अमेरिका), कांगो बेसिन (अफ्रीका), दक्षिण-पूर्व एशिया। यहाँ वर्ष भर अधिक वर्षा (200 सेमी से अधिक) और उच्च तापमान होता है। प्रमुख वृक्षों में महोगनी, इबोनी, रबड़ और बेंत शामिल हैं। - उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन (Tropical Deciduous Forests):
ये वन भारत, ब्राजील, थाईलैंड, और अफ्रीका के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये कम वर्षा (100-200 सेमी) वाले क्षेत्रों में होते हैं और वृक्ष पत्तियाँ झाड़ते हैं। प्रमुख वृक्ष: साल, टीक, नीम, सागौन। - शीतोष्ण पर्णपाती वन (Temperate Deciduous Forests):
यूरोप, पूर्वी अमेरिका, चीन और जापान में पाए जाते हैं। इनमें साल भर मध्यम वर्षा होती है। वृक्षों में ओक, मेपल, बर्च शामिल हैं। - शंकुधारी वन (Coniferous Forests या Taiga):
ये वन कनाडा, साइबेरिया, स्कैंडेनेविया में पाए जाते हैं। यहाँ सर्दी अधिक और वर्षा कम होती है। वृक्ष सदाबहार होते हैं जैसे – स्प्रूस, फिर्स, पाइंस। - भूमध्यसागरीय वन (Mediterranean Forests):
इटली, ग्रीस, कैलिफोर्निया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ शुष्क गर्मी और हल्की सर्दी होती है। वृक्ष छोटे और मोटे पत्तों वाले होते हैं – ओलिव, सिट्रस, कॉर्क ओक। - पर्वतीय वन (Montane Forests):
पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे – हिमालय, एंडीज़, रॉकी। ऊँचाई के अनुसार इन वनों का प्रकार बदलता है। - शुष्क एवं मरुस्थलीय वन (Desert and Xerophytic Forests):
यहाँ वनस्पति विरल होती है। वृक्षों की पत्तियाँ छोटी, मोटी और कांटेदार होती हैं – कैक्टस, कीकर आदि।
विश्व में वनों का वितरण असमान है, परन्तु यह जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में वनों की कटाई से जैव पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः वनों का संरक्षण अति आवश्यक है।
प्रश्न-6. संसाधन भूगोल की प्रकृति एवं विषयक्षेत्र को समझाइए।
उत्तर:- प्रश्न 1 सेक्शन स
प्रश्न-7. विश्व में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए।
उत्तर:- विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है। कुछ देशों में यह वृद्धि अत्यंत तीव्र रही है, जिससे संसाधनों पर दबाव, बेरोजगारी, प्रदूषण और गरीबी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।
प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
- जन्म दर में वृद्धि:
विशेष रूप से विकासशील देशों में पारंपरिक सोच, धार्मिक मान्यताएँ और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के कारण जन्म दर अधिक है। कई समाजों में बच्चों को श्रमशक्ति के रूप में देखा जाता है। - मृत्यु दर में कमी:
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, टीकाकरण, पोषण में वृद्धि और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के कारण मृत्यु दर में भारी कमी आई है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। - अशिक्षा और जागरूकता की कमी:
शिक्षा का अभाव विशेषकर महिलाओं में परिवार नियोजन के उपायों के प्रति जागरूकता की कमी का कारण बनता है। यह अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है। - बाल विवाह और स्त्री-पुरुष असमानता:
विकासशील देशों में लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती है, जिससे उनकी प्रजनन अवधि लंबी होती है। साथ ही महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। - कृषि पर निर्भरता:
ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम आधारित अर्थव्यवस्था होने से अधिक बच्चों को श्रमिक के रूप में देखा जाता है, जिससे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। - धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास:
कुछ समुदायों में अधिक बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है और जनसंख्या नियंत्रण को धर्म विरोधी समझा जाता है। - प्रवासन:
कुछ क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवास के कारण जनसंख्या अचानक बढ़ जाती है, जैसे खाड़ी देशों में।
तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक वैश्विक चुनौती है जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।
प्रश्न-8. विश्व में आन्तरिक जल परिवहन को विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- आन्तरिक जल परिवहन (Inland Water Transport) वह प्रणाली है जिसमें नदियाँ, नहरें, झीलें और अन्य अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग माल और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने हेतु किया जाता है।
महत्त्व: यह परिवहन का सस्ता, पर्यावरणीय रूप से अनुकूल एवं ऊर्जा कुशल साधन है। यह भारी एवं थोक माल के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
मुख्य जल परिवहन मार्ग:
- अमेरिका:
मिसिसिपी-ओहायो जलमार्ग: यह अमेरिका का सबसे प्रमुख जलमार्ग है। इसमें मालवाहन की उच्च क्षमता है।
ग्रेट लेक्स-सेन्ट लॉरेंस जलमार्ग: यह अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाला अत्यधिक महत्वपूर्ण मार्ग है।
- यूरोप:
रेन नदी जलमार्ग: यह जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स को जोड़ता है और यूरोप का अत्यधिक व्यस्त जलमार्ग है।
डेन्यूब नदी: मध्य और पूर्वी यूरोप के कई देशों को जोड़ती है।
- रूस:
वोल्गा नदी जलमार्ग: यह रूस की आर्थिक जीवनरेखा मानी जाती है। यह काले सागर से बाल्टिक सागर तक पहुँच प्रदान करता है।
- एशिया:
चीन: यांग्त्ज़ी नदी दुनिया का सबसे व्यस्त आन्तरिक जलमार्ग है। इसमें आधुनिक जल परिवहन सुविधाएँ हैं।
भारत: गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियाँ आन्तरिक जल परिवहन के लिए प्रयुक्त होती हैं। भारत में ‘राष्ट्रीय जलमार्ग’ अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न जलमार्गों का विकास किया जा रहा है।
- अफ्रीका:
कांगो और नाइजर नदियाँ आंतरिक जल परिवहन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
लाभ:
कम लागत में भारी माल परिवहन संभव।
ईंधन की बचत और प्रदूषण कम।
सड़क और रेल परिवहन पर दबाव कम।
सीमाएँ:
मौसमी निर्भरता।
गति धीमी होती है।
कई स्थानों पर पर्याप्त गहराई और बुनियादी सुविधाओं की कमी।
आन्तरिक जल परिवहन एक पारंपरिक किंतु सशक्त साधन है जिसे आधुनिक तकनीकों द्वारा और सशक्त बनाकर विश्व के सतत विकास में योगदान दिया जा सकता है।
प्रश्न-9. संसाधन संरक्षण एवं संसाधन प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- संसाधन संरक्षण (Resource Conservation) का तात्पर्य उन उपायों से है जिनके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इसका उद्देश्य संसाधनों की बर्बादी को रोकना, उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना तथा भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें सुरक्षित रखना है। संरक्षण में जल, वन, खनिज, मृदा आदि के संरक्षण की नीति अपनाई जाती है।
वहीं, संसाधन प्रबंधन (Resource Management) का अर्थ है संसाधनों की वैज्ञानिक योजना, विकास, वितरण और उनके कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना। इसमें संसाधनों की उपलब्धता, उनकी गुणवत्ता, उनका उपयोग एवं पुनः उपयोग (recycling), और जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार रणनीति तैयार करना शामिल है।
संक्षेप में, संरक्षण मुख्यतः सुरक्षा और बचाव पर केंद्रित है जबकि प्रबंधन संसाधनों के कुशल, न्यायसंगत और निरंतर उपयोग पर आधारित है। दोनों ही पर्यावरणीय संतुलन एवं सतत विकास के लिए आवश्यक हैं।
प्रश्न-10. संसाधनों के संधृत विकास की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- संधृत विकास (Sustainable Resource Development) का तात्पर्य ऐसे विकास से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी नुकसान न पहुँचाए। इसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण, संतुलित एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल उपयोग शामिल है।
इस संकल्पना के अनुसार, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनका उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे पुनः उत्पन्न हो सकें। उदाहरण के लिए, वनों की कटाई के स्थान पर वृक्षारोपण, जल के अत्यधिक उपयोग की बजाय जल संरक्षण तकनीकों का अपनाना आदि।
संधृत विकास में पर्यावरणीय सुरक्षा, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास तीनों का संतुलन आवश्यक है। यह विकास की ऐसी दिशा है जिसमें पारिस्थितिक संतुलन बना रहे, संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे और मानव जीवन की गुणवत्ता सुधरे।
vmou GE-04 paper , vmou ba 2nd year exam paper , vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4