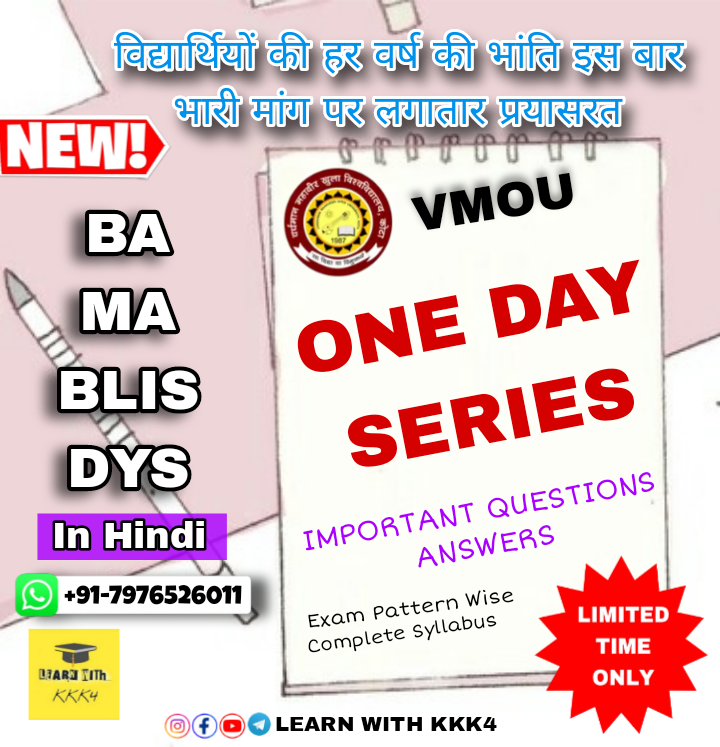VMOU MAED-01 Paper MA 1ST Year ; vmou exam paper
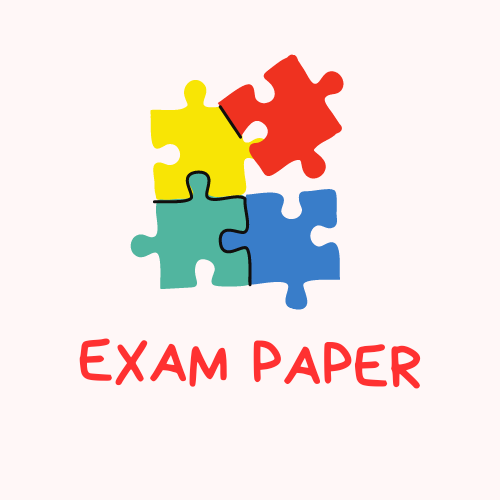
VMOU MA First Year के लिए MA-Education ( MAED-01 , ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग क्या है?
उत्तर:- बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग दुःख निवारण का आठ अंगों वाला मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीव, प्रयास, स्मृति और समाधि शामिल हैं।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण कौन-कौन से हैं?
उत्तर:- न्याय दर्शन के अनुसार चार प्रमाण हैं – प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द।
प्रश्न-3.विनोबा भावे के अनुसार, गीता क्या है?
उत्तर:- विनोबा भावे के अनुसार गीता आत्मा की आवाज़ और कर्मयोग का सजीव संदेश है।
प्रश्न-4. परा तथा अपरा विद्या से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- परा विद्या ब्रह्मज्ञान देने वाली आध्यात्मिक विद्या है, जबकि अपरा विद्या लौकिक और भौतिक ज्ञान है।
प्रश्न-5. जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के अनिवार्य साधन कौन-कौन से हैं?
उत्तर:- जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष प्राप्ति के अनिवार्य साधन हैं।
प्रश्न-6. मुल्ला निजामुद्दीन द्वारा प्रतिपादित इस्लामिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों के घटकों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:-इस पाठ्यक्रम में कुरान, हदीस, अरबी व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन, गणित और चिकित्सा शास्त्र शामिल थे।
प्रश्न-7. मनोमय कोष क्या है?
उत्तर:- मनोमय कोष वह आंतरिक आवरण है जो मन, विचारों और भावनाओं से संबंधित होता है।
प्रश्न-8. रूसी के प्रकृतिवाद और टैगोर के प्रकृतिवाद में क्या अंतर है?
उत्तर:- रूसी का प्रकृतिवाद बालक को प्रकृति के अनुसार स्वतः बढ़ने देता है, जबकि टैगोर का प्रकृतिवाद प्रकृति को सौंदर्य और आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम मानता है।
प्रश्न-9. प्रयोजनवाद की किन्हीं दो शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- अनुभवात्मक विधि और प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद की प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं।
प्रश्न-10. एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है?
उत्तर:- फ्रांसिस बेकन
प्रश्न-11. दांत अलीगेहिरी द्वारा रचित किसी एक विख्यात पुस्तक का नाम लिखिए।
उत्तर:- दांते अलीघिएरी की प्रसिद्ध पुस्तक “डिवाइन कॉमेडी” है।
प्रश्न-12. इरैस्यस द्वारा किस शिक्षण विधि को विकसित किया गया ?
उत्तर:-संवाद विधि (Dialectic Method)
प्रश्न-13. “संस्कृति एक सामाजिक विरासत है।” यह विचार किसके द्वारा दिया गया है ?
उत्तर:- लेवी ब्रूहल (Lévy-Bruhl)
प्रश्न-14. चैपिन के अनुसार परिवार के संरचनात्मक प्रतिरूप के किन्हीं दो पहलुओं के बारे में लिखिए।
उत्तर:- पारिवारिक आकार और पारिवारिक भूमिकाएँ
प्रश्न-15. आधुनिकीकरण की दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- तकनीकी उन्नति और सामाजिक गतिशीलता।
प्रश्न-16. रेडियो कार्यक्रम की कोई दो सीमाएँ बताइए।
उत्तर:- रेडियो कार्यक्रम की सीमाएँ हैं – दृश्य सहायता का अभाव और श्रोताओं की भागीदारी की कमी।
प्रश्न-17. विनोबा भावे ने किस प्रकार से गीता की व्याख्या की है?
उत्तर:- विनोबा भावे ने गीता को एक “मातृ-संवाद” के रूप में देखा जो मानवता को निष्काम कर्म की शिक्षा देता है।
प्रश्न-18. निष्काम कर्मयोग क्या है?
उत्तर:- निष्काम कर्मयोग वह योग है जिसमें बिना फल की इच्छा किए अपना कर्तव्य निभाया जाता है।
प्रश्न-19. इस्लाम धर्म के कोई से दो आधारभूत सिद्धांत लिखिए।
उत्तर:- तौहीद (एक ईश्वर में विश्वास), 2. नमाज़ (प्रार्थना करना)।
प्रश्न-20. न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं?
उत्तर:-न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि (अक्शपाद गौतम) माने जाते हैं।
प्रश्न-21. शिक्षा में यथार्थवाद क्या है?
उत्तर:-शिक्षा में यथार्थवाद वह दर्शन है जो वस्तुनिष्ठ ज्ञान और अनुभव को प्राथमिकता देता है।
प्रश्न-22. आधुनिकीकरण की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- 1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, 2. तकनीकी उन्नति और शहरीकरण।
प्रश्न-23. सांस्कृतिक विलंबन को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:-सांस्कृतिक विलंबन वह स्थिति है जब भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है परंतु गैर-भौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है।
प्रश्न-24. सूचना क्रांति का शिक्षा में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर:- सूचना प्रौद्योगिकी से ऑनलाइन शिक्षण, ई-पुस्तकें, और डिजिटल क्लासरूम संभव होते हैं।
प्रश्न-25. शैक्षिक दर्शन क्या है ?
उत्तर:- शैक्षिक दर्शन शिक्षा से जुड़े मूल सिद्धांतों, उद्देश्यों और मूल्यों का अध्ययन है।
प्रश्न-26. संख्या क्या है ?
उत्तर:-संख्या गणित की एक मूलभूत अवधारणा है जो मात्रा या गणना को दर्शाती है।
प्रश्न-27. त्रि शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- त्रि शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, आचार और व्यवहार – ये तीनों शिक्षा के मुख्य घटक हैं।
प्रश्न-28. अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे ?
उत्तर:- शंकराचार्य
प्रश्न-29. शिक्षा में अस्तित्ववाद क्या है ?
उत्तर:- शिक्षा में अस्तित्ववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव और व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देता है।
प्रश्न-30. CAI का पूर्ण नाम क्या है ?
उत्तर:- Computer Assisted Instruction।
प्रश्न-31. मानव अधिकार के कोई दो उद्देश्य लिखिए
उत्तर:- (1) व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना।
(2) समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देना।
प्रश्न-32. सूचना क्रांति को क्या महत्वता है ?
उत्तर:- सूचना क्रांति ज्ञान के प्रचार, त्वरित संचार और डिजिटल प्रगति को संभव बनाती है।
प्रश्न-33. यान्त्रिक प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- यान्त्रिक प्रकृतिवाद वह दर्शन है जो ब्रह्मांड और जीवन को एक मशीन की तरह मानता है जहाँ हर वस्तु कारण और प्रभाव के नियमों से संचालित होती है।
प्रश्न-34. आधुनिकीकरण प्रक्रिया को किन चार पक्षों में बाँटा गया है?
उत्तर:- सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक।
प्रश्न-35. हिज सेलेब्रेशन ऑफ अवेअरनेस’ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
उत्तर:- इवान इलिच (Ivan Illich)
प्रश्न-36. जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष के कोई दो साधन लिखिए।
उत्तर:- सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र।
प्रश्न-37. शून्यवाद का क्या अर्थ है ?
उत्तर:- शून्यवाद का अर्थ है—सब कुछ शून्य है; कोई स्थायी तत्व नहीं होता
प्रश्न-38. धर्म के कौनसे चार पक्ष होते हैं ?
उत्तर:- धर्म के चार पक्ष हैं—ज्ञान, कर्म, उपासना और नैतिकता।
प्रश्न-39. पहले मुस्लिम दार्शनिक का नाम लिखिए।
उत्तर:- ल-किन्दी (Al-Kindi)
प्रश्न-40. इवान इलिच की कोई दो कृतियों के नाम लिखिए।
उत्तर:- इवान इलिच की दो कृतियाँ हैं—‘Deschooling Society’ और ‘Tools for Conviviality’
Section-B
प्रश्न-1.चार्वाक दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- चार्वाक दर्शन प्राचीन भारत का एक नास्तिक और भौतिकवादी दर्शन है। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। इस दर्शन के अनुसार केवल प्रत्यक्ष अनुभव (इंद्रिय ज्ञान) ही सत्य है, और किसी भी अदृश्य या अलौकिक वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। चार्वाक के अनुसार आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि केवल कल्पनाएँ हैं जिनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों को भी चार्वाक अस्वीकार करता है।
चार्वाक जीवन को भोगवादी दृष्टिकोण से देखता है—”जब तक जीवन है, तब तक सुखपूर्वक जियो, ऋण लेकर भी घी पीयो” इसकी प्रमुख उक्ति है। यह दर्शन आत्मा की अमरता, पाप-पुण्य और परलोक को भी नकारता है। चार्वाक मानव जीवन को केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति का साधन मानता है। इस प्रकार यह एक व्यावहारिक, इंद्रियबोध पर आधारित दर्शन है, जो धर्म और अध्यात्म से रहित है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
उत्तर:- प्रकृतिवादी शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी को प्रकृति के अनुरूप शिक्षित करने पर बल देती हैं। यह विचारधारा मानती है कि बालक का स्वाभाविक विकास तभी संभव है जब उसे प्रकृति के निकट, मुक्त वातावरण में शिक्षा दी जाए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की प्राकृतिक प्रवृत्तियों का विकास करना है।
इस पद्धति में कक्षा की कठोर सीमाओं के बजाय प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक शिक्षण को महत्व दिया जाता है। बालकों को प्रकृति के बीच जैसे—उद्यान, खेत, नदी, आदि में रखकर वास्तविक अनुभवों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसमें रटने के बजाय अन्वेषण, अवलोकन, प्रयोग और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है।
रूसो, फ्रॉबेल, और मोंटेसरी जैसे शिक्षाशास्त्रियों ने प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का समर्थन किया। इन विधियों में शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है, और बालक अपनी जिज्ञासा के अनुसार सीखता है। संक्षेप में, प्रकृतिवादी शिक्षण विधियाँ बालक के स्वाभाविक विकास और अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित होती हैं।
प्रश्न-3.अस्तित्ववाद के अनुसार स्वयं के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- अस्तित्ववाद के अनुसार “स्वयं” (Self) एक स्वतंत्र, सजग और उत्तरदायी सत्ता है। यह दर्शन मानता है कि व्यक्ति अपने निर्णयों, कर्मों और विकल्पों से स्वयं अपना अस्तित्व निर्मित करता है। अस्तित्ववाद के प्रमुख विचारक जैसे जीन पॉल सार्त्र के अनुसार, “मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर वह अपने कर्मों द्वारा अपने स्वरूप का निर्माण करता है।”
अस्तित्ववाद में ‘स्वयं’ की अवधारणा व्यक्ति की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व से जुड़ी है। व्यक्ति के पास यह स्वतंत्रता है कि वह क्या बनेगा—और उसे ही अपने चुनावों का उत्तरदायित्व भी उठाना होता है। अस्तित्ववादी दर्शन आत्म-ज्ञान, आत्म-निरीक्षण और आत्म-साक्षात्कार पर बल देता है।
शिक्षा के क्षेत्र में इसका अर्थ यह है कि शिक्षार्थी को अपने अस्तित्व को जानने, चुनने और उसे सार्थक बनाने के अवसर दिए जाएं। अस्तित्ववाद में ‘स्वयं’ केवल समाज या ईश्वर द्वारा दिया गया परिचय नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की अपनी खोज और अनुभव से बना हुआ सत्य है।
प्रश्न-4.सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- सांख्य दर्शन भारतीय दर्शनों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि दो मूल तत्वों—प्रकृति और पुरुष—से बनी है। प्रकृति जड़ (अचेतन) है, जबकि पुरुष चेतन है। प्रकृति से सृष्टि की समस्त भौतिक वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं और इसमें त्रिगुण—सत्त्व, रजस और तमस—विद्यमान होते हैं।
प्रकृति ही कारण है शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार जैसे तत्वों की उत्पत्ति की। यह परिवर्तनशील और सक्रियरूप है। दूसरी ओर, पुरुष चेतना का प्रतीक है, जो निरपेक्ष, अकर्ता और दर्शा मात्र है। पुरुष अनेक हो सकते हैं लेकिन सभी स्वतंत्र और शुद्ध हैं।
जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, तभी संसार (जीवन) उत्पन्न होता है। मोक्ष की स्थिति तब आती है जब पुरुष यह जान लेता है कि वह प्रकृति से भिन्न है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का यह द्वैतवाद बहुत महत्वपूर्ण है और आत्मा (पुरुष) को प्रकृति से अलग समझने पर ही ज्ञान और मोक्ष संभव होता है।
प्रश्न-5.बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, नैतिकता और ध्यान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना है। बौद्ध शिक्षा में पाठ्यक्रम को इस प्रकार रचा गया है कि वह व्यक्ति को चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्य मार्ग की ओर ले जाए।
इसमें मुख्यतः तीन शील (त्रिसिक्षा) को महत्व दिया गया है—शील (नैतिक अनुशासन), समाधि (मानसिक एकाग्रता) और प्रज्ञा (ज्ञान)। पाठ्यक्रम में इन तीनों तत्वों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, ध्यान और आत्मचिंतन शामिल किया जाता है।
बौद्ध शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है। हिंसा का त्याग, करुणा, संयम, और आत्मविकास जैसे विषयों को शिक्षा का मूल उद्देश्य माना गया है। बौद्ध विहारों और संघों में शिक्षण व्यवस्था परंपरागत रूप से श्रमण परंपरा पर आधारित थी, जहाँ गुरु-शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान का संवहन होता था।
इस प्रकार बौद्ध दर्शन में शिक्षा का पाठ्यक्रम आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर केंद्रित था।
प्रश्न-6.विवेकानन्द के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है
उत्तर:- स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के भीतर निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनका मानना था कि शिक्षा का कार्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, आत्मबल, और सेवा-भाव का विकास करना है। वे कहते थे—”शिक्षा वह है जिससे व्यक्ति जीवन में खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके और नैतिक दृष्टि से बलशाली हो सके।”
विवेकानन्द की दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की दिव्यता और मानवता की सेवा भावना को जागृत करना है। उन्होंने शिक्षा को आत्मा के भीतर की शक्तियों को प्रकट करने का माध्यम बताया। उनके अनुसार, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को निडर, स्वावलंबी और चरित्रवान बनाए।
विवेकानन्द भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को शिक्षा का मूल आधार मानते थे। वे आधुनिक विज्ञान, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के पक्षधर थे लेकिन उसे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने की बात करते थे। इस प्रकार, उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास है—शरीर, मन और आत्मा तीनों का।
प्रश्न-7.वर्कले के आदर्शवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- जॉर्ज बर्कले एक प्रमुख आदर्शवादी दार्शनिक थे। उन्होंने “सार्वभौमिक आदर्शवाद” (Subjective Idealism) का प्रतिपादन किया, जिसमें यह कहा गया कि भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व केवल हमारी चेतना में है। उनके अनुसार, “अस्तित्व का अर्थ है अनुभव किया जाना” (Esse est percipi)। यानी, कोई वस्तु तभी अस्तित्व में है जब कोई उसे देखता, सुनता या महसूस करता है।
वर्कले के आदर्शवाद में यह माना गया है कि दुनिया का कोई भी पदार्थ स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बल्कि वह हमारी इंद्रियों के माध्यम से ही अस्तित्व में आता है। इस विचारधारा के अनुसार, संसार का अस्तित्व केवल चेतना में है, और सब कुछ ईश्वर की चेतना में बना रहता है।
वर्कले ने भौतिकवाद का खंडन करते हुए कहा कि वस्तुओं का कोई स्वतंत्र भौतिक अस्तित्व नहीं होता। वे केवल चेतना में अनुभव की गई घटनाएँ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वर्कले का दर्शन यह बताता है कि ज्ञान और अनुभव का स्रोत हमारा मन और चेतना है। इसलिए शिक्षक को छात्रों की चेतना और मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए।
प्रश्न-8.गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा (नयी तालीम) का उद्देश्य जीवनोपयोगी, आत्मनिर्भर और नैतिक शिक्षा देना था। उन्होंने 1937 में ‘वर्धा योजना’ के अंतर्गत इस शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। गाँधीजी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को हाथ, दिल और मस्तिष्क—तीनों से प्रशिक्षित करे।
गाँधीजी की शिक्षा प्रणाली में श्रम आधारित शिक्षा को महत्व दिया गया। उन्होंने कहा कि बालकों को प्रारंभ से ही किसी उत्पादक कार्य से जोड़ा जाए, जैसे कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, आदि। इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे और शिक्षा को अपने जीवन से जोड़ पाएँगे।
गाँधीजी का ज़ोर मातृभाषा में शिक्षा देने, नैतिक मूल्यों को शिक्षा में शामिल करने, और ग्रामीण विकास पर आधारित शिक्षा प्रणाली को लागू करने पर था। उन्होंने शिक्षा को केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि नैतिक और व्यावहारिक बताया। इस प्रकार, गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा एक सर्वांगीण और ग्राम्य समाज के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था थी।
प्रश्न-9. प्रयोजनवाद के किन्हीं चार स्वरूपों के बारे में विस्तार से लिखिए।
उत्तर:- प्रयोजनवाद (Pragmatism) एक आधुनिक दार्शनिक विचारधारा है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक अनुभवों एवं प्रयोगों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति है। इसके चार प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित हैं:
- मानवतावादी प्रयोजनवाद (Humanistic Pragmatism): यह स्वरूप मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है। इसमें समाज कल्याण, नैतिकता, और सामाजिक सहयोग को महत्व दिया जाता है।
- प्रायोगिक प्रयोजनवाद (Experimental Pragmatism): इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रयोग एवं अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना है। जॉन डेवी इसके प्रमुख प्रवक्ता हैं।
- ज्योतिषीय प्रयोजनवाद (Biological Pragmatism): यह स्वरूप जैविक सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अनुसार शिक्षा का कार्य बालक की प्राकृतिक प्रवृत्तियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार विकास करना है।
- राजनीतिक प्रयोजनवाद (Political Pragmatism): इस स्वरूप में शिक्षा को सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम माना गया है। यह समाज सुधार व लोकतांत्रिक विकास पर बल देता है।
इन चारों स्वरूपों का उद्देश्य है शिक्षा को अधिक उपयोगी, व्यावहारिक और अनुभवाधारित बनाना।
प्रश्न-10. यथार्थवाद के अनुसार बालक के लिए शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में लिखिए।
उत्तर:- यथार्थवाद (Realism) एक ऐसी दार्शनिक प्रणाली है जो यथार्थ को वास्तविक मानती है और कहती है कि वस्तुएं हमारे अनुभव से स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं। यथार्थवाद के अनुसार बालक के लिए शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- वस्तुनिष्ठ ज्ञान की प्राप्ति: यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को वास्तविक जगत के तथ्यों और सिद्धांतों से अवगत कराना है।
- इंद्रिय-बोध पर बल: यह मानता है कि ज्ञान का आरंभ इंद्रियों से होता है। अतः शिक्षा में इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है।
- प्राकृतिक नियमों की समझ: बालकों को प्राकृतिक नियमों और विज्ञान के आधार पर तर्कशील बनाना शिक्षा का उद्देश्य है।
- चरित्र निर्माण: यथार्थवाद चरित्र निर्माण को भी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता है। इसमें नैतिकता और अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता है।
- व्यावसायिक दक्षता: यथार्थवादी शिक्षा बालक को भविष्य में आजीविका के लिए तैयार करती है, जिससे वह स्वावलंबी बन सके।
इस प्रकार यथार्थवाद बालक की शिक्षा को यथार्थ, तर्क और विज्ञान पर आधारित बनाता है।
प्रश्न-11. विद्यालय के प्रमुख कार्य कौन-कौनसे हैं?
उत्तर:- विद्यालय समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो न केवल ज्ञान प्रदान करता है बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का माध्यम भी है। विद्यालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
- ज्ञान प्रदान करना: विद्यालय का मुख्य कार्य बच्चों को विभिन्न विषयों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान देना है।
- चरित्र निर्माण: विद्यालय में नैतिक शिक्षा, अनुशासन, और मूल्यों के माध्यम से चरित्र निर्माण किया जाता है।
- सामाजिक विकास: विद्यालय बालकों को सामाजिकता, सहयोग, सह-अस्तित्व और नेतृत्व जैसे गुणों का विकास करता है।
- व्यक्तित्व विकास: विद्यालय विभिन्न पाठ्य और सह-पाठ्य गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक, और भावनात्मक विकास करता है।
- राष्ट्रीय चेतना: विद्यालय राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है।
- रचनात्मकता का विकास: विद्यालय बच्चों को रचनात्मक और नवाचार के लिए प्रेरित करता है।
इस प्रकार विद्यालय एक बहुआयामी संस्था है, जो बालकों को समाज के योग्य नागरिक बनाता है।
प्रश्न-12. भविष्योन्मुखी शिक्षा के ढांचे के लिए महत्वपूर्ण आधार कौन-कौनसे हैं?
उत्तर:- भविष्योन्मुखी शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा जो आने वाली आवश्यकताओं, तकनीकी प्रगति, और सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर दी जाए। इसके महत्वपूर्ण आधार निम्नलिखित हैं:
- तकनीकी साक्षरता: भविष्य की शिक्षा में कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डिजिटल तकनीकों का ज्ञान आवश्यक होगा।
- आजीवन शिक्षा: भविष्य में शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी।
- मूल्य आधारित शिक्षा: नैतिकता, सहिष्णुता और वैश्विक नागरिकता के गुण भविष्य की शिक्षा के मूल आधार होंगे।
- अनुकूलता और नवाचार: बच्चों को परिवर्तनों के अनुसार ढलने और नए विचारों को अपनाने की क्षमता विकसित करनी होगी।
- बहु-विषयक ज्ञान: भविष्योन्मुखी शिक्षा में विभिन्न विषयों के आपसी संबंधों की समझ आवश्यक होगी।
- समावेशी शिक्षा: इसमें सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना जरूरी होगा।
इस प्रकार भविष्योन्मुखी शिक्षा एक लचीला, समावेशी और नवीनता-प्रधान ढांचा होना चाहिए।
प्रश्न-13. समाजवाद के अनुसार जीवन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- समाजवाद एक सामाजिक-राजनीतिक विचारधारा है जो समानता, सामाजिक न्याय और सार्वजनिक कल्याण पर आधारित होती है। समाजवाद के अनुसार जीवन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- सामाजिक समानता: समाजवाद मानता है कि जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति को समान अवसर और संसाधन प्रदान करना है।
- सामूहिक कल्याण: व्यक्ति का कल्याण तब संभव है जब समाज का समुचित विकास हो। अतः व्यक्तिगत लाभ के बजाय सामाजिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है।
- नैतिकता और न्याय: समाजवादी दृष्टिकोण जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और सामाजिक न्याय को महत्वपूर्ण मानता है।
- शोषण-मुक्त जीवन: समाजवाद जीवन में शोषण, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ है, और यह हर वर्ग के लिए समान अधिकारों की वकालत करता है।
- मानवता का विकास: व्यक्ति का उद्देश्य केवल स्वयं का विकास नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की भलाई होनी चाहिए।
इस प्रकार समाजवाद जीवन को एक समग्र, न्यायपूर्ण और मानवतावादी दिशा में ले जाने का प्रयास करता है।
प्रश्न-14. धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का आशय ऐसी शिक्षा से है जो किसी एक धर्म को बढ़ावा न देकर सभी धर्मों का सम्मान करती है और धार्मिक तटस्थता बनाए रखती है। इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं:
- धार्मिक सहिष्णुता: धर्मनिरपेक्ष शिक्षा बच्चों में सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का भाव उत्पन्न करती है।
- विज्ञान और तर्क पर आधारित: यह शिक्षा धार्मिक विश्वासों से ऊपर उठकर तर्क, विज्ञान और अनुभव पर आधारित होती है।
- राष्ट्र निर्माण: धर्मनिरपेक्ष शिक्षा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और लोकतंत्र को मजबूत करती है।
- समाज में सामंजस्य: यह शिक्षा विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है।
- नैतिकता पर बल: धर्मनिरपेक्ष शिक्षा में नैतिक मूल्यों को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है।
धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
प्रश्न-15. भारत में शिक्षा के प्रजातंत्रीकरण पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए।
उत्तर:- भारत में शिक्षा का प्रजातंत्रीकरण (Democratization of Education) का आशय शिक्षा को सभी वर्गों के लिए सुलभ और समान बनाने से है। यह एक सकारात्मक प्रयास है, परंतु इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं।
सकारात्मक पक्ष:
- सर्व शिक्षा अभियान और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम ने शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाया है।
- पिछड़े, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं को विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं।
- ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों ने दूरदराज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा है।
नकारात्मक पक्ष:
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में गुणवत्ता का भारी अंतर है।
- आर्थिक असमानता के कारण गरीब बच्चे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
- निजीकरण ने शिक्षा को व्यापार बना दिया है जिससे शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य कमजोर हुआ है।
इस प्रकार, भारत में शिक्षा का प्रजातंत्रीकरण एक सराहनीय प्रयास है, परंतु इसे प्रभावी बनाने के लिए गुणवत्ता, समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
प्रश्न-16.शिक्षा द्वारा किस प्रकार सांस्कृतिक विलंबन को रोका जा सकता है?
उत्तर:- सांस्कृतिक विलंबन (Cultural Lag) का अर्थ है कि समाज में भौतिक विकास तेजी से होता है लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य धीरे-धीरे बदलते हैं, जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है। शिक्षा इस समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है:
- समकालीन ज्ञान प्रदान करना: शिक्षा नई तकनीकों और वैज्ञानिक खोजों को समाज में तेजी से स्वीकार कराने में मदद करती है।
- संवेदनशीलता का विकास: शिक्षा लोगों को बदलती सामाजिक परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- परंपरा और नवाचार में संतुलन: शिक्षा परंपरागत मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिकता को अपनाने की क्षमता देती है।
- सांस्कृतिक जागरूकता: शिक्षा के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी देकर लोगों में सहिष्णुता और समन्वय की भावना उत्पन्न की जा सकती है।
- समाजिक परिवर्तन में सहायक: शिक्षा सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने और आधुनिक सोच को विकसित करने का माध्यम है।
इस प्रकार शिक्षा सांस्कृतिक विलंबन को कम कर, समाज को संतुलित एवं प्रगतिशील बनाने में सहायक बनती है।
प्रश्न-17. भारतीय दर्शन की मूलभूत विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- भारतीय दर्शन की विशेषताएँ अत्यंत गूढ़ और गहन हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- आध्यात्मिकता पर बल: भारतीय दर्शन आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे विषयों पर केंद्रित है।
- प्रायोगिक दृष्टिकोण: भारतीय दर्शन केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन में उसका प्रयोग भी महत्वपूर्ण मानता है।
- मुक्ति की कामना: प्रत्येक दर्शन की अंतिम मंज़िल मोक्ष या आत्मज्ञान है।
- शास्त्रों पर आधारित: वेद, उपनिषद, गीता आदि शास्त्रों का इसमें प्रमुख स्थान है।
- सर्वात्मवाद: समस्त जीवों में एक ही आत्मा का वास माना गया है।
- कर्म और पुनर्जन्म: भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को महत्त्व दिया गया है।
- सहिष्णुता: यह विभिन्न विचारधाराओं को स्वीकार करता है।
इस प्रकार भारतीय दर्शन न केवल तात्त्विक ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह व्यवहारिक जीवन को भी दिशा देता है।
प्रश्न-18. श्रीकृष्ण को मनोविद कैसे कह सकते हैं ?
उत्तर:- श्रीकृष्ण को मनोविद (Psychologist) कहना उचित है क्योंकि उन्होंने मानव मनोविज्ञान की गहराई को समझते हुए विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सलाह दी।
- गीता में अर्जुन की मानसिक अवस्था को समझना: महाभारत में युद्ध से पूर्व अर्जुन मानसिक भ्रम में पड़ गया था, तब श्रीकृष्ण ने उसे अध्यात्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से मार्गदर्शन दिया।
- भावनात्मक नियंत्रण: श्रीकृष्ण ने सिखाया कि भावनाओं को नियंत्रित कर कार्य करना चाहिए।
- प्रेरणा देना: उन्होंने अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिलाया और प्रेरित किया।
- स्थिति के अनुसार सलाह: श्रीकृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की मनःस्थिति को समझकर यथोचित मार्गदर्शन करते थे।
इन गुणों के कारण श्रीकृष्ण एक श्रेष्ठ मनोविद कहे जा सकते हैं, जिन्होंने न केवल अर्जुन को मानसिक द्वंद्व से उबारा, बल्कि आज भी उनके उपदेश लोगों को मानसिक शांति देते हैं।
प्रश्न-19. परा तथा अपरा विद्या का भेद स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- परा विद्या और अपरा विद्या वेदों में वर्णित दो प्रकार की विद्याएँ हैं।
अपरा विद्या: यह भौतिक ज्ञान है, जैसे वेद, व्याकरण, ज्योतिष, गणित, इतिहास आदि। इसका उद्देश्य सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना है। यह इंद्रियजगत से संबंधित होती है।
परा विद्या: यह आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान है। इसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। यह उच्च ज्ञान है जो आत्मसाक्षात्कार कराता है।
भेद:
अपरा विद्या से हम संसार को समझते हैं, जबकि परा विद्या से स्वयं को।
अपरा ज्ञान से व्यक्ति विद्वान बनता है, पर परा ज्ञान से ज्ञानी और मुक्त होता है।
अपरा विद्या सीमित होती है जबकि परा विद्या असीम होती है।
इस प्रकार परा विद्या आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का साधन है, जबकि अपरा विद्या सांसारिक जीवन के संचालन में सहायक है।
प्रश्न-20. इस्लामिक शिक्षा के लक्ष्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- इस्लाम धर्म में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। “इल्म” (ज्ञान) को ईश्वर के निकट ले जाने वाला साधन माना गया है।
इस्लामिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- अल्लाह की जानकारी देना: विद्यार्थी को यह सिखाना कि वह अल्लाह की रचना का हिस्सा है और उसका जीवन अल्लाह की इबादत के लिए है।
- नैतिकता और चरित्र निर्माण: ईमानदारी, सहिष्णुता, दया, नम्रता, और न्याय जैसे गुणों को विकसित करना।
- मानवता की सेवा: शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी बने।
- शांति और समानता का प्रचार: सभी मनुष्यों को बराबरी से देखना और समाज में सौहार्द बनाए रखना।
इस्लामिक शिक्षा व्यक्ति के आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास को संतुलित रूप से बढ़ावा देती है।
प्रश्न-21. वेदान्त दर्शन के अनुरूप पाठन विधियों के बारे में लिखिए।
उत्तर:- वेदान्त दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की पहचान और मोक्ष की प्राप्ति है। इसकी शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं:
- श्रवण (सुनना): गुरु से उपदेश या ज्ञान सुनना और समझना।
- मनन (चिंतन): सुने गए ज्ञान पर गहराई से विचार करना।
- निदिध्यासन (ध्यान): उस ज्ञान को जीवन में उतारना और आत्मसात करना।
- संवाद विधि: गुरु-शिष्य के मध्य संवाद द्वारा शंका समाधान।
- अनुभव आधारित शिक्षण: ज्ञान को केवल रटना नहीं, बल्कि उसे अनुभव करना प्रमुख है।
वेदान्त शिक्षण में बाह्य साधनों से अधिक आत्मिक जागृति और आत्मानुभूति पर बल दिया जाता है। यह शिक्षण विधियाँ आत्मिक उन्नति में सहायक होती हैं।
प्रश्न-22. शान्तिनिकेतन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:-शान्तिनिकेतन की स्थापना रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है।
इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा: यहाँ शिक्षा प्रकृति के निकट दी जाती है, जिससे विद्यार्थी का समग्र विकास हो।
- गुरुकुल पद्धति: शिक्षक और छात्र का रिश्ता पारंपरिक भारतीय शैली में होता है।
- साहित्य, कला और संगीत का समावेश: यहाँ रचनात्मक विषयों को विशेष स्थान प्राप्त है।
- अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण: शांति निकेतन ने विश्वभारती विश्वविद्यालय के माध्यम से वैश्विक संस्कृति को भी अपनाया।
यह एक ऐसा संस्थान है जहाँ भारतीय संस्कृति और आधुनिक विचारधारा का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है।
प्रश्न-23. हेगल का द्वन्द्ववाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:-हेगल एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने द्वन्द्ववाद (Dialecticism) की संकल्पना दी।
हेगल के अनुसार विचार की प्रगति तीन चरणों में होती है:
- थीसिस (Thesis): प्रारंभिक विचार या स्थिति।
- एंटीथीसिस (Antithesis): थीसिस का विरोध या उसका विपरीत।
- सिंथेसिस (Synthesis): दोनों का मिलन जो एक नई स्थिति उत्पन्न करता है।
हेगल का मानना था कि संसार की हर चीज़ परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन द्वंद्व के माध्यम से होता है। इस सिद्धांत का प्रभाव दर्शन, इतिहास, राजनीति और शिक्षा पर भी पड़ा।
उनका यह विचार ज्ञान और विचारों के विकास की गहन प्रक्रिया को दर्शाता है, जो आज भी उपयोगी सिद्ध होता है।
प्रश्न-24. यान्त्रिक प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद में क्या अंतर है?
उत्तर:- यान्त्रिक प्रकृतिवाद (Mechanical Naturalism):
यह मानता है कि मनुष्य एक मशीन की तरह है।
इसमें चेतना, आत्मा या भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती।
यह केवल भौतिक नियमों और कार्यों पर आधारित होता है।
शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक और बौद्धिक विकास माना जाता है।
जैविक प्रकृतिवाद (Biological Naturalism):
यह मनुष्य को एक जीवधारी मानता है, जो विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है।
इसमें मनुष्य की संवेदनाएँ, भावनाएँ और अनुकूलन की शक्ति को महत्व दिया जाता है।
यह शिक्षा में पर्यावरण, अनुभव और अनुकूलन को प्राथमिकता देता है।
अंतर: यान्त्रिक प्रकृतिवाद केवल मशीनी ढंग से सोचता है जबकि जैविक प्रकृतिवाद जीवन की जटिलता और विकासशील प्रकृति को स्वीकार करता है।
प्रश्न-25. जैन धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:-जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्म है जिसकी स्थापना भगवान ऋषभदेव ने की थी, परंतु इसके अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को इसका व्यावहारिक प्रवर्तक माना जाता है।
इस धर्म के मुख्य सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म आत्मा की शुद्धता और मोक्ष प्राप्ति को सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। इसमें कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य, और संयम को प्रमुख स्थान प्राप्त है।
अहिंसा का पालन इतना कठोर है कि जैन साधु चलते समय भूमि पर झाड़ू लगाकर चलते हैं ताकि किसी जीव की हत्या न हो।
विशेषताएँ:
यह कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है।
यह ईश्वर को सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता नहीं मानता, बल्कि आत्मा की मुक्ति पर बल देता है।
जैन धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त है, क्योंकि यह अनेकांतवाद के माध्यम से हर विषय को कई दृष्टिकोणों से देखने की प्रेरणा देता है।
प्रश्न-26. वेदान्त दर्शन में तत्व मीमांसा के बारे में लिखिए।
उत्तर:- वेदान्त दर्शन में तत्व मीमांसा अर्थात मेटाफिज़िक्स का प्रमुख विषय ब्रह्म, आत्मा और जगत का स्वरूप है। इसके अनुसार “ब्रह्म सत्य है, जगत माया है और जीव ब्रह्म का ही अंश है।”
ब्रह्म— यह एक निराकार, सर्वव्यापी, अनादि और अविनाशी तत्व है। इसे सत् (अस्तित्व), चित् (चेतना) और आनन्द (सुख) स्वरूप माना गया है।
आत्मा— आत्मा को ब्रह्म का ही अंश माना गया है। आत्मा अविनाशी है, लेकिन अज्ञान के कारण वह स्वयं को शरीर मान बैठती है।
जगत— वेदान्त के अनुसार यह संसार माया है, जो अस्थायी और बदलता रहता है।
तत्व मीमांसा की विशेषता यह है कि यह आत्मा की मुक्ति को ही अंतिम लक्ष्य मानता है और ज्ञान को मुक्ति का साधन बताता है।
इसमें ब्रह्म और आत्मा की एकता पर बल दिया गया है, जो अद्वैतवाद की मूल भावना है।
प्रश्न-27. शिक्षा किस प्रकार समाज में परिवर्तन ला सकती है?
उत्तर:-शिक्षा समाज में परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण, विचारधारा, और व्यवहार को बदलती है।
- चेतना का विकास: शिक्षा व्यक्ति को जागरूक बनाती है। इससे वह अंधविश्वास, रूढ़ियों और सामाजिक बुराइयों से लड़ने में सक्षम होता है।
- समानता की भावना: शिक्षा जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव को मिटाने में मदद करती है और एक समतामूलक समाज की रचना करती है।
- आर्थिक उन्नति: शिक्षित व्यक्ति नौकरी, व्यवसाय आदि के माध्यम से समाज में आर्थिक विकास लाता है।
- लोकतांत्रिक मूल्य: शिक्षा व्यक्ति को अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराती है, जिससे वह जिम्मेदार नागरिक बनता है।
इस प्रकार शिक्षा केवल ज्ञान का साधन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का इंजन है। यह समाज को प्रगतिशील, सहिष्णु और न्यायपूर्ण बनाती है।
प्रश्न-28. राजनीति किस प्रकार शिक्षा से संबंधित है?
उत्तर:-राजनीति और शिक्षा का गहरा संबंध है क्योंकि शिक्षा नीति का निर्धारण राजनीतिक निर्णयों के माध्यम से होता है।
- नीति निर्माण: शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम और बजट सरकार द्वारा तय किए जाते हैं।
- संसाधन वितरण: विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके संचालन के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है।
- सामाजिक न्याय: राजनीतिक निर्णयों से ही शिक्षा में आरक्षण, समानता, और विशेष योजनाएं लागू होती हैं।
- वैचारिक प्रभाव: राजनीतिक विचारधारा शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे पाठ्यक्रम में बदलाव होते हैं।
इस प्रकार राजनीति शिक्षा को दिशा देती है और शिक्षा समाज में राजनीतिक जागरूकता लाती है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।
प्रश्न-29. शिक्षा का प्रजातांत्रीकरण पर संक्षेप में लिखिए
उत्तर:-शिक्षा का प्रजातांत्रीकरण (Democratization of Education) का अर्थ है—हर वर्ग, जाति, लिंग और क्षेत्र के व्यक्ति को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना।
इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा केवल गरीबी, लिंगभेद या सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।
मुख्य विशेषताएँ:
समानता पर आधारित शिक्षा प्रणाली
निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा
लड़कियों, विकलांगों और पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर
डिजिटल शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सुलभता
प्रजातांत्रिक शिक्षा से हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। यह एक सशक्त और समतामूलक समाज की नींव है।
प्रश्न-30.मानवतावादी प्रयोजनवाद और प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद में अन्तर लिखिए।
उत्तर:- मानवतावादी प्रयोजनवाद और प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद प्रयोजनवाद (Pragmatism) के दो प्रमुख रूप हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि अलग है।
मानवतावादी प्रयोजनवाद का उद्देश्य मनुष्य के सम्पूर्ण विकास पर केंद्रित होता है। यह दर्शन व्यक्ति की भावनाओं, इच्छाओं, मूल्यों और आत्मा के विकास को महत्त्व देता है। विलियम जैम्स इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। यह शिक्षा को आत्मा के विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति का माध्यम मानता है। इसमें नैतिकता, स्वतंत्रता, सह-अस्तित्व और करुणा पर विशेष बल होता है।
प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद का मूल उद्देश्य वैज्ञानिक प्रयोग, अनुभव और परीक्षण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना है। इसके प्रमुख प्रवर्तक जॉन ड्यूई हैं। यह दर्शन मानता है कि शिक्षा एक सतत प्रयोगात्मक प्रक्रिया है जहाँ विद्यार्थी समस्या को पहचानकर, उसका समाधान ढूँढकर सीखता है। इसमें ‘करते हुए सीखो’ (learning by doing) को प्राथमिकता दी जाती है।
अतः मानवतावादी प्रयोजनवाद व्यक्ति के आंतरिक विकास को प्राथमिकता देता है जबकि प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद बाह्य अनुभवों और प्रयोगों द्वारा समस्या-समाधान को महत्त्व देता है।
Section-C
प्रश्न-1.डॉ. राधाकृष्णन के शिक्षा सम्बन्धी विचारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षक एवं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। उन्होंने शिक्षा को मानव जीवन के समग्र विकास का माध्यम माना। उनके शिक्षा संबंधी विचारों में भारतीय संस्कृति, नैतिकता, धर्म, तथा अध्यात्म का समावेश था।
डॉ. राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करना, नैतिक मूल्यों की स्थापना करना और व्यक्ति को आत्मबोध की ओर ले जाना है। वे कहते थे कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति को आत्म-साक्षात्कार की ओर प्रेरित करना है जिससे वह ‘सत्य’ को जान सके।
उन्होंने शिक्षक की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार शिक्षक समाज का पथप्रदर्शक होता है। शिक्षक केवल ज्ञानदाता नहीं, बल्कि प्रेरणादाता होता है। उन्होंने यह भी कहा कि “सच्चा शिक्षक वह है जो छात्रों के हृदय को छू सके।”
उनका मानना था कि शिक्षा को धर्म और नैतिकता से जोड़ा जाना चाहिए। वे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की भौतिकतावादी प्रवृत्तियों से असंतुष्ट थे और भारतीय शिक्षा प्रणाली की आध्यात्मिक परंपराओं को प्राथमिकता देते थे। वे शिक्षा के माध्यम से ‘राष्ट्र निर्माण’ पर बल देते थे।
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा में स्वतंत्रता, रचनात्मकता और विवेक को बढ़ावा मिलना चाहिए। विद्यार्थी को केवल रटंत प्रणाली से बाहर लाकर, चिंतनशील और मानवतावादी बनाया जाना चाहिए।
निष्कर्षतः, डॉ. राधाकृष्णन की शिक्षा-दृष्टि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिकता और अध्यात्म पर आधारित थी। उनका शिक्षा-दर्शन आज भी प्रासंगिक है और समग्र शिक्षा-प्रणाली के विकास के लिए प्रेरणादायक है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.शिक्षा और मानवीकरण पर निबंध लिखिए।
उत्तर:-मानवीकरण का तात्पर्य है—व्यक्ति को मानवोचित गुणों से सम्पन्न बनाना, जैसे सहानुभूति, करुणा, नैतिकता, न्याय एवं सामाजिक चेतना। शिक्षा इस मानवीकरण की प्रक्रिया का मूल साधन है।
शिक्षा और मानवीकरण का संबंध:
शिक्षा केवल ज्ञान, जानकारी या तकनीकी दक्षता का नाम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को एक बेहतर मानव बनाने की प्रक्रिया है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल बुद्धिजीवी होता है, बल्कि वह संवेदनशील, उत्तरदायी एवं नैतिक होता है। जब शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी तक सीमित हो जाता है, तो वह मानवीकरण की प्रक्रिया को क्षीण कर देती है।
मानवीकरण के प्रमुख पहलू:
- नैतिक विकास – शिक्षा व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, न्याय आदि मूल्यों का विकास करती है।
- सामाजिक उत्तरदायित्व – शिक्षा व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है।
- संवेदनशीलता और करुणा – शिक्षा से व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को समझता है और सेवा भावना विकसित करता है।
- आत्मबोध – शिक्षा व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है।
आज की स्थिति:
वर्तमान समय में शिक्षा अधिकतर व्यावसायिक और तकनीकी बनती जा रही है, जिसमें मानवीय मूल्यों की उपेक्षा होती है। ऐसे में आवश्यक है कि शिक्षा को पुनः मानवीकरण की दिशा में मोड़ा जाए।
शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण हो। शिक्षा का मानवीकरण वर्तमान समय की अनिवार्यता है।
प्रश्न-3. अद्वैत वेदांत दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं?
उत्तर:- अद्वैत वेदांत दर्शन भारतीय चिंतन की एक महान धारा है, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की। इस दर्शन के अनुसार ‘ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और आत्मा ब्रह्म के समान है।’ इस विचारधारा के शैक्षिक निहितार्थ गहरे और व्यापक हैं।
मुख्य शैक्षिक निहितार्थ:
- स्व-ज्ञान और आत्मबोध: शिक्षा का उद्देश्य आत्मा के स्वरूप को जानना और आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करना होना चाहिए।
- एकता और समत्व का भाव: अद्वैत वेदांत व्यक्ति और ब्रह्म में कोई भेद नहीं मानता। यह शिक्षा में समानता, समरसता और वैश्विक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है।
- नैतिक शिक्षा: आत्मा के ज्ञान से व्यक्ति में नैतिकता, संयम और सत्यनिष्ठा आती है।
- गुरु-शिष्य परंपरा: इस दर्शन में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा में व्यक्तिगत मार्गदर्शन को महत्व दिया जाता है।
- आध्यात्मिक विकास: शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आत्मा के जागरण और आध्यात्मिक उन्नति को भी साधे।
वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव:
आज की भौतिकवादी शिक्षा प्रणाली में आत्मा, नैतिकता और आध्यात्मिकता की उपेक्षा हो रही है। अद्वैत वेदांत इस ओर संकेत करता है कि हमें शिक्षा को पुनः आत्मबोध और चरित्र निर्माण की ओर केंद्रित करना चाहिए।
अद्वैत वेदांत शिक्षा को एक उच्च साधना मानता है। इसके शैक्षिक निहितार्थ व्यक्ति के समग्र विकास और मानव समाज में एकता, नैतिकता और शांति की स्थापना हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
प्रश्न-4. श्रीमद्भगवद्गीता में निहित शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा की संकल्पना का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- श्रीमद्भगवद्गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक गहन शिक्षाशास्त्रीय ग्रंथ भी है। इसमें जीवन, कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग से संबंधित गहन शिक्षाएं दी गई हैं। इसकी शिक्षाएँ आज भी मानव जीवन को दिशा देने में सक्षम हैं।
- शिक्षा की संकल्पना:
गीता के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की पहचान, धर्म पालन और कर्मयोग है। यह व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग करती है तथा उसे स्थिर बुद्धि, विवेक और आत्मसंयम की ओर प्रेरित करती है। - शिक्षा के उद्देश्य:
आत्मबोध एवं आत्मानुशासन
कर्तव्य परायणता
नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास
सर्वांगीण विकास
संघर्षशील जीवन में स्थिरता प्राप्त करना
- पाठ्यक्रम:
गीता में कोई पारंपरिक पाठ्यक्रम नहीं दिया गया, लेकिन इसके मुख्य विषय निम्न हैं:
ज्ञान योग (बुद्धि और विवेक का विकास)
भक्ति योग (आध्यात्मिक आस्था का विकास)
कर्म योग (कर्तव्य निर्वहन का अभ्यास)
सांख्य योग (विवेकपूर्ण निर्णय लेना)
संयम और इंद्रियनिग्रह
- शिक्षक-शिष्य संबंध:
गीता का संवाद अर्जुन (शिष्य) और कृष्ण (गुरु) के बीच हुआ, जो आदर्श शिक्षक-शिष्य संबंध को दर्शाता है। गुरु न केवल ज्ञान देता है, बल्कि शिष्य को जीवन की दिशा भी दिखाता है।
श्रीमद्भगवद्गीता एक जीवनोपयोगी शिक्षाशास्त्रीय ग्रंथ है। इसकी शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को आत्मबोध, कर्तव्यनिष्ठा और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में गीता की शिक्षाओं को शामिल करना समय की आवश्यकता है।
प्रश्न-5. भारतीय दर्शन की मूलभूत विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- भारतीय दर्शन की विशेषताएँ अत्यंत गूढ़ और गहन हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- आध्यात्मिकता पर बल: भारतीय दर्शन आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे विषयों पर केंद्रित है।
- प्रायोगिक दृष्टिकोण: भारतीय दर्शन केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन में उसका प्रयोग भी महत्वपूर्ण मानता है।
- मुक्ति की कामना: प्रत्येक दर्शन की अंतिम मंज़िल मोक्ष या आत्मज्ञान है।
- शास्त्रों पर आधारित: वेद, उपनिषद, गीता आदि शास्त्रों का इसमें प्रमुख स्थान है।
- सर्वात्मवाद: समस्त जीवों में एक ही आत्मा का वास माना गया है।
- कर्म और पुनर्जन्म: भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को महत्त्व दिया गया है।
- सहिष्णुता: यह विभिन्न विचारधाराओं को स्वीकार करता है।
इस प्रकार भारतीय दर्शन न केवल तात्त्विक ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह व्यवहारिक जीवन को भी दिशा देता है।
प्रश्न-6. बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धान्त के बारे में विस्तार से लिखिए।
उत्तर:- बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धान्त अत्यंत गहन, वैज्ञानिक और तर्कसंगत हैं। इन सिद्धान्तों का उद्देश्य मानव जीवन के दुःखों को समझना और उनसे मुक्ति पाना है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन की वास्तविकताओं को स्पष्ट करते हुए चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को जीवन का आधार बताया।
- चार आर्य सत्य (Four Noble Truths):
- दुःख – जीवन में दुःख है। जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था, बिछोह आदि सभी दुःख हैं।
- दुःख का कारण – तृष्णा (इच्छा) ही समस्त दुःखों की जड़ है।
- दुःख निरोध – तृष्णा का अंत ही दुःखों का अंत है।
- दुःख निरोध का मार्ग – अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है।
- अष्टांगिक मार्ग (Eightfold Path):
- सम्यक दृष्टि
- सम्यक संकल्प
- सम्यक वाक्
- सम्यक कर्म
- सम्यक आजीविका
- सम्यक प्रयास
- सम्यक स्मृति
- सम्यक समाधि
- अनित्य (Impermanence):
बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि यह संसार नश्वर है। सभी वस्तुएँ बदलती रहती हैं। यह परिवर्तनशीलता ही संसार का सत्य है।
- अनात्मवाद (No Soul Theory):
बुद्ध ने आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नकारा। उन्होंने कहा कि पाँच स्कंध (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) ही व्यक्ति का गठन करते हैं, आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं है।
- प्रतीत्यसमुत्पाद (Dependent Origination):
यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक वस्तु या घटना किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है। कुछ भी स्वतः उत्पन्न नहीं होता।
- मध्यम मार्ग (Middle Path):
बुद्ध ने जीवन के दोनों अतियों (भोगवाद और कठोर तप) से बचकर मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी।
बौद्ध दर्शन एक तर्कपूर्ण और व्यावहारिक पथ है जो मानव को स्वयं के आचरण, चिंतन और आत्मविकास के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की राह दिखाता है।
प्रश्न-7. स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक और सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान चिंतक, संत और राष्ट्रनिर्माता थे। उनके दर्शन में भारतीय संस्कृति, वेदांत और मानवता का गहन समन्वय मिलता है।
दार्शनिक विचार:
- अद्वैत वेदांत – उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए कहा कि “संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही ब्रह्म तत्व से बना है।” हर जीव में वही ईश्वर निवास करता है।
- आत्मा की एकता – उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में दिव्यता है और उसका उद्देश्य उसी दिव्यता को जानना है।
- प्रैक्टिकल वेदांत – उन्होंने वेदांत को जीवन में व्यावहारिक रूप में अपनाने पर बल दिया, जैसे सेवा, करुणा और नैतिकता।
- धर्म की व्याख्या – विवेकानंद का मानना था कि धर्म का उद्देश्य केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है।
सामाजिक विचार:
- शिक्षा पर बल – वे शिक्षा को मनुष्य निर्माण का सबसे बड़ा साधन मानते थे। उनका कहना था, “शिक्षा वह है जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके।”
- नारी सशक्तिकरण – उन्होंने कहा कि जब तक नारी को सम्मान और समान अवसर नहीं मिलेगा, भारत का उत्थान असंभव है।
- जातिवाद और छुआछूत के विरोधी – उन्होंने जाति-भेद को सामाजिक बुराई मानते हुए समता और भाईचारे की बात की।
- राष्ट्रीयता और आत्मगौरव – उन्होंने युवाओं को देश के प्रति समर्पित करने का आह्वान किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने को कहा।
स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने भारतीय समाज को आत्मबोध, आत्मगौरव और सेवा का मार्ग दिखाया।
प्रश्न-8. सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है? विस्तार से लिखिए।
उत्तर:- सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा:
सांस्कृतिक परिवर्तन का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो समय के साथ समाज की मान्यताओं, परंपराओं, रीति-रिवाजों, मूल्य-व्यवस्थाओं, जीवन शैली आदि में होते हैं। यह परिवर्तन प्राकृतिक, सामाजिक, तकनीकी, आर्थिक या राजनीतिक कारणों से हो सकता है।
सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण:
- प्रौद्योगिकी में विकास (जैसे इंटरनेट, मोबाइल)
- शिक्षा का प्रसार
- आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण
- संचार माध्यमों का प्रभाव (टीवी, सोशल मीडिया)
- धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन
शिक्षा की भूमिका:
शिक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण वाहक है। यह समाज को नवीन विचारों से जोड़ती है और पुरानी रूढ़ियों को चुनौती देती है।
- चेतना का विकास: शिक्षा व्यक्ति में आत्मबोध और सामाजिक चेतना लाती है जिससे वह सांस्कृतिक सुधार की दिशा में सोचता है।
- नवाचार की प्रेरणा: शिक्षा लोगों को नवीन तकनीकों और विचारों को अपनाने के लिए तैयार करती है।
- समाज में समानता लाना: शिक्षा जाति, लिंग, धर्म के भेद को मिटाकर समता और बंधुत्व को बढ़ावा देती है।
- मूल्य शिक्षा: शिक्षा द्वारा नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन होता है, जो स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है।
- वैश्विक दृष्टिकोण: शिक्षा व्यक्ति को केवल स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक नागरिक बनाती है, जिससे विविध संस्कृतियों का समावेश होता है।
सांस्कृतिक परिवर्तन समाज का स्वाभाविक अंग है और शिक्षा इसके संचालन एवं दिशा निर्धारण में एक प्रमुख भूमिका निभाती है।
प्रश्न-9. मानवीय शक्ति नियोजन क्या है? इसकी भारत में आवश्यकता क्यों है?
उत्तर:- मानवीय शक्ति नियोजन की परिभाषा:
मानवीय शक्ति नियोजन (Manpower Planning) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संस्था या राष्ट्र को वर्तमान और भविष्य में आवश्यक मानव संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता का आकलन कर उसकी पूर्ति की योजना बनाई जाती है।
यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि देश या संस्था के पास आवश्यक संख्या में योग्य, प्रशिक्षित और सक्षम जनशक्ति उपलब्ध हो।
मानवीय शक्ति नियोजन के तत्व:
- उपलब्ध जनशक्ति का मूल्यांकन
- भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान
- प्रशिक्षण और विकास की रणनीति
- बेरोजगारी या अधिकता की स्थिति में समाधान
भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है?
- जनसंख्या वृद्धि: भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, जहां जनशक्ति की अधिकता है लेकिन उचित नियोजन के अभाव में यह उत्पादक नहीं बन पाती।
- बेरोजगारी की समस्या: यदि मानव संसाधनों का उचित प्रशिक्षण और नियोजन न हो, तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती है।
- औद्योगीकरण और डिजिटल युग: तकनीकी प्रगति के साथ श्रमिकों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है।
- शिक्षा और कौशल में असंतुलन: शिक्षा व्यवस्था अक्सर नौकरी की मांग के अनुरूप कौशल नहीं दे पाती, जिससे युवाओं का क्षमता विकास नहीं हो पाता।
- आर्थिक विकास: संगठित और प्रशिक्षित जनशक्ति आर्थिक वृद्धि में सहायक होती है।
- समाजिक असमानता का समाधान: उचित मानवीय शक्ति नियोजन से पिछड़े वर्गों को रोजगार और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता है।
भारत जैसे विकासशील देश में मानवीय शक्ति नियोजन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है, बल्कि देश की समग्र प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रश्न-10. अस्तित्ववाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा ? विस्तार से लिखिए।
उत्तर:- अस्तित्ववाद (Existentialism) एक दार्शनिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, चयन, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल देती है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रभाव बहुत गहरा रहा है, विशेष रूप से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में।
अस्तित्ववाद की प्रमुख मान्यताएँ:
- व्यक्ति की प्राथमिकता: अस्तित्ववाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों, सोच और निर्णयों के द्वारा अपना अस्तित्व गढ़ता है।
- स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व: हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार भी है।
- चयन का महत्व: विद्यार्थी को अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। शिक्षा उसे सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करे।
- अर्थ की खोज: शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं कि वह केवल जानकारी दे, बल्कि यह कि विद्यार्थी अपने जीवन का उद्देश्य और अर्थ स्वयं खोजे।
शिक्षा पर प्रभाव:
- विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा: अस्तित्ववाद शिक्षा को विद्यार्थी के अनुभवों और रुचियों पर आधारित बनाता है।
- नैतिक शिक्षा पर बल: यह दर्शन नैतिक निर्णय लेने और जीवन में जिम्मेदार बनने की शिक्षा देता है।
- शिक्षक की भूमिका: शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक होता है जो विद्यार्थी को आत्म-खोज में सहायता करता है।
- स्वतंत्रता की शिक्षा: विद्यार्थी को सोचने, प्रश्न करने और अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।
अस्तित्ववाद का शिक्षा पर प्रभाव यह है कि उसने शिक्षा को अधिक मानवीय, नैतिक और व्यक्ति-केंद्रित बना दिया है। यह दर्शन विद्यार्थियों को अपने जीवन का मार्ग स्वयं तय करने की क्षमता देता है।
प्रश्न-11. शिक्षा में आर्थिक विकास की भूमिका लिखिए।
उत्तर:- शिक्षा और आर्थिक विकास के बीच गहरा संबंध होता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षित मानव संसाधन अनिवार्य होता है। शिक्षा न केवल व्यक्तियों की क्षमताओं को बढ़ाती है, बल्कि देश की उत्पादन क्षमता और आय स्तर को भी सुधारती है।
आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका:
- मानव पूंजी का निर्माण: शिक्षा एक निवेश है जो प्रशिक्षित, कुशल और नवाचारी जनशक्ति तैयार करती है। इससे उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
- रोजगार के अवसर: शिक्षा से व्यक्ति योग्य बनता है जिससे वह बेहतर नौकरी प्राप्त कर सकता है और आर्थिक रूप से सक्षम हो सकता है।
- उद्यमिता को बढ़ावा: शिक्षित व्यक्ति नए व्यवसाय शुरू करने में सक्षम होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।
- गरीबी उन्मूलन: शिक्षा से लोग बेहतर आय अर्जित कर सकते हैं जिससे गरीबी घटती है।
- तकनीकी विकास: उच्च शिक्षा और तकनीकी ज्ञान से नए आविष्कार और नवाचार संभव होते हैं जो आर्थिक प्रगति को गति देते हैं।
- महिला सशक्तिकरण: जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वे भी आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती हैं जिससे समाज और देश दोनों को लाभ होता है।
शिक्षा किसी भी देश की आर्थिक नींव होती है। यह न केवल व्यक्ति के विकास का माध्यम है, बल्कि पूरे राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का स्रोत भी है।
प्रश्न-12. जैन धर्म के अनीश्वरवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:-जैन धर्म एक अनीश्वरवादी दर्शन है, जिसका अर्थ है कि यह ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता या सृष्टि के रचयिता के रूप में किसी ईश्वर को नहीं मानता। जैन दर्शन के अनुसार यह संसार स्वतः ही कार्यरत है और इसका संचालन किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा नहीं किया जाता। जैन धर्म मानता है कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र, अनादि और शुद्ध है, तथा मोक्ष की प्राप्ति आत्मा के अपने प्रयासों से संभव है न कि किसी ईश्वर की कृपा से।
जैन विचारधारा के अनुसार, संसार छह द्रव्यों (जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल) से बना है और ये द्रव्य शाश्वत हैं। इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं मानी जाती। जैन धर्म में तीर्थंकरों की पूजा की जाती है, परंतु उन्हें ईश्वर नहीं माना जाता बल्कि वे सिद्ध पुरुष होते हैं जिन्होंने आत्म-साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त किया होता है। इस प्रकार, जैन धर्म आत्मनिर्भरता, तप, अहिंसा और नैतिक जीवन पर आधारित है और सृष्टि तथा मोक्ष की व्याख्या किसी ईश्वरीय हस्तक्षेप के बिना करता है।
प्रश्न-13. वर्कले के व्यक्तिवादी आदर्शवाद के बारे में चर्चा कीजिए।
उत्तर:- वर्कले (George Berkeley) अठारहवीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक थे जिन्होंने व्यक्तिवादी आदर्शवाद (Subjective Idealism) का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार “अस्तित्व का अर्थ है अनुभूति करना” (Esse est percipi)। इसका आशय यह है कि किसी वस्तु का अस्तित्व तभी है जब उसे कोई अनुभव करता है।
मुख्य सिद्धांत:
- मन ही अंतिम सत्य है – वर्कले के अनुसार केवल चेतन मन और उसकी धारणाएँ ही वास्तविक हैं, भौतिक वस्तुएँ केवल अनुभूति का परिणाम हैं।
- भौतिकता का निषेध – वर्कले ने यह कहा कि किसी वस्तु का अस्तित्व केवल तभी है जब वह हमारे मन में अनुभव के रूप में उपस्थित हो।
- ईश्वर की भूमिका – वे मानते थे कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नहीं देख रहा होता, तब भी वह वस्तु ईश्वर द्वारा अनुभव की जाती है, इसलिए उसका अस्तित्व बना रहता है।
शिक्षा के क्षेत्र में वर्कले के विचार यह दर्शाते हैं कि ज्ञान केवल अनुभवों और चेतन मन की गतिविधियों पर आधारित होता है। अतः शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव और धारणाओं को महत्व देना चाहिए।
प्रश्न-14. समाजवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए?
उत्तर:- समाजवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ समानता, सामाजिक न्याय, सहयोग और वर्गहीनता हो। समाजवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि समाज के समग्र विकास का माध्यम है।
- सामाजिक समानता – समाजवादी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देती है ताकि किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक भेदभाव न हो।
- आर्थिक न्याय – शिक्षा को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और पूंजीवादी शोषण से बच सके।
- सहयोग की भावना – समाजवाद प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग और सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। शिक्षा में समूह कार्य, सह-अध्ययन, और सामूहिक उत्तरदायित्व को महत्त्व दिया जाता है।
- नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व – शिक्षा व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है, जिससे वह राष्ट्र के विकास में सहभागी बन सके।
- राजनीतिक जागरूकता – समाजवादी शिक्षा विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग बनाती है।
इस प्रकार समाजवादी शिक्षा का उद्देश्य एक समतामूलक, नैतिक और जागरूक समाज की स्थापना करना है।
प्रश्न-15. विद्यालय के चार प्रमुख कार्य लिखिए।
उत्तर:- विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं होता, बल्कि यह समाज निर्माण और व्यक्तित्व विकास का मुख्य स्थान होता है। इसके चार प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
- बौद्धिक विकास (Intellectual Development): विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को विकसित करना है। इसके अंतर्गत भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है जिससे सोचने, समझने और विश्लेषण करने की शक्ति बढ़ती है।
- नैतिक एवं चारित्रिक विकास (Moral and Character Development): विद्यालय विद्यार्थियों में नैतिकता, ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास करता है।
- सामाजिक विकास (Social Development): विद्यालय में सामूहिक गतिविधियाँ, खेलकूद, समूह कार्य आदि से विद्यार्थियों में सामाजिकता, नेतृत्व क्षमता और सह-अस्तित्व की भावना उत्पन्न होती है।
- व्यावसायिक तैयारी (Vocational Preparation): आधुनिक विद्यालयों में छात्रों को भविष्य के व्यावसायिक जीवन के लिए भी तैयार किया जाता है जैसे कि कौशल प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन आदि।
इस प्रकार विद्यालय सर्वांगीण विकास का केंद्र होता है।
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE
vmou maed-01 paper , vmou ma 1st year exam paper , vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4