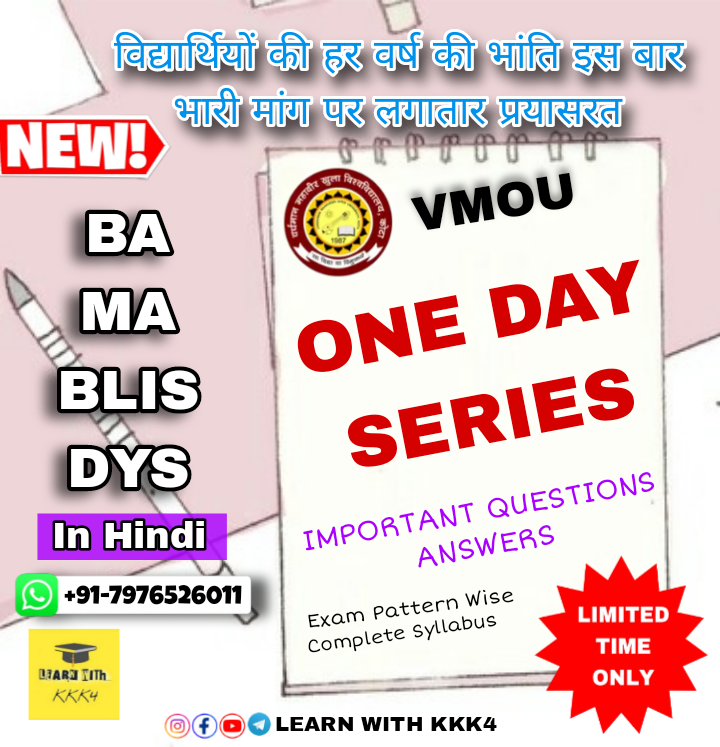VMOU MAED-06 Paper MA Final Yearr ; vmou exam paper
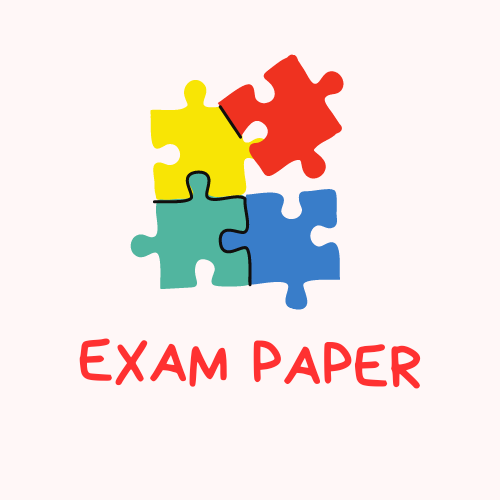
VMOU MA Final Year के लिए Education ( MAED-06 , ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.दूरस्थ शिक्षा की पाँच अवस्थाओं के नाम लिखिए।
उत्तर:- पत्राचार शिक्षा, 2. मल्टीमीडिया शिक्षा, 3. टेली-शिक्षा, 4. ऑनलाइन शिक्षा, 5. आभासी शिक्षा (Virtual Learning)।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.CD ROM का पूर्ण नाम लिखिए।
उत्तर:- CD ROM का पूर्ण नाम है – Compact Disc Read Only Memory।
प्रश्न-3.दूरस्थ शिक्षा की पाँच अवस्थाएँ कौन-कौनसी हैं?
उत्तर:- 1. पत्राचार शिक्षा,2. मल्टीमीडिया शिक्षा,3. टेली-लर्निंग,4. ऑनलाइन शिक्षा,5. इमर्सिव (AI/VR आधारित) शिक्षा।
प्रश्न-4. भारत का प्रथम राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का क्या नाम है?
उत्तर:- आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे अब डॉ. बी.आर. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है,-1982 ME
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-5. स्व-अधिगम सामग्रियाँ लिखने की कोई चार तकनीकें लिखिए।
उत्तर:- 1) संवादात्मक शैली, (2) स्व-परीक्षण प्रश्न, (3) सरल भाषा, (4) उद्देश्य आधारित लेखन।
प्रश्न-6. URL का फुल फॉर्म क्या है?
उत्तर:- Uniform Resource Locator, जो किसी वेब पते को दर्शाता है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-7. एम-लर्निंग के मुख्य लाभ क्या हैं?
उत्तर:- एम-लर्निंग में शिक्षा कभी भी और कहीं भी मोबाइल उपकरणों के माध्यम से संभव होती है; यह लचीलापन, सहजता और इंटरैक्टिव अधिगम को बढ़ाता है।
प्रश्न-8. श्रव्य-दृश्य सामग्री के कोई दो लाभ लिखिए।
उत्तर:- श्रव्य-दृश्य सामग्री से शिक्षा रोचक बनती है, समझ आसान होती है और दृश्य उदाहरणों से ज्ञान की पकड़ मजबूत होती है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-9. शिक्षा का औद्योगिकीकृत रूप का सिद्धान्त किसके द्वारा दिया गया है ?
उत्तर:-इवान इलीच (Ivan Illich) और अन्य आधुनिक शिक्षाशास्त्रियों द्वारा दिया गया, जिन्होंने शिक्षा को उत्पादन प्रणाली से जोड़कर देखा।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-10. एस.एन.डी.टी. प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई?
उत्तर:- इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में डॉ. धुनीवाला रामाबाई रणाडे और भरत रत्न डॉ. धोंडो केशव कर्वे ने की थी।
प्रश्न-11. टेलीटेक्स्ट से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- टेलीटेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट आधारित सूचना सेवा है जो टेलीविजन स्क्रीन पर शैक्षिक और सूचना सामग्री प्रदर्शित करती है।—
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-12. विश्व के किन्हीं दो वर्चुअल विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए।
उत्तर:- IGNOU, VMOU, (UK Open University), (Athabasca University, Canada)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-13. इग्नू की पाँच प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:-इग्नू की प्रमुख विशेषताएँ हैं: खुला प्रवेश, लचीलापन, श्रेयांक प्रणाली, विविध पाठ्यक्रम, और तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन।
प्रश्न-14. “दूरस्थ शिक्षा दिशा-निर्देशित शैक्षिक वार्तालाप है।” यह कथन किसके द्वारा दिया गया है?
उत्तर:- बोरो जे. होल्मबर्ग (Börje Holmberg)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-15. दूरस्थ शिक्षा में ISD का पूर्ण नाम क्या है?
उत्तर:- ISD का पूर्ण नाम है “Instructional System Design” अर्थात् शिक्षण प्रणाली अभिकल्पना।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-16. आवश्यकता सर्वेक्षण से क्या अभिप्राय है?
उत्तर:- यह एक प्रक्रिया है जिससे यह ज्ञात किया जाता है कि लक्षित शिक्षार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा, पाठ्यक्रम या सुविधा की आवश्यकता है।
प्रश्न-17. डिजिटल सेल्युलर सिस्टम (DCS) 1800 की शुरुआत कब हुई?
उत्तर:- डिजिटल सेल्युलर सिस्टम 1800 (DCS 1800) की शुरुआत वर्ष 1991 में यूरोप में हुई थी।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-18. दूरस्थ शिक्षा में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर की क्या भूमिका है?
उत्तर:- यह केंद्र शैक्षिक ऑडियो, वीडियो एवं मल्टीमीडिया सामग्री का निर्माण करता है, जिससे शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
प्रश्न-19. वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी ?
उत्तर:-वर्ष 1987 में राजस्थान के कोटा शहर में
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-20. पीटर्स (1968) के अनुसार पहला दूरस्थ शिक्षण विश्वविद्यालय 1929 में कहाँ स्थापित हुआ?
उत्तर:-1929 में जर्मनी के बर्लिन में
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-21. सतत् मूल्यांकन के कोई दो पैरामीटर लिखिए।
उत्तर:-सतत् मूल्यांकन के दो पैरामीटर हैं – कक्षा में सहभागिता और नियमित असाइनमेंट की गुणवत्ता व समयबद्ध प्रस्तुति।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-22. रचनात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन के मध्य कोई दो अन्तर लिखिए।
उत्तर:- रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान होता है, सुधार पर केंद्रित होता है; संकलनात्मक मूल्यांकन अंत में होता है और अंतिम प्रदर्शन को मापता है।
प्रश्न-23. दूरस्थ शिक्षा के सिद्धान्तवादी हॉल्सबर्ग (1981) ने कौन सा सिद्धान्त प्रस्तुत किया?
उत्तर:- हॉल्सबर्ग ने “मार्गदर्शित शिक्षण वार्तालाप (Guided Didactic Conversation)” का सिद्धान्त प्रस्तुत किया।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-24. दिशा निर्देशित शैक्षिक वार्तालाप का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया?
उत्तर:-यह सिद्धांत बोरो जे होल्मबर्ग (Börje Holmberg) द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो दूरस्थ शिक्षा में संवादात्मक अधिगम को महत्त्वपूर्ण मानते थे।
प्रश्न-25. ज्ञानदर्शन चैनल की शुरुआत कब की गई थी?
उत्तर:- ज्ञानदर्शन शैक्षिक टीवी चैनल की शुरुआत 26 जनवरी 2000 को
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-26. प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय का नाम बताइए।
उत्तर:- एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुंबई।
प्रश्न-27. ISD का पूर्ण नाम लिखिए।
उत्तर:- International Subscriber Dialing (अंतरराष्ट्रीय ग्राहक डायलिंग)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-28. मुद्रित सामग्रियों के कोई दो लाभ बताइए।
उत्तर:- (1) यह सुलभ और किफायती होती है, (2) अधिगम की गति और समय पर नियंत्रण देती है।
प्रश्न-29. EMPC का पूर्ण नाम लिखिए।
उत्तर:- EMPC का पूर्ण नाम है – Electronic Media Production Centre (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन केंद्र)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-30. विश्व के किसी दो वर्चुअल विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए।
उत्तर:- (1) ब्रिटेन का Open University, (2) Athabasca University, कनाडा।
प्रश्न-31. दूरस्थ शिक्षा में सम्प्रेषण के तीन स्तर कौन से हैं?
उत्तर:- प्रेषक (Sender), माध्यम (Medium), और ग्रहणकर्ता (Receiver)।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-32. सहकारी अधिगम की संकल्पना किसके द्वारा दी गई?
उत्तर:- डेविड और रोजर जॉनसन (David & Roger Johnson)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-33. एक श्रेयांक में कितनी परामर्श कक्षाएँ होती है?
उत्तर:- एक श्रेयांक में सामान्यतः 10 से 12 परामर्श कक्षाएँ आयोजित की जाती हैं ताकि छात्रों को विषयवस्तु की स्पष्टता मिल सके।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-34. शैक्षिक परामर्शदाता का अर्थ लिखिए।
उत्तर:- शैक्षिक परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जो छात्रों को पाठ्यक्रम, अध्ययन विधियों और शैक्षिक समस्याओं में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है।
प्रश्न-35. मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस का अर्थ लिखिए।
उत्तर:- यह एक मोबाइल सेवा है जिसमें चित्र, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज भेजे जा सकते हैं।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-36. प्रवन्धन सूचना प्रणाली से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:-यह एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो संगठन के प्रबंधन को योजना, नियंत्रण और निर्णय में सहायता देती है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Section-B
प्रश्न-1.मुक्त दूरस्थ अधिगम के चार उदीयमान मॉडलों के BARE में लिखिए।
उत्तर:- मुक्त दूरस्थ अधिगम (Open Distance Learning – ODL) के क्षेत्र में तकनीकी और शैक्षिक परिवर्तनों के चलते कई नवीन और उदीयमान मॉडल विकसित हुए हैं। इनमें प्रमुख चार मॉडलों का वर्णन निम्नलिखित है:
- ऑनलाइन लर्निंग मॉडल: यह मॉडल इंटरनेट आधारित होता है जिसमें शिक्षण-सामग्री, वीडियो लेक्चर, मूल्यांकन, और फीडबैक सभी ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।
- ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल: इसमें पारंपरिक शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षा का सम्मिलन होता है। कुछ हिस्से ऑफलाइन पढ़ाए जाते हैं और कुछ ऑनलाइन।
- मोबाइल लर्निंग मॉडल: यह स्मार्टफोन, टैबलेट आदि उपकरणों के माध्यम से अधिगम को बढ़ावा देता है। एप्स, SMS, पॉडकास्ट और मोबाइल ब्राउज़र आधारित सामग्री का उपयोग होता है।
- MOOCs (Massive Open Online Courses): ये मुफ्त या न्यूनतम शुल्क में ऑनलाइन कोर्स होते हैं, जिनमें हजारों छात्र एक साथ भाग ले सकते हैं। Coursera, SWAYAM जैसे प्लेटफॉर्म इसके उदाहरण हैं।
इन मॉडलों से शिक्षा अधिक सुलभ, लचीली और व्यक्तिगत हुई है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.खुला विश्वविद्यालय के स्वरूप को समझाइये।
उत्तर:- खुला विश्वविद्यालय (Open University) एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो पारंपरिक विश्वविद्यालयों की तुलना में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उन छात्रों को उच्च शिक्षा देना है जो कार्यरत हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं या नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते। इसका स्वरूप मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताओं पर आधारित होता है:
- खुला प्रवेश – योग्यता की सीमाएं कम होती हैं, जिससे अधिक लोग नामांकन ले सकते हैं।
- दूरस्थ अधिगम – अध्ययन सामग्री डाक, ऑनलाइन या ऑडियो-विजुअल माध्यम से भेजी जाती है।
- स्व-अधिगम सामग्री – छात्र अपनी गति से पढ़ाई कर सकते हैं।
- मल्टीमीडिया तकनीक का उपयोग – ऑडियो, वीडियो, टेलीविजन, रेडियो, और इंटरनेट का प्रयोग होता है।
- समर्थन सेवाएँ – शिक्षार्थियों के लिए संपर्क केंद्र और परामर्श सेवाएं उपलब्ध होती हैं।
खुला विश्वविद्यालय शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाता है और आजीवन अधिगम को प्रोत्साहित करता है।
प्रश्न-3.कीगन द्वारा परिभाषित दूरस्थ शिक्षा की सात विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर:- कीगन (Keegan) ने दूरस्थ शिक्षा की सात प्रमुख विशेषताओं को निम्न रूप में परिभाषित किया है –
स्वायत्तता और स्वतंत्रता – विद्यार्थी अपनी गति से, अपने समय पर अध्ययन कर सकता है।
शिक्षार्थी और शिक्षक का पृथक्करण – शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी आमने-सामने नहीं होते।
शैक्षणिक संगठन का प्रभाव – शिक्षा की योजना, संचालन और मूल्यांकन एक संगठित संस्थान द्वारा किया जाता है।
तकनीकी माध्यमों का उपयोग – मुद्रित, ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर आदि जैसे साधनों द्वारा शिक्षण-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
सम्पर्क का दो-तरफा प्रवाह – शिक्षार्थी और संस्थान के बीच संवाद हेतु पत्राचार, टेलीफोन, ई-मेल आदि का प्रयोग होता है।
स्व-अध्ययन का प्रावधान – शिक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार अध्ययन कर सकता है।
समवर्ती एवं असमवर्ती माध्यमों का प्रयोग – लाइव क्लासेज़, रिकॉर्डेड वीडियो आदि दोनों का उपयोग होता है।
प्रश्न-4. दिशा-निर्देशित शैक्षिक वार्तालाप सिद्धान्त पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- दिशा-निर्देशित शैक्षिक वार्तालाप (Guided Didactic Conversation) सिद्धांत का प्रतिपादन बोरिस लाम्सडॉर्फ (Börje Holmberg) ने किया था। यह सिद्धांत मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच के संवाद पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत, आकर्षक और प्रभावी बनाना है।
इस सिद्धांत के अनुसार, जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संवाद का वातावरण बनाया जाता है, तब शिक्षार्थी अधिक सक्रिय रूप से भाग लेता है और सीखने में उसकी रुचि बढ़ती है। इसमें शिक्षण सामग्री इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि जैसे शिक्षक सीधे शिक्षार्थी से संवाद कर रहा हो।
इस सिद्धांत में व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं, फीडबैक, प्रश्नोत्तरी और शिक्षार्थी केंद्रित रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। यह सिद्धांत भावनात्मक सहभागिता और आत्मनिर्देशित अधिगम को भी प्रोत्साहित करता है। दिशा-निर्देशित वार्तालाप शिक्षार्थी को अकेलेपन की भावना से बचाता है और उसे सीखने की प्रक्रिया में लगे रहने के लिए प्रेरित करता है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-5.दूरस्थ शिक्षा के संचालन में पीसीपी (पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम) की भूमिका का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम (PCP) दूरस्थ शिक्षा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को एक निश्चित समय पर अध्ययन केंद्रों में आमंत्रित किया जाता है, जहाँ वे विशेषज्ञ शिक्षकों से प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं।
PCP की भूमिकाएं:
- संदेह समाधान: छात्र अपनी शंकाओं को विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
- पुनरीक्षण: अध्ययन की गई सामग्री का पुनरावलोकन कराया जाता है।
- मूल्यांकन: असाइनमेंट व परियोजनाओं की समीक्षा व मार्गदर्शन दिया जाता है।
- प्रेरणा: प्रत्यक्ष संपर्क से छात्र अधिक प्रेरित होते हैं और अनुशासित रूप से पढ़ाई करते हैं।
- सामूहिक अधिगम: सहपाठियों से संवाद के माध्यम से सामूहिक अधिगम का अवसर मिलता है।
PCP से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है और शिक्षार्थियों को अधिक सहायता मिलती है।
प्रश्न-6. सहायता सेवा की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- दूरस्थ शिक्षा में सहायता सेवाएं (Support Services) छात्रों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। पारंपरिक शिक्षा की तरह दूरस्थ शिक्षा में निरंतर मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होता, इसलिए सहायता सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
सहायता सेवाओं की आवश्यकता:
- शैक्षणिक सहायता: अध्ययन सामग्री को समझने में मदद।
- तकनीकी सहायता: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व तकनीकी उपकरणों के प्रयोग में सहयोग।
- प्रशासनिक सहायता: नामांकन, परीक्षा, प्रमाणपत्र, फीस आदि से संबंधित जानकारी।
- भावनात्मक सहयोग: आत्मविश्वास व प्रेरणा बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन।
- समय प्रबंधन: अध्ययन योजना बनाने में सहायता।
इस प्रकार सहायता सेवाएं दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी व शिक्षार्थी केंद्रित बनाती हैं।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-7. मुक्त अधिगम क्या है? उदाहरण की माध्यम से बताइए।
उत्तर:-मुक्त अधिगम (Open Learning) एक ऐसा शिक्षण दृष्टिकोण है जिसमें छात्रों को अध्ययन का समय, स्थान, गति और माध्यम चुनने की स्वतंत्रता होती है। इसमें प्रवेश, उपस्थिति और मूल्यांकन की कठोरता कम होती है।
विशेषताएँ:
- कोई उम्र या समय की बाध्यता नहीं।
- छात्र केंद्रित अधिगम प्रक्रिया।
- अध्ययन सामग्री स्वयं सीखने योग्य होती है।
- तकनीकी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है।
उदाहरण:
कोई कार्यरत व्यक्ति इग्नू (IGNOU) जैसे खुले विश्वविद्यालय से बी.ए. कर रहा है। वह शाम को ऑफिस से लौटने के बाद वीडियो लेक्चर देखता है और ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करता है। उसे क्लास जाने की आवश्यकता नहीं होती। यह मुक्त अधिगम का उदाहरण है।
प्रश्न-8. ‘द ओपन यूनिवर्सिटी यू.के.’ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- द ओपन यूनिवर्सिटी (यू.के.) की स्थापना वर्ष 1969 में ब्रिटेन सरकार द्वारा की गई थी। यह विश्व की पहली प्रमुख ओपन यूनिवर्सिटी मानी जाती है जिसने उच्च शिक्षा को घर बैठे उपलब्ध कराने की क्रांति लाई। इसका मुख्यालय इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स (Milton Keynes) में स्थित है।
यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो पारंपरिक शिक्षा में भाग नहीं ले सकते, जैसे नौकरीपेशा, महिलाएँ, दिव्यांग आदि। यहाँ प्रवेश हेतु कोई पूर्व योग्यता आवश्यक नहीं होती।
ओपन यूनिवर्सिटी यू.के. ने अध्ययन के लिए प्रिंट सामग्री, ऑडियो-वीडियो, टेलीविज़न प्रसारण (BBC के साथ साझेदारी में), और हाल ही में ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग शुरू किया है। इसके मॉड्यूल आधारित पाठ्यक्रम और क्रेडिट प्रणाली इसे विशेष बनाते हैं। इस विश्वविद्यालय ने वैश्विक स्तर पर दूरस्थ शिक्षा की दिशा को नया आयाम दिया है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-9. दृश्य-श्रव्य सामग्री के लाभों को लिखिए।
उत्तर:- दृश्य-श्रव्य (Audio-Visual) सामग्री शिक्षा को रोचक, प्रभावशाली और समझने योग्य बनाती है। यह पारंपरिक शैक्षणिक विधियों की तुलना में अधिक व्यावहारिक और प्रेरणादायक होती है।
मुख्य लाभ:
- समझने में आसानी: चित्र, वीडियो और ऑडियो के माध्यम से कठिन विषय भी सरल हो जाते हैं।
- ध्यान आकर्षण: छात्र अधिक रुचि से पढ़ाई करते हैं।
- स्मृति में वृद्धि: चित्रात्मक और श्रव्य सूचनाएं अधिक समय तक याद रहती हैं।
- विविधता: पढ़ाई में विविध माध्यमों के प्रयोग से एकरूपता नहीं आती।
- स्वतंत्र अधिगम: छात्र अपनी गति से सामग्री देख और सुन सकते हैं।
इस प्रकार, दृश्य-श्रव्य सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को आधुनिक और प्रभावशाली बनाती है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-10. आथाबास्का विश्वविद्यालय में मॉनिटरिंग प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- आथाबास्का विश्वविद्यालय, कनाडा में स्थित एक अग्रणी मुक्त विश्वविद्यालय है जो दूरस्थ शिक्षा प्रदान करता है। इस विश्वविद्यालय में मॉनिटरिंग प्रणाली एक सुदृढ़ एवं योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखना और छात्रों की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखना है। यह प्रणाली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता, अधिगम सामग्रियों की गुणवत्ता, शिक्षण पद्धतियों तथा शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। मॉनिटरिंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों की भागीदारी, समय पर असाइनमेंट सबमिशन, परीक्षा परिणाम तथा फीडबैक को विश्लेषित किया जाता है। यह प्रणाली न केवल शिक्षार्थियों को ट्रैक करती है बल्कि शिक्षकों को भी समय-समय पर प्रशिक्षण देकर गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता करती है। इससे पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं और छात्रों को बेहतर अनुभव प्राप्त होता है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-11. एकाधिकार दूरस्थ प्रशिक्षण कॉलेज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- एकाधिकार दूरस्थ प्रशिक्षण कॉलेज मॉडल (Proprietary Distance Training College Model) वह प्रणाली है जिसमें कोई निजी संस्था या कंपनी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत नियंत्रण रखती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- केन्द्रित नियंत्रण: यह मॉडल पूरी तरह से एक संस्था द्वारा नियंत्रित होता है जो सामग्री निर्माण, शिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन का कार्य करती है।
- पूर्वनिर्धारित पाठ्यक्रम: इसमें पाठ्यक्रम संरचना और अध्ययन सामग्री पहले से तय की जाती है, और शिक्षार्थी को उसी के अनुसार अध्ययन करना होता है।
- सुव्यवस्थित सामग्री वितरण: शिक्षण सामग्री छपी हुई पुस्तकों, ऑडियो-वीडियो, सीडी, या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से भेजी जाती है।
- सीमित अंतःक्रियात्मकता: यह मॉडल संवाद आधारित कम होता है; शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन पत्र और फीडबैक के माध्यम से सहायता दी जाती है।
- प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति: यह संस्थाएँ अपने स्तर पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र जारी करती हैं।
यह मॉडल कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा में अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-12. स्वअधिगम सामग्रियों के मुख्य सिद्धांत पर चर्चा कीजिए।
उत्तर:- स्व-अधिगम सामग्री (Self-Learning Material – SLM) ऐसी शिक्षण सामग्री होती है जो विद्यार्थी स्वयं पढ़ और समझ सके। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:1. छात्र-केंद्रितता: सामग्री छात्रों की रुचि, आवश्यकता और स्तर के अनुसार बनाई जाती है।2. सरल भाषा: विषयवस्तु को आसान, स्पष्ट और संवादात्मक भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।3. स्व-परीक्षण (Self-assessment): हर इकाई के अंत में प्रश्न और उत्तर दिए जाते हैं ताकि छात्र स्वयं अपनी प्रगति जाँच सके।4. स्पष्ट उद्देश्य: प्रत्येक इकाई के आरंभ में अधिगम उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है।5. चरणबद्ध प्रस्तुति: सामग्री को क्रमिक और तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।6. प्रेरक गतिविधियाँ: शिक्षण को रोचक बनाने के लिए उदाहरण, चित्र, गतिविधियाँ और अभ्यास जोड़े जाते हैं।इन सिद्धांतों के अनुसार बनाई गई सामग्री दूरस्थ शिक्षार्थियों को आत्मनिर्भर बनाती है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-13. स्व-अधिगम सामग्रियों की विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर:- स्व-अधिगम सामग्री (Self-Learning Materials – SLMs) विशेष प्रकार की शैक्षणिक सामग्री होती है जो विद्यार्थियों को शिक्षक की अनुपस्थिति में भी अध्ययन के योग्य बनाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
छात्र-केंद्रित लेखन शैली: संवादात्मक भाषा और शैली में लिखा होता है।
स्पष्ट उद्देश्य: प्रत्येक इकाई की शुरुआत में उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिए जाते हैं।
मॉड्यूलर संरचना: छोटी-छोटी इकाइयों में सामग्री विभाजित होती है।
स्व-मूल्यांकन अभ्यास: हर इकाई के अंत में अभ्यास प्रश्न होते हैं ताकि छात्र अपनी प्रगति की जाँच कर सके।
उदाहरणों और चित्रों का समावेश: पाठ को रोचक और बोधगम्य बनाने के लिए।
प्रश्नोत्तर और सारांश: सामग्री के अंत में प्रमुख बिंदुओं का पुनरावलोकन और प्रश्न दिए जाते हैं।
समर्थक भाषा: प्रोत्साहित करने वाली और स्पष्ट भाषा प्रयोग की जाती है।
प्रश्न-14. मुक्त दूरस्थ अधिगम के उदीयमान विभिन्न मॉडलों के बारे में चर्चा कीजिए।
उत्तर:- मुक्त दूरस्थ अधिगम में आधुनिक तकनीक और शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार अनेक नवीन मॉडल उभरकर सामने आए हैं। पहला, ऑनलाइन लर्निंग मॉडल है जिसमें इंटरनेट आधारित अधिगम सामग्री और आभासी कक्षाओं का प्रयोग होता है। दूसरा, ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल है जो पारंपरिक शिक्षा और ऑनलाइन अधिगम का मिश्रण है। तीसरा, मूक्स (MOOCs) आधारित मॉडल है जो व्यापक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। चौथा, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है जिसमें विद्यार्थी पहले सामग्री घर पर पढ़ते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं। पाँचवां, मोबाइल लर्निंग मॉडल है जिसमें मोबाइल एप्स और स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से अधिगम होता है। ये सभी मॉडल लचीलापन, पहुंच, समय और संसाधनों की दृष्टि से प्रभावी हैं। इनके माध्यम से शिक्षार्थियों को अपनी सुविधा अनुसार अधिगम करने का अवसर प्राप्त होता है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-15. दूरस्थ शिक्षा को मॉडलों का वर्गीकरण करते हुए विस्तार से लिखिए।
उत्तर:- दूरस्थ शिक्षा के मॉडलों को शिक्षण विधियों, संचार तकनीकों, तथा संस्थागत संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख प्रकार हैं:1. सामान्य पत्राचार मॉडल (Correspondence Model): पारंपरिक मॉडल जिसमें पाठ्य सामग्री डाक द्वारा भेजी जाती है। शिक्षक-छात्र संपर्क न्यूनतम होता है।2. मल्टीमीडिया मॉडल (Multimedia Model): प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, एवं कंप्यूटर आधारित सामग्री का उपयोग किया जाता है।3. टेलीविजन/रेडियो आधारित मॉडल: ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों से शिक्षण सामग्री प्रसारित की जाती है, जैसे कि Gyan Darshan या Gyan Vani।4. ऑनलाइन शिक्षा मॉडल (Online Learning Model): इंटरनेट पर आधारित मॉडल जिसमें LMS, ई-मेल, वीडियो कॉल आदि का प्रयोग होता है।5. मिश्रित या हाइब्रिड मॉडल (Blended Model): इसमें परंपरागत और आधुनिक दोनों तरीकों को सम्मिलित किया जाता है।ये मॉडल समय, संसाधन और छात्र की सुविधा के अनुसार प्रयुक्त होते हैं।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-16. नील के वर्गीकरण का, दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के वर्गीकरण में क्या योगदान है?
उत्तर:- नील (R. G. Neil) ने दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के वर्गीकरण के लिए एक विशिष्ट टाइपोलॉजी प्रस्तुत की जो संस्थानों की संरचना, क्रियाविधि और कार्यक्षेत्र के आधार पर उन्हें चार वर्गों में बाँटती है:
- प्रारंभिक शिक्षा सह संस्थान – ये संस्थाएँ पारंपरिक विश्वविद्यालयों की सहायक इकाई होती हैं जो दूरस्थ शिक्षा प्रदान करती हैं।
- द्वैध-मोड संस्थान (Dual-mode Institutions) – ये संस्थान नियमित और दूरस्थ दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं।
- एकल-मोड संस्थान (Single-mode Institutions) – जैसे इग्नू, जो केवल दूरस्थ शिक्षा प्रदान करते हैं।
- कंसोर्टियम और नेटवर्क आधारित संस्थान – ये संस्थाएँ कई संगठनों के सहयोग से चलती हैं और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण पर केंद्रित होती हैं।
नील का यह वर्गीकरण संस्थागत कार्यप्रणाली को समझने और दूरस्थ शिक्षा की रणनीति तैयार करने में सहायक होता है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-17. दूरस्थ शिक्षा में प्रणाली अधिगम के पाँच उद्देश्य लिखिए।
उत्तर:- दूरस्थ शिक्षा में प्रणाली दृष्टिकोण (System Approach) शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत पूरा शिक्षण एक योजनाबद्ध प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है।
प्रणाली अधिगम के पाँच उद्देश्य:
- लक्ष्य निर्धारण: स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना।
- नियोजन: पाठ्यक्रम, समय-सारणी और संसाधनों की योजना बनाना।
- कार्यान्वयन: योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू करना।
- मूल्यांकन: अधिगम की प्रगति और परिणामों का आकलन करना।
- प्रतिक्रिया (Feedback): त्रुटियों को सुधारना और प्रक्रिया को बेहतर बनाना।
यह दृष्टिकोण दूरस्थ शिक्षा को अधिक संगठित और प्रभावी बनाता है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-18. कॉपीराइट में आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- कॉपीराइट एक वैधानिक अधिकार है जो किसी रचनात्मक कार्य के निर्माता को उसकी रचना पर एकाधिकार देता है। इसमें साहित्य, संगीत, चित्रकला, फिल्म, सॉफ़्टवेयर आदि शामिल होते हैं।
कॉपीराइट का उद्देश्य रचनाकार को उसकी रचना के प्रयोग, प्रकाशन, वितरण और लाभ पर नियंत्रण देना है ताकि वह आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से संरक्षित रह सके।
भारत में ‘कॉपीराइट अधिनियम 1957’ इसके लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। यह अधिकार सामान्यतः रचनाकार के जीवनकाल + 60 वर्षों तक प्रभावी रहता है।
शैक्षणिक क्षेत्र में महत्व:
दूरस्थ शिक्षा सामग्री जैसे कि प्रिंट, ऑडियो-वीडियो, डिजिटल पाठ्यक्रम आदि का संरक्षण कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। इससे सामग्री की चोरी या अनुचित उपयोग रोका जा सकता है।
प्रश्न-19. प्रणाली अभिगम के गुण और दोष।
उत्तर:- प्रणाली अभिगम (Systems Approach) एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें किसी भी प्रक्रिया को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव आपस में जुड़े होते हैं और एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं।
गुण:
- संगठित प्रक्रिया: यह एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध विधि है जो लक्ष्य आधारित होती है।
- स्पष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति: इसमें प्रत्येक चरण का उद्देश्य निर्धारित होता है, जिससे परिणामों को मापा जा सकता है।
- प्रभावी योजना और मूल्यांकन: यह प्रक्रिया मूल्यांकन के आधार पर सुधार की संभावना देती है।
- लचीलापन: यह विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन की क्षमता रखती है।
दोष:
- जटिलता: यह कभी-कभी अत्यधिक तकनीकी और जटिल हो सकती है।
- व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा: यह व्यक्तिगत जरूरतों और मानवीय भावनाओं को अनदेखा कर सकती है।
- अत्यधिक संसाधन आवश्यकताएँ: इसमें समय, धन और तकनीकी विशेषज्ञता की अधिक आवश्यकता होती है।
इस प्रकार, प्रणाली अभिगम शिक्षा और प्रशिक्षण को लक्ष्य की ओर केन्द्रित करने वाला प्रभावशाली उपकरण है, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक लागू करना आवश्यक है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-20. मुद्रित सामग्री की तुलना में श्रव्य-दृश्य अधिगम सामग्री अधिक लाभदायक क्यों है?
उत्तर:- श्रव्य-दृश्य (Audio-Video) सामग्री दूरस्थ शिक्षा में प्रभावी अधिगम का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसकी तुलना में मुद्रित सामग्री सीमित अनुभव प्रदान करती है।
लाभ:
- बहु इंद्रिय अनुभव: ऑडियो-विज़ुअल सामग्री आँखों और कानों दोनों से ग्रहण की जाती है, जिससे स्मरण क्षमता बढ़ती है।
- व्यावहारिकता: जटिल विषयों को एनिमेशन, मॉडल या डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से समझाया जा सकता है।
- रुचिकर अधिगम: चित्र, ध्वनि और गति अध्ययन को आकर्षक बनाते हैं।
- समय की लचीलता: रिकॉर्डेड वीडियो को कभी भी देखा जा सकता है।
सीमाएँ:
हालांकि तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता, धीमे नेटवर्क, और कम पहुँच जैसे कुछ अवरोध हो सकते हैं, फिर भी यह माध्यम शिक्षा को अधिक जीवंत और प्रभावशाली बनाता है
प्रश्न-21. पाठ्यक्रम संशोधन का महत्व बताइए।
उत्तर:- पाठ्यक्रम संशोधन एक आवश्यक प्रक्रिया है जो शैक्षिक गुणवत्ता, प्रासंगिकता और अद्यतनता बनाए रखने में सहायक होती है। समय के साथ ज्ञान, तकनीक और समाज में परिवर्तन आते हैं, ऐसे में पाठ्यक्रम को अद्यतन करना आवश्यक हो जाता है। इससे छात्र वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम संशोधन से विषयवस्तु में नवीन अनुसंधानों, सामाजिक परिवर्तनों और रोजगार की मांगों को शामिल किया जा सकता है। यह शिक्षण में नवीन विधियों एवं तकनीकों को एकीकृत करने का अवसर भी प्रदान करता है। साथ ही यह शिक्षकों को नई दिशा देता है और छात्रों को प्रेरित करता है। इस प्रकार, पाठ्यक्रम संशोधन शैक्षणिक संस्थानों की प्रासंगिकता और गुणवत्ता को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-22. दूरस्थ शिक्षा में वित्तीय प्रबंधन के मूलभूत आधार कौन-कौनसे हैं?
उत्तर:- दूरस्थ शिक्षा में वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसके मुख्य आधार निम्नलिखित हैं:1. बजट निर्माण: संस्थान की आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार वार्षिक बजट का नियोजन किया जाता है।2. संसाधनों का समुचित आवंटन: मानव, तकनीकी और भौतिक संसाधनों पर व्यय का संतुलन बनाया जाता है।3. लागत प्रभावशीलता (Cost-effectiveness): न्यूनतम लागत में अधिकतम परिणाम प्राप्त करना।4. लेखा-परीक्षण और निगरानी: सभी वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु नियमित लेखा-परीक्षण एवं निगरानी आवश्यक होती है।5. पारदर्शिता: वित्तीय निर्णयों में पारदर्शिता बनाए रखना, ताकि विश्वास बना रहे।6. स्वावलंबन: संस्थान को दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु आय के नए स्रोत तलाशना।ये सिद्धांत दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को आर्थिक रूप से स्थायित्व प्रदान करते हैं।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-23. दूरस्थ शिक्षा निधिकरण के कारक कौन-कौनसे हैं ?
उत्तर:- दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) के संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसे निधिकरण (funding) कहा जाता है। इसके प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:
- सरकारी सहायता: राज्य या केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि, योजनाएँ और परियोजनाएँ निधिकरण का मुख्य स्रोत हैं।
- छात्र शुल्क: छात्र द्वारा भुगतान की गई फीस संस्थान के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- विकास परियोजनाएँ एवं अनुदान: यूनेस्को, यूजीसी, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से मिलने वाली परियोजनाएँ निधिकरण का स्रोत होती हैं।
- उद्योग एवं कॉर्पोरेट सहायता: कुछ निजी कंपनियाँ सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहयोग देती हैं।
- मुद्रित और डिजिटल सामग्री की बिक्री: अध्ययन सामग्री की बिक्री से प्राप्त आय भी निधिकरण का साधन बनती है।
- शोध परियोजनाएँ: शोध संस्थानों से जुड़ी परियोजनाओं से भी वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं।
इन कारकों से दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की संरचना, सामग्री विकास, तकनीकी सुधार और मानव संसाधन का संचालन संभव होता है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-24. दूरस्थ शिक्षा में शैक्षिक सहायता सेवा के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- दूरस्थ शिक्षा में शैक्षिक सहायता सेवाएं (Academic Support Services) छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें अध्ययन सामग्री की व्याख्या, शंकाओं का समाधान, मार्गदर्शन और प्रेरणा देना शामिल होता है। ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट (TMA), व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (PCP), टेली-काउंसलिंग, ऑनलाइन चर्चा मंच, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) इसके प्रमुख घटक हैं। ये सेवाएं छात्रों को सीखने में आत्मनिर्भर बनाती हैं और समयबद्ध रूप से उत्तरदायित्व निभाने में सहायता करती हैं। शैक्षिक सहायता सेवाएं विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझकर उन्हें उपयुक्त समाधान देती हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है और अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-25. सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के लाभों को बताइए।
उत्तर:- सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, विशेषतः दूरस्थ शिक्षा में इसका व्यापक उपयोग हुआ है।
मुख्य लाभ:
- सुलभता: किसी भी स्थान व समय पर अध्ययन संभव होता है।
- इंटरैक्टिव अधिगम: वीडियो, क्विज़, लाइव क्लास आदि से सीखना अधिक रोचक होता है।
- व्यक्तिगत अधिगम: छात्र अपनी गति और शैली में पढ़ सकते हैं।
- संसाधनों की उपलब्धता: ई-पुस्तकें, ऑनलाइन लेक्चर, ट्यूटोरियल आदि।
- तेज़ संचार: शिक्षकों व छात्रों के बीच त्वरित संवाद संभव होता है।
ICT शिक्षा को आधुनिक, लचीला और व्यापक बनाता है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-26. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की विद्यार्थी सहायता सेवाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:-वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU), कोटा, राजस्थान की प्रमुख ओपन यूनिवर्सिटी है। यह विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए विविध प्रकार की विद्यार्थी सहायता सेवाएँ उपलब्ध कराता है, जो निम्नलिखित हैं:
- अध्ययन केंद्रों की स्थापना: राज्यभर में कई अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ से विद्यार्थी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
- शैक्षणिक परामर्श कक्षाएँ: सप्ताहांत या छुट्टियों में विशेषज्ञों द्वारा क्लासेज़ आयोजित होती हैं।
- पुस्तकालय और संदर्भ सेवा: अध्ययन केंद्रों में पुस्तकालय और संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
- हेल्पलाइन और ईमेल सहायता: विद्यार्थी अपनी समस्याओं को टोल फ्री नंबर या ईमेल से पूछ सकते हैं।
- ऑनलाइन पोर्टल: विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण, परीक्षा फॉर्म, रिजल्ट आदि सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- प्रिंट और डिजिटल सामग्री वितरण: पाठ्य सामग्री छात्रों को डाक द्वारा भेजी जाती है तथा डिजिटल रूप में भी उपलब्ध है।
यह सेवाएँ छात्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-27. सार्वभौम अभिकल्प के सात सिद्धान्त क्या-क्या हैं?
उत्तर:- सार्वभौम अभिकल्प (Universal Design) वह सिद्धांत है जो सभी व्यक्तियों, चाहे वे किसी भी क्षमता के हों, के लिए सुलभ और उपयोगी शिक्षण वातावरण तैयार करता है। इसके सात सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:
समान उपयोग का सिद्धांत (Equitable Use): सभी के लिए समान रूप से उपयोगी।
लचीलापन (Flexibility in Use): उपयोग के विभिन्न तरीकों की अनुमति।
सरलता और सहजता (Simple and Intuitive): समझने और उपयोग करने में आसान।
सूचना की स्पष्टता (Perceptible Information): आवश्यक सूचना सभी उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्ट।
गलतियों के लिए सहनशीलता (Tolerance for Error): उपयोगकर्ता की गलतियों के दुष्परिणाम को कम करना।
कम शारीरिक प्रयास (Low Physical Effort): उपयोग में कम प्रयास की आवश्यकता।
आकार और स्थान की उपयुक्तता (Size and Space for Approach and Use): सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच और उपयोग की सुविधा।
ये सिद्धांत एक समावेशी शिक्षण वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं।
प्रश्न-28. स्वअधिगम सामग्रियों के पाँच प्रसिद्ध मॉडलों के बारे में लिखिए।
उत्तर:- स्वअधिगम सामग्री शिक्षार्थियों को आत्मनिर्भर रूप से अध्ययन करने में सहायता प्रदान करती है। इसके पाँच प्रसिद्ध मॉडल निम्नलिखित हैं:
मोबाइल लर्निंग मॉडल: मोबाइल एप्स और स्मार्टफोन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।
ये मॉडल छात्रों की सुविधा, लचीलापन और स्वावलंबन को बढ़ावा देते हैं और कहीं भी कभी भी अधिगम को संभव बनाते हैं।
प्रकाशन मॉडल (Print Model): इसमें मुद्रित पुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं और गाइड का उपयोग किया जाता है।
ऑडियो-विजुअल मॉडल: इस मॉडल में ऑडियो टेप, वीडियो टेप, सीडी आदि के माध्यम से अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है।
सीएआई मॉडल (Computer Assisted Instruction): इसमें कंप्यूटर आधारित इंटरेक्टिव प्रोग्राम उपयोग किए जाते हैं।
ऑनलाइन लर्निंग मॉडल: इस मॉडल में ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, वेब आधारित पाठ्यक्रम और वर्चुअल क्लासरूम होते हैं।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-29. इकाई के संघटक कौन-कौनसे होते हैं ?
उत्तर:- शैक्षिक इकाई (Instructional Unit) एक संगठित शिक्षण खंड होती है जिसमें किसी एक विषयवस्तु को सिखाने के लिए आवश्यक सभी तत्व शामिल होते हैं। इसकी रचना में निम्नलिखित संघटक होते हैं:
- शीर्षक (Title): इकाई का नाम या विषय।
- अधिगम उद्देश्य (Learning Objectives): यह बताता है कि छात्र को इकाई पढ़ने के बाद क्या सीखना है।
- पूर्वज्ञान (Prerequisites): अध्ययन शुरू करने से पहले कौन-कौनसी जानकारी आवश्यक है।
- मुख्य सामग्री (Main Content): यह इकाई का प्रमुख भाग होता है, जिसमें पाठ्यवस्तु, उदाहरण, चित्र आदि होते हैं।
- सारांश (Summary): इकाई के अंत में दिया गया सारांश, जो पूरे पाठ की पुनरावृत्ति करता है।
- मूल्यांकन प्रश्न (Assessment Questions): इससे यह जांचा जाता है कि छात्र ने कितना सीखा।
- गतिविधियाँ (Activities): अधिगम को व्यावहारिक रूप देने के लिए क्रियाएँ शामिल होती हैं।
- संदर्भ (References): अतिरिक्त अध्ययन के लिए उपयोगी स्रोत।
इन सभी संघटकों से एक प्रभावी और पूर्ण शिक्षण इकाई का निर्माण होता है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-30. ‘त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में शिक्षा’ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।/”शिक्षा एक त्रिधुवीय प्रक्रिया है।” व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- शिक्षा को एक त्रिधुवीय प्रक्रिया (Tripolar Process) माना गया है क्योंकि इसमें तीन प्रमुख घटक होते हैं—शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु।
शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान, अनुभव और मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुँचाता है।
शिक्षार्थी वह होता है जो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है और ज्ञान को आत्मसात करता है।
पाठ्यवस्तु वह सामग्री है जो शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को दी जाती है।
इन तीनों के मध्य संतुलित और समन्वित संबंध होने पर ही शिक्षा की प्रक्रिया सफल होती है। शिक्षक मार्गदर्शन देता है, छात्र सीखता है और पाठ्यवस्तु दोनों के मध्य पुल का कार्य करती है। इस प्रकार, ये तीनों घटक परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं और शिक्षा प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं।
प्रश्न-31. सार्वभौम अभिकल्प के सात सिद्धान्त कौन-कौनसे हैं?
उत्तर:- सार्वभौम अभिकल्प (Universal Design) के सिद्धांत ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों, चाहे वे किसी भी योग्यता के हों, के लिए उपयोगी व सुलभ डिज़ाइन सुनिश्चित करते हैं। इसके सात प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:1. समान उपयोगिता (Equitable Use): सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग समान रूप से संभव हो।2. उपयोग में लचीलापन (Flexibility in Use): अलग-अलग पसंद व क्षमताओं के अनुसार विकल्प देना।3. सरल और सहज उपयोग (Simple and Intuitive Use): डिज़ाइन को समझना व उपयोग करना आसान हो।4. सूचना की बोधगम्यता (Perceptible Information): सभी उपयोगकर्ताओं तक सूचना स्पष्टता से पहुँचे।5. त्रुटि सहिष्णुता (Tolerance for Error): उपयोगकर्ता की गलतियों से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया हो।6. कम शारीरिक प्रयास (Low Physical Effort): उपयोग में कम शारीरिक प्रयास की आवश्यकता हो।7. उपयोग के लिए आकार और स्थान (Size and Space for Approach and Use): सभी आकार व क्षमता के उपयोगकर्ता सामग्री तक पहुँच सकें।ये सिद्धांत शैक्षिक व तकनीकी संसाधनों को समावेशी बनाने में सहायक होते हैं।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-32. ब्लूटूब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
उत्तर:- ब्लूटूथ (Bluetooth) एक वायरलेस तकनीक है जो दो या दो से अधिक उपकरणों को सीमित दूरी में आपस में जोड़ने की सुविधा देती है। इसकी खोज 1994 में एरिक्सन कंपनी ने की थी और अब यह मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर आदि में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।
ब्लूटूथ रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके डेटा और आवाज के आदान-प्रदान को संभव बनाता है। यह सामान्यतः 10 मीटर की दूरी तक प्रभावी रहता है। इसका उपयोग फाइल ट्रांसफर, वायरलेस ऑडियो स्ट्रीमिंग, इनपुट डिवाइसेज़ (कीबोर्ड, माउस) को जोड़ने में किया जाता है।
ब्लूटूथ की मुख्य विशेषताएँ हैं:
वायरलेस संचार
ऊर्जा की कम खपत
ऑटोमेटिक पेयरिंग
कम लागत
ब्लूटूथ ने जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, विशेष रूप से शिक्षण में इसका उपयोग सामग्री साझा करने, ऑडियो सुनने और ई-लर्निंग डिवाइसेज़ को जोड़ने में होता है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-33. टेलीकांफ्रेंसिंग क्या है? इसके प्रमुख लाभ क्या हैं
उत्तर:- टेलीकांफ्रेंसिंग एक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से लोग अलग-अलग स्थानों पर होते हुए भी एक साथ बातचीत कर सकते हैं, चाहे वह ऑडियो हो या वीडियो आधारित। यह विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा में उपयोगी है।
प्रमुख लाभ:
- प्रत्यक्ष संपर्क: शिक्षक और छात्र एक साथ संवाद कर सकते हैं।
- समय और स्थान की बचत: बिना यात्रा के शिक्षा संभव।
- विशेषज्ञों से संवाद: दूरस्थ क्षेत्रों में बैठे छात्र भी विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं।
- सामूहिक अधिगम: कई छात्रों को एक साथ लाभ मिलता है।
- लाइव प्रश्नोत्तर: छात्र तुरंत प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर पा सकते हैं।
इससे शिक्षा अधिक गतिशील, संवादात्मक और प्रभावशाली बनती है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-34. दूरस्थ शिक्षा में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री के बारे में विस्तार से लिखिए।
उत्तर:- दूरस्थ शिक्षा में अधिगम सामग्री का विशेष महत्व है क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहते। प्रमुख अधिगम सामग्रियाँ निम्नलिखित हैं:1. प्रिंट सामग्री: यह सबसे सामान्य रूप है, जिसमें पुस्तकें, पाठ्यक्रम, अभ्यास पत्र आदि शामिल होते हैं। ये स्वअध्ययन हेतु तैयार की जाती हैं।2. ऑडियो-विज़ुअल सामग्री: सीडी, पॉडकास्ट, वीडियो लेक्चर आदि के माध्यम से विषय को रोचक व व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है।3. ऑनलाइन सामग्री: ई-लर्निंग पोर्टल, ई-बुक्स, वेबिनार, एमओओसी आदि के रूप में सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध होती है।4. स्व-अधिगम सामग्री (SLM): यह ऐसी सामग्री होती है जो स्वयं पढ़ने, समझने व अभ्यास करने के लिए डिज़ाइन की जाती है।5. अनुपूरक सामग्री: समाचार-पत्र, पत्रिकाएं या संदर्भ पुस्तकें जो विषय को और व्यापक बनाती हैं।इन सामग्रियों से छात्र कहीं भी और कभी भी अध्ययन कर सकते हैं।
प्रश्न-35. भाषा सम्पादन क्यों आवश्यक है ?
उत्तर:- भाषा सम्पादन (Language Editing) लेखन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से शैक्षिक, तकनीकी, और अकादमिक लेखन में आवश्यक होती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:
- स्पष्टता और सुगमता: सम्पादन से वाक्य स्पष्ट, सटीक और आसानी से समझने योग्य बनते हैं।
- त्रुटियों का सुधार: व्याकरण, वर्तनी, विराम चिह्न और वाक्य संरचना में हुई त्रुटियाँ सुधारी जाती हैं।
- प्रभावी संप्रेषण: सम्पादित भाषा पाठक के लिए अधिक आकर्षक और संवादात्मक होती है।
- पेशेवर प्रस्तुति: सम्पादन से सामग्री की गुणवत्ता बढ़ती है और वह पेशेवर रूप में प्रस्तुत होती है।
- अर्थ की शुद्धता: गलत भाषा से अर्थ का अनर्थ हो सकता है; सम्पादन से सही भाव प्रस्तुत होता है।
इसलिए, विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा की सामग्री में भाषा सम्पादन अनिवार्य होता है ताकि शिक्षार्थी स्पष्ट रूप से समझ सकें और विषय में रुचि बनाए रखें।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Section-C
प्रश्न-1.स्वअधिगम सामग्रियों के विकास की विधियों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- स्वअधिगम सामग्री (Self-Learning Material – SLM) ऐसी शैक्षिक सामग्री होती है जिसे विद्यार्थी स्वयं पढ़कर ज्ञान अर्जित कर सकता है। यह विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में उपयोग की जाती है जहाँ शिक्षकों की सीधी उपस्थिति नहीं होती। इसकी विशेषता यह होती है कि यह संवादात्मक, स्पष्ट, सरल, और चरणबद्ध होती है।
स्वअधिगम सामग्री के विकास की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं:
- आवश्यकताओं का मूल्यांकन (Needs Assessment):
सबसे पहले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, आयु, भाषा, उपलब्ध संसाधन आदि को ध्यान में रखा जाता है। - पाठ्यक्रम निर्माण और पाठ्यवस्तु निर्धारण:
पाठ्यक्रम विशेषज्ञ संबंधित विषय की रूपरेखा तय करते हैं। पाठ्यवस्तु का विभाजन इकाइयों और पाठों में किया जाता है जिससे अध्ययन आसान हो। - लेखन कार्य (Writing Process):
विषय विशेषज्ञों द्वारा सामग्री को विद्यार्थियों की भाषा शैली में लिखा जाता है। इसे संवादात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित बनाया जाता है। उदाहरण, गतिविधियाँ, पुनरावलोकन प्रश्न आदि जोड़े जाते हैं। - संपादन (Editing):
भाषा विशेषज्ञ और विषय संपादक द्वारा सामग्री का संपादन किया जाता है ताकि भाषा, व्याकरण और सामग्री में त्रुटियाँ न रहें। - रचना और डिजाइन (Design and Layout):
ग्राफिक डिजाइनर और प्रकाशन विशेषज्ञ सामग्री को आकर्षक और सुगम रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें चित्र, आरेख, चार्ट आदि शामिल होते हैं। - पायलट परीक्षण (Pilot Testing):
तैयार सामग्री को सीमित छात्रों पर आजमाया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि यह प्रभावी है या नहीं। फीडबैक लेकर आवश्यक सुधार किए जाते हैं। - प्रकाशन और वितरण:
अंतिम संस्करण प्रकाशित किया जाता है और विद्यार्थियों को डाक, पोर्टल या अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराया जाता है। - फीडबैक और अद्यतन (Feedback and Revision):
उपयोग के बाद छात्रों और शिक्षकों से फीडबैक लेकर समय-समय पर सामग्री का पुनरीक्षण किया जाता है।
स्वअधिगम सामग्री का विकास एक वैज्ञानिक, योजनाबद्ध और सहभागिता-आधारित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थी को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वह बिना शिक्षक की सीधी मदद के भी ज्ञान अर्जित कर सके।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.दूरस्थ शिक्षा में कम्प्यूटर के लाभों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- दूरस्थ शिक्षा में कम्प्यूटर का उपयोग एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा गया है। यह न केवल अध्ययन की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाता है, बल्कि इसे अधिक प्रभावी, लचीला और इंटरैक्टिव भी बनाता है। नीचे कंप्यूटर के प्रमुख लाभों की व्याख्या की गई है:
- सामग्री की सुलभता:
कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण सामग्री को डिजिटल रूप में कहीं भी और कभी भी उपलब्ध कराया जा सकता है। विद्यार्थी पाठ्यक्रम, ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर, एनिमेशन आदि का उपयोग अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। - समय और स्थान की स्वतंत्रता:
दूरस्थ शिक्षा का मुख्य लाभ यही है कि छात्र समय और स्थान की सीमाओं से स्वतंत्र होकर अध्ययन कर सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से वे कहीं से भी कक्षा से जुड़ सकते हैं। - इंटरएक्टिव लर्निंग:
कंप्यूटर आधारित शिक्षा में मल्टीमीडिया टूल्स का प्रयोग करके छात्रों को आकर्षक और सहभागिता आधारित शिक्षा दी जाती है, जैसे कि क्विज़, ऑनलाइन फीडबैक, सिमुलेशन आदि। - संचार में आसानी:
कंप्यूटर ई-मेल, चैट, वीडियो कॉलिंग और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों के बीच संपर्क बनाए रखता है। यह शिक्षक-छात्र संबंध को सुदृढ़ बनाता है। - मूल्यांकन और निगरानी:
ऑनलाइन मूल्यांकन, टेस्ट और असाइनमेंट सबमिशन कंप्यूटर के माध्यम से सहजता से संभव है। इससे शिक्षकों को छात्र की प्रगति पर नजर रखने और समय पर फीडबैक देने में सुविधा होती है। - लागत में कमी:
शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता न होने के कारण यात्रा, आवास और मुद्रित सामग्री जैसी लागतों में कमी आती है, जिससे शिक्षा अधिक किफायती बनती है। - अद्यतन जानकारी:
कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से छात्र नवीनतम जानकारी, शोध पत्र, लेख और अन्य शैक्षिक संसाधनों तक तत्काल पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। - विकलांग विद्यार्थियों के लिए सहायक:
श्रवण या दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए विशेष सॉफ्टवेयर और उपकरण उपलब्ध हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में मदद करते हैं।
कंप्यूटर ने दूरस्थ शिक्षा को नए आयाम दिए हैं। यह न केवल सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विश्व के किसी भी कोने तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम भी बन चुका है।
प्रश्न-3. मोबाइल प्रौद्योगिकी और दूरस्थ शिक्षा के सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- मोबाइल प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है, विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक और गहन रहा है। आज स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे उपकरणों की पहुँच ने शिक्षार्थियों को कहीं से भी सीखने की स्वतंत्रता दी है।
मोबाइल प्रौद्योगिकी और दूरस्थ शिक्षा के मध्य संबंध:
- सुलभता और लचीलापन:
मोबाइल डिवाइसेज के माध्यम से छात्र कभी भी, कहीं से भी अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इससे शिक्षा अधिक लचीली और सहज हो गई है। - लर्निंग ऐप्स का उपयोग:
आज विभिन्न शिक्षण ऐप्स जैसे BYJU’S, Vedantu, Coursera, Khan Academy आदि मोबाइल पर उपलब्ध हैं जो दूरस्थ शिक्षा को सरल बनाते हैं। - इंटरनेट आधारित कक्षाएँ:
मोबाइल के माध्यम से छात्र Google Meet, Zoom और MS Teams जैसी सेवाओं का उपयोग करके ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। - ऑडियो-विजुअल सामग्री:
मोबाइल तकनीक के माध्यम से वीडियो लेक्चर, पॉडकास्ट और इंटरैक्टिव कंटेंट तक तुरंत पहुंच संभव है। - एसएमएस और नोटिफिकेशन:
संस्थाएं मोबाइल के माध्यम से छात्रों को समय-समय पर जानकारी, रिमाइंडर और नोटिफिकेशन भेज सकती हैं। - ई-बुक्स और पीडीएफ:
मोबाइल पर ई-पाठ्यपुस्तकों को पढ़ना और डाउनलोड करना आसान होता है, जिससे शिक्षण सामग्री हर समय सुलभ रहती है। - सामाजिक मीडिया से जुड़ाव:
व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप्स के माध्यम से छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के बीच संवाद बना रहता है। - कम लागत में उच्च लाभ:
मोबाइल प्रौद्योगिकी दूरस्थ शिक्षा को अधिक सुलभ और किफायती बनाती है, जिससे समाज के वंचित वर्ग भी शिक्षा से जुड़ सकते हैं।
मोबाइल प्रौद्योगिकी ने दूरस्थ शिक्षा को गतिशील और समावेशी बना दिया है। इसके माध्यम से शिक्षा अब केवल पुस्तकालयों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर हाथ में स्मार्टफोन ने उसे घर-घर तक पहुँचा दिया है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-4. दूरस्थ शिक्षा के उभरते मॉडलों पर विस्तार से लिखिए।
उत्तर:- दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और शैक्षणिक आवश्यकताओं के चलते कई नवीन और उभरते मॉडल विकसित हुए हैं। इन मॉडलों का उद्देश्य शिक्षार्थियों को लचीलापन, पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नीचे कुछ प्रमुख उभरते मॉडलों का वर्णन किया गया है:1. ऑनलाइन शिक्षा मॉडल (Online Learning Model):यह सबसे व्यापक और प्रचलित मॉडल है जिसमें शिक्षार्थी इंटरनेट के माध्यम से पाठ्य सामग्री प्राप्त करते हैं, वीडियो लेक्चर देखते हैं, क्विज़ हल करते हैं और आभासी कक्षा (Virtual Classroom) का हिस्सा बनते हैं। इसमें Zoom, Google Meet, Moodle जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग होता है।2. मिश्रित अधिगम मॉडल (Blended Learning Model):इसमें पारंपरिक संपर्क शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षा का सम्मिलन होता है। विद्यार्थी कुछ समय के लिए कैंपस में उपस्थित होकर अधिगम करते हैं, और शेष समय ऑनलाइन संसाधनों से। यह मॉडल सीखने में लचीलापन और सहभागिता बढ़ाता है।3. मोबाइल शिक्षा मॉडल (Mobile Learning):स्मार्टफोन, टैबलेट और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना इस मॉडल की विशेषता है। यह ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ बनाने में सहायक है।4. ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मॉडल (OER):इसमें निःशुल्क डिजिटल संसाधनों का उपयोग किया जाता है जो किसी भी विद्यार्थी के लिए सुलभ होते हैं। जैसे NPTEL, SWAYAM, Coursera आदि प्लेटफॉर्म शिक्षण के लिए संसाधन प्रदान करते हैं।5. मूक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉडल (MOOCs – Massive Open Online Courses):यह मॉडल उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के रूप में विकसित किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी एक साथ पंजीकरण कर सकते हैं। यह वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हुआ है।6. स्वनिर्देशित अधिगम मॉडल (Self-Paced Learning):इस मॉडल में विद्यार्थी अपनी गति से अध्ययन करते हैं। इसमें कोई समयबद्ध कक्षा नहीं होती और मूल्यांकन भी स्व-अभ्यास आधारित होता है।7. एआई आधारित शिक्षा मॉडल (AI-Based Learning Models):कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित टूल्स जैसे चैटबॉट, पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम और वर्चुअल असिस्टेंट का प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को अनुकूल और प्रभावी बनाया जा रहा है।दूरस्थ शिक्षा के उभरते मॉडल शिक्षण को अधिक सुलभ, सस्ती और प्रभावशाली बना रहे हैं। ये मॉडल न केवल शिक्षार्थी केंद्रित हैं, बल्कि जीवन पर्यंत अधिगम की अवधारणा को भी साकार करते हैं।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-5. वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न सिद्धान्त लिखिए।
उत्तर:- वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संस्था, संगठन या व्यक्ति की वित्तीय गतिविधियों का योजनाबद्ध ढंग से नियमन, नियंत्रण और निगरानी की जाती है। इसका उद्देश्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का अधिकतम और कुशलतम उपयोग करना होता है।
वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख कार्य:
निधियों का अर्जन (Fund Raising)
निधियों का नियोजन (Planning)
निधियों का निवेश (Investment)
लागत नियंत्रण और लाभ अधिकतमकरण
वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
- लाभ अधिकतमकरण का सिद्धांत (Profit Maximization):
इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। वित्तीय निर्णय इस आधार पर लिए जाते हैं कि वे कितना लाभ प्रदान करेंगे। - धन का समय मूल्य (Time Value of Money):
इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में प्राप्त एक रुपये का मूल्य भविष्य के एक रुपये से अधिक होता है। अतः निवेश निर्णय लेते समय वर्तमान मूल्य का ध्यान रखा जाता है। - जोखिम और प्रतिफल सिद्धांत (Risk-Return Trade Off):
निवेश करते समय हमेशा यह देखा जाता है कि उच्च लाभ की संभावना के साथ अधिक जोखिम भी होता है। संतुलन बनाकर ही निर्णय लेना उचित होता है। - लिक्विडिटी बनाम लाभप्रदता (Liquidity vs Profitability):
वित्तीय प्रबंधन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्था के पास इतनी नकदी हो जिससे दैनिक जरूरतें पूरी की जा सकें और साथ ही निवेश से लाभ भी हो। - इष्टतम पूंजी संरचना (Optimum Capital Structure):
यह सिद्धांत बताता है कि इक्विटी और ऋण का ऐसा संतुलन स्थापित किया जाए जिससे पूंजी की लागत न्यूनतम हो और संगठन का मूल्य अधिकतम हो। - नियंत्रण का सिद्धांत (Principle of Control):
वित्तीय गतिविधियों पर निरंतर निगरानी और नियंत्रण रखा जाना चाहिए ताकि अपव्यय न हो और लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। - लाभांश नीति (Dividend Policy):
कंपनी को यह तय करना होता है कि वह कितना लाभ शेयरधारकों को देगी और कितना निवेश में लगाएगी। यह निर्णय वित्तीय रणनीति का हिस्सा होता है।
वित्तीय प्रबंधन किसी भी संस्था के संचालन में रीढ़ की हड्डी के समान है। यह केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि रणनीति, निर्णय और योजना का विज्ञान है। इसके सिद्धांतों के माध्यम से संस्था आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती है।
प्रश्न-6. दूरस्थ शिक्षा में सतत् मूल्यांकन के विभिन्न पैरामीटर पर विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- सतत् मूल्यांकन (Continuous Assessment) दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में एक आवश्यक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की नियमित प्रगति को मापने, सुधारने और उन्हें अधिगम में निरंतर बनाए रखने के लिए किया जाता है।सतत मूल्यांकन के प्रमुख पैरामीटर:1. असाइनमेंट मूल्यांकन (Assignment Evaluation):विद्यार्थी को प्रत्येक इकाई या पाठ्यक्रम के अनुसार असाइनमेंट दिया जाता है, जिससे उनकी पाठ्य सामग्री पर पकड़ और व्यावहारिक समझ आंकी जाती है।2. ऑनलाइन क्विज़ और टेस्ट (Online Quizzes and Tests):विभिन्न समयांतराल पर ऑनलाइन माध्यम से बहुविकल्पीय प्रश्नों या लघु परीक्षणों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है।3. स्वमूल्यांकन (Self-Assessment):शिक्षार्थियों को स्वयं ही अपनी प्रगति का विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। इससे वे अपनी कमजोरियों और सुधार की संभावनाओं को पहचानते हैं।4. समूह कार्य और प्रोजेक्ट मूल्यांकन (Group Work and Project Evaluation):समूहों में किए गए कार्यों और परियोजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की सहभागिता, नेतृत्व और समस्या समाधान की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।5. शैक्षिक फीडबैक (Academic Feedback):विद्यार्थियों को नियमित रूप से व्यक्तिगत या सामूहिक फीडबैक दिया जाता है जिससे वे अपनी कमियों को दूर कर सकें।6. नियमित उपस्थिति और सहभागिता (Regular Participation):ऑनलाइन फोरम, वेबिनार, परामर्श सत्रों में भागीदारी को भी मूल्यांकन का हिस्सा माना जाता है।7. पोर्टफोलियो मूल्यांकन (Portfolio Assessment):विद्यार्थी द्वारा पूरे सेमेस्टर के दौरान की गई सभी शैक्षिक गतिविधियों को एक पोर्टफोलियो में संकलित कर उसका मूल्यांकन किया जाता है।सतत् मूल्यांकन से न केवल विद्यार्थियों की नियमित निगरानी होती है, बल्कि यह उन्हें सक्रिय, उत्तरदायी और समर्पित बनाता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो शिक्षण-सीखने की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-7. मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के मध्य अंतर बताइये। अनुसंधान और विकास में मॉनिटरिंग की भूमिका निर्णायक है। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर:- मॉनिटरिंग (Monitoring) और मूल्यांकन (Evaluation) दोनों ही शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रक्रियाओं के महत्त्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन इनमें मूलभूत अंतर होता है।
मॉनिटरिंग और मूल्यांकन में अंतर:
आधार मॉनिटरिंग मूल्यांकन
उद्देश्य प्रक्रिया की नियमित निगरानी करना परिणामों का विश्लेषण और आकलन करना
समय प्रक्रिया के दौरान होता है प्रक्रिया के अंत में होता है
प्रकार सतत प्रक्रिया एक निश्चित बिंदु पर किया जाता है
दृष्टिकोण प्रक्रिया-केंद्रित परिणाम-केंद्रित
उपयोगकर्ता प्रबंधन और प्रशासक नीति निर्माता और विश्लेषक
अनुसंधान और विकास में मॉनिटरिंग की भूमिका:
- सतत प्रगति का आकलन:
मॉनिटरिंग अनुसंधान की प्रत्येक अवस्था की निगरानी करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्य निर्धारित दिशा में हो रहा है या नहीं। - समस्याओं की पहचान:
यदि अनुसंधान या विकास में कोई रुकावट आती है, तो मॉनिटरिंग के माध्यम से उसे तुरंत पहचाना और सुधारा जा सकता है। - गुणवत्ता नियंत्रण:
यह सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान की गुणवत्ता मानकों के अनुसार बनी रहे। - संसाधनों का प्रभावी उपयोग:
मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि समय, धन और मानव संसाधन का सही उपयोग हो। - पारदर्शिता और उत्तरदायित्व:
निरंतर निगरानी से परियोजना की पारदर्शिता बनी रहती है और शोधकर्ता उत्तरदायी रहते हैं।
मॉनिटरिंग अनुसंधान और विकास की आत्मा है। यह केवल निगरानी नहीं, बल्कि मार्गदर्शन, सुधार और लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। जबकि मूल्यांकन अंतिम परिणामों की समीक्षा करता है, मॉनिटरिंग पूरी प्रक्रिया को दिशा प्रदान करती है।
प्रश्न-8. सम्मिलित पाठ्यक्रम विकास और पाठ्यक्रम अभिकल्पन पर एक निबंध लिखिए।
उत्तर:- सम्मिलित पाठ्यक्रम विकास (Inclusive Curriculum Development) और पाठ्यक्रम अभिकल्पन (Course Designing) आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अत्यंत आवश्यक पहलू बन चुके हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, समान, विविधतापूर्ण और सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाना है।सम्मिलित पाठ्यक्रम विकास का अर्थ:सम्मिलित पाठ्यक्रम वह है जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, जिसमें लिंग, जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो।पाठ्यक्रम अभिकल्पन की प्रक्रिया:1. शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण:सबसे पहले यह तय किया जाता है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को क्या-क्या सिखाया जाएगा।2. विषयवस्तु का चयन:विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और स्तर को देखते हुए विषयवस्तु का चयन किया जाता है जो उन्हें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करे।3. अधिगम अनुभव का निर्माण:शिक्षण सामग्री, गतिविधियाँ, ऑडियो-विजुअल टूल्स आदि के माध्यम से एक समृद्ध अधिगम अनुभव विकसित किया जाता है।4. मूल्यांकन रणनीति:छात्रों की प्रगति मापने हेतु उचित और निष्पक्ष मूल्यांकन पद्धति का समावेश किया जाता है।सम्मिलन के तत्व:बहुभाषिक सामग्री का समावेशलिंग-संवेदनशील भाषाविकलांग व्यक्तियों के अनुकूल सामग्री (Braille, Audio Format आदि)सांस्कृतिक विविधता का आदरसहयोगात्मक अधिगम का वातावरणमहत्त्व:सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलता है।सामाजिक न्याय की स्थापना होती है।शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है।सम्मिलित पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम अभिकल्पन एक समतामूलक और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली की आधारशिला हैं। इनके माध्यम से हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहाँ शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और सुलभ हो।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-9. इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। इसको लेने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएँ बताइए और इंटरनेट कनैक्शन के प्रकार लिखिए।
उत्तर:- इंटरनेट की परिभाषा:
इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो लाखों कंप्यूटरों, सर्वरों और अन्य डिवाइसेस को जोड़ता है। यह सूचनाओं के आदान-प्रदान, ईमेल, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, शिक्षा, मनोरंजन और सरकारी सेवाओं के लिए एक माध्यम है। इसे “नेटवर्क्स का नेटवर्क” भी कहा जाता है।
इंटरनेट एक्सेस के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ:
- कंप्यूटर/स्मार्टफोन/टैबलेट:
इंटरनेट उपयोग के लिए एक ऐसा यंत्र आवश्यक है जिसमें वेब ब्राउज़र और अन्य आवश्यक ऐप्स हों। - नेटवर्क डिवाइस (Router/Modem):
इंटरनेट सिग्नल को कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस तक पहुंचाने के लिए राउटर या मॉडम की आवश्यकता होती है। - इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP):
एक प्रमाणित इंटरनेट सेवा प्रदाता जैसे Jio, Airtel, BSNL आदि से कनेक्शन लेना पड़ता है। - ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र:
जैसे Windows, Android, Chrome, Firefox आदि ब्राउज़र जो वेब को एक्सेस करने की सुविधा दें। - डेटा प्लान या वाई-फाई नेटवर्क:
इंटरनेट चलाने के लिए डेटा प्लान (मोबाइल नेटवर्क) या वाई-फाई कनेक्शन की आवश्यकता होती है।
इंटरनेट कनेक्शन के प्रमुख प्रकार:
- डायल-अप कनेक्शन:
यह पुराना तरीका है जिसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट जुड़ता है। स्पीड धीमी होती है। - ब्रॉडबैंड कनेक्शन:
यह हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा है जो DSL, केबल या फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से उपलब्ध होती है। - वायरलेस कनेक्शन (Wi-Fi):
इसमें बिना तार के इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। यह मोबाइल डाटा, राउटर आदि के जरिए उपयोग होता है। - मोबाइल इंटरनेट (3G/4G/5G):
यह मोबाइल नेटवर्क द्वारा दिया जाने वाला इंटरनेट होता है। यह सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। - सैटेलाइट इंटरनेट:
यह दूरदराज क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाने का तरीका है। - FTTH (Fiber to the Home):
यह फाइबर ऑप्टिक केबल द्वारा सीधे घर तक इंटरनेट पहुंचाने की नई तकनीक है, जो तेज और स्थायी होती है।
इंटरनेट आज के युग की आवश्यकता बन चुका है। इसकी मदद से शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा और शासन में क्रांति आई है। सही कनेक्शन और न्यूनतम उपकरणों के साथ व्यक्ति इंटरनेट की असीम दुनिया से जुड़ सकता है।
प्रश्न-10. एसाइनमेंट सतत् मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। विस्तृत व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- सतत मूल्यांकन (Continuous Evaluation) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्र की सीखने की प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रक्रिया में एसाइनमेंट एक प्रमुख उपकरण के रूप में कार्य करता है।
एसाइनमेंट के माध्यम से सतत मूल्यांकन के लाभ:
- निरंतर सीखने की प्रक्रिया:
एसाइनमेंट के माध्यम से छात्र नियमित रूप से अध्ययन करते रहते हैं, जिससे उनके अध्ययन में सततता बनी रहती है। - सीखने की गहराई:
जब छात्र किसी विषय पर लिखते हैं, तो वे उसे गहराई से समझते हैं। यह केवल रटने की प्रक्रिया नहीं होती। - व्यक्तिगत प्रगति का आकलन:
एसाइनमेंट छात्रों की सोचने की क्षमता, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और अभिव्यक्ति कौशल को दर्शाते हैं। इससे शिक्षक उनकी व्यक्तिगत प्रगति को समझ सकते हैं। - रचनात्मकता को बढ़ावा:
अच्छे एसाइनमेंट रचनात्मकता, मौलिकता और नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। इससे छात्रों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। - शिक्षक-छात्र संवाद:
एसाइनमेंट के मूल्यांकन और फीडबैक के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद होता है जो सीखने को सुदृढ़ करता है। - प्रेरणा का स्रोत:
अच्छे अंक मिलने पर छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे वे और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। - समय प्रबंधन का अभ्यास:
नियत समय में एसाइनमेंट पूरा करने से छात्रों में अनुशासन और समय प्रबंधन की भावना विकसित होती है। - परीक्षा का विकल्प:
विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा में, जहाँ नियमित परीक्षाएं संभव नहीं होतीं, वहाँ एसाइनमेंट परीक्षा का एक विकल्प बनकर उभरता है।
एसाइनमेंट केवल एक औपचारिक कार्य नहीं है, बल्कि यह छात्र की संपूर्ण अकादमिक यात्रा का एक अभिन्न अंग है। यह सतत मूल्यांकन का प्रभावी उपकरण है जो न केवल छात्रों की प्रगति को दर्शाता है, बल्कि उन्हें बेहतर सोचने, समझने और व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है।
प्रश्न-11. इग्नू द्वारा कार्यक्रमों के विकास और अनुमोदन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) भारत का प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालय है जो विभिन्न स्तरों के शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करता है। इग्नू द्वारा किसी शैक्षिक कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले उसके विकास और अनुमोदन की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कार्यक्रम शैक्षणिक गुणवत्ता, व्यावसायिकता तथा शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
- आवश्यकता की पहचान (Need Identification):
किसी भी नए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उसकी आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है। यह प्रक्रिया सर्वेक्षण, कार्यशालाओं, विशेषज्ञ परामर्श तथा समाज की मांग के आधार पर होती है। - परिकल्पना दस्तावेज़ का निर्माण (Preparation of Concept Paper):
कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य को परिभाषित करते हुए एक संक्षिप्त परिकल्पना पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें कार्यक्रम का उद्देश्य, लक्षित समूह, स्तर, संभावित पाठ्यक्रम, और शिक्षण विधियाँ होती हैं। - विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा (Expert Committee Review):
यह दस्तावेज़ विशेषज्ञ समिति को प्रस्तुत किया जाता है जो विषय विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और अकादमिक सदस्यों से मिलकर बनी होती है। समिति कार्यक्रम की उपयुक्तता पर चर्चा करती है। - स्कूल बोर्ड और अकादमिक परिषद् की स्वीकृति (Approval from School Board and Academic Council):
विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर संबंधित स्कूल बोर्ड कार्यक्रम को अपनी स्वीकृति देता है। तत्पश्चात इसे विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। - वित्तीय स्वीकृति (Financial Approval):
प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए आवश्यक बजट का आकलन कर उसे वित्त समिति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। - पाठ्यक्रम विकास (Curriculum Development):
अनुमोदन के बाद पाठ्यक्रम लेखन कार्य शुरू होता है। इसमें पाठ्य सामग्री की योजना, लेखन, संपादन, समीक्षा और मुद्रण सम्मिलित होते हैं। - परीक्षण और मूल्यांकन (Pilot Testing and Feedback):
कभी-कभी कार्यक्रम को सीमित रूप में शुरू किया जाता है ताकि प्रतिक्रिया के आधार पर आवश्यक सुधार किए जा सकें। - कार्यक्रम की शुरूआत (Launching of the Programme):
सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर कार्यक्रम औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया जाता है और उसका प्रचार-प्रसार किया जाता है।
इस प्रकार, इग्नू में कार्यक्रमों का विकास और अनुमोदन एक बहुस्तरीय, वैज्ञानिक एवं भागीदारी प्रक्रिया है, जो गुणवत्ता और उपयोगिता सुनिश्चित करती है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-12. दूरस्थ शिक्षा में वेब को अधिक प्रभावी रूप से कैसे प्रयोग किया जा सकता है? विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- वेब प्रौद्योगिकी ने दूरस्थ शिक्षा को अधिक सुलभ, संवादात्मक और गतिशील बनाया है। इंटरनेट के माध्यम से न केवल अध्ययन सामग्री तक पहुंच आसान हुई है, बल्कि शिक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच प्रभावी संवाद भी संभव हुआ है। वेब का प्रभावी उपयोग दूरस्थ शिक्षा को और अधिक परिणामदायक बना सकता है।
- ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग:
Learning Management Systems (LMS) जैसे Moodle, SWAYAM, Google Classroom आदि के माध्यम से शिक्षार्थी अध्ययन सामग्री, असाइनमेंट, वीडियो व्याख्यान आदि तक पहुंच सकते हैं। इनसे शिक्षण अधिक व्यवस्थित और सुलभ हो जाता है। - वीडियो लेक्चर और वेबिनार:
YouTube, Zoom, Google Meet आदि प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करके शिक्षकों द्वारा सीधे या रिकॉर्डेड व्याख्यान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वेबिनार के माध्यम से विषय विशेषज्ञों से सीधा संवाद भी संभव होता है। - ई-पुस्तकालय और डिजिटल संसाधन:
वेब आधारित ई-लाइब्रेरी, जर्नल्स, ई-बुक्स और डेटाबेस का प्रयोग शिक्षार्थियों को विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। - संवाद और फोरम:
ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, चैट, ईमेल, टेलीग्राम समूहों आदि का उपयोग करके शिक्षार्थियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे सामूहिक अधिगम की भावना विकसित होती है। - मूल्यांकन प्रणाली का डिजिटलीकरण:
ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन, क्विज़, प्रैक्टिकल मूल्यांकन और फीडबैक प्रणाली को वेब के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। - मोबाइल और ऐप आधारित शिक्षण:
मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से शिक्षण को और अधिक लचीला और सुलभ बनाया जा सकता है। IGNOU की “eGyankosh” और “IGNOU eContent” जैसी सेवाएँ इसका उदाहरण हैं। - व्यक्तिगत शिक्षण और ट्रैकिंग:
वेब टूल्स की सहायता से प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति की निगरानी की जा सकती है और उन्हें व्यक्तिगत फीडबैक प्रदान किया जा सकता है। - बहुभाषी और समावेशी शिक्षा:
वेब पर सामग्री को विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत कर अधिक शिक्षार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। दृष्टिबाधित या श्रवणबाधित शिक्षार्थियों के लिए विशेष टूल्स भी उपलब्ध हैं।
इस प्रकार, वेब का प्रभावी प्रयोग दूरस्थ शिक्षा को अधिक संवादात्मक, व्यक्तिगत, गुणवत्तापूर्ण और पहुँच योग्य बनाता है। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों के समावेश से यह क्षेत्र और अधिक समृद्ध होगा।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-13. आधाचास्का विश्वविद्यालय की मोनिटरिंग प्रणाली पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- आधाचास्का विश्वविद्यालय (Athabasca University), कनाडा का एक प्रमुख ओपन विश्वविद्यालय है जो दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी है। इसकी विशेषता यह है कि यह पूर्णतः ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली अपनाता है। इस विश्वविद्यालय की निगरानी प्रणाली (Monitoring System) अत्यंत विकसित और शिक्षार्थी केंद्रित है।
मोनिटरिंग प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ:
- निरंतर मूल्यांकन प्रणाली (Continuous Assessment):
यहां अध्ययन के दौरान नियमित असाइनमेंट, क्विज़, और प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति पर नज़र रखी जाती है। - लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS):
विश्वविद्यालय में Moodle, Blackboard जैसे प्लेटफार्मों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों की लॉगिन गतिविधियाँ, पाठ्यसामग्री उपयोग, फीडबैक, और समय पर कार्य जमा करने की जानकारी एकत्र की जाती है। - ट्यूटर आधारित निगरानी:
प्रत्येक विद्यार्थी को एक ट्यूटर नियुक्त किया जाता है जो उसके प्रगति रिपोर्ट, समस्याओं और शंकाओं पर निगरानी रखता है। ट्यूटर ऑनलाइन संवाद और ईमेल के माध्यम से नियमित संपर्क में रहते हैं। - ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली:
विश्वविद्यालय एक सुरक्षित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का उपयोग करता है। इसमें समय-सीमा, वेबकैम निगरानी, और ब्राउज़र लॉक जैसी तकनीकों का प्रयोग होता है। - फीडबैक आधारित सुधार:
विद्यार्थियों से नियमित फीडबैक लिया जाता है और उसके आधार पर शिक्षण प्रणाली में बदलाव किए जाते हैं। - डेटा एनालिटिक्स:
विश्वविद्यालय छात्रों के प्रदर्शन, उपस्थिति, असाइनमेंट सबमिशन आदि का डेटा एकत्र कर विश्लेषण करता है जिससे कमजोर छात्रों की पहचान कर उन्हें सहायता दी जा सके। - समय प्रबंधन निगरानी:
छात्रों को साप्ताहिक योजनाएँ दी जाती हैं और LMS के माध्यम से उनकी समय प्रबंधन क्षमता पर नज़र रखी जाती है।
आधाचास्का विश्वविद्यालय की निगरानी प्रणाली तकनीक और शिक्षाशास्त्र का उत्कृष्ट संयोजन है। यह न केवल शिक्षार्थियों की प्रगति पर नज़र रखती है, बल्कि उन्हें प्रेरित और मार्गदर्शित भी करती है। यह प्रणाली अन्य ओपन यूनिवर्सिटीज के लिए अनुकरणीय मॉडल है।
प्रश्न-14. दूरस्थ शिक्षा में किसी कार्यक्रम के विकास में मुख्य सोपान कौनसे होते हैं? वर्णन कीजिए।
उत्तर:- दूरस्थ शिक्षा में किसी शैक्षिक कार्यक्रम के विकास की प्रक्रिया बहुस्तरीय होती है, जो शिक्षार्थी केंद्रितता, सामयिकता और तकनीकी उपयोगिता पर आधारित होती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण हो और विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
- आवश्यकता निर्धारण (Needs Assessment):
किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व उसकी सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक और क्षेत्रीय आवश्यकता का आकलन किया जाता है। - परिकल्पना और योजना (Programme Planning):
कार्यक्रम का उद्देश्य, लक्षित समूह, विषय-वस्तु और शिक्षण विधियों की रूपरेखा तैयार की जाती है। यह कार्य योजना निर्माण की आधारशिला है। - पाठ्यक्रम संरचना (Curriculum Design):
इस सोपान में पाठ्यक्रम की रूपरेखा, श्रेयांक, पाठ्य-पुस्तकों की रूपरेखा, मूल्यांकन प्रणाली, और शैक्षिक संसाधनों की योजना बनाई जाती है। - अध्ययन सामग्री का विकास (Development of Learning Material):
दूरस्थ शिक्षा में स्वाध्याय सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विषय विशेषज्ञ, लेखक, संपादक और ग्राफिक डिजाइनरों की सहायता से अध्ययन सामग्री तैयार की जाती है। - तकनीकी संसाधनों का समावेश (Integration of Technology):
ऑडियो-वीडियो, वेब सामग्री, ई-लर्निंग मॉड्यूल आदि को पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है ताकि शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और रोचक बनाया जा सके। - शैक्षिक परामर्श योजना (Academic Counseling Plan):
शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (PCP) और अन्य परामर्श सुविधाएं नियोजित की जाती हैं। - मूल्यांकन एवं परीक्षा योजना (Assessment and Examination Plan):
आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, टर्म-एंड परीक्षा, और परियोजना कार्य आदि की योजना बनाई जाती है। - गुणवत्ता सुनिश्चित करना (Quality Assurance):
सभी सामग्री और गतिविधियों की समीक्षा की जाती है ताकि वे शैक्षिक मानकों पर खरी उतरें। प्रतिक्रिया प्रणाली भी विकसित की जाती है। - प्रचार-प्रसार और प्रवेश प्रक्रिया (Promotion and Admission Process):
कार्यक्रम के प्रचार हेतु विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है और प्रवेश प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाया जाता है।
इस प्रकार, एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का विकास एक सुव्यवस्थित, शिक्षार्थी उन्मुख एवं गुणवत्ता आधारित प्रक्रिया होती है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});प्रश्न-15. दूरस्थ शिक्षा में शैक्षिक परामर्श की कौन-कौनसी गतिविधियां शामिल होती हैं? व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- दूरस्थ शिक्षा में शैक्षिक परामर्श (Academic Counselling) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शिक्षार्थियों को अध्ययन में मार्गदर्शन, प्रेरणा और सहयोग प्रदान करता है। शैक्षिक परामर्श की निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ होती हैं:1. अधिगम मार्गदर्शन (Learning Guidance):परामर्शदाता विद्यार्थियों को यह बताने में सहायता करते हैं कि उन्हें पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ना है, किन इकाइयों से शुरुआत करनी चाहिए, कौन-से विषय अधिक महत्वपूर्ण हैं आदि।2. शंका समाधान (Doubt Clearing Sessions):परामर्श कक्षाओं के दौरान विद्यार्थी अपनी शंकाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। यह संवादात्मक गतिविधि होती है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रत्यक्ष संवाद होता है।3. प्रेरणा और मनोबल बढ़ाना (Motivational Support):दूरस्थ शिक्षा में स्व-अध्ययन कठिन हो सकता है। इसलिए परामर्शदाता विद्यार्थियों को मानसिक रूप से उत्साहित करते हैं ताकि वे अध्ययन में निरंतरता बनाए रखें।4. पाठ्यक्रम समझाना (Explaining Course Content):कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाकर विद्यार्थियों की सहायता की जाती है, जिससे वे विषय को बेहतर समझ सकें।5. मूल्यांकन से संबंधित सहायता (Assessment Support):असाइनमेंट लिखने के निर्देश, उत्तर शैली, परीक्षा की तैयारी और समय प्रबंधन जैसे विषयों पर परामर्श दिया जाता है।6. तकनीकी सहायता (Technical Support):ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग, लॉगिन समस्या, वीडियो लेक्चर देखने की प्रक्रिया आदि में विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है।7. करियर मार्गदर्शन (Career Counselling):परामर्शदाता छात्रों को उनके भविष्य के लिए उचित कोर्स चयन, उच्च अध्ययन के अवसर और रोजगार की संभावनाओं की जानकारी देते हैं।शैक्षिक परामर्श एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षण, मानसिक और व्यावसायिक सभी प्रकार के सहयोग प्रदान करती है। इससे उनकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});vmou so-02 paper , vmou ba 2nd year exam paper , vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4
VMOU EXAM PAPER