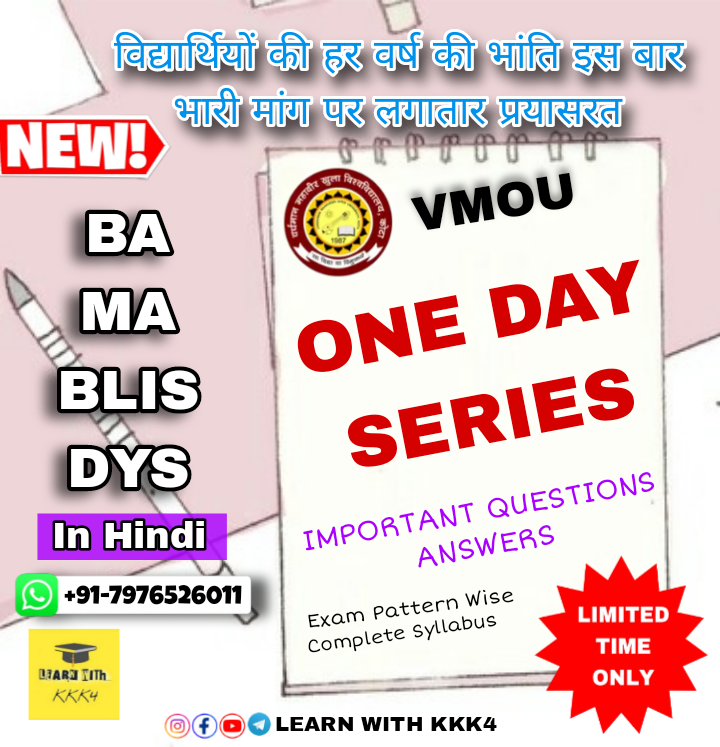VMOU MAGE-02 Paper MA 1st Year (semester-I) ; vmou exam paper
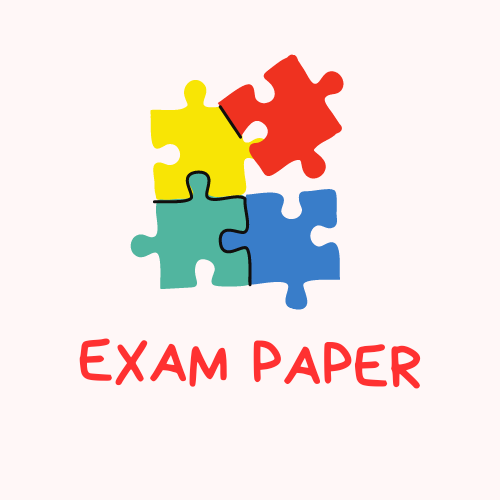
VMOU MA st Year के लिए राज Geograpy ( MAGE-02 , ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.SIAL
उत्तर:- SIAL पृथ्वी की ऊपरी परत है, जो सिलिका (Si) और एल्युमिनियम (Al) से बनी है, इसे महाद्वीपीय परत भी कहते हैं।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.Tidal Hypothesis (ज्वारीय परिकल्पना)
उत्तर:- ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार सूर्य के पास से गुजरते समय किसी तारे के गुरुत्वीय खिंचाव से सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति हुई।
प्रश्न-3.Tethys Sea (टेथिस सागर)
उत्तर:- टेथिस सागर एक प्राचीन सागर था जो गोंडवाना और लौरेशिया के बीच स्थित था, जिससे आज के पर्वत जैसे हिमालय बने
प्रश्न-4. Fringing Reef (तटीय प्रवाल भित्ति):
उत्तर:- तटीय प्रवाल भित्तियाँ समुद्र तट के पास स्थित होती हैं, ये प्रवाल जीवों द्वारा निर्मित होती हैं और समुद्री पारिस्थितिकी में महत्त्वपूर्ण होती हैं।
प्रश्न-5. Fiord Coast (फियोर्ड तट)
उत्तर:- फियोर्ड तट ग्लेशियरों द्वारा कटे गहरे समुद्री खाड़ियों वाले तटीय क्षेत्र होते हैं, जो नॉर्वे जैसे देशों में पाए जाते हैं।
प्रश्न-6. Yardang (पारडंग)
उत्तर:- पारडंग शुष्क क्षेत्रों में हवा द्वारा अपरदन से बनी लंबी, संकीर्ण चट्टानी संरचनाएँ होती हैं जो हवा की दिशा में स्थित होती हैं।
प्रश्न-7. Corals (कोरल्स):
उत्तर:- कोरल्स समुद्री जीवों द्वारा निर्मित कैल्सियम कार्बोनेट की संरचनाएँ होती हैं, जो उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में प्रवाल भित्तियाँ बनाती हैं।
प्रश्न-8. Asthenosphere (दुर्बलतामण्डल):
उत्तर:- दुर्बलतामण्डल पृथ्वी की परत है जो मेंटल में स्थित होती है, यह अर्धद्रव रूप में होती है और प्लेट विवर्तनिकी में सहायक होती है।
प्रश्न-9. Level of compensation (क्षतिपूर्ति तल):
उत्तर:- क्षतिपूर्ति तल वह गहराई है जहाँ सतह पर भार में अंतर के बावजूद पृथ्वी के नीचे द्रव्यमान संतुलित रहता है।
प्रश्न-10. Insolation (सूर्यातप)
उत्तर:- सूर्यातप वह सौर ऊर्जा है जो सूर्य से पृथ्वी की सतह पर सीधे विकिरण के रूप में प्राप्त होती है और जलवायु को प्रभावित करती है।
प्रश्न-11. Insolation (सूर्यताप):
उत्तर:- सूर्यताप वह ऊर्जा है जो सूर्य से पृथ्वी की सतह पर विकिरण के रूप में पहुँचती है और तापमान को प्रभावित करती है।
प्रश्न-12. Sima (सीमा):
उत्तर:- सीमा पृथ्वी की सतही परत का निचला भाग है, जो सिलिका (Si) और मैग्नीशियम (Ma) से मिलकर बना होता है।
प्रश्न-13. Planetesimals (ग्रहिकाएँ)
उत्तर:- उत्तर: ग्रहिकाएँ प्रारंभिक सौर मंडल में धूल और गैस से बनी ठोस पिंड थीं, जिनसे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ।
प्रश्न-14. Structural Benches (संरचनात्मक सीपान):
उत्तर:- संरचनात्मक सीपान ढलानदार भूमि पर कठोर और सॉफ्ट परतों के अवरोध के कारण बनने वाले सीढ़ीनुमा धरातल होते हैं।
प्रश्न-15. Trade Winds (व्यापारिक पवने)
उत्तर:- व्यापारिक पवने भूमध्यरेखीय क्षेत्र से उपोष्ण कटिबंध की ओर नियमित पूर्वी दिशा में बहने वाली स्थायी पवनें होती हैं।
प्रश्न-16. Epicentre (अभिकेन्द्र)
उत्तर:- अभिकेन्द्र क्या होता है?
उत्तर: अभिकेन्द्र वह स्थान होता है जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के झटकों का सीधा केन्द्र होता है, जो भ्रंश रेखा के ऊपर स्थित होता है।
प्रश्न-17. Ozone layer (ओजोन परत):
उत्तर:- ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है।
प्रश्न-18. Graben (ग्राबेन)
उत्तर:- ग्राबेन एक अवनत भ्रंशित क्षेत्र है जो दो भ्रंशों के बीच नीचे धँस जाता है, जैसे – राइन ग्राबेन।
प्रश्न-19. Continental Shelf (महाद्वीपीय निम्नांत तह)
उत्तर:-महाद्वीपीय निम्नांत तह समुद्र में महाद्वीप के किनारे फैली हुई समतल और उथली भूमि है, जो समुद्री संसाधनों से भरपूर होती है।
प्रश्न-20. Metamorphic Rocks (कार्यातरित चट्टानें):
उत्तर:-वे चट्टानें जो उच्च ताप और दाब के कारण रूपांतरित हो जाती हैं, कार्यातरित चट्टानें कहलाती हैं, जैसे- स्लेट, नीस।
प्रश्न-21. Baikal Lake (बैकाल झील):
उत्तर:-बैकाल झील रूस में स्थित विश्व की सबसे गहरी और सबसे प्राचीन मीठे पानी की झील है।
प्रश्न-22. Atoll (एटोल)
उत्तर:- एटोल एक गोलाकार प्रवाल भित्ति द्वीप है, जो समुद्र के बीचोंबीच मृत ज्वालामुखी के चारों ओर बनता है।
प्रश्न-23. Plate Tectonics (प्लेट विवर्तनिकी):
उत्तर:- यह सिद्धांत पृथ्वी की सतह को कई टेक्टोनिक प्लेटों में बाँटा हुआ मानता है, जो परस्पर गति करके भूकंप, पर्वत आदि उत्पन्न करती हैं।
प्रश्न-24. Roaring Forties (गरजता चालीसा)
उत्तर:- गरजता चालीसा दक्षिणी गोलार्द्ध में 40° से 50° अक्षांशों के बीच बहने वाली तेज़ पश्चिमी पवनें होती हैं।
प्रश्न-25. Satellites (उपग्रह):
उत्तर:- उपग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं; ये प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं।
प्रश्न-26. Isostasy (भूसन्तुलन):
उत्तर:- यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी गुरुत्वीय संतुलन में है, भारी पर्वत नीचे धँसे रहते हैं और हल्की सतह ऊपर उठती है।
प्रश्न-27. Gulf Stream (गल्फ स्ट्रीम)
उत्तर:-गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म समुद्री धारा है, जो अमेरिका से यूरोप तक जाती है।
प्रश्न-28. Aphelion (अपसौर):
उत्तर:- यह वह बिंदु होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, सामान्यतः 4 जुलाई के आसपास।
प्रश्न-29. Gorge (गॉर्ज):
उत्तर:- गॉर्ज एक संकीर्ण, गहरी घाटी होती है जो नदी के अपरदन द्वारा कठोर चट्टानों में निर्मित होती है।
प्रश्न-30. Homosphere (सममण्डल)
उत्तर:- सममण्डल वायुमंडल की वह निचली परत है जिसमें गैसों का मिश्रण समान अनुपात में होता है, जो लगभग 80 किमी तक फैली होती है।
प्रश्न-31. Relative Humidity (सापेक्ष आर्द्रता):
उत्तर:- यह वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को अधिकतम संभावित जलवाष्प की तुलना में प्रतिशत में दर्शाती है।
प्रश्न-32. Batholith (बैथोलिथ):
उत्तर:- यह एक विशाल आग्नेय चट्टानी पिंड होता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होकर कठोर बन जाता है, अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
प्रश्न-33. Limestone (चूना पत्थर):
उत्तर:- चूना पत्थर एक तलछटी चट्टान है, जो मुख्यतः कैल्सियम कार्बोनेट से बनी होती है और सीमेंट उद्योग में उपयोगी है।
प्रश्न-34. Mohorovicic Discontinuity (मीहीरोचिसिक असम्बद्धता):
उत्तर:- यह पृथ्वी की बाह्य एवं आन्तरिक परतों के बीच स्थित सीमा है जहाँ भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन होता है।
प्रश्न-35. Dolphin Rise (डॉल्फिन राइज़)
उत्तर:- डॉल्फिन राइज़ दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक पनडुब्बी पर्वत श्रृंखला है, जो समुद्री स्थलाकृति का हिस्सा है।
प्रश्न-36. Granite (ग्रेनाइट):
उत्तर:- ग्रेनाइट एक कठोर आग्नेय चट्टान है जो गहराई में शीतलन द्वारा बनती है और भवन निर्माण में प्रयोग होती है।
प्रश्न-37. Inselberg (इन्सलबर्ग)
उत्तर:- इन्सलबर्ग समतल मैदान में स्थित एक प्राचीन पृथक चट्टानी पहाड़ी होती है, जो अपरदन के कारण अलग दिखती है।
प्रश्न-38. Continental Shelf (महाद्वीपीय मग्नहट):
उत्तर:- यह समुद्र के नीचे फैला महाद्वीप का किनारी क्षेत्र होता है जो धीरे-धीरे गहराई में जाता है और जैव विविधता से भरपूर होता है।
प्रश्न-39. Caldera (कैल्डेरा):
उत्तर:- कैल्डेरा एक विशाल ज्वालामुखीय गड्ढा होता है जो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद शिखर धंसने से बनता है।
प्रश्न-40. Great Barrier Reef (ग्रेट बैरियर रीफ):
उत्तर:- यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित है और समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
Section-B
प्रश्न-1.पृथ्वी को आन्तरिक संरचना के आधुनिक मत को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आधुनिक वैज्ञानिक मत भू-तरंगों, गुरुत्वीय बल, चुम्बकीय क्षेत्र, और उल्कापिंडों के अध्ययन से जाना गया है। पृथ्वी को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है —
- भूपर्पटी (Crust): यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जिसकी मोटाई महाद्वीपीय भागों में लगभग 30-70 किमी और महासागरीय भागों में लगभग 5-10 किमी होती है।
- मंडल (Mantle): यह भूपर्पटी के नीचे स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 2900 किमी तक है। इसे दो भागों में बाँटा गया है — ऊपरी और निचला मंडल।
- कोर (Core): यह पृथ्वी का केंद्र है जो मुख्यतः लोहा और निकेल से बना है। इसे भी बाह्य और आंतरिक कोर में विभाजित किया गया है।
आधुनिक मत पृथ्वी की परतों को उनके भौतिक गुणों जैसे कठोरता, तापमान, और द्रव्यता के आधार पर वर्गीकृत करता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत (Continental Drift Theory) को सर्वप्रथम 1912 में जर्मन भूविज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सभी महाद्वीप पहले एक विशाल महाद्वीप “पैन्जिया” के रूप में एक साथ थे, जो बाद में खंडित होकर वर्तमान स्थिति में आ गए।
सिद्धांत के समर्थन में प्रमाण:
महाद्वीपों की आकृति में समानता (विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका)।
विभिन्न महाद्वीपों पर समान जीवाश्मों की उपस्थिति।
चट्टानों और पर्वत शृंखलाओं की समान रचना।
जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य (ग्लेशियरों के निशान)।
आलोचना:
वेगनर यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि महाद्वीप किस बल से विस्थापित हुए।
उन्होंने महासागरों की पिंड को स्थिर माना, जो आज गलत सिद्ध हो चुका है।
उनका तंत्र केवल प्रेक्षणों पर आधारित था, न कि भौतिक सिद्धांतों पर।
प्लेट विवर्तनिकी (Plate Tectonics) सिद्धांत आने के बाद यह सिद्धांत अधूरा माना गया।
वेगनर का सिद्धांत यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधूरा था, परंतु यह भूगोल और भूविज्ञान में क्रांतिकारी विचार लेकर आया।
प्रश्न-3.महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- महासागरों के जल का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है:
अक्षांश: भूमध्यरेखा के निकट तापमान अधिक होता है और ध्रुवों की ओर घटता है।
सौर विकिरण: सूर्य से प्राप्त ऊर्जा तापमान का मुख्य स्रोत है।
समुद्री धाराएँ: गर्म धाराएँ जल का तापमान बढ़ाती हैं, जबकि ठंडी धाराएँ तापमान घटाती हैं।
पवनें: गर्म हवाएँ सतही जल का तापमान बढ़ाती हैं, जबकि ठंडी हवाएँ घटाती हैं।
समुद्र की गहराई: सतही जल गर्म होता है, परन्तु गहराई के साथ तापमान घटता है।
जल की पारदर्शिता: पारदर्शी जल सूर्य की किरणों को गहराई तक पहुँचने देता है, जिससे तापमान अधिक रहता है।
स्थानीय मौसम: वर्षा, वाष्पीकरण और तूफान भी तापमान को प्रभावित करते हैं।
इन सभी कारकों से महासागरों की जलवायु प्रणाली और समुद्री जीवन प्रभावित होता है।
प्रश्न-आग्नेय चट्टानों की विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:- आग्नेय चट्टानें उन चट्टानों को कहते हैं जो गर्म मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनती हैं। इनकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
मजबूत एवं कठोर: ये सामान्यतः कठोर और घनी होती हैं।
आग्नेय चट्टानें निर्माण उद्योग और वास्तुकला में बहुत उपयोगी मानी जाती हैं।
प्राकृतिक उत्पत्ति: ये चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले मैग्मा के शीतलन से बनती हैं।
क्रिस्टलीय संरचना: इनमें खनिजों के कण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, जो ठंडा होने की गति पर निर्भर करते हैं।
कोई जीवाश्म नहीं: इनमें कोई जैविक अवशेष नहीं होते।
मूल चट्टान: ये सभी प्रकार की अन्य चट्टानों (अवसादी और कायांतरणी) की जनक होती हैं।
दो प्रकार: अंत:शिल (जैसे ग्रेनाइट) और बहिर्शिल (जैसे बेसाल्ट)।
प्रश्न-5.ज्वालामुखी के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- ज्वालामुखी मुख्यतः उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पृथ्वी के भीतर से मैग्मा, गैस और राख बाहर निकलते हैं। इनके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं:
सक्रिय ज्वालामुखी: ये समय-समय पर विस्फोट करते रहते हैं। जैसे — माउंट एटना (इटली)।
निष्क्रिय ज्वालामुखी: इनमें लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, पर भविष्य में हो सकता है। जैसे — फ्यूजी (जापान)।
मृत ज्वालामुखी: ये पूरी तरह शांत हो चुके हैं और इनमें विस्फोट की संभावना नहीं रहती। जैसे — एडम (हवाई)।
दरार ज्वालामुखी: इनमें लावा लंबी दरारों से निकलता है, जैसे — डेक्कन ट्रैप (भारत)।
कैलडेरा: अत्यधिक विस्फोट के बाद जब मुख ढह जाता है, तो गड्ढा बनता है जिसे कैलडेरा कहते हैं।
प्रत्येक प्रकार का ज्वालामुखी क्षेत्रीय भू-आकृति और पर्यावरण को प्रभावित करता है।
प्रश्न-6.वायुमण्डल के संगठन एवं विभिन्न परतों की संरचना का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसकी प्रमुख परतें ऊँचाई के आधार पर विभाजित हैं:
क्षोभमंडल (Troposphere):
पृथ्वी से लगभग 0–12 किमी तक। यहीं पर मौसम की घटनाएँ होती हैं। तापमान ऊँचाई के साथ घटता है।
समतापमंडल (Stratosphere):
12–50 किमी तक। इसमें ओजोन परत होती है जो UV किरणों को अवशोषित करती है। यहाँ तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है।
मध्य मण्डल (Mesosphere):
50–80 किमी तक। यहाँ तापमान पुनः घटता है। यह उल्काओं को जलाने वाला क्षेत्र है।
थर्मोस्फीयर:
80–500 किमी तक। यहाँ आयनमंडल होता है, जो रेडियो संचार में सहायक है।
एक्सोस्फीयर:
सबसे ऊपरी परत, जहाँ गैसें अत्यंत विरल होती हैं और अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं।
प्रश्न-7.ज्वालामुखी क्रिया से सम्बन्धित भू-स्वरूपों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- ज्वालामुखी क्रिया के परिणामस्वरूप पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के भू-स्वरूप बनते हैं। इन्हें दो प्रकारों में बाँटा जा सकता है – बाह्य (extrusive) और आंतरिक (intrusive) स्वरूप।
बाह्य स्वरूप:
ज्वालामुखी शंकु: शंकु आकार का पर्वत, जैसे – फुजीयामा।
लावा पठार: लावा के फैलने से निर्मित पठार, जैसे – डेक्कन ट्रैप।
काल्डेरा: ज्वालामुखी विस्फोट के बाद धँसी हुई गड्ढी।
लावा गुंबद: धीरे-धीरे ठंडा होता लावा जो गुंबद बनाता है।
आंतरिक स्वरूप:
लैकोलिथ: गुंबदाकार संरचना जो चट्टानों के बीच जमती है।
सिल और डाइक: क्षैतिज (sil) या ऊर्ध्व (dyke) दिशा में जमी हुई मैग्मा की चट्टानें।
इन स्वरूपों का अध्ययन भूपटल की रचना और भू-गतिकीय प्रक्रियाओं को समझने में सहायक होता है।
प्रश्न-8.प्रवाल भित्ति के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs) समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी जीवित संरचनाएँ होती हैं जो उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती हैं।
महत्व:
जैव विविधता का केंद्र: प्रवाल भित्तियाँ समुद्री जीवों के लिए आवास प्रदान करती हैं।
मत्स्य उद्योग: मछलियों और अन्य जलीय जीवों की भरपूर मात्रा के कारण यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहयोग देती हैं।
तट सुरक्षा: यह समुद्री लहरों को तोड़कर तटीय भूमि की रक्षा करती हैं।
पर्यटन: प्रवाल भित्तियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं जिससे आय में वृद्धि होती है।
वैज्ञानिक महत्व: जलवायु परिवर्तन, जैव विकास और समुद्री पारिस्थितिकी के अध्ययन में सहायक।
हालांकि, मानवीय गतिविधियाँ जैसे प्रदूषण, गरम जल प्रवाह और अति दोहन इनकी हानि का कारण बन रहे हैं।
इनकी सुरक्षा वैश्विक पारिस्थितिक संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
प्रश्न-9. पृथ्वी की आंतरिक संरचना की नवीन अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अब आधुनिक भौगोलिक तकनीकों, विशेषतः भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से समझा जाता है। पृथ्वी को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है: क्रस्ट (भूपर्पटी), मेंटल (मिथरक), और कोर (केन्द्रक)।
क्रस्ट: यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है, जो महाद्वीपीय (सियाल) और महासागरीय (सिमा) भागों में विभाजित है।
मेंटल: यह क्रस्ट के नीचे स्थित है और लगभग 2900 किमी गहराई तक फैला है। इसमें ऊपरी और निचला मेंटल शामिल होता है।
कोर: यह पृथ्वी का केंद्र है, जो बाह्य तरल कोर और आंतरिक ठोस कोर में विभाजित है।
भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर मोहोरोविसिक असम्बद्धता (क्रस्ट और मेंटल के बीच) और गुटेनबर्ग असम्बद्धता (मेंटल और कोर के बीच) की पहचान की गई है। यह आधुनिक अवधारणा पृथ्वी की परतों के रासायनिक और भौतिक गुणों को स्पष्ट करती है।
प्रश्न-10. प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति की भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए और उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- उत्पत्ति की भौगोलिक दशाएँ:
- गर्म जल (20–30°C): प्रवाल केवल गर्म जल में विकसित होते हैं।
- उथला जल (30-150 मीटर): सूर्य प्रकाश आवश्यक है।
- नमकीन पानी: प्रवाल समुद्री जल में ही पनपते हैं।
- स्वच्छ और निर्मल जल: गंदे पानी में प्रवाल जीवित नहीं रह सकते।
प्रकार:
- प्रत्यास्थ भित्तियाँ (Fringing Reefs):
समुद्र तट के पास विकसित होती हैं। - रुकावट भित्तियाँ (Barrier Reefs):
तट से कुछ दूरी पर होती हैं, बीच में लैगून होता है। - एटोल (Atoll):
एक वृत्ताकार भित्ति जो डूबे हुए ज्वालामुखी द्वीप के चारों ओर बनती है।
प्रवाल भित्तियाँ समुद्री पारितंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जैव विविधता को संरक्षित करती हैं।
प्रश्न-11. आधारतल की संकल्पना को समझाइए।
उत्तर:- आधारतल (Base Level) वह सैद्धांतिक तल है, जिसके नीचे कोई नदी भू-आकृति को अपक्षय (Erosion) नहीं कर सकती। यह जलप्रवाह की अपरदन की अंतिम सीमा होती है।
मुख्यतः दो प्रकार के आधारतल होते हैं:
सामान्य आधारतल (Ultimate Base Level): यह समुद्र तल होता है जो अधिकांश नदियों का अंतिम प्रवाह बिंदु होता है।
स्थानीय आधारतल (Local Base Level): यह झील, कठोर चट्टान, या किसी अन्य बाधा के कारण बनता है जो नदी के अपरदन को अस्थायी रूप से रोकता है।
आधारतल की संकल्पना से यह समझने में सहायता मिलती है कि नदी किस सीमा तक भूमि को काट सकती है। यह भू-आकृति विकास और जल निकासी प्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
प्रश्न-12. भूसंतुलन से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- भूसंतुलन या भौगोलिक समस्थिति (Geo-Isostasy) वह स्थिति है जिसमें पृथ्वी की पर्पटी अपने भार के अनुसार अधस्तल की ओर धँसती या उठती है ताकि संतुलन बना रहे। यह सिद्धांत आर्कटिक खोजकर्ता डटन, एयरिज और प्रैट जैसे वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया।
प्रमुख सिद्धांत:
एयरिज का सिद्धांत (Airy’s Hypothesis): सभी स्थलखंडों की गहराई अलग-अलग होती है लेकिन घनत्व समान होता है। ऊँचे स्थल अधिक गहरे अधस्तल तक जाते हैं।
प्रैट का सिद्धांत (Pratt’s Hypothesis): सभी स्थलखंडों की गहराई एक समान होती है लेकिन घनत्व अलग-अलग होता है।
महत्व:
पर्वतों, पठारों और महासागरों के संतुलन को समझने में सहायक।
हिमनदों के पिघलने से होने वाले ऊँचाई परिवर्तनों को स्पष्ट करता है।
भूसंतुलन पृथ्वी की सतह को संतुलन में बनाए रखने वाली एक मूलभूत भू-भौतिकीय प्रक्रिया है।
प्रश्न-13. सियाल एवं सिमा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- पृथ्वी की ऊपरी सतह को दो प्रमुख परतों में बाँटा गया है – सियाल (SIAL) और सिमा (SIMA)।
सियाल शब्द ‘सिलिकॉन’ (Si) और ‘एल्युमिनियम’ (Al) से मिलकर बना है। यह पृथ्वी की बाहरी परत है जिसे स्थलमंडल भी कहा जाता है। इसमें ग्रेनाइट जैसे हल्के चट्टानी पदार्थ पाए जाते हैं और इसका घनत्व लगभग 2.7 से 2.9 ग्राम/सेमी³ होता है। यह परत महाद्वीपों के नीचे प्रमुख रूप से पाई जाती है।
सिमा शब्द ‘सिलिकॉन’ (Si) और ‘मैग्नीशियम’ (Ma) से बना है। यह सियाल के नीचे स्थित होती है और इसमें बेसाल्ट जैसी भारी चट्टानें होती हैं। इसका घनत्व 2.9 से 3.3 ग्राम/सेमी³ होता है। यह महासागरीय तल के नीचे प्रमुख रूप से पाई जाती है।
सियाल और सिमा का पृथ्वी की संरचना और प्लेट विवर्तनिकी में महत्वपूर्ण स्थान है।
प्रश्न-14. प्रवाल भित्तियों के विकास हेतु उपयुक्त दशाएँ बताइए।
उत्तर:-प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs) समुद्र में रहने वाले जीवों द्वारा निर्मित कैल्शियम कार्बोनेट की संरचनाएँ हैं। इनके विकास के लिए निम्नलिखित दशाएँ आवश्यक होती हैं:
- उष्ण कटिबंधीय तापमान (20°C–30°C): प्रवाल जीव गर्म पानी में पनपते हैं।
- स्वच्छ एवं पारदर्शी जल: सूर्य के प्रकाश की पहुँच आवश्यक है क्योंकि प्रवालों में पाए जाने वाले ज़ूज़ैंथली शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
- छिछला जल (30-50 मीटर): गहराई अधिक होने पर प्रकाश नहीं पहुँचता।
- लवणता: मध्यम लवणता वाला जल उपयुक्त होता है।
- कम गाद/तलछट: गाद वाले जल में प्रवालों का विकास बाधित होता है।
- मध्यम लहरें और धाराएँ: यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में सहायक होती हैं।
इन दशाओं में प्रवाल बहुल क्षेत्रों में फ्रिंजिंग, बैरियर और एटोल जैसी भित्तियों का निर्माण होता है।
प्रश्न-15. नदी के अपरदनात्मक स्थलरूपों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- नदी अपने प्रवाह के दौरान विभिन्न चरणों में अपरदन करती है और कई स्थलरूपों का निर्माण करती है। यह स्थलरूप मुख्यतः ऊपरी या युवावस्था में बनते हैं।
मुख्य अपरदनात्मक स्थलरूप:
वी-आकारी घाटी: तेज प्रवाह के कारण घाटी का निर्माण वी-आकार में होता है।
गॉर्ज (खड्ड): अत्यंत गहरी और संकरी घाटी, जैसे – नर्मदा घाटी।
कैस्केड और जलप्रपात: अचानक ढाल परिवर्तन पर जल प्रपात बनता है, जैसे – जोग जलप्रपात।
पॉथ होल्स (घूर्ण नाल): नदी तल में घूर्णन की प्रक्रिया से बने गोलाकार छेद।
स्पर (स्पर कटिंग): नदी के तीव्र मोड़ पर पार्श्व अपरदन से कटे हुए स्थल।
ये स्थलरूप नदी के ऊर्जावान और अपरदनशील स्वरूप को दर्शाते हैं।
प्रश्न-16. वायुमण्डल के संगठन को समझाइए।
उत्तर:- क्षोभमण्डल (Troposphere):
पृथ्वी से 8–18 किमी तक
मौसम की सभी घटनाएँ इसी में होती हैं
- समतापमण्डल (Stratosphere):
18 से 50 किमी
ओज़ोन परत मौजूद होती है
- मध्यमण्डल (Mesosphere):
50 से 80 किमी
यहाँ तापमान न्यूनतम होता है
- थर्मोस्पीयर (Thermosphere):
80 से 500 किमी
आयनमंडल का भाग, रेडियो संचार में सहायक
- एक्सोस्फियर (Exosphere):
अंतिम परत, जहाँ वायुगणत्व अत्यंत न्यून होता है
संरचना:
78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अन्य गैसें (CO₂, Argon आदि)।
वायुमण्डल पृथ्वी पर तापमान, जलवायु, एवं जीवन के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है।
प्रश्न-17. अटलांटिक महासागर के नितल उच्चावच वर्णन कीजिए।
उत्तर:- अटलांटिक महासागर का नितल (ocean floor) विविध स्थलरूपों से युक्त है जो इसे भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट बनाते हैं।
मुख्य नितल उच्चावच इस प्रकार हैं:
महाद्वीपीय शेल्फ (Continental Shelf): तट के पास उथला क्षेत्र जो समुद्री जीवन के लिए उपयुक्त है।
महाद्वीपीय ढाल (Continental Slope): शेल्फ के बाद की ढलानदार सतह जो गहराई की ओर जाती है।
अटलांटिक मध्य महासागरीय पर्वतमाला (Mid-Atlantic Ridge): यह महासागर के बीचोंबीच स्थित एक विशाल समुद्री पर्वत श्रृंखला है, जो प्लेट विवर्तनिकी के कारण बनी है।
गहरे समुद्री गर्त (Abyssal Plain): समतल और गहरे भाग जो तलछट से भरे होते हैं।
उभार और गर्त: नितल पर कई ज्वालामुखी द्वीप और गर्त पाए जाते हैं, जैसे प्यूर्टो रिको गर्त।
यह विविधता अटलांटिक महासागर को भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत रोचक बनाती है।
प्रश्न-18. पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को अनेक भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारक प्रभावित करते हैं:
- अक्षांश (Latitude): सूर्य की ऊष्मा सीधी या तिरछी मिलने से तापमान भिन्न होता है।
- ऊँचाई (Altitude): ऊँचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड अधिक होती है।
- समुद्र निकटता: समुद्र के समीप स्थित स्थानों का तापमान सम रहता है जबकि अंतर्देशीय क्षेत्रों में तापमान अधिक भिन्न होता है।
- समुद्री धाराएँ: गर्म और ठंडी धाराएँ तटीय क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं।
- वायु प्रवाह: गर्म या ठंडी हवाएँ क्षेत्रीय तापमान में बदलाव लाती हैं।
- मौसमी परिवर्तन: वर्ष के विभिन्न ऋतुओं में सूर्य की ऊँचाई बदलने से तापमान में अंतर आता है।
- मेघावरण और वर्षा: बादल सूर्य की किरणों को रोकते हैं, जिससे तापमान कम रहता है।
इन सभी कारकों से पृथ्वी पर असमान तापमान वितरण होता है।
प्रश्न-19. सूर्यताप क्या है? सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- सूर्यताप (Insolation):
यह पृथ्वी की सतह पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा है। यह तापमान, मौसमी चक्र व जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रभावित करने वाले कारक:
- सौर कोण: सूर्य की किरणें सीधे पड़ने पर अधिक ऊर्जा मिलती है। विषुवत रेखा के निकट अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है।
- दिन की अवधि: लम्बा दिन अधिक ऊर्जा संचित करता है।
- धरातल की प्रकृति: जल, रेत, वन आदि सतहें अलग-अलग मात्रा में सूर्यताप अवशोषित करती हैं।
- वायुमंडलीय स्थिति: बादल, धूल, ओजोन आदि सूर्यताप को रोक सकते हैं।
- ऊँचाई: ऊँचाई बढ़ने पर सूर्यताप अधिक होता है, पर तापमान कम होता है।
इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से पृथ्वी पर तापमान वितरण होता है।
प्रश्न-20. भूसंतुलन को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- भूसंतुलन (Isostasy) वह स्थिति है जिसमें पृथ्वी की सतह की विभिन्न भौगोलिक विशेषताएँ गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध संतुलन बनाए रखती हैं। यह अवधारणा बताती है कि पृथ्वी के ऊँचे क्षेत्र जैसे पर्वत, निचले क्षेत्रों की तुलना में मंथरा में गहराई तक धंसे होते हैं।
इस सिद्धांत को दो प्रमुख वैज्ञानिकों – एयरि (Airy) और प्रैट (Pratt) – ने अलग-अलग रूपों में प्रस्तुत किया।
एयरि सिद्धांत के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र मोटे होते हैं और वे अधिक गहराई तक मंथरा में धँसे होते हैं, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है।
प्रैट सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न भागों का घनत्व अलग-अलग होता है; पर्वतीय क्षेत्र हल्के होते हैं इसलिए ऊँचे उठे होते हैं, जबकि मैदान भारी होते हैं।
भूसंतुलन पृथ्वी की ऊर्ध्व दिशा में स्थिरता को समझाने के लिए उपयोगी सिद्धांत है।
प्रश्न-21. वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- वर्षा के तीन प्रमुख प्रकार हैं:
संवहनात्मक वर्षा (Convectional Rainfall): यह गर्मी के कारण धरातल से जलवाष्प के ऊपर उठने और ठंडा होकर संघनन से होती है। यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य है।
संवर्तनी वर्षा (Cyclonic or Frontal Rainfall): यह तब होती है जब गर्म और ठंडी हवाएँ मिलती हैं। ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर उठाती है जिससे संघनन और वर्षा होती है। यह मध्य अक्षांशों में होती है।
पर्वतीय वर्षा (Orographic Rainfall): यह तब होती है जब नम हवाएँ पर्वतों से टकराकर ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट में यह देखने को मिलती है।
इन तीनों प्रकार की वर्षा का वैश्विक जलवायु पर प्रभाव पड़ता है और ये कृषि एवं पारिस्थितिकी के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं।
प्रश्न-22. वलनों के प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- वलन पृथ्वी की सतह पर संपीड़न बलों के कारण चट्टानों की तहों में उत्पन्न होने वाली लहरदार संरचनाएँ होती हैं। इनके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं:
- प्रकाश वलन (Symmetrical Fold): इसमें दोनों भुजाएँ समान रूप से झुकी होती हैं और अक्ष रेखा सीधी होती है।
- असम वलन (Asymmetrical Fold): इसमें एक भुजा दूसरी की अपेक्षा अधिक झुकी होती है।
- झुका हुआ वलन (Overturned Fold): इसमें दोनों भुजाएँ एक ही दिशा में झुकी होती हैं, और एक भुजा दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है।
- निवलन (Recumbent Fold): इसमें वलन की धुरी क्षैतिज होती है और वलन लगभग लेटा हुआ प्रतीत होता है।
- सम्बन्ध विच्छिन्न वलन (Isoclinal Fold): इसकी दोनों भुजाएँ समान रूप से एक ही दिशा में झुकी होती हैं और परतें समानांतर दिखाई देती हैं।
वलनों का निर्माण भूगर्भीय दबाव और चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करता है।
प्रश्न-23. वायु राशियाँ क्या हैं? विश्व वायु राशियों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- वायु राशियाँ (Air Masses):
वायु राशियाँ वे विशाल वायुमंडलीय भाग हैं जिनमें तापमान, आर्द्रता व घनत्व लगभग समान होता है। ये पृथक वायुगुणों के साथ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होती हैं।
वर्गीकरण:
- स्थल आधारित (Continental):
cT (Continental Tropical): गर्म और शुष्क
cP (Continental Polar): ठंडी और शुष्क
- समुद्र आधारित (Maritime):
mT (Maritime Tropical): गर्म और आर्द्र
mP (Maritime Polar): ठंडी और आर्द्र
- आर्कटिक और अंटार्कटिक (A, AA):
बहुत ठंडी और शुष्क वायु राशियाँ।
विशेषताएँ:
वायु राशियाँ मौसमी बदलाव लाती हैं।
इनके मिलने से मोर्चे (Fronts) बनते हैं, जो वर्षा या तूफान लाते हैं।
ये जलवायु और मौसम प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग हैं।
प्रश्न-24. अटलांटिक महासागर के नितल के उभारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- अटलांटिक महासागर का नितल (seafloor) जटिल स्थलाकृति वाला है, जिसमें अनेक उभार व गहराइयाँ हैं:
- मध्य अटलांटिक पर्वत (Mid-Atlantic Ridge): यह महासागर को उत्तर-दक्षिण दिशा में विभाजित करता है। यह एक विवर्तनिक सीमा है जहाँ नयी महासागरीय प्लेट बनती है।
- गहराइयाँ (Abyssal Plains): समुद्र तल के समतल भाग जो तलछट से ढके होते हैं।
- उपसागरीय घाटियाँ (Submarine Canyons): ये नदियों द्वारा कटाव से बनी गहरी घाटियाँ हैं जो महाद्वीपीय ढाल तक फैली होती हैं।
- महाद्वीपीय ढाल और तली (Continental Slope & Rise): महाद्वीपीय प्लेट का महासागर की ओर ढलान और उसके बाद धीरे-धीरे गहराता भाग।
- समुद्री पर्वत (Seamounts): पानी के नीचे स्थित ज्वालामुखी पर्वत।
यह नितल विवर्तनिकी, महासागरीय धाराओं और तलछट के वितरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रश्न-25. स्थलजात निक्षेप एवं अगाध सागरीय निक्षेप से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- सागरीय निक्षेप (marine deposits) वे पदार्थ होते हैं जो समुद्र की तलहटी पर जमा होते हैं। इन्हें दो भागों में बाँटा जाता है:
- स्थलजात निक्षेप (Terrigenous Deposits):
ये निक्षेप स्थल से नदियों, पवन या हिमनदों द्वारा समुद्र में लाए जाते हैं।
इनमें बालू, मृत्तिका, गाद, और चट्टानों के टुकड़े होते हैं।
ये मुख्यतः तटीय क्षेत्रों और महाद्वीपीय ढाल पर मिलते हैं।
- अगाध सागरीय निक्षेप (Pelagic Deposits):
ये समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं।
इनका स्रोत जैविक (जैसे – प्लवक) या रासायनिक होता है।
इसमें सिलिशियस और कैल्केरियस ऊज़ (ooze), रेड क्ले आदि होते हैं।
इन दोनों प्रकार के निक्षेप महासागर की सतह और तलछट विज्ञान को समझने में सहायक हैं।
प्रश्न-26. बालनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- जब पृथ्वी की सतह पर संपीड़न (compression) बल कार्य करता है तो शिलाएं मोड़ खाकर वक्राकार हो जाती हैं, जिससे ‘बालन’ (Fold) बनते हैं। यह स्थलरूप पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः पाए जाते हैं।
बालनों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:
सम बालन (Symmetrical Fold): इसमें दोनों पार्श्व समान होते हैं और अक्षरेखा लंबवत होती है।
असम बालन (Asymmetrical Fold): इसमें एक पार्श्व लंबा और दूसरा छोटा होता है। अक्षरेखा तिरछी होती है।
पारित बालन (Overturned Fold): जब संपीड़न अत्यधिक हो तो एक पार्श्व दूसरी परत के ऊपर चला जाता है।
नत बालन (Recumbent Fold): इसमें दोनों परतें क्षैतिज हो जाती हैं और बालन लगभग लेटी हुई स्थिति में होता है।
प्रतिक्षेप बालन (Anticline) एवं सिंक्लाइन (Syncline): ऊपरी वक्रता को प्रतिक्षेप एवं निचली वक्रता को सिंक्लाइन कहा जाता है।
ये बालन पर्वत निर्माण की प्रक्रियाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रश्न-27. उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्री क्षेत्रों में विकसित होने वाले तीव्र कम दबाव तंत्र होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में बनते हैं। ये समुद्र की सतह के गर्म जल (26.5°C या अधिक) से ऊर्जा लेकर विकसित होते हैं।
मुख्य विशेषताएँ:
इनका केंद्र ‘आँख’ (Eye) कहलाता है जहाँ शांत वातावरण होता है।
चारों ओर तीव्र वर्षा और तेज हवाएँ होती हैं।
हवाओं की गति 119 किमी/घंटा से अधिक हो सकती है।
इन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नामों से जाना जाता है — जैसे ‘साइक्लोन’ (बंगाल), ‘हैरिकेन’ (अटलांटिक), ‘टाइफून’ (पैसिफिक)।
भारत में यह अधिकतर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनते हैं।
ये चक्रवात व्यापक तबाही कर सकते हैं, इसलिए इनका पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली अत्यंत आवश्यक होती है।
प्रश्न-28. अश्व अक्षांशों पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- अश्व अक्षांश (Horse Latitudes) पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध में भूमध्य रेखा से लगभग 30° अक्षांश पर स्थित उच्च दबाव क्षेत्र होते हैं। यह क्षेत्र सामान्यतः शुष्क, शांत व स्थिर होते हैं।
मुख्य विशेषताएँ:
इन क्षेत्रों में वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है।
वायु की ऊर्ध्वगामी गति होती है जिससे वर्षा नहीं होती, और रेगिस्तान बनते हैं (जैसे सहारा)।
व्यापारिक हवाएँ इन क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं।
नाविकों को इन क्षेत्रों में हवा की कमी के कारण कठिनाई होती थी, इसलिए कभी-कभी घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था, जिससे इनका नाम “Horse Latitudes” पड़ा।
ये क्षेत्र वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
प्रश्न-29. महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले पाँच कारकों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- महासागरीय लवणता समुद्री जल में घुले हुए लवणों की मात्रा को दर्शाती है। यह कई भौगोलिक और भौतिक कारणों पर निर्भर करती है:
- वर्षा और वाष्पन:
जहाँ वाष्पन अधिक होता है (जैसे – उष्ण कटिबंध), वहाँ लवणता अधिक होती है।
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लवणता घट जाती है।
- नदी जल का प्रवाह:
जहाँ बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, वहाँ ताजे पानी के कारण लवणता कम होती है।
- समुद्री धाराएँ:
गर्म धाराएँ लवणता को बढ़ाती हैं, ठंडी धाराएँ कम करती हैं।
- पार्दर्शिता और तापमान:
अधिक पारदर्शी जल में वाष्पन अधिक होता है, जिससे लवणता बढ़ती है।
- वायुमण्डलीय दबाव:
उच्च दबाव क्षेत्रों में वाष्पन तेज होता है, जिससे लवणता बढ़ती है।
ये सभी कारक मिलकर विभिन्न महासागरों में लवणता के वितरण को प्रभावित करते हैं।
प्रश्न-30. वायुदाब किसे कहते हैं? भूमण्डल पर वायुदाब पेटियों का सचित्र वर्णन कीजिए।
उत्तर:- वायुदाब (Air Pressure) पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल के भार के कारण उत्पन्न बल है। इसे मिलीबार (mb) में मापा जाता है। सामान्य वायुदाब समुद्र तल पर 1013.25 mb होता है।
वायुदाब पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पाया जाता। इसके वितरण से ‘वायुदाब पेटियाँ’ बनती हैं।
मुख्य वायुदाब पेटियाँ:
भूमध्यरेखीय निम्नदाब पेटी (0°): अत्यधिक गर्मी के कारण हवा ऊपर उठती है, जिससे निम्न दाब होता है।
उष्णकटिबंधीय उच्चदाब पेटियाँ (30°N और 30°S): यहाँ हवा नीचे गिरती है जिससे उच्चदाब बनता है।
काटिबंधीय निम्नदाब पेटियाँ (60°N और 60°S): यहाँ वायु मिलती है और ऊपर उठती है जिससे निम्नदाब क्षेत्र बनता है।
ध्रुवीय उच्चदाब पेटियाँ (90°N और 90°S): अत्यधिक ठंड के कारण वायु भारी होती है जिससे उच्चदाब बनता है।
प्रश्न-31. भू-संतुलन के सिद्धान्त को परिभाषित कीजिए। सर जॉर्ज एरी व ए. प्रैट के विचारों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए।
उत्तर:- परिभाषा:
भू-संतुलन (Isostasy) वह स्थिति है जिसमें पृथ्वी की परतें गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष संतुलन की स्थिति में होती हैं। यह सिद्धान्त बताता है कि पृथ्वी की ऊँची व नीची संरचनाएँ एक प्रकार के संतुलन में हैं।
सर जॉर्ज एरी का दृष्टिकोण:
एरी के अनुसार पृथ्वी की पर्पटी की मोटाई भिन्न होती है। ऊँचे पर्वतों की जड़ें गहराई तक जाती हैं और इसी कारण वे तैरते रहते हैं, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में।
ए. प्रैट का दृष्टिकोण:
प्रैट के अनुसार पृथ्वी की पर्पटी की मोटाई समान है लेकिन घनत्व में अंतर होता है। ऊँचे स्थल कम घनत्व के होते हैं और नीचे वाले अधिक घनत्व के, जिससे संतुलन बनता है।
तुलना:
एरी ने मोटाई में भिन्नता को कारण माना जबकि प्रैट ने घनत्व में। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि दोनों ही स्थितियाँ पृथ्वी पर पाई जाती हैं।
प्रश्न-32. वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में “महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत” प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, वर्तमान महाद्वीप किसी समय ‘पैंजिया’ नामक एक एकीकृत महाद्वीप का भाग थे। कालांतर में यह महाद्वीप विभाजित होकर विभिन्न दिशाओं में बहकर आज की स्थिति में पहुँच गए।
वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह के समर्थन में निम्न प्रमाण दिए:
अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के तटीय रेखाओं की आकृति में समानता।
विभिन्न महाद्वीपों पर पाए गए समान जीवाश्म जैसे Mesosaurus।
चट्टानों की बनावट और पर्वत श्रृंखलाओं की समानता।
जलवायु संबंधी प्रमाण जैसे गोंडवाना भूमि में हिमनदों के चिह्न।
हालाँकि इस सिद्धांत को उस समय बल प्रदान नहीं किया गया क्योंकि वेगनर महाद्वीपों के गति के कारण को स्पष्ट नहीं कर सके। बाद में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने उनके विचारों को वैज्ञानिक आधार दिया।
प्रश्न-33. दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर:- दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अनेक समुद्री धाराएँ प्रवाहित होती हैं जो जलवायु और नौवहन को प्रभावित करती हैं।
मुख्य धाराएँ:
- दक्षिण विषुवतीय धारा (South Equatorial Current):
पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है।
यह धारा गर्म होती है और विषुवतीय क्षेत्र से निकलती है।
- ब्राजील धारा (Brazil Current):
यह दक्षिण विषुवतीय धारा की शाखा है जो दक्षिण अमेरिका के तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है।
- बंगुएला धारा (Benguela Current):
ठंडी धारा जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से उत्तर दिशा में बहती है।
- पश्चिमी प्रवाह (West Wind Drift):
यह अंटार्कटिका के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है।
इन धाराओं से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तापमान संतुलन, समुद्री जीवन और मौसम प्रणालियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
प्रश्न-34. चातुर्मुख पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- चातुर्मुख’ या ‘फ्रंट’ (Front) वह क्षेत्र होता है जहाँ दो भिन्न वायुराशियाँ एक-दूसरे से मिलती हैं। यह वह संक्रमण क्षेत्र होता है जहाँ तापमान, आर्द्रता, घनत्व आदि में तीव्र अंतर होता है।
मुख्य प्रकार:
गरम मोर्चा (Warm Front): जब गर्म वायुराशि ठंडी वायुराशि को विस्थापित करती है। इससे लगातार वर्षा होती है।
शीत मोर्चा (Cold Front): जब ठंडी वायुराशि गर्म वायुराशि को ऊपर उठाकर विस्थापित करती है। इससे तेज वर्षा और आंधी आ सकती है।
स्थिर मोर्चा (Stationary Front): जब दोनों वायुराशियाँ गतिहीन होती हैं।
प्रतिचक्रवातीय मोर्चा (Occluded Front): जब शीत मोर्चा गरम मोर्चे को पकड़ लेता है और एक मिश्रित मोर्चा बनता है।
फ्रंट्स मौसम परिवर्तन, वर्षा, चक्रवात आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रश्न-35. हिन्द महासागर के नितल उच्चावच का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- हिन्द महासागर का नितल (Ocean Floor) विविध उच्चावच रूपों से युक्त है, जो निम्न प्रकार के हैं:
मध्य महासागरीय पर्वत माला (Mid Oceanic Ridge): यह मध्य हिन्द महासागर में फैली हुई पर्वत श्रंखला है, जहाँ से नई समुद्री सतह बनती है।
यह नितल उच्चावच महासागर की गतिशील प्रक्रियाओं, जैसे प्लेट विवर्तनिकी और समुद्री जीवन, को समझने में सहायक होते हैं।
महाद्वीपीय शेल्फ: तटीय क्षेत्रों के पास समुद्र तल का समतल भाग, जो महाद्वीप का ही विस्तारित भाग होता है।
महाद्वीपीय ढलान: शेल्फ के बाद अचानक गहराई वाली ढाल होती है, जहाँ तल तेजी से नीचे जाता है।
समुद्री मैदान (Abyssal Plain): महासागर का सबसे गहरा और समतल भाग।
समुद्री पर्वत और द्वीप: जैसे — लक्षद्वीप, मालदीव, जो प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण बने हैं।
प्रश्न-36. वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में कीजिए।
उत्तर:- वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि आज के महाद्वीप पहले एक विशाल भूखंड ‘पैन्जिया’ का भाग थे, जो बाद में अलग हो गए। उन्होंने जीवाश्म, चट्टानों और तटीय रेखाओं की समानता को इसका प्रमाण माना।
आलोचना: वेगनर इस विस्थापन का यांत्रिक कारण स्पष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने ज्वार या पृथ्वी के घूर्णन को इसका कारण बताया जो वैज्ञानिक दृष्टि से अस्वीकृत थे।
प्लेट विवर्तनिकी संदर्भ में: 1960 के दशक में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त ने वेगनर की धारणा को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इस सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी की पर्पटी कई प्लेटों में विभाजित है जो मेन्टल की धाराओं द्वारा गतिमान रहती हैं। इससे समुद्र-मध्य कटक, उपसरण क्षेत्र आदि का पता चला, जिसने महाद्वीपीय विस्थापन को सिद्ध किया।
इस प्रकार वेगनर की थ्योरी आज के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त की आधारशिला मानी जाती है, हालाँकि प्रारंभ में उनके द्वारा प्रस्तुत कारण अवैज्ञानिक थे।
प्रश्न-37. वायुमण्डलीय आपदाओं के कारणों और प्रकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- वायुमंडलीय आपदाएँ वे प्राकृतिक घटनाएँ हैं जो वातावरण में असामान्य परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं और जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
प्रमुख प्रकार:
- चक्रवात:
निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर घूमती तेज हवाएँ। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विनाशकारी होते हैं। - बवंडर (Tornado):
छोटे क्षेत्र में तीव्र, घूर्णनशील हवाएँ। अमेरिका में अधिक सामान्य। - गर्मी की लहरें:
लंबे समय तक असामान्य रूप से उच्च तापमान। - तूफान व आंधी:
बिजली, वर्षा और तेज हवा के साथ आने वाली घटनाएँ। - ओलावृष्टि, हिमपात, अतिवृष्टि और सूखा भी वायुमंडलीय आपदाओं में शामिल हैं।
कारण:
जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, समुद्र तापमान में वृद्धि आदि इन आपदाओं की तीव्रता को बढ़ाते हैं।
प्रश्न-38. ज्वालामुखी के विश्व वितरण का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह से मैग्मा, गैस और राख के विस्फोट के रूप में उत्पन्न होते हैं। इनका वितरण प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित होता है।
विश्व में ज्वालामुखियों का प्रमुख वितरण निम्नलिखित क्षेत्रों में पाया जाता है:
प्रशांत ज्वालामुखीय घेरा (Ring of Fire): यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला है, जहाँ विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं।
भूमध्यसागरीय क्षेत्र: यूरोप और एशिया के मिलन स्थल पर स्थित है, जहाँ इटली का विसुवियस और एटना ज्वालामुखी प्रमुख हैं।
अफ्रीकी दरार क्षेत्र: अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है जहाँ किलिमंजारो और माउंट केन्या जैसे ज्वालामुखी हैं।
मध्य-अटलांटिक क्षेत्र: यहाँ महासागरीय रिजों पर ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं।
ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक गतिशीलता और नवभूमि निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
प्रश्न-39. पवन के अपरदन तथा निक्षेप से विकसित होने वाले भू-आकार की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन एक प्रमुख भू-आकृतिक शक्ति है। यह मिट्टी और रेत को उड़ाकर अपरदन तथा निक्षेपण करती है।
अपरदनात्मक स्थलरूप:
- यार्डंग – कठोर और नरम चट्टानों के असमान अपरदन से बनी लम्बी, संकरी रेखीय पहाड़ियाँ।
- डिफ्लेशन होल्स – हवा द्वारा मिट्टी हटाने से बने गड्ढे।
- मशरूम रॉक – आधार पर अधिक अपरदन से छत्र जैसी चट्टानें।
निक्षेपात्मक स्थलरूप:
- बालू के टीले (Dunes) – जैसे बारखान, लम्बी दिशा में बनने वाले रेत के ढेर।
- लोएस – हवा द्वारा लाई गई महीन धूल का व्यापक निक्षेपण जो उपजाऊ होता है।
इस प्रकार पवन द्वारा बनाये गए स्थलरूपों में अपरदन व निक्षेपण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
Section-C
प्रश्न-1.पृथ्वी की उत्पत्ति की ग्रहाणु परिकल्पना समझाइए।
उत्तर:- ग्रहाणु परिकल्पना (Planetesimal Hypothesis) सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित एक प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे 1905 में थॉमस सी. चैम्बरलिन (Thomas C. Chamberlin) और फॉरेस्ट आर. मूल्टन (Forest R. Moulton) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस परिकल्पना ने नव-कैंट लैप्लास सिद्धांत के विकल्प के रूप में वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया।
मुख्य धारणा:
इस परिकल्पना के अनुसार, सूर्य पहले से ही एक स्वतंत्र तारा था और एक दूसरा तारा सूर्य के पास से गुजरा। इस समीपता के कारण सूर्य के बाहरी भागों से पदार्थ खिंचकर बाहर आ गया। इस निकले हुए पदार्थ के छोटे-छोटे कणों को “ग्रहाणु” (Planetesimals) कहा गया। बाद में इन्हीं ग्रहाणुओं ने परस्पर संघटन कर ग्रहों, उपग्रहों और अन्य पिंडों को जन्म दिया।
परिकल्पना की प्रक्रिया:
- निकटता की घटना: सूर्य के पास से एक विशाल तारा गुजरा, जिससे गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण सूर्य के वायुमंडल से पदार्थ खिंच गया।
- ग्रहाणुओं की उत्पत्ति: खिंचे हुए पदार्थ से असंख्य ठोस कण बने, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया।
- ग्रह निर्माण: ग्रहाणुओं के बीच टकराव और संघटन के माध्यम से धीरे-धीरे बड़े-बड़े पिंड बने, जो ग्रहों में परिवर्तित हो गए।
- ग्रहों की कक्षा: इन ग्रहों ने सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमना शुरू कर दिया।
परिकल्पना की विशेषताएँ:
यह सिद्धांत सौरमंडल में ग्रहों की विविधता और उनकी सूर्य से दूरी के अनुसार आकार में अंतर को समझाने का प्रयास करता है।
यह ग्रहों के सापेक्ष छोटे आकार को भी स्पष्ट करता है।
आलोचना:
खिंचे हुए पदार्थ की मात्रा से पर्याप्त ग्रह निर्माण नहीं हो सकता।
सौरमंडल में सभी ग्रह एक ही तल में क्यों घूमते हैं, इसका उत्तर नहीं दे पाता।
पास से तारे का आना एक अत्यंत दुर्लभ खगोलीय घटना है।
ग्रहाणु परिकल्पना ने सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या का एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, किंतु आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार यह परिकल्पना अब अप्रचलित हो चुकी है। वर्तमान में नेब्युलर हाइपोथेसिस (Nebular Hypothesis) को अधिक वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.अपरदन चक्र’ पर डेविस व पेनक के विचारों की तुलना कीजिए।
उत्तर:- ‘अपरदन चक्र’ (Cycle of Erosion) भू-आकृति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विलियम मॉरिस डेविस और वॉल्डर पेनक ने इस सिद्धांत को भिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया। इन दोनों के विचारों की तुलना इस प्रकार की जा सकती है:
- डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत:
डेविस ने 1899 में “Geographical Cycle” का प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि जब किसी स्थल को ऊँचा उठाया जाता है, तो वहाँ अपरदन शुरू होता है और समय के साथ तीन अवस्थाओं में यह प्रक्रिया पूरी होती है:
प्रारंभिक अवस्था (youth): क्षेत्र ऊँचा और खड़ी ढाल वाला होता है। नदियाँ तेज गति से बहती हैं और वी-आकार की घाटियाँ बनती हैं।
मध्य अवस्था (maturity): ढाल कम होती है, अपरदन स्थिर हो जाता है और नदियाँ मेन्डरिंग करने लगती हैं।
वृद्धावस्था (old age): स्थल काफी समतल हो जाता है, जिसे ‘पेनप्लेन’ कहा जाता है।
डेविस का मॉडल समय आधारित और काल्पनिक है, जो स्थिर जलवायु व बिना टेक्टोनिक गतिविधि के अधीन होता है।
- पेनक का अपरदन चक्र सिद्धांत:
पेनक, एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने डेविस के समय-आधारित सिद्धांत की आलोचना करते हुए, एक ढाल-आधारित (slope-controlled) अपरदन चक्र प्रस्तुत किया। उनके अनुसार:
ढाल परिवर्तनशील होती है और स्थलरूप का विकास निरंतर होता है।
उनका सिद्धांत ‘समसामयिक उत्थान और अपरदन’ (simultaneous uplift and denudation) पर आधारित है।
पेनक के अनुसार, नदियों की कटाव क्षमता ढाल की तीव्रता पर निर्भर करती है, न कि समय पर।
- तुलना:
तत्व डेविस पेनक
दृष्टिकोण समय-आधारित ढाल-आधारित
आधार काल्पनिक अवस्थाएँ गतिशील और वास्तविक परिस्थिति
प्रक्रिया क्रमबद्ध अवस्थाएँ निरंतर परिवर्तनशील अवस्था
जलवायु स्थिर जलवायु परिवर्तनशील जलवायु
भू-उत्थान तात्कालिक सतत और क्रमिक
डेविस का सिद्धांत सरल व शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी है, जबकि पेनक का दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी व वैज्ञानिक है। आज आधुनिक भूगोल में पेनक का सिद्धांत अधिक प्रासंगिक माना जाता है क्योंकि यह भूगर्भीय घटनाओं और जलवायु परिवर्तनों को समाहित करता है।
प्रश्न-3. वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत (Continental Drift Theory) की प्रस्तावना जर्मन भू-वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर (Alfred Wegener) ने वर्ष 1912 में की थी। इस सिद्धांत के अनुसार आज के महाद्वीप एक समय में एक ही विशाल महाद्वीप “पैन्जिया (Pangaea)” के भाग थे, जो धीरे-धीरे टूटकर आज की स्थिति में पहुँच गए।
मुख्य बिंदु –
- पैन्जिया की संकल्पना –
वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर केवल एक ही विशाल महाद्वीप था जिसे ‘पैन्जिया’ कहा जाता है। यह दो भागों में विभाजित हुआ – उत्तरी भाग ‘लारेशिया’ और दक्षिणी भाग ‘गोंडवाना लैंड’। इनके बीच टेथिस सागर स्थित था। - महाद्वीपों का विचलन –
समय के साथ ये भाग अलग-अलग दिशाओं में बहते रहे और वर्तमान महाद्वीप बने। यह प्रक्रिया अब भी जारी है। - प्रमाण –
भौगोलिक प्रमाण: अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के तटों की आकृति एक-दूसरे से मेल खाती है।
जीवाश्म प्रमाण: एक जैसे जीवाश्म जैसे Mesosaurus, Glossopteris आदि विभिन्न महाद्वीपों में पाए गए हैं।
शैल-रचनात्मक प्रमाण: भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के चट्टानों में समानता।
जलवायु प्रमाण: अंटार्कटिका में कोयले के भंडार, जो संकेत देते हैं कि वह एक समय में गर्म प्रदेश रहा होगा।
- कमियाँ –
वेगनर यह नहीं बता सके कि महाद्वीपों को खिसकाने वाली शक्ति क्या है। इस कारण उस समय वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। - महत्त्व –
यह सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी (Plate Tectonics) के विकास का आधार बना और पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं की समझ को आगे बढ़ाया।
हालाँकि वेगनर का सिद्धांत कुछ वैज्ञानिक कमियों के कारण प्रारंभ में विवादास्पद रहा, परंतु यह भूगोल और भूगर्भशास्त्र के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ।
प्रश्न-4. वायुराशियों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न वायुराशियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर:- वायुराशि (Air Mass) वह विशाल वायुमंडलीय भाग होती है जिसमें हजारों किलोमीटर तक क्षैतिज रूप से लगभग समान तापमान, आर्द्रता एवं दाब जैसी विशेषताएँ पाई जाती हैं। ये वायुराशियाँ पृथ्वी की सतह के ऊपर उस क्षेत्र के गुणों को अवशोषित कर लेती हैं, जहाँ वे उत्पन्न होती हैं, और उन्हें अपने साथ अन्य क्षेत्रों तक ले जाती हैं।
वायुराशि की परिभाषा:
वायुराशि एक विशाल वायुमंडलीय खंड है जिसमें क्षैतिज रूप में एकरूप तापमान और आर्द्रता होती है तथा जो एक विशेष स्रोत क्षेत्र से उत्पन्न होती है।
वायुराशि के प्रमुख घटक:
- स्रोत क्षेत्र (Source Region): जहाँ वायुराशि बनती है, जैसे महासागर, रेगिस्तान या बर्फीले क्षेत्र।
- तापमान और आर्द्रता: वायुराशि का तापमान एवं नमी उसके स्रोत क्षेत्र पर निर्भर करता है।
वायुराशियों के प्रकार:
मुख्यतः वायुराशियों को उनके स्रोत क्षेत्र के आधार पर पाँच प्रमुख प्रकारों में बाँटा गया है:
- स्थलीय ध्रुवीय वायुराशि (Continental Polar – cP):
स्रोत: महाद्वीपीय बर्फीले क्षेत्र (उत्तरी कनाडा, साइबेरिया)
गुण: ठंडी और शुष्क
प्रभाव: ठंडी हवाएँ, शीत लहरें
- समुद्री ध्रुवीय वायुराशि (Maritime Polar – mP):
स्रोत: ठंडे समुद्री क्षेत्र (उत्तर अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत)
गुण: ठंडी और नम
प्रभाव: वर्षा एवं बादल, विशेषकर तटीय क्षेत्रों में
- स्थलीय उष्णकटिबंधीय वायुराशि (Continental Tropical – cT):
स्रोत: गर्म शुष्क स्थल जैसे सहारा, थार मरुस्थल
गुण: गर्म और शुष्क
प्रभाव: लू जैसी गर्म हवाएँ, शुष्कता
- समुद्री उष्णकटिबंधीय वायुराशि (Maritime Tropical – mT):
स्रोत: गर्म समुद्री क्षेत्र जैसे बंगाल की खाड़ी, कैरेबियन सागर
गुण: गर्म और नम
प्रभाव: भारी वर्षा, मानसून
- आर्कटिक या अंटार्कटिक वायुराशि (Arctic/Antarctic – A):
स्रोत: ध्रुवीय क्षेत्र
गुण: अत्यंत ठंडी और शुष्क
प्रभाव: कड़ाके की ठंड, बर्फबारी
महत्त्व:
वायुराशियाँ जलवायु को प्रभावित करती हैं।
इनके टकराव से मौसमी परिवर्तन, चक्रवात, तूफान और वर्षा होती है।
मानसूनी हवाओं का गठन भी वायुराशियों पर निर्भर करता है।
वायुराशियाँ पृथ्वी के मौसम तंत्र का महत्वपूर्ण घटक हैं। ये अपने स्रोत क्षेत्र के गुणों को लेकर लंबी दूरी तक प्रभाव डालती हैं और विभिन्न मौसमीय घटनाओं की जननी बनती हैं।
प्रश्न-5. विश्व की सौरमंडलीय पवनों का विवरण दीजिए।
उत्तर:- सौरमंडलीय या ग्रहकीय पवनें (Planetary Winds) वे स्थायी पवनें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में उच्च दाब व निम्न दाब के क्षेत्रों के कारण उत्पन्न होती हैं। ये पवनें बड़े पैमाने पर भूमध्यरेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और पृथ्वी के घूर्णन तथा कोरिऑलिस बल के कारण मुड़ जाती हैं।
मुख्य सौरमंडलीय पवनों के प्रकार:
- व्यापारिक पवनें (Trade Winds):
ये पवनें विषुवत रेखा से लगभग 30° अक्षांश तक के क्षेत्र में चलती हैं।
उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर-पूर्वी दिशा से और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण-पूर्वी दिशा से चलती हैं।
ये पवनें भूमध्यरेखा की ओर चलती हैं और वहां बादल व वर्षा उत्पन्न करती हैं।
- पश्चिमी पवनें (Westerlies):
ये पवनें 30° से 60° अक्षांश के बीच चलती हैं।
उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण-पश्चिम से और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर-पश्चिम से चलती हैं।
ये शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु को प्रभावित करती हैं और चक्रवातों को जन्म देती हैं।
- ध्रुवीय पवनें (Polar Easterlies):
ये पवनें 60° से 90° अक्षांश के बीच उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती हैं।
ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं और अत्यधिक ठंडी व शुष्क होती हैं।
इन पवनों के प्रभाव:
जलवायु पर प्रभाव: ये पवनें विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु को नियंत्रित करती हैं।
महासागरीय धाराओं पर प्रभाव: ये महासागरीय धाराओं की दिशा निर्धारित करती हैं।
वर्षा वितरण: ये पवनें वर्षा के क्षेत्रों को निर्धारित करती हैं।
ग्रहकीय पवनें पृथ्वी के वायुमंडलीय संतुलन का प्रमुख आधार हैं। इनका अध्ययन मौसम पूर्वानुमान, कृषि, व जलवायु विज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है।
प्रश्न-6. धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- पृथ्वी के धरातल पर तापमान का वितरण असमान होता है और यह विभिन्न भौगोलिक, भौतिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:
- अक्षांश (Latitude):
अक्षांशीय स्थिति के अनुसार सूर्य की किरणों की तीव्रता बदलती है। विषुवत रेखा पर किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ अधिक तापमान होता है। जैसे-जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान घटता है। - समुद्र तल से ऊँचाई (Altitude):
जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, तापमान घटता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। - समुद्र तट से दूरी (Distance from Sea):
समुद्र के पास स्थित क्षेत्रों में तापमान में कम अंतर होता है जबकि आंतरिक क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान भिन्नता देखी जाती है। - महासागरीय धाराएँ (Ocean Currents):
गर्म धाराएँ तापमान को बढ़ाती हैं जबकि ठंडी धाराएँ तापमान को घटाती हैं। जैसे – गल्फ स्ट्रीम यूरोप के पश्चिमी तट को गर्म बनाए रखती है। - पवनें (Winds):
स्थानीय और वैश्विक हवाएँ तापमान वितरण को प्रभावित करती हैं। गरम या ठंडी पवनें अपने साथ उस क्षेत्र का तापमान लेकर आती हैं। - बादल और वर्षा:
बादलों की उपस्थिति सूर्य की किरणों को धरातल तक पहुँचने से रोकती है जिससे दिन का तापमान कम और रात का तापमान अधिक रहता है। - वनस्पति और भूमि की प्रकृति:
हरित क्षेत्र अधिक नमी बनाए रखते हैं और तापमान को संतुलित करते हैं, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्र अधिक गर्म होते हैं।
इस प्रकार उपर्युक्त कारक धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं और जलवायु विविधता का कारण बनते हैं।
प्रश्न-7. पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलरूपों का सचित्र विवरण दीजिए।
उत्तर:- मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन एक प्रमुख भू-आकृतिक कारक है। यह रेत और धूल कणों को उड़ाकर विभिन्न स्थलरूपों का निर्माण करती है। नीचे प्रमुख पवन अपरदनात्मक स्थलरूपों का सचित्र विवरण दिया गया है:
(1) यार्डंग (Yardang)
यह कठोर और मुलायम शिलाओं की परतों पर पवन के द्वारा की गई असमान अपघर्षण से निर्मित होता है।
कठोर चट्टानें उभरी रहती हैं और मुलायम चट्टानें कटकर हट जाती हैं।
यह संरचना पवन की दिशा में लंबवत होती है।
📌 चित्र:
(2) मशरूम शिला (Mushroom Rock)
यह पवन के द्वारा जमीन के निकट तल पर अधिक अपघर्षण होने के कारण चट्टान के निचले भाग को काटती है।
परिणामस्वरूप चट्टान ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली होकर मशरूम के आकार की बन जाती है।
📌 चित्र:
(3) जिप्सम की खुरदुरी सतह (Ventifacts)
ये वे चट्टानें होती हैं जो एक या अधिक दिशाओं से आने वाली पवनों द्वारा घिसी जाती हैं।
इस पर त्रिकोणीय कटान उभर आते हैं।
(4) डिफ्लेशन हॉलो (Deflation Hollow)
जब पवन किसी क्षेत्र से रेत और मिट्टी को हटाकर गड्ढा बना देती है, तो उसे डिफ्लेशन हॉलो कहते हैं।
यह मरुस्थलीय बेसिन निर्माण का कारण बनता है।
पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलरूप मरुस्थलों में पवन की शक्तिशाली भूमिका को दर्शाते हैं और ये भू-आकृतिक विविधता को समृद्ध करते हैं।
प्रश्न-8. ज्वार-भाटा के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
उत्तर:- ज्वार-भाटा (Tides) समुद्र के जलस्तर में नियमित उतार-चढ़ाव की प्रक्रिया है, जो मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होती है।
प्रमुख प्रकार –
(1) सम ज्वार (Spring Tide)
जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं (पूर्णिमा और अमावस्या के दिन),
तब चंद्र और सूर्य के गुरुत्व बल मिलकर अधिकतम ज्वार उत्पन्न करते हैं।
इसे सम ज्वार कहते हैं।
जलस्तर: अत्यधिक ज्वार (High Tide) और अत्यधिक भाटा (Low Tide)।
(2) निःसृत ज्वार (Neap Tide)
जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र से 90 डिग्री कोण पर होते हैं (अष्टमी और अष्टमी से ठीक पहले-पश्चात),
तब उनका संयुक्त प्रभाव कम होता है।
इससे ज्वार और भाटा की ऊँचाई कम होती है।
जलस्तर: मध्यम ज्वार और मध्यम भाटा।
(3) दैनिक ज्वार (Diurnal Tide)
एक दिन में एक उच्च ज्वार और एक निम्न भाटा आता है।
यह अधिकतर मैक्सिको की खाड़ी जैसे स्थानों में होता है।
(4) अर्धदैनिक ज्वार (Semi-diurnal Tide)
एक दिन में दो उच्च ज्वार और दो निम्न भाटा आते हैं।
यह विश्व के अधिकांश समुद्रों में सामान्य है।
(5) मिश्रित ज्वार (Mixed Tide)
जब ज्वार-भाटा की ऊँचाई समान नहीं होती और समय अंतराल भी अनियमित होता है।
यह मिश्रित ज्वारीय प्रदेश कहलाता है।
ज्वार-भाटा समुद्र तटीय क्षेत्रों के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिससे नौवहन, मत्स्य पालन, ऊर्जा उत्पादन आदि प्रभावित होते हैं। इनके प्रकार भौगोलिक स्थिति और चंद्र-सूर्य की स्थिति पर निर्भर करते हैं।
प्रश्न-9. महासागरीय धाराओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- महासागरीय धाराएँ (Ocean Currents) समुद्र के सतही जल की विशाल धाराएँ होती हैं, जो विभिन्न दिशाओं में निरंतर गति से बहती हैं। ये गर्म एवं ठंडी दोनों प्रकार की होती हैं और पृथ्वी की जलवायु, मौसम तथा मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव डालती हैं।
- जलवायु पर प्रभाव:
गर्म धाराएँ जैसे – गल्फ स्ट्रीम, तटीय क्षेत्रों को गर्म बनाती हैं।
ठंडी धाराएँ जैसे – कैलिफोर्निया या पेरू धारा, तटवर्ती क्षेत्रों को ठंडा बनाती हैं।
ये धाराएँ हवाओं को भी प्रभावित करती हैं, जिससे वर्षा और सूखा प्रभावित होते हैं।
- कृषि पर प्रभाव:
जहाँ ठंडी धाराएँ बहती हैं वहाँ नमी कम होती है और सूखा पड़ता है। वहीं गर्म धाराएँ वर्षा में सहायक होती हैं, जिससे कृषि को लाभ होता है। - मत्स्य उद्योग पर प्रभाव:
ठंडी धाराएँ पोषक तत्त्वों को ऊपर लाती हैं जिससे मछलियों की संख्या अधिक होती है। पेरू और जापान तट पर समृद्ध मत्स्य क्षेत्र इसी कारण हैं। - समुद्री परिवहन पर प्रभाव:
धाराओं की दिशा और वेग जहाजों के मार्ग निर्धारण में सहायक होते हैं। इन्हें समझ कर ईंधन की बचत की जाती है। - समुद्री जीवन पर प्रभाव:
धाराएँ समुद्र के तापमान और पोषक तत्वों को प्रभावित करती हैं जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। - प्राकृतिक आपदाओं पर प्रभाव:
कुछ धाराओं के असंतुलन जैसे ‘एल नीनो’ और ‘ला नीना’ से वैश्विक जलवायु में असामान्यता आती है जिससे बाढ़, सूखा आदि उत्पन्न होते हैं।
इस प्रकार महासागरीय धाराएँ वैश्विक जलवायु प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनका प्रभाव प्राकृतिक और मानवीय जीवन दोनों पर पड़ता है।
प्रश्न-10. चक्रवात क्या है? शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- चक्रवात (Cyclone) एक कम वायुदाब का क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर उच्च दाब से हवाएँ केंद्र की ओर घूमती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में घूमती हैं।
चक्रवातों के प्रकार:
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone)
- शीतोष्ण चक्रवात (Temperate or Extra-Tropical Cyclone)
शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति:
शीतोष्ण चक्रवात 30° से 60° अक्षांश के बीच पश्चिमी पवन क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है:
- वायुदाब व तापमान विपरीतता:
शीत व गर्म वायुमंडलीय पिंडों (air masses) के संपर्क से एक ‘फ्रंट’ बनता है।
गर्म व शीत वायु के मध्य यह फ्रंट अस्थिर हो जाता है और चक्रवात बनता है।
- उत्पत्ति क्षेत्र:
अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, अमेरिका के पूर्वी तट, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आदि।
- संरचना:
शीतोष्ण चक्रवातों में गर्म व ठंडी वायु की सीमाओं पर दो प्रकार के फ्रंट होते हैं:
गर्म फ्रंट (Warm Front)
ठंडा फ्रंट (Cold Front)
यह चक्रवात कई सौ किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है।
- दिशा व गति:
ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं।
इनकी गति 30 से 50 किमी/घंटा तक हो सकती है।
- प्रभाव:
भारी वर्षा, बर्फबारी, तूफान व तेज हवाएँ।
कृषि व परिवहन पर प्रभाव।
शीतोष्ण चक्रवात पृथ्वी के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। इनका अध्ययन मौसम विज्ञान व कृषि के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है।
प्रश्न-11. प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत (Plate Tectonic Theory) भूगोल और भूगर्भ विज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत है, जो पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों की संरचना एवं गतिशीलता को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत 1960 के दशक में विकसित हुआ और वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तथा समुद्री विस्तार सिद्धांत का एक विस्तृत रूप है।
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी की बाहरी कठोर परत को स्थलमंडल (Lithosphere) कहते हैं, जो कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें ठोस होती हैं और इनके नीचे स्थित अधस्तल (Asthenosphere) नामक अर्ध-पिघली परत पर तैरती हैं।
मुख्य प्रकार की प्लेट सीमाएँ:
- संमिलन सीमा (Convergent Boundaries): जहाँ दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। इससे पर्वत श्रृंखलाएँ और उपसरण क्षेत्र (Subduction Zones) बनते हैं, जैसे – हिमालय।
- विचलन सीमा (Divergent Boundaries): जहाँ दो प्लेटें दूर हटती हैं, जिससे नई भूपर्पटी बनती है, जैसे – मिड-अटलांटिक रिज।
- संधान सीमा (Transform Boundaries): जहाँ दो प्लेटें एक-दूसरे के पास से खिसकती हैं, जैसे – सैन एंड्रियास भ्रंश।
प्रमुख प्रभाव:
भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण प्लेटों की गति से जुड़े हैं।
समुद्री तल का विस्तार और महासागरीय गर्त का निर्माण होता है।
भूपटल के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है।
यह सिद्धांत पृथ्वी की सतह पर होने वाले सभी भूगर्भीय परिवर्तनों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है और इसे आधुनिक भूगोल का आधार स्तंभ माना जाता है।
प्रश्न-12. डेविस द्वारा दिए गए अपरदन चक्र की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- विलियम मॉरिस डेविस (William Morris Davis) ने 1899 में “अपरदन चक्र” (Cycle of Erosion) की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे भू-आकृतिक विकास की ‘सिद्धांतात्मक व्याख्या’ के रूप में जाना जाता है। डेविस को ‘आधुनिक भू-आकृतिक विज्ञान का जनक’ भी कहा जाता है।
अपरदन चक्र की परिभाषा:
डेविस के अनुसार, किसी क्षेत्र की भू-आकृति समय के साथ तीन अवस्थाओं से होकर गुजरती है – युवा (Youth), प्रौढ़ (Maturity), और वृद्धावस्था (Old Age)। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही ‘अपरदन चक्र’ कहा जाता है।
चक्र की अवस्थाएँ:
- युवा अवस्था (Youth):
क्षेत्र का ऊँचाई अन्तर (Relief) अधिक होता है।
नदियाँ तीव्र गति से बहती हैं, खड़ी घाटियाँ और जल प्रपात बनते हैं।
अपरदन की दर अधिक होती है।
- प्रौढ़ अवस्था (Maturity):
जलविभाजक (Divides) स्पष्ट होते हैं।
घाटियाँ विस्तृत हो जाती हैं और नदी घाटियों में स्थिर हो जाती है।
भूमि अपेक्षाकृत समतल होने लगती है।
- वृद्ध अवस्था (Old Age):
अधिकांश क्षेत्र समतल हो जाता है जिसे पैनीप्लेन (Peneplain) कहा जाता है।
नदियाँ मन्द गति से बहती हैं, अपरदन की दर न्यूनतम होती है।
अपवर्तन या रिउथ (Rejuvenation):
यदि किसी भूभाग में कोई नवीन उन्नयन (upliftment) या जलवायु परिवर्तन हो जाए, तो पुनः अपरदन सक्रिय हो सकता है। इस प्रक्रिया को पुनर्यौवन (Rejuvenation) कहते हैं।
विशेषताएँ:
यह सिद्धांत भू-आकृति के क्रमिक विकास को समझाता है।
यह समय को एक महत्वपूर्ण कारक मानता है।
यह एक आदर्श मॉडल है जो स्थिर जलवायु और स्थलाकृतिक अवस्थाओं को आधार मानता है।
आलोचना:
यह सिद्धांत बहुत आदर्शवादी है और आधुनिक प्रक्रियाओं की विविधता को नहीं दर्शाता।
डेविस ने जलवायु और शैल प्रकारों की भूमिका को कम आंका।
समय को परिभाषित करने में अस्पष्टता है।
डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत भू-आकृतिक विकास को समझाने की दिशा में एक मील का पत्थर रहा है। हालाँकि इसे अब कई आधुनिक सिद्धांतों ने चुनौती दी है, फिर भी इसकी शैक्षिक और ऐतिहासिक महत्ता बनी हुई है।
प्रश्न-13. पृथ्वी के ऊष्मा बजट का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- पृथ्वी का ऊष्मा बजट (Heat Budget) उस संतुलन को दर्शाता है जो पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में विकीर्ण ऊर्जा के बीच होता है। यह संतुलन पृथ्वी के तापमान को स्थिर बनाए रखता है।
- ऊष्मा प्राप्ति –
पृथ्वी को ऊर्जा मुख्यतः सूर्य से मिलती है।
कुल सौर ऊर्जा का मात्र 100% पृथ्वी तक आती है, लेकिन:
30% परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है (Albedo)।
20% वायुमंडल और बादल अवशोषित कर लेते हैं।
50% पृथ्वी की सतह अवशोषित करती है।
- ऊष्मा हानि –
पृथ्वी प्राप्त ऊर्जा को विभिन्न रूपों में खोती है:
दीर्घतरंग विकिरण (Infrared Radiation) के रूप में।
वाष्पन (Evaporation) और चालन (Conduction) द्वारा।
पृथ्वी विकिरण का कुछ भाग वायुमंडल द्वारा वापस अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ‘ग्रीनहाउस प्रभाव’ होता है।
- ऊष्मा संतुलन –
जो ऊष्मा पृथ्वी को मिलती है, वही अंततः अंतरिक्ष में लौटती है।
इस प्रकार ग्रह का ताप संतुलित रहता है।
यदि यह संतुलन बिगड़े तो जलवायु परिवर्तन (Climate Change) हो सकता है।
- कारक –
बादलों की उपस्थिति, वायुमंडलीय संघटन, सतह का प्रकार, अक्षांश आदि।
पृथ्वी का ऊष्मा बजट पृथ्वी के जलवायु तंत्र और तापमान संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन वैश्विक स्तर पर असर डाल सकता है।
प्रश्न-14. प्रवाल भित्तियों के प्रकार उचित उदाहरण से समझाइए।
उत्तर:- प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs) समुद्र की सतह के पास पाए जाने वाले कठोर ढांचे हैं जो प्रवाल पॉलीप्स (Coral Polyps) द्वारा निर्मित होते हैं। ये जैविक और खनिजीय प्रक्रिया से निर्मित होती हैं तथा समुद्री पारिस्थितिकी का आधार होती हैं।
प्रवाल भित्तियों की विशेषताएँ:
इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है।
ये उष्णकटिबंधीय समुद्रों में 30° उत्तर से 30° दक्षिण अक्षांश के मध्य पाई जाती हैं।
जल का तापमान 20°C से अधिक होना चाहिए।
प्रवाल भित्तियों के प्रकार:
- किनारी भित्ति (Fringing Reef):
यह तटीय क्षेत्र से सटी हुई होती है।
समुद्र तट के पास उथले पानी में पाई जाती है।
समुद्र से भूमि तक सीधा जुड़ाव होता है।
उदाहरण: रेड सी (Red Sea) और अंडमान द्वीपों के पास।
- आवरण भित्ति (Barrier Reef):
यह तट से कुछ दूरी पर होती है और इनके बीच एक लैगून (lagoon) होता है।
यह आकार में बड़ी और समुद्र तल से ऊँचाई में अधिक होती है।
उदाहरण: ग्रेट बैरियर रीफ (Great Barrier Reef), ऑस्ट्रेलिया — विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति।
- एटोल भित्ति (Atoll Reef):
यह वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार होती है, जिसमें केंद्र में लैगून होता है।
यह ज्वालामुखी द्वीपों के चारों ओर बनती है जो बाद में डूब जाते हैं।
उदाहरण: मालदीव और लक्षद्वीप समूह।
प्रवाल भित्तियों का महत्त्व:
ये जैव विविधता के केंद्र हैं।
तटीय क्षेत्रों को समुद्री तूफानों और कटाव से बचाती हैं।
मछली पालन एवं पर्यटन का स्रोत हैं।
समुद्री पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती हैं।
खतरे और संरक्षण:
प्रदूषण, समुद्री तापमान में वृद्धि, अम्लीकरण (ocean acidification) और मानवीय गतिविधियाँ प्रवाल भित्तियों के लिए खतरा हैं।
संरक्षण उपाय: जैव आरक्षित क्षेत्र, सतत पर्यटन, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम।
प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के सुंदरतम और महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। इनके संरक्षण की आवश्यकता है ताकि जैव विविधता और समुद्री जीवन बना रहे।
प्रश्न-15. नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूपों का सचित्र विवरण दोजिए।
उत्तर:- नदियाँ अपनी धारा में बहते हुए भूमि को काटती (अपकर्षण), ले जाती (परिवहन) और कहीं-कहीं जमा करती (निक्षेपण) हैं। इन प्रक्रियाओं से अनेक प्रकार के अपरदनात्मक स्थलरूप बनते हैं। निम्नलिखित प्रमुख स्थलरूप हैं:
- वी-आकारी घाटी (V-Shaped Valley):
नदी जब ऊँचे पर्वतीय भागों में बहती है तो तेज गति से कटाव करती है, जिससे वी-आकार की घाटियाँ बनती हैं। - जलप्रपात (Waterfall):
जब नदी कठोर चट्टान से नरम चट्टान पर गिरती है, तो एक जलप्रपात बनता है। - खड्ड (Gorge):
यह बहुत गहरी और सँकरी घाटी होती है, जो निरंतर कटाव से बनती है। - पोथोल्स (Potholes):
नदी के तल में गोल-गोल गड्ढे होते हैं जो पत्थरों के घूमने से बनते हैं। - इंटरलॉकिंग स्पर (Interlocking Spurs):
यह तब बनते हैं जब नदी कठोर चट्टानों के बीच से होकर बहती है और मार्ग में ज़िगज़ैग करती है।
चित्रात्मक विवरण:
आप एक सरल रेखाचित्र बना सकते हैं जिसमें:
ऊपर पहाड़ी क्षेत्र हो, उसमें वी-आकारी घाटी और जलप्रपात दर्शाया जाए।
घाटी के किनारों पर इंटरलॉकिंग स्पर दिखाएं।
नदी तल में गोल गड्ढों के रूप में पोथोल्स दिखाएं।
ये स्थलरूप नदी के अपरदन की प्रक्रिया के प्रमाण होते हैं और समय के साथ स्थलाकृति को पूरी तरह बदल देते हैं।
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4
VMOU MAGE-02 Paper , vmou ma geographyr exam paper ,vmou exam paper 2030 vmou exam paper 2028-29 vmou exam paper 2027 vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU EXAM PAPER