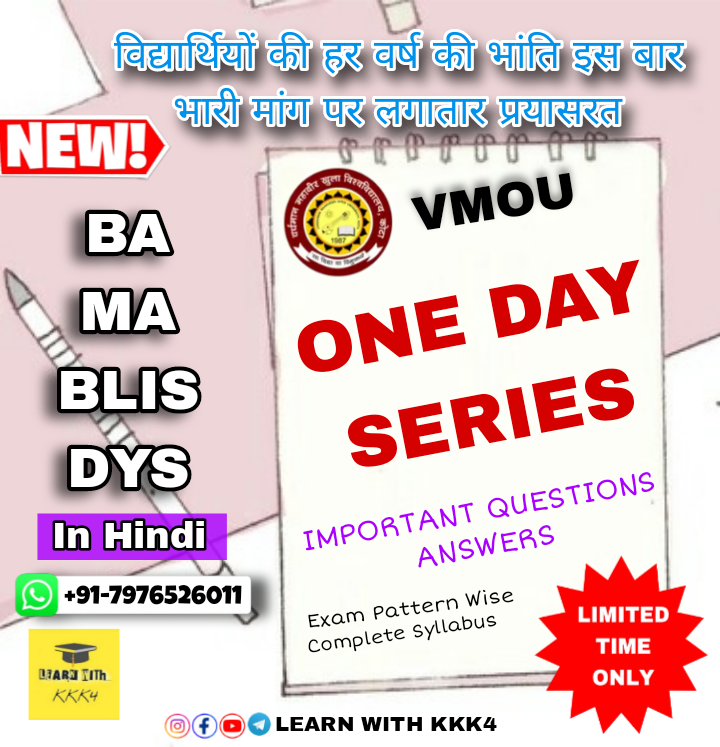VMOU MAHI-06 Paper MA Final Year ; vmou exam paper
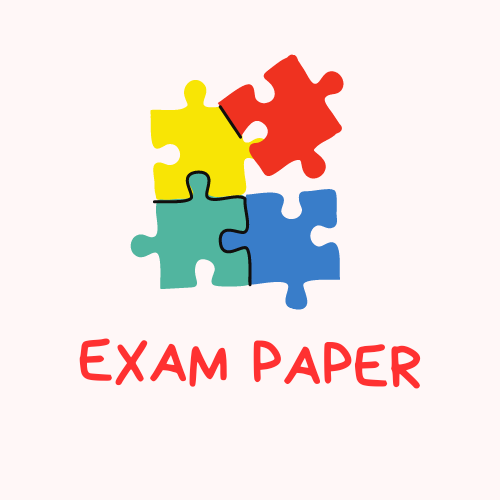
VMOU MA Final Year के लिए HISTORY ( MAHI-06 , प्राचीन भारत में व्यापार एवं नगरीकरण
( Trade and Urbanization in incident india)
) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे?
उत्तर:- चाणक्य (कौटिल्य या विष्णुगुप्त) ,जो मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त के प्रमुख मंत्री थे।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.प्राचीन भारत के किन्हीं दो समुद्री व्यापारिक मार्गों के नाम बताइए।
उत्तर:- ताम्रलिप्ति से श्रीलंका और भरुच से रोमन साम्राज्य तक
प्रश्न-3.प्राचीन भारत के किन्हीं दो व्यापारिक मार्गों के नाम बताइए।
उत्तर:-उत्तरापथ (Uttarapatha) और दक्षिणापथ (Dakshinapatha)
प्रश्न-4. प्राचीन भारत के दक्षिणापथ मार्ग के प्रमुख शहरों के नाम बताइए।
उत्तर:- प्रतीष्ठान (Paithan) और अमरावती (Amaravati)
प्रश्न-5. राजस्थान के किन जिलों में कालीबंगा और बैराट स्थित हैं?
उत्तर:- कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जबकि बैराट (पुराना नाम विराटनगर) जयपुर जिले में स्थित है।
प्रश्न-6. पुनर्जागरण के क्या कारण थे?
उत्तर:- पुनर्जागरण के प्रमुख कारणों में व्यापार का विकास, प्राचीन ग्रंथों की खोज, मुद्रण कला का आविष्कार, वैज्ञानिक सोच का उदय और चर्च की शक्ति में कमी शामिल हैं।
प्रश्न-7. मौर्यकाल के दो अभिलेखों के नाम बताइए।
उत्तर:- अशोक के शिलालेख और लघु शिलालेख (Minor Rock Edicts) हैं।
प्रश्न-8. सातवाहन शासकों के दो अभिलेखों के नाम बताइए।
उत्तर:- सातवाहन शासकों के प्रमुख अभिलेख नासिक गुफा अभिलेख और कनकगिरि अभिलेख हैं।
प्रश्न-9. श्रेणी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- श्रेणी व्यवस्था प्राचीन भारत में विभिन्न कारीगरों और व्यापारियों के संगठनों को कहते थे, जो आर्थिक कार्यों का संचालन और सदस्यों के हितों की रक्षा करते थे।
प्रश्न-10. बोस्टन टी पार्टी के विषय में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:- 1773 में अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने ब्रिटिश चाय पर कर के विरोध में बोस्टन बंदरगाह में चाय की पेटियाँ फेंक दीं, इसे बोस्टन टी पार्टी कहते हैं।
प्रश्न-11. पुनर्जागरण की परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- पुनर्जागरण 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में हुआ एक बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक जागरण था, जिसने मध्ययुगीन विचारधारा को चुनौती दी।
प्रश्न-12. वैदिक काल में ‘निष्का’ को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- निष्का वैदिक काल की एक स्वर्ण धातु की मुद्रा या आभूषण थी, जिसका उपयोग लेनदेन और दान में किया जाता था।
प्रश्न-13. हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
उत्तर:- “माइन कैम्पफ” (Mein Kampf)
प्रश्न-14. साम्राज्यवाद से आपका का तात्पर्य है
उत्तर:- साम्राज्यवाद वह नीति है जिसमें कोई शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है और उनका शोषण करता है।
प्रश्न-15. प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर:- प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था, जो आर्थिक गतिविधियों और व्यापार को नियंत्रित करता था।
प्रश्न-16. राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंगों के नाम बताइए।
उत्तर:- राष्ट्रसंघ के मुख्य अंग थे— महासभा, परिषद, स्थायी सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन।
प्रश्न-17. प्राक् मौर्यकालीन व्यापार और वाणिज्य की जानकारी देने वाले मुख्य बौद्ध स्रोतों के नाम बताए।
उत्तर:- प्राक् मौर्यकालीन व्यापार की जानकारी अंगुत्तर निकाय, जातक कथाएँ और विनय पिटक जैसे बौद्ध स्रोतों से मिलती है।
प्रश्न-18. नेपोलियन कौन था?
उत्तर:- नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान सैन्य नेता और सम्राट था, जिसने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में कई युद्धों के माध्यम से साम्राज्य स्थापित किया।
प्रश्न-19. चाणक्य कौन थे ?
उत्तर:-चाणक्य मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और चन्द्रगुप्त मौर्य के गुरु थे; उन्होंने ‘अर्थशास्त्र’ ग्रंथ की रचना की।
प्रश्न-20. सर्वेन्टीज’ कौन था ?
उत्तर:- मिगुएल द सर्वेन्टीज एक प्रसिद्ध स्पेनिश लेखक थे, जिन्होंने ‘डॉन किहोते’ नामक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास की रचना की थी।
प्रश्न-21. धार्मिक सुधार आन्दोलन की परिभाषित कीजिए।
उत्तर:-धार्मिक सुधार आन्दोलन वह आंदोलन था जिसने ईसाई धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार, पाखंड और चर्च की सत्ता को चुनौती देकर धर्म में नवीनता और शुद्धता लाई।
प्रश्न-22. बास्तिल के बारे में आप क्या जानते हो?
उत्तर:-बास्तिल पेरिस का एक किला और जेल थी, जिसकी 1789 में भीड़ द्वारा की गई ध्वंस की घटना फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है।
प्रश्न-23. शहरीकरण से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:- शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होता है, जिससे शहरों का विस्तार और विकास होता है।
प्रश्न-24. औद्योगिक क्रान्ति के दौरान दो प्रसिद्ध आविष्कारों के नाम बताइए।
उत्तर:- औद्योगिक क्रांति के दौरान ‘स्पिनिंग जेनी’ और ‘स्टीम इंजन’ जैसे प्रसिद्ध आविष्कार हुए, जिन्होंने उत्पादन को तीव्र गति दी।
प्रश्न-25. बर्लिन समझौता कब हुआ था?
उत्तर:- बर्लिन समझौता 1878 ई. में हुआ था, जिसमें यूरोप के प्रमुख देशों ने बाल्कन क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर आपसी समझौता किया था।
प्रश्न-26. रोम-बर्लिन-टोकियो धुरी का निर्माण कब हुआ था ?
उत्तर:- रोम-बर्लिन-टोकियो धुरी का निर्माण वर्ष 1940 में हुआ, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का गठन हुआ।
प्रश्न-27. आहत मुद्रा की परिभाषित कीजिए।/आहत मुद्रा से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- आहत मुद्रा वे प्रारंभिक सिक्के थे, जिन्हें हाथ से पीटकर बनाया जाता था और इन पर चिन्ह उकेरे जाते थे।
प्रश्न-28. इटली के एकीकरण के तीन प्रमुख नेताओं के नाम बताइए।
उत्तर:- इटली के एकीकरण के तीन प्रमुख नेता मैजिनी, गैरीबाल्डी और कवूर थे, जिन्होंने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व द्वारा एकता स्थापित की।
प्रश्न-29. लोधल क्या था?
उत्तर:- लोधल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, जो गुजरात में स्थित है और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था।
प्रश्न-30. हड़प्पा सभ्यता के दो जानवरों के नाम बताइए।
उत्तर:- बैल (zebu) और गैंडा
प्रश्न-31. सिन्धु सरस्वती सभ्यता के दो पालतू जानवरों के नाम बताइए।
उत्तर:- प्रमुख पालतू जानवर बैल और भैंस थे, जो कृषि व व्यापारिक उपयोग में लाए जाते थे।
प्रश्न-32. . श्रेष्ठी’ से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- श्रेष्ठी प्राचीन भारत में व्यापारिक गिल्ड या समूह के प्रमुख को कहा जाता था, जो आर्थिक गतिविधियों का नेतृत्व करता था।
प्रश्न33. . मार्टिन लूथर के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर:- मार्टिन लूथर एक जर्मन धार्मिक सुधारक थे, जिन्होंने 1517 में ’95 थेसिस’ लिखकर कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार का विरोध किया।
प्रश्न-34. . प्राचीन भारत में व्यापार और शहरीकरण में अन्तर्सम्बन्धों को समझाइए।
उत्तर:- व्यापार के विकास ने नगरों के निर्माण को बढ़ावा दिया, और नगरों में व्यापारिक केंद्र बनने से नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई।
प्रश्न-35. इटली एकीकरण का नेतृत्य किसने किया था?
उत्तर:- इटली के एकीकरण का नेतृत्व ग्यूसेपे गैरीबाल्डी, कावूर और विक्टर इम्मानुएल द्वितीय ने किया, जिन्होंने विभिन्न राज्यों को एक राष्ट्र में संगठित किया।
प्रश्न-36. मौर्य अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:- मौर्य अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जिसमें कर व्यवस्था, व्यापारिक नियंत्रण और शिल्प उद्योग का विशेष योगदान था।
प्रश्न-37. द्वितीय विश्व युद्ध को काल को इंगित कीजिए।
उत्तर:- द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ई. में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से शुरू होकर 1945 ई. में जापान की हार और हिरोशिमा-नागासाकी पर परमाणु बम से समाप्त हुआ।
प्रश्न-38. बिलाफ्रांका संधि पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
उत्तर:- 1859 में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच बिलाफ्रांका संधि हुई, जिससे इटली की एकता की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई।
प्रश्न-39. नगरीकरण को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या, संसाधन और आर्थिक गतिविधियाँ ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर स्थानांतरित होती हैं।
प्रश्न-40. कब और कहाँ एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था ?
उत्तर:- एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनाऊ एम इन नामक स्थान पर हुआ था।
प्रश्न-41. बर्लिन की संधि पर कब हस्ताक्षर किये गये ?
उत्तर:- बर्लिन की संधि पर 13 जुलाई 1878 को हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बाल्कन देशों की राजनीतिक स्थिति तय की गई।
प्रश्न-42. प्राचीन भारत के किन्हीं चार मेलों के नाम बताइए।
उत्तर:- प्राचीन भारत के प्रमुख मेले: प्रयाग मेला, कुंभ मेला, वैशाली मेला, और पुष्कर मेला।
प्रश्न-43. वॉटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया ?
उत्तर:- वॉटर फ्रेम का आविष्कार 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने किया, जो कपड़ा उद्योग में क्रांतिकारी मशीन थी।
प्रश्न-44. प्राक् मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के दो प्रमुख बौद्ध स्रोतों के नाम बताइए।
उत्तर:- प्राक् मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के प्रमुख बौद्ध स्रोत “जतकों” और “विनय पिटक” को माना जाता है।
Section-B
प्रश्न-1.हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन की मुख्य विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:- हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन विकसित और संगठित था। प्रमुख विशेषताओं में कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और श्रम विभाजन प्रमुख थे। लोग गेंहू, जौ, तिल, कपास आदि की खेती करते थे और बैल चालित हल का प्रयोग करते थे। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों होते थे — मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, और ईरान से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। मुद्रा के रूप में आहत मुद्राएँ (पंचमार्क) चलन में थीं। मृदभांड, मनके, धातु के औज़ार, कपड़े और आभूषणों का निर्माण होता था। दस्तकार और व्यापारी वर्ग स्पष्ट रूप से विभाजित थे। बंदरगाह नगर लोथल से समुद्री व्यापार संचालित होता था। कुल मिलाकर, हड़प्पा काल का आर्थिक जीवन सुनियोजित और समृद्ध था।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित और संगठित था। कृषि, पशुपालन, कारीगरी, व्यापार और शिल्प इस काल की मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ थीं। सिंचाई की उन्नत प्रणाली के माध्यम से गेहूं, जौ, कपास आदि की खेती होती थी। पशुपालन में गाय, बैल, भेड़, बकरी, हाथी आदि का पालन किया जाता था।
कारीगरी में मिट्टी के बर्तन, धातु के उपकरण, मणिकाओं की माला, मुहरें एवं मूर्तियाँ प्रमुख थीं। हस्तशिल्प के केंद्र जैसे चन्हुदड़ो, लोथल आदि प्रसिद्ध थे।
अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकसित था। मेसोपोटामिया, फारस और खाड़ी देशों से व्यापारिक संबंध थे। व्यापार के लिए आहत मुद्राओं (Punch Marked Coins) का उपयोग होता था और लोथल में एक समुद्री बंदरगाह भी था।
इस काल में नियोजित नगर निर्माण, ग्रंथियों वाला लेखन, और समृद्ध व्यापार प्रणाली आर्थिक जीवन की साक्षी देती है। यह भारत की सबसे पुरानी और व्यवस्थित आर्थिक प्रणाली थी।
प्रश्न-3. प्राचीन भारत में संचार के साधनों की विवेचना कीजिए।/प्राचीन भारत में संचार के साधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में संचार के साधन सीमित होते हुए भी सशक्त थे। राजकीय दूत, घुड़सवार संदेशवाहक, और डाक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों और संदेशवाहकों की महत्ता का उल्लेख है। अशोक के शिलालेख भी तत्कालीन संचार व्यवस्था को दर्शाते हैं। धार्मिक स्थलों, तीर्थयात्राओं, मेलों और व्यापारिक मार्गों से भी जानकारी का आदान-प्रदान होता था। शिक्षा संस्थानों जैसे नालंदा और तक्षशिला में भी बौद्धिक विचारों का आदान-प्रदान संचार का माध्यम था। सम्राटों के फरमान, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि भी संचार के प्राचीन साधन माने जाते हैं।
प्रश्न-4. प्राचीन भारत में प्रमुख मेलों के नाम बताइए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में अनेक धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक मेले आयोजित होते थे। ये मेले जनसमुदाय के लिए मिलन स्थल का कार्य करते थे और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र होते थे। प्रमुख मेलों में प्रयाग का कुंभ मेला, पुष्कर मेला, हरिद्वार मेला, नासिक मेला, और सौराष्ट्र का शिवरात्रि मेला प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त राजगृह, काशी, मथुरा, और उज्जयिनी जैसे नगरों में भी वार्षिक मेले आयोजित होते थे, जो धार्मिक स्थलों से संबंधित होते थे। इन मेलों में हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, कपड़े, धातु वस्तुएं आदि का व्यापार होता था। मेला न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक था, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी अभिन्न अंग था।
प्रश्न-5.प्राचीन भारत में राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में राजस्व व्यवस्था मुख्यतः भूमि कर पर आधारित थी। राजा अपनी आमदनी का मुख्य स्रोत भूमि से प्राप्त कर को मानता था। इस कर को ‘भाग’ या ‘बलि’ कहा जाता था, जो आमतौर पर पैदावार का छठा या चौथाई भाग होता था। किसान अपनी उपज का एक भाग राज्य को देता था। मनु स्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में इस व्यवस्था का उल्लेख है। इसके अलावा व्यापार, पशुपालन, जंगल और खनिजों से भी कर लिया जाता था। कुछ क्षेत्रों में सारस्वतीकर, व्यापार कर और सड़क कर भी लिया जाता था। यह व्यवस्था शासकीय कार्यों, सेना, निर्माण कार्यों और जनसेवा में उपयोग की जाती थी।
प्रश्न-6.प्रचीन भारत में नगरीकरण के द्वितीय चरण के स्वरूप को विवेचना कीजिए
उत्तर:- प्राचीन भारत में नगरीकरण का द्वितीय चरण मौर्य काल (लगभग 4वीं शताब्दी ई.पू.) के बाद प्रारंभ होता है। यह काल शुंग, सातवाहन, कुषाण और गुप्त साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। इस काल में राजनैतिक स्थायित्व, कृषि का विस्तार, व्यापार का विकास और धातु मुद्रा का उपयोग बढ़ने से नगरीकरण को नई गति मिली।
इस चरण में प्रमुख नगरों जैसे पाटलिपुत्र, उज्जयिनी, काशी, वैशाली, तक्षशिला आदि का विकास हुआ। शिल्प और कुटीर उद्योगों का प्रसार, धार्मिक केंद्रों का नगरीकरण (जैसे नालंदा, सारनाथ), तथा व्यापारिक मार्गों के विकास से नगरों की संख्या एवं उनकी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ीं।
बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रचार से भी नगरों की महत्ता बढ़ी। नगर अब केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केंद्र भी बन गए थे। इस चरण में नगरों में सामाजिक विविधता, श्रेणी व्यवस्था, श्रमिक वर्ग और व्यापारिक संघों का विकास दिखाई देता है।
प्रश्न-7.प्राचीन भारत के प्रमुख उत्सवों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में उत्सव सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग थे। ये उत्सव ऋतु-परिवर्तन, कृषि कार्यों, धार्मिक अनुष्ठानों और देवी-देवताओं की पूजा से संबंधित होते थे। वसंतोत्सव (वसंत ऋतु का स्वागत), नवरात्र, दीपोत्सव (दीपावली), होलिका (होली) आदि प्रमुख उत्सव थे। दीपावली विशेषकर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और व्यापारिक लेखा-जोखा के आरंभ के लिए प्रसिद्ध थी। दशहरा असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक था। इसके अतिरिक्त कृषक समुदाय अन्न प्राप्ति हेतु इंद्र और वरुण देव की पूजा करते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा मनाते थे जबकि जैन समुदाय महावीर जयंती मनाता था। इन उत्सवों से सामाजिक एकता, आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बल मिलता था। यह उत्सव न केवल धार्मिक भावना बल्कि मनोरंजन और सामाजिक मेल-जोल के भी साधन थे।
प्रश्न-8.गुप्तकालीन भू-राजस्व व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- गुप्त काल (चौथी से छठी शताब्दी ई.) में भू-राजस्व व्यवस्था राज्य की आर्थिक रीढ़ थी। भूमि कर (भू-राजस्व) राज्य का प्रमुख आय स्रोत था। किसानों से उपज का एक भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिसे ‘उदक-भोग’, ‘कर’ या ‘भाग’ कहा जाता था। भूमि की उर्वरता, सिंचाई की सुविधा और उत्पादन क्षमता के अनुसार कर की दर निर्धारित होती थी। अधिकारी वर्ग जैसे ‘उग्र’, ‘विशयपति’, और ‘भूमिचर’ राजस्व संग्रह का कार्य करते थे। गुप्त शासकों ने धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि (अग्रहार) दान में देना शुरू किया, जिससे राजस्व संग्रहण में कमी आई। भूमि से संबंधित लेख (ताम्रपत्र) में कर की शर्तें, माप, ग्राम सीमाएँ आदि वर्णित होती थीं। इस व्यवस्था ने प्रशासनिक केंद्रीकरण, कृषि विस्तार और सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया।
प्रश्न-9. गुप्तकाल में मुद्रा प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
उत्तर:- गुप्तकाल (लगभग 320 से 550 ई.) में मुद्रा प्रणाली अत्यंत समृद्ध और संगठित थी। इस काल में स्वर्ण मुद्राओं का विशेष महत्व था, जिन्हें “दीनार” कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं।
इन मुद्राओं पर राजाओं की छवियाँ, धार्मिक प्रतीक, देवी-देवताओं की आकृतियाँ और संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। इनके माध्यम से न केवल आर्थिक लेन-देन होता था, बल्कि वे राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश भी देती थीं।
गुप्तकाल में चांदी और तांबे की मुद्राओं का भी प्रचलन था, विशेषतः स्थानीय व्यापार में। इन मुद्राओं की गुणवत्ता और शुद्धता उच्चस्तर की थी, जिससे व्यापार और कर संग्रहण में सुविधा हुई।
इस काल की मुद्राएँ भारतीय कला, धर्म और संस्कृति का सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। गुप्तकालीन मुद्रा प्रणाली ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संगठित एवं समृद्ध रूप प्रदान किया।
प्रश्न-10. प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था?
उत्तर:- प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। 28 जून 1914 को सर्बिया के एक राष्ट्रवादी गुट ‘ब्लैक हैंड’ के सदस्य गॅव्रिलो प्रिंसिप ने युवराज की हत्या कर दी। यह घटना बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हुई।
इस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आरोप लगाते हुए 23 जुलाई 1914 को एक कठोर अल्टीमेटम दिया। जब सर्बिया ने उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, तो 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी।
इसके बाद जर्मनी, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन एक-एक कर युद्ध में शामिल हो गए, जिससे यह क्षेत्रीय युद्ध विश्व युद्ध में बदल गया।
हालाँकि युद्ध के कई दीर्घकालिक कारण थे जैसे – साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, और गुटबंदी की नीति – परंतु फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या इस युद्ध का तात्कालिक कारण बना।
प्रश्न-11. फ्रांसीसी की क्रांति का तात्कालिक कारण बताइए।
उत्तर:- फ्रांसीसी क्रांति (1789) के तात्कालिक कारणों में सबसे प्रमुख था – आर्थिक संकट और खाद्य संकट। 1788-89 में फ्रांस में भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे अनाज की भारी कमी हो गई और कीमतें आसमान छूने लगीं। आम जनता को भोजन मिलना मुश्किल हो गया।
इसके साथ ही, राजा लुई 16वाँ ने अत्यधिक कर लगाए और दरबार के भव्य जीवन पर खर्च जारी रखा। राजकोष खाली हो चुका था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। इसी बीच, 1789 में जब राजा ने ‘एस्टेट्स जनरल’ की बैठक बुलाई, तो तृतीय वर्ग (जनसाधारण) को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इससे जनता में असंतोष और भड़क उठा।
7 जुलाई 1789 को पेरिस की जनता ने बास्तिल किले पर हमला किया, जो क्रांति की शुरुआत बन गई। इस प्रकार आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता और राजा की असंवेदनशीलता फ्रांसीसी क्रांति के तात्कालिक कारण बने।
प्रश्न-12. प्राचीन भारत में विभिन्न व्यापारिक समूहों के नाम व उनके कार्य बताइए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में व्यापारिक गतिविधियों को संगठित रूप में चलाने के लिए विभिन्न व्यापारिक समूहों की स्थापना हुई थी जिन्हें “श्रेणियाँ” कहा जाता था। कुछ प्रमुख व्यापारिक समूहों के नाम और कार्य निम्नलिखित हैं:
- श्रेष्ठी (Shreshthi) – ये धनाढ्य व्यापारी होते थे जो व्यापार का संचालन करते थे।
- सेठ – स्थानीय स्तर पर व्यापारिक वस्तुओं की खरीद-बिक्री में संलग्न रहते थे।
- गणिक/गणिकायन – यह व्यापारिक संघ होते थे जिनमें व्यापारी संगठित रूप में व्यापार करते थे।
- निगम (Nigama) – नगरों में स्थित व्यापारिक समूह जो शासकीय नियंत्रण में व्यापार करते थे।
- कारुक (Karuka) – ये शिल्पकारों और दस्तकारों के समूह थे जो उत्पादन में संलग्न रहते थे।
इन समूहों के कार्यों में व्यापारिक वस्तुओं का संग्रहण, विनिमय, मूल्य निर्धारण, कर भुगतान, व्यापार मार्गों की सुरक्षा, सामाजिक सेवा, धर्मार्थ कार्य आदि शामिल थे। इन श्रेणियों ने व्यापारिक जीवन को संगठित, न्यायिक और अनुशासित बनाया।
प्रश्न-13. प्राचीन भारत में विभिन्न व्यापारिक समूहों के नाम व उनके कार्य बताइए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में व्यापारियों के विभिन्न संगठन होते थे, जिन्हें “श्रेणियाँ” कहा जाता था। प्रमुख व्यापारिक समूहों में सेठी, श्रेणी, निगम, गणिक, और वणिक शामिल थे। इनका कार्य व्यापार को व्यवस्थित करना, मूल्य निर्धारण, वस्तु विनिमय और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करना था।
‘श्रेणियाँ’ कारीगरों और व्यापारियों का समूह होता था, जो सामूहिक रूप से कार्य करता था। ‘निगम’ एक उच्चतर संगठन था जो अंतर-नगर व्यापार में संलग्न होता था। ये समूह धर्मार्थ कार्यों, दान, मंदिरों के निर्माण आदि में भी योगदान देते थे। व्यापारी वर्ग समाज में प्रतिष्ठित था और कई व्यापारिक समूह राज्य से विशेष संरक्षण प्राप्त करते थे।
प्रश्न-14. वैदिक काल में तोल व माप प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:-वैदिक काल में तोल और माप की प्रणाली पूर्णतः व्यवस्थित नहीं थी, परंतु व्यापार, यज्ञ एवं सामाजिक कार्यों में माप-तौल का प्रयोग होता था। उस समय अनाज, धातु, भूमि, दूरी एवं समय की माप के लिए कुछ प्राचीन इकाइयाँ प्रचलित थीं। “अंगुल”, “हस्त”, “गव्यूति”, “योजन” आदि दूरी मापने की इकाइयाँ थीं। भार मापने के लिए “कर्ष”, “पाल”, “शतमान”, “निष्क” जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में इनका उल्लेख होता है। भूमि मापने के लिए “निवर्तन” का प्रयोग होता था। इस काल में मापन अधिकतर शारीरिक अंगों पर आधारित थे, जो सटीक नहीं होते थे। बाद में जब व्यापार में वृद्धि हुई, तब मापन प्रणाली अधिक व्यवस्थित होने लगी। वैदिक काल की माप प्रणाली प्राचीन भारतीय गणित और खगोल शास्त्र की नींव भी रखती है।
प्रश्न-15. प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली के उद्भव का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली का प्रारंभिक प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिलता है, जहाँ धातु की मुहरों का प्रयोग होता था। वैदिक काल में विनिमय प्रणाली (Barter System) प्रमुख थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में ‘पंचमार्क’ (आहत मुद्राएँ) का प्रचलन हुआ। मौर्य काल में राज्य नियंत्रित सिक्का प्रणाली विकसित हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में चाँदी, ताँबे और सोने के सिक्कों का चलन था। ‘कार्षापण’, ‘सुवर्ण’, ‘माषक’ आदि मुद्राएँ प्रमुख थीं। कुषाण और सातवाहन काल में स्वर्ण मुद्राएँ अत्यधिक मात्रा में ढाली गईं। गुप्त काल को स्वर्ण मुद्रा प्रणाली का स्वर्णकाल माना जाता है – सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के उच्च गुणवत्ता के थे। इन सिक्कों पर देवी-देवताओं, राजाओं और प्रतीकों की आकृतियाँ अंकित होती थीं। मुद्रा प्रणाली ने व्यापार, कर-संग्रह और राजनीतिक शक्ति को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाई।
प्रश्न-16. लियोनार्डो-दा-विंसी पर एक लेख लिखिए।/लियोनार्डो-दा-विंची पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
उत्तर:- लियोनार्डो दा विंची (Leonardo da Vinci) पुनर्जागरण काल का एक महान कलाकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, आविष्कारक और विचारक था। उसका जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची गाँव में हुआ था। उसे “पुनर्जागरण मानव” (Renaissance Man) कहा जाता है क्योंकि वह अनेक क्षेत्रों में निपुण था।
वह विश्वविख्यात चित्रकार था और उसकी कृतियाँ “मोनालिसा” और “द लास्ट सपर” आज भी कला की उत्कृष्टतम मिसालें मानी जाती हैं। विज्ञान के क्षेत्र में उसने शरीर रचना (anatomy), यांत्रिकी, विमान विज्ञान और भूगोल में अनेक प्रयोग और रेखाचित्र बनाए।
उसने मानव शरीर के भीतरी अंगों की बारीक चित्रकारी की और उड़ने वाली मशीनों के प्रारूप बनाए, जो आधुनिक विमानों की नींव बने।
लियोनार्डो का जीवन विज्ञान और कला के समन्वय का प्रतीक है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने युग से बहुत आगे की सोच रखी। उसका योगदान आज भी मानव सभ्यता के लिए प्रेरणास्रोत है।
प्रश्न-17. पुनर्जागरण में रूसी के योगदान पर संक्षिप्त लेख लिखिए।
उत्तर:- रूसे (Jean Jacques Rousseau) अठारहवीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी विचारक थे जिन्होंने समाज, राजनीति और शिक्षा पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। यद्यपि पुनर्जागरण काल का मुख्य दौर उनके पहले हो चुका था, परंतु उनके विचारों ने आधुनिक जागरण और फ्रांसीसी क्रांति में विशेष भूमिका निभाई।
उनकी प्रसिद्ध कृति “The Social Contract” (1762) में उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि “मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा है।” उन्होंने यह विचार रखा कि सरकार जनता की इच्छाओं से बननी चाहिए और शासक का अधिकार जनता से आता है।
रूसे का विचार था कि शिक्षा व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने प्राकृतिक जीवन और स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनके विचारों ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की नींव रखी।
इस प्रकार, रूसे के विचारों ने यूरोप में नए विचारों के आगमन और समाज में चेतना लाने का कार्य किया, जो पुनर्जागरण के मूल उद्देश्यों के अनुरूप था।
प्रश्न-18. प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के सामाजिक परिणाम अत्यंत गहरे और व्यापक थे। इस युद्ध ने यूरोपीय समाज की संरचना और जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया।
- जनसंख्या में भारी हानि:
युद्ध में करोड़ों सैनिक और नागरिक मारे गए, जिससे जनसंख्या में भारी गिरावट आई। कई परिवार उजड़ गए और महिलाओं को कामकाजी जीवन में प्रवेश करना पड़ा। - सामाजिक असंतुलन:
युद्ध के बाद समाज में असमानता और अस्थिरता बढ़ी। अमीर और गरीब के बीच अंतर गहरा हुआ और बेरोजगारी, भूख और महंगाई बढ़ी। - महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन:
महिलाओं ने युद्धकाल में कारखानों, दफ्तरों और अस्पतालों में कार्य किया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हुई और उन्हें मताधिकार मिला। - शरणार्थियों की समस्या:
युद्ध के दौरान लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए और शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ।
इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया और आधुनिक विश्व के सामाजिक ढांचे को नई दिशा दी।
प्रश्न-19. प्राचीन भारत में प्रमुख श्रेणियों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में श्रेणियाँ (Guilds) आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। ये स्वायत्त व्यापारिक व औद्योगिक संगठन होते थे जिनमें कारीगर, व्यापारी, और विभिन्न पेशेवर वर्ग शामिल होते थे। प्रमुख श्रेणियों में लोहारों (लोहकर्म श्रेणी), कुम्हारों (घटकर्म श्रेणी), बुनकरों (सूत्रकर्म), जौहरियों और तेलियों की श्रेणियाँ उल्लेखनीय थीं। ये श्रेणियाँ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती थीं, मूल्य निर्धारण करती थीं, श्रम विभाजन सुनिश्चित करती थीं, और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती थीं। श्रेणियों के अपने नियम-कानून, अध्यक्ष (श्रेष्ठी), और निधि होती थी। ये राजनीतिक दृष्टि से भी प्रभावशाली थीं और कभी-कभी दान, निर्माण कार्य (मंदिर, सराय) तथा व्यापार में राज्य की सहायता भी करती थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जातक कथाएँ और विभिन्न अभिलेखों में इनका वर्णन मिलता है।
प्रश्न-20. वाल्टेयर पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
उत्तर:- वाल्टेयर (Voltaire) अठारहवीं सदी का एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखक एवं प्रबोधनकाल (Enlightenment) का मुख्य विचारक था। उसका असली नाम फ्रांस्वा मैरी अरूए था। वह धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, और राजशाही के दमन के विरुद्ध लिखता था। वाल्टेयर ने स्वतंत्रता, तर्क और मानव अधिकारों की वकालत की। उसकी प्रसिद्ध रचना कैंडीड (Candide) में उसने अपने व्यंग्यात्मक शैली में तत्कालीन समाज की कुरीतियों का वर्णन किया।
वाल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता और विचारों की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया। वह चर्च की निरंकुशता और धार्मिक दमन का कटु आलोचक था। वह कहता था – “अगर कोई मूर्खता कहे तो भी उसे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए।” उसके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति के मूल विचारों – स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व – को जन्म दिया। वाल्टेयर का योगदान यूरोप में बौद्धिक जागृति लाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा।
प्रश्न-21. जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- जर्मनी में नाजीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण हुआ:
वर्साय की संधि (1919): इस अपमानजनक संधि से जर्मनी को भारी युद्ध क्षतिपूर्ति और क्षेत्रीय नुकसान झेलना पड़ा।
आर्थिक संकट: 1929 की विश्व आर्थिक मंदी ने बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ाया। लोग मजबूत नेतृत्व की तलाश में थे।
राजनीतिक अस्थिरता: वीमर गणराज्य कमजोर थी और बार-बार सरकारें बदल रही थीं।
प्रचार और नेतृत्व: हिटलर के शक्तिशाली भाषण, प्रचार, और ‘Mein Kampf’ जैसे ग्रंथों ने जनमानस को प्रभावित किया।
कम्युनिज्म का भय: जर्मन मध्यम वर्ग कम्युनिस्ट आंदोलन से डरा हुआ था और नाजियों को सुरक्षा का प्रतीक मानता था।
राष्ट्रवाद: हिटलर ने गर्व, सैन्यवाद और जर्मन श्रेष्ठता की भावना को उभारा।
इन कारणों से नाजी पार्टी को व्यापक समर्थन मिला और हिटलर सत्ता में आया।
प्रश्न-22. नेपोलियन के नागरिक प्रशासन की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- नेपोलियन बोनापार्ट (1769-1821) न केवल एक महान सैनिक नेता थे, बल्कि उन्होंने फ्रांस का एक सुव्यवस्थित नागरिक प्रशासन भी स्थापित किया। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ने फ्रांस में स्थायित्व और कानून का शासन सुनिश्चित किया।
उन्होंने “नेपोलियन संहिता (Napoleonic Code)” नामक एक नागरिक कानून संहिता बनाई, जिसमें समानता, संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं उत्तराधिकार से संबंधित स्पष्ट नियम थे। यह संहिता यूरोप के कई देशों के कानूनों का आधार बनी।
उन्होंने विभागीय प्रणाली लागू की और नौकरशाही को संगठित किया। अधिकारी मेरिट के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। उन्होंने कर प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाया तथा राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की।
शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थापना की और योग्य शिक्षकों की भर्ती की। उन्होंने धर्म और राज्य को अलग रखने का प्रयास किया।
नेपोलियन का प्रशासनिक ढांचा आज भी आधुनिक राष्ट्र-राज्य की नींव माना जाता है। उनकी नीतियाँ न्याय, समानता और कुशल शासन का प्रतीक हैं।
प्रश्न-23. पूर्वी समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- पूर्वी समस्या (Eastern Question) 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय राजनैतिक इतिहास की एक प्रमुख समस्या थी, जो मुख्यतः कमजोर हो रहे ओटोमन साम्राज्य की स्थिति और उसके क्षेत्रों के बंटवारे से जुड़ी थी। जैसे-जैसे ओटोमन साम्राज्य का पतन होने लगा, यूरोपीय शक्तियाँ (जैसे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और बाद में जर्मनी) अपने-अपने हितों के अनुसार बाल्कन और मध्य पूर्व के क्षेत्रों पर प्रभाव स्थापित करना चाहती थीं। यह प्रतिस्पर्धा संघर्षों और युद्धों का कारण बनी, जैसे क्रीमियन युद्ध (1853-56), रूस-तुर्की युद्ध, और अंततः प्रथम विश्व युद्ध। रूस ने स्लाव लोगों की रक्षा के नाम पर हस्तक्षेप किया, जबकि ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए ओटोमन साम्राज्य को बचाने की कोशिश की। इस तरह पूर्वी समस्या केवल एक भू-राजनैतिक प्रश्न नहीं, बल्कि यूरोपीय शक्तियों के टकराव और संतुलन का केंद्र भी बन गई थी।
प्रश्न-24. सातवाहन काल में दक्षिणी भारत की व्यापारिक गतिविधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- सातवाहन काल (1 शताब्दी ईसा पूर्व – 3 शताब्दी ई.) में दक्षिण भारत में व्यापारिक गतिविधियाँ अत्यंत विकसित थीं। यह काल अंतर्राज्यीय और विदेशी व्यापार के विकास के लिए प्रसिद्ध है। सातवाहनों ने तटीय क्षेत्रों जैसे कोंकण, आंध्र और तमिलनाडु में बंदरगाहों को प्रोत्साहित किया, जिससे रोमन साम्राज्य से व्यापार बढ़ा। मसाले, मोती, कपड़ा, हाथी दांत, रत्न और मसाले विदेशों में निर्यात किए जाते थे जबकि सोने-चांदी के सिक्के, शराब और बर्तन आयात होते थे। आंतरिक व्यापार के लिए सड़कों और मार्गों का विकास हुआ। व्यापारिक गिल्ड (श्रेणियाँ) और वणिक समुदाय व्यापार को नियंत्रित करते थे। सातवाहन राजाओं ने व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया और कुछ स्थानों पर कर छूट भी दी। समुद्री मार्गों से सिरेन्क, मिस्र और रोम तक व्यापार किया जाता था। यह काल दक्षिण भारत के व्यापारिक गौरव का प्रतीक है।
प्रश्न-25. प्राचीन भारत में व्यापारिक वस्तुओं की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में व्यापारिक वस्तुएँ कृषि, शिल्प, धातु, और वन उत्पादों से संबंधित थीं। प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं में कपास, रेशम, मसाले, गेंहू, चावल, मोती, हीरे, सोना, चांदी, मृदभांड, लोहे-तांबे के औजार, चंदन, कपूर, और हाथी-दांत शामिल थे। दक्षिण भारत से मसाले और मोती विदेशों को निर्यात किए जाते थे। उत्तर भारत से ऊन, कपड़ा और खाद्यान्न वस्तुएँ आती थीं। समुद्री मार्ग से पश्चिमी एशिया और रोमन साम्राज्य तक व्यापार होता था। सिल्क रूट और समुद्री मार्ग व्यापार के मुख्य साधन थे। व्यापारिक वस्तुओं की विविधता से भारत की आर्थिक समृद्धि स्पष्ट होती है।
प्रश्न-26. राष्ट्र संघ के उद्देश्यों पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- राष्ट्र संघ (League of Nations) की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साय संधि के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में युद्धों को रोकना और विश्व में शांति स्थापित करना था। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:
- अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना:
राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाकर युद्ध को रोकना था। - निरस्त्रीकरण:
संघ हथियारों की होड़ को रोकना चाहता था ताकि देशों के बीच तनाव न बढ़े। - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना:
संघ आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और मानवाधिकार के क्षेत्रों में देशों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहता था। - संधियों का सम्मान:
संघ चाहता था कि सभी देश अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों का पालन करें।
हालाँकि राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका, परंतु उसने भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी।
प्रश्न-27. साम्राज्यवाद के उदय के दो कारण बताइए।
उत्तर:- साम्राज्यवाद का अर्थ है किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे कमजोर देशों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करना। 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के उदय के प्रमुख दो कारण निम्नलिखित हैं:
- औद्योगिक क्रांति:
औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों को कच्चे माल और नए बाजारों की आवश्यकता हुई। एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में संसाधनों की प्रचुरता और सस्ता श्रम मिलने के कारण यूरोपीय देश वहां उपनिवेश स्थापित करने लगे। - राष्ट्रवाद और प्रतिस्पर्धा:
यूरोपीय देशों के बीच शक्ति की होड़ बढ़ गई थी। हर राष्ट्र अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहता था जिससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़े। इस प्रतिस्पर्धा ने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को तेज कर दिया।
इन दोनों कारणों ने विश्व में साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जिसके दूरगामी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम हुए।
प्रश्न-28. विश्व आर्थिक मंदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- 1929 में अमेरिका में शुरू हुई विश्व आर्थिक मंदी (Great Depression) एक वैश्विक आर्थिक संकट था, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया।
कारण:
अमेरिका के शेयर बाजार का पतन (Wall Street Crash)।
अति उत्पादन और मांग में गिरावट।
बैंकिंग प्रणाली की असफलता और ऋण चूक।
प्रभाव:
उद्योगों और व्यापार का पतन हुआ।
करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए।
किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई।
अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और भारत सहित विश्व के कई देश आर्थिक संकट में फँस गए।
राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, जिससे चरमपंथी विचारधाराओं को बल मिला जैसे जर्मनी में नाजीवाद।
इस आर्थिक मंदी ने विश्व इतिहास को नया मोड़ दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भूमि तैयार की।
प्रश्न-29. प्राचीन भारत में जैन स्रोतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:-प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में जैन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये ग्रंथ धार्मिक के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जानकारी भी प्रदान करते हैं। प्रमुख जैन स्रोतों में आचारांग सूत्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, और परिशिष्ट पर्वन उल्लेखनीय हैं। इन ग्रंथों में मौर्य वंश, नंद वंश और मगध की राजनीति का वर्णन है। जैन साहित्य व्यापारिक समाज, नगरीय जीवन, कर व्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी देता है। इनमें महावीर स्वामी की जीवनी के साथ उनके समय के समाज की झलक भी मिलती है। इन स्रोतों से प्राचीन भारत के इतिहास की पुनर्रचना में सहायता मिलती है।
प्रश्न-30. द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का परीक्षण कीजिए।
उत्तर:- द्वितीय विश्व युद्ध (1939–1945) के परिणाम अत्यंत व्यापक और निर्णायक रहे:
- मानव और आर्थिक हानि: इस युद्ध में लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए और कई देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए।
- जर्मनी और जापान की हार: जर्मनी को दो भागों में बाँटा गया और जापान पर परमाणु बम गिराए गए।
- संयुक्त राष्ट्र का गठन: 1945 में शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र (UNO) की स्थापना हुई।
- शीत युद्ध की शुरुआत: अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे, और वैचारिक संघर्ष शुरू हुआ।
- उपनिवेशवाद का अंत: भारत, इंडोनेशिया, अफ्रीका के देश स्वतंत्र होने लगे।
- यूरोप का पुनर्निर्माण: अमेरिका ने ‘मार्शल योजना’ के तहत यूरोप को आर्थिक सहायता दी।
इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में गहरे परिवर्तन लाए।
प्रश्न-31. प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार के विकास की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। वहाँ से मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तान से व्यापार होता था। वैदिक काल में विदेशी व्यापार सीमित था लेकिन मौर्य काल में इसका विकास तीव्र गति से हुआ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विदेशी व्यापारियों के लिए विशेष नियम बताए गए हैं। गुप्त और सातवाहन काल में विदेशी व्यापार अपने चरम पर था। भारत से मसाले, वस्त्र, रत्न, हाथी दांत, चंदन और इत्र विदेशों को निर्यात किए जाते थे। बदले में रोम, यूनान और चीन से सिक्के, शराब, रेशमी वस्त्र और कांच के बर्तन आते थे। बंदरगाह जैसे भरूच, ताम्रलिप्ति, अरिकमेडु, और मसुलीपट्टनम विदेशी व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। रेशम मार्ग (Silk Route) के माध्यम से भी चीन से व्यापार होता था। इस व्यापार ने भारत की आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा दिया।
प्रश्न-32. यूरोपीय साम्राज्यवाद के बारे में आप क्या जानते हो ?
उत्तर:- यूरोपीय साम्राज्यवाद वह प्रक्रिया थी जिसमें यूरोपीय राष्ट्रों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देशों पर राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित किया। यह प्रक्रिया 15वीं शताब्दी के समुद्री अन्वेषण से शुरू होकर 19वीं और 20वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुँची।
ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी और बेल्जियम जैसे राष्ट्रों ने उपनिवेशों की स्थापना की। इनका उद्देश्य था कच्चे माल की प्राप्ति, नए बाजारों की खोज और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण। भारत, चीन, अफ्रीका और अमेरिका इस साम्राज्यवाद के मुख्य शिकार बने।
साम्राज्यवाद के कारण उपनिवेशों में शोषण, संसाधनों की लूट, संस्कृति का विनाश और सामाजिक असमानता बढ़ी। वहीं दूसरी ओर, यूरोप में औद्योगीकरण और व्यापार का विकास हुआ।
यूरोपीय साम्राज्यवाद ने दुनिया को वैश्विक रूप में जोड़ा, परंतु यह प्रक्रिया शोषण और उत्पीड़न पर आधारित थी।
प्रश्न-33. जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख हैं:
- वर्साय संधि (1919): इस संधि ने जर्मनी को कठोर दंड दिए, जैसे – क्षेत्रीय हानि, युद्ध क्षतिपूर्ति और सेना की सीमाएँ। इससे जर्मन जनता में अपमान और असंतोष फैल गया।
- आर्थिक संकट: प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ गई। 1929 की महामंदी ने हालात और खराब कर दिए।
- राजनैतिक अस्थिरता: वीमार गणराज्य कमजोर था और लगातार सरकारें गिरती थीं। इससे जनता तानाशाही की ओर आकर्षित हुई।
- हिटलर का प्रचार: एडॉल्फ हिटलर और उसकी पार्टी (नाज़ी पार्टी) ने देशभक्ति, आर्य जाति की श्रेष्ठता और यहूदियों के खिलाफ प्रचार करके जनता को प्रभावित किया।
- प्रचार तकनीक: हिटलर ने रेडियो, पोस्टर और भाषणों के ज़रिए नाज़ी विचारधारा को फैलाया।
इन कारणों से जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय हुआ, जिसने आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया।
प्रश्न-34. इटली के एकीकरण में मेज़िनी के योगदान पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- जोसेपे मेज़िनी (1805-1872) इटली के एक महान राष्ट्रवादी, विचारक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने इटली के एकीकरण में वैचारिक और आंदोलनात्मक दोनों स्तरों पर अहम भूमिका निभाई।
मेज़िनी ने युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए “यंग इटली (Young Italy)” नामक संगठन की स्थापना की। इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, एकीकृत और गणराज्यात्मक इटली की स्थापना करना था।
उन्होंने इटलीवासियों को यह विचार दिया कि वे एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हो सकते हैं और विदेशी शासन से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने इटली के विभिन्न राज्यों और लोगों के बीच एकता का भाव पैदा किया।
यद्यपि मेज़िनी के प्रयासों को तत्कालिक सफलता नहीं मिली, फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की नींव रखी। उनके विचारों और प्रयासों से प्रेरणा लेकर बाद में गारिबाल्डी और कैवूर जैसे नेताओं ने इटली का एकीकरण पूर्ण किया।
इस प्रकार, मेज़िनी को इटली के एकीकरण का “वैचारिक अग्रदूत” कहा जाता है।
प्रश्न-35. इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत के कारणों को विवेचना कीजिए।
उत्तर:- इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति (लगभग 1750–1850) कई कारणों से आरंभ हुई:
प्राकृतिक संसाधन: इंग्लैंड में कोयला और लोहे के विशाल भंडार थे, जो उद्योगों के लिए आवश्यक थे।
वैज्ञानिक खोजें: नए आविष्कार जैसे जेम्स वाट का स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी, और पावर लूम ने उत्पादन की गति को तेज किया।
पूंजी निवेश: उपनिवेशों और व्यापार से अर्जित धन को उद्योगों में निवेश किया गया।
राजनीतिक स्थिरता: इंग्लैंड की सरकार व्यापार और उद्योग के पक्ष में थी।
उपनिवेशों का बाज़ार: इंग्लैंड को अपने उत्पादों के लिए बड़े उपनिवेशीय बाज़ार मिल गए।
कृषि सुधार: कृषि क्षेत्र में सुधारों से खाद्य उत्पादन बढ़ा, जिससे अधिक लोग शहरों की ओर गए और श्रमिक वर्ग तैयार हुआ।
इन सभी कारकों ने मिलकर इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति का जन्मस्थल बनाया।
प्रश्न-36. गुप्तोत्तर काल में व्यापार के विकास का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- गुप्तोत्तर काल (6वीं से 12वीं शताब्दी) में भारत के व्यापार में अनेक परिवर्तन आए। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता तो थी, लेकिन क्षेत्रीय शक्तियों के उत्थान के कारण व्यापारिक गतिविधियाँ पुनः सशक्त हुईं।
भूमध्यसागर से चीन तक के सिल्क रूट पर भारत एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बना। अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तटों पर व्यापार करने लगे। इस काल में कांचीपुरम, बनारस, मदुरै, पाटलिपुत्र जैसे नगर व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे।
तांबे, चांदी, वस्त्र, हाथी दांत, मसाले, गंधद्रव्य आदि का व्यापार बढ़ा। समुद्री मार्गों के साथ-साथ स्थल मार्गों का भी प्रयोग होता रहा। श्रेणियों और निगमों की सहायता से व्यापार नियंत्रित होता था। व्यापारी अब धर्मस्थलों और शिक्षा संस्थानों को भी दान देने लगे।
हालाँकि इस काल में विदेशी आक्रमणों और राजनीतिक विखंडन का प्रभाव व्यापार पर पड़ा, फिर भी व्यापारिक संगठन, बाजार व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली ने व्यापार को सशक्त बनाए रखा।
प्रश्न-37. सितम्बर 1938 के म्यूनिख समझौते पर एक टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:-म्यूनिख समझौता सितम्बर 1938 में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के बीच हुआ था। यह समझौता जर्मन तानाशाह हिटलर की माँग पर किया गया, जिसके तहत उसे चेकोस्लोवाकिया के सूडेटेनलैंड क्षेत्र पर अधिकार दे दिया गया।
इस समझौते में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलिन और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री डलाडियर ने “शांति बनाए रखने” के लिए हिटलर की माँग को मान लिया। परंतु चेकोस्लोवाकिया को इस वार्ता में शामिल नहीं किया गया।
म्यूनिख समझौता अपीज़मेंट (तुष्टिकरण) नीति का प्रतीक माना गया, जिसमें आक्रामक तानाशाहों को रोकने की बजाय उन्हें रियायतें दी गईं। हिटलर ने बाद में इस समझौते का उल्लंघन कर पूरा चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया।
यह समझौता द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण पूर्वापाय था और इससे यह सिद्ध हुआ कि तानाशाहों से शांति की अपेक्षा करना भ्रम है।
प्रश्न-38. अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों को विवेचना कीजिए।
उत्तर:- अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम (1775–1783) के कई प्रमुख कारण थे।
राजनैतिक स्वतंत्रता की भावना: उपनिवेश अब स्वतंत्र शासन की भावना रखने लगे थे और इंग्लैंड की निरंकुशता से मुक्ति चाहते थे।
इन सभी कारणों ने मिलकर अमेरिकी क्रांति की भूमि तैयार की।
कर नीति: इंग्लैंड ने उपनिवेशों पर ‘स्टैम्प एक्ट’, ‘शुगर एक्ट’, और ‘टी एक्ट’ जैसे कर लगाए, जिससे उपनिवेशवासियों में असंतोष उत्पन्न हुआ।
प्रतिनिधित्व का अभाव: उपनिवेशवासी “No taxation without representation” के सिद्धांत को मानते थे, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था।
बोस्टन टी पार्टी (1773): जब उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश चाय कर का विरोध करते हुए चाय की खेप समुद्र में फेंक दी, तो ब्रिटिश सरकार ने कठोर दंडात्मक कदम उठाए, जिससे संघर्ष बढ़ गया।
प्राकृतिक अधिकारों की चेतना: जॉन लॉक जैसे विचारकों के विचारों ने स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों के प्रति जनमानस को जागरूक किया।
प्रश्न-39. वाकाटक काल में व्यापार के विकास का वर्णन कीजिए
उत्तर:- वाकाटक वंश (तीसरी-चौथी शताब्दी ई.) के शासनकाल में व्यापार का अच्छा विकास हुआ। इस काल में आंतरिक व्यापार के साथ-साथ विदेशी व्यापार का भी विस्तार हुआ। वाकाटक शासकों ने व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाया और व्यापारियों को संरक्षण दिया। इस काल में कपड़ा, धातु, मिट्टी के बर्तन, गंधद्रव्य, और बहुमूल्य रत्नों का व्यापार होता था। दक्षिण भारत से रत्न, मोती और मसाले उत्तर भारत व विदेशों तक जाते थे। अजन्ता की गुफाएँ, जो इस काल की हैं, व्यापारिक समृद्धि की साक्षी हैं। व्यापारिक नगरों की वृद्धि, श्रेणियों की सक्रियता और मंदिरों को दिए गए दानों से आर्थिक विकास का पता चलता है।
प्रश्न-40. प्राचीन भारत में व्यापार के प्रमुख पतन के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में व्यापार का पतन कई कारणों से हुआ। सबसे पहला कारण विदेशी आक्रमण थे – शक, कुषाण और अंततः हूणों के आक्रमण से व्यापारिक मार्ग बाधित हुए। दूसरा प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता था, जिससे स्थायी शासकीय समर्थन नहीं मिल सका। गुप्तकाल के पश्चात बड़े साम्राज्य विघटित हो गए और छोटे-छोटे राज्यों में विभाजन से व्यापारिक व्यवस्था प्रभावित हुई। तीसरा कारण समुद्री मार्गों का ग्रीक और रोमन नियंत्रण में जाना था जिससे भारत का समुद्री व्यापार घटा। चौथा कारण बुनियादी संरचना का अभाव और व्यापारिक गिल्डों की कमजोर होती स्थिति थी। पाँचवाँ कारण यह था कि धार्मिक दृष्टिकोण में भी व्यापार को द्वितीय श्रेणी का कार्य समझा जाने लगा। अंततः आंतरिक मार्गों के अवरुद्ध होने और बंदरगाहों के महत्व घटने से भी व्यापार को हानि पहुँची।
प्रश्न-41. पुनर्जागरण के समय साहित्य की प्रगति का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- पुनर्जागरण काल (14वीं से 17वीं सदी) में साहित्य ने नई ऊँचाइयों को छुआ। यह काल तर्क, मानवतावाद और ज्ञान की पुनर्स्थापना का समय था।
- मानवतावाद का प्रभाव: इस युग में साहित्य मानव के अनुभव, स्वतंत्रता, और विवेक पर केंद्रित हुआ। लेखकों ने धर्म के बजाय मनुष्य को साहित्य का केंद्र बनाया।
- प्रमुख लेखक:
दांते (Dante): “डिवाइन कॉमेडी” जैसे ग्रंथ ने धर्म और दर्शन को कविता में प्रस्तुत किया।
पेत्रार्क: इटली के इस कवि ने प्रेम और मानव संवेदना पर आधारित काव्य रचना की।
बोक्काचियो: “डेकामेरोन” जैसी कहानियाँ सामाजिक यथार्थ का चित्रण करती हैं।
शेक्सपियर (Shakespeare): अंग्रेज़ी साहित्य में नाटक और कविता की ऊँचाइयों को छुआ। उनके नाटक जैसे “हैमलेट”, “मैकबेथ”, और “रोमियो एंड जूलियट” आज भी प्रासंगिक हैं।
इस प्रकार पुनर्जागरण काल में साहित्य ने धार्मिक जड़ता को तोड़कर नई सोच, स्वतंत्रता और मानव अनुभवों को अपनाया।
प्रश्न-42. स्पेन के गृह युद्ध के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- स्पेन का गृह युद्ध (1936–1939) कई सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कारणों का परिणाम था:
विदेशी हस्तक्षेप: जर्मनी और इटली ने फ्रांको का समर्थन किया, जबकि रूस और अन्य वामपंथी देशों ने रिपब्लिकन सरकार का समर्थन किया।
यह युद्ध फासीवाद और लोकतंत्र के बीच वैचारिक संघर्ष भी था।
राजनैतिक अस्थिरता: राजशाही, तानाशाही और लोकतंत्र के बीच सत्ता संघर्ष ने देश को अस्थिर किया।
वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ: समाजवादी, कम्युनिस्ट और अराजकतावादी दलों की सरकार से रुढ़िवादी शक्तियाँ असंतुष्ट थीं।
भूमि सुधार: सरकार द्वारा ज़मींदारों की भूमि जब्त कर किसानों को देने की नीति से अमीर वर्ग नाराज़ हुआ।
धार्मिक संघर्ष: चर्च की शक्तियों को सीमित करने की कोशिशों से धार्मिक संगठन भड़क उठे।
सेना की भूमिका: फ्रांसिस्को फ्रांको के नेतृत्व में सेना ने विद्रोह कर दिया और गृह युद्ध शुरू हो गया।
Section-C
प्रश्न-1.प्राचीन भारत में प्रमुख मेलों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में मेले सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। ये मेले केवल धार्मिक उद्देश्य के लिए ही नहीं होते थे, बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के भी केंद्र होते थे।
- प्रयाग (इलाहाबाद) का मेला:
प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगने वाला माघ मेला अत्यंत प्रसिद्ध था। यह धार्मिक आस्था के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र था। अनेक व्यापारी वर्ग इस अवसर पर एकत्र होते थे। - पुष्कर मेला:
राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर का मेला धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता था और यहाँ पशु व्यापार भी होता था, विशेष रूप से ऊँटों और घोड़ों का। - वैशाली मेला:
लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में भी बड़े मेले लगते थे। ये बौद्ध और जैन धर्म के प्रचार और व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे। - काशी मेला:
काशी (वाराणसी) में नियमित रूप से धार्मिक उत्सवों के अवसर पर मेले लगते थे। यह शहर व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ के मेलों में शिल्पकार, व्यापारी, साधु और तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आते थे। - कुंभ मेला:
प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में लगने वाला कुंभ मेला भी प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था। यह 12 वर्षों में एक बार लगता था और इसमें विशाल जनसमूह एकत्र होता था। यह मेला व्यापारिक आदान-प्रदान का भी अवसर होता था। - अन्य क्षेत्रीय मेले:
दक्षिण भारत में मदुरै, कांची और पुहार जैसे नगरों में भी मंदिरों के उत्सवों के साथ मेले आयोजित होते थे, जो धार्मिक आस्था और व्यापारिक गतिविधियों के मिलन बिंदु होते थे।
प्राचीन भारत में मेलों की परंपरा ने धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को एकसूत्र में पिरोया। ये मेले जनसंपर्क, व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामुदायिक भावना को सुदृढ़ करते थे। मेलों के माध्यम से नगरों और ग्रामों के बीच संबंध भी स्थापित होते थे।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.औद्योगिक क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- औद्योगिक क्रांति अठारहवीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड से शुरू होकर पूरे यूरोप और बाद में विश्व के अन्य भागों में फैल गई। यह क्रांति एक सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया थी, जिसने उत्पादन के परंपरागत तरीकों को बदलकर मशीन आधारित उत्पादन को जन्म दिया। इसके कई कारण थे:
- वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी प्रगति: औद्योगिक क्रांति के पीछे प्रमुख कारण तकनीकी आविष्कार थे। जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन का आविष्कार, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, और फ्लाइंग शटल जैसी मशीनों का विकास उत्पादन प्रक्रिया को तीव्र करने में सहायक रहा।
- कृषि क्रांति: इससे पहले हुई कृषि क्रांति ने अनाज उत्पादन में वृद्धि की और श्रमिकों को अतिरिक्त रोजगार की आवश्यकता से मुक्त किया, जिससे वे औद्योगिक क्षेत्रों की ओर गए।
- ब्रिटेन की उपनिवेश नीति: ब्रिटेन की उपनिवेशिक नीतियों ने उसे कच्चा माल और तैयार माल के लिए बड़ा बाजार प्रदान किया। भारत, अमेरिका, और अफ्रीकी देशों से कपास, कोयला और अन्य संसाधन प्राप्त हुए।
- वाणिज्यिक पूंजीवाद का विकास: व्यापारिक वर्ग के पास पूंजी का भंडार था, जिसे उन्होंने औद्योगिक निवेश में लगाया। इससे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों और उद्योगों की स्थापना संभव हो सकी।
- संचार और परिवहन का विकास: सड़कों, नहरों, और रेलवे का विकास औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में सहायक रहा। इससे कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल की बिक्री सरल हो गई।
- राजनीतिक स्थिरता और कानूनी संरचना: इंग्लैंड में एक स्थिर लोकतांत्रिक शासन और निजी संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा से उद्योगपतियों को अनुकूल वातावरण मिला।
- उद्योगों के लिए श्रम की उपलब्धता: ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के कारण उद्योगों को सस्ते श्रमिक मिल गए।
औद्योगिक क्रांति अनेक कारकों का परिणाम थी—जिसमें वैज्ञानिक सोच, आर्थिक अवसर, सामाजिक बदलाव और तकनीकी नवाचार ने मिलकर एक वैश्विक परिवर्तन को जन्म दिया। इसका प्रभाव विश्व के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर गहरा पड़ा।
प्रश्न-3. प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली के उद्भव व विकास का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग मुद्रा प्रणाली रही है। मुद्रा का प्रयोग विनिमय प्रणाली की जटिलताओं को दूर करने के लिए किया गया। इसका विकास विभिन्न कालों में हुआ, जिसमें प्रारंभिक काल से लेकर गुप्त काल तक अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
ऋग्वैदिक काल में मुद्रा का प्रयोग नहीं था, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। गाय, अनाज, वस्त्र आदि को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन समय के साथ जनसंख्या और व्यापार के बढ़ने से मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई।
महाजनपद काल (छठी शताब्दी ई.पू.) में आहत मुद्राओं (Punch-marked coins) का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ये चांदी की छोटी-छोटी चपटी मुद्राएँ होती थीं जिन पर विभिन्न चिन्हों की छपाई होती थी। ये मुद्राएँ मगध, कौशांबी, अवंती आदि राज्यों में प्रचलित थीं।
मौर्य काल में मुद्रा प्रणाली और विकसित हुई। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त पंचचिह्नित मुद्राओं का उपयोग हुआ। कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ में मुद्रा निर्माण, धातु की शुद्धता और निरीक्षण की व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है।
शुंग, सातवाहन और कुषाण काल में स्वर्ण और चांदी की मुद्राएँ जारी की गईं। कुषाण शासक कनिष्क ने यूनानी शैली की मुद्राओं को अपनाया, जिसमें राजा की आकृति और देवी-देवताओं के चित्र अंकित होते थे। इससे भारतीय मुद्रा प्रणाली में सौंदर्यबोध और कलात्मकता का समावेश हुआ।
गुप्त काल में मुद्रा प्रणाली अपने उत्कर्ष पर पहुँची। इस काल में मुख्यतः स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ, जिन्हें ‘दीनार’ कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की मुद्राएँ अत्यंत सुंदर और कलात्मक थीं। इन पर राजा की आकृति, सैन्य क्रियाएँ, धार्मिक प्रतीक आदि अंकित होते थे।
इस प्रकार, प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली का विकास क्रमिक रूप से हुआ – वस्तु विनिमय से आहत मुद्राओं तक, और वहाँ से स्वर्ण, चांदी व तांबे की मुद्राओं तक। यह विकास भारत की बढ़ती हुई व्यापारिक, शिल्पिक और राजनीतिक समृद्धि को दर्शाता है।
प्रश्न-4. प्राचीन भारत में कर नीति पर एक निबंध लिखिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में कर नीति (Taxation Policy) राज्य की आय का प्रमुख स्रोत थी। कर प्रणाली का स्वरूप समय-समय पर भिन्न रहा, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य राजकोष को समृद्ध बनाना तथा सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करना था।
वैदिक काल में कर प्रणाली सीमित थी। राजा को ‘बलि’, ‘शुल्क’, और ‘कर’ जैसे अंशदान प्राप्त होते थे। ‘बलि’ स्वेच्छा से दिया गया कर था। उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हुआ और भूमि कर प्रमुख कर बन गया। महाजनपद काल तक आते-आते कर प्रणाली संगठित रूप लेने लगी।
मौर्य काल में कर नीति अत्यंत विकसित थी। कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ में विभिन्न प्रकार के करों का वर्णन मिलता है। इस काल में भूमि कर (भोग), व्यापारिक कर, पेय, खनिज, वनों, पशुपालन और श्रम आदि पर कर लगाए जाते थे। भूमि कर को ‘भाग’ कहा जाता था, जो उत्पादन का छठा, चौथा या आठवाँ भाग होता था।
व्यापार और शिल्प पर भी कर लगाए जाते थे। व्यापारिक वस्तुओं पर चुंगी (customs duty) ली जाती थी। “शुल्काध्यक्ष” नामक अधिकारी व्यापारिक कर एकत्र करता था। सिंचाई के लिए जल कर, पशुओं पर ‘पशु कर’, और घरेलू उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं पर ‘उत्पादन कर’ लगाया जाता था।
गुप्त काल में भी कर नीति सुव्यवस्थित थी। हालांकि करों की संख्या मौर्य काल से कम थी, लेकिन उनकी वसूली नियमित थी। भूमि कर प्रमुख बना रहा। गुप्त शिलालेखों में ‘उदयंग’, ‘हिरण्य’, ‘भोग’, ‘कर’, ‘शुल्क’ जैसे करों का उल्लेख मिलता है। इस काल में धार्मिक संस्थाओं को कर मुक्त भूमि देने की परंपरा भी प्रचलित हुई।
धार्मिक ग्रंथों जैसे मनुस्मृति में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कर वसूली न्यायसंगत होनी चाहिए। राजा को अपने प्रजा के कल्याण के लिए ही कर लेना चाहिए। कर अत्यधिक नहीं होना चाहिए और समय पर वसूला जाना चाहिए।
प्राचीन भारत की कर नीति का उद्देश्य केवल राजकोष की वृद्धि नहीं था, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखना, राज्य के कार्यों को संचालित करना और प्रजा की रक्षा करना भी था। यह नीति नैतिकता, धर्म और आर्थिक संतुलन पर आधारित थी।
प्रश्न-5. प्राचीन काल में दक्षिण भारत में व्यापार के विकास पर एक निबंध लिखिए।
उत्तर:- प्राचीन काल में दक्षिण भारत व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध रहा। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, समुद्र तटों और व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल बंदरगाहों के कारण व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बन गया था।
दक्षिण भारत में संगम युग (लगभग 300 ई.पू. – 300 ई.) के दौरान व्यापार की उल्लेखनीय प्रगति हुई। चोल, पांड्य और चेर राजवंशों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़कों, बंदरगाहों और व्यापारिक मंडियों का विकास किया। इस काल में करिकाल चोल जैसे शासकों ने समुद्री व्यापार को संगठित किया।
दक्षिण भारत की प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं में मसाले (काली मिर्च, इलायची), मोती, हाथीदांत, रत्न, कपास, रेशम और सुगंधित लकड़ियाँ शामिल थीं। ये वस्तुएँ रोम, अरब, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया तक निर्यात की जाती थीं। समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटीय बंदरगाह जैसे पुहार, मस्की, अरिकमेडु, ताम्रलिप्ति, नागपट्टिनम, तथा बारकूर प्रसिद्ध थे।
अरिकमेडु बंदरगाह विशेष रूप से रोमन व्यापारियों के साथ संपर्क का केन्द्र था। यहाँ से रोमन साम्राज्य में भारतीय वस्तुएँ भेजी जाती थीं और बदले में सोना, चाँदी, शराब व अन्य वस्तुएँ आती थीं।
चोल काल (9वीं – 12वीं सदी) में दक्षिण भारत का व्यापार अत्यधिक उन्नत हो गया। इस काल में दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों – इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड व कम्बोडिया से व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। चोलों की नौसेना शक्तिशाली थी, जिससे समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित होती थी।
भीतर के व्यापार में भी दक्षिण भारत अग्रणी था। नगरों, बाजारों और मेलों के माध्यम से आंतरिक व्यापार होता था। व्यापारी संघ (गिल्ड्स) जैसे ‘मणिग्रामम’, ‘नानादेसियों’ ने व्यापार को संगठित रूप दिया।
इस प्रकार, प्राचीन काल में दक्षिण भारत का व्यापार न केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, बल्कि यह सांस्कृतिक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का माध्यम भी बना। इससे न केवल भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई, बल्कि भारत की संस्कृति का प्रसार भी हुआ।
प्रश्न-6. द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें लगभग सात करोड़ लोग मारे गए। यह युद्ध यूरोप, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत महासागर में लड़ा गया। इसके परिणाम अनेक और दूरगामी थे:
- मानव और भौतिक क्षति: युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, शहर नष्ट हुए, और औद्योगिक ढांचा बर्बाद हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों ने भयावह विनाश मचाया।
- नाज़ीवाद का अंत: जर्मनी में हिटलर की पराजय और नाजी शासन का अंत हुआ। नूरेमबर्ग में युद्ध अपराधियों पर मुकदमे चलाए गए।
- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना: शांति बनाए रखने हेतु 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना हुई।
- द्विध्रुवीय विश्व का निर्माण: अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे और शीत युद्ध की शुरुआत हुई।
- यूरोप का पुनर्निर्माण: अमेरिका ने “मार्शल योजना” के माध्यम से यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता की।
- औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत: युद्ध के बाद उपनिवेशों में स्वतंत्रता की मांग तेज हुई। भारत, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की।
- इजराइल का निर्माण: यहूदियों को अपनी मातृभूमि देने के लिए 1948 में इजराइल की स्थापना हुई।
- जापान और जर्मनी का पुनर्गठन: इन देशों में लोकतांत्रिक शासन स्थापित किए गए और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई।
द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व राजनीति, समाज, और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। इसने एक नई विश्व व्यवस्था की नींव डाली, जिसमें शांति, सहयोग और मानव अधिकारों को केंद्र में रखा गया।
प्रश्न-7. धर्म सुधार आन्दोलन के धार्मिक कारणों को विवेचना कीजिए।
उत्तर:-धर्म सुधार आन्दोलन (Reformation) 16वीं शताब्दी का एक प्रमुख धार्मिक आन्दोलन था, जिसने ईसाई धर्म की परंपरागत व्यवस्था को चुनौती दी और आधुनिक ईसाई संप्रदायों की नींव रखी। इस आन्दोलन के अनेक धार्मिक कारण थे जो इस प्रकार हैं –
- रोमन चर्च की भ्रांतियाँ:
कैथोलिक चर्च के पादरी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। चर्च की गतिविधियाँ धर्म के बजाय धन के इर्द-गिर्द घूमने लगी थीं। ‘इंडलजेंस’ (पापों से मुक्ति पत्र) की बिक्री ने आम जनता की आस्था को चोट पहुँचाई। - बाइबिल की व्याख्या पर एकाधिकार:
चर्च के अधिकारी ही बाइबिल की व्याख्या करते थे और आम जनता को उसकी स्वतंत्र व्याख्या की अनुमति नहीं थी। यह धार्मिक अधिनायकवाद लोगों को असंतुष्ट कर रहा था। - धार्मिक अनुष्ठानों की जटिलता:
धार्मिक कृत्य जैसे पूजा-पाठ, संस्कार आदि अत्यधिक जटिल हो चुके थे। इन सबका सामान्य जीवन से कोई व्यावहारिक संबंध नहीं रह गया था। - चर्च के नेतृत्व की नैतिक गिरावट:
पोप और अन्य उच्चाधिकारी विलासिता एवं राजनीतिक षड्यंत्रों में संलग्न थे। इससे लोगों का विश्वास चर्च से उठने लगा। - व्यक्तिगत आध्यात्मिकता पर बल:
मास्टर मार्टिन लूथर और अन्य विचारकों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। इसने धार्मिक स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। - धार्मिक ग्रंथों की स्थानीय भाषाओं में उपलब्धता:
प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद बाइबिल का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ, जिससे आम जनता को धार्मिक ज्ञान हुआ और चर्च की एकाधिकारिता टूटी। - पवित्रता के स्थान पर धन की प्रधानता:
चर्च ने धार्मिक अनुष्ठानों और तीर्थों को भी आय का साधन बना लिया था। इससे धर्म की पवित्रता पर प्रश्न उठने लगे।
धार्मिक सुधार आन्दोलन के धार्मिक कारण मुख्यतः चर्च की नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक गिरावट से जुड़े हुए थे। यह आन्दोलन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ।
प्रश्न-8. गुप्तों के आर्थिक जीवन पर एक निबंध लिखिए।
उत्तर:- गुप्त काल (चौथी से छठी शताब्दी ई.) को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में न केवल कला, साहित्य, धर्म और विज्ञान का उत्कर्ष हुआ, बल्कि आर्थिक जीवन में भी अभूतपूर्व प्रगति देखी गई। यह काल भारत के आर्थिक सुदृढ़ता और व्यापारिक समृद्धि का प्रतीक रहा है।
गुप्तकालीन कृषि व्यवस्था अत्यंत समृद्ध थी। भूमि करों का उल्लेख विभिन्न अभिलेखों में मिलता है। कृषकों को भूमि के बदले में राजा को उपज का भाग देना होता था। सिंचाई के साधनों का विकास हुआ और नहरों, कुओं तथा तालाबों का निर्माण हुआ। इससे उत्पादन में वृद्धि हुई और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई।
उद्योग और शिल्प में भी पर्याप्त विकास हुआ। कांच, मिट्टी, धातु, हाथीदांत, वस्त्र, आभूषण आदि के निर्माण में भारत अग्रणी था। इस काल में वस्त्र उद्योग विशेष रूप से विख्यात था, विशेषकर कौशांबी और वाराणसी के रेशमी वस्त्रों की विदेशों में भी माँग थी। धातु विज्ञान भी विकसित था, जिसका प्रमाण है दिल्ली का लौह स्तंभ।
गुप्तकाल में व्यापार और वाणिज्य भी अत्यधिक उन्नत था। स्थलीय और समुद्री व्यापार दोनों ही प्रचलित थे। आंतरिक व्यापार नगरों, मंडियों और बाजारों में होता था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार रोम, चीन, श्रीलंका, दक्षिण-पूर्व एशिया और अरब देशों तक फैला हुआ था। व्यापार में सहूलियत के लिए सड़कें, पुल और विश्राम गृह बनाए गए थे।
मुद्रा प्रणाली गुप्त काल की एक विशेषता थी। इस काल में स्वर्ण मुद्रा ‘दीनार’ तथा चांदी और तांबे की मुद्राएँ प्रचलन में थीं। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएँ उनकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाती हैं। ये मुद्राएँ सुन्दर कलाकृति और शुद्ध धातु की बनी होती थीं।
गुप्तों के समय सामाजिक वर्गों में व्यापारियों और शिल्पियों की स्थिति भी मजबूत थी। शहरीकरण बढ़ा और अनेक नगर व्यापारिक केन्द्रों में बदल गए। पाटलिपुत्र, उज्जयिनी, प्रयाग, वैशाली आदि नगर प्रमुख आर्थिक केन्द्र बन गए।
इस प्रकार, गुप्तकाल का आर्थिक जीवन कृषि, उद्योग, व्यापार और मुद्रा व्यवस्था के सुदृढ़ विकास पर आधारित था। यह युग भारतीय अर्थव्यवस्था के चरम उत्कर्ष का प्रतीक है, जिसने भारत को एक समृद्ध और सुसंगठित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।
प्रश्न-9. बिस्मार्क की ‘रक्त व लौह’ नीति को समझाइए।
उत्तर:- बिस्मार्क, प्रशिया (जर्मनी) के एक महान राजनीतिज्ञ और राजनयिक थे, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी “रक्त और लौह” नीति (Blood and Iron Policy) ने सैन्य बल और रणनीति के माध्यम से इस एकीकरण को संभव बनाया।
- नीति का अर्थ:
बिस्मार्क की “रक्त और लौह” नीति का अर्थ है – समस्याओं का समाधान भाषणों और प्रस्तावों से नहीं, बल्कि युद्ध (रक्त) और सैन्य शक्ति (लौह) द्वारा किया जाए। - इसका उद्देश्य:
इस नीति का मुख्य उद्देश्य जर्मन राज्यों का एकीकरण था, जिसे बिस्मार्क ने प्रशिया के नेतृत्व में सैन्य और कूटनीतिक उपायों से पूरा किया। - डेनमार्क युद्ध (1864):
बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर हमला किया और श्लेसविग-होलस्टीन क्षेत्र को जीता। - ऑस्ट्रिया युद्ध (1866):
डेनमार्क युद्ध के बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर जर्मन परिसंघ से बाहर कर दिया और उत्तर जर्मन परिसंघ बनाया। - फ्रांस-प्रशिया युद्ध (1870-71):
इस युद्ध में फ्रांस को हराकर बिस्मार्क ने दक्षिण जर्मन राज्यों को भी एकीकृत कर लिया। इस प्रकार समग्र जर्मनी का एकीकरण हुआ। - सैनिक शक्ति और राष्ट्रीयता का मिश्रण:
बिस्मार्क ने सैनिक बल के साथ-साथ जर्मन राष्ट्रवाद की भावना को भी प्रेरित किया, जिससे लोगों में एकता की भावना जगी। - कूटनीति और रणनीति:
बिस्मार्क ने युद्धों से पूर्व और पश्चात कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा। उन्होंने यूरोपीय शक्तियों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर प्रशिया की शक्ति को बढ़ाया।
बिस्मार्क की “रक्त और लौह” नीति ने जर्मनी को एकीकृत किया और उसे यूरोप की एक महाशक्ति बनाया। यह नीति यह दर्शाती है कि राष्ट्रीय एकता के लिए कठोर, यथार्थवादी और साहसिक कदम कभी-कभी आवश्यक हो सकते हैं।
प्रश्न-10. अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम (1775-1783) ब्रिटेन और उसकी तेरह अमेरिकी उपनिवेशों के बीच लड़ा गया था। यह संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई ही नहीं था, बल्कि यह आधुनिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों की नींव भी था। इसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं:
- अमेरिका की स्वतंत्रता: इस संग्राम का प्रमुख परिणाम था—संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। 1783 की पेरिस संधि के अंतर्गत ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना: स्वतंत्रता के बाद अमेरिका ने एक लिखित संविधान (1787) के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें संघीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई।
- वैश्विक प्रभाव: इस संग्राम ने फ्रांस, लैटिन अमेरिका और भारत जैसे अन्य देशों में स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा दी। फ्रांस की क्रांति (1789) पर इस संग्राम का गहरा प्रभाव पड़ा।
- ब्रिटेन में राजनीतिक सुधार: इस हार के बाद ब्रिटेन में भी सुधारों की मांग उठने लगी। संसद में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बल मिला और उपनिवेशों के साथ संबंधों में परिवर्तन हुआ।
- फ्रांस पर आर्थिक प्रभाव: अमेरिका की सहायता के लिए फ्रांस ने भारी ऋण लिया, जिससे वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई।
- भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभाव: ब्रिटिश ध्यान अमेरिका से हटकर भारत पर केंद्रित हो गया, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और मजबूत हुआ।
- समाज में समानता की भावना: अमेरिका में दास प्रथा और महिलाओं के अधिकारों को लेकर नई बहसें शुरू हुईं। हालाँकि यह तत्काल समाप्त नहीं हुआ, लेकिन सामाजिक जागरूकता बढ़ी।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम न केवल अमेरिका के लिए स्वतंत्रता का कारण बना, बल्कि इसने विश्व भर में लोकतांत्रिक विचारों को भी बल दिया। यह आधुनिक युग का आरंभिक परिवर्तनकारी आंदोलन था।
प्रश्न-11. प्राचीन भारत में नगरीय केन्द्रों के पतन के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में नगरीय केन्द्रों (Urban Centers) का उत्थान सिंधु सभ्यता से लेकर गुप्तकाल तक देखा गया। परन्तु गुप्तकाल के पश्चात धीरे-धीरे इन नगरीय केन्द्रों का पतन होने लगा। इसके पीछे कई कारण उत्तरदायी थे:
- राजनीतिक अस्थिरता: गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद देश छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया। बार-बार के आक्रमण, विशेषकर हूणों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के कारण शांति भंग हुई और नगरों की सुरक्षा कमज़ोर हो गई।
- आर्थिक गिरावट: विदेशी आक्रमणों, राजनीतिक विघटन और व्यापार मार्गों के विघटन से आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ। इससे नगरों की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। शिल्प और उद्योग भी ठप पड़ने लगे।
- व्यापार मार्गों का परिवर्तन: समुद्री व्यापार मार्गों में परिवर्तन तथा नए व्यापारिक केंद्रों के उभरने से पुराने नगरों का महत्व कम हो गया। इससे कई नगर उजड़ गए या पिछड़ गए।
- प्राकृतिक आपदाएँ: कुछ क्षेत्रों में बाढ़, भूकंप या जलवायु परिवर्तन ने भी नगरों के विनाश में भूमिका निभाई। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, जिससे नगरीय जनसंख्या में कमी आई।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रधानता: गुप्तकाल के बाद ग्रामीण जीवन की ओर पुनः झुकाव बढ़ा। ज़मींदारी व्यवस्था और आत्मनिर्भर ग्राम-व्यवस्था ने शहरी जीवन को पीछे छोड़ दिया। समाज कृषि आधारित हो गया।
- धार्मिक कारण: बौद्ध और जैन धर्म के मठों और शिक्षा केन्द्रों के विघटन से कई नगरों का धार्मिक महत्व समाप्त हो गया। धार्मिक यात्राएँ और सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो नगरीय जीवन का आधार थीं, उनका ह्रास हुआ।
इस प्रकार, प्राचीन भारत में नगरीय केन्द्रों के पतन के पीछे बहुआयामी कारण थे – राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक। इन कारणों ने मिलकर शहरी जीवन की गति को धीमा किया और भारत एक बार फिर ग्रामीणता की ओर लौट गया।
प्रश्न-12. व्यापार एवं शहरीकरण के अन्तः सम्बन्धों के विभिन्न आयामों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में व्यापार और शहरीकरण (Urbanization) का गहरा अंतर्संबंध था। व्यापार के विस्तार ने नगरों की उत्पत्ति और विकास को प्रेरित किया, वहीं विकसित नगर व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बन गए।
- हड़प्पा कालीन नगरों में व्यापार:
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर व्यापार आधारित सभ्यताएँ थीं। वहाँ से मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों तक व्यापार होता था। व्यापार ने इन नगरों को समृद्ध बनाया और उन्हें योजनाबद्ध ढंग से बसाया गया। - वैदिक काल में नगरों का विकास:
प्रारंभिक वैदिक काल में गाँव प्रमुख थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपयोग से कृषि और व्यापार बढ़ा, जिससे नगरों का जन्म हुआ। - महाजनपद और मौर्य काल:
इस काल में राजकीय मार्ग, नदी व्यापार और सिक्का प्रणाली से व्यापार का अभूतपूर्व विकास हुआ। पाटलिपुत्र, उज्जयिनी, तक्षशिला, वैशाली आदि नगर व्यापार के केंद्र बने। मौर्य प्रशासन व्यापार को प्रोत्साहित करता था। चुंगी कर, मार्ग व्यवस्था, तथा व्यापारिक अधिकारियों की नियुक्ति से व्यापार और नगरीकरण को गति मिली। - शिल्प और वाणिज्यिक श्रेणियाँ:
व्यापारियों और कारीगरों की श्रेणियाँ (Guilds) शहरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थीं। उन्होंने नगरों में उत्पादन, वितरण और श्रम व्यवस्था को संगठित किया। - समुद्री व्यापार और तटीय नगर:
दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में समुद्री व्यापार से नगरों का विकास हुआ। पुहार, कांची, भृगुकच्छ, सौराष्ट्र के लोथल जैसे बंदरगाह नगरों ने व्यापारिक शहरीकरण को बढ़ावा दिया। - धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र:
धार्मिक तीर्थस्थलों पर व्यापारिक मेलों और उत्सवों से शहरीकरण को बल मिला। उदाहरण: प्रयाग, काशी, गया।
व्यापार और शहरीकरण का संबंध सहकारात्मक रहा है। व्यापार ने संसाधनों का आवागमन और धन का संकेन्द्रण किया, जिससे नगरों का विकास संभव हुआ। वहीं नगरों ने व्यापारिक गतिविधियों को स्थायित्व और संरचना प्रदान की।
प्रश्न-13. औद्योगिक क्रान्ति के कारणों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में शुरू हुई एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जिसने उत्पादन के पारंपरिक तरीकों को बदलकर यंत्र आधारित उत्पादन की दिशा में समाज को अग्रसर किया। इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे –
- वैज्ञानिक आविष्कार एवं नवाचार:
नई मशीनों और तकनीकों जैसे स्पिनिंग जेनी, वॉटर फ्रेम, स्टीम इंजन आदि के आविष्कार ने उत्पादन को तेज़ और सस्ता बनाया। - पूंजी का संचय:
औपनिवेशिक व्यापार, लूट और दास व्यापार से इंग्लैंड में पर्याप्त पूंजी जमा हो चुकी थी, जिसे उद्योगों में लगाया गया। - कृषि क्रांति:
अठारहवीं शताब्दी में कृषि में सुधार हुए। इससे उत्पादन बढ़ा और श्रमिक वर्ग नगरों की ओर रोजगार की तलाश में गया। - प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता:
इंग्लैंड में कोयला, लोहा और जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे, जो औद्योगीकरण के लिए आवश्यक थे। - राजनीतिक स्थिरता:
ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र और कानून व्यवस्था ने औद्योगीकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया। - व्यापार और उपनिवेश:
ब्रिटेन के विशाल उपनिवेशों ने कच्चा माल और उत्पादों के लिए बाज़ार उपलब्ध कराए। - परिवहन का विकास:
नदी मार्ग, नहरें, सड़कों और बाद में रेलवे के विकास ने औद्योगिक उत्पादन और वितरण को सुगम बनाया। - श्रमिक वर्ग की उपलब्धता:
गांवों से नगरों की ओर पलायन करने वाले लोगों ने श्रमिक के रूप में कार्यबल की पूर्ति की।
औद्योगिक क्रांति अनेक तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों का परिणाम थी। इसने मानव समाज के जीवन, कार्य पद्धति, उत्पादन प्रणाली और सामाजिक संरचना को पूरी तरह बदल दिया।
प्रश्न-14. जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बताइए।
उत्तर:- जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था, और इसमें ओट्टो वॉन बिस्मार्क की भूमिका केंद्रीय रही। बिस्मार्क प्रशिया का प्रधानमंत्री था और उसे “आयरन चांसलर” के नाम से जाना जाता है। उसने रणनीति, कूटनीति और युद्ध के माध्यम से जर्मन राज्यों को एकीकृत किया।
- यथार्थवाद और ‘आयरन एंड ब्लड’ की नीति: बिस्मार्क ने कहा था कि “समय के महान प्रश्न भाषणों और प्रस्तावों से नहीं, बल्कि लोहा और रक्त से हल होंगे।” उसने यथार्थवादी नीति अपनाकर केवल व्यावहारिक लक्ष्यों पर ध्यान दिया।
- डेनमार्क युद्ध (1864): बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क से श्लेसविग और होल्स्टीन को छीना। यह उसकी पहली विजय थी जिसने प्रशिया की शक्ति को बढ़ाया।
- ऑस्ट्रिया युद्ध (1866): बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराकर उसे जर्मन मामलों से बाहर कर दिया और उत्तरी जर्मन परिसंघ (North German Confederation) की स्थापना की।
- फ्रांस युद्ध (1870-71): बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित कर राष्ट्रवाद की भावना को उभारा। युद्ध के बाद 1871 में वर्साय महल में जर्मन सम्राट विल्हेल्म प्रथम की ताजपोशी हुई और जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ।
- राजनीतिक चतुराई: बिस्मार्क ने सभी विरोधियों को आपसी संघर्ष में उलझा दिया। उसने कूटनीति और युद्ध दोनों का कुशल प्रयोग किया।
- प्रशिया का प्रभुत्व: बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण प्रशिया की प्रधानता के तहत हुआ, जिससे वह यूरोप की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन गया।
बिस्मार्क की दूरदर्शिता, सैन्य नीति, और कूटनीति ने जर्मनी के एकीकरण को संभव बनाया। उसने जर्मनी को एक शक्तिशाली और संगठित राष्ट्र में बदल दिया।
प्रश्न-15. अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम (1775-1783) ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का संघर्ष था। इस संग्राम के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए, जो इस प्रकार हैं –
- संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण:
13 उपनिवेश स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में संगठित हुए और एक नया गणराज्य बना। - लोकतंत्र और गणराज्यवाद की स्थापना:
अमेरिका में एक लोकतांत्रिक संविधान बना जिसमें नागरिकों को अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी दी गई। - ब्रिटेन की शक्ति में गिरावट:
इस युद्ध के पश्चात ब्रिटेन की शक्ति में गिरावट आई और वह विश्व की एकमात्र महाशक्ति नहीं रहा। - फ्रांस पर प्रभाव:
अमेरिका की क्रांति ने फ्रांस की जनता को भी प्रेरित किया, जिसका परिणाम फ्रांसीसी क्रांति (1789) के रूप में सामने आया। - उपनिवेशवाद पर चोट:
इस युद्ध ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक संदेश दिया कि उपनिवेश अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर स्वतंत्रता पा सकते हैं। - आर्थिक परिणाम:
अमेरिका को युद्ध के बाद पुनर्निर्माण करना पड़ा, वहीं ब्रिटेन को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। - मानव अधिकारों पर बल:
अमेरिकी क्रांति ने ‘मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों’ की अवधारणा को स्थापित किया, जिससे वैश्विक मानवाधिकार आन्दोलन को बल मिला। - प्रभावशाली संविधान का निर्माण:
अमेरिका का संविधान लोकतंत्र का प्रतीक बना, जिसमें शक्ति का विभाजन, कानून का शासन और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम न केवल एक उपनिवेश की स्वतंत्रता का संघर्ष था, बल्कि यह आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इसके प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़े।
प्रश्न-16. राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में क्यों असफल रहा ?
उत्तर:- राष्ट्र संघ (League of Nations) की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साय संधि के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक शांति बनाए रखना, युद्ध को रोकना, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना था। किंतु यह अपने उद्देश्यों में असफल रहा, जिसके पीछे कई कारण थे:
- अमेरिका की सदस्यता न होना: यद्यपि राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की प्रमुख भूमिका थी, फिर भी अमेरिका स्वयं इसमें शामिल नहीं हुआ। इससे इसकी शक्ति और प्रभावशीलता कम हो गई।
- अनिवार्य सैन्य शक्ति का अभाव: राष्ट्र संघ के पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। वह केवल अपील या प्रतिबंधों के माध्यम से ही काम करता था, जो प्रभावी नहीं थे।
- महाशक्तियों की उपेक्षा: जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों ने राष्ट्र संघ के आदेशों की अवहेलना की। उन्होंने आक्रामक नीतियाँ अपनाईं, लेकिन राष्ट्र संघ उन्हें रोक नहीं पाया।
- अन्यायपूर्ण संधियाँ: वर्साय संधि जैसे समझौतों ने जर्मनी में असंतोष को जन्म दिया। इन अन्यायपूर्ण शर्तों के चलते जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में राष्ट्र संघ को अस्वीकार कर दिया।
- आर्थिक संकट: 1930 के दशक की वैश्विक आर्थिक मंदी के चलते राष्ट्रों में अस्थिरता बढ़ी। इस अवसर का लाभ उठाकर फासीवादी ताकतों ने राष्ट्र संघ की उपेक्षा की।
- भीतरू नेतृत्व: राष्ट्र संघ के नेताओं में दृढ़ संकल्प की कमी थी। उन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई, जिससे आक्रामक देशों को बढ़ावा मिला।
- द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत: राष्ट्र संघ की असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण द्वितीय विश्व युद्ध (1939) का आरंभ था, जिसे रोकने में वह पूरी तरह असफल रहा।
राष्ट्र संघ का पतन उसके कमजोर ढांचे, सामूहिक नेतृत्व की कमी और वैश्विक राजनीतिक वास्तविकताओं को न समझ पाने के कारण हुआ। इसकी असफलता के अनुभवों से संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की नींव डाली गई।
vmou MAHI-06 paper , vmou MA History exam paper , vmou exam paper 2029-30 , vmou exam paper 2027-28 vmou exam paper 2026 vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4
VMOU EXAM PAPER