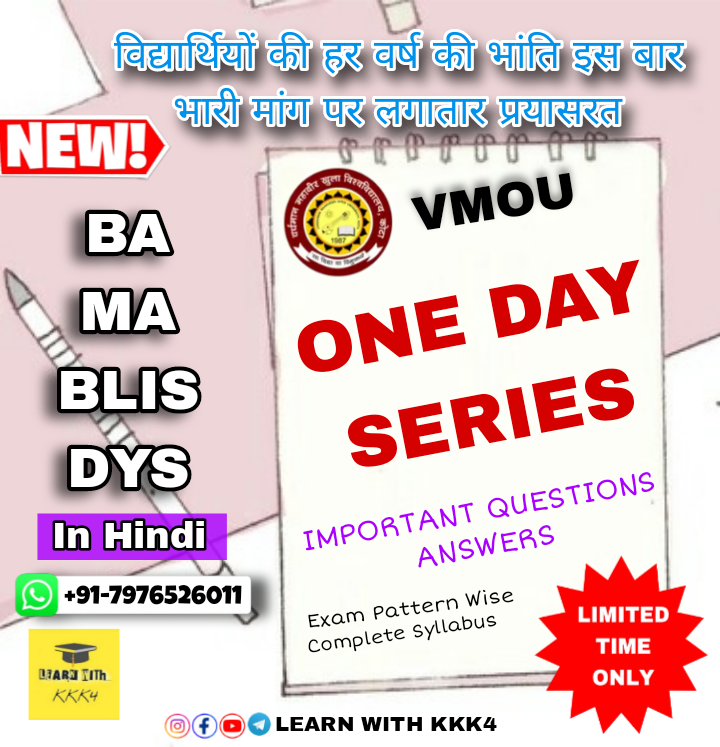VMOU MAPS-02 Paper MA POLITICAL SCIENCE MA PERVIOUS YEAR ; vmou exam paper
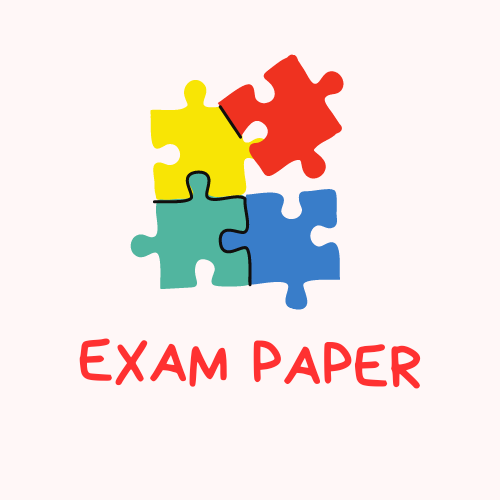
VMOU MA PERVIOUS YEAR के लिए राजनीति विज्ञान (MAPS -02 , Comparative politics ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.इतिहासबाद के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- इतिहासबाद का पतन तात्त्विक जटिलताओं, वैज्ञानिक विश्लेषण की कमी, भविष्यवाणी में विफलता और समकालीन सामाजिक परिवर्तनों की उपेक्षा के कारण हुआ।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.इतिहासवाद के विरुद्ध किन्हीं दो प्रतिक्रियाओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- इतिहासवाद के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं में तार्किक प्रतिवाद (Rational Criticism) और अनुभववादी दृष्टिकोण (Empiricism) प्रमुख रहे हैं।
प्रश्न-राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- राजनीतिक दल वह संगठित समूह होता है जो सत्ता प्राप्त करने हेतु चुनाव लड़ता है और अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने का प्रयास करता है।
प्रश्न-समाजवादी संविधान की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- (1) इसमें समाजिक और आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है।
(2) संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है।
प्रश्न-समाजवादी संविधानवाद की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- समाजवादी संविधानवाद का आशय राज्य द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, कल्याण और संसाधनों का समवितरण सुनिश्चित करना है।
प्रश्न-आत्मण्ड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था की दो विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:- (1) यह प्रणाली बहु-कार्यात्मक होती है।
(2) इसमें संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है।
प्रश्न-राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- section-b question-1
प्रश्न-अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से आपका क्या तात्पर्य है?
उत्तर:- अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वह विधायिका से स्वतंत्र होता है।
प्रश्न-राजनीतिक विकास की विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:- राजनीतिक विकास की विशेषताएँ हैं—संस्थागत स्थिरता, जन सहभागिता, वैधता, अधिकारों का विस्तार और शासन की क्षमता में वृद्धि।
प्रश्न-राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- राजनीतिक संस्कृति नागरिकों के राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों का समुच्चय है जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है।
प्रश्न-एस.ई. फाइनर द्वारा विवेचित तुलनात्मक राजनीति के किन्हीं दो आधारों को बताइए।
उत्तर:- एस.ई. फाइनर ने तुलनात्मक राजनीति के आधार के रूप में संस्थागत ढाँचा (Structure) और कार्यप्रणाली (Function) को प्रमुख रूप से स्वीकार किया है।
प्रश्न-राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- राजनीतिक आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक, जटिल, सहभागी और संस्थागत रूप ग्रहण करती है।
प्रश्न-अभिजन सिद्धान्त पर पेरेटों के विचार बताइए।
उत्तर:- पेरेटो के अनुसार समाज में एक अल्पसंख्यक समूह ‘अभिजन’ सत्ता और निर्णयों पर नियंत्रण रखता है, जो समय-समय पर परिवर्तनशील होता है।
प्रश्न-संसदीय शासन प्रणाली से आपका क्या तात्पर्य है ?
उत्तर:- संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है।
प्रश्न-अभिजन से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- अभिजन वे प्रभावशाली लोग होते हैं जो समाज या राजनीति में निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं, जैसे राजनेता, अधिकारी या उद्योगपति।
प्रश्न-प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:-प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति वह है जिसमें नागरिक सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं जैसे मतदान, प्रदर्शन और जनमत निर्माण।
प्रश्न-‘कानून की उचित प्रक्रिया’ एवं ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ में अन्तर बताइए।
उत्तर:-‘कानून की उचित प्रक्रिया’ एवं ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ में अन्तर बताइए।
उत्तर: ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ व्यक्ति के अधिकारों की न्यायसंगत समीक्षा करती है, जबकि ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ केवल विधिक प्रक्रिया का पालन करती है चाहे वह न्यायसंगत हो या नहीं।
प्रश्न-व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:-व्यवस्थापिका वह संस्था है जो कानून बनाने, संशोधन करने और सरकार की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, जैसे संसद या विधानसभा।
प्रश्न-राजनीतिक आधुनिकीकरण के किन्ही चार पक्षों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- धर्मनिरपेक्षता, विधिक समानता, लोकतांत्रिक सहभागिता और नौकरशाही का विकास।
प्रश्न-राजनीतिक विकास को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- राजनीतिक विकास वह प्रक्रिया है जिससे राजनीतिक संस्थाएँ, प्रक्रियाएँ और भागीदारी अधिक स्थिर, उत्तरदायी और प्रभावी बनती हैं।
प्रश्न-दबाव समूह को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार पर नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालते हैं, परंतु स्वयं सत्ता में भागीदार नहीं होते।
प्रश्न-राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- राजनीतिक प्रतिनिधित्व वह प्रक्रिया है जिसमें नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार में भागीदारी करते हैं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
प्रश्न-संविधान से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- संविधान एक ऐसा सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है जो राज्य की शासन प्रणाली, अधिकारों, कर्तव्यों और संस्थाओं की संरचना व कार्यविधि को निर्धारित करता है।
प्रश्न-राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- राजनीतिक आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिससे परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक, सहभागी और संस्थागत रूप में परिवर्तित होती है।
प्रश्न-संविधान के सम्मुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:-संविधान के समक्ष चुनौतियाँ हैं—सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार और विधिक प्रक्रिया की धीमी गति।
प्रश्न-संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में कोई दो अंतर बताइए।
उत्तर:- (1) संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है; अध्यक्षात्मक में नहीं।
(2) अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष होता है; संसदीय में प्रधानमंत्री होता है।
प्रश्न-संविधानवाद की किन्हीं दो आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- संविधानवाद की मुख्य आवश्यकताएँ हैं—सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण तथा नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा।
प्रश्न-प्रजातंत्र की संवैधानिक शर्तों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- प्रजातंत्र की संवैधानिक शर्तों में विधि का शासन, मौलिक अधिकारों की गारंटी और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रमुख हैं।
प्रश्न-राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है, जनता के हितों और विचारों को विधायिका में प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत करना।
प्रश्न-गैर-पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- गैर-पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं में पारंपरिक संस्थाओं की भूमिका प्रमुख होती है और यह जाति, धर्म व समुदाय आधारित निर्णय प्रणाली पर निर्भर होती हैं।
प्रश्न-संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण की किन्हीं दो आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- इसकी आलोचना में कहा गया कि यह पश्चिमी मानदंडों पर आधारित है और यह परिवर्तनशील समाजों की व्याख्या में असमर्थ है।
प्रश्न-राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य नागरिकों के राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों, दृष्टिकोणों और सहभागिता की परंपरागत एवं आधुनिक समझ से है।
प्रश्न-संविधान के कोई दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- (1) नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
(2) शासन की रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली निर्धारित करना।
प्रश्न-न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- न्यायिक पुनरावलोकन वह प्रक्रिया है जिसमें न्यायपालिका संसद या सरकार के कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती है।
प्रश्न-संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रधान मंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है।
प्रश्न-‘कानून के शासन’ से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- ‘कानून का शासन’ वह सिद्धांत है जिसमें सभी व्यक्ति और संस्थाएँ कानून के अधीन समान रूप से उत्तरदायी होते हैं।
प्रश्न-शक्ति विभाजन से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:- शक्ति विभाजन का अर्थ है—शासन की विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों को अलग-अलग संस्थाओं में बाँटना
प्रश्न-शक्ति पृथक्करण क्या है ?
उत्तर:- शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार शासन की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शाखाएँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जिससे सत्ता का दुरुपयोग न हो।
प्रश्न-आमंड एवं सिडनी वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के कोई दो प्रकार बताइए।
उत्तर:- आमंड एवं वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार हैं—परंपरागत संस्कृति (Parochial) और अधीनस्थ संस्कृति (Subject Political Culture)।
प्रश्न-अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन प्रणालियों में कोई दो अन्तर बताइए।
उत्तर:- अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है जबकि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री; साथ ही कार्यपालिका संसद से स्वतंत्र होती है जबकि संसदीय में उत्तरदायी होती है।
Section-B
प्रश्न-1.राजनीतिक दल का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- राजनीतिक दल ऐसे संगठनों को कहते हैं जो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने, चुनाव में भाग लेने और सत्ता प्राप्त करने हेतु कार्य करते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- राजनीतिक उद्देश्य – राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य शासन प्राप्त करना और अपने कार्यक्रम लागू करना होता है।
- संगठित ढांचा – दल के भीतर नेता, कार्यकर्ता, सदस्य आदि का एक व्यवस्थित ढांचा होता है।
- आदर्श और नीति – प्रत्येक दल की एक विचारधारा और नीति होती है, जो उसे अन्य दलों से अलग करती है।
- जनसमर्थन – राजनीतिक दल जनमत प्राप्त करने हेतु प्रचार, जनसंपर्क व रैलियों आदि का सहारा लेते हैं।
- चुनावों में भागीदारी – वे चुनावों में भाग लेकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं।
राजनीतिक दल लोकतंत्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जनमत को संगठित करने का कार्य करते हैं।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.राजनीतिक विकास के प्रचलित मॉडलों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- राजनीतिक विकास के विभिन्न मॉडल विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। ये मॉडल यह स्पष्ट करते हैं कि समाज में राजनीति किस दिशा में विकसित होती है।
प्रमुख मॉडल:
- आधुनिकीकरण मॉडल: लूसियन पाइ (Lucian Pye) के अनुसार यह प्रक्रिया आर्थिक विकास, शिक्षा, शहरीकरण आदि के साथ जुड़ी होती है।
- संरचनात्मक कार्यात्मक मॉडल: गैब्रिएल आलमंड ने यह मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें राजनीतिक संस्थाओं के कार्य और संरचना पर बल दिया गया।
- साम्यवाद बनाम लोकतंत्र मॉडल: साम्यवादी देशों में एक प्रकार की विकास प्रक्रिया होती है जबकि लोकतांत्रिक देशों में अलग।
- राजनीतिक संस्कृति मॉडल: इसमें यह देखा जाता है कि नागरिकों की राजनीतिक चेतना और सहभागिता विकास को कैसे प्रभावित करती है।
ये मॉडल किसी देश की राजनीतिक स्थिरता, सहभागिता और संस्थागत क्षमताओं के विश्लेषण में सहायक होते हैं।
प्रश्न-3.लोकतांत्रिक अभिजन सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर:- लोकतांत्रिक अभिजन सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र में शक्ति वास्तविक रूप से जनता के पास नहीं होती, बल्कि चुनिंदा अभिजनों (elites) के पास होती है। ये अभिजन राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से प्रभावशाली होते हैं।
आलोचनात्मक परीक्षण:
यह सिद्धांत लोकतंत्र की मूल आत्मा—जन-शक्ति—को नकारता है।
यह अल्पसंख्यकों के प्रभुत्व को वैध ठहराता है।
परंतु यह सिद्धांत यह यथार्थ प्रस्तुत करता है कि आज के लोकतंत्र में निर्णय प्रक्रिया में सामान्य जनता की भूमिका सीमित हो गई है।
इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी हो सकती है।
प्रश्न-राजनीतिक समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक समाजीकरण की विभिन्न एजेन्सियों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों को सीखता है और समाज के एक सक्रिय नागरिक के रूप में विकसित होता है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता एवं विकास में सहायक होती है।
मुख्य एजेंसियाँ:
धार्मिक एवं सामाजिक संगठन: ये संस्था भी व्यक्ति के राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं।
परिवार: प्रारंभिक राजनीतिक धारणाओं की नींव परिवार में ही रखी जाती है।
शिक्षा संस्थान: स्कूल व कॉलेज नागरिक शास्त्र, संविधान आदि के माध्यम से राजनीतिक चेतना पैदा करते हैं।
मीडिया: समाचार पत्र, टीवी, सोशल मीडिया आदि राजनीतिक जानकारी प्रदान करते हैं।
राजनीतिक दल: व्यक्ति को सक्रिय राजनीतिक भागीदारी सिखाते हैं।
सहकर्मी समूह (peer group): दोस्तों के समूह में चर्चा से राजनीतिक विचार विकसित होते हैं।
प्रश्न-5.तुलनात्मक राजनीति में तुलना के आधारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- तुलनात्मक राजनीति एक ऐसी विधा है जो विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और नीतियों की तुलना करती है। इसमें तुलना के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं:
- संस्थागत आधार – विभिन्न देशों की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दलों व ब्यूरोक्रेसी की संरचना और कार्यप्रणाली की तुलना।
- कार्यक्षमता आधारित तुलना – राजनीतिक संस्थाएं अपने कार्य कितनी कुशलता से करती हैं, इसकी तुलना।
- आदर्श और मूल्य आधारित आधार – लोकतंत्र, मानवाधिकार, स्वतंत्रता आदि मूल्यों की तुलना विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में।
- ऐतिहासिक-सांस्कृतिक आधार – राजनीतिक संरचनाएं कैसे संस्कृति, धर्म, परंपरा और इतिहास से प्रभावित होती हैं।
- आर्थिक-सामाजिक आधार – राजनीति पर आर्थिक स्थिति, वर्ग संरचना, जाति, लिंग, और शिक्षा का प्रभाव।
इन आधारों से तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान होता है और यह वैश्विक राजनीतिक समझ को व्यापक बनाता है।
प्रश्न-6.द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति में क्या नये परिवर्तन आये ?
उत्तर:- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पहले यह अध्ययन मुख्यतः संस्थागत और कानूनी पहलुओं तक सीमित था, लेकिन युद्ध के बाद यह व्यवहारवादी (behavioral) दृष्टिकोण की ओर बढ़ा। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों जैसे डेविड ईस्टन, गेब्रियल आल्मंड आदि ने तुलनात्मक राजनीति को अधिक वैज्ञानिक और अनुभवजन्य (empirical) बनाने का प्रयास किया।
इस युग में तुलनात्मक अध्ययन के लिए विकासशील देशों, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की राजनीतिक प्रणालियों को भी शामिल किया गया। अब अध्ययन केवल पश्चिमी लोकतंत्रों तक सीमित नहीं रहा। इसके अलावा, तुलनात्मक राजनीति में अब राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण जैसे विषयों को भी महत्व मिला।
इसके साथ ही तुलनात्मक राजनीति ने संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण (structural-functional analysis), प्रणाली सिद्धांत (system theory) और अभिजन सिद्धांत (elite theory) जैसे नए दृष्टिकोणों को अपनाया। इस प्रकार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति अधिक वैज्ञानिक, समावेशी और व्यापक बन गई।
प्रश्न-7.संविधानवाद की मुख्य आवश्यकताओं को विवेचना कीजिए।
उत्तर:- संविधानवाद का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार की शक्ति सीमित हो और वह कानून के अधीन हो। इसके लिए कुछ आवश्यकताएँ होती हैं:
- लिखित संविधान: जिससे नागरिकों के अधिकार एवं शासन की सीमाएँ स्पष्ट हों।
- शक्ति का विभाजन: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति का बँटवारा।
- न्यायिक पुनरावलोकन: न्यायालय को यह अधिकार कि वह असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सके।
- मौलिक अधिकारों की गारंटी: नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
संविधानवाद लोकतंत्र की आत्मा है जो शासन को निरंकुश होने से रोकता है।
प्रश्न-तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पर आसण्ड के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- गेब्रियल आलमंड ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह उपागम समाज को विभिन्न संरचनाओं (संस्थाओं) जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि के कार्यों (प्रकार्यों) के आधार पर समझने का प्रयास करता है।
आलमंड के अनुसार, सभी राजनीतिक प्रणालियों में तीन प्रमुख प्रकार्य होते हैं:
- इनपुट प्रकार्य (Input Functions): जिसमें राजनीतिक समाजीकरण, हित अभिव्यक्ति, हित समाकलन और राजनीतिक संचार शामिल हैं।
- आउटपुट प्रकार्य (Output Functions): जिसमें नियम निर्माण, नियम प्रवर्तन एवं नियम की व्याख्या आती है।
यह दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है क्योंकि यह केवल संस्थाओं के स्वरूप पर नहीं बल्कि उनके कार्यों पर भी ध्यान देता है।
प्रश्न-तुलनात्मक राजनीति के क्लासिकल परिप्रेक्ष्य की विवेचना कीजिए
उत्तर:- तुलनात्मक राजनीति का क्लासिकल परिप्रेक्ष्य राजनीतिक विचारों और संस्थाओं का ऐतिहासिक व दार्शनिक विश्लेषण करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- दार्शनिक दृष्टिकोण – प्लेटो, अरस्तू, लॉक, रूसो, मार्क्स जैसे विचारकों ने राज्य, सत्ता और न्याय की अवधारणाओं को स्पष्ट किया।
- संस्थात्मक अध्ययन – क्लासिकल दृष्टिकोण मुख्यतः राज्य की संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की तुलना पर केंद्रित था।
- मानव मूल्यों पर बल – यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे आदर्शों की व्याख्या करता है।
- सांस्कृतिक दृष्टिकोण – समाज, परंपरा और संस्कृति को राजनीतिक व्यवस्था के साथ जोड़ा गया।
हालांकि, क्लासिकल दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति और व्यवहारिक विश्लेषण की कमी थी, लेकिन इसने राजनीतिक अध्ययन की नींव रखी और आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का मार्ग प्रशस्त किया।
प्रश्न-तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक एवं अनुभवजन्य होती है। यह अध्ययन विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार की तुलना के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं, नीतियों और संरचनाओं के बीच समानता और भिन्नताओं को समझना होता है।
तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह केवल सरकारों या संविधानों की तुलना तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें राजनीतिक संस्कृति, समाजीकरण, दल, चुनाव, नीतिनिर्माण, अभिजन, ब्यूरोक्रेसी आदि का अध्ययन भी किया जाता है। यह पश्चिमी और गैर-पश्चिमी दोनों प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को शामिल करता है।
इसका क्षेत्र अंतर-विषयी भी होता है क्योंकि यह समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि से भी विचार उधार लेता है। तुलनात्मक राजनीति आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक केंद्रीय क्षेत्र बन चुका है, जो न केवल सैद्धांतिक विश्लेषण, बल्कि व्यावहारिक समझ और नीति-निर्माण में भी सहायक होता है।
प्रश्न-तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं प्रकृति को विवेचना कीजिए।
उत्तर:- तुलनात्मक राजनीति वह राजनीतिक अध्ययन की शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों की तुलना की जाती है। इसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक ढाँचों को समझना, विश्लेषण करना एवं उनके बीच समानता व भिन्नता की पहचान करना है।
इसकी प्रकृति तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा वैज्ञानिक होती है। यह केवल संस्थाओं की तुलना नहीं करती बल्कि राजनीतिक संस्कृति, समाजीकरण, विकास, आधुनिकीकरण जैसे पहलुओं को भी समाहित करती है। यह परंपरागत अध्ययन से हटकर अनुभवजन्य एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाती है। तुलनात्मक राजनीति लोकतंत्र, अधिनायकवाद, राजनीतिक दल, चुनाव प्रणाली आदि की तुलना करके वैश्विक राजनीति की समग्र समझ को विस्तृत करती है।
प्रश्न-समाजवादी व्यवस्था में संविधान की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- समाजवादी व्यवस्था में संविधान की प्रकृति राज्य के समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्धारित की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और राज्य के माध्यम से संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना होता है।
मुख्य विशेषताएँ:
- राज्य की सर्वोच्चता: राज्य उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है।
- सामाजिक व आर्थिक समानता: निजी संपत्ति की सीमाएँ होती हैं।
- मौलिक अधिकारों का सामूहिक स्वरूप: व्यक्ति से अधिक समाज के हित को प्राथमिकता दी जाती है।
- नियोजित विकास: संविधान में आर्थिक योजनाओं का उल्लेख किया जाता है।
सोवियत संघ, चीन जैसे देशों में समाजवादी संविधान का उदाहरण देखने को मिलता है। भारत के संविधान में भी समाजवाद को उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है।
प्रश्न-उदारवाद में संविधानवाद की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- उदारवाद में संविधानवाद एक मूलभूत सिद्धांत है जो राज्यशक्ति को सीमित करने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और कानून के शासन की स्थापना पर बल देता है। इसकी प्रमुख प्रकृति निम्नलिखित है:
- सीमित सरकार – उदारवाद में यह माना जाता है कि सरकार की शक्ति संविधान द्वारा सीमित होनी चाहिए जिससे मनमानी न हो सके।
- न्यायिक स्वतंत्रता – संविधानवाद न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने पर जोर देता है।
- नागरिक अधिकारों की गारंटी – उदार संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी होती है।
- कानून का शासन – सभी नागरिक और शासक कानून के अधीन होते हैं।
- विभाजन की प्रणाली – कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन संविधानवाद की आधारशिला है।
इस प्रकार उदारवाद में संविधानवाद का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और राज्य को उत्तरदायी बनाना है।
प्रश्न-गैर-पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- गैर-पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाएं वे हैं जो पश्चिमी देशों (जैसे अमेरिका, ब्रिटेन) के बाहर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को दर्शाती हैं। इनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और आर्थिक पृष्ठभूमियाँ होती हैं।
मुख्य विशेषताएँ:
लोकतंत्र की प्रक्रिया अधूरी: चुनाव तो होते हैं, पर लोकतंत्र के मूल तत्वों का अभाव होता है।
परंपरागत मूल्यों का प्रभाव: इनमें परंपराएं और धर्म राजनीति में गहरी भूमिका निभाते हैं।
व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व: नेता अक्सर करिश्माई या पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं।
संस्थागत दुर्बलता: लोकतांत्रिक संस्थाएं अक्सर सशक्त नहीं होतीं।
सैन्य हस्तक्षेप: सेना का राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप सामान्य होता है।
जाति, धर्म, भाषा आधारित राजनीति: मतदाता का निर्णय इन आधारों पर प्रभावित होता है।
प्रश्न-‘सीमित सरकार’ की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- सीमित सरकार (Limited Government) वह सरकार होती है जिसकी शक्तियों और कार्यक्षेत्र को संविधान, क़ानूनों या संस्थागत ढाँचों द्वारा नियंत्रित और सीमित किया गया हो। इसका उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है।
मुख्य विशेषताएँ:
जनउत्तरदायित्व: सरकार जनता को उत्तरदायी होती है और पारदर्शिता बनाए रखती है।
संवैधानिकता: सरकार संविधान द्वारा सीमित होती है, जिससे सत्ता का दुरुपयोग रोका जाता है।
न्यायिक पुनरावलोकन: न्यायालय यह देखता है कि सरकार अपने अधिकारों की सीमा लांघ तो नहीं रही।
बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा: नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सीमित सरकार का मूल उद्देश्य होता है।
प्रश्न-संरचनात्मक कार्यात्मक’ विश्लेषण पर आमण्ड के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- गैब्रियल आलमण्ड ने राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन में ‘संरचनात्मक-कार्यात्मक’ दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने समाजशास्त्र के सिद्धांतों को राजनीति विज्ञान में लागू किया।
मुख्य बिंदु:
तुलनात्मक अध्ययन: इस मॉडल के माध्यम से विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की जा सकती है।
संरचना: प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में कुछ संरचनाएँ (जैसे विधायिका, कार्यपालिका) होती हैं।
कार्य: ये संरचनाएं कुछ निश्चित कार्य (जैसे नियम बनाना, न्याय देना) करती हैं।
सार्वभौमिक कार्य: आलमण्ड ने कहा कि हर राजनीतिक व्यवस्था में कुछ कार्य जैसे राजनीतिक समाजीकरण, संचार, निर्णय-निर्माण आदि अनिवार्य होते हैं।
प्रश्न-प्रजातंत्र की संवैधानिक शर्तों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ संवैधानिक शर्तों का होना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं:
- संविधान का अस्तित्व – एक लिखित या अलिखित संविधान जो नागरिकों के अधिकारों और सरकार के कर्तव्यों को परिभाषित करता है।
- शक्ति का विभाजन – कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट शक्तिविभाजन।
- स्वतंत्र न्यायपालिका – न्यायालय स्वतंत्र हो ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
- चुनाव प्रणाली – स्वतंत्र, निष्पक्ष और समय-समय पर होने वाले चुनाव।
- अधिकारों की गारंटी – नागरिकों को स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म और संघ की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त हों।
- कानून का शासन – राज्य के सभी अंग और नागरिक कानून के अधीन हों।
इन शर्तों के बिना लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है और वास्तविक जनहित साध्य नहीं हो पाता।
प्रश्न-ईस्टन की सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित सामान्य व्यवस्था सिद्धांत (General Systems Theory) राजनीति को एक जीवंत प्रणाली (political system) के रूप में देखता है। उनके अनुसार, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था एक खुली प्रणाली होती है, जो समाज से निरंतर सूचना, मांग और समर्थन के रूप में “इनपुट” प्राप्त करती है और निर्णय व नीतियों के रूप में “आउटपुट” प्रदान करती है।
इस सिद्धांत के मुख्य घटक हैं: इनपुट (मांग और समर्थन), राजनीतिक प्रणाली की प्रक्रिया (निर्णयन), आउटपुट (नीतियाँ और कार्य), फीडबैक और पर्यावरण। ईस्टन के अनुसार, यह प्रणाली तब तक स्थिर रहती है जब तक उसे पर्यावरण से पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है।
यह सिद्धांत तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के तहत विकसित हुआ और राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की तुलना और विश्लेषण कर सकते हैं।
प्रश्न-राजनीतिक विकास पर लुशियन पाई के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में देखा। उनके अनुसार यह केवल संस्थाओं का विकास नहीं, बल्कि समाज के राजनीतिक व्यवहार में परिपक्वता लाना भी है।
मुख्य बिंदु:
- समस्याओं का उत्तर: राजनीतिक विकास समस्याओं से निपटने की क्षमता को दर्शाता है।
- व्यवस्था का विभेदन: संस्थाएं अधिक विशिष्ट और कार्यक्षम बनती हैं।
- भागीदारी में वृद्धि: नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ती है।
- धर्मनिरपेक्षता: परंपरागत मूल्यों से हटकर आधुनिक, वैज्ञानिक सोच की ओर झुकाव।
- संस्थागतरण: राजनीतिक संस्थाएं मजबूत और उत्तरदायी बनती हैं।
लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास केवल संरचनात्मक परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति और वैधता का विकास भी है।
प्रश्न-राजनीतिक आधुनिकीकरण पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- राजनीतिक आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को अपनाती है। इसमें कानून का शासन, जनभागीदारी, राजनीतिक दलों का विकास, नौकरशाही का व्यावसायिकरण, और नागरिक अधिकारों की स्थापना जैसे तत्व सम्मिलित होते हैं।
आधुनिकीकरण का तात्पर्य केवल आर्थिक या तकनीकी उन्नति नहीं है, बल्कि राजनीतिक चेतना और संस्थागत परिवर्तन भी इसका महत्वपूर्ण भाग हैं। डेविड अप्टर, लूसियन पाइ और सैमुअल हंटिंगटन जैसे विचारकों ने इस सिद्धांत का विस्तार किया है। हंटिंगटन के अनुसार, राजनीतिक आधुनिकीकरण की सफलता राजनीतिक संस्थाओं की स्थिरता और उनकी क्षमता पर निर्भर करती है।
राजनीतिक आधुनिकीकरण विकासशील देशों में स्थिर शासन, उत्तरदायी सरकार और राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने में सहायक होता है। यह प्रक्रिया अनेक बार असंतुलन और संघर्ष भी उत्पन्न करती है, विशेषकर जब संस्थागत विकास सामाजिक परिवर्तन के साथ मेल नहीं खाता।
प्रश्न-राजनीतिक दल, दवाब समूह एवं हित समूह के मध्य अंतर बताइए।
उत्तर:- section-b ques-1
प्रश्न-राजनीतिक दल एवं दवाव समूह के मध्य अन्तर बताइए।
उत्तर:- section-b ques-1
प्रश्न-अभिजन सिद्धांत पर पेरेटों के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- विल्फ्रेडो पेरेटो (Vilfredo Pareto) एक इटालियन समाजशास्त्री थे जिन्होंने अभिजन सिद्धांत (Elite Theory) को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं – शासक अभिजन (Ruling Elites) और शासित जनसमूह (Masses)।
मुख्य विचार:
- अभिजन का संचलन: पेरेटो के अनुसार, समय-समय पर पुराने अभिजन हटते हैं और नए अभिजन सत्ता में आते हैं – इसे उन्होंने “एलीट सर्कुलेशन” कहा।
- 80/20 सिद्धांत: पेरेटो ने यह भी बताया कि समाज के 20% लोग 80% संसाधनों को नियंत्रित करते हैं।
- करिश्माई नेतृत्व: अभिजन में नेतृत्व के विशेष गुण होते हैं जो उन्हें सामान्य जन से अलग बनाते हैं।
पेरेटो ने यह विचार रखा कि लोकतंत्र के बावजूद सत्ता सीमित लोगों के हाथ में ही रहती है।
प्रश्न-अभिजन सिद्धांत पर पेरेटो के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- विलफ्रेडो पेरेटो ने अभिजन (Elite) सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनका मानना था कि समाज में सदैव एक छोटा समूह शासन करता है जिसे ‘अभिजन’ कहा जाता है।
- सामाजिक विभाजन – पेरेटो ने समाज को दो वर्गों में बाँटा: अभिजन (शासक वर्ग) और गैर-अभिजन (शासित वर्ग)।
- अभिजन का चक्र सिद्धांत – पेरेटो ने कहा कि एक प्रकार का अभिजन धीरे-धीरे निष्क्रिय हो जाता है और दूसरा नया समूह उसकी जगह लेता है। इसे ‘Elite Circulation’ कहते हैं।
- शेर और लोमड़ी अभिजन – उन्होंने अभिजनों को दो प्रकारों में बाँटा: शेर (बल प्रयोग करने वाले) और लोमड़ी (चालाक और चतुर)।
- लोकतंत्र का खंडन – पेरेटो का मानना था कि लोकतंत्र एक मिथक है, वास्तव में सदैव कुछ ही लोग शासन करते हैं।
इस प्रकार पेरेटो का अभिजन सिद्धांत लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष को उजागर करता है और सत्ता संरचना की वास्तविकता को दिखाता है।
प्रश्न-बहुल अभिजन सिद्धांत की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- बहुल अभिजन सिद्धांत (Pluralistic Elite Theory) यह मानता है कि सत्ता समाज में केवल एक ही नहीं, बल्कि विभिन्न समूहों में बंटी होती है और अनेक अभिजन (elites) सत्ता की भागीदारी करते हैं। यह सिद्धांत लोकतंत्र के यथार्थ रूप को स्पष्ट करता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनीति, व्यवसाय, धर्म, शिक्षा, मीडिया आदि के प्रभावशाली व्यक्ति मिलकर निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक रोबर्ट डाल, सी. राइट मिल्स और डेविड ट्रूमैन रहे हैं। डाल का मानना था कि “बहुलतावादी लोकतंत्र” में नीति निर्माण विभिन्न प्रतिस्पर्धी अभिजनों के बीच संतुलन से होता है। यह सिद्धांत यह भी कहता है कि कोई भी अभिजन समूह पूर्ण रूप से हावी नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न अभिजन समूहों के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है।
बहुल अभिजन सिद्धांत लोकतंत्र को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखता है और यह मानता है कि आम जनता सीधे सत्ता में नहीं होती, लेकिन विभिन्न अभिजन समूहों के माध्यम से उसकी इच्छा प्रतिबिंबित होती है। यह सिद्धांत लोकतंत्र की व्याख्या करते समय शक्ति के वितरण को समझने में सहायक होता है।
प्रश्न-अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका से स्वतंत्र होती है और राष्ट्रपति राज्य प्रमुख एवं शासन प्रमुख दोनों होता है। अमेरिका इसका प्रमुख उदाहरण है।
मुख्य विशेषताएँ:
- राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव: जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करती है।
- कार्यपालिका और विधायिका में पृथक्करण: दोनों शाखाएँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं।
- स्थिरता: राष्ट्रपति निर्धारित कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जिससे शासन स्थिर होता है।
- सशक्त नेतृत्व: राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्तियाँ होती हैं जो त्वरित निर्णय लेने में सहायक होती हैं।
हालाँकि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण और विधायिका पर नियंत्रण की संभावना भी होती है।
प्रश्न-आल्मण्ड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के आगत एवं निर्गत कार्यों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- गेब्रियल आल्मण्ड ने राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को दो भागों में बाँटा – आगत (Input) और निर्गत (Output)। यह वर्गीकरण उनके संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण का हिस्सा है, जिसके माध्यम से वे विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करते हैं।
आगत कार्य (Input Functions):
(1) राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती – नागरिकों को राजनीतिक मूल्यों, विचारों से परिचित कराना।
(2) हित समुच्चयन – नागरिकों की समस्याओं और हितों को एकत्र करना।
(3) हित अभिव्यक्ति – उन हितों को राजनीतिक मंच पर व्यक्त करना।
(4) राजनीतिक संप्रेषण – नागरिकों और राजनीतिक प्रणाली के बीच संचार।
निर्गत कार्य (Output Functions):
(1) नियम निर्माण – कानून बनाना।
(2) नियम अनुप्रयोग – उन नियमों को लागू करना।
(3) नियम अधिरोपण – नियमों के उल्लंघन पर दंड देना।
यह मॉडल सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में लागू होता है, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या अधिनायकवादी। इससे राजनीतिक प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक ढंग से समझा जा सकता है।
प्रश्न-संविधानवाद की मुख्य आवश्यकताओं को विवेचना कीजिए।
उत्तर:- संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो यह सुनिश्चित करती है कि शासक वर्ग का शासन सीमित एवं कानून द्वारा नियंत्रित हो। इसकी प्रमुख आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:
- लिखित संविधान: एक स्पष्ट और संगठित संविधान जो नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करता है।
- कानून का शासन: राज्य का संचालन कानूनों के अनुसार हो, किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं।
- अधिकारों की सुरक्षा: मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो जैसे स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति आदि।
- शक्ति का विभाजन: कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका में संतुलन और नियंत्रण बना रहे।
- न्यायिक पुनरावलोकन: न्यायपालिका को यह अधिकार हो कि वह विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सके।
संविधानवाद लोकतांत्रिक शासन की नींव है जो सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है।
प्रश्न-व्यवस्थापिका के कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- व्यवस्थापिका किसी भी राज्य की वह संस्था होती है जो कानून निर्माण, नीति निर्धारण और सरकार पर नियंत्रण का कार्य करती है। इसके कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित है:
- सकारात्मक पक्ष
कानून निर्माण – व्यवस्थापिका समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाती है।
सरकार पर नियंत्रण – यह कार्यपालिका पर निगरानी रखती है और उसे उत्तरदायी बनाती है।
जनप्रतिनिधित्व – यह जनता की आकांक्षाओं को नीति में बदलने का कार्य करती है।
- नकारात्मक पक्ष
दलीय अनुशासन – अधिकांश समय व्यवस्थापिका सरकार की कठपुतली बन जाती है और स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती।
विलंब – कई बार निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक धीमी हो जाती है।
विलासिता और भ्रष्टाचार – कुछ स्थानों पर विधायकों में भ्रष्टाचार और सुविधाभोगिता बढ़ रही है।
इस प्रकार, व्यवस्थापिका लोकतंत्र की आत्मा होते हुए भी कई व्यावहारिक चुनौतियों से जूझ रही है।
प्रश्न-व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- लोकतांत्रिक प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय अपनाती है:
प्रश्नकाल और अल्पकालिक चर्चा: मंत्रीगण से उनके विभागों पर प्रश्न पूछे जाते हैं।
विश्वास प्रस्ताव/अविश्वास प्रस्ताव: संसद के माध्यम से सरकार पर विश्वास या अविश्वास जताया जाता है।
बजट स्वीकृति: कार्यपालिका को बजट के लिए विधायिका की स्वीकृति आवश्यक होती है।
संसदीय समितियाँ: प्रशासन की निगरानी हेतु विभिन्न स्थायी समितियाँ कार्य करती हैं।
प्रश्न-हाल के वर्षों में कार्यपालिका के बढ़ते हुए महत्व की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- हाल के वर्षों में कार्यपालिका का महत्व वैश्विक स्तर पर अत्यधिक बढ़ा है। इसका कारण यह है कि निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में कार्यपालिका की भूमिका अधिक सशक्त और प्रभावशाली हो गई है।
- आपात स्थितियों में भूमिका: महामारी, युद्ध, आतंकवाद आदि स्थितियों में कार्यपालिका को त्वरित निर्णय लेने होते हैं।
- विकासात्मक योजनाओं का संचालन: आर्थिक सुधार, कल्याणकारी योजनाओं और विदेश नीति को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है।
- प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण: कार्यपालिका नौकरशाही के माध्यम से शासन का संचालन करती है।
इस प्रकार कार्यपालिका, जो पहले केवल नीति कार्यान्वयन की भूमिका में थी, अब नीति निर्माण में भी प्रमुख भूमिका निभा रही है।
प्रश्न-उदारवाद में संविधानवाद की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- उदारवाद में संविधानवाद एक मूलभूत सिद्धांत है, जो राज्य की शक्ति को सीमित कर नागरिक स्वतंत्रता और विधि के शासन की रक्षा करता है। संविधानवाद का अर्थ है – ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासकों की शक्ति एक लिखित या अलिखित संविधान द्वारा नियंत्रित हो।
उदारवादी विचारकों जैसे लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू ने सरकार की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए संवैधानिक सीमाओं और शक्ति पृथक्करण का समर्थन किया। संविधानवाद विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाकर निरंकुशता को रोकता है।
इस सिद्धांत में व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, विधि का शासन, न्यायिक समीक्षा आदि को विशेष महत्व प्राप्त है। उदारवाद मानता है कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवन्त प्रक्रिया है जो शासन को उत्तरदायी और पारदर्शी बनाती है।
अतः, उदारवाद में संविधानवाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आत्मा है, जो व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और सत्ता के संतुलन को सुनिश्चित करता है।
प्रश्न-‘संसदीय शासन प्रणाली’ का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- संसदीय शासन प्रणाली वह शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका (Executive) संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और विधायिका (Legislature) के विश्वास पर टिकी रहती है।
मुख्य विशेषताएँ:
- प्रधानमंत्री नेतृत्व: कार्यपालिका का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, जो संसद का सदस्य होता है।
- विधानपालिका को उत्तरदायित्व: सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और विश्वास मत खोने पर इस्तीफा देना पड़ता है।
- कार्यपालिका की द्वैधता: इसमें राज्य प्रमुख (राष्ट्रपति/राजा) और सरकार प्रमुख (प्रधानमंत्री) अलग होते हैं।
- पार्टी प्रणाली: आमतौर पर यह प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था में कार्य करती है।
उदाहरण: भारत, ब्रिटेन आदि में यह प्रणाली प्रचलित है।
प्रश्न-संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य सम्बन्ध की प्रकृति क्या है ?
उत्तर:- संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका (executive) और व्यवस्थापिका (legislature) के बीच घनिष्ठ और सहयोगात्मक संबंध होता है। कार्यपालिका, विशेषकर मंत्रिपरिषद, सीधे-सीधे व्यवस्थापिका से ही निकलती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री सांसद होते हैं और उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होना आवश्यक होता है।
इस प्रणाली में ‘कार्यपालिका’ कानूनों के कार्यान्वयन की जिम्मेदार होती है, जबकि ‘व्यवस्थापिका’ कानून बनाती है। लेकिन चूंकि दोनों एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए उनके कार्यों में अंतर के बावजूद तालमेल बना रहता है। कार्यपालिका को हटाने का अधिकार भी संसद के पास अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से होता है।
यह संबंध संसदीय उत्तरदायित्व, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित होता है। यदि संसद कार्यपालिका को समर्थन देना बंद कर दे, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए कार्यपालिका को संसद की इच्छा के अनुरूप कार्य करना पड़ता है।
प्रश्न-भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- भारत में न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान के आधार पर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की वैधता की समीक्षा कर सकते हैं।
- संवैधानिक प्रावधान – अनुच्छेद 13 के अनुसार, कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, अमान्य घोषित किया जा सकता है।
- प्रमुख निर्णय – केसवानंद भारती केस (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- लोकतंत्र की रक्षा – न्यायिक पुनरावलोकन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और कार्यपालिका को मनमानी से रोकता है।
- सीमाएँ – हालांकि यह शक्ति व्यापक है, परंतु न्यायपालिका केवल विधिक पहलू देखती है, नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती।
इस प्रकार, न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय लोकतंत्र की मूल आत्मा की रक्षा करता है।
प्रश्न-अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन पर एक लेख लिखिए।
उत्तर:- अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1803 के Marbury v. Madison प्रकरण में स्थापित किया गया। इसके अनुसार, यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होता है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है।
मुख्य विशेषताएँ:
- संविधान की सर्वोच्चता: कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं।
- सत्ता का नियंत्रण: विधायिका एवं कार्यपालिका की गतिविधियों पर निगरानी।
- लोकतंत्र की रक्षा: नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा।
अमेरिका की संघीय न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वह केन्द्र व राज्य दोनों के कानूनों की समीक्षा करे। यह सिद्धांत अमेरिका में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र एवं सशक्त संस्था बनाता है
प्रश्न-विभिन्न निर्वाचन प्रणालियों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- निर्वाचन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। विश्व में प्रमुखतः तीन प्रकार की निर्वाचन प्रणालियाँ प्रचलित हैं:
- बहुसंख्यक प्रणाली (Majoritarian): इसमें वह प्रत्याशी विजयी होता है जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, जैसे भारत की ‘प्रथम-पद-पर-पूर्व’ (First-Past-The-Post) प्रणाली।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation): इसमें राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं, जैसे इजरायल और नीदरलैंड्स में।
- मिश्रित प्रणाली (Mixed System): इसमें दोनों प्रणालियों के तत्वों को मिलाया जाता है। जैसे जर्मनी में।
प्रत्येक प्रणाली के अपने लाभ और दोष होते हैं। बहुसंख्यक प्रणाली सरल होती है पर अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, जबकि आनुपातिक प्रणाली अधिक न्यायसंगत होती है।
प्रश्न-कानून के शासन की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- कानून का शासन (Rule of Law) वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो या राज्य का प्रमुख, कानून के अधीन होते हैं। यह विधि की प्रधानता को स्थापित करता है।
मुख्य विशेषताएँ:
- समानता: सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान होते हैं।
- कानून का सर्वोच्चता: किसी भी संस्था या व्यक्ति की मर्जी कानून से ऊपर नहीं होती।
- न्यायिक स्वतंत्रता: न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए।
- मूल अधिकारों की रक्षा: नागरिकों के मौलिक अधिकार संरक्षित रहते हैं।
- प्रक्रियात्मक न्याय: दंड प्रक्रिया निष्पक्ष और पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार होती है।
इस सिद्धांत का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करना है।
प्रश्न-व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को नियन्त्रित करने को विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- व्यवस्थापिका का कार्य न केवल कानून बनाना है, बल्कि कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाना भी है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं:
बहस और चर्चा: महत्वपूर्ण विषयों पर बहस से कार्यपालिका को विवश किया जाता है।
प्रश्नकाल (Question Hour): मंत्रीगण से प्रश्न पूछे जाते हैं।
अस्थगन प्रस्ताव: अचानक मुद्दे पर बहस कर कार्यपालिका को उत्तर देना पड़ता है।
विश्वास प्रस्ताव/अविश्वास प्रस्ताव: सरकार का बहुमत सिद्ध होता है या हटाया जाता है।
वित्तीय नियंत्रण: बजट, अनुदान, व्यय आदि की स्वीकृति से कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है।
संसदीय समितियाँ: स्थायी समिति, लोक लेखा समिति आदि जांच करती हैं।
प्रश्न-राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- राजनीतिक प्रतिनिधित्व वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था में भाग लेती है। ये प्रतिनिधि संसद, विधानसभा, पंचायत आदि में जाकर जनता के हितों की अभिव्यक्ति करते हैं।
मुख्य बिंदु:
लोकतंत्र का मूल आधार: यह नागरिकों की भागीदारी का साधन है।
विधायिका में भागीदारी: प्रतिनिधि कानून निर्माण में भाग लेते हैं।
उत्तरदायित्व: प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
अधिकारों की सुरक्षा: प्रतिनिधि जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
नीति निर्माण में भागीदारी: जनता की इच्छाओं के अनुसार नीतियाँ बनाई जाती हैं।
Section-C
प्रश्न-1.संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण पर डेविड ईस्टन के विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
उत्तर:- डेविड ईस्टन एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने राजनीति के विश्लेषण के लिए “प्रणाली सिद्धांत” और “संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण” (Structural Functional Analysis) को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान में समाहित करते हुए यह प्रयास किया कि राजनीतिक व्यवस्था को एक “प्रणाली” के रूप में समझा जाए।
डेविड ईस्टन के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण के प्रमुख तत्व:
- राजनीति एक प्रणाली है: ईस्टन के अनुसार राजनीति एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें समाज से मांगें और समर्थन (inputs) आते हैं और सरकार नीतियों (outputs) के रूप में प्रतिक्रिया देती है।
- प्रतिक्रिया चक्र (Feedback Loop): यदि नीतियां समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप होती हैं तो समर्थन बढ़ता है, अन्यथा असंतोष उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है।
- पर्यावरण से अंतःक्रिया: राजनीतिक प्रणाली अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश के साथ सतत अंतःक्रिया करती है।
- प्रकार्यात्मक संस्थाएं: ईस्टन ने सत्ता, नीति-निर्माण, नियंत्रण, मत-संग्रह आदि कार्यों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्पन्न होते हुए दिखाया।
आलोचनात्मक विश्लेषण:
- अत्यधिक अमूर्तता: ईस्टन की प्रणाली अत्यधिक अमूर्त और जटिल है। यह व्यवहारिक वास्तविकताओं को पकड़ने में असमर्थ रहती है।
- सत्ता और संघर्ष की अनदेखी: संरचनात्मक प्रकार्यवाद सत्ता संघर्ष, वर्ग विभाजन और विरोधी समूहों की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं देता।
- विकासशील देशों पर लागू नहीं: यह मॉडल मुख्यतः पश्चिमी लोकतंत्रों पर केंद्रित है। इसे विकासशील देशों की जटिल संरचनाओं पर लागू करना कठिन है।
- परिवर्तन की उपेक्षा: ईस्टन की प्रणाली स्थायित्व और संतुलन पर आधारित है, जबकि राजनीतिक परिवर्तन और असंतुलन को समुचित स्थान नहीं दिया गया।
डेविड ईस्टन का योगदान राजनीतिक विश्लेषण की पद्धति को एक वैज्ञानिक और प्रणालीगत दिशा में ले जाने का रहा है, किंतु उसकी सीमाओं के कारण इसके व्यावहारिक उपयोग में कई अड़चनें हैं।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम का परीक्षण कीजिए।
उत्तर:- संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम (Structural-Functional Approach) तुलनात्मक राजनीति में एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक पद्धति है, जिसे विशेष रूप से गैब्रिएल आल्मंड (Gabriel Almond) और सिडनी वर्बा (Sidney Verba) द्वारा विकसित किया गया। यह उपागम राजनीति की तुलना करते समय विभिन्न संरचनाओं (जैसे – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल आदि) और उनके प्रकार्यों (जैसे – नीति निर्माण, सामाजिकीकरण, संचार, हित अभिव्यक्ति आदि) के परस्पर संबंधों का विश्लेषण करता है।
इस उपागम का मूल उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलनात्मक समझ विकसित करना है, जिससे विभिन्न समाजों में राजनीतिक क्रियाओं को एक समान रूप से देखा जा सके।
मुख्य विशेषताएँ –
- प्रत्येक प्रणाली में संरचनाएँ होती हैं – यह मानता है कि हर राजनीतिक प्रणाली में विभिन्न संरचनाएं होती हैं जो विशिष्ट प्रकार्य (Function) करती हैं।
- सर्वव्यापकता का सिद्धांत – यह उपागम यह मानता है कि सभी समाजों में कुछ सामान्य प्रकार्य मौजूद होते हैं, भले ही उन्हें अंजाम देने वाली संरचनाएँ अलग-अलग हों।
- बहुल प्रकार्यात्मकता – एक ही संरचना एक से अधिक प्रकार्य कर सकती है और एक ही प्रकार्य को अनेक संरचनाएँ निभा सकती हैं।
- प्रकार्यात्मक आवश्यकताएँ – राजनीतिक प्रणाली के अस्तित्व और स्थिरता के लिए कुछ बुनियादी प्रकार्य आवश्यक होते हैं जैसे सामाजिकीकरण, निर्णय निर्माण, हित समाकलन आदि।
महत्व –
यह उपागम पश्चिमी और गैर-पश्चिमी दोनों प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन संभव बनाता है।
इससे राजनीतिक प्रक्रियाओं को अधिक वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है।
यह परंपरागत और आधुनिक व्यवस्थाओं के बीच समानताओं और अंतरों को स्पष्ट करता है।
आलोचना –
कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अत्यधिक अमूर्त (abstract) और जटिल है।
यह पश्चिमी राजनीतिक अवधारणाओं पर अधिक आधारित है, जिससे गैर-पश्चिमी व्यवस्थाओं की विशिष्टताएँ उपेक्षित रह जाती हैं।
इसमें संरचना और प्रकार्य के बीच स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना कठिन है।
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में उपयोगी उपकरण है, जो राजनीतिक संरचनाओं और उनके प्रकार्यों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। यह राजनीति को केवल संस्थाओं तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उनके क्रियाकलापों का विश्लेषण भी करता है।
प्रश्न-तुलनात्मक राजनीति में तुलना के आधारों का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- तुलनात्मक राजनीति (Comparative Politics) राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों की तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित होती है। इस अध्ययन का उद्देश्य है विभिन्न शासन प्रणालियों की कार्यप्रणाली को समझना, उनके बीच समानता-असमानता को पहचानना और राजनीतिक सिद्धांतों का विकास करना।
तुलना के प्रमुख आधार –
- संविधानात्मक आधार:
विभिन्न देशों के संविधान, उनकी संरचना, मौलिक अधिकार, शक्ति विभाजन आदि की तुलना की जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि कौन-सा संवैधानिक ढाँचा कितना सफल है। - संस्थागत आधार:
राजनीतिक संस्थाएँ जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और ब्यूरोक्रेसी की संरचना और कार्यप्रणाली की तुलना की जाती है। - सांस्कृतिक आधार:
राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण और नागरिक सहभागिता जैसे पहलुओं के आधार पर तुलना की जाती है। इससे समाज की राजनीतिक चेतना को समझा जाता है। - आर्थिक-सामाजिक आधार:
विकास का स्तर, औद्योगीकरण, सामाजिक संरचना, जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर भी तुलनात्मक अध्ययन होता है। - ऐतिहासिक आधार:
राजनीतिक संस्थाओं और व्यवहारों के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तुलना से यह समझा जा सकता है कि राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुए। - आदर्शात्मक आधार:
लोकतंत्र बनाम तानाशाही, संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक प्रणाली जैसे आदर्श आधारित तुलना से राजनीतिक सिद्धांतों का विकास होता है।
मूल्यांकन –
तुलनात्मक राजनीति में तुलना के यह आधार राजनीतिक विश्लेषण को गहराई देते हैं। यह समझने में सहायक होते हैं कि कोई भी राजनीतिक प्रणाली क्यों सफल या विफल होती है। परंतु कई बार सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं के कारण निष्कर्ष पूरी तरह समान नहीं होते। इसके अलावा तुलनात्मक अध्ययन में मूल्य-निरपेक्षता बनाए रखना कठिन होता है।
तुलनात्मक राजनीति में विविध आधारों पर तुलना करना राजनीतिक समझ को समृद्ध करता है। यह सरकारों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं के कामकाज की व्याख्या करता है। लेकिन इन आधारों को अपनाते समय क्षेत्रीय और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है ताकि तुलनात्मक अध्ययन निष्पक्ष और वैज्ञानिक बन सके।
प्रश्न-तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर:- तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है जो विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों की तुलना के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांतों को समझने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं को तुलनात्मक ढंग से विश्लेषित करना है।
प्रकृति:
- वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति: तुलनात्मक राजनीति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाती है और राजनीतिक संरचनाओं व क्रियाओं का तथ्यात्मक अध्ययन करती है।
- व्यवहारवादी दृष्टिकोण: परंपरागत दृष्टिकोण की अपेक्षा अब नागरिकों के व्यवहार, चुनावी प्रवृत्तियों, राजनीतिक संस्कृति आदि का अध्ययन किया जाता है।
- अंतर-विषयक स्वभाव: इसका संबंध समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों से होता है।
- तुलनात्मक पद्धति: विभिन्न देशों की नीतियों व प्रणालियों की तुलना कर समरूपता एवं अंतर को उजागर किया जाता है।
क्षेत्र:
- सरकारी संस्थाएँ: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही आदि की तुलना।
- राजनीतिक प्रक्रियाएँ: राजनीतिक दल, चुनाव प्रणाली, हित समूह, जनमत आदि का अध्ययन।
- राजनीतिक संस्कृति एवं सामाजिक ढाँचा: राजनीतिक समाजीकरण, सांस्कृतिक अंतर, सामाजिक गतिशीलता आदि का विश्लेषण।
- विकासशील बनाम विकसित राष्ट्रों का तुलनात्मक अध्ययन।
आलोचनात्मक परीक्षण:
तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है, लेकिन कुछ समस्याएँ भी हैं:
देशों की भिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व आर्थिक स्थितियाँ तुलना को जटिल बनाती हैं।
पूर्णतः तटस्थ व वस्तुनिष्ठ तुलना कठिन है।
व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने यद्यपि अनुसंधान को सशक्त किया है, लेकिन इससे मूल राजनीतिक चिंतन उपेक्षित हुआ है।
तुलनात्मक राजनीति आधुनिक युग में राजनीतिक अध्ययन का आधार बन गई है, जो राजनीतिक विश्लेषण को अधिक व्यापक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक बनाती है, यद्यपि इसमें कई व्यावहारिक सीमाएँ भी हैं।
प्रश्न-व्यवस्थापिका से संबंधित आधुनिक विवाद को विवेचना कीजिए।
उत्तर:- विधायिका या व्यवस्थापिका (Legislature) किसी भी लोकतांत्रिक शासन का केंद्रीय अंग है, जो कानून निर्माण, नीति निर्धारण और सरकार पर नियंत्रण का कार्य करती है। परंतु आधुनिक काल में विधायिका से संबंधित अनेक विवाद सामने आए हैं, जो इसके प्रभावशीलता और भूमिका को चुनौती देते हैं।
मुख्य आधुनिक विवाद –
- कार्यपालिका का प्रभुत्व – कई देशों में कार्यपालिका विधायिका पर हावी होती जा रही है। कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों का अति प्रयोग इसका उदाहरण है।
- दलबदल और अनुशासन – पार्टी प्रणाली के कारण विधायकों की स्वतंत्रता सीमित हो गई है। दल का अनुशासन विधायिका की स्वायत्तता को प्रभावित करता है।
- संसदीय कार्य की गिरती गुणवत्ता – बहस का स्तर घटा है, प्रश्नकाल और शून्यकाल के माध्यम से प्रभावी संवाद कम होता जा रहा है।
- भ्रष्टाचार और अपराधीकरण – विधायिका में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ी है, जिससे उसकी गरिमा पर प्रश्न उठते हैं।
- जनहित की उपेक्षा – कई बार विधायिका जनभावनाओं की उपेक्षा कर राजनीतिक दलों के एजेंडे को प्राथमिकता देती है।
- बिलों का अल्पचर्चित पारित होना – कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना पर्याप्त बहस के पारित हो जाते हैं, जिससे विधायिका की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठते हैं।
- मीडिया और न्यायपालिका का हस्तक्षेप – कभी-कभी विधायिका के कार्यों में अन्य अंगों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, जिससे शक्तियों का संतुलन बिगड़ता है।
आधुनिक युग में व्यवस्थापिका अनेक चुनौतियों से जूझ रही है। इसके लिए आवश्यक है कि इसकी गरिमा, स्वायत्तता और कार्यक्षमता को पुनर्स्थापित किया जाए, ताकि लोकतांत्रिक शासन की आत्मा सुरक्षित रह सके
प्रश्न-गैर-पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- गैर-पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाएं उन देशों की राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को दर्शाती हैं, जो यूरोपीय या अमेरिकी लोकतांत्रिक परंपराओं से अलग हैं। इनमें अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन अमेरिकी तथा मध्य-पूर्वी देशों की व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। इनका विकास औपनिवेशिक अनुभवों, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक मूल्यों, परंपराओं एवं सामाजिक संरचनाओं के आधार पर हुआ है।
गैर-पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- औपनिवेशिक प्रभाव: अधिकांश गैर-पश्चिमी देश कभी न कभी उपनिवेश रहे हैं, जिससे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया पर पश्चिमी देशों का गहरा प्रभाव पड़ा है।
- सामाजिक-धार्मिक विविधता: इन देशों में जाति, धर्म, भाषा एवं समुदायों की बहुलता पाई जाती है, जो राजनीतिक निर्णयों और नीतियों को प्रभावित करती है।
- परंपरागत संस्थाओं का महत्व: गांव पंचायत, जनजातीय परिषद, धार्मिक नेता आदि आज भी कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह व्यवस्था पश्चिमी लोकतंत्र की तुलना में अधिक सामुदायिक और परंपरावादी होती है।
- केंद्रित सत्ता संरचना: अनेक गैर-पश्चिमी देशों में शक्ति का केंद्रीकरण देखने को मिलता है, जैसे एकदलीय व्यवस्था, सैनिक शासन या अधिनायकवादी नेतृत्व।
- लोकतंत्र का संक्रमण काल: बहुत से देशों में लोकतांत्रिक संस्थाएं अभी भी विकासशील अवस्था में हैं। चुनाव तो होते हैं, परन्तु संस्थागत पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी रहती है।
- नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्य: इन देशों में राजनीति को अक्सर धर्म और संस्कृति से जोड़ा जाता है, जिससे वैचारिक दृष्टिकोण पश्चिमी लोकतंत्र से भिन्न होता है।
- आर्थिक पिछड़ापन और अशिक्षा: निर्धनता और कम साक्षरता के कारण जनता राजनीतिक रूप से पूर्णत: जागरूक नहीं हो पाती, जिससे लोक सहभागिता सीमित रहती है।
गैर-पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुआयामी हैं जो अपने-अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के आधार पर कार्य करती हैं। इनके विश्लेषण के लिए केवल पश्चिमी मॉडल पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि स्थानीय संदर्भों को भी समाहित करना आवश्यक है।
प्रश्न-अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली (Presidential Form of Government) वह शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधायिका से पूर्णतः पृथक होती है और राष्ट्राध्यक्ष (अध्यक्ष या राष्ट्रपति) कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। इस प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है, जहाँ राष्ट्रपति शासन का प्रमुख होता है और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ:
यह शासन प्रणाली एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट पृथक्करण होता है। कार्यपालिका (राष्ट्रपति और उसके मंत्री) जनता के प्रति नहीं बल्कि संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान संसद से प्रभावित हुए बिना कार्य करता है।
प्रमुख विशेषताएँ –
- सत्ता का पृथक्करण:
इस प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट सीमा रेखा होती है। सभी अंग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। - राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव:
राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। जैसे अमेरिका में यह कार्यकाल चार वर्षों का होता है। - स्थिर कार्यपालिका:
राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, इसलिए सरकार में स्थायित्व बना रहता है। - एकल नेतृत्व:
राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का एकमात्र प्रमुख होता है, जिससे निर्णय लेने में तेजी और स्पष्टता आती है। - विधायिका से स्वतंत्रता:
राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसलिए कार्यपालिका पर संसद का सीधा नियंत्रण नहीं होता। - उत्तरदायित्व का अभाव:
इस प्रणाली में राष्ट्रपति और उनके सहयोगी विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते, जिससे कभी-कभी सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली निर्णय लेने में तीव्र, स्थिर और केंद्रित होती है, परंतु इसमें कार्यपालिका के निरंकुश हो जाने का खतरा भी बना रहता है। यह प्रणाली उन देशों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जहाँ शक्तिशाली और स्थायी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली (checks and balances) आवश्यक होती है।
प्रश्न-अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन प्रणालियों में अन्तर की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन प्रणालियाँ लोकतांत्रिक शासन की दो प्रमुख प्रणालियाँ हैं जिनमें कार्यपालिका की संरचना, सत्ता विभाजन, उत्तरदायित्व आदि के आधार पर अनेक अंतर पाए जाते हैं।
अध्यक्षीय शासन प्रणाली (Presidential System):
राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है और प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है।
राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और विधायिका से पृथक होता है।
अमेरिका इसका प्रमुख उदाहरण है।
संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System):
कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो संसद के बहुमत दल का नेता होता है।
कार्यपालिका विधायिका से जन्म लेती है और उसी को उत्तरदायी होती है।
भारत, ब्रिटेन जैसे देशों में यह प्रणाली प्रचलित है।
मुख्य अंतर:
पक्ष अध्यक्षीय प्रणाली संसदीय प्रणाली
कार्यपालिका विधायिका से पृथक विधायिका में समाहित
प्रमुख का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा संसद द्वारा निर्वाचित
कार्यकाल निश्चित संसद में बहुमत पर निर्भर
उत्तरदायित्व राष्ट्रपति सीधे संसद को उत्तरदायी नहीं प्रधानमंत्री संसद को उत्तरदायी
सत्ता पृथक्करण कठोर लचीला
स्थायित्व उच्च कम, गठबंधन सरकारें टूट सकती हैं
आलोचना:
अध्यक्षीय प्रणाली में सत्ता के केंद्रीकरण का खतरा होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन की मजबूरी।
संसदीय प्रणाली अधिक उत्तरदायी मानी जाती है, परंतु निर्णय प्रक्रिया धीमी होती है।
अध्यक्षीय प्रणाली में नेतृत्व सशक्त होता है, परंतु सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है।
दोनों प्रणालियों की अपनी-अपनी विशेषताएँ और कमियाँ हैं। किसी भी देश की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त प्रणाली का चुनाव किया जाना चाहिए।
प्रश्न-लोकतंत्र की संवैधानिक शर्तों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- लोकतंत्र (Democracy) केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह संविधानिक मूल्यों, नियमों और संस्थाओं पर आधारित शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए कुछ संवैधानिक शर्तों का होना आवश्यक है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं और सत्ता का संतुलन बनाए रखती हैं।
लोकतंत्र की प्रमुख संवैधानिक शर्तें –
- संविधान का अस्तित्व – लोकतंत्र में एक लिखित या अलिखित संविधान होना चाहिए, जो सरकार की सीमाओं, नागरिकों के अधिकारों और शासन प्रणाली को परिभाषित करता हो।
- मौलिक अधिकारों की गारंटी – नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म, समानता और निजी स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी मिलनी चाहिए।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता – एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक है, जो कानून के शासन को सुनिश्चित करती है और सरकार के कार्यों की समीक्षा कर सकती है।
- नियंत्रित कार्यपालिका – कार्यपालिका को सीमित और उत्तरदायी होना चाहिए। उसे विधायिका और न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए।
- नियमित चुनाव – लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है, जिससे सत्ता में परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से हो सके।
- संविधानिकता का पालन – शासन की सभी गतिविधियाँ संविधान के दायरे में रहकर होनी चाहिए।
- संघीय या एकात्मक संरचना – सरकार की शक्ति का वितरण स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों/प्रांतों के बीच होना चाहिए।
महत्व –
ये शर्तें नागरिकों को सत्ता के दुरुपयोग से बचाती हैं।
ये शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती हैं।
लोकतंत्र को केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहने देतीं, बल्कि एक संवैधानिक संस्कृति की स्थापना करती हैं।
लोकतंत्र की संवैधानिक शर्तें एक स्वस्थ, उत्तरदायी और जवाबदेह शासन प्रणाली की नींव होती हैं। इन शर्तों की अनुपस्थिति में लोकतंत्र केवल नाममात्र रह जाता है।
प्रश्न-राजनीतिक समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक समाजीकरण की विभिन्न एजेन्सियों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को सीखता है। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है, जो व्यक्ति को एक ‘राजनीतिक प्राणी’ बनाती है।
राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख उद्देश्य:
राजनीतिक संस्कृति का हस्तांतरण
राजनीतिक व्यवहार का निर्माण
नागरिकों में राजनीतिक चेतना और भागीदारी की भावना का विकास
राजनीतिक समाजीकरण की प्रमुख एजेंसियाँ (संस्थान):
- परिवार: यह प्राथमिक संस्था है जहाँ बच्चे राजनीतिक भाषा, विचारधारा और राजनीतिक झुकाव ग्रहण करते हैं। माता-पिता का दृष्टिकोण बच्चों पर प्रभाव डालता है।
- शिक्षा प्रणाली: विद्यालयों के पाठ्यक्रम, शिक्षक, सह-पाठ्य गतिविधियाँ, नागरिक शास्त्र की शिक्षा आदि राजनीतिक विचारों का विकास करती हैं।
- सहकर्मी समूह: मित्रों और साथियों का व्यवहार राजनीतिक झुकाव को प्रभावित करता है, विशेषकर किशोरावस्था में।
- मीडिया: टेलीविजन, समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि आधुनिक युग की सबसे प्रभावशाली एजेंसी है जो व्यापक राजनीतिक जानकारी प्रदान करती है।
- राजनीतिक दल: दल विचारधारा, प्रचार, आंदोलन आदि के माध्यम से नागरिकों का राजनीतिकीकरण करते हैं।
- धार्मिक संस्थाएँ: कई बार धार्मिक नेता या संस्थान भी राजनीतिक मत-निर्माण में भूमिका निभाते हैं।
- सरकारी संस्थाएँ: सरकार की नीतियाँ, चुनाव आयोग, न्यायपालिका आदि संस्थाएँ नागरिकों को कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अवगत कराती हैं।
राजनीतिक समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है, जो समाज के हर सदस्य को प्रभावित करती है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि नागरिक राजनीतिक रूप से जागरूक और उत्तरदायी बनें।
प्रश्न-आधुनिकीकरण पर हंटिंगटन के विचारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- सैमुअल पी. हंटिंगटन (Samuel P. Huntington) एक प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आधुनिकीकरण (Modernization) की प्रक्रिया को सत्ता, स्थायित्व और संस्थागत विकास के संदर्भ में समझाया। उनकी पुस्तक “Political Order in Changing Societies” (1968) इस विषय पर प्रमुख मानी जाती है।
हंटिंगटन के अनुसार आधुनिकीकरण –
केवल आर्थिक विकास या औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक संस्थाओं के विकास से जुड़ी प्रक्रिया है।
वह मानते हैं कि तेजी से हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन यदि राजनीतिक संस्थाओं के विकास से मेल नहीं खाते, तो अस्थिरता और असंतोष उत्पन्न होता है।
मुख्य बिंदु –
- राजनीतिक संस्थाओं का विकास – हंटिंगटन के अनुसार आधुनिकीकरण की सफलता के लिए मजबूत राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है, जैसे – पार्टियाँ, नौकरशाही, न्यायपालिका आदि।
- राजनीतिक स्थिरता बनाम भागीदारी – यदि जनसंख्या में राजनीतिक भागीदारी तेजी से बढ़ती है लेकिन संस्थागत ढांचे कमजोर होते हैं, तो यह अस्थिरता को जन्म देता है।
- राजनीतिक संस्थाकरण (Institutionalization) – यह प्रक्रिया संस्थाओं को स्थायी, प्रभावी और वैध बनाती है। यह आधुनिकीकरण की आधारशिला है।
- पारंपरिक बनाम आधुनिक संरचना – हंटिंगटन ने यह भी समझाया कि परंपरागत संरचनाएं अगर समय के साथ आधुनिक नहीं बनतीं तो सामाजिक तनाव पैदा होता है।
महत्त्व –
हंटिंगटन ने आधुनिकीकरण को एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में देखा जिसमें केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि राजनीतिक स्थायित्व भी अनिवार्य है।
उनका दृष्टिकोण विकासशील देशों में राजनीतिक अस्थिरता को समझने में सहायक सिद्ध हुआ।
आलोचना –
कुछ विद्वानों ने उनके विचारों को पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं पर अधिक आधारित माना।
वह जन आंदोलन और असहमति को अस्थिरता के रूप में देखते हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक आलोच्य बिंदु है।
हंटिंगटन का आधुनिकीकरण संबंधी दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं और स्थायित्व की आवश्यकता पर बल देता है। उनके विचार आज भी विकासशील देशों की राजनीतिक समस्याओं को समझने में सहायक हैं।
प्रश्न-भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए।
उत्तर:- न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यह निर्धारित करते हैं कि संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। यदि कोई कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है।
न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, शून्य और अमान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 32, 131-136 और 226 के तहत न्यायालयों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
प्रमुख विशेषताएँ –
- संवैधानिक सर्वोच्चता की रक्षा:
न्यायिक पुनरावलोकन संविधान को सर्वोच्च बनाता है और विधायिका या कार्यपालिका को उसकी सीमाओं में रहने हेतु बाध्य करता है। - मौलिक अधिकारों की सुरक्षा:
यदि कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। - लोकतंत्र की रक्षा:
यह प्रक्रिया विधायिका की निरंकुशता को नियंत्रित करती है और लोकतंत्र को स्थायित्व देती है।
आलोचनात्मक पक्ष –
- लोकतांत्रिक इच्छा का विरोध:
कभी-कभी न्यायपालिका जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों को निरस्त कर देती है, जिससे लोकतंत्र की भावना पर आघात होता है। - न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism):
हाल के वर्षों में न्यायालय कई बार नीति-निर्माण की भूमिका में आ गए हैं, जिससे शक्ति का असंतुलन उत्पन्न हुआ है। - न्यायिक सर्वोच्चता का खतरा:
न्यायिक पुनरावलोकन की आड़ में कभी-कभी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती है, जो संविधान की भावना के विपरीत है।
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन एक आवश्यक संवैधानिक तंत्र है जो कानूनों को संविधान के अनुरूप बनाए रखने में सहायक है। हालांकि, इसका संतुलित प्रयोग ही न्यायपालिका की विश्वसनीयता और लोकतंत्र की मजबूती के लिए उपयुक्त है।
प्रश्न-अध्यात्मक शासन प्रणाली का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- अध्यात्मक शासन प्रणाली (Presidential Form of Government) वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका अलग-अलग होती हैं और राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) सरकार का प्रमुख होता है। यह प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है।
अर्थ:
यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है और वह शासन का प्रमुख होता है। वह विधायिका से स्वतंत्र होता है और उसे हटाना सरल नहीं होता।
प्रमुख विशेषताएँ:
- शक्ति पृथक्करण: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है जबकि संसद कानून निर्माण का कार्य करती है।
- स्थिर कार्यपालिका: राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। वह संसद के विश्वास मत से नहीं हटाया जा सकता, जिससे सरकार स्थायित्व बनाए रखती है।
- प्रत्यक्ष निर्वाचन: राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, जिससे उसे जनमत का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त होता है।
- कार्यपालिका की एकता: राष्ट्रपति ही कार्यपालिका प्रमुख होता है और वह अपने मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है, जो उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि संसद के प्रति।
- संसद को भंग करने का अधिकार नहीं: राष्ट्रपति को संसद को भंग करने का अधिकार नहीं होता और संसद भी राष्ट्रपति को सामान्य परिस्थिति में पद से नहीं हटा सकती।
- संविधान का सर्वोच्चता सिद्धांत: राष्ट्रपति प्रणाली में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, और सभी संस्थाएँ उसके अधीन कार्य करती हैं।
राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका अधिक सशक्त होती है और सरकार अधिक स्थिर होती है। परन्तु यदि अध्यक्ष अधिनायकवादी प्रवृत्ति वाला हो, तो तानाशाही के आसार भी बन सकते हैं। अतः इस प्रणाली में संतुलन और उत्तरदायित्व बनाए रखना आवश्यक है।
प्रश्न-संविधानवाद को मुख्य आवश्यकताओं का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:- संविधानवाद (Constitutionalism) वह सिद्धांत है जिसमें राज्य की शक्ति को एक संविधान के माध्यम से सीमित किया जाता है ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह केवल संविधान के अस्तित्व को नहीं, बल्कि उसके प्रभावी कार्यान्वयन को भी महत्व देता है।
संविधानवाद की मुख्य आवश्यकताएँ:
- लिखित संविधान: एक स्पष्ट व लिखित संविधान आवश्यक है जो शासन की रूपरेखा, नागरिक अधिकारों और संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करे।
- कानून का शासन (Rule of Law): संविधानवाद में सभी नागरिक और शासक समान रूप से कानून के अधीन होते हैं।
- न्यायिक स्वतंत्रता: एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है जो संविधान की व्याख्या कर सके और सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रख सके।
- मूल अधिकारों की सुरक्षा: नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित किया जाना संविधानवाद की आधारशिला है।
- सत्ता का विभाजन: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन और नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है।
- लोकतांत्रिक शासन प्रणाली: जनता की भागीदारी और उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार संविधानवाद के मूल में है।
आलोचनात्मक मूल्यांकन:
कुछ देशों में संविधान होते हुए भी संविधानवाद की भावना अनुपस्थित रहती है क्योंकि व्यावहारिक क्रियान्वयन नहीं होता।
निरंकुश सरकारें संविधान की भावना का दुरुपयोग कर सकती हैं।
संविधानवाद की सफलता की पूर्व शर्त है—जनता में संवैधानिक चेतना और राजनीतिक साक्षरता।
केवल कानूनी उपायों से संविधानवाद को स्थापित नहीं किया जा सकता, इसके लिए संस्थागत और नैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक है।
संविधानवाद लोकतंत्र की आत्मा है जो सत्ता के अनुशासन, अधिकारों की रक्षा और कानून के शासन को सुनिश्चित करता है, लेकिन इसकी सफलता के लिए सशक्त संस्थाएँ और सजग नागरिक समाज आवश्यक हैं।
प्रश्न-अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए।
उत्तर:- न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय यह निर्णय करता है कि विधायिका या कार्यपालिका द्वारा पारित कोई कानून या निर्णय संविधान के अनुरूप है या नहीं। अमेरिका इस सिद्धांत का जन्मदाता है।
अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत:
1803 के Marbury v. Madison केस में मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने पहली बार इसकी व्याख्या की।
सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सके।
विशेषताएँ:
- संविधान सर्वोच्च: अमेरिकी संविधान को सर्वोच्च कानून माना गया है।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पूर्णतः स्वतंत्र है, जो न्यायिक पुनरावलोकन को निष्पक्ष रूप से लागू करता है।
- संवैधानिक संतुलन: यह विधायिका और कार्यपालिका की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का माध्यम है।
आलोचनात्मक मूल्यांकन:
यह सिद्धांत न्यायपालिका को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे ‘न्यायिक सर्वोच्चता’ (Judicial Supremacy) का खतरा उत्पन्न होता है।
यह लोकतांत्रिक सिद्धांत की भावना को चुनौती दे सकता है, क्योंकि न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते।
कई बार न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए किया गया है।
किंतु यह नागरिक अधिकारों की रक्षा में सहायक सिद्ध हुआ है, जैसे कि नस्लीय भेदभाव, धार्मिक स्वतंत्रता आदि से संबंधित मामलों में।
अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र के संतुलन और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रभावशाली माध्यम बना है, लेकिन इसका दुरुपयोग या अति-व्यापकता लोकतांत्रिक संरचना के लिए चुनौती बन सकता है। अतः इसका विवेकपूर्ण एवं संतुलित प्रयोग आवश्यक है।
vmou so-02 paper , vmou ba 2nd year exam paper , vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4
VMOU EXAM PAPER