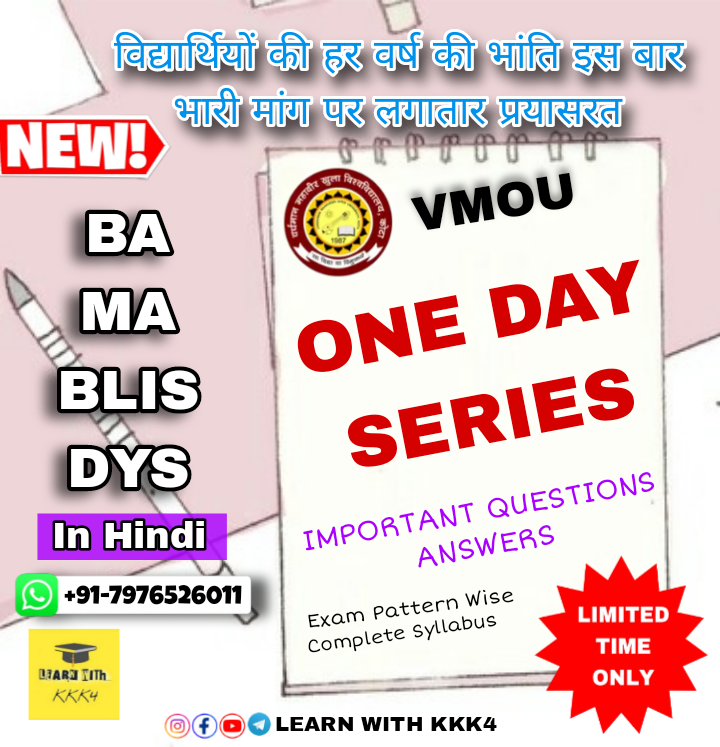VMOU MASO-01 Paper MA 1st Year (Semester-I & II) ; vmou Sociology exam paper
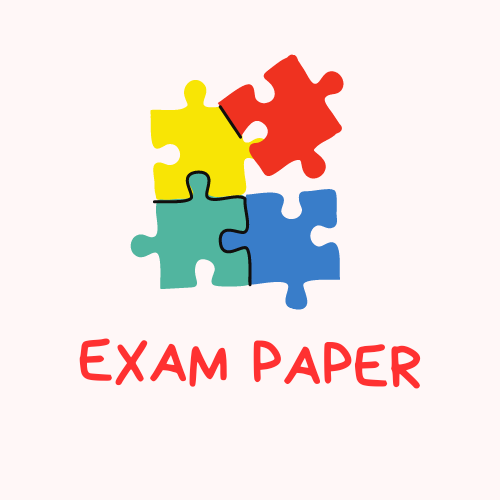
VMOU MA Pervious Year के लिए समाजशास्त्र ( MASO-01 , ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.समाजशास्त्र के जनक के रूप में किस विद्वान को जाना जाता है?
उत्तर:- अगस्ट कॉन्ते
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.’इथिक्स’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- अरस्तू (Aristotle)
प्रश्न-3.सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए
उत्तर:- सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न घटकों के बीच स्थापित नियमबद्ध संबंधों का संगठन होता है।
प्रश्न-4. सामाजिक व्यवस्था की कोई दो विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:- सामाजिक व्यवस्था संगठित होती है और यह आपसी सहयोग पर आधारित होती है।
प्रश्न-5. आत्म दर्पण का सिद्धांत किसने दिया है?
उत्तर:- चार्ल्स हॉर्टन कूली ने
प्रश्न-6. समिति से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर:-समिति एक संगठित सामाजिक समूह है जो विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है।
प्रश्न-7. द्वितीयक समूह के कोई दो उदाहरण बताइए।
उत्तर:- विद्यालय और कार्यालय द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं।
प्रश्न-8. समूह की परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- समूह वह सामाजिक इकाई है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक क्रिया में संलग्न होते हैं।
प्रश्न-9. भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है?
उत्तर:- भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रारंभ 1919 ई. से माना जाता है।
प्रश्न-10. ‘द थ्योरी ऑफ सोशल एण्ड इकोनोमिक अर्गनाइजेशन’ के लेखक का नाम बताइए।
उत्तर:- मैक्स वेबर
प्रश्न-11. स्व-अलगाव से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर:-स्व-अलगाव वह स्थिति है जब व्यक्ति स्वयं को अपने कार्य, समाज या आत्मा से अजनबी अनुभव करता है।
प्रश्न-12. संस्कृति को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- संस्कृति मानव जीवन से संबंधित मान्यताओं, रीति-रिवाजों, ज्ञान, कला, नैतिकता आदि का संपूर्ण स्वरूप है।
प्रश्न-13. द्वितीयक समूह को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- द्वितीयक समूह वह होता है जिसमें संबंध औपचारिक, अल्पकालिक और उद्देश्य आधारित होते हैं।
प्रश्न-14. प्रगति की दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- प्रगति की दो विशेषताएँ हैं— यह एक निरंतर प्रक्रिया है और यह मानव कल्याण की दिशा में होती है।
प्रश्न-15. चक्रीय सिद्धांत से सम्बंधित दो विद्वानों के नाम लिखिए।
उत्तर:- ऑसवाल्ड स्पेंग्लर और अर्नाल्ड टॉयनबी
प्रश्न-16. ‘द सोशल ऑर्डर’ पुस्तक के लेखक कौन है?
उत्तर:- रॉबर्ट निस्बेट
प्रश्न-17. अलगाव को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- जब व्यक्ति स्वयं, समाज या कार्य से आत्मीयता खो देता है, तो उसे अलगाव (Alienation) कहते हैं।
प्रश्न-18. समाज को निर्मित करने वाली दो आधारभूत प्रक्रियाएँ कौनसी हैं?
उत्तर:- समाज को निर्मित करने वाली दो आधारभूत प्रक्रियाएँ सहक्रिया (Interaction) और समाजीकरण (Socialization) हैं।
प्रश्न-19. ‘सिंडेश्मियन परिवार’ से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:-सिंडेश्मियन परिवार वह होता है जिसमें विवाह संबंध अस्थायी होते हैं और पति-पत्नी के बीच संबंध कमजोर होते हैं।
प्रश्न-20. ‘संस्कृति पर्यावरण का मानवनिर्मित भाग है’ यह परिभाषा किसने दी?
उत्तर:-हरशी कोविंग (Herskovits) ने दी
प्रश्न-21. ‘प्रकट’ एवं ‘अप्रकट प्रकार्य’ की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई?
उत्तर:-रॉबर्ट के. मर्टन (Robert K. Merton) द्वारा
प्रश्न-22. समनर द्वारा दिए गए समूह के वर्गीकरण लिखिए।
उत्तर:- इन-ग्रुप (In-group) और आउट-ग्रुप (Out-group)।
प्रश्न-23. रुक्षियों किसे कहते हैं?
उत्तर:- रुक्षियाँ (Mores) वे सामाजिक नियम हैं जिनका पालन अनिवार्य होता है और उल्लंघन पर समाज द्वारा दंड दिया जाता है।
प्रश्न-24. क्रांति की परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- क्रांति एक तीव्र एवं मौलिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो समाज की संरचना को पूरी तरह बदल देती है।
प्रश्न-25. संस्कृति के उपादानों के नाम लिखिए।
उत्तर:- भाषा, कला, मूल्य, मान्यता, रीति-रिवाज, तकनीक, परंपराएँ।
प्रश्न-26. सामाजिक व्यवस्था की दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- यह संरचित होती है।
यह परस्पर संबंधित घटकों से मिलकर बनती है।
प्रश्न-27. सामाजिक नियंत्रण के कोई दो उद्देश्य लिखिए।
उत्तर:- सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना।
सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना।
प्रश्न-28. ‘हम’ की भावना के आधार पर समूह का वर्गीकरण कीजिए।
उत्तर:- प्राथमिक समूह
द्वितीयक समूह
प्रश्न-29. समुदाय की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- भौगोलिक क्षेत्र में निवास।
साझा जीवन और भावना।
प्रश्न-30. प्रदत्त प्रस्थिति के निर्धारण के आधार लिखिए।
उत्तर:- जन्म जाति लिंग वंश
प्रश्न-31. चेतन नियंत्रण क्या है ?
उत्तर:-चेतन नियंत्रण वह सामाजिक नियंत्रण है जो व्यक्ति की चेतना, नैतिकता और आत्म-नियंत्रण के माध्यम से होता है।
प्रश्न-32. ‘सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर’ पुस्तक के लेखक कौन हैं ?
उत्तर:- रॉबर्ट के. मर्टन (Robert K. Merton)
प्रश्न-33. ‘आत्म-दर्पण का सिद्धान्त किसने दिया है?
उत्तर:- चार्ल्स हॉर्टन कूले
प्रश्न-34. सरल समाज क्या है?
उत्तर:- सरल समाज वह समाज होता है जिसमें वर्गभेद, जटिल संस्थाएँ और तकनीकी विकास कम होते हैं।
प्रश्न-35. जनरीतियाँ क्या हैं?
उत्तर:- जनरीतियाँ वे सामाजिक परंपराएँ और व्यवहार हैं जिन्हें समाज के सदस्य स्वाभाविक रूप से अपनाते हैं।
प्रश्न-36. सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- सामाजिक संरचना समाज में व्यक्तियों और संस्थाओं के आपसी संबंधों और व्यवस्थाओं का ढाँचा है
प्रश्न-37. समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन
उत्तर:- समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम 1838 ई. में फ्रांस में प्रारम्भ हुआ।
प्रश्न-38. ‘The Study of Sociology’ पुस्तक के लेखक
उत्तर:- हर्बर्ट स्पेंसर
प्रश्न-39. सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्य सिद्धांत के प्रतिपादक
उत्तर:- किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर (Kingsley Davis & Wilbert Moore)
प्रश्न-40. सामाजिक संरचना की चार विशेषताएँ
उत्तर:- यह संगठित सामाजिक संबंधों का ढाँचा होती है।
यह अपेक्षाकृत स्थायी होती है।
यह विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से मिलकर बनती है।
यह समाज में भूमिकाओं एवं प्रतिष्ठाओं को निर्धारित करती है।
Section-B
प्रश्न-1.प्राथमिक समूह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- प्राथमिक समूह वे सामाजिक समूह होते हैं जिनमें सदस्य भावनात्मक रूप से घनिष्ठ होते हैं और आपसी संबंध प्रत्यक्ष होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण परिवार है। समाजशास्त्री चार्ल्स एच. कूली ने ‘प्राथमिक समूह’ की संकल्पना दी। इसमें घनिष्ठता, आत्मीयता, सहयोग और सह-अस्तित्व की भावना होती है। यह समूह व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक समूहों में व्यक्ति का चरित्र, नैतिकता, विचार और व्यवहार का निर्माण होता है। ये समूह छोटे आकार के होते हैं और उनके संबंध दीर्घकालिक व आत्मीय होते हैं। मित्रमंडली, खेल टोली, और कार्य समूह भी कभी-कभी प्राथमिक समूह बन सकते हैं।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.प्रदत्त और अर्जित प्रस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- प्रदत्त प्रस्थिति (Ascribed Status) जन्म के साथ प्राप्त होती है, जैसे जाति, लिंग, धर्म, वंश। इसे व्यक्ति स्वयं नहीं चुनता।
अर्जित प्रस्थिति (Achieved Status) व्यक्ति के प्रयास, योग्यता और कार्यों पर आधारित होती है, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, नेता आदि।
आधार प्रदत्त प्रस्थिति अर्जित प्रस्थिति
प्राप्ति का आधार जन्म प्रयास
परिवर्तन की संभावना नहीं हाँ
उदाहरण जाति, लिंग इंजीनियर, खिलाड़ी
इस प्रकार, प्रदत्त प्रस्थिति जन्म से प्राप्त होती है, जबकि अर्जित प्रस्थिति मेहनत और योग्यता का परिणाम होती है
प्रश्न-3.नगरीय समुदाय की विशेषताओं का विवेचन कीजिए।
उत्तर:- नगरीय समुदाय आधुनिक समाज का महत्वपूर्ण रूप है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं:
निजी जीवन और एकाकीपन: व्यक्ति की निजीता अधिक होती है, किंतु सामाजिक अलगाव भी अधिक होता है।
नगरीय समुदाय औद्योगीकरण, आधुनिकता और प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है।
जनसंख्या का घनत्व: शहरों में अधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व होता है।
विविधता: नगरों में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग साथ रहते हैं।
औपचारिक संबंध: शहरी जीवन में व्यक्तिगत के बजाय व्यवसायिक और औपचारिक संबंध प्रमुख होते हैं।
आजीविका के विविध साधन: उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध होता है।
सामाजिक गतिशीलता: व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक स्थिति में शीघ्र परिवर्तन कर सकता है।
प्रश्न-4. प्राचीन भारत में सामाजिक अध्ययन की प्रकृति स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- प्राचीन भारत में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य समाज की संरचना, परंपराओं, मूल्यों और सामाजिक संस्थाओं की समझ प्रदान करना था। वेदों, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में सामाजिक जीवन के नियम, वर्ग-व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, विवाह के नियम, स्त्री-पुरुष संबंधों और सामाजिक उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन मिलता है। आश्रम व्यवस्था (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) सामाजिक जीवन का प्रमुख आधार था। वर्ण व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के माध्यम से समाज का विभाजन कार्य आधारित था, जो सामाजिक दायित्वों का निर्धारण करता था। धर्म और कर्तव्य को सामाजिक आचरण का मूल माना गया। कुल मिलाकर, प्राचीन भारत का सामाजिक अध्ययन धार्मिकता, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और सामूहिक हित पर केंद्रित था।
प्रश्न-5.”मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।” स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- मनुष्य को ‘सामाजिक प्राणी’ कहा जाता है क्योंकि उसका जीवन समाज के बिना अधूरा है। मनुष्य जन्म से ही दूसरों पर निर्भर रहता है — माता-पिता, परिवार, मित्र और समाज पर। वह भाषा, संस्कृति, मूल्यों और आचरण को समाज से ही सीखता है। अरस्तु ने कहा था कि “जो व्यक्ति समाज में न रह सके, वह या तो देवता है या पशु।” मनुष्य के विकास, सुरक्षा और व्यक्तित्व निर्माण के लिए सामाजिक संबंध आवश्यक हैं। समाज में रहकर ही वह अपने कर्तव्यों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझता है। सहयोग, सामंजस्य, अनुशासन और प्रेम जैसे गुण सामाजिक परिवेश में ही विकसित होते हैं। अतः मनुष्य स्वभावतः समाज में रहने वाला प्राणी है, और उसके अस्तित्व की पूर्णता समाज में ही संभव है।
प्रश्न-6.कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए समाज के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- कार्ल मार्क्स ने समाज का वर्गीकरण आर्थिक संरचना के आधार पर किया। उन्होंने दो मुख्य वर्ग बताए:
- बुर्जुआ वर्ग (Bourgeoisie): यह वह वर्ग है जिसके पास उत्पादन के साधन जैसे – कारखाने, भूमि, पूंजी होती है।
- प्रोलितारिय वर्ग (Proletariat): यह श्रमिक वर्ग होता है जो अपनी श्रमशक्ति बेचता है।
मार्क्स के अनुसार, इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। पूँजीवादी व्यवस्था में बुर्जुआ वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है। उन्होंने माना कि यह संघर्ष अंततः सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा जिससे वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। उनका वर्गीकरण समाज में असमानता, शोषण और संघर्ष को समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
प्रश्न-7.प्रगति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- प्रगति (Progress) का अर्थ है समाज का सतत सकारात्मक विकास। यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सुधार और उन्नति को दर्शाती है। प्रगति वह प्रक्रिया है जिससे मानव जीवन में सुविधाएं, न्याय, समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से, प्रगति का आशय सामाजिक संरचना और मूल्यों में गुणात्मक परिवर्तन से है। यह एक दिशा विशेष में होती है — जैसे शिक्षा का प्रसार, तकनीकी विकास, महिला सशक्तिकरण आदि। हालाँकि कुछ विचारकों ने प्रगति की आलोचना भी की है कि यह केवल भौतिक उन्नति तक सीमित न हो, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए।
प्रश्न-8.आदर्शात्मक संस्कृति पर एक लघु टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:- आदर्शात्मक संस्कृति (Ideal Culture) वह संस्कृति है, जिसे समाज उच्च मानदंड और मूल्य मानता है। यह वह सांस्कृतिक रूप है, जिसे लोग मानने योग्य और अनुसरणीय मानते हैं। इसमें समाज की नैतिकता, आदर्श व्यवहार, धर्म, आचार-संहिता, तथा अपेक्षित सामाजिक भूमिका शामिल होती है। यह संस्कृति एक आदर्श स्थिति को दर्शाती है, जबकि वास्तविक संस्कृति (Real Culture) में व्यवहार भिन्न हो सकता है। उदाहरणस्वरूप, ईमानदारी को आदर्श माना जाता है, परंतु व्यवहार में सभी ईमानदार नहीं होते। आदर्शात्मक संस्कृति समाज को दिशा देती है, उसे आदर्शों की ओर प्रेरित करती है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती है।
प्रश्न-9. संघर्ष के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:- सामाजिक संघर्ष (Conflict) समाज में हितों, विचारों और संसाधनों के टकराव से उत्पन्न होता है। इसके मुख्य स्वरूप निम्नलिखित हैं:
- प्रत्यक्ष संघर्ष: जब दो व्यक्ति या समूह आमने-सामने होकर संघर्ष करते हैं, जैसे युद्ध।
- अप्रत्यक्ष संघर्ष: यह छिपे रूप में होता है, जैसे ईर्ष्या, घृणा।
- आर्थिक संघर्ष: संसाधनों के असमान वितरण के कारण, जैसे श्रमिक और पूंजीपति के बीच।
- राजनीतिक संघर्ष: सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों के बीच।
- सांस्कृतिक संघर्ष: जब विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताएँ टकराती हैं, जैसे पाश्चात्य और पारंपरिक मूल्यों का टकराव।
संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का कारण भी बनता है और समाज में नई व्यवस्थाएँ स्थापित करता है।
प्रश्न-10. ‘एक समाज’ एवं ‘समाज’ में अंतर लिखिए।
उत्तर:- ‘एक समाज’ और ‘समाज’ दोनों शब्दों का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया जाता है:
‘एक समाज’ किसी विशेष समुदाय या समूह को दर्शाता है, जैसे – ग्रामीण समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज। यह सीमित, विशिष्ट और पहचान योग्य होता है।
‘समाज’ एक व्यापक और सामान्य अवधारणा है जो सभी प्रकार के मानव समूहों को सम्मिलित करती है। इसमें विविध जातियाँ, वर्ग, धर्म, क्षेत्र सम्मिलित होते हैं।
उदाहरण: “भारतीय समाज” में कई ‘एक समाज’ शामिल हैं जैसे ब्राह्मण समाज, व्यापारी समाज आदि। अतः ‘एक समाज’ एक इकाई है, जबकि ‘समाज’ उसकी संपूर्ण व्यवस्था है।
प्रश्न-11. संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है।” स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- संस्कृति वह सब कुछ है जो मनुष्य ने प्रकृति से अलग स्वयं निर्मित किया है। प्रकृति से मनुष्य को जंगल, नदी, पर्वत आदि प्राप्त हुए, लेकिन वह अपनी आवश्यकता अनुसार घर, वस्त्र, भाषा, धर्म, कला, विज्ञान आदि का निर्माण करता है। यही निर्माण “संस्कृति” कहलाता है। यह ज्ञान, विश्वास, मूल्य, नैतिकता, परंपराओं, और जीवनशैली का समुच्चय है।
पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं:
प्राकृतिक पर्यावरण – जो ईश्वर निर्मित है (जैसे नदी, पहाड़)।
मानव निर्मित पर्यावरण (संस्कृति) – जो मनुष्य ने बनाया है (जैसे मंदिर, पुस्तकें, कानून)।
इस प्रकार संस्कृति मानव की सृजनात्मकता का प्रतीक है और वह प्रकृति का रूपांतरण है, इसलिए इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहा गया है।
प्रश्न-12. सामाजिक व्यवहार की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- सामाजिक व्यवहार वे क्रियाएँ हैं जो व्यक्ति समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- समूह-संबंधी – यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है।
- परस्पर क्रियात्मक – इसमें संवाद, प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया की प्रक्रिया शामिल होती है।
- सांस्कृतिक रूप से निर्धारित – समाज की संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होता है।
- प्रभावशाली – यह सामाजिक संबंधों को मजबूत या कमजोर कर सकता है।
- प्रेरित – व्यक्ति की इच्छाओं, आवश्यकताओं और लक्ष्यों से प्रेरित होता है।
- सीखने योग्य – यह व्यवहार सामाजिकरण (socialization) के माध्यम से सीखा जाता है।
इस प्रकार सामाजिक व्यवहार मानव जीवन को संचालित और नियमित करता है।
प्रश्न-13. सहयोग के विभिन्न स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-सहयोग (Co-operation) वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु एकसाथ कार्य करते हैं। इसके प्रमुख स्वरूप हैं:
- प्रत्यक्ष सहयोग – जब लोग आमने-सामने कार्य करते हैं, जैसे – खेल में टीम के खिलाड़ी।
- अप्रत्यक्ष सहयोग – जब लोग अलग-अलग कार्य करके एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, जैसे – किसान और व्यापारी।
- सकारात्मक सहयोग – जिसमें सभी लाभ की भावना से कार्य करते हैं।
- नकारात्मक सहयोग – जहाँ बाध्यता या दबाव में कार्य किया जाता है, जैसे – युद्ध में सैनिक।
- आंशिक सहयोग – सीमित समय या उद्देश्य के लिए सहयोग किया जाता है।
इस प्रकार सहयोग समाज को एकता, सह-अस्तित्व और प्रगति की दिशा में अग्रसर करता है।
प्रश्न-14. सामाजिक मानदंड की आधारभूत विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:-सामाजिक मानदंड (Social Norms) वे नियम और अपेक्षाएँ हैं, जिनके अनुसार समाज में व्यवहार किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- समाज द्वारा स्वीकृत – ये नियम समाज द्वारा बनाए और स्वीकारे जाते हैं।
- व्यवहार नियंत्रक – यह लोगों के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करता है।
- अनौपचारिक एवं औपचारिक – कुछ मानदंड लिखित होते हैं (कानून), तो कुछ परंपराओं पर आधारित होते हैं।
- सामाजिक प्रतिबंध – इनका उल्लंघन करने पर आलोचना, बहिष्कार आदि का सामना करना पड़ता है।
- समूह-विशेष – विभिन्न समाजों के मानदंड भिन्न होते हैं।
- परिवर्तनशील – समय के साथ मानदंड बदल सकते हैं।
सामाजिक मानदंड समाज में अनुशासन और स्थिरता बनाए रखते हैं।
प्रश्न-15. आधुनिक भारत में समाजशास्त्र के विकास पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- आधुनिक भारत में समाजशास्त्र का विकास औपनिवेशिक काल से प्रारंभ होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना, भूमि सुधार, जातीय अध्ययन एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण समाज का अध्ययन आरंभ हुआ। प्रारंभ में समाजशास्त्र का उद्देश्य भारतीय समाज की संरचना और समस्याओं को समझना था।
भारत में समाजशास्त्र की शिक्षा सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी (1919) और फिर लखनऊ, दिल्ली तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों में आरंभ हुई। जी.एस. घुर्ये, डी.पी. मुखर्जी, इरावती कर्वे, एम.एन. श्रीनिवास जैसे विद्वानों ने समाजशास्त्र को भारतीय दृष्टिकोण से परिभाषित किया। स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत हुआ और इसमें ग्रामीण समाज, जाति, धर्म, स्त्री अध्ययन, आदिवासी समाज, शहरीकरण आदि विषयों को सम्मिलित किया गया।
आज समाजशास्त्र भारत में सामाजिक समस्याओं के समाधान, नीति निर्माण और सामाजिक योजना के विकास में सहायक विज्ञान के रूप में स्थापित हो चुका है।
प्रश्न-16. मानव एवं प्रकृति के अंतःसंबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:- मानव और प्रकृति के मध्य एक गहरा और परस्परनिर्भर संबंध है। प्रारंभिक मानव प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर था – भोजन, जल, आश्रय, वायु आदि सभी आवश्यकताएँ प्रकृति से ही पूरी होती थीं। जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य ने प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, परंतु आज भी उसकी जीवन प्रणाली पूरी तरह प्रकृति से जुड़ी हुई है।
पर्यावरणीय असंतुलन, वनों की कटाई, प्रदूषण आदि मानवीय गतिविधियाँ प्रकृति को नुकसान पहुँचा रही हैं, जिससे बदले में मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, और महामारी इसके उदाहरण हैं। अतः यह स्पष्ट है कि यदि मनुष्य प्रकृति का संरक्षण करेगा, तभी उसका स्वयं का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा।
इस अंतःसंबंध को समझना और संतुलित विकास की दिशा में कार्य करना आज की आवश्यकता है।
प्रश्न-17. ‘सामाजिक व्यवस्था’ एवं ‘सामाजिक व्यवहार’ के मध्य के संबंध को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- सामाजिक व्यवस्था एक संगठित संरचना है जिसमें संस्थाएँ, मान्यताएँ, भूमिका और नियम सम्मिलित होते हैं, जो समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। जबकि सामाजिक व्यवहार उन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का समुच्चय है, जो व्यक्ति समाज में दूसरों के साथ करता है।
दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों के व्यवहार के लिए ढाँचा प्रदान करती है, वहीं सामाजिक व्यवहार सामाजिक व्यवस्था को जीवित और गतिशील बनाए रखता है। उदाहरण स्वरूप, विवाह एक सामाजिक संस्था है, परंतु विवाह से संबंधित व्यवहार, रीति-रिवाज एवं परंपराएँ समय व स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं।
यदि सामाजिक व्यवस्था कमजोर होती है, तो सामाजिक व्यवहार अनियंत्रित हो जाता है। अतः कहा जा सकता है कि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार एक-दूसरे के पूरक हैं और एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर करता है।
प्रश्न-18. सामाजिक क्रिया के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया सिद्धांत के अनुसार, वह क्रिया जो दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होती है या उसे प्रभावित करने की आशा रखती है, सामाजिक क्रिया कहलाती है। इसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:
- कर्म करने वाला व्यक्ति (Actor): सामाजिक क्रिया का आरंभकर्ता होता है जो सोच-विचार कर निर्णय लेता है।
- लक्ष्य या उद्देश्य (Goal): क्रिया का कोई न कोई उद्देश्य होता है, जैसे लाभ प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना आदि।
- स्थिति (Situation): क्रिया जिस सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होती है, वह क्रिया की दिशा तय करती है।
- प्रेरणा (Motivation): यह आंतरिक या बाह्य कारण हो सकते हैं जो व्यक्ति को क्रिया के लिए प्रेरित करते हैं।
- दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति (Social Context): सामाजिक क्रिया तभी होती है जब उसका संबंध अन्य व्यक्तियों से हो।
इस प्रकार, ये तत्व सामाजिक क्रिया को समझने में सहायक हैं।
प्रश्न-19. प्रकार्यात्मक उपागम की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- प्रकार्यात्मक उपागम (Functional Approach) समाज को एक अंगों की तरह जुड़ी संरचना मानता है, जहाँ प्रत्येक अंग का कोई विशेष कार्य होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- समाज की जैविक उपमा: यह उपागम समाज को शरीर की तरह मानता है, जिसमें प्रत्येक संस्था (जैसे – परिवार, शिक्षा, धर्म) एक अंग की तरह कार्य करती है।
- सामाजिक स्थायित्व पर बल: यह उपागम सामाजिक संतुलन एवं स्थायित्व को महत्व देता है।
- हर संस्था का कार्य: समाज की हर संस्था का कोई विशेष उद्देश्य होता है, जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है।
- परस्पर निर्भरता: समाज के सभी घटक एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक में परिवर्तन से पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है।
- सकारात्मक दृष्टिकोण: यह उपागम समाज की सकारात्मक विशेषताओं और संतुलन पर केंद्रित रहता है।
मूलतः कार्यात्मक उपागम समाज की स्थिरता और संगठन को समझने का एक प्रभावी तरीका है।
प्रश्न-20. सामाजिक नियंत्रण में जन-रीतियों की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- जन-रीतियाँ (folkways) समाज की वे सामान्य परंपराएँ, रीति-रिवाज़ और आचरण नियम हैं जिन्हें समाज में अधिकांश लोग अनजाने में ही मानते हैं। ये सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख उपकरण हैं।
- व्यवहार को निर्देशित करना: जन-रीतियाँ यह तय करती हैं कि कौनसा व्यवहार उपयुक्त है और कौनसा नहीं।
- सामूहिक स्वीकृति: जन-रीतियाँ सामाजिक जीवन के प्रति एकरूपता और अनुशासन लाती हैं।
- अनौपचारिक नियंत्रण: ये किसी लिखित कानून की तरह नहीं होतीं, फिर भी इनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को सामाजिक आलोचना या बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है।
- सामाजिक एकता: जन-रीतियाँ सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती हैं और पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखती हैं।
- नैतिकता का विकास: ये नैतिक मूल्यों को जन्म देती हैं, जिससे सामाजिक जीवन में मर्यादा और संतुलन बना रहता है।
अतः जन-रीतियाँ सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावी साधन हैं।
प्रश्न-21. ग्रामीण समुदाय में अवलोकित विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- ग्रामीण समुदाय भारतीय समाज की मूल इकाई है, जिसकी विशिष्ट विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- छोटी जनसंख्या: ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों की तुलना में कम होती है।
- सामाजिक एकता: वहाँ सामाजिक संबंध व्यक्तिगत और घनिष्ठ होते हैं, जिससे सहयोग की भावना अधिक होती है।
- परंपरा पर आधारित जीवन: ग्रामीण जीवन शैली अधिकतर परंपरागत होती है और बदलाव धीरे-धीरे होते हैं।
- कृषि आधारित अर्थव्यवस्था: अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या कृषि एवं संबंधित कार्यों पर निर्भर होती है।
- सामूहिक जीवन: गाँवों में सामूहिक निर्णय, पंचायत व्यवस्था और लोक परंपराएँ विद्यमान रहती हैं।
- अंधविश्वास एवं धार्मिकता: ग्रामीण लोग धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों में अधिक विश्वास रखते हैं।
- कम सामाजिक गतिशीलता: शिक्षा और संसाधनों की कमी के कारण वहाँ सामाजिक परिवर्तन धीमा होता है।
इस प्रकार ग्रामीण समुदाय की संरचना पारंपरिक और आत्मनिर्भर होती है।
प्रश्न-22. मर्टन के व्यक्तिगत अनुकूलन मॉडल को प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर:-रॉबर्ट के. मर्टन ने समाज में सामाजिक तनाव (strain) की स्थिति में व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रतिक्रियाओं को “व्यक्तिगत अनुकूलन मॉडल” (Modes of Individual Adaptation) के रूप में प्रस्तुत किया। यह मॉडल समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के वैध साधनों के बीच संबंध पर आधारित है। मर्टन ने पाँच प्रकार के अनुकूलन बताए:
- अनुरूपता (Conformity): व्यक्ति सामाजिक लक्ष्यों और साधनों को स्वीकार करता है।
- नवप्रवर्तन (Innovation): लक्ष्य स्वीकार करता है, परंतु अवैध या वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करता है।
- औपचारिकता (Ritualism): साधनों का पालन करता है, पर लक्ष्य को त्याग देता है।
- वियोजन (Retreatism): दोनों को त्याग देता है, जैसे नशेड़ी या साधु।
- विद्रोह (Rebellion): लक्ष्य और साधनों दोनों को अस्वीकार कर नए विकल्प प्रस्तुत करता है।
यह मॉडल बताता है कि समाज में असमानता और दबाव के कारण व्यक्ति अलग-अलग तरीके से अनुकूलन करता है।
प्रश्न-23. समाजशास्त्र के विकास का परिचय दीजिए।
उत्तर:- समाजशास्त्र एक नवोदित सामाजिक विज्ञान है जिसका उद्भव औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात् हुआ। इसका औपचारिक आरंभ 19वीं शताब्दी में माना जाता है। आधुनिक समाज की जटिलताओं को समझने की आवश्यकता ने समाजशास्त्र के विकास को प्रेरित किया। औगस्त कॉन्त ने ‘समाजशास्त्र’ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और इसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया।
इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इमाइल दुर्खीम जैसे विचारकों ने समाज की संरचना, कार्य-प्रणाली, संघर्ष, धर्म, आत्महत्या आदि पर गहन अध्ययन प्रस्तुत किए। भारत में समाजशास्त्र का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेजी से हुआ। भारतीय समाजशास्त्रियों जैसे गोविंद सदाशिव गुइले, ईश्वरन, एम.एन. श्रीनिवास आदि ने जाति, ग्राम, धर्म और सामाजिक परिवर्तन पर महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार समाजशास्त्र का विकास सामाजिक यथार्थ को समझने और समाज के निर्माण की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने हेतु हुआ।
प्रश्न-24. समाज और व्यक्ति के मध्य के सम्बन्ध के समाजशास्त्रीय पक्ष प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर:- समाज और व्यक्ति के संबंध समाजशास्त्र का मूल विषय हैं। व्यक्ति और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति समाज में जन्म लेता है, समाज से ही भाषा, संस्कृति, परंपराएँ, मूल्य और आचरण सीखता है। वहीं, समाज व्यक्ति की गतिविधियों, विचारों और संबंधों से ही निर्मित होता है।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, समाज व्यक्ति को नियमों, संस्थाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के माध्यम से नियंत्रित करता है, जबकि व्यक्ति समाज में नवाचार, विचार परिवर्तन और विकास का कारण बनता है। ए.आर. ब्राउन के अनुसार, “समाज व्यक्तियों का संगठित समूह है।” वहीं मैकाइवर के अनुसार, “कोई भी व्यक्ति समाज के बाहर अस्तित्व नहीं रख सकता।”
समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को समाज के योग्य बनाती है। समाज व्यक्ति को सामाजिक भूमिका निभाने का अवसर देता है और उसकी पहचान निर्धारित करता है। अतः समाज और व्यक्ति का संबंध पारस्परिक, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील होता है।
प्रश्न-25. सांस्कृतिक विलम्बना सिद्धान्त पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- सांस्कृतिक विलम्बना (Cultural Lag) का सिद्धांत अमेरिकी समाजशास्त्री डब्ल्यू. एफ. ओगबर्न ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार, संस्कृति के भौतिक पक्ष (जैसे – तकनीकी विकास) और अमूर्त पक्ष (जैसे – मूल्य, परंपरा, नैतिकता) में विकास की गति समान नहीं होती। जब भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है लेकिन गैर-भौतिक संस्कृति उसी गति से नहीं बदलती, तो समाज में असंतुलन उत्पन्न होता है जिसे सांस्कृतिक विलम्बना कहते हैं।
उदाहरणतः, नई तकनीकों जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि ने जीवन को सरल बनाया है, परंतु उनके नैतिक और सामाजिक प्रभावों को अपनाने में समाज को समय लगता है। इससे पीढ़ियों में टकराव, मूल्य-संघर्ष, और सामाजिक विकृति जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
यह सिद्धांत हमें बताता है कि समाज में परिवर्तन केवल तकनीकी उन्नति से नहीं होता, बल्कि उसके साथ सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं में भी समायोजन आवश्यक है। सांस्कृतिक विलम्बना सामाजिक परिवर्तन की जटिलताओं को समझने में सहायक है।
प्रश्न-26. सामाजिक व्यवस्था की ‘पूर्व आवश्यकताएँ’ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- सामाजिक व्यवस्था (Social System) के सुचारू संचालन के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएँ होती हैं जिन्हें टाल्कोट पार्सन्स ने विशेष रूप से चार AGIL आवश्यकताओं में विभाजित किया है:
- अनुकूलन (Adaptation) – समाज को अपने वातावरण से संसाधन प्राप्त करने और उनका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
- लक्ष्य प्राप्ति (Goal Attainment) – समाज को अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधन एवं दिशा निर्धारित करनी होती है।
- समेकन (Integration) – समाज के विभिन्न अंगों, संस्थाओं और व्यक्तियों के मध्य सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
- नैतिक संरक्षण (Latency or Pattern Maintenance) – सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं और सांस्कृतिक मानदंडों को संरक्षित रखना जरूरी है।
इनके अलावा, सामाजिक व्यवस्था के लिए संचार व्यवस्था, भूमिकाओं का विभाजन, मान्यता प्राप्त नियम, सामाजिक संस्थाएँ और नियंत्रण तंत्र भी आवश्यक होते हैं। ये सभी पूर्व आवश्यकताएँ मिलकर समाज को एक संगठित रूप में बनाए रखती हैं।
प्रश्न-27. आदिम समुदाय को विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- आदिम समुदाय (Primitive Community) उन समाजों को कहा जाता है जो तकनीकी रूप से पिछड़े, आत्मनिर्भर, और परंपराओं पर आधारित होते हैं। ये समुदाय प्राचीन समय से अस्तित्व में हैं और आज भी कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं जैसे भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्र।
आदिम समुदायों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
लघु आकार – ये समुदाय संख्या में छोटे होते हैं।
समानता पर आधारित – इनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता नगण्य होती है।
परंपरागत जीवनशैली – जीवन कृषि, शिकार, मछली पकड़ने और हस्तशिल्प पर आधारित होता है।
मजबूत सामाजिक बंधन – परिवार और कबीले पर आधारित संबंध बहुत मजबूत होते हैं।
धार्मिक विश्वास – ये लोग प्रकृति पूजा, आत्मा और पूर्वज पूजा में विश्वास रखते हैं।
लिखित कानून नहीं – इन समुदायों में मौखिक परंपराएँ और प्रथाएँ ही कानून का कार्य करती हैं।
आदिम समुदाय समाजशास्त्रियों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं क्योंकि ये मानव समाज के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाते हैं।
प्रश्न-28. समिति एवं संस्था में अंतर कीजिए।
उत्तर:-परिभाषा यह लोगों का एक छोटा समूह होता है जो विशेष कार्य हेतु गठित होता है। यह समाज की स्थापित संरचना है जो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करती है।
स्थायित्व यह अस्थायी या स्थायी हो सकती है। यह प्रायः स्थायी और दीर्घकालीन होती है।
सदस्यता सीमित सदस्य होते हैं जिन्हें चुना या नामित किया जाता है। सदस्यता खुली या सीमित हो सकती है, समाज पर निर्भर करती है।
उदाहरण पंचायत समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति। विवाह संस्था, शिक्षा संस्था, धर्म संस्था।
क्रियाकलाप विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेना। समाज को दिशा देने वाले कार्य करना।
इस प्रकार समिति कार्य विशेष के लिए गठित समूह है जबकि संस्था समाज के मूल ढांचे का अंग होती है।
प्रश्न-29. सामाजिक नियमहीनता सम्बन्धी दुर्खीम के विचारों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- इमाइल दुर्खीम ने “सामाजिक नियमहीनता” (Anomie) की अवधारणा को आत्महत्या के अध्ययन के दौरान प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, जब समाज के नियम, मूल्य और मानदंड कमजोर पड़ जाते हैं या अप्रभावी हो जाते हैं, तो व्यक्ति दिशाहीनता की स्थिति में पहुँच जाता है, जिसे ‘Anomie’ कहते हैं।
दुर्खीम का मानना था कि समाज में आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक उथल-पुथल जैसे – औद्योगिकीकरण, युद्ध, बेरोजगारी, आदि से सामाजिक नियंत्रण कमजोर हो जाता है। परिणामस्वरूप, व्यक्ति असमंजस और तनाव में जीता है, जिससे आत्महत्या, अपराध और मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
उन्होंने बताया कि समाज की एकता और नैतिक अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों की स्पष्टता और सामाजिक नियंत्रण आवश्यक हैं। Anomie की स्थिति समाज में असंतुलन और विघटन उत्पन्न करती है। दुर्खीम की यह अवधारणा आधुनिक समाजशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
प्रश्न-30. समाजशास्त्र को ‘सामाजिक प्रस्थितियों का जाल’ के रूप में परिभाषित करने वाले समाजशास्त्री का नाम लिखिए।
उत्तर:- मैकआइवर ने समाजशास्त्र को ‘सामाजिक प्रस्थितियों का जाल’ कहा है।
प्रश्न-31. वंशानुक्रमण को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- वंशानुक्रमण वह प्रक्रिया है जिससे वंश या कुल की पहचान माता या पिता के माध्यम से की जाती है।
प्रश्न-32. ‘धर्म’ की परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- धर्म वह सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है जो किसी व्यक्ति को समाज में निर्धारित भूमिका निभाने के लिए मार्गदर्शन करता है।
प्रश्न-33. ‘आदर्शात्मक संस्कृति’ के समाजशास्त्रीय संदर्श बताइए।
उत्तर:- आदर्शात्मक संस्कृति समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों, मानदंडों और नैतिक सिद्धांतों को दर्शाती है जो लोगों के व्यवहार के लिए आदर्श माने जाते हैं।
प्रश्न-34. ‘द थ्योरी ऑफ सोशल एण्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- मैक्स वेबर
प्रश्न-35. अमेरिका में समाजशास्त्र के विकास पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:-अमेरिका में समाजशास्त्र का विकास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। प्रारंभ में यूरोपीय विचारों से प्रेरित होकर अमेरिकी विद्वानों ने समाजशास्त्रीय अध्ययन की नींव रखी। शिकागो विश्वविद्यालय (1892) ने समाजशास्त्र को शैक्षणिक स्तर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ “शिकागो स्कूल” की स्थापना हुई, जिसने शहरीकरण, आप्रवासन और सामाजिक समस्याओं पर शोध किया।
अमेरिकी समाजशास्त्र व्यवहारवाद और अनुभववाद पर आधारित था। रॉबर्ट पार्क, अर्नेस्ट बर्गेस, और थॉमस जैसे विद्वानों ने शहरी समाज, मानव व्यवहार और सांस्कृतिक विविधता का गहन अध्ययन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजशास्त्र के व्यावहारिक उपयोग में वृद्धि हुई और यह नीति निर्माण, सामाजिक कल्याण और अपराध नियंत्रण में सहयोगी बना।
ताल्कोट पारसन्स, रॉबर्ट किंग मर्टन जैसे विद्वानों ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद को लोकप्रिय बनाया। अमेरिका में समाजशास्त्र अब सामाजिक समस्याओं, नस्लीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, और मानव अधिकारों के मुद्दों पर गंभीर शोध का माध्यम बन चुका है।
प्रश्न-36. “मनुष्य नियंत्रक है” इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-“मनुष्य नियंत्रक है” इस कथन का तात्पर्य यह है कि मनुष्य समाज और प्रकृति दोनों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। सामाजिक दृष्टिकोण से मनुष्य न केवल समाज में रहने वाला प्राणी है, बल्कि वह सामाजिक नियमों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को निर्मित और संचालित करता है।
मनुष्य अपने ज्ञान, तर्क और नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने व्यवहार, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। उसने समाज में शासन, कानून, शिक्षा और नैतिकता जैसी व्यवस्थाओं को बनाकर सामाजिक जीवन को नियंत्रित किया है।
प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक की सहायता से प्रकृति के अनेक पहलुओं को नियंत्रित किया है—जैसे बिजली उत्पादन, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएँ आदि।
यह नियंत्रण सकारात्मक के साथ-साथ नकारात्मक भी हो सकता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। फिर भी, यह कथन सत्य है कि मनुष्य न केवल सामाजिक ढाँचे का अंग है, बल्कि उसका सक्रिय नियंत्रक और निर्माता भी है।
प्रश्न-37. बच्चे का समाजीकरण कौन करता है?
उत्तर:- बच्चे का समाजीकरण विभिन्न सामाजिक एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जो उसे समाज के नियम, मूल्यों और व्यवहारों से परिचित कराते हैं। समाजीकरण का प्रारंभिक चरण परिवार में होता है। माता-पिता, दादा-दादी और भाई-बहन बच्चे को बोलना, चलना, शिष्टाचार, धर्म, भाषा और संस्कृति सिखाते हैं।
इसके बाद विद्यालय, सहपाठी, मीडिया और धार्मिक संस्थाएँ समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान करती हैं। शिक्षक अनुशासन, ज्ञान और सामाजिक नियमों की समझ देते हैं। मित्रों के समूह से बच्चा आपसी सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक भूमिकाओं को समझता है।
मीडिया (जैसे टीवी, इंटरनेट) आधुनिक समाज में समाजीकरण का एक प्रभावशाली साधन बन चुका है जो बच्चे के सोचने और समझने के ढंग को प्रभावित करता है।
अतः बच्चे का समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें परिवार, विद्यालय, समूह और समाज की विविध संस्थाएँ भूमिका निभाती हैं।
प्रश्न-38. प्राथमिक समूह का महत्व स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- प्राथमिक समूह समाज के वे छोटे समूह होते हैं जिनमें सदस्य आपसी स्नेह, आत्मीयता और प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। परिवार, मित्र मंडली और पड़ोस इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
इन समूहों का महत्व अत्यधिक होता है क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिकरण और भावनात्मक विकास में सहायक होते हैं। बच्चे का प्रथम समाजीकरण परिवार में होता है, जहाँ वह भाषा, आचरण, संस्कार और मूल्य सीखता है।
प्राथमिक समूह भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। व्यक्ति को प्रेम, सुरक्षा और आत्म-सम्मान की अनुभूति इन्हीं समूहों से होती है। यह समूह व्यक्ति को सामाजिकता सिखाते हैं, जैसे सहयोग, सहानुभूति, और जिम्मेदारी।
साथ ही, ये समूह सामाजिक नियंत्रण का भी माध्यम होते हैं क्योंकि वे अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं।
इस प्रकार प्राथमिक समूह समाज के आधारभूत इकाई होते हैं जो सामाजिक ताने-बाने को सशक्त बनाते हैं।
प्रश्न-39. समिति की विशेषताएँ लिखिए
उत्तर:- समिति (Association) एक संगठित समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- संगठित संरचना – समिति एक व्यवस्थित समूह होता है जिसमें सदस्यों की भूमिका और कार्य निर्धारित होते हैं।
- सामान्य उद्देश्य – इसके सदस्यों का कोई एक समान लक्ष्य या उद्देश्य होता है, जैसे—शिक्षा, धर्म, व्यापार आदि।
- नियम और व्यवस्था – समिति के संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है।
- सदस्यता – इसमें सीमित अथवा खुली सदस्यता हो सकती है, जो स्वैच्छिक होती है।
- सहयोग की भावना – समिति के सदस्य मिल-जुलकर कार्य करते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं।
- निरंतरता – समितियाँ अक्सर दीर्घकालिक होती हैं और निरंतर क्रियाशील रहती हैं।
उदाहरण के लिए—विद्यालय समिति, सहकारी समिति, महिला मंडल आदि। समिति सामाजिक जीवन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
प्रश्न-40. सामाजिक मूल्य के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- सामाजिक मूल्य वे नैतिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक मानदंड होते हैं जो समाज के सदस्यों को उचित आचरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये समाज को एकजुट बनाए रखते हैं।
महत्त्व:
- समाज में अनुशासन बनाए रखना: सामाजिक मूल्य व्यक्ति को यह बताते हैं कि क्या करना उचित है और क्या नहीं।
- सामाजिक एकता: समान मूल्यों के कारण समाज के लोग एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं।
- संस्कृति का संरक्षण: मूल्य परंपराओं और संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं।
- नैतिक विकास: ये व्यक्ति में नैतिकता, सहिष्णुता और न्याय की भावना विकसित करते हैं।
- समाज में स्थिरता: जब सभी लोग साझा मूल्यों का पालन करते हैं, तो समाज में स्थिरता बनी रहती है।
इस प्रकार, सामाजिक मूल्य समाज के ढांचे को बनाए रखने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
Section-C
प्रश्न-1. सामाजिक स्तरीकरण के आधारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:-सामाजिक स्तरीकरण (Social Stratification) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता का एक ढांचा है, जिसमें व्यक्ति या समूह को सामाजिक हैसियत, अधिकार, धन, शिक्षा आदि के आधार पर ऊँच-नीच का दर्जा प्राप्त होता है। यह असमानता विभिन्न आधारों पर निर्मित होती है, जिनका विवेचन निम्नलिखित है –
- आर्थिक आधार:
धन-संपत्ति की उपलब्धता सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। समाज में अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब जैसे वर्ग बनते हैं। पूंजीवादी समाज में आर्थिक शक्ति के अनुसार व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है। - जाति आधारित आधार (Caste):
भारत जैसे देशों में जाति व्यवस्था एक प्रमुख स्तरीकरण का आधार है। इसमें व्यक्ति का स्थान जन्म के अनुसार निर्धारित होता है और यह परिवर्तनशील नहीं होता। - वर्ग (Class):
मार्क्स और वेबर जैसे समाजशास्त्रियों ने वर्ग को एक लचीला स्तरीकरण माना। यह संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, प्रतिष्ठा आदि पर आधारित होता है। इसमें ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की संभावनाएँ होती हैं। - धर्म:
धार्मिक मान्यताएँ और परंपराएँ भी लोगों को ऊँच-नीच की स्थिति में बाँट देती हैं। जैसे, पुरोहितों को उच्च और शूद्रों को निम्न माना गया। - लिंग (Gender):
सामाजिक रूप से पुरुषों को अधिक अधिकार और स्त्रियों को सीमित भूमिका में बाँध देना भी स्तरीकरण का एक रूप है। लैंगिक असमानता आज भी समाज में विद्यमान है। - शिक्षा:
शिक्षा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। शिक्षित लोगों को समाज में अधिक सम्मान और अवसर प्राप्त होते हैं। - व्यवसाय:
व्यक्ति का पेशा उसकी सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। जैसे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि को उच्च दर्जा प्राप्त होता है।
सामाजिक स्तरीकरण समाज की संरचना का अभिन्न भाग है। यह समाज में संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण करता है और सामाजिक गतिशीलता को भी प्रभावित करता है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण समाज को एक जीवंत तंत्र (living system) के रूप में देखता है, जिसमें हर संरचना (Structure) एक विशेष कार्य (Function) करती है। इस दृष्टिकोण का विकास विशेष रूप से टाल्कॉट पार्सन्स और रॉबर्ट के. मर्टन द्वारा किया गया।
- मुख्य विशेषताएँ:
समाज विभिन्न संस्थाओं (जैसे – परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति) से मिलकर बना है।
प्रत्येक संस्था समाज के कार्य और स्थायित्व बनाए रखने में योगदान देती है।
यदि एक संस्था विफल हो जाती है, तो अन्य संस्थाएँ उसे संतुलित करने की कोशिश करती हैं।
- टाल्कॉट पार्सन्स का दृष्टिकोण:
पार्सन्स ने AGIL मॉडल प्रस्तुत किया, जो चार आवश्यक प्रकार्यों को दर्शाता है –
A (Adaptation): पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन – आर्थिक व्यवस्था।
G (Goal Attainment): लक्ष्य प्राप्त करना – राजनीतिक व्यवस्था।
I (Integration): सामाजिक एकता बनाए रखना – धर्म व कानून।
L (Latency): मूल्यों की रक्षा और प्रसारण – परिवार व शिक्षा।
- रॉबर्ट के. मर्टन का योगदान:
मर्टन ने कार्यों को दो भागों में बाँटा –
प्रकट कार्य (Manifest Functions): जो जानबूझकर होते हैं।
गुप्त कार्य (Latent Functions): जो अनजाने में होते हैं।
उन्होंने विध्वंसात्मक कार्य (Dysfunction) की संकल्पना भी दी – जब कोई संस्था समाज को नुकसान पहुँचाती है।
- उदाहरण:
परिवार सामाजिककरण करता है, भावनात्मक सुरक्षा देता है।
शिक्षा सामाजिक मूल्य और ज्ञान प्रदान करती है।
कानून व्यवस्था बनाए रखता है।
- आलोचना:
यह दृष्टिकोण परिवर्तन को कम महत्व देता है।
वर्ग संघर्ष, असमानता, और शोषण की उपेक्षा करता है।
संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण समाज की स्थिरता, समरसता और संस्थाओं की भूमिका को समझने का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह समाज को एक संगठित तंत्र मानता है जिसमें हर हिस्सा पूरे समाज की भलाई के लिए कार्य करता है।
प्रश्न-3. सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:-सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों और व्यवहार में होने वाले स्थायी और व्यापक परिवर्तनों से है। समाजशास्त्र में विभिन्न प्रतिमानों (patterns) के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को समझा जाता है। ये प्रतिमान हमें यह जानने में सहायता करते हैं कि समाज किस दिशा में और किस रूप में बदल रहा है।
- रैखिक प्रतिमान (Linear Pattern):
इस प्रतिमान के अनुसार समाज निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है। इसमें परिवर्तन एक सीधी रेखा की तरह होते हैं। उदाहरण के लिए, विज्ञान और तकनीक की उन्नति को देखकर ऐसा कहा जाता है कि समाज लगातार विकास कर रहा है। इस प्रतिमान में समाज आदिम स्थिति से आधुनिकता की ओर बढ़ता है। - चक्रीय प्रतिमान (Cyclical Pattern):
चक्रीय प्रतिमान के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक चक्र में होता है, जिसमें समाज जन्म लेता है, विकसित होता है, और फिर पतन की ओर जाता है। अर्नाल्ड टॉयन्बी, स्पेंगलर आदि समाजशास्त्रियों ने इस प्रतिमान का समर्थन किया। यह प्रतिमान बताता है कि समाज एक ही चक्र को दोहराता है। - द्वंदात्मक प्रतिमान (Dialectical Pattern):
कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित यह प्रतिमान समाज को द्वंद्व के आधार पर देखता है। इसमें परिवर्तन संघर्ष के माध्यम से होता है – जैसे पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष के कारण समाज में क्रांति और परिवर्तन आते हैं। - कार्यात्मक प्रतिमान (Functional Pattern):
तालकोट पार्सन्स और रॉबर्ट के मर्टन जैसे समाजशास्त्रियों के अनुसार समाज की हर संस्था एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखती है। जब संतुलन टूटता है, तब समाज परिवर्तन की ओर बढ़ता है ताकि नया संतुलन स्थापित हो सके। - उत्क्रांतिवादी प्रतिमान (Evolutionary Pattern):
इस प्रतिमान के अनुसार समाज क्रमिक विकास की प्रक्रिया से गुजरता है, जैसे जीवों की जैविक विकास प्रक्रिया होती है। ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर ने इस प्रतिमान का समर्थन किया। समाज क्रमशः सरल से जटिल और आदिम से आधुनिक रूप में परिवर्तित होता है।
सामाजिक परिवर्तन के ये प्रतिमान समाज की गतिशील प्रकृति को समझने के लिए उपयोगी हैं। ये विभिन्न दृष्टिकोणों से समाज में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने में सहायता करते हैं।
प्रश्न-4. कुले और मीड द्वारा दिए गए समाजीकरण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:-समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखता है और समाज का सक्रिय सदस्य बनता है। चार्ल्स हॉर्टन कुले और जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने समाजीकरण को समझाने हेतु महत्त्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं।
- चार्ल्स हॉर्टन कुले का “द लुकिंग ग्लास सेल्फ” सिद्धांत:
कुले के अनुसार व्यक्ति की आत्म-छवि (self-image) समाज में अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित होती है। उन्होंने इसे “आत्म-दर्पण” (Looking Glass Self) कहा। यह तीन चरणों में कार्य करता है:
(i) हम कल्पना करते हैं कि दूसरों की नजर में हम कैसे दिखाई देते हैं।
(ii) हम यह अनुमान लगाते हैं कि वे हमारे व्यवहार की कैसे व्याख्या करते हैं।
(iii) हम उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपनी आत्म-छवि बनाते हैं।
उदाहरणतः, यदि एक बच्चा सोचता है कि लोग उसे चतुर मानते हैं, तो वह खुद को चतुर समझने लगता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है।
- जॉर्ज हर्बर्ट मीड का समाजीकरण सिद्धांत:
मीड ने प्रतीकात्मक अन्तःक्रिया (Symbolic Interactionism) के आधार पर समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने “I” और “Me” की अवधारणाएँ दीं:
“I” आत्म का सक्रिय और स्वैच्छिक भाग है, जो स्वतंत्र निर्णय लेता है।
“Me” समाज द्वारा निर्धारित भूमिका और अपेक्षाओं को दर्शाता है, जो व्यक्ति में विकसित होती है।
मीड के समाजीकरण के तीन चरण:
(i) अनुकरण चरण (Imitation Stage): बचपन में बच्चा दूसरों की नकल करता है।
(ii) खेल चरण (Play Stage): बच्चा विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं (जैसे – माँ, शिक्षक) का अभिनय करता है।
(iii) प्रतियोगिता चरण (Game Stage): बच्चा एक साथ कई भूमिकाओं को समझता है और सामाजिक नियमों को अपनाता है।
कुले और मीड दोनों ने बताया कि समाजीकरण व्यक्ति और समाज के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। इनके सिद्धांतों से हम समझ पाते हैं कि व्यक्ति का आत्म, सामाजिक परिवेश में कैसे विकसित होता है।
प्रश्न-5. सामाजिक नियंत्रण की विभिन्न संस्थाओं का विवेचन कीजिए।
उत्तर:- सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है – समाज द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहार को नियमित करना और उन्हें सामाजिक नियमों के अनुरूप बनाए रखना। यह समाज में व्यवस्था और स्थायित्व बनाए रखने हेतु आवश्यक है। सामाजिक नियंत्रण के लिए समाज ने कई संस्थाओं का निर्माण किया है। ये संस्थाएँ दो प्रकार की होती हैं – औपचारिक एवं अनौपचारिक।
- अनौपचारिक संस्थाएँ:
(i) परिवार: समाजीकरण की प्रथम इकाई परिवार है। यह बच्चों को नैतिकता, अनुशासन, मर्यादा और सामाजिक व्यवहार सिखाता है।
(ii) परंपरा और रीति-रिवाज: ये लोगों को निर्धारित व्यवहार की दिशा में निर्देशित करते हैं। जैसे, शादी, त्यौहार आदि में सामाजिक अपेक्षाओं का पालन होता है।
(iii) जनमत (Public Opinion): समाज में लोगों की सामूहिक राय व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है।
(iv) धर्म: यह लोगों के व्यवहार को नैतिक दिशा देता है और बुराई से दूर रहने की प्रेरणा देता है।
- औपचारिक संस्थाएँ:
(i) विधि और कानून: यह सबसे शक्तिशाली नियंत्रण माध्यम है। कानून उल्लंघन पर दंड निर्धारित होते हैं, जिससे लोग भयवश नियमों का पालन करते हैं।
(ii) न्यायपालिका: यह विधि की व्याख्या करती है और निष्पक्ष निर्णय के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है।
(iii) सरकार और प्रशासन: यह नियमों को लागू करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
(iv) शैक्षणिक संस्थाएँ: ये नागरिकों में सामाजिक मूल्यों और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करती हैं।
सामाजिक नियंत्रण की ये संस्थाएँ समाज में अनुशासन, नैतिकता और एकता बनाए रखने में सहायक होती हैं। इनके बिना समाज में अराजकता और विघटन हो सकता है।
प्रश्न-6. विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए समाज के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- समाज का वर्गीकरण सामाजिक संरचना, संस्कृति, आर्थिक आधार और विकास की अवस्था के आधार पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किया है। यह वर्गीकरण हमें समाज की विविधताओं को समझने में सहायता करता है।
- अगस्ट कॉम्ट (Auguste Comte):
कॉम्ट ने समाज के विकास को तीन अवस्थाओं में बाँटा —
धार्मिक अवस्था (Theological Stage): इस अवस्था में समाज धर्म और अंधविश्वास पर आधारित होता है।
दार्शनिक अवस्था (Metaphysical Stage): इस चरण में तर्क और दार्शनिक विचारों का प्रभुत्व होता है।
वैज्ञानिक अवस्था (Positive Stage): इस अवस्था में समाज विज्ञान और प्रयोगों के आधार पर चलता है।
- लुईस मौरगन (Lewis Morgan):
मौरगन ने समाज को तकनीकी विकास के आधार पर तीन भागों में बाँटा —
विकट बर्बरता (Savagery),
बर्बरता (Barbarism),
सभ्यता (Civilization)।
यह वर्गीकरण सामाजिक विकास की दिशा को दर्शाता है।
- फर्डिनेंड टॉननीज़ (Ferdinand Tönnies):
उन्होंने दो प्रकार के समाजों की व्याख्या की —
गेमाइन्सशाफ्ट (Gemeinschaft): यह समाज परंपरागत, ग्रामीण और भावनात्मक संबंधों पर आधारित होता है।
गेसलशाफ्ट (Gesellschaft): यह आधुनिक, शहरी और औपचारिक संबंधों वाला समाज होता है।
- एमीले दुर्खीम (Emile Durkheim):
दुर्खीम ने सामाजिक एकता के आधार पर दो प्रकार के समाज बताए —
यांत्रिक एकता (Mechanical Solidarity): समान कार्यों और विश्वासों पर आधारित समाज।
कार्बनिक एकता (Organic Solidarity): कार्य विभाजन और परस्पर निर्भरता पर आधारित समाज।
- कार्ल मार्क्स (Karl Marx):
मार्क्स ने समाज को आर्थिक आधार पर वर्गीकृत किया —
सम्पत्तिवान वर्ग (Bourgeoisie): उत्पादन के साधनों का स्वामी।
श्रमिक वर्ग (Proletariat): श्रम बेचने वाला वर्ग।
उनके अनुसार समाज का इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास है।
- गेरहार्ड और जीन लेन्स्की (Gerhard & Jean Lenski):
इन्होंने समाज को तकनीकी विकास के आधार पर छह वर्गों में बाँटा:
शिकारी-संग्राहक,
कृषि समाज,
औद्योगिक समाज,
पोस्ट-इंडस्ट्रियल समाज आदि।
समाज का वर्गीकरण सामाजिक परिवर्तन, तकनीकी प्रगति, आर्थिक ढाँचे और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होता है। इससे हमें मानव समाज के विकास को समझने और विभिन्न सामाजिक संरचनाओं का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है।
प्रश्न-7. संस्कृति की परिभाषित कीजिए तथा इसके सांस्कृतिक विलंबन (Cultural Lag) सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डालिए।
उत्तर:- संस्कृति की परिभाषा:
संस्कृति मानव समाज द्वारा अर्जित, सीखी एवं संप्रेषित उन समस्त ज्ञान, विश्वासों, कलाओं, नैतिकताओं, विधियों, रीति-रिवाजों एवं परंपराओं का समुच्चय है जो किसी विशेष समाज को विशिष्ट बनाती है। टेलर के अनुसार, “संस्कृति वह जटिल संहिता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रिवाज एवं अन्य क्षमताएँ व आदतें सम्मिलित होती हैं जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है।”
संस्कृति केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि उसमें निहित विचार, मूल्य, भाषा, धर्म एवं प्रतीकात्मक स्वरूप भी शामिल हैं। यह सामाजिक जीवन की दिशा निर्धारित करती है।
सांस्कृतिक विलंबन (Cultural Lag) सिद्धांत:
सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत प्रसिद्ध समाजशास्त्री डब्ल्यू. एफ. ओगबर्न (W.F. Ogburn) ने प्रतिपादित किया। उनका मानना था कि संस्कृति के दो पक्ष होते हैं – भौतिक (Material) एवं अमूर्त (Non-material)। भौतिक पक्ष में प्रौद्योगिकी, यंत्र, वस्तुएँ आती हैं जबकि अमूर्त पक्ष में नैतिकता, विश्वास, मूल्य, परंपराएँ आदि सम्मिलित होते हैं।
ओगबर्न के अनुसार, भौतिक संस्कृति तीव्र गति से परिवर्तन करती है जबकि अमूर्त संस्कृति धीमी गति से। इस कारण भौतिक और अमूर्त संस्कृति के मध्य असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे ही सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं।
उदाहरण:
विज्ञान और तकनीक ने “क्लोनिंग” या “टेस्ट ट्यूब बेबी” जैसी चीजें संभव बना दीं, परंतु समाज की नैतिक मान्यताएँ एवं धार्मिक धारणाएँ इतनी शीघ्र नहीं बदल पाईं।
सोशल मीडिया एवं इंटरनेट की तीव्र प्रगति के साथ-साथ समाज में गोपनीयता, नैतिकता एवं व्यवहारगत मूल्यों में समरसता नहीं बन पाई।
प्रभाव:
सामाजिक तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न होते हैं।
नैतिक असंतुलन एवं वैचारिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है।
सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बाधित होती है।
संस्कृति समाज का आधार है, परंतु जब इसके विभिन्न पक्ष असमान गति से विकसित होते हैं, तो सांस्कृतिक विलंबन उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत सामाजिक असंतुलन को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है।
प्रश्न-8. समाजीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके सोपानों की विस्तार से व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- समाजीकरण की परिभाषा:
समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति समाज के मूल्यों, मान्यताओं, व्यवहारों, नियमों, परंपराओं एवं सामाजिक भूमिकाओं को सीखता है और सामाजिक जीवन में सम्मिलित होता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को “जैविक प्राणी” से “सामाजिक प्राणी” में परिवर्तित करती है।
हर्टन और हंट के अनुसार, “समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में रहने के योग्य बनता है।”
समाजीकरण के सोपान (Stages of Socialization):
- प्राथमिक समाजीकरण (Primary Socialization):
यह जीवन के प्रारंभिक वर्षों में होता है, मुख्यतः परिवार के माध्यम से। बच्चा भाषा, आचरण, नैतिकता आदि की मूल शिक्षा प्राप्त करता है। - माध्यमिक समाजीकरण (Secondary Socialization):
यह विद्यालय, मित्र समूह, धार्मिक संस्थाएँ, मीडिया आदि के माध्यम से होता है। यहाँ बच्चा समाज के विस्तृत नियमों को सीखता है। - व्यावसायिक समाजीकरण (Professional Socialization):
व्यक्ति जब किसी पेशे या व्यवसाय में प्रवेश करता है तो वह उस क्षेत्र की विशिष्ट भूमिकाओं, नियमों एवं नैतिकता को अपनाता है। - पुनः समाजीकरण (Resocialization):
जब व्यक्ति को किसी नए सामाजिक वातावरण में ढलना पड़ता है (जैसे – जेल, सेना, मानसिक अस्पताल), तब वह पुनः सामाजिक भूमिका सीखता है। - राजनीतिक समाजीकरण (Political Socialization):
व्यक्ति राजनीति, अधिकारों, कर्तव्यों, राष्ट्रवाद आदि को राजनीतिक माध्यमों से सीखता है।
समाजीकरण व्यक्ति के सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया है। यह जीवनपर्यंत चलती है और समाज को बनाए रखने एवं संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
प्रश्न-9. प्रदत्त प्रस्थिति के निर्धारण के आधारों को विस्तार से समझाते हुए स्पष्ट कीजिए कि भूमिका प्रस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है।
उत्तर:- प्रदत्त प्रस्थिति की परिभाषा:
प्रदत्त प्रस्थिति (Ascribed Status) वह सामाजिक स्थिति है जो जन्म के साथ ही व्यक्ति को स्वतः प्राप्त होती है, जिसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। यह जाति, लिंग, धर्म, वंश, वर्ग आदि पर आधारित होती है।
प्रदत्त प्रस्थिति के निर्धारण के आधार:
- जाति: भारत में जाति आधारित प्रस्थिति जन्म के साथ तय हो जाती है।
- लिंग: स्त्री एवं पुरुष की सामाजिक भूमिकाएँ भिन्न होती हैं।
- परिवार और वंश: प्रतिष्ठित या निम्न वंश में जन्म व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है।
- धर्म और संस्कृति: किस धर्म और परंपरा में व्यक्ति जन्म लेता है, वह भी उसकी सामाजिक पहचान को निर्धारित करता है।
भूमिका और प्रस्थिति का गत्यात्मक पक्ष:
प्रस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति है जबकि भूमिका उस स्थिति से जुड़ा हुआ व्यवहार है। यद्यपि प्रदत्त प्रस्थिति स्थायी प्रतीत होती है, किंतु उससे जुड़ी भूमिका गत्यात्मक होती है। उदाहरणतः एक महिला का जन्म लिंग के आधार पर हुआ, परंतु वह माता, बहन, नेता, डॉक्टर आदि विभिन्न भूमिकाएँ निभा सकती है।
गत्यात्मक पक्ष के उदाहरण:
एक ब्राह्मण पुरोहित का पुत्र शिक्षित होकर डॉक्टर बन सकता है।
एक दलित महिला सामाजिक कार्यकर्ता बनकर सामाजिक परिवर्तन की भूमिका निभा सकती है।
प्रदत्त प्रस्थिति सामाजिक पहचान का आधार है, किंतु सामाजिक भूमिका उस प्रस्थिति को सार्थक बनाती है और व्यक्ति को समाज में गत्यात्मकता प्रदान करती है।
प्रश्न-10. सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभेदीकरण में अंतर कीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- प्रश्न 1
प्रश्न-11. पारसन्स द्वारा दिए गए संरचनात्मक प्रकार्यवाद पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- ताल्कोट पारसन्स ने समाज को एक प्रणाली के रूप में देखा जिसमें विभिन्न संस्थाएं (जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म) एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखती हैं। उनके संरचनात्मक प्रकार्यवाद (Structural Functionalism) के अनुसार, समाज एक जैविक इकाई की तरह है, जहाँ प्रत्येक भाग (संरचना) का कोई विशिष्ट कार्य (प्रकार्य) होता है जो सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है।
पारसन्स ने AGIL मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें चार मूलभूत आवश्यकताएं बताई गईं—
- Adaptation (अनुकूलन)
- Goal Attainment (लक्ष्य प्राप्ति)
- Integration (एकीकरण)
- Latency (रूपविन्यास बनाए रखना)
इन आवश्यकताओं के माध्यम से कोई भी सामाजिक प्रणाली संतुलित रह सकती है। पारसन्स का मानना था कि समाज में परिवर्तन धीरे-धीरे होता है और हर संस्थान समाज की स्थिरता में योगदान देता है।
संरचनात्मक प्रकार्यवाद ने सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान किया, परंतु इसे आलोचना भी मिली कि यह सामाजिक संघर्ष और बदलाव की उपेक्षा करता है।
- “मनुष्य नियंत्रक है” इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
“मनुष्य नियंत्रक है” इस कथन का तात्पर्य यह है कि मनुष्य समाज और प्रकृति दोनों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। सामाजिक दृष्टिकोण से मनुष्य न केवल समाज में रहने वाला प्राणी है, बल्कि वह सामाजिक नियमों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को निर्मित और संचालित करता है।
मनुष्य अपने ज्ञान, तर्क और नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने व्यवहार, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। उसने समाज में शासन, कानून, शिक्षा और नैतिकता जैसी व्यवस्थाओं को बनाकर सामाजिक जीवन को नियंत्रित किया है।
प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक की सहायता से प्रकृति के अनेक पहलुओं को नियंत्रित किया है—जैसे बिजली उत्पादन, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएँ आदि।
यह नियंत्रण सकारात्मक के साथ-साथ नकारात्मक भी हो सकता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। फिर भी, यह कथन सत्य है कि मनुष्य न केवल सामाजिक ढाँचे का अंग है, बल्कि उसका सक्रिय नियंत्रक और निर्माता भी है।
प्रश्न-12. कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए समाज के वर्गीकरण की स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-
प्रश्न-13. संस्कृति को परिभाषित कीजिए एवं संस्कृति के उपादान (अंग) लिखिए।
उत्तर:- संस्कृति वह जटिल संकल्पना है जो किसी समाज में प्रचलित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति-रिवाजों एवं किसी व्यक्ति को समाज का सदस्य बनाने हेतु अर्जित सभी योग्यताओं एवं आदतों को सम्मिलित करती है। संस्कृति मानव द्वारा अर्जित एक सामाजिक धरोहर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है।
संस्कृति की परिभाषाएँ:
- ई. बी. टायलर के अनुसार – “संस्कृति वह समग्र है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति-रिवाज, और मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त की गई अन्य क्षमताएँ तथा आदतें सम्मिलित हैं।”
- रेडफील्ड के अनुसार – “संस्कृति का अर्थ जीवन की शैली से है, जो किसी समाज में लोगों के मध्य स्वीकृत होती है।”
संस्कृति के उपादान (अंग):
संस्कृति विभिन्न घटकों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम इसके उपादान कहते हैं:
- भाषा (Language):
भाषा संस्कृति का आधार है। यह विचारों, भावनाओं एवं ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। - प्रतीक (Symbols):
प्रतीक वह संकेत हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे – तिरंगा झंडा भारत का प्रतीक है। - मान्यताएँ (Beliefs):
किसी समाज में प्रचलित विश्वास जैसे – आत्मा का अस्तित्व, ईश्वर की सत्ता आदि। - मूल्य (Values):
ये ऐसे आदर्श होते हैं जिनका समाज में विशेष महत्व होता है, जैसे – सत्य, अहिंसा, समानता। - नियम (Norms):
यह सामाजिक आचरण के नियम हैं। यह दो प्रकार के होते हैं:
लोकाचार (Folkways) – जैसे भोजन के समय हाथ धोना।
नैतिकाचार (Mores) – जैसे चोरी या हत्या करना वर्जित है।
- वस्तु संस्कृति (Material Culture):
इसमें मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएँ आती हैं जैसे – मकान, कपड़े, वाहन आदि। - अवस्तु संस्कृति (Non-material Culture):
इसमें विचार, मूल्यों, नियमों आदि का समावेश होता है। - रीति-रिवाज (Customs):
यह व्यवहार के परंपरागत ढंग होते हैं जो लंबे समय से प्रचलित होते हैं।
संस्कृति मानव समाज की आत्मा होती है। इसके विविध उपादान मिलकर समाज को एक विशेष पहचान और दिशा प्रदान करते हैं। संस्कृति की समझ सामाजिक संरचना को समझने में सहायक होती है।
प्रश्न-14. प्रकार्य को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- समाजशास्त्र में ‘प्रकार्य’ (Function) का अर्थ किसी संस्था, परंपरा या व्यवहार द्वारा समाज के समुचित संचालन और संतुलन में किए गए योगदान से है। प्रकार्य यह दर्शाता है कि समाज का कोई भी घटक किस प्रकार समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है।
प्रकार्य की परिभाषा:
- रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार – “प्रकार्य उस योगदान को कहते हैं जो किसी सामाजिक तत्व द्वारा सामाजिक जीवन के निरंतरता हेतु किया जाता है।”
- मैलिनोवस्की के अनुसार – “प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है।”
प्रकार्य की विशेषताएँ:
- सामाजिक संरचना से संबंधित:
प्रत्येक प्रकार्य समाज की संरचना एवं संगठन को बनाए रखने में सहायक होता है। - आवश्यकता पूर्ति:
समाज के विभिन्न प्रकार्य मानव की जैविक, सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। - सामंजस्य बनाए रखना:
प्रकार्य समाज में संतुलन, सामंजस्य और अनुशासन को बनाए रखता है। - प्रत्येक संस्था का प्रकार्य होता है:
जैसे – परिवार का प्रमुख प्रकार्य प्रजनन और समाजीकरण है, शिक्षा का प्रकार्य ज्ञान का संप्रेषण है। - जटिल और परस्पर संबंधी:
समाज के प्रकार्य एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक में परिवर्तन अन्य पर भी प्रभाव डालता है। - मूल्य आधारित:
प्रकार्य सामाजिक मूल्यों पर आधारित होते हैं और उन्हें संरक्षित रखते हैं। - सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रकार्य:
सकारात्मक प्रकार्य: समाज में स्थिरता और प्रगति लाते हैं।
नकारात्मक प्रकार्य: जैसे – जातिवाद, सामाजिक विषमता।
- गोपनीय (Latent) एवं प्रकट (Manifest) प्रकार्य:
प्रकट प्रकार्य: जानबूझकर और स्पष्ट रूप से किया गया प्रकार्य जैसे – शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्ति।
गोपनीय प्रकार्य: जो अप्रत्यक्ष होता है जैसे – शिक्षा द्वारा विवाह के अवसर बढ़ना।
प्रकार्य समाज की जीवनधारा को गतिशील बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समाजशास्त्रीय विश्लेषण का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।
प्रश्न-15. संघर्ष का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- संघर्ष समाजशास्त्र का एक प्रमुख तत्व है, जिसमें व्यक्ति, समूह या वर्ग के बीच विरोध, मतभेद या टकराव होता है। जब दो या अधिक व्यक्ति अपने लक्ष्यों, विचारों या संसाधनों को लेकर एक-दूसरे से असहमति रखते हैं, तब संघर्ष उत्पन्न होता है।
संघर्ष की परिभाषा:
- गिलिन और गिलिन के अनुसार – “संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह एक-दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं।”
- सिमेल के अनुसार – “संघर्ष सामाजिक जीवन का अनिवार्य अंग है जो समाज को गतिशील बनाता है।”
संघर्ष के स्वरूप (Forms of Conflict):
- व्यक्तिगत संघर्ष (Personal Conflict):
दो व्यक्तियों के बीच होने वाला मतभेद जैसे – पड़ोसियों या सहकर्मियों के बीच। - वर्गीय संघर्ष (Class Conflict):
यह संघर्ष आर्थिक वर्गों के बीच होता है, जैसे – पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच। - राजनीतिक संघर्ष:
विभिन्न राजनीतिक दलों या विचारधाराओं के बीच सत्ता को लेकर प्रतिस्पर्धा। - सांस्कृतिक संघर्ष:
जब दो संस्कृतियों के मूल्य या परंपराएँ आपस में टकराती हैं जैसे – आधुनिकता बनाम परंपरा। - धार्मिक संघर्ष:
अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच आस्था को लेकर संघर्ष। - राष्ट्रीय संघर्ष:
यह संघर्ष एक राष्ट्र और उपनिवेश या स्वतंत्रता के बीच हो सकता है, जैसे – भारत का स्वतंत्रता संग्राम। - अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष:
जब दो देशों के बीच युद्ध, शीत युद्ध या राजनीतिक तनाव हो जैसे – रूस-यूक्रेन संघर्ष।
संघर्ष सामाजिक जीवन का स्वाभाविक एवं अपरिहार्य भाग है। यह यद्यपि नकारात्मक प्रतीत होता है, परंतु कभी-कभी यह परिवर्तन, सुधार और सामाजिक चेतना लाने में सहायक सिद्ध होता है।
vmou MASO-01 paper , vmou MA exam paper , vmou exam paper 2028 vmou exam paper 2027 vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4
VMOU EXAM PAPER