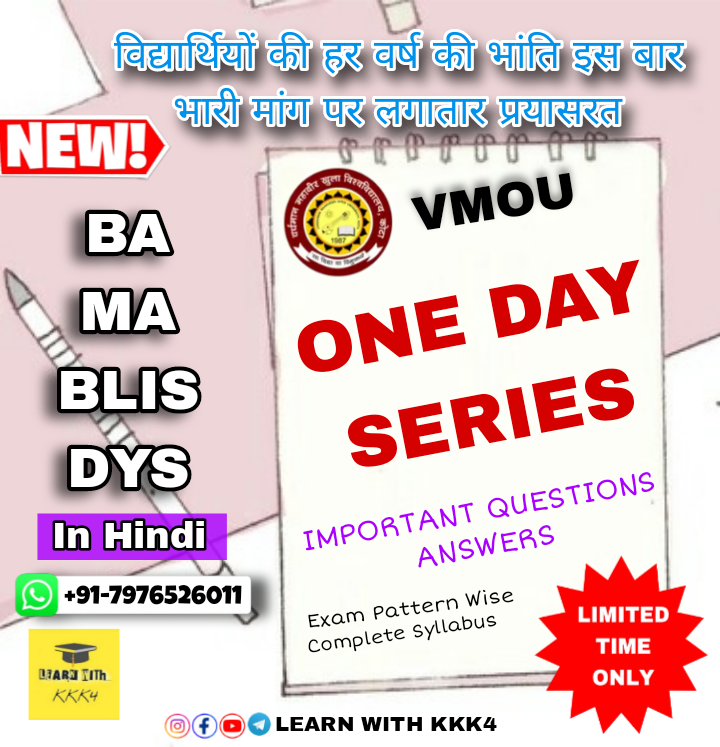VMOU MASO-05 Paper MA 2ND Year ; vmou exam paper
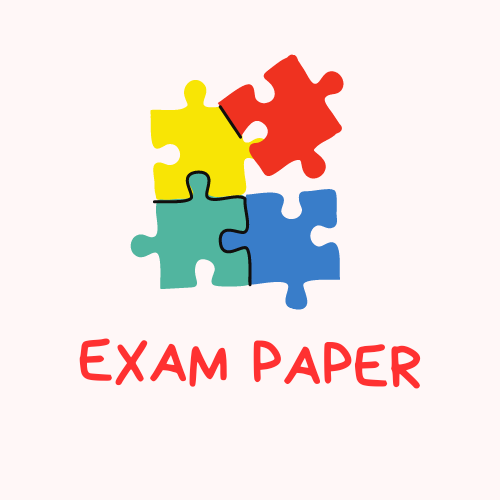
VMOU MA 2ND Year के लिए समाजशास्त्र ( MASO-05 , ) का पेपर उत्तर सहित दे रखा हैं जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे उन सभी को शामिल किया गया है आगे इसमे पेपर के खंड वाइज़ प्रश्न दे रखे हैं जिस भी प्रश्नों का उत्तर देखना हैं उस पर Click करे –
Section-A
प्रश्न-1.’एन इनविटेशन टू सोशियोलॉजी’ किसकी रचना है?
उत्तर:- पीटर एल. बर्जर (Peter L. Berger)
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.’नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी’ पुस्तक के लेखक कौन हैं?
उत्तर:- एलन जॉनसन (Alan Johnson)
प्रश्न-3.’द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड’ के लेखक कौन हैं?
उत्तर:- एमिल दुर्खीम (Emile Durkheim)
प्रश्न-4 कौन-सा समाजशास्त्रीय सिद्धांत लोगों के ‘दैनंदिन जीवन-जगत’ का अध्ययन करना पसंद करता है?
उत्तर:- प्रतीकात्मक अन्तःक्रियावाद
प्रश्न-5. ‘ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर’ के लेखक बताइए।
उत्तर:- चार्ल्स हॉर्टन कूले (Charles Horton Cooley)
प्रश्न-6. ‘पॉवर इलीट’ पुस्तक के लेखक कौन हैं?
उत्तर:- पॉवर इलीट’ पुस्तक के लेखक सी. राइट मिल्स (C. Wright Mills) हैं।
प्रश्न-7. माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी’ के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर:- जॉर्ज हर्बर्ट मीड (George Herbert Mead)
प्रश्न-8. जे. हैबरमास की किन्हीं दो पुस्तकों का नाम लिखिए।
उत्तर:- The Theory of Communicative Action, Knowledge and Human Interests
प्रश्न-9. ‘मध्यवर्ती सिद्धांतों’ की अवधारणा किसने दी?
उत्तर:- रॉबर्ट के. मर्टन ने ‘मध्यवर्ती सिद्धांतों’ (Middle Range Theories) की अवधारणा दी।
प्रश्न-10. समाजशास्त्र में ‘आदर्श प्रारूप’ की अवधारणा किसकी देन है?
उत्तर:-मैक्स वेबर ने ‘आदर्श प्रारूप’ (Ideal Types) की
प्रश्न-11. ‘द्वंद्वात्मक भौतिकवाद’ की स्थापना किसने की?
उत्तर:- कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने
प्रश्न-12. तथ्य को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- तथ्य वह वस्तुनिष्ठ यथार्थ होता है जिसे प्रत्यक्ष अनुभव या अवलोकन द्वारा सत्यापित किया जा सकता है
प्रश्न-13. उद्विकास को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- उद्विकास एक प्रक्रिया है जिसमें जीव या समाज सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर क्रमिक रूप से विकसित होते हैं।
प्रश्न-14. उत्तेजन’ से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- उत्तेजन (Stimulus) वह बाहरी या आंतरिक संकेत है जो किसी प्रतिक्रिया या व्यवहार को उत्पन्न करता है।
प्रश्न-15. सामाजिक तथ्य को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- सामाजिक तथ्य वे बाह्य और बाध्यकारी नियम होते हैं जो व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करते हैं — दुर्खीम।
प्रश्न-16. चर को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- चर वह गुण है जो विभिन्न व्यक्तियों या समूहों में बदलता रहता है।
प्रश्न-17. उपकल्पना को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- उपकल्पना एक अस्थायी कथन या अनुमान है जिसे परीक्षण और विश्लेषण के माध्यम से सत्यापित किया जाता है
प्रश्न-18. प्रत्यक्षवाद को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:-प्रत्यक्षवाद वह दृष्टिकोण है जो सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और अनुभवजन्य अध्ययन पर बल देता है।
प्रश्न-19. प्रकार्य’ को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- प्रकार्य किसी संस्था या तत्व द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया कार्य होता है
प्रश्न-20. ऐतिहासिक भौतिकवाद को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- यह एक सिद्धांत है जिसके अनुसार भौतिक आर्थिक स्थितियाँ इतिहास के विकास का आधार होती हैं।
प्रश्न-21. सामाजिक मानदण्ड को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:-सामाजिक मानदण्ड वे नियम हैं जो समाज में स्वीकार्य व्यवहार को निर्धारित करते हैं।
प्रश्न-22. विकास को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:- विकास वह प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक व तकनीकी उन्नति होती है।
प्रश्न-23. उदविकासीय सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में से दो नाम लिखिए।
उत्तर:- हर्बर्ट स्पेंसर, आगस्ट कॉन्त
प्रश्न-24. प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी?
उत्तर:-ऑगस्त कॉन्ते (Auguste Comte) ने
प्रश्न-25. प्रकार्यात्मक अध्ययन के कोई दो लक्षण लिखिए।
उत्तर:- (1) समाज को एक समग्र इकाई माना जाता है। (2) प्रत्येक संस्था की समाज में एक विशिष्ट भूमिका होती है।
प्रश्न-26. किन्हीं दो संघर्षवादी विचारकों के नाम का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- कार्ल मार्क्स और राल्फ डाहरेंडोर्फ।
प्रश्न-27. प्रत्ययनशास्त्र से जुड़े किन्हीं दो सामाजिक विचारकों के नाम लिखिए।
उत्तर:- एडमंड हसर्रल (Edmund Husserl) और अल्फ्रेड शुट्ज़ (Alfred Schutz)।
प्रश्न-28. ‘सामाजिक जीववाद’ से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- सामाजिक जीववाद समाज की तुलना एक जीवित जीव से करता है जिसमें सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं।
प्रश्न-29. ऐतिहासिक पद्धति को कोई दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- 1. यह घटनाओं के कालक्रम और कारणों का अध्ययन करती है। 2.यह प्राथमिक स्रोतों (दस्तावेज़, अभिलेख आदि) पर आधारित होती है।
प्रश्न-30. सिद्धान्त की दो विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:- (1) सिद्धान्त व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता है। (2) यह अनुभवों की व्याख्या और भविष्यवाणी करने में सहायक होता है।
प्रश्न-31. प्रत्यक्षवाद से सम्बंधित किसी एक चिंतक का नाम बताइए।
उत्तर:-ओगस्त कॉन्ते (Auguste Comte) प्रत्यक्षवाद से सम्बंधित प्रमुख चिंतक हैं।
प्रश्न-32. सतत विकास की सार्थक बनाने वाली दो पूर्व शर्ते लिखिए।
उत्तर:- पर्यावरणीय संरक्षण। संसाधनों का न्यायसंगत और विवेकपूर्ण उपयोग।
प्रश्न-33. नृजाति पद्धति की कोई दो अध्ययन पद्धतियाँ लिखिए।
उत्तर:- वार्तालाप विश्लेषण (Conversation Analysis), प्रेक्षण (Observation)
Section-B
प्रश्न-1.मर्टन द्वारा बताये गये सिद्धान्त और अनुसंधान के बीच के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त कीजिए।
उत्तर:- रॉबर्ट के. मर्टन ने सिद्धांत (Theory) और अनुसंधान (Research) के बीच घनिष्ठ पारस्परिक संबंध की व्याख्या की। मर्टन के अनुसार, सिद्धांत और अनुसंधान एक-दूसरे के पूरक हैं। न तो केवल सिद्धांत पर्याप्त होता है और न ही मात्र अनुभवजन्य अनुसंधान। उन्होंने ‘मध्यवर्ती सिद्धांतों’ (Middle Range Theories) की अवधारणा दी, जो कि बहुत व्यापक या अमूर्त न होकर विशिष्ट सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं और जिनका परीक्षण अनुभवजन्य अनुसंधान द्वारा किया जा सकता है।
मर्टन के अनुसार, अनुसंधान से सिद्धांतों का विकास होता है और सिद्धांत अनुसंधान को दिशा प्रदान करते हैं। अनुसंधान सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण करता है, जबकि सिद्धांत सामाजिक वास्तविकता को समझने की एक रूपरेखा प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण ने समाजशास्त्र में एक वैज्ञानिक पद्धति को बल प्रदान किया और अनुभव और वैचारिक विश्लेषण के बीच की दूरी को पाटने में मदद की। मर्टन का यह योगदान समाजशास्त्रीय पद्धति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.स्मैंगलर द्वारा प्रतिपादित परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- ओस्वाल्ड स्पैंगलर (Spengler) ने परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत (Theory of Circular Change) प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक “The Decline of the West” में विस्तार से बताया। इस सिद्धांत के अनुसार, सभी सभ्यताएं एक निश्चित चक्र में विकसित होती हैं—जन्म, विकास, परिपक्वता और पतन।
स्पैंगलर के अनुसार, सभ्यताएं भी जीवों की तरह होती हैं जिनका एक जीवन-चक्र होता है। उनकी राय में कोई भी संस्कृति स्थायी नहीं होती; हर संस्कृति अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद पतन की ओर अग्रसर होती है। उन्होंने मिस्र, भारतीय, चीनी, पश्चिमी आदि कई सभ्यताओं का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक का पतन अनिवार्य होता है।
स्पैंगलर ने आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को भी इसी चक्रीय प्रक्रिया में पतनशील अवस्था में बताया। उनके अनुसार सभ्यताओं का अंत बाहरी शक्तियों के कारण नहीं होता बल्कि आंतरिक सांस्कृतिक क्षरण के कारण होता है।
यह सिद्धांत इतिहास और समाज को स्थिर न मानकर उन्हें गतिशील और परिवर्तनशील मानता है, परंतु इसकी आलोचना इस आधार पर भी हुई कि यह अत्यधिक निराशावादी और नियतिवादी (Deterministic) है।
प्रश्न-3.सामाजिक व्यवहारवाद क्या है?
उत्तर:- सामाजिक व्यवहारवाद (Social Behaviorism) एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है जिसकी नींव जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने रखी। यह सिद्धांत मानता है कि मानव व्यवहार केवल जैविक या व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होता है। इस सिद्धांत का मुख्य फोकस ‘स्व’ (Self) और ‘समाज’ (Society) के बीच के संबंध पर होता है।
मीड ने बताया कि व्यक्ति अपने व्यवहार को समाज के अन्य सदस्यों के साथ संवाद और सांकेतिक प्रतीकों (Symbols) के माध्यम से विकसित करता है। उदाहरण के लिए, भाषा और इशारे जैसे प्रतीक, व्यक्ति को समाज में भूमिका निभाने में सहायता करते हैं। मीड के अनुसार, “स्व” (Self) दो भागों में विभाजित होता है—‘I’ और ‘Me’। ‘Me’ सामाजिक अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है जबकि ‘I’ आत्म-प्रतिक्रिया है।
इस सिद्धांत ने प्रतीकात्मक अन्तःक्रियावाद (Symbolic Interactionism) की नींव रखी और यह दिखाया कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक संरचना से प्रभावित होता है और समाज के साथ निरंतर संपर्क में बदलता रहता है।
प्रश्न-4.आलोचनात्मक समाजशास्त्र के अनुसार प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों की प्रमुख कमियाँ क्या हैं?
उत्तर:- आलोचनात्मक समाजशास्त्र (Critical Sociology), विशेष रूप से फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों द्वारा प्रत्यक्षवादी (Positivist) सिद्धांतों की कई प्रमुख कमियाँ बताई गईं।
मानव चेतना की उपेक्षा – प्रत्यक्षवाद मानव व्यवहार को वस्तु-जैसा समझता है और उसमें स्वायत्त चेतना व अनुभवों की उपेक्षा करता है।
मूल्य-निरपेक्षता का भ्रम – यह मानता है कि वैज्ञानिक अध्ययन पूरी तरह से निष्पक्ष और मूल्य-रहित हो सकता है, जबकि आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहता है कि समाजशास्त्र में मूल्यों की भूमिका अपरिहार्य है।
समाज में बदलाव की क्षमता की उपेक्षा – प्रत्यक्षवाद वर्तमान सामाजिक ढांचे को निष्पक्ष रूप से देखने का प्रयास करता है, जिससे शोषण और असमानता जैसे मुद्दे अनदेखे रह जाते हैं।
मानव एजेंसी की अवहेलना – यह समाज को संरचना के रूप में देखता है और व्यक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति को नगण्य मानता है।
इस प्रकार, आलोचनात्मक समाजशास्त्र ने प्रत्यक्षवाद की सीमाओं को उजागर कर समाजशास्त्रीय सोच को अधिक मानवीय, नैतिक और परिवर्तनकारी दिशा दी।
प्रश्न-5.पीटर एम. ब्लाउ के संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- पीटर एम. ब्लाउ (Peter M. Blau) ने संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत (Structural Exchange Theory) प्रस्तुत किया, जो कि सामाजिक व्यवहार को विनिमय की दृष्टि से देखता है। इस सिद्धांत के अनुसार, समाज के सदस्य आपसी संबंधों में लाभ-हानि का मूल्यांकन करते हैं और जहां लाभ अधिक होता है, वहां संबंध बनाए रखते हैं।
ब्लाउ ने कहा कि सभी सामाजिक संबंध किसी न किसी प्रकार के विनिमय पर आधारित होते हैं—यह विनिमय भौतिक भी हो सकता है और सांस्कृतिक या भावनात्मक भी। जैसे, व्यक्ति प्रशंसा, सहयोग या सामाजिक प्रतिष्ठा की अपेक्षा से कार्य करता है।
ब्लाउ का योगदान यह था कि उन्होंने व्यक्तिगत स्तर के विनिमय से ऊपर उठकर सामाजिक संरचना की व्याख्या की। उनके अनुसार, विनिमय संबंधों से सत्ता, नियंत्रण और सामाजिक स्तरीकरण (Social Stratification) जैसी संरचनाएं निर्मित होती हैं। जैसे-जैसे विनिमय असमान होता है, एक पक्ष प्रभावशाली बन जाता है।
इस सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक संरचनाएं केवल नियमों और संस्थाओं से नहीं बनती, बल्कि व्यक्ति-व्यक्ति के व्यवहारों और विनिमयों से भी निर्मित होती हैं।
प्रश्न-6.सोरोकिन के सांस्कृतिक गत्यात्मकता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:- पितिरिम सोरोकिन (Pitirim Sorokin) ने सांस्कृतिक गत्यात्मकता (Cultural Dynamics) का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार समाजों और संस्कृतियों का विकास तीन प्रमुख प्रकार की संस्कृति प्रणालियों के बीच होता है:
इन्द्रियवादी संस्कृति (Sensate Culture) – जो भौतिकता और इंद्रिय सुखों पर आधारित होती है।
आदर्शवादी संस्कृति (Idealistic Culture) – जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्वों को महत्व देती है।
वैचारिक/धार्मिक संस्कृति (Ideational Culture) – जो आध्यात्मिकता और आत्मिक मूल्यों को प्रधानता देती है।
सोरोकिन का मानना था कि समाज इन तीनों प्रणालियों के बीच चक्रीय रूप से बदलते रहते हैं। जब एक प्रकार की संस्कृति चरम पर पहुंच जाती है और अपनी उपयोगिता खो देती है, तो समाज अगली संस्कृति की ओर अग्रसर होता है।
इस सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि सांस्कृतिक परिवर्तन न तो एकरेखीय होता है और न ही पूर्णतः यादृच्छिक, बल्कि उसमें कुछ चक्रीय नियम दिखाई देते हैं। सोरोकिन ने यह भी कहा कि अत्यधिक भौतिकतावादी संस्कृति (Sensate) अंततः समाज में नैतिक पतन और अराजकता लाती है, जिससे पुनः आध्यात्मिक मूल्यों की ओर झुकाव होता है। यह सिद्धांत आज भी सांस्कृतिक अध्ययन में अत्यंत प्रभावी है।
प्रश्न-7.वृहद सिद्धांत को विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:- वृहद सिद्धान्त (Macro Theory) समाज के व्यापक ढाँचे और संरचनाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं:
- समाज का समग्र दृष्टिकोण – वृहद सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज या बड़ी सामाजिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं जैसे – वर्ग, संस्थाएँ, राज्य आदि।
- संरचनात्मक विश्लेषण – ये सिद्धान्त सामाजिक ढाँचों, भूमिकाओं और उनके आपसी संबंधों की व्याख्या करते हैं।
- सामाजिक प्रक्रियाओं पर बल – वृहद सिद्धान्त सामाजिक स्थिरता, परिवर्तन, व्यवस्था और संघर्ष जैसी प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं।
- न्यायिक विश्लेषण – समाज को एक संगठित प्रणाली मानते हुए उसके कार्यात्मक पहलुओं को समझाते हैं।
- विचारधारात्मक प्रभाव – ये सिद्धान्त किसी वैचारिक दृष्टिकोण (जैसे मार्क्सवाद, संरचनात्मक-कार्यात्मकवाद) से प्रेरित होते हैं।
इस प्रकार, वृहद सिद्धान्त समाजशास्त्र में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि वे समाज की व्यापक समझ प्रदान करते हैं।
सेक्शन ब का प्रश्न -18 भी देखे
प्रश्न-8.नव-मार्क्सवाद क्या है ?
उत्तर:- नव-मार्क्सवाद (Neo-Marxism) मार्क्सवाद का एक परिष्कृत रूप है, जो पारंपरिक मार्क्सवादी विचारों की सीमाओं को पहचानते हुए उन्हें आधुनिक संदर्भों में ढालने का प्रयास करता है। यह विचारधारा आर्थिक निर्धारणवाद (Economic Determinism) से आगे बढ़कर संस्कृति, विचारधारा, भाषा, शिक्षा और मीडिया जैसे पहलुओं को भी सामाजिक नियंत्रण के उपकरण मानती है।
फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक जैसे – थिओडोर अडोर्नो, मैक्स हॉरखाइमर, हर्बर्ट मार्कूजे, एंटोनियो ग्राम्शी आदि प्रमुख नव-मार्क्सवादी रहे हैं। ग्राम्शी ने “हेजेमनी” की अवधारणा दी, जिसके अनुसार सत्ताधारी वर्ग केवल भौतिक साधनों से नहीं बल्कि विचारों के माध्यम से भी वर्चस्व कायम करता है। नव-मार्क्सवाद पूंजीवाद की आलोचना करता है, लेकिन उसे केवल आर्थिक शोषण तक सीमित नहीं रखता, बल्कि सांस्कृतिक शोषण और विचारधारा के प्रभाव को भी विश्लेषण में शामिल करता है। यह समकालीन पूंजीवाद के जटिल स्वरूप को समझने में सहायक है।
प्रश्न-9. सिद्धांत निर्माण में आने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:- सिद्धांत निर्माण (Theory Building) एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक समस्याएँ आती हैं:
- सामाजिक वास्तविकता की जटिलता – समाज बहुआयामी और परिवर्तनशील होता है, जिसे सामान्यीकृत रूप में प्रस्तुत करना कठिन होता है।
- माप की कठिनाई – कई सामाजिक अवधारणाएँ (जैसे प्रेम, संस्कृति, मूल्य) को मापा नहीं जा सकता, जिससे अनुभवजन्य पुष्टि मुश्किल होती है।
- पारदर्शिता की कमी – सामाजिक व्यवहार हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः उसका विश्लेषण चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- मानवीय पक्षपात – शोधकर्ता की वैयक्तिक मान्यताएँ सिद्धांत निर्माण को प्रभावित कर सकती हैं।
- सांस्कृतिक विविधता – विभिन्न समाजों की विविधताओं के कारण कोई एक सार्वभौमिक सिद्धांत बनाना कठिन है।
- डेटा की अपर्याप्तता – पर्याप्त और विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव सिद्धांत के निर्माण में बाधा बनता है।
इन समस्याओं के बावजूद, समाजशास्त्र में सतत प्रयासों से नए सिद्धांतों का निर्माण होता रहा है।
प्रश्न-10. सोरीकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धान्त स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-पिटिरिम सोरीकिन ने सांस्कृतिक गतिशीलता (Cultural Mobility) का सिद्धान्त प्रस्तुत किया, जो यह बताता है कि संस्कृति स्थिर नहीं रहती, बल्कि वह लगातार परिवर्तनशील होती है।
उन्होंने तीन प्रमुख सांस्कृतिक प्रणालियाँ बताई:
- संवेदी (Sensate) – जहाँ भौतिकता, विज्ञान और इंद्रिय सुखों को प्राथमिकता दी जाती है।
- आदर्शवादी (Idealistic) – जिसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का संतुलन होता है।
- आध्यात्मिक (Ideational) – जहाँ आत्मा, धर्म, और ईश्वर के प्रति विश्वास को सर्वोपरि माना जाता है।
सोरीकिन के अनुसार, समाज इन तीनों प्रणालियों के बीच चक्राकार रूप से गतिशील रहता है। जब एक प्रणाली चरम पर पहुँचती है और असंतुलित हो जाती है, तो समाज दूसरी प्रणाली की ओर बढ़ता है।
सीरोकिन के अनुसार समाज इन तीनों संस्कृतियों के चक्र में गतिशील रहता है। जब एक संस्कृति चरम पर पहुंचती है, तो वह स्वयं को नष्ट कर देती है और दूसरी संस्कृति जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी सभ्यता इंद्रियवादी संस्कृति की ओर अत्यधिक झुकाव दिखा रही है, जिससे वह असंतुलन की स्थिति में है। यह सिद्धांत संस्कृति की स्थायित्व और परिवर्तनशीलता दोनों को समझने में सहायक है।यह सिद्धान्त यह भी बताता है कि संस्कृति का विकास केवल तकनीकी उन्नति से नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और आस्थाओं के परिवर्तन से भी होता है।
प्रश्न-11. नृजातिपद्धतिशास्त्र के क्षेत्र में गर्फिंकेल के योगदान बताइए।
उत्तर:- हेरोल्ड गर्फिंकेल (Harold Garfinkel) ने समाजशास्त्र में ‘नृजातिपद्धतिशास्त्र’ (Ethnomethodology) की स्थापना की, जो यह अध्ययन करता है कि सामान्य लोग अपने दैनिक जीवन में सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाते और बनाए रखते हैं। गर्फिंकेल का मुख्य उद्देश्य यह था कि सामाजिक व्यवस्था को एक ‘प्राकृतिक’ तथ्य न मानकर, उसे लोगों की सक्रिय मानसिक प्रक्रिया का परिणाम माना जाए।
उन्होंने बताया कि सामाजिक नियमों का पालन केवल बाहर से थोपा गया नहीं होता, बल्कि लोग स्वयं उन्हें हर दिन ‘पुनः-निर्मित’ करते हैं। गर्फिंकेल ने ‘ब्रीच प्रयोग’ (Breaching Experiments) के माध्यम से यह दिखाया कि जब हम सामान्य सामाजिक अपेक्षाओं को तोड़ते हैं, तब लोग कितनी तेजी से स्थिति को ‘सामान्य’ करने की कोशिश करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सामाजिक व्यवहार गहराई से नियमबद्ध और प्रक्रिया-आधारित होता है।
गर्फिंकेल का कार्य समाज की आंतरिक कार्यविधियों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है और यह दिखाता है कि सामान्य व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करता है। नृजातिपद्धतिशास्त्र आज समाजशास्त्रीय अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति बन चुकी है।
प्रश्न-12. अवधारणा और सिद्धान्त के बीच सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- अवधारणा (Concept) और सिद्धान्त (Theory) समाजशास्त्र के मूलभूत तत्व हैं। अवधारणा किसी वस्तु, घटना या प्रक्रिया की बौद्धिक समझ होती है जो अनुभवजन्य तथ्य को सामान्यीकृत रूप में व्यक्त करती है। उदाहरणस्वरूप, ‘वर्ग’, ‘स्थानान्तरण’, ‘सामाजिक स्तरीकरण’ आदि अवधारणाएँ हैं।
सिद्धान्त, अवधारणाओं का एक व्यवस्थित ढांचा होता है जो सामाजिक घटनाओं को समझाने, पूर्वानुमान लगाने और व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरणस्वरूप, मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धान्त। सिद्धान्त में कई अवधारणाएँ आपस में संगठित होकर एक स्पष्ट संरचना बनाती हैं।
इस प्रकार, अवधारणा सिद्धान्त की आधारशिला है। बिना अवधारणा के कोई भी सिद्धान्त विकसित नहीं किया जा सकता। वहीं सिद्धान्त, अवधारणाओं को एक तार्किक एवं विश्लेषणात्मक ढाँचे में प्रस्तुत करता है। अतः अवधारणा और सिद्धान्त का संबंध पूरक है—अवधारणा सिद्धान्त को जन्म देती है, और सिद्धान्त अवधारणाओं को अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करता है।
प्रश्न-13. जातिपद्धतिशास्त्र के संदर्भ में गारफिंकल का योगदान स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- हेरोल्ड गारफिंकल (Harold Garfinkel) जातिपद्धतिशास्त्र (Ethnomethodology) के संस्थापक माने जाते हैं। यह सिद्धान्त यह समझने का प्रयास करता है कि साधारण लोग दैनिक जीवन में सामाजिक व्यवस्था कैसे बनाए रखते हैं।
गारफिंकल का मानना था कि समाजशास्त्र को केवल संस्थाओं और संरचनाओं पर नहीं, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की क्रियाओं और बातचीत पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि लोग आपसी संवाद और प्रतीकों के माध्यम से अर्थ का निर्माण करते हैं।
उन्होंने ‘ब्रीच प्रयोग’ (Breaching Experiments) का प्रयोग करके यह दिखाया कि जब सामान्य सामाजिक मानकों का उल्लंघन किया जाता है, तो लोग असहज हो जाते हैं और व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
इस प्रकार, गारफिंकल ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक वास्तविकता कोई ठोस संरचना नहीं है, बल्कि यह लगातार लोगों की पारस्परिक क्रिया से निर्मित होती रहती है।
प्रश्न-14.जॉर्ज होमान्स के विनिमय व्यवहारवाद की अवधारणा को वर्णन कीजिए।
उत्तर:- जॉर्ज होमान्स ने सामाजिक व्यवहार को आर्थिक लेन-देन की तरह समझने का प्रयास किया जिसे “विनिमय व्यवहारवाद” (Exchange Behaviourism) कहा जाता है।
होमान्स के अनुसार, सामाजिक व्यवहार पुरस्कार (rewards) और लागत (costs) पर आधारित होता है। व्यक्ति वही व्यवहार करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि हो।
उनका सिद्धान्त छह प्रमुख प्रस्तावों पर आधारित है, जिनमें से प्रमुख हैं:
- सफलता प्रस्ताव (Success Proposition) – जिस व्यवहार से लाभ मिलता है, उसे दोहराया जाता है।
- मूल्य प्रस्ताव (Value Proposition) – जो व्यवहार व्यक्ति को मूल्यवान लगे, वह उसे अपनाता है।
- वंचन प्रस्ताव (Deprivation-Satiation Proposition) – बार-बार पुरस्कार मिलने से उसकी आकर्षण शक्ति कम हो जाती है।
होमान्स ने समाज को जटिल संबंधों के नेटवर्क के रूप में देखा, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति विनिमय संबंधों में संलग्न होता है। यह सिद्धान्त व्यवहार को विश्लेषित करने के लिए मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को जोड़ता है।
प्रश्न-15. समाजशास्त्रीय सिद्धान्त की उपयोगिताओं पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- समाजशास्त्रीय सिद्धान्त समाज के अध्ययन, विश्लेषण एवं समझने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इनकी प्रमुख उपयोगिताएँ निम्नलिखित हैं:
- समझ एवं व्याख्या – सिद्धान्त सामाजिक व्यवहार, संस्थाओं और प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं।
- अनुसंधान का मार्गदर्शन – सिद्धान्त अनुसंधान के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिससे शोध की दिशा और उद्देश्य स्पष्ट होता है।
- सामाजिक समस्याओं का समाधान – सामाजिक विषमता, अपराध, गरीबी जैसी समस्याओं के कारणों को समझने में सिद्धान्त सहायक होते हैं।
- नीति निर्माण में सहायक – समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर सरकारें एवं संस्थाएँ प्रभावी नीतियाँ बना सकती हैं।
- विकास एवं परिवर्तन का विश्लेषण – सिद्धान्त यह स्पष्ट करते हैं कि समाज में परिवर्तन कैसे और क्यों होता है।
अतः समाजशास्त्रीय सिद्धान्त सामाजिक वास्तविकताओं को बेहतर समझने और सामाजिक सुधार की दिशा में कार्य करने हेतु एक सशक्त उपकरण सिद्ध होते हैं।
प्रश्न-16. प्रतीकात्मक अन्तःक्रियावाद के मौलिक आधार स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- प्रतीकात्मक अन्तःक्रियावाद (Symbolic Interactionism) एक सूक्ष्म समाजशास्त्रीय सिद्धान्त है जो यह बताता है कि लोग एक-दूसरे के साथ प्रतीकों और अर्थों के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं। इसके प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं:
- अर्थ की महत्ता – मनुष्य अपने कार्यों का अर्थ स्वयं निर्मित करता है और वही अर्थ उसके व्यवहार को निर्देशित करता है।
- प्रतीकों का प्रयोग – भाषा, संकेत, वस्त्र, हाव-भाव आदि प्रतीकों के माध्यम से सामाजिक अर्थ संप्रेषित होते हैं।
- मानव का सक्रिय रूप – मनुष्य केवल बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह उन्हें समझकर प्रतिक्रिया देता है।
- सामाजिक संदर्भ में आत्म की रचना – व्यक्ति का ‘स्व’ (Self) सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान निर्मित होता है।
इस सिद्धान्त के प्रमुख विचारक जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर हैं। यह दृष्टिकोण सामाजिक व्यवहार को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से समझने का सशक्त माध्यम प्रदान करता है।
प्रश्न-17. दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर:- एमिल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र का मूल विषय माना। उनके अनुसार सामाजिक तथ्य (Social Facts) वे तरीके, नियम, या विश्वास हैं जो व्यक्ति पर बाहरी रूप से थोपे जाते हैं और जिनका उसके व्यवहार पर नियंत्रण होता है।
सामाजिक तथ्यों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- बाह्य (Externality): सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाहर अस्तित्व रखते हैं। वे व्यक्ति के जन्म से पहले से समाज में विद्यमान होते हैं।
- बाध्यकारी शक्ति (Constraint): ये तथ्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यदि व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता, तो समाज दंड देता है।
- सामूहिक चेतना (Collective Conscience): सामाजिक तथ्य समाज के सामूहिक विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होते हैं और एक प्रकार की सामाजिक चेतना को प्रकट करते हैं।
- वस्तुनिष्ठता (Objectivity): सामाजिक तथ्य का अध्ययन वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाना चाहिए, जैसे प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन होता है।
दुर्खीम के अनुसार, आत्महत्या, कानून, धर्म, नैतिकता, भाषा आदि सभी सामाजिक तथ्य हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र की मुख्य जिम्मेदारी है।
प्रश्न-18. समाजशास्त्र के वृहद सिद्धांतों की सूची बनाइए।
उत्तर:- समाजशास्त्र में वृहद (Macro) सिद्धांत वे हैं जो समाज की बड़ी संरचनाओं, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इनके माध्यम से समाज के समग्र रूप को समझा जाता है। प्रमुख वृहद सिद्धांतों की सूची निम्नलिखित है:
सांस्कृतिक सिद्धांत (Cultural Theory) – यह सिद्धांत संस्कृति की भूमिका और प्रभाव को समाज की संरचना में मुख्य रूप से देखता है।
संरचनात्मक प्रकार्यवाद (Structural Functionalism) – यह सिद्धांत समाज को एक व्यवस्थित तंत्र मानता है जहाँ प्रत्येक संस्था का एक विशिष्ट कार्य होता है। प्रमुख चिंतक: टैल्कॉट पार्सन्स, रोबर्ट के. मर्टन।
संघर्ष सिद्धांत (Conflict Theory) – यह सिद्धांत समाज में वर्ग संघर्ष और असमानता पर केंद्रित है। प्रमुख चिंतक: कार्ल मार्क्स।
प्रणाली सिद्धांत (System Theory) – यह समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है जिसमें विभिन्न अवयव आपस में जुड़े होते हैं।
कार्यात्मक साम्यवाद (Neo-functionalism) – यह प्रकार्यवाद का परिष्कृत रूप है जिसमें सामाजिक परिवर्तन को भी महत्व दिया जाता है। प्रमुख चिंतक: जेफरी अलेक्जेंडर।
प्रश्न-19. रेडिकल समाजशास्त्र के कोई दो उद्देश्य लिखिए।
उत्तर:- रेडिकल समाजशास्त्र पारंपरिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों की आलोचना करता है और समाज में व्याप्त असमानताओं, शोषण, तथा प्रभुत्व की संरचनाओं को उजागर करता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- सामाजिक अन्याय और दमन के विरुद्ध चेतना विकसित करना: रेडिकल समाजशास्त्र समाज में वर्ग, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर होने वाले शोषण को उजागर करता है और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करता है।
- सामाजिक परिवर्तन की पहल करना: यह सिद्धांत केवल समाज की व्याख्या नहीं करता, बल्कि उसे बदलने की आवश्यकता पर जोर देता है। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी सोच को बढ़ावा देना और वैकल्पिक सामाजिक संरचना की कल्पना करना है।
रेडिकल समाजशास्त्र मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होता है और इसे एक “क्रांतिकारी समाजशास्त्र” भी कहा जाता है।
सेक्शन c प्रश्न 7 भी देखे
प्रश्न-20. रोबर्ट के. मर्टन के अनुसार प्रकार्यवाद की तीन अभिधारणाएँ क्या हैं?
उत्तर:- रोबर्ट के. मर्टन ने प्रकार्यवाद (Functionalism) की आलोचना करते हुए इसे और अधिक यथार्थवादी बनाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रकार्यवाद की तीन प्रमुख अभिधारणाओं (Postulates) की पहचान की:
- सर्वव्यापकता की अभिधारणा (Postulate of Universal Functionalism): पारंपरिक प्रकार्यवाद मानता है कि समाज की हर संस्था का कोई न कोई सकारात्मक कार्य होता है। मर्टन ने कहा कि यह मान्यता गलत है — सभी कार्य नकारात्मक भी हो सकते हैं।
- सहमति की अभिधारणा (Postulate of Functional Unity of Society): यह धारणा कहती है कि समाज की सभी संस्थाएँ आपस में सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़ी होती हैं। मर्टन ने इस पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि समाज में विरोध और असंगति भी मौजूद रहती है।
- अनिवार्यता की अभिधारणा (Postulate of Indispensability): यह मान्यता थी कि प्रत्येक सामाजिक संस्था अपरिहार्य है। मर्टन ने इसका खंडन करते हुए कहा कि एक संस्था के कार्य को अन्य संस्था भी कर सकती है।
इस प्रकार मर्टन ने प्रकार्यवाद को अधिक लचीला और यथार्थवादी बनाने का कार्य किया।
प्रश्न-21. मार्शल मेकलुहन की विश्व गाँव की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- मार्शल मेकलुहन, एक कनाडाई मीडिया चिंतक थे, जिन्होंने ‘Global Village’ या “विश्व गाँव” की अवधारणा प्रस्तुत की। इस सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक संचार तकनीकों (विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट) ने दुनिया को इतना समीप ला दिया है कि यह एक छोटे से गाँव जैसा प्रतीत होता है।
मेकलुहन का तात्पर्य यह था कि जैसे एक गाँव में सभी व्यक्ति एक-दूसरे के जीवन से सीधे जुड़े होते हैं, वैसे ही वैश्विक संचार माध्यमों ने दुनिया के लोगों को आपस में जोड़ा है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से अब कोई भी घटना कुछ ही क्षणों में पूरी दुनिया तक पहुँच जाती है।
उन्होंने यह भी कहा था कि “माध्यम ही संदेश है” (The medium is the message), जिससे उनका आशय था कि संचार का माध्यम ही हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। ‘विश्व गाँव’ की अवधारणा वैश्वीकरण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सूचना क्रांति को समझने में अत्यंत सहायक है। यह आज के डिजिटल युग की सामाजिक संरचना का सार प्रस्तुत करती है।
प्रश्न-22. प्रघटनाशास्त्र के क्षेत्र में एडमंड हुसर्ल के योगदान को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- एडमंड हुसर्ल (Edmund Husserl) को प्रघटनाशास्त्र (Phenomenology) का जनक माना जाता है। उन्होंने दर्शन और समाजशास्त्र दोनों को गहराई से प्रभावित किया। हुसर्ल का मुख्य उद्देश्य “चेतना के अनुभव” का विश्लेषण करना था। उन्होंने यह कहा कि किसी भी वस्तु को समझने के लिए पहले उस पर आधारित हमारे अनुभव और चेतना को समझना आवश्यक है। उन्होंने ‘Intuition’, ‘Intentionality’ और ‘Epoché’ जैसी अवधारणाओं का विकास किया।
प्रघटनाशास्त्र का मूल उद्देश्य “चीजों को उनके स्वरूप में जानना” है — यानि वस्तुनिष्ठ और पूर्वग्रह रहित दृष्टि से देखना। समाजशास्त्र में हुसर्ल के विचारों का प्रभाव अल्फ्रेड शुट्ज और बर्गर-लुकमान जैसे समाजशास्त्रियों पर पड़ा, जिन्होंने ‘सार्थक सामाजिक क्रिया’ और ‘सामान्य ज्ञान’ जैसे पहलुओं का अध्ययन किया। हुसर्ल ने दिखाया कि सामाजिक दुनिया को समझने के लिए व्यक्तियों के अनुभवों को गंभीरता से लेना आवश्यक है।
प्रश्न-23. उद्विकासीय सिद्धांत की मान्यताओं को प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर:- उद्विकासीय सिद्धांत (Evolutionary Theory) यह मानता है कि समाज धीरे-धीरे सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर विकसित होता है। इसके प्रमुख सिद्धांतकार हर्बर्ट स्पेन्सर, अगस्ट कॉम्ट, और मॉर्गन रहे हैं। इस सिद्धांत की मुख्य मान्यताएँ निम्नलिखित हैं:
- क्रमिक विकास: समाज का विकास धीरे-धीरे, एक सतत प्रक्रिया के रूप में होता है।
- सरल से जटिल की ओर: समाज प्रारंभ में साधारण रूप में होता है, जो समय के साथ जटिल संरचनाओं और संस्थाओं का निर्माण करता है।
- समायोजन और अनुकूलन: समाज अपने परिवेश के अनुसार ढलता है और नया ज्ञान अपनाता है।
- प्राकृतिक चयन के समान प्रक्रिया: समाज में जो तत्व अनुकूल होते हैं, वही टिकते हैं।
प्रगति का विश्वास: यह मान्यता रहती है कि विकास समाज को बेहतर स्थिति की ओर ले जाता है।
यह सिद्धांत आधुनिक समाज के अध्ययन और तुलना के लिए आधार प्रदान करता है, लेकिन इसकी आलोचना यह कहकर की गई कि यह सभी समाजों को एक ही विकासात्मक मार्ग पर देखता है।
प्रश्न-24. अनुभविका अनुसंधान में समाजशास्त्रीय सिद्धांत की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-सामाजिक अनुसंधान में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अनुभविक (Empirical) अनुसंधान तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है, लेकिन यह तथ्य तभी उपयोगी बनते हैं जब उन्हें किसी सैद्धांतिक ढांचे के अंतर्गत विश्लेषित किया जाए। सिद्धांत अनुसंधान को दिशा देते हैं, अनुसंधान के प्रश्न तय करते हैं और डेटा के संग्रहण एवं व्याख्या में मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरणतः, संघर्ष सिद्धांत सामाजिक असमानताओं पर केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है, वहीं कार्यात्मकतावाद सामाजिक स्थिरता और संतुलन पर शोध को प्रेरित करता है। इस प्रकार सिद्धांत अनुभवजन्य शोध को केवल सूचनाओं के ढेर से एक वैज्ञानिक विश्लेषण की ओर अग्रसर करते हैं। इसके बिना शोध बिखरा हुआ और उद्देश्यहीन हो सकता है।
प्रश्न-25. समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:- समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ होती हैं:
- व्यवस्थित ढांचा: ये सिद्धांत सामाजिक तथ्यों को एक सुसंगठित रूप में प्रस्तुत करते हैं।
- सामाजिक प्रक्रिया की व्याख्या: यह सामाजिक संस्थाओं, संबंधों और प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हैं।
- परिकल्पनाओं का आधार: सिद्धांत कई परिकल्पनाओं पर आधारित होते हैं, जिन्हें अनुभवजन्य रूप से परखा जा सकता है।
- सामाजिक परिवर्तन की समझ: ये सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं।
- व्यापकता: ये केवल किसी एक घटना तक सीमित नहीं होते, बल्कि सामाजिक जीवन के कई पहलुओं को समाहित करते हैं।
पूर्वानुमान की क्षमता: सिद्धांत भविष्य की सामाजिक प्रवृत्तियों के बारे में अनुमान लगाने में सहायक होते हैं।
इस प्रकार समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक जगत को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का माध्यम हैं।
प्रश्न-26. विज्ञानों के संस्तरण में समाजशास्त्र की स्थिति स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- विज्ञानों के संस्तरण (Hierarchy of Sciences) की अवधारणा ओगस्ट कॉम्ट ने प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार विज्ञानों को उनके जटिलता और सामान्यता के आधार पर एक क्रम में रखा जाता है: गणित → खगोल विज्ञान → भौतिकी → रसायन विज्ञान → जीवविज्ञान → समाजशास्त्र। इस श्रृंखला में समाजशास्त्र को उच्चतम स्थान प्राप्त है क्योंकि यह सबसे जटिल विषय है, जिसमें मानव व्यवहार, संस्कृति, मूल्य, परंपराएं, संस्थाएं आदि का अध्ययन होता है। समाजशास्त्र को “मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज” भी कहा जाता है, क्योंकि यह मानव समाज के समग्र अध्ययन का कार्य करता है। यद्यपि इसमें सटीकता भौतिक विज्ञानों की तरह नहीं होती, फिर भी समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है और अनुभवजन्य डेटा पर आधारित होता है। अतः विज्ञानों के संस्तरण में इसकी भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट मानी जाती है।
प्रश्न-27. सीरोकिन के सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- प्रश्न 10 सेक्शन ब
प्रश्न-28.अवधारणा और सिद्धान्त के अन्तर्सम्बन्धों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
उत्तर:- प्रश्न 12 सेक्शन ब
प्रश्न-29. नृपद्धतिशास्त्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- नृपद्धतिशास्त्र (Ethnomethodology) की स्थापना हेरॉल्ड गारफिंकल ने की थी। यह दृष्टिकोण यह समझने का प्रयास करता है कि लोग अपने दैनिक जीवन में सामाजिक व्यवस्था को कैसे निर्मित और बनाए रखते हैं।
मुख्य विचार:
- लोग रोजमर्रा की बातचीत और व्यवहार में निहित सामान्य विधियों के द्वारा सामाजिक अर्थों की रचना करते हैं।
- यह परंपरागत समाजशास्त्र से भिन्न है, जो संरचनात्मक नियमों पर ध्यान केंद्रित करता है।
आलोचनात्मक विश्लेषण:
- सीमित दायरा: नृपद्धतिशास्त्र केवल सूक्ष्म (micro) स्तर की क्रियाओं पर ध्यान देता है और व्यापक सामाजिक संरचनाओं की उपेक्षा करता है।
- अत्यधिक वर्णनात्मक: यह अधिक व्याख्यात्मक और कम विश्लेषणात्मक होता है, जिससे सामाजिक बदलावों को समझना कठिन होता है।
- राजनीतिक दृष्टिकोण की कमी: यह सामाजिक असमानताओं या संघर्षों पर ध्यान नहीं देता, जिससे इसकी आलोचना होती है।
प्रश्न30.विकास के सांस्कृतिक उपागम को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:- विकास के सांस्कृतिक उपागम में यह मान्यता है कि आर्थिक और सामाजिक विकास केवल तकनीकी और पूंजीगत साधनों से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों से भी प्रभावित होता है।
मुख्य विचार:
- विकास की प्रक्रिया समाज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी होती है।
- यदि किसी समाज की संस्कृति नवाचार, शिक्षा और समानता को बढ़ावा देती है, तो विकास अधिक तीव्र होता है।
- परंपरागत मूल्यों, जातिवाद, लिंगभेद आदि अवरोधक भी बन सकते हैं।
उदाहरण:
- जापान में कार्य-संस्कृति, अनुशासन और श्रम के प्रति सम्मान ने तीव्र औद्योगिक विकास को संभव बनाया।
- भारत में कई क्षेत्रों में सामाजिक संरचनाएँ, जैसे जाति-व्यवस्था, विकास की राह में बाधा बनती हैं।
महत्व:
यह उपागम यह स्पष्ट करता है कि विकास के कार्यक्रम तभी सफल होंगे जब वे स्थानीय संस्कृति के अनुरूप होंगे। केवल आर्थिक योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं, उन्हें सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त बनाना अनिवार्य है।
Section-C
प्रश्न-1.कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
उत्तर:-कार्ल मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत (Conflict Theory) समाजशास्त्र में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है, जो समाज में वर्ग संघर्ष को केंद्र में रखता है। मार्क्स के अनुसार, इतिहास की समस्त घटनाएं वर्ग संघर्ष का परिणाम हैं, और सामाजिक परिवर्तन का मूल स्रोत उत्पादन के साधनों पर अधिकार को लेकर होने वाला टकराव है।
मुख्य तत्व:
- वर्ग विभाजन: मार्क्स ने समाज को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया — पूंजीपति वर्ग (Bourgeoisie) जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है, और श्रमिक वर्ग (Proletariat) जो अपनी श्रम शक्ति बेचकर जीविकोपार्जन करता है।
- शोषण: पूंजीपति वर्ग श्रमिकों के श्रम का शोषण करता है और श्रम का पूरा मूल्य नहीं देता। इस कारण श्रमिक वर्ग आर्थिक रूप से पीड़ित होता है।
- वर्ग संघर्ष: शोषण के विरुद्ध श्रमिक वर्ग में असंतोष उत्पन्न होता है और वह वर्ग चेतना (Class Consciousness) प्राप्त करता है। यह चेतना उन्हें शोषण के विरुद्ध संगठित संघर्ष की ओर ले जाती है।
- क्रांति और सामाजिक परिवर्तन: मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था अंततः अपने अंतर्विरोधों के कारण नष्ट हो जाएगी और श्रमिक वर्ग क्रांति कर एक वर्गविहीन समाज की स्थापना करेगा, जिसे समाजवाद कहा जाता है।
- ऐतिहासिक भौतिकवाद: मार्क्स ने कहा कि समाज की सभी संस्थाओं (धर्म, शिक्षा, राज्य) का आधार भौतिक उत्पादन होता है। जैसे-जैसे उत्पादन प्रणाली बदलती है, वैसे-वैसे सामाजिक संरचना और संस्थाएं भी बदलती हैं।
आलोचना:
मार्क्स का दृष्टिकोण आर्थिक निर्धारणवाद पर अधिक केंद्रित है और अन्य कारकों जैसे संस्कृति, लिंग, जाति आदि की भूमिका को कम महत्व देता है।
वह हिंसात्मक क्रांति पर अधिक विश्वास करते हैं, जबकि आधुनिक समाज में परिवर्तन अधिक शांतिपूर्ण तरीकों से होता है।
उनके द्वारा भविष्यवाणी की गई समाजवादी क्रांति बहुत से पूंजीवादी देशों में नहीं हुई।
मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत सामाजिक असमानताओं और सत्ता संबंधों को समझने का एक प्रभावशाली उपकरण है। यद्यपि इसकी सीमाएं हैं, फिर भी यह आज भी सामाजिक समस्याओं और शोषण की संरचनाओं को उजागर करने में उपयोगी है।
(जिस भी प्रश्न का उत्तर देखना हैं उस पर क्लिक करे)
प्रश्न-2.नारीवादी सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- नारीवादी सिद्धान्त (Feminist Theory) एक सामाजिक आंदोलन और वैचारिक दृष्टिकोण है, जो समाज में स्त्रियों की स्थिति, अधिकार, और उनके साथ होने वाले भेदभाव को समझने और चुनौती देने का प्रयास करता है। यह सिद्धान्त लैंगिक असमानताओं को उजागर करता है और समाज की पितृसत्तात्मक संरचना की आलोचना करता है।
मुख्य पहलू:
- पितृसत्ता की आलोचना: नारीवादी सिद्धान्त के अनुसार समाज की संरचना पुरुषों के वर्चस्व पर आधारित है। स्त्रियों को ऐतिहासिक रूप से द्वितीयक और अधीन स्थिति में रखा गया है।
- लैंगिक विभाजन: यह सिद्धान्त बताता है कि कैसे स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं और इन्हें प्राकृतिक मानकर स्त्रियों को सीमित किया जाता है।
- समान अधिकार की मांग: नारीवाद शिक्षा, रोजगार, राजनीति, स्वास्थ्य, और विवाह जैसे क्षेत्रों में स्त्रियों को समान अवसर और अधिकार दिलाने का समर्थन करता है।
- विभिन्न धाराएँ: नारीवाद कई धाराओं में विभाजित है जैसे — उदार नारीवाद (Liberal Feminism), समाजवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, और उत्तरआधुनिक नारीवाद। प्रत्येक धारा लैंगिक असमानता के कारणों और समाधान को अलग-अलग ढंग से प्रस्तुत करती है।
आलोचनात्मक पक्ष:
- नारीवादी सिद्धान्तों की कुछ धाराएँ केवल मध्यवर्गीय, श्वेत महिलाओं के अनुभवों पर आधारित रही हैं और विविधता (जाति, वर्ग, संस्कृति) को पर्याप्त स्थान नहीं देतीं।
- मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवाद को आर्थिक निर्धारणवाद का आरोप झेलना पड़ा है।
- कुछ आलोचकों का मानना है कि नारीवाद पुरुष विरोधी दृष्टिकोण अपनाता है, जबकि इसका उद्देश्य समानता है।
नारीवादी सिद्धान्त ने समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में लैंगिक दृष्टिकोण को सशक्त किया है। इसकी आलोचनाएं इसे और अधिक समावेशी और व्यवहारिक बनाने में सहायक रही हैं। आज यह केवल स्त्रियों तक सीमित न रहकर समग्र लैंगिक न्याय की दिशा में कार्य कर रहा है।
प्रश्न-3. उत्तर-आधुनिकतावाद का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
उत्तर:- आधुनिकतावाद (Postmodernism) 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा एक वैचारिक आंदोलन है, जो आधुनिकतावादी विचारों की आलोचना करता है। यह विज्ञान, प्रगति, तर्क और सार्वभौमिक सत्य जैसे आधुनिकतावादी मूल्यों को चुनौती देता है और बहुलता, अस्थिरता, विविधता और विखंडन पर बल देता है।
मुख्य विशेषताएँ:
- सार्वभौमिक सत्य की अस्वीकृति: उत्तर-आधुनिकतावाद यह मानता है कि कोई एक सार्वभौमिक सत्य नहीं होता, बल्कि सत्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भाषायी संदर्भों में निर्मित होते हैं।
- सत्ता और ज्ञान का संबंध: फूको जैसे विचारकों ने दिखाया कि कैसे ज्ञान सत्ता का उपकरण बन जाता है और ज्ञान का उत्पादन ही सत्ता संरचना को बनाए रखता है।
- विखंडन और बहुलता: यह विचारधारा मानती है कि समाज और व्यक्ति की पहचान स्थिर नहीं होती बल्कि वे निरंतर विखंडित और पुनर्निर्मित होते रहते हैं।
- महान आख्यानों का विरोध: उत्तर-आधुनिकतावादी विचारक “महान आख्यानों” (Grand Narratives) जैसे प्रगति, तर्कवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि पर विश्वास नहीं करते।
आलोचनात्मक विश्लेषण:
उत्तर-आधुनिकतावाद में स्पष्ट दिशा या समाधान का अभाव होता है, जिससे यह समाजिक परिवर्तन हेतु व्यावहारिक उपकरण नहीं बन पाता।
यह कभी-कभी निराशावादी और विघटनकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक एकता की अवधारणा कमजोर होती है।
इसकी अत्यधिक सापेक्षता वैज्ञानिक और तर्कसंगत विश्लेषण की संभावना को चुनौती देती है।
उत्तर-आधुनिकतावाद ने आधुनिकतावादी दृष्टिकोणों की सीमाओं को उजागर किया है और सामाजिक यथार्थ की जटिलता को समझने का नया तरीका दिया है।
प्रश्न-4. सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- सिद्धांत निर्माण (Theory Building) समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न पक्षों की व्याख्या, विश्लेषण और पूर्वानुमान किया जाता है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो अनुभवजन्य तथ्यों और वैचारिक चिंतन दोनों पर आधारित होती है।
- समस्या की पहचान (Identification of Problem):
सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत सामाजिक समस्या या विषय की पहचान से होती है। शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना या व्यवहार को समझने के लिए एक स्पष्ट समस्या कथन तैयार करता है। - अवधारणाओं का चयन (Selection of Concepts):
अवधारणाएँ सिद्धांत का मूलभूत ढाँचा होती हैं। उदाहरण के लिए – वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, स्थिति आदि अवधारणाएँ समाजशास्त्र में प्रमुख हैं। इन्हीं के माध्यम से समाज की संरचना को समझा जाता है। - परिकल्पना का निर्माण (Formulation of Hypothesis):
परिकल्पना एक संभावित उत्तर होती है जो किसी प्रश्न का परीक्षण योग्य उत्तर देती है। परिकल्पना यह संकेत देती है कि कौन-से चर (Variables) एक-दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं। - अनुभवजन्य अनुसंधान (Empirical Research):
परिकल्पना की सत्यता को परखने के लिए आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। यह प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों से हो सकता है, जैसे कि सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रेक्षण आदि। - आंकड़ों का विश्लेषण (Data Analysis):
संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय या गुणात्मक तरीकों से किया जाता है ताकि यह ज्ञात हो सके कि परिकल्पना सत्य है या असत्य। - निष्कर्ष (Conclusion):
विश्लेषण के आधार पर शोधकर्ता कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालता है जो किसी सामाजिक घटना को समझाने में सहायता करता है। - सामान्यीकरण (Generalization):
यदि निष्कर्ष व्यापक स्तर पर लागू होते हैं, तो यह एक सिद्धांत का रूप ले लेते हैं। यह सिद्धांत समाज के अन्य संदर्भों में भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। - परीक्षण और संशोधन (Testing and Revision):
सिद्धांत की वैधता को समय-समय पर पुनः परखा जाता है और आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन किए जाते हैं।
इस प्रकार सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया गतिशील और चक्रीय होती है। यह केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर परीक्षण, अनुभव और संशोधन से परिपक्व होती है। समाजशास्त्र में सिद्धांत निर्माण के माध्यम से हम समाज को गहराई से समझ सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन की दिशा को जान सकते हैं।
प्रश्न-5. आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रमुख विवादों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:- आलोचनात्मक सिद्धांत (Critical Theory) एक बौद्धिक परंपरा है जो समाज, संस्कृति और सत्ता के गहन विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की वकालत करता है। इसका आरंभ फ्रैंकफर्ट स्कूल (Frankfurt School) के चिंतकों जैसे मैक्स हॉर्कहाइमर, थियोडोर अडोर्नो, हर्बर्ट मारकूज़ और युर्गेन हैबरमास द्वारा किया गया।
प्रमुख विवाद और बिंदु:
- सांस्कृतिक उद्योग की आलोचना (Critique of Culture Industry):
अडोर्नो और हॉर्कहाइमर ने तर्क दिया कि पूंजीवादी समाज में संस्कृति को एक उपभोक्ता वस्तु बना दिया गया है, जिससे व्यक्ति की आलोचनात्मक चेतना कुंद हो जाती है। - प्रबुद्धि की विफलता (Failure of Enlightenment):
उन्होंने यह दावा किया कि आधुनिकता और वैज्ञानिक प्रगति ने स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा दिया है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक युक्तिवाद की आलोचना करता है। - वर्ग संघर्ष की पुनर्व्याख्या:
क्रिटिकल थ्योरी पारंपरिक मार्क्सवाद की ‘आर्थिक निर्धारणवाद’ की आलोचना करती है। वह मानती है कि विचारधारा, संस्कृति और भाषा भी सत्ता को बनाए रखने में सहायक होती है। - संचारात्मक कार्य-प्रणाली (Communicative Action):
युर्गेन हैबरमास ने तर्क दिया कि एक आदर्श संप्रेषण स्थिति में संवाद के ज़रिए सत्ता की आलोचना और सामाजिक समरसता प्राप्त की जा सकती है। यह विवादास्पद रहा कि क्या केवल संवाद से परिवर्तन संभव है। - व्यावहारिक अनुप्रयोग की कठिनाई:
आलोचनात्मक सिद्धांत के कई तत्व अमूर्त और दार्शनिक होते हैं, जिससे इन्हें वास्तविक सामाजिक अनुसंधान में लागू करना कठिन हो जाता है। - राजनीतिक निष्क्रियता का आरोप:
कई आलोचक कहते हैं कि आलोचनात्मक सिद्धांत केवल सैद्धांतिक आलोचना तक सीमित है और व्यावहारिक सामाजिक आंदोलन या नीति निर्माण में इसका योगदान कम है।
आलोचनात्मक सिद्धांत समाज की सत्ता संरचनाओं की आलोचना और सामाजिक मुक्ति की संभावना की खोज करता है। इसके विवाद इस बात से जुड़े हैं कि क्या यह व्यवहारिक है या केवल बौद्धिक विमर्श का माध्यम। फिर भी, इसकी विचारशील आलोचना ने समाजशास्त्रीय चिंतन को समृद्ध किया है।
प्रश्न-6. सामाजिक विनिमय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- सामाजिक विनिमय सिद्धांत (Social Exchange Theory) एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जिसका विकास जॉर्ज होमन्स (George Homans), पीटर ब्लाउ (Peter Blau) और रिचर्ड एमरसन (Richard Emerson) जैसे समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया। यह सिद्धांत मानता है कि सामाजिक संबंध लाभ और हानि के गणनात्मक सिद्धांत पर आधारित होते हैं।
सिद्धांत की मूल अवधारणाएँ: सामाजिक विनिमय सिद्धांत के अनुसार, मनुष्य अपने सामाजिक व्यवहार में हमेशा ऐसे निर्णय लेता है जो उसे अधिकतम लाभ और न्यूनतम लागत प्रदान करे। व्यक्ति सामाजिक रिश्तों में भी एक प्रकार का ‘लेन-देन’ करता है। यह लेन-देन केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें स्नेह, आदर, समय, सेवाएं, और जानकारी जैसी अमूल्य सामाजिक वस्तुएं भी शामिल होती हैं।
मुख्य तत्व:
- प्रतिफल और लागत: हर व्यवहार में व्यक्ति को कुछ लाभ (rewards) और कुछ लागत (costs) होती है।
- लाभ की गणना: व्यक्ति लाभ और हानि का तुलनात्मक विश्लेषण करके निर्णय करता है।
- आपसी निर्भरता: संबंधों में दोनों पक्षों की अपेक्षाएं होती हैं, जो उनके व्यवहार को प्रभावित करती हैं।
- संतुलन की खोज: यदि किसी पक्ष को लगातार हानि हो रही हो, तो वह संबंध तोड़ सकता है।
आलोचनात्मक विश्लेषण:
- आर्थिक दृष्टिकोण का अत्यधिक प्रयोग: यह सिद्धांत मानवीय संबंधों को अत्यधिक आर्थिक रूप से देखता है। यह स्नेह, प्रेम और नैतिक कर्तव्यों जैसे पहलुओं की उपेक्षा करता है।
- सांस्कृतिक संदर्भ की अनदेखी: यह सिद्धांत सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों की विविधता को नहीं समझता। जैसे भारतीय समाज में पारिवारिक संबंध अक्सर लाभ-हानि के गणित से परे होते हैं।
- अत्यधिक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण: यह सिद्धांत समाज के सामूहिक पहलुओं की उपेक्षा करता है और केवल व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता देता है।
- मूल्य और नैतिकता की उपेक्षा: सामाजिक व्यवहार केवल प्रतिफल और लागत के गणित पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें सामाजिक मूल्य, नैतिकता और परंपराएं भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
सामाजिक विनिमय सिद्धांत ने यह स्पष्ट करने में सहायता की है कि लोग किस प्रकार अपने व्यवहार को प्रतिफल और हानि के आधार पर नियोजित करते हैं। यह आधुनिक समाज में उभरते यथार्थवादी सामाजिक संबंधों की व्याख्या करता है, किन्तु इसकी सीमाएँ इसे पूर्णतः सार्वभौमिक सिद्धांत बनने से रोकती हैं।
प्रश्न-7.उग्रवादी/रेडिकल समाजशास्त्र पर एक विस्तृत लेख लिखिए।
उत्तर:- रेडिकल समाजशास्त्र (Radical Sociology) समाजशास्त्रीय विचारधारा की वह धारा है जो समाज में व्याप्त शोषण, असमानता, उत्पीड़न और सत्ता के ढांचे की आलोचना करते हुए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाती है। यह मुख्यतः 1960-70 के दशक में पश्चिमी देशों में उभरी जब पूंजीवाद, नस्लवाद, साम्राज्यवाद और पितृसत्ता के विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों ने जोर पकड़ा।
मुख्य विशेषताएँ:
- संघर्ष की प्रधानता:
रेडिकल समाजशास्त्र यह मानता है कि समाज विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संघर्ष पर आधारित है। विशेष रूप से शोषक (उच्च वर्ग) और शोषित (निम्न वर्ग) के बीच की टकराहट को केंद्र में रखा जाता है। - राजनीतिक चेतना:
यह दृष्टिकोण केवल समाज को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे बदलने की आकांक्षा भी रखता है। इसमें राजनीतिक परिवर्तन और क्रांतिकारी परिवर्तन को प्रमुख माना जाता है। - वर्गीय विश्लेषण:
रेडिकल समाजशास्त्री समाज का विश्लेषण आर्थिक आधार पर करते हैं, जहाँ वे उत्पादन के साधनों पर अधिकार को सामाजिक असमानता की जड़ मानते हैं। - मार्क्सवादी प्रभाव:
रेडिकल समाजशास्त्र पर कार्ल मार्क्स के विचारों का गहरा प्रभाव है। पूंजीवाद की आलोचना और समाजवादी व्यवस्था की वकालत इसकी मूल भावना में शामिल है। - प्रभावी सामाजिक आंदोलनों से जुड़ाव:
रेडिकल समाजशास्त्र महिलाओं, अश्वेतों, मजदूरों, दलितों और हाशिए पर खड़े वर्गों के आंदोलनों से गहराई से जुड़ा हुआ है।
प्रमुख चिंतक:
हर्बर्ट मारकूज़: नव-मार्क्सवादी और फ्रैंकफर्ट स्कूल के सदस्य, जिन्होंने पूंजीवादी समाज में व्यक्ति की चेतना के दमन की आलोचना की।
सी. राइट मिल्स: जिन्होंने सत्ता के केंद्रीकरण और “पावर एलीट” की अवधारणा दी।
एरिक ओलिन राइट: वर्गीय संरचना के विश्लेषण में नए दृष्टिकोण लाए।
आलोचना:
रेडिकल समाजशास्त्र पर यह आरोप है कि यह अत्यधिक वैचारिक और पक्षपाती होता है।
यह कभी-कभी अनुभवजन्य तथ्यों की उपेक्षा करता है और केवल आलोचना पर केंद्रित रहता है।
रेडिकल समाजशास्त्र ने समाजशास्त्र को क्रांतिकारी दृष्टिकोण से देखा और बदलाव के लिए प्रेरित किया। इसने समाज में व्याप्त अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का कार्य किया और सामाजिक न्याय की अवधारणा को बल दिया।
प्रश्न-8. ऐतिहासिक दृष्टिकोण की सीमाएँ विस्तार से समझाइए।
उत्तर:- ऐतिहासिक दृष्टिकोण समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है जो समाज के विकास को समय के क्रम में समझने का प्रयास करता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि समाज और उसकी संस्थाएं समय के साथ क्रमिक रूप से विकसित होती हैं और उनके वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक विकास का अध्ययन आवश्यक है। परन्तु इस दृष्टिकोण की कुछ सीमाएँ भी हैं, जिनकी विवेचना निम्नलिखित रूप से की जा सकती है:
- वस्तुनिष्ठता की कमी: ऐतिहासिक दृष्टिकोण अक्सर व्यक्तिपरक होता है क्योंकि इतिहास लेखन में लेखकों की व्यक्तिगत धारणाएं, विचारधाराएं और पूर्वाग्रह शामिल हो सकते हैं। इससे सामाजिक घटनाओं की निष्पक्ष व्याख्या प्रभावित हो सकती है।
- अपूर्ण स्रोत: ऐतिहासिक तथ्य प्रायः अपूर्ण, विखंडित या नष्ट हो चुके स्रोतों पर आधारित होते हैं। इससे ऐतिहासिक विश्लेषण की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।
- परिवर्तनशील व्याख्या: ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या समय, स्थान और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बदल सकती है। एक ही घटना को अलग-अलग समाजशास्त्री विभिन्न रूपों में समझते हैं, जिससे निष्कर्षों में असंगति आती है।
- वर्तमान समस्याओं के समाधान में अयोग्यता: यह दृष्टिकोण अतीत की घटनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और वर्तमान सामाजिक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान देने में अपेक्षाकृत कम सक्षम होता है।
- व्यापक विश्लेषण की कमी: ऐतिहासिक दृष्टिकोण में कभी-कभी संरचनात्मक और कार्यात्मक विश्लेषण की गहराई नहीं होती। यह दृष्टिकोण घटनाओं के कालक्रमिक विवरण तक सीमित रह सकता है।
- अन्य दृष्टिकोणों की उपेक्षा: यह दृष्टिकोण कभी-कभी मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, या सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की उपेक्षा कर देता है, जिससे समाज का समग्र अध्ययन प्रभावित हो सकता है।
- कारण और परिणाम की अस्पष्टता: ऐतिहासिक दृष्टिकोण में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि किन घटनाओं ने किन सामाजिक परिणामों को जन्म दिया, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जटिल और बहुस्तरीय होती हैं।
ऐतिहासिक दृष्टिकोण समाज को समझने का एक सशक्त माध्यम है, परन्तु इसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही इसका उपयोग करना चाहिए।
प्रश्न-9. नारीवाद को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- नारीवाद (Feminism) एक सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है जो महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। इसका मूल उद्देश्य पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव, हिंसा और दमन का विरोध करना तथा लैंगिक समानता की स्थापना करना है।
नारीवाद की परिभाषा:
“नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि समाज में स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कमतर समझा गया है और यह असमानता एक सामाजिक निर्माण है जिसे बदला जा सकता है।”
नारीवाद के प्रमुख प्रकार:
- उदारवादी नारीवाद (Liberal Feminism):
यह सबसे प्रारंभिक और मुख्यधारा की विचारधारा है। यह कानूनी और राजनीतिक समानता की बात करती है। जैसे – मतदान का अधिकार, शिक्षा और नौकरी में समान अवसर। - मार्क्सवादी नारीवाद (Marxist Feminism):
यह पूंजीवाद को महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण मानता है। इसके अनुसार महिलाएं श्रमिक और परिवार दोनों में उत्पीड़न झेलती हैं। - समाजवादी नारीवाद (Socialist Feminism):
यह वर्ग और लिंग दोनों को शोषण के कारक मानता है। यह आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों की संयुक्त आलोचना करता है। - रेडिकल नारीवाद (Radical Feminism):
यह पितृसत्ता को महिलाओं के शोषण की जड़ मानता है और मानता है कि केवल क्रांतिकारी परिवर्तन से स्त्रियाँ मुक्त हो सकती हैं। यह शरीर, यौनता, प्रजनन आदि पर स्त्रियों के नियंत्रण की वकालत करता है। - अस्तित्ववादी नारीवाद (Existential Feminism):
साइमन दी बोउवार द्वारा प्रतिपादित, यह मानता है कि ‘स्त्री’ होना एक सामाजिक स्थिति है, न कि जैविक। - उत्तर-आधुनिक नारीवाद (Postmodern Feminism):
यह नारीवाद की सार्वभौमिक धारणाओं की आलोचना करता है और जाति, वर्ग, नस्ल, यौनिकता आदि के अनुसार विविध अनुभवों को मान्यता देता है। - दलित नारीवाद (Dalit Feminism):
यह ब्राह्मणवादी पितृसत्ता और जाति आधारित शोषण की दोहरी मार को उजागर करता है और दलित स्त्रियों की अलग पहचान पर ज़ोर देता है।
नारीवाद एक बहुआयामी आंदोलन है जो स्त्रियों की मुक्ति और समाज में लैंगिक समानता की स्थापना के लिए प्रयासरत है। इसके विभिन्न प्रकार समाज की विविध परिस्थितियों को उजागर करते हैं और स्त्रीवादी संघर्ष को और सशक्त बनाते हैं।
प्रश्न-10. समाजशास्त्रीय सिद्धान्त का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:- अर्थ:
समाजशास्त्रीय सिद्धांत वे व्यवस्थित विचारों के समूह होते हैं जो समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, और सामाजिक व्यवहारों को समझाने एवं विश्लेषण करने का कार्य करते हैं। ये सिद्धांत समाज के क्रियात्मक ढांचे, संघर्षों, परिवर्तनों और विकास की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं।
परिभाषा:
- केनेथ ए. गुड: “समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक संगठित विचारों की प्रणाली है जो सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करती है।”
- एंथनी गिडेन्स: “समाजशास्त्रीय सिद्धांत समाज और सामाजिक व्यवहारों को समझने का विश्लेषणात्मक उपकरण है।”
विशेषताएँ:
- वैज्ञानिक प्रकृति:
समाजशास्त्रीय सिद्धांत तार्किक एवं विश्लेषणात्मक होते हैं। यह अनुभवजन्य (empirical) तथ्यों पर आधारित होते हैं। - व्याख्यात्मक भूमिका:
ये सिद्धांत समाज में होने वाली घटनाओं की गहन व्याख्या करने में सहायता करते हैं। उदाहरणतः – परिवार, जाति, वर्ग, संघर्ष, आदि की। - अनुमान और पूर्वानुमान:
सिद्धांत सामाजिक व्यवहार के संभावित परिणामों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। - सामाजिक व्यवहार की दिशा:
यह मानव व्यवहार को समझने, उसे नियंत्रित करने और सामाजिक योजना बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। - सैद्धांतिक विविधता:
समाज में विविधता के कारण अनेक सिद्धांत जैसे संरचनात्मक क्रियावाद, संघर्ष सिद्धांत, अन्तःक्रियावाद, नारीवादी सिद्धांत, आदि विकसित हुए हैं। - परिवर्तनशीलता:
समाजशास्त्रीय सिद्धांत स्थिर नहीं होते, वे समय और समाज के साथ विकसित होते रहते हैं।
समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों को समझने का माध्यम हैं। ये न केवल समाज की यथास्थिति की व्याख्या करते हैं, बल्कि उसमें परिवर्तन की संभावनाओं को भी उजागर करते हैं। इनके माध्यम से समाज का गहन विश्लेषण संभव हो पाता है।
प्रश्न-11. आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं ? इसके विकास में एल्विन डब्ल्यू. गोल्डनर के योगदान को रेखांकित कीजिए।
उत्तर:- अर्थ:
आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र (Radical Sociology) समाज में विद्यमान शोषण, असमानता, वर्गभेद, और सत्ता के दमनकारी स्वरूप की आलोचना करता है और उनके उन्मूलन की प्रक्रिया पर बल देता है। यह समाज को केवल समझने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसे बदलने का उद्देश्य भी रखता है।
मुख्य सिद्धांत:
यह समाज की संरचनात्मक विषमताओं जैसे – पूंजीवाद, पितृसत्ता, नस्लभेद आदि को केंद्र में रखता है। यह सोचता है कि समाज में परिवर्तन केवल तब संभव है जब इन शोषणकारी संरचनाओं को जड़ से उखाड़ा जाए।
विशेषताएँ:
- आलोचनात्मक दृष्टिकोण
- वर्ग संघर्ष और सत्ता संरचना की व्याख्या
- क्रांतिकारी चेतना का विकास
- परिवर्तन पर बल
एल्विन डब्ल्यू. गोल्डनर का योगदान:
एल्विन गोल्डनर (Alvin W. Gouldner) ने 1960 और 1970 के दशक में आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र को एक सशक्त वैचारिक आधार प्रदान किया।
- ‘नव-आलोचनात्मक समाजशास्त्र’ का प्रतिपादन:
गोल्डनर ने पारंपरिक समाजशास्त्र की निष्पक्षता की धारणा को चुनौती दी और बताया कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक समस्याओं के प्रति पक्षधर होना चाहिए। - ‘Coming Crisis of Western Sociology’ (1970):
इस प्रसिद्ध पुस्तक में उन्होंने पश्चिमी समाजशास्त्र की तटस्थता की आलोचना की और ‘Reflexive Sociology’ का समर्थन किया जिसमें समाजशास्त्री को अपने वर्ग, विचारधारा और स्थान के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। - सत्ता के विश्लेषण में योगदान:
उन्होंने कहा कि सत्ता संबंध केवल आर्थिक नहीं होते, बल्कि ज्ञान और विचारधाराएं भी सत्ता के उपकरण बन जाते हैं। - बौद्धिक स्वतंत्रता का समर्थन:
गोल्डनर ने समाजशास्त्र को सत्ता और प्रभुत्व के विरुद्ध खड़े रहने वाला बौद्धिक उपकरण बनाने की बात कही।
आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र समाज को समझने के साथ-साथ उसे बदलने की आकांक्षा रखता है। एल्विन डब्ल्यू. गोल्डनर ने इस सिद्धांत को बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाया और समाजशास्त्रियों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराया।
प्रश्न-12. पीटर एम. ब्लाउ के संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत को समझाइए।
उत्तर:- पीटर एम. ब्लाउ (Peter M. Blau) अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने ‘Structural Exchange Theory’ की अवधारणा दी। यह सिद्धांत सामाजिक विनिमय को एक संरचनात्मक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। ब्लाउ ने जॉर्ज होमन्स के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक विनिमय को संरचनात्मक संदर्भ में व्याख्यायित किया।
मुख्य अवधारणाएँ:
- सामाजिक विनिमय और संरचना:
ब्लाउ के अनुसार, सामाजिक विनिमय केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, बल्कि यह बड़े सामाजिक ढांचे जैसे – संगठन, संस्थाएं, वर्ग आदि में भी होता है। - अधिकार और असमानता:
जब एक पक्ष बार-बार दूसरे पक्ष को लाभ देता है, तो एक प्रकार की निर्भरता उत्पन्न होती है जो शक्ति असमानता को जन्म देती है। यहीं से सामाजिक संरचना की जटिलता शुरू होती है। - नियमितीकरण और संस्थागतरण:
समय के साथ विनिमय संबंध नियमित हो जाते हैं और औपचारिक संस्थाओं का रूप ले लेते हैं, जिससे सामाजिक ढांचे बनते हैं। - सामाजिक पुरस्कार और दंड:
ब्लाउ ने बताया कि सामाजिक व्यवहारों को सामाजिक स्वीकृति, प्रतिष्ठा, या बहिष्कार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
उदाहरण:
एक कार्यस्थल पर मालिक और कर्मचारी के बीच संबंध को देखें – मालिक वेतन देता है, कर्मचारी श्रम देता है। यह विनिमय शक्ति असंतुलन, पदानुक्रम और संगठनात्मक संरचना को जन्म देता है।
विशेषताएँ:
- व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर लागू।
- शक्ति, निर्भरता और असमानता को स्पष्ट करता है।
- सामाजिक संरचना के उद्भव को विनिमय से जोड़ता है।
पीटर ब्लाउ का संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत सामाजिक संबंधों और संरचनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह सिद्धांत दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत आदान-प्रदान से सामाजिक ढांचे का निर्माण होता है और सामाजिक असमानताएं उत्पन्न होती हैं। इसने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में शक्ति और संस्थागत विनिमय को एक नई दृष्टि प्रदान की।
प्रश्न-13.नारीवाद सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये।
उत्तर:-नारीवाद (Feminism) एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है जो लैंगिक असमानता, महिलाओं के शोषण, दमन और समाज में उनकी स्थिति को केंद्र में रखकर विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य स्त्रियों को समान अधिकार और अवसर दिलाना है।
मुख्य विचार:
नारीवादी सिद्धांत मानता है कि समाज एक पितृसत्तात्मक संरचना में बँधा है जहाँ पुरुषों को श्रेष्ठ और महिलाओं को अधीन माना जाता है।
प्रमुख प्रकार:
- उदार नारीवाद:
यह समान अधिकारों की वकालत करता है, जैसे – शिक्षा, रोजगार, मतदान का अधिकार। - मार्क्सवादी नारीवाद:
यह मानता है कि महिलाओं का शोषण पूँजीवाद की देन है। - सामाजिक नारीवाद:
यह पूँजीवाद और पितृसत्ता को मिलकर स्त्री शोषण का कारण मानता है। - रेडिकल नारीवाद:
यह पुरुष वर्चस्व को स्त्री समस्याओं की जड़ मानता है और सामाजिक संरचना में बुनियादी बदलाव की माँग करता है। - उत्तर-आधुनिक नारीवाद:
यह मानता है कि स्त्री अनुभव विविध और संदर्भ विशेष होते हैं, किसी एक रूप में नहीं बाँधे जा सकते।
आलोचनात्मक विवेचना:
- अत्यधिक स्त्री-केंद्रित दृष्टिकोण:
कुछ नारीवादी सिद्धांत पुरुषों को शोषक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे संतुलन की कमी रहती है। - सभी महिलाओं को एक रूप में देखना:
नारीवाद अक्सर सभी स्त्रियों को एक समान मानता है, जबकि वर्ग, जाति, धर्म, नस्ल आदि उनके अनुभवों को भिन्न बनाते हैं। - पारिवारिक संरचना की उपेक्षा:
कुछ दृष्टिकोण परिवार संस्था को केवल दमन का स्थल मानते हैं, जो पूरी तरह यथार्थ नहीं है। - सांस्कृतिक विविधताओं की उपेक्षा:
पश्चिमी नारीवाद अक्सर विकासशील देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नज़रअंदाज करता है। - सिद्धांत और व्यवहार में अंतर:
कई बार नारीवादी विचार व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो पाते, जैसे ग्रामीण या अशिक्षित महिलाओं तक इसकी पहुँच सीमित है।
नारीवाद ने लैंगिक समानता की दिशा में क्रांतिकारी कार्य किया है, किंतु इसकी आलोचनाएँ यह इंगित करती हैं कि इसे अधिक समावेशी, संतुलित और विविधतापूर्ण बनाना आवश्यक है। एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर ही नारीवादी सिद्धांत सामाजिक बदलाव में सशक्त भूमिका निभा सकता है।
प्रश्न-14. संघर्ष के प्रकार्य को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:-सामाजिक संघर्ष को अक्सर समाज के लिए विघटनकारी माना जाता है, किंतु संघर्षात्मक दृष्टिकोण इसे समाज के विकास और परिवर्तन के एक आवश्यक अंग के रूप में देखता है। कार्ल मार्क्स, राल्फ डाहरडोर्फ, लुईस कोज़र जैसे विचारकों ने संघर्ष के प्रकार्यात्मक पहलुओं पर बल दिया है।
संघर्ष का अर्थ:
संघर्ष का अर्थ है – दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच लक्ष्यों, हितों या संसाधनों की प्राप्ति के लिए टकराव।
संघर्ष के प्रमुख प्रकार्य:
- सामाजिक परिवर्तन का स्रोत:
संघर्ष समाज में परिवर्तन और नवाचार को जन्म देता है। मार्क्स के अनुसार, वर्ग संघर्ष ही समाज को आगे बढ़ाता है। - सामाजिक ढांचे की पुनर्रचना:
संघर्ष से सामाजिक व्यवस्था में संतुलन पुनः स्थापित होता है। जैसे – आंदोलनों के माध्यम से नीतियाँ बदलती हैं। - समूह पहचान और एकता:
बाहरी संघर्ष आंतरिक एकता को मज़बूत करता है। उदाहरण: स्वतंत्रता संग्राम में भारत की सामाजिक एकता। - अन्याय के प्रति जागरूकता:
संघर्ष शोषण और असमानता के प्रति लोगों को जागरूक करता है, जिससे सामाजिक चेतना बढ़ती है। - नए संस्थानों का निर्माण:
संघर्ष के कारण नए कानून, संस्थाएँ और सामाजिक व्यवस्थाएँ अस्तित्व में आती हैं। जैसे – श्रम कानून। - विकासशील नेतृत्व:
संघर्षों से नए नेता और विचारक उभरते हैं, जो सामाजिक दिशा को प्रभावित करते हैं। - सामाजिक गतिशीलता:
संघर्ष समाज की स्थिरता को चुनौती देता है, जिससे वह गतिशील बनता है।
संघर्ष समाज का अभिन्न अंग है, जो न केवल समस्याओं की पहचान करता है, बल्कि उनके समाधान और सुधार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसे केवल नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए।
प्रश्न-15. सामाजिक विनिमय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
उत्तर:- सामाजिक विनिमय सिद्धांत (Social Exchange Theory) एक सूक्ष्म समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, जो इस धारणा पर आधारित है कि मानव व्यवहार लाभ और हानि के आकलन पर आधारित होता है। इस सिद्धांत का विकास जॉर्ज होमन्स, पीटर ब्लाउ, और रिचर्ड एमर्सन जैसे विद्वानों ने किया।
मुख्य विचार:
इस सिद्धांत के अनुसार, मनुष्य प्रत्येक सामाजिक संबंध में लाभ (rewards) प्राप्त करने का प्रयास करता है और हानि (cost) से बचता है। यदि किसी संबंध में लाभ अधिक होता है, तो वह संबंध बना रहता है, अन्यथा समाप्त हो जाता है।
मुख्य बिंदु:
- होमन्स का दृष्टिकोण:
उन्होंने व्यवहारवादी मनोविज्ञान के आधार पर यह तर्क दिया कि व्यक्ति सामाजिक संबंधों में उसी व्यवहार को दोहराता है, जिससे उसे पुरस्कार (rewards) प्राप्त होता है। - पीटर ब्लाउ का योगदान:
उन्होंने सिद्ध किया कि सामाजिक जीवन में विनिमय केवल भौतिक नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों पर भी आधारित होता है। - रिचर्ड एमर्सन:
उन्होंने इस सिद्धांत को सत्ता और निर्भरता के दृष्टिकोण से जोड़ा।
आलोचनात्मक विश्लेषण:
- अत्यधिक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण:
यह सिद्धांत सामाजिक संबंधों को केवल व्यक्तिगत लाभ-हानि के दृष्टिकोण से देखता है, जबकि सामूहिकता, भावनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करता है। - भावनात्मक पहलुओं की उपेक्षा:
यह प्रेम, त्याग, कर्तव्य जैसे मानवीय पक्षों की अवहेलना करता है, जो सामाजिक संबंधों के मूल आधार हैं। - संरचनात्मक तत्वों की उपेक्षा:
यह सिद्धांत सामाजिक संरचना, संस्थाओं और वर्गभेद जैसे बड़े मुद्दों को नहीं देखता। - संस्कृति की भूमिका की उपेक्षा:
समाज में मूल्य और मान्यताएँ संस्कृति पर आधारित होती हैं, जिन्हें यह सिद्धांत पर्याप्त महत्व नहीं देता। - मूल्यांकन कठिन:
लाभ और हानि को मापना जटिल होता है, क्योंकि यह व्यक्ति की धारणाओं पर निर्भर करता है।
सामाजिक विनिमय सिद्धांत ने सामाजिक व्यवहार को एक नए दृष्टिकोण से समझने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, किंतु इसकी सीमाएँ इसे एक पूर्ण समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनने से रोकती हैं। इसलिए इसका उपयोग अन्य सिद्धांतों के पूरक के रूप में किया जाना अधिक उपयुक्त है।
VMOU Solved Assignment PDF – Click Here
VMOU WHATSAPP GROUP जॉइन कर सकते हो और साथ ही VMOU विश्वविद्यालय संबंधित और भी दोस्तों के साथ DISCUSSION कर सकते हो। -CLICK HERE

अपनी परीक्षा तैयारी को और मजबूत करने और बेहतर परिणाम के लिए आज ही अपनी वन वीक सीरीज ऑर्डर करवाए अभी अपने पेपर कोड भेजे और ऑर्डर कंफिरम् करवाये
Subscribe Our YouTube Channel – learn with kkk4
vmou MASO-05 paper , vmou ma 2nd year exam paper , vmou exam paper 2026 , vmou exam paper 2025 , vmou exam news today
VMOU EXAM PAPER